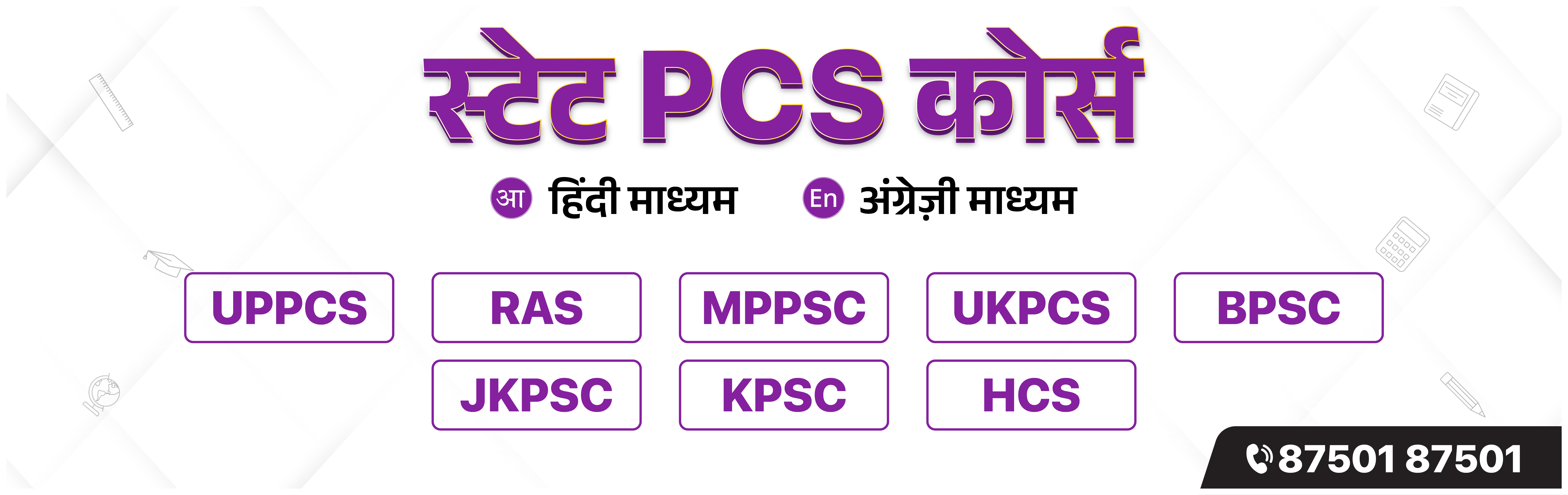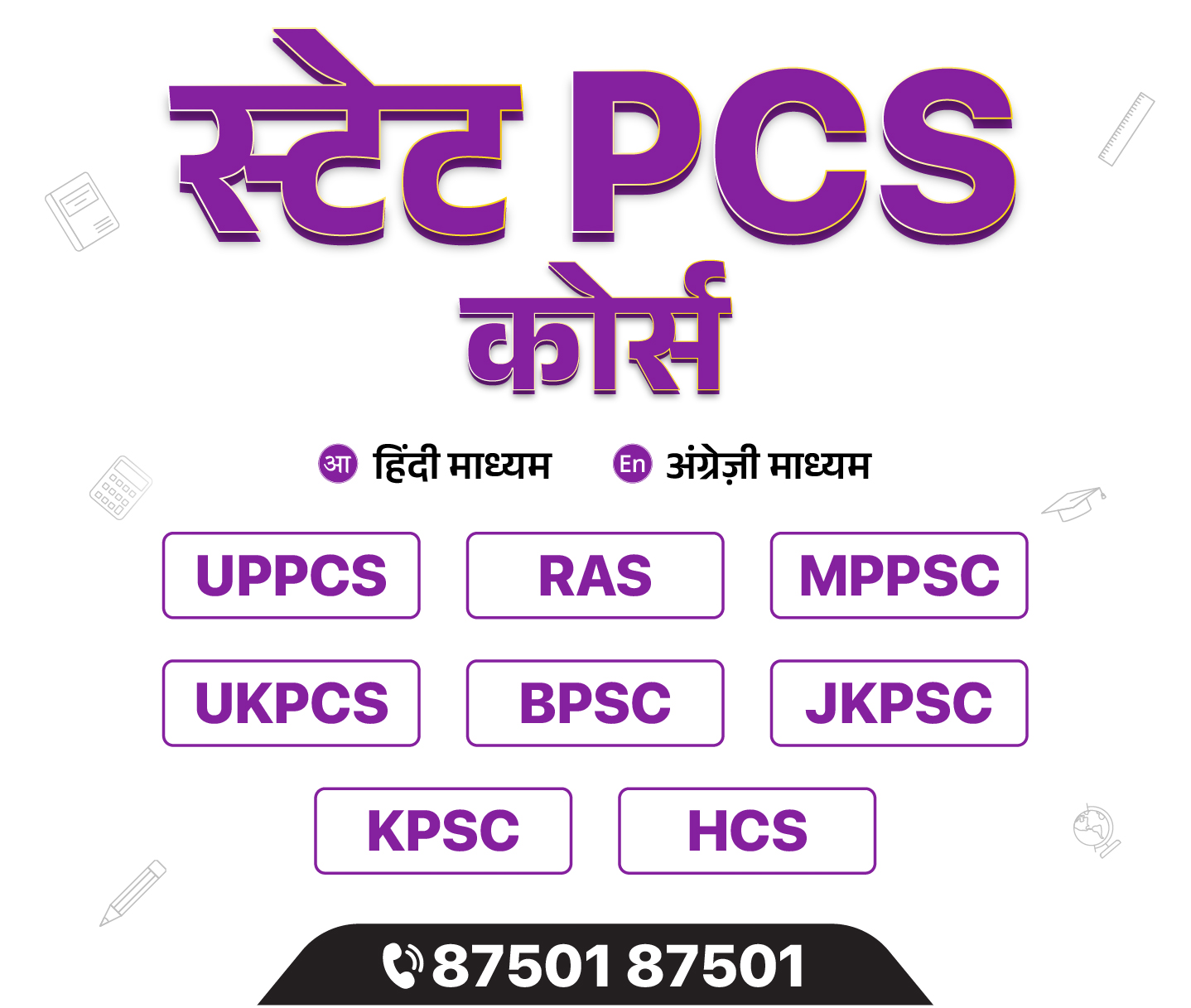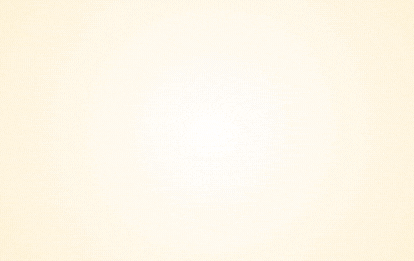उत्तर प्रदेश Switch to English
चिवनिंग-अटल बिहारी वाजपेई छात्रवृत्ति योजना
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश सरकार ने चिवनिंग-अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना के लिये ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं।
मुख्य बिंदु
- योजना के बारे में:
- इस समझौता ज्ञापन पर भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) में इसके लिये 2 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।
- योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पाँच मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष ब्रिटेन के अग्रणी विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री करने का अवसर मिलेगा।
- उद्देश्य:
- इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, अनुसंधान और नेतृत्व में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है।
- साथ ही इसका उद्देश्य राज्य की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाना तथा छात्रों को वैश्विक नेतृत्व की भूमिका के लिये तैयार करना है।
- इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, अनुसंधान और नेतृत्व में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है।
- समय-सीमा:
- कार्यक्रम वर्ष 2025-26 के शैक्षणिक सत्र से प्रारम्भ होगा और तीन वर्षों तक चलेगा। वर्ष 2028-29 से इसे पुनः नवीनीकृत करने की संभावना है।
- वित्तीय प्रावधान:
- छात्रवृत्ति के अंतर्गत ट्यूशन फीस, परीक्षा एवं अनुसंधान शुल्क, जीवन-यापन भत्ता तथा ब्रिटेन आने-जाने का हवाई किराया शामिल है।
- लागत:
- प्रति छात्र अनुमानित कुल व्यय 38,048 पाउंड से 42,076 पाउंड (लगभग 45–48 लाख रुपए) होगा।
- राज्य सरकार का योगदान: लगभग 19,800 पाउंड (23 लाख रुपए)। शेष राशि का वहन FCDO द्वारा किया जाएगा।
- छात्र चयन:
- प्रत्येक वर्ष पाँच छात्रों को प्रतिष्ठित ब्रिटिश विश्वविद्यालयों, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन हेतु पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- सामरिक महत्त्व:
- यह योजना भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाती है, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की ब्रिटेन यात्रा के बाद, जहाँ उन्होंने व्यापार समझौते तथा विज़न 35 पर हस्ताक्षर किये, जिससे व्यापार एवं शिक्षा के लिये नए रास्ते खुले।

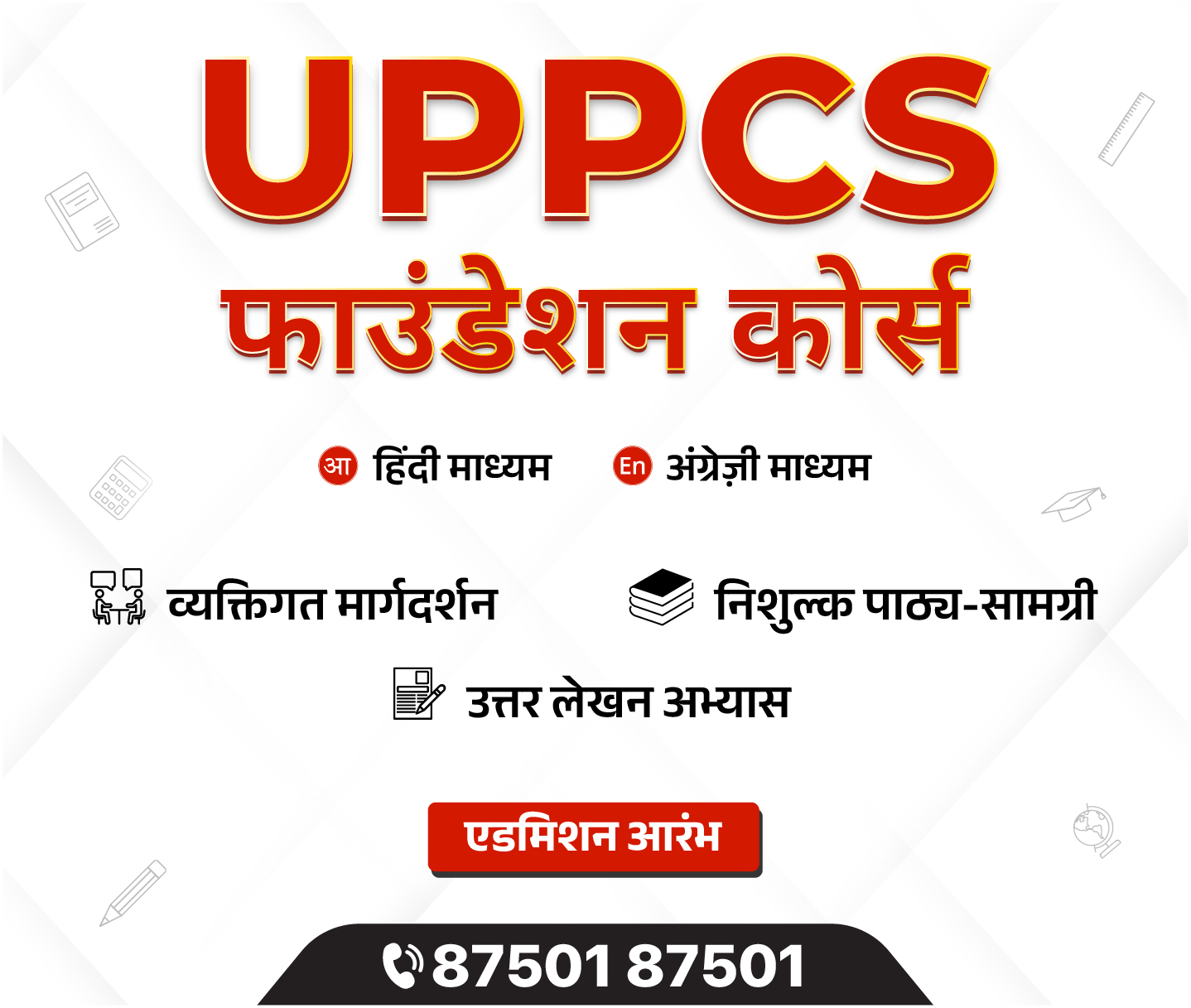
उत्तर प्रदेश Switch to English
डॉ. शंकर दयाल शर्मा की 104वीं जयंती
चर्चा में क्यों?
भारत के नौवें राष्ट्रपति (25 जुलाई, 1992 से 25 जुलाई, 1997 तक ) डॉ. शंकर दयाल शर्मा की 104 वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पुष्पांजलि अर्पित की।
मुख्य बिंदु
डॉ. शंकर दयाल शर्मा के बारे में:
- परिचय:
- डॉ. शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल (मध्य प्रदेश) में हुआ था।
- वे एक प्रतिष्ठित वकील, राजनीतिज्ञ और भारत के नौवें राष्ट्रपति थे।
- उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई तथा विभिन्न राजनीतिक दायित्वों में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
- शिक्षा:
- उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा आगरा और लखनऊ विश्वविद्यालयों से प्राप्त की।
- कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से विधि में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद, उन्होंने लंदन में लिंकन इन और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया।
- उन्होंने वर्ष 1940 में लखनऊ में अपनी वकालत शुरू की।
- साहित्यिक कार्य:
- वे एक प्रख्यात कवि और लेखक भी थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं और लखनऊ लॉ जर्नल (1941-43) तथा सोशलिस्ट इंडिया (1971-74) जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया।
- राजनीतिक यात्रा:
- वर्ष 1952 से 1956 तक वे भोपाल विधानसभा के सदस्य रहे और राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने।
- वह 1956 से 1971 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के लिये पुनः निर्वाचित हुए और उन्होंने आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया।
- वर्ष 1971 में वे लोकसभा के लिये चुने गए और वर्ष 1974 से 1977 तक संचार मंत्री रहे।
- उपराष्ट्रपति पद और राष्ट्रपति पद:
- वर्ष 1984 में वे भारत के आठवें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए और दो कार्यकाल तक इस पद पर रहे।
- वर्ष 1992 में वे भारत के राष्ट्रपति बने।
- अक्तूबर 2000 में राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने उनके सम्मान में विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया।
- मृत्यु:
- 26 दिसंबर 1999 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया।
भारत के राष्ट्रपति के बारे में मुख्य तथ्य
- दो कार्यकाल: भारत के एकमात्र राष्ट्रपति, जिन्होंने दो कार्यकाल पूरे किये – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद।
- राष्ट्रपति की मृत्यु : अब तक दो राष्ट्रपतियों, डॉ. जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का अपने कार्यकाल के दौरान निधन हो चुका है।
- कार्यवाहक राष्ट्रपति : मई,1969 में जब डॉ. जाकिर हुसैन का निधन हुआ, तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने।
- इसके बाद वी.वी. गिरि ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिये इस्तीफा दे दिया।
- CJI कार्यवाहक राष्ट्रपति: वी.वी. गिरि के इस्तीफे के बाद, मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्ला ने 20 जुलाई,1969 से 24 अगस्त,1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
नोट: न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर कार्य किया है: भारत के मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति।
भारत के राष्ट्रपति (1950-2025)
|
क्र.सं. |
नाम |
पदग्रहण |
पदमुक्त |
अवधि |
मुख्य विवरण |
|
1 |
डॉ. राजेंद्र प्रसाद |
26 जनवरी, 1950 |
13 मई, 1962 |
12 वर्ष, 107 दिन |
भारत के प्रथम राष्ट्रपति; दो कार्यकाल तक सेवा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति |
|
2 |
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन |
13 मई, 1962 |
13 मई, 1967 |
5 साल |
दार्शनिक-राष्ट्रपति; उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। |
|
3 |
डॉ. ज़ाकिर हुसैन |
13 मई, 1967 |
3 मई, 1969 |
1 वर्ष, 355 दिन |
प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति; पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। |
|
कार्यवाहक |
वी.वी. गिरि |
3 मई, 1969 |
20 जुलाई, 1969 |
78 दिन |
ज़ाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति |
|
कार्यवाहक |
न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह |
20 जुलाई, 1969 |
24 अगस्त, 1969 |
35 दिन |
CJI ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया; वी.वी. गिरि ने चुनाव लड़ने के लिये इस्तीफा दिया |
|
4 |
वी.वी. गिरि |
24 अगस्त. 1969 |
24 अगस्त. 1974 |
5 साल |
आधिकारिक कॉन्ग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की |
|
5 |
फखरुद्दीन अली अहमद |
24 अगस्त, 1974 |
11 फरवरी, 1977 |
2 वर्ष, 171 दिन |
आपातकालीन अवधि के दौरान कार्यालय में मृत्यु हो गई |
|
कार्यवाहक |
बी.डी. जट्टी |
11 फरवरी, 1977 |
25 जुलाई, 1977 |
164 दिन |
कार्यवाहक राष्ट्रपति; कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री |
|
6 |
नीलम संजीव रेड्डी |
25 जुलाई, 1977 |
25 जुलाई, 1982 |
5 साल |
प्रथम राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए |
|
7 |
ज्ञानी जैल सिंह |
25 जुलाई, 1982 |
25 जुलाई, 1987 |
5 साल |
पहले सिख राष्ट्रपति |
|
8 |
आर. वेंकटरमन |
25 जुलाई, 1987 |
25 जुलाई, 1992 |
5 साल |
पूर्व उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री |
|
9 |
डॉ. शंकर दयाल शर्मा |
25 जुलाई, 1992 |
25 जुलाई, 1997 |
5 साल |
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री |
|
10 |
के.आर. नारायणन |
25 जुलाई, 1997 |
25 जुलाई, 2002 |
5 साल |
प्रथम दलित राष्ट्रपति; राजनयिक |
|
11 |
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम |
25 जुलाई, 2002 |
25 जुलाई, 2007 |
5 साल |
"जनता के राष्ट्रपति"; भारत के मिसाइल मैन |
|
12 |
प्रतिभा पाटिल |
25 जुलाई, 2007 |
25 जुलाई, 2012 |
5 साल |
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति |
|
13 |
प्रणब मुखर्जी |
25 जुलाई, 2012 |
25 जुलाई, 2017 |
5 साल |
अनुभवी राजनीतिज्ञ; पूर्व वित्त मंत्री |
|
14 |
राम नाथ कोविंद |
25 जुलाई, 2017 |
25 जुलाई, 2022 |
5 साल |
दूसरे दलित राष्ट्रपति; बिहार के पूर्व राज्यपाल |
|
15 |
द्रौपदी मुर्मू |
25 जुलाई, 2022 |
वर्तमान |
3+ वर्ष |
वर्तमान राष्ट्रपति; पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति |
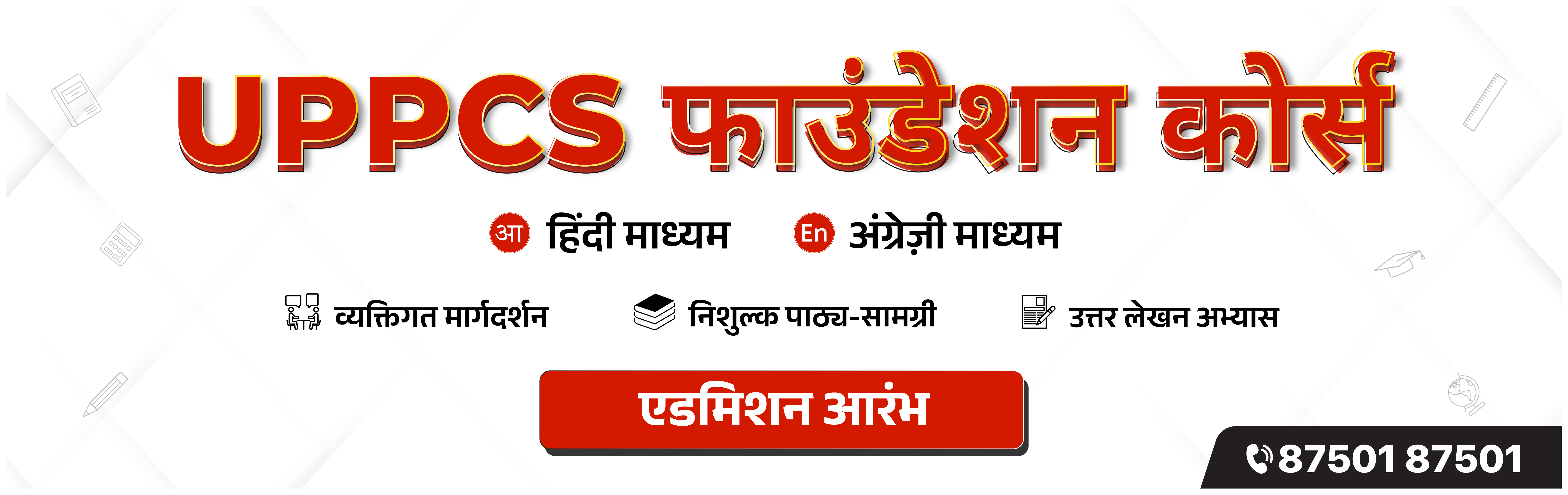
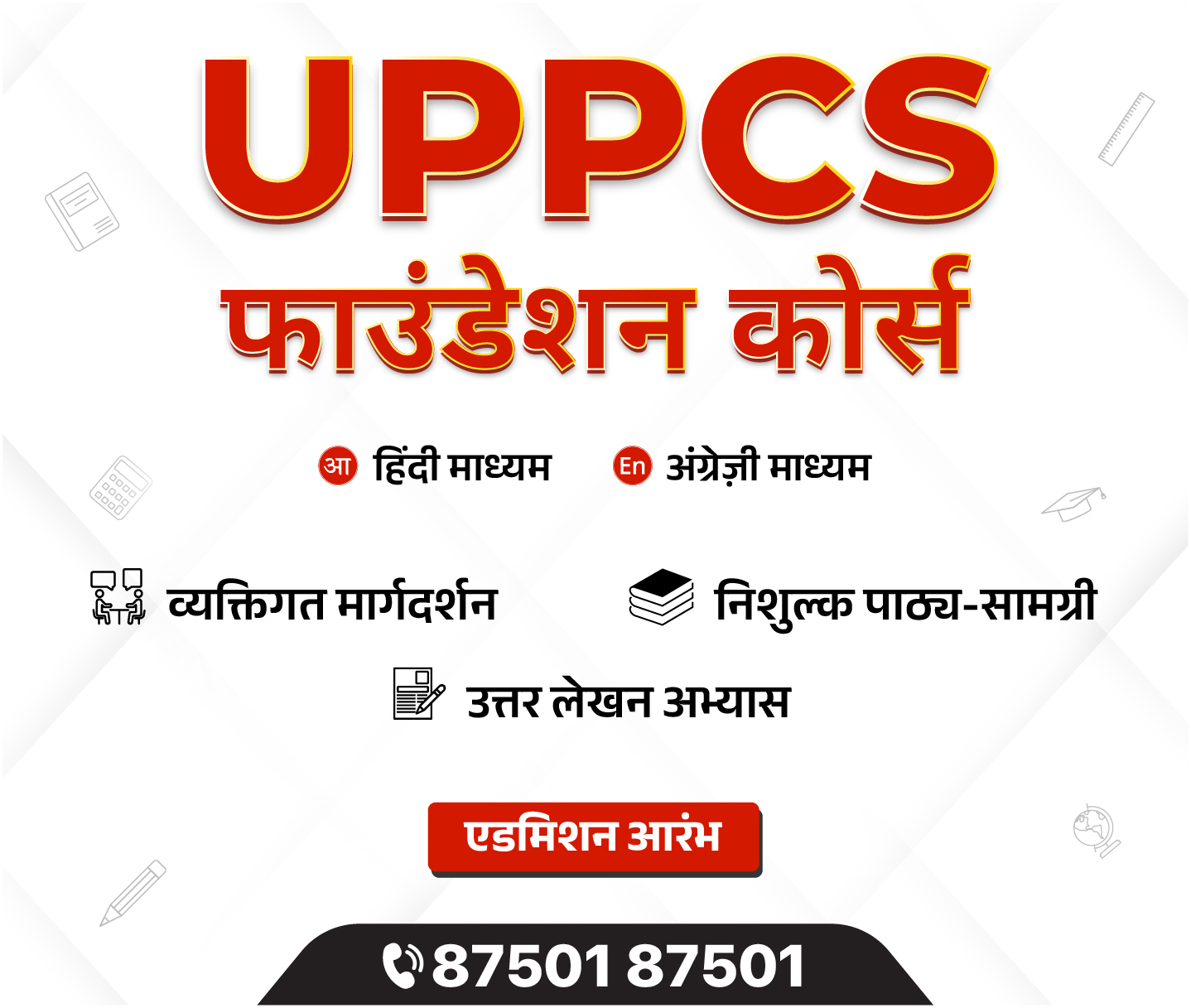
उत्तर प्रदेश Switch to English
राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कारों की 10वीं वर्षगाँठ
चर्चा में क्यों?
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विज्ञान भवन में आयोजित समारोह के दौरान 57वीं सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श कार्यशाला के साथ 8वें "राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार" प्रदान किये।
मुख्य बिंदु
- पुरस्कार 2025 के बारे में:
- वर्ष 2025 में अनुभव पुरस्कार की 10वीं वर्षगाँठ पर शासन और विविधता में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया।
- इस वर्ष पुरस्कार प्राप्त करने वालों में एक-तिहाई महिलाएँ थीं, जो शासन में महिला अधिकारियों की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है।
- 11 मंत्रालयों और विभागों के कुल 15 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया, जिनमें पहली बार एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के अधिकारी भी शामिल थे।
- उल्लेखनीय पुरस्कार विजेता:
- एम. वेंकटेशन: वर्ष 2014 की कश्मीर बाढ़ और वर्ष 2022 में यूक्रेन से निकासी अभियान सहित संकट काल में उत्कृष्ट सेवाओं के लिये सम्मानित।
- हुकुम सिंह मीणा: 6.4 लाख से अधिक गाँवों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का नेतृत्व किया।
- शालिनी कक्कड़ (SBI): प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, पेंशन सुधार और डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र अभियान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- ओ. विरुपाक्षप्पा (डाक विभाग): ग्रामीण क्षेत्रों में डाक बचत और बीमा योजनाओं का विस्तार किया।
- साजू पी.के. (CRPF): असम और पुलवामा जैसे संवेदनशील परिचालन क्षेत्रों में सेवा प्रदान की।
- नई पहलों का शुभारंभ:
- कार्यक्रम में कई पहलें प्रारम्भ की गईं, जिनमें प्रमुख हैं–
- डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र अभियान 4.0 के लिये दिशानिर्देश जारी किये गए।
- विशेष अभियान 2.0 की सफलता की कहानियों पर आधारित कॉफी टेबल ई-बुक का विमोचन।
- अनुभव पोर्टल पर प्रस्तुत संस्मरणों के विश्लेषण के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करने की घोषणा की गई।
- कार्यक्रम में कई पहलें प्रारम्भ की गईं, जिनमें प्रमुख हैं–
राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार
- परिचय: अनुभव पुरस्कार की शुरुआत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के अनुभवों को सम्मानित एवं प्रलेखित करना है।
- प्रारंभ: इस पहल की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार मार्च 2015 में अनुभव पोर्टल के माध्यम से की गई। इसका लक्ष्य अनुभव साझा करने की संस्कृति विकसित करना, सुशासन को बढ़ावा देना और प्रशासनिक सुधारों को प्रोत्साहित करना है।
- पात्रता: सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी इसके पात्र हैं। DoPPW द्वारा अधिसूचित समयावधि के अंतर्गत अनुभव पोर्टल पर प्रकाशित लेखन को इन पुरस्कारों के लिये विचारार्थ लिया जाता है।

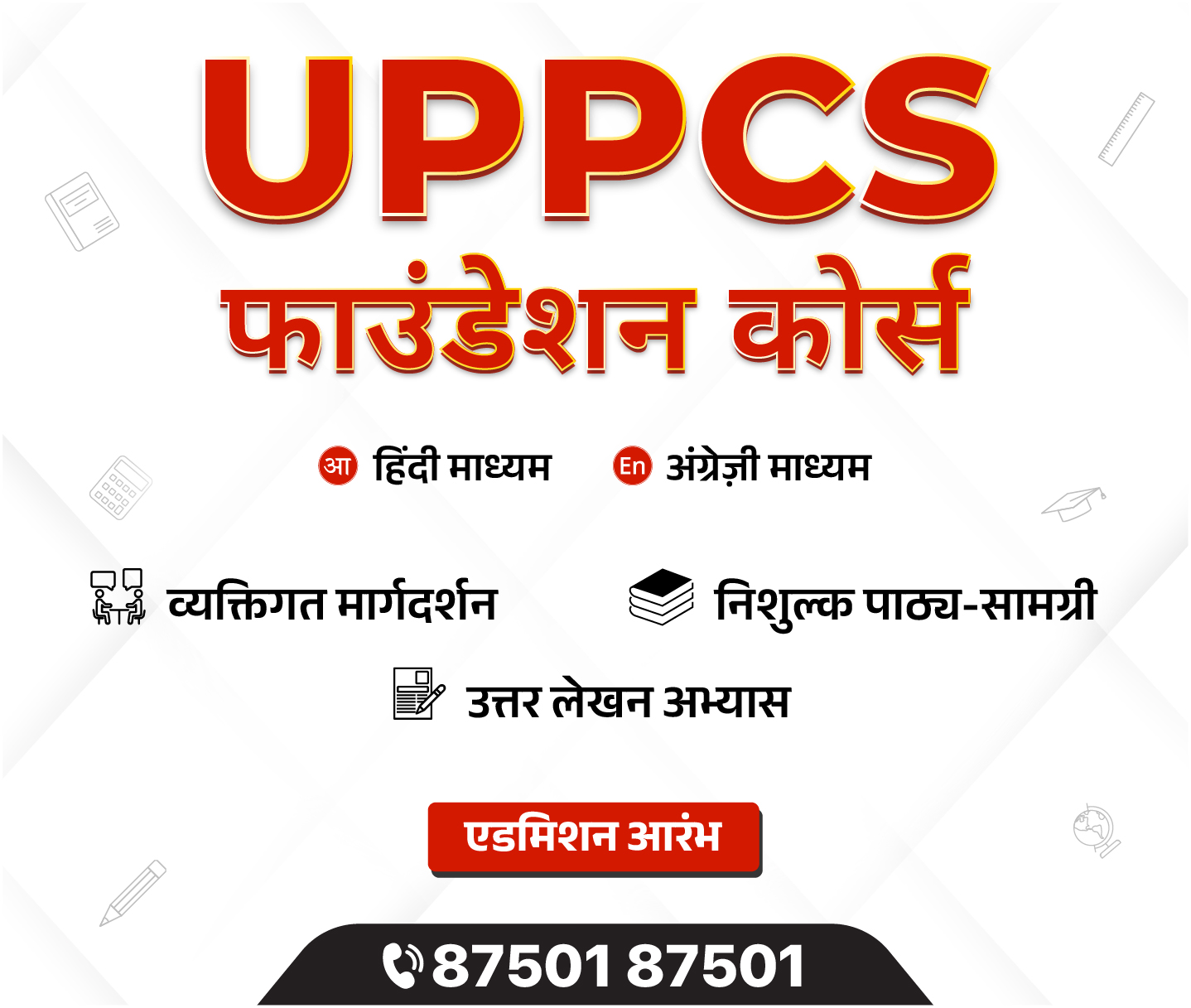
उत्तर प्रदेश Switch to English
विश्व मानवतावादी दिवस
चर्चा में क्यों?
हर साल 19 अगस्त को मनाया जाने वाला विश्व मानवतावादी दिवस का उद्देश्य उन समर्पित व्यक्तियों के प्रयासों को मान्यता देना है, जो संकट की घड़ी में दूसरों की सहायता करने के लिये अपने प्राणों को जोखिम में डालते हैं।
- यह दिवस उन लाखों लोगों के प्रति समर्थन व्यक्त करने का भी अवसर है, जिनका जीवन संघर्ष और आपदाओं के कारण संकटग्रस्त हो जाता है।
मुख्य बिंदु
विश्व मानवतावादी दिवस के बारे में:
- परिचय
- यह दिवस मानवीय मामलों के समन्वय हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (OCHA) के नेतृत्व में मनाया जाता है।
- इसका उद्देश्य संकटों से प्रभावित लोगों की कल्याण, गरिमा और अस्तित्व सुनिश्चित करना तथा मानवीय कार्यकर्त्ताओं की सुरक्षा का समर्थन करना है।
- इतिहास
- 19 अगस्त, 2003 को बगदाद स्थित कैनाल होटल पर हुए बम हमले में 22 मानवीय सहयोगी मारे गए थे, जिनमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के इराक हेतु विशेष प्रतिनिधि सर्जियो विएरा डी मेलो भी शामिल थे।
- उनके सम्मान में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर इस दिन को विश्व मानवतावादी दिवस (WHD) के रूप में घोषित किया।
- विषय (Theme)
- इस वर्ष का विषय मानवतावादियों और नागरिकों पर हो रहे हमलों को समाप्त करने तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत दंड-मुक्ति की प्रवृत्ति को रोकने का आह्वान करता है।
- यह सत्ता में बैठे लोगों से #ActForHumanity का आग्रह करता है।
- #ActForHumanity अभियान का आह्वान:
- मानवीय कार्यकर्त्ताओं और उनके द्वारा सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों की सुरक्षा।
- अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून को बनाए रखना।
- मानवीय सहायता द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले महत्त्वपूर्ण जीवन-रेखीय (Vital Lifelines) संसाधनों हेतु वित्तपोषण।