बिहार Switch to English
मुफ्त बिजली और सौर ऊर्जा पहल
चर्चा में क्यों?
बिहार सरकार 1.67 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देगी और उपभोक्ताओं की सहमति से अगले तीन वर्षों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी।
मुख्य बिंदु
घोषणा के मुख्य अंश:
- मुफ्त बिजली योजना:
- 1 अगस्त 2025 से बिहार के 1.67 करोड़ परिवारों को प्रति माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी।
- वित्तीय प्रभाव:
- इस योजना से राज्य सरकार पर लगभग 3,375 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इस पूरी पहल के लिये लगभग 19,370 करोड़ रुपए की सब्सिडी की आवश्यकता होगी।
- सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना:
- अगले तीन वर्षों में, घरेलू उपभोक्ताओं की सहमति से, राज्य सरकार छतों और आस-पास के सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की भी योजना बना रही है।
- इस पहल का उद्देश्य स्थायी ऊर्जा समाधान प्रदान करना तथा पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम करना है।
- वित्तीय सहायता:
- अन्य उपभोक्ताओं के लिये सरकार सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- बिहार सरकार कुटीर ज्योति योजना के तहत अत्यंत गरीब परिवारों के लिये सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की पूरी लागत वहन करेगी।
- सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य:
- अनुमान है कि अगले तीन वर्षों में राज्य में 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध होगी, जो राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास होगा।
कुटीर ज्योति योजना
- यह भारत में एक सरकारी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले ग्रामीण परिवारों को बिजली उपलब्ध कराकर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- वित्त वर्ष 1988-89 में केंद्र द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में BPL परिवारों को एकल-बिंदु विद्युत कनेक्शन (single-point light connections) प्रदान करना था, जिसमें अनुसूचित जाति (SC) और जनजातीय समुदायों के परिवार भी शामिल थे।


उत्तर प्रदेश Switch to English
पीलीभीत टाइगर रिज़र्व (PTR)
चर्चा में क्यों?
पीलीभीत टाइगर रिज़र्व के निकट एक संदिग्ध बाघ हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जो तीन दिनों में इस तरह की दूसरी घटना है, जिसके बाद अधिकारियों ने बाघ को गोली मारने की अनुमति लेने पर विचार किया है।
मुख्य बिंदु
पीलीभीत टाइगर रिज़र्व के बारे में:
- यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और शाहजहाँपुर ज़िलों में स्थित है। इसे वर्ष 2014 में बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- वर्ष 2020 में, इसने पिछले चार वर्षों में बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 जीता।
- यह ऊपरी गंगा के मैदान में तराई आर्क परिदृश्य का हिस्सा है।
- गोमती नदी इसी अभयारण्य से निकलती है, जो शारदा, चूका और माला खन्नोट जैसी कई अन्य नदियों का जलग्रहण क्षेत्र भी है।
- वनस्पति और जीव:
- यह 128 से अधिक जानवरों, 326 पक्षी प्रजातियों और 2,100 पुष्पीय पौधों का निवास स्थान है।
- जंगली जानवरों में बाघ, दलदली हिरण, बंगाल फ्लोरिकन, तेंदुआ आदि शामिल हैं।
- इसमें घने साल के जंगल, वृक्षारोपण और घास के मैदान तथा कई जल निकाय शामिल हैं।
मानव-पशु संघर्ष
- परिचय:
- मानव-पशु संघर्ष उन स्थितियों को संदर्भित करता है, जहाँ मानव गतिविधियों, जैसे कि कृषि, बुनियादी ढाँचे का विकास अथवा संसाधन निष्कर्षण, में वन्य पशुओं के साथ संघर्ष की स्थिति होती हैं, इसकी वजह से मानव एवं पशुओं दोनों के लिये नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं।
मानव-पशु संघर्ष से निपटने के लिये सरकारी उपाय
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: यह अधिनियम गतिविधियों, शिकार पर प्रतिबंध, वन्यजीव आवासों की सुरक्षा और प्रबंधन तथा संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि के लिये कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002: भारत, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का एक हिस्सा है। यह सुनिश्चित करता है कि जैविक विविधता अधिनियम वनों और वन्यजीवों से संबंधित मौजूदा कानूनों का खंडन करने के बजाय पूरक है।
- राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016): यह संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को मज़बूत करने और बढ़ाने, लुप्तप्राय वन्यजीवों तथा उनके आवासों के संरक्षण, वन्यजीव उत्पादों में व्यापार को नियंत्रित करने एवं अनुसंधान, शिक्षा व प्रशिक्षण पर केंद्रित है।
- प्रोजेक्ट टाइगर: प्रोजेक्ट टाइगर एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो वर्ष 1973 में शुरू की गई थी। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के लिये आश्रय प्रदान करती है
- हाथी परियोजना: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और हाथियों, उनके आवासों तथा गलियारों की सुरक्षा के लिये फरवरी 1992 में शुरू की गई थी।

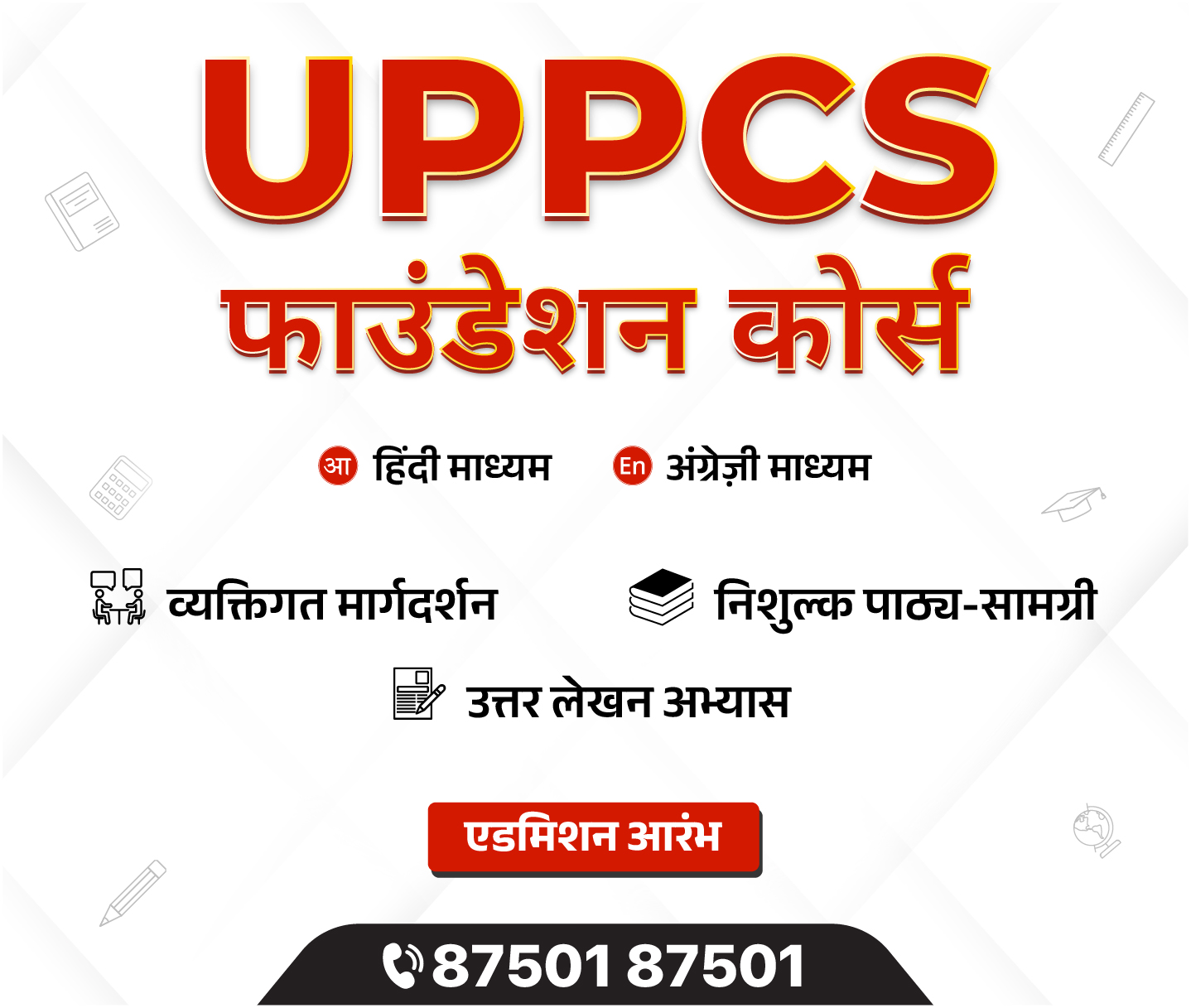
उत्तर प्रदेश Switch to English
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY)
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिये नव-प्रवर्तित प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) में महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी सुनिश्चित करने हेतु केंद्र सरकार को एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
मुख्य बिंदु
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के बारे में
- परिचय:
- PMDDKY एक व्यापक कृषि कार्यक्रम है, जिसे उत्पादकता बढ़ाने, सतत् कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने और कृषकों की आजीविका सुधारने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है।
- इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी।
- यह योजना वर्ष 2025-26 से शुरू होकर छह वर्षों तक चलेगी, जिसका वार्षिक परिव्यय 24,000 करोड़ रुपए है।
- योजना का उद्देश्य बेहतर सिंचाई, भंडारण, तथा कृषि ऋण की पहुँच सुनिश्चित करना, सतत् कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना एवं देश के 100 कमज़ोर प्रदर्शन वाले ज़िलों में कृषि उत्पादकता सुधारना है।
- यह 11 केंद्रीय मंत्रालयों की 36 योजनाओं को मिलाकर एक एकीकृत कृषि सहायता प्रणाली तैयार करती है।
- यह नीति आयोग के आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम से प्रेरित है।
- ज़िला चयन के मानदंड
- निम्न कृषि उत्पादकता: प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन की दर कम होना।
- कम फसल तीव्रता: प्रति वर्ष फसल चक्र की संख्या कम या फसल विविधता की कमी।
- सीमित ऋण वितरण: कृषि ऋण और वित्तीय संसाधनों की पहुँच का अभाव।।
- राज्य प्रतिनिधित्व: चयन में प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में शुद्ध फसल क्षेत्र और परिचालन जोत के हिस्से पर विचार किया जाएगा। संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक राज्य से कम-से-कम एक ज़िला चुना जाएगा।
- कार्यान्वयन और निगरानी व्यवस्था
- ज़िला कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ योजनाएँ:
- प्रत्येक ज़िले में ‘ज़िला धन धान्य समिति’ द्वारा एक समर्पित योजना तैयार की जाएगी, जिसमें प्रगतिशील किसान सदस्य होंगे। ये योजनाएँ फसल विविधीकरण, जल संरक्षण और कृषि आत्मनिर्भरता जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप होंगी।
- निगरानी और मूल्यांकन:
- मासिक समीक्षा के साथ एक समर्पित डैशबोर्ड के माध्यम से 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI) का उपयोग करके प्रगति पर नज़र रखी जाएगी।
- सुचारू कार्यान्वयन के लिये प्रत्येक ज़िले में केंद्रीय नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाएंगे।
- नीति आयोग नियमित मार्गदर्शन प्रदान करेगा और ज़िला योजनाओं की समीक्षा करेगा।
- विभिन्न स्तरों पर समितियाँ:
- योजना की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियाँ योजना, कार्यान्वयन तथा प्रगति की निगरानी करेंगी।
- ज़िला कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ योजनाएँ:
- अपेक्षित परिणाम:
- किसान लाभार्थी: भारत में लगभग 1.7 करोड़ किसानों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है।
- संबद्ध क्षेत्रों का एकीकरण: यह योजना मूल्य संवर्द्धन और स्थानीय आजीविका सृजन के लिये पशुधन, डेयरी एवं मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों को एकीकृत करती है।
- फोकस क्षेत्र: फसलोपरांत भंडारण, बेहतर सिंचाई, आसान ऋण पहुँच तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण आर्थिक मज़बूती सुनिश्चित की जा सके।
- राज्य सरकार की तैयारी के बारे में
- उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के लाभ का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा सुनिश्चित करने के लिये योजना बनाना प्रारंभ कर दिया है।
- राज्य के कृषि विभाग ने क्षेत्रीय विवरण की समीक्षा की है तथा योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु केंद्र सरकार को एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
- उत्तर प्रदेश एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है, अतः उसे इस योजना के आवंटन में महत्त्वपूर्ण भागीदारी मिलने की उम्मीद है।
अन्य पूरक योजनाएँ
- यूपी-एग्रीस योजना:
- PMDDKY, विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त यूपी-एग्रीस योजना का पूरक है, जिसका उद्देश्य पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों के 28 ज़िलों में कृषि उत्पादन में सुधार करना है।
- इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है।
- इस परियोजना से 10,000 महिला उत्पादक समूहों को जोड़ा जाएगा तथा 500 किसानों को उन्नत प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजा जाएगा।
- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम:
- ज़िलों को उनकी छिपी हुई क्षमता को उजागर करने के लिये सशक्त बनाकर "पिछड़ेपन" से "आकांक्षा" की ओर बदलाव।
- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम भी राज्य में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिये कार्य कर रहा है।
- यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में 112 सबसे कमज़ोर ज़िलों के उत्थान के लिये शुरू किया गया।
- मूल दर्शन:
- फोकस क्षेत्र: स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, बुनियादी ढाँचा और आर्थिक अवसर।
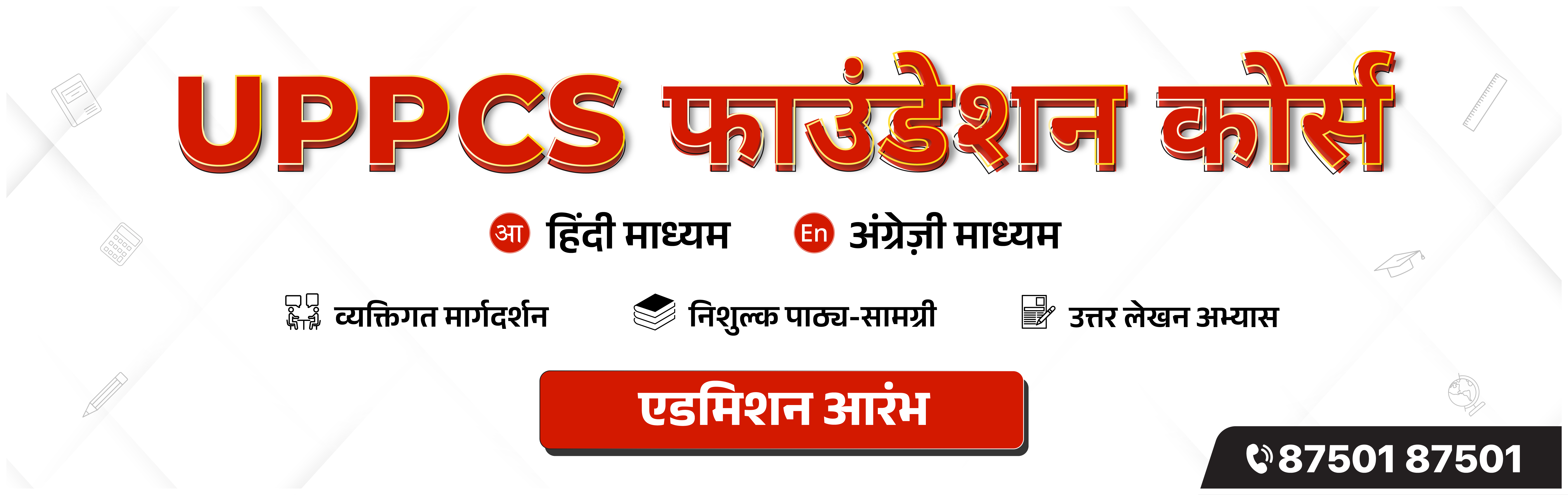
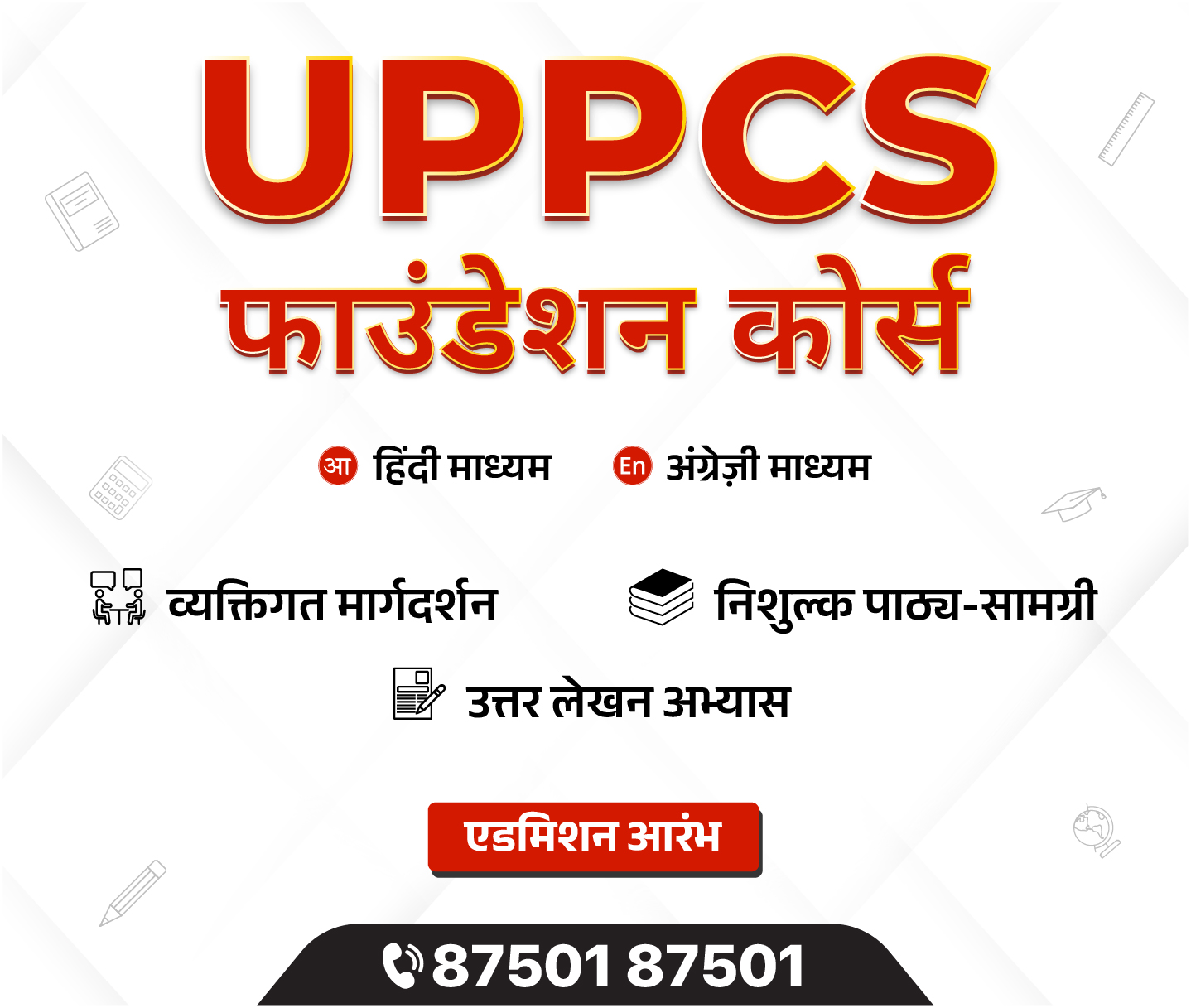
उत्तर प्रदेश Switch to English
उन्नत ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना पर राष्ट्रीय कार्यशाला
चर्चा में क्यों?
पंचायती राज मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में उन्नत ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया, जिसका शीर्षक था "नवीनग्राम - गाँव की पुनर्कल्पना"।
मुख्य बिंदु
राष्ट्रीय कार्यशाला के बारे में:
- कार्यक्रम विवरण: यह एक ऐतिहासिक पहल है, जो नियोजन और वास्तुकला के 19 साझेदार संस्थानों को एक साथ ला रही है।
- इसमें 14 राज्यों की 36 ग्राम पंचायतों के लिये उन्नत स्थानिक योजनाएँ प्रस्तुत की गई हैं, जो भारत के ग्रामीण स्थानिक विकास के इतिहास में सबसे बड़ा सहयोगात्मक प्रयास है।
- यह कार्यशाला फरवरी 2024 में आयोजित ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना पर क्रॉस लर्निंग-कम-इंटरैक्टिव राष्ट्रीय कार्यशाला की सफलता पर आधारित है।
- यह पंचायती राज प्रशासन के साथ आधुनिक नियोजन सिद्धांतों को एकीकृत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- यह कार्यशाला माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों के दृष्टिकोण पर आधारित है।
- कार्यशाला ग्रामीण शासन और विकास के लिये नए मानदंड स्थापित करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि वैज्ञानिक स्थानिक नियोजन भारत में सतत् ग्रामीण विकास का आधार बने।
- प्रतिभागी एवं हितधारक: कार्यशाला में निम्नलिखित हितधारकों ने भाग लिया:
- पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि।
- विभिन्न राज्यों के पंचायती राज विभागों के अधिकारी।
- योजना एवं वास्तुकला संस्थानों के संकाय एवं छात्र।
- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारी और सरकारी एजेंसियाँ।
- वित्तीय सततता और हितधारक भागीदारी पर केंद्रित प्रयास:
- इस पहल के तहत ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और क्रियान्वयन (RADPFI) दिशानिर्देशों के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है।
- यह समुदाय के सदस्यों, वित्त प्रदाताओं, नीतिनिर्माताओं और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं जैसे हितधारकों से सहयोग प्राप्त कर ग्रामीण परिदृश्यों में रूपांतरण लाने का उद्देश्य रखती है।
- ग्राम पंचायतों को वित्तीय रूप से सतत् बनाने के लिये स्वयं के राजस्व स्रोत (OSR) सृजन तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) साझेदारियों के महत्त्व पर विशेष ज़ोर दिया गया है।
- भौगोलिक प्रतिनिधित्व:
- उद्घाटन दिवस पर मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड तथा कर्नाटक सहित सात राज्यों द्वारा प्रस्तुतियाँ दी गईं।
- इन प्रस्तुतियों में देशव्यापी गति और विभिन्न भौगोलिक संदर्भों में विविध कार्यान्वयन दृष्टिकोणों पर प्रकाश डाला गया।
- मध्य प्रदेश में प्रगति:
- मध्य प्रदेश में बिलकिसगंज और मुरवास ग्राम पंचायतें अपने व्यापक स्थानिक नियोजन कार्यान्वयन में अच्छी प्रगति कर रही हैं।
- राज्य की पाँच अन्य ग्राम पंचायतों में भी इसी प्रकार की कार्यप्रणाली अपनाई जाएगी, जिसमें पंचायती राज विभाग इस पहल के लिये पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।
नोट:
- ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना एक समग्र योजना होती है, जो किसी ग्राम पंचायत के भौतिक और स्थानिक विकास को मार्गदर्शित करती है।
- यह निर्धारित करती है कि भूमि का उपयोग कैसे किया जाए, किस प्रकार की अवसंरचना का निर्माण हो तथा सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विकास का प्रबंधन कैसे किया जाए।
नवीनग्राम पहल के बारे में:
- नवीनग्राम पहल का उद्देश्य भारत को ग्रामीण स्थानिक विकास योजना निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना है।
- यह पहल योजनाबद्ध विकास के अनुकरणीय मॉडल तैयार करती है, जो ग्रामीण भारत के हर कोने तक पहुँचते हुए विरासत के संरक्षण और समावेशी विकास को बढ़ावा देती है।
- यह गाँवों को केवल प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि सुनियोजित समुदायों में रूपांतरित करती है, जहाँ भूमि उपयोग, अवसंरचना विकास और सतत् संसाधन प्रबंधन का समुचित संतुलन होता है।

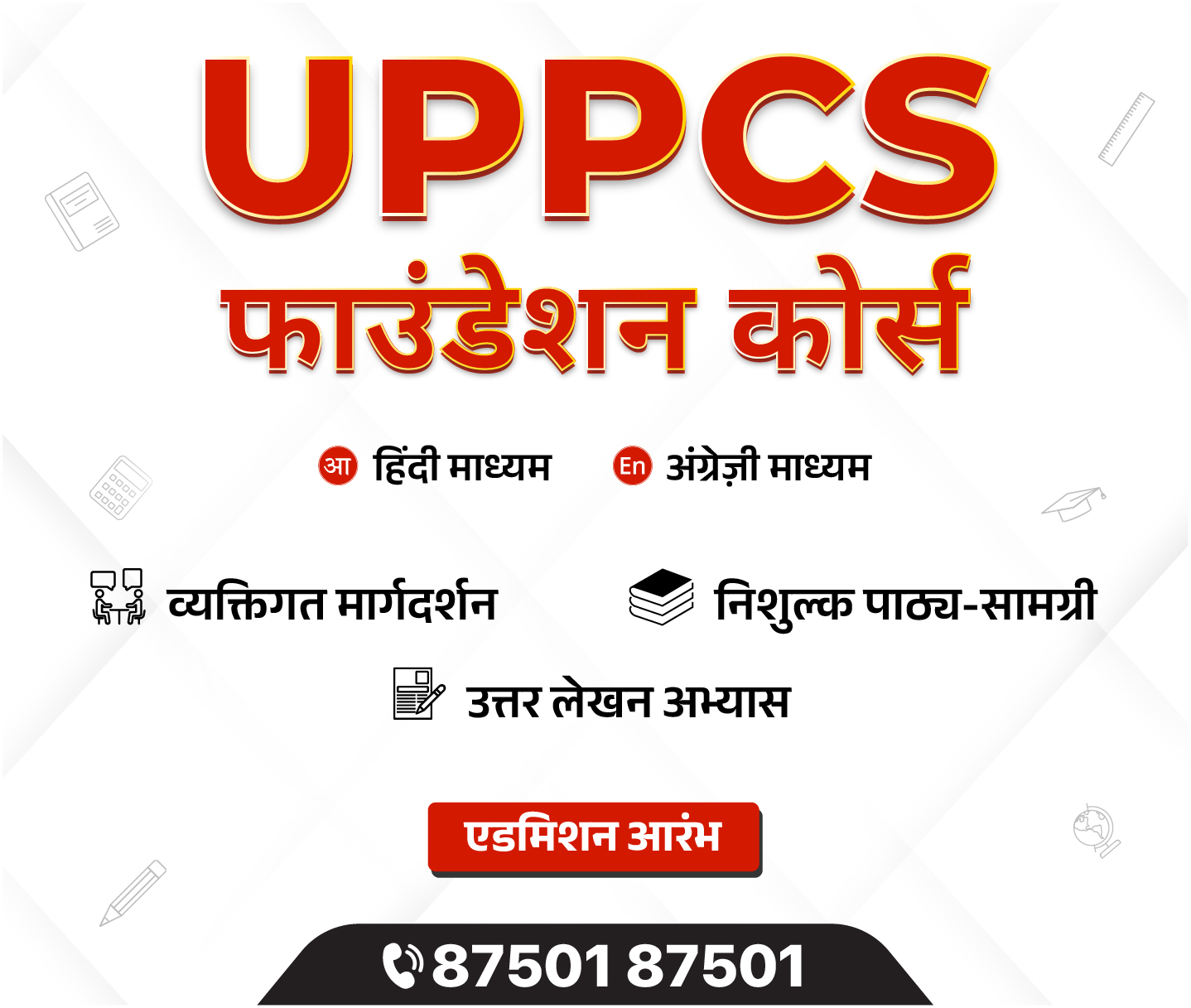
उत्तर प्रदेश Switch to English
स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन
चर्चा में क्यों?
स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के तहत दस लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में लखनऊ को अहमदाबाद और भोपाल के बाद देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर माना गया।
मुख्य बिंदु
शीर्ष प्रदर्शनकर्त्ता:
- लखनऊ:
- रैंकिंग: देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर (दस लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में)।
- उपलब्धि: 7-स्टार कचरा GFC रेटिंग प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर बना।
- प्रयागराज:
- सबसे स्वच्छ गंगा नगरी के रूप में विशेष पहचान अर्जित की, वाराणसी को पीछे छोड़कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- नोएडा:
- रैंकिंग: 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में सुपर स्वच्छ लीग में शीर्ष स्थान।
- शीर्ष स्तर के प्रदर्शनकर्त्ताओं को अलग से रैंक करने के लिये एक नई श्रेणी शुरू की गई।
- अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियाँ:
- 10 लाख से अधिक आबादी श्रेणी में उत्तर प्रदेश के सात शहर टॉप 20 में शामिल हैं: लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, गाज़ियाबाद, प्रयागराज और नोएडा।
- महाकुंभ 2025 के लिये पुरस्कार:
- महाकुंभ के दौरान स्वच्छता और साफ-सफाई की बेहतरीन व्यवस्थाओं के लिये विशेष पुरस्कार प्रदान किये गए, जो बड़े आयोजनों के दौरान राज्य की सफल स्वच्छता नीति को दर्शाते हैं।
- शीर्ष रेटिंग वाले शहर:
- 5-स्टार रेटिंग: आगरा, गोरखपुर, कानपुर, गाज़ियाबाद, प्रयागराज, नोएडा
- सफाईमित्र सुरक्षित शहर श्रेणी में तीसरा स्थान: गोरखपुर
- शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ शहर (3-10 लाख जनसंख्या): गोरखपुर (तीसरा ), मुरादाबाद (10वाँ )
- उभरता हुआ स्वच्छ शहर: आगरा (राष्ट्रीय स्तर पर 32वाँ स्थान )
- नई जल-प्लस उपलब्धियाँ:
- बिजनौर और शम्साबाद सहित 16 शहरों को पहली बार वाटर-प्लस का दर्जा मिला।
- स्वच्छता, जल प्रबंधन और पुनर्चक्रण प्रथाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले स्थानीय निकायों को जल-प्लस का दर्जा प्रदान किया जाता है।
- 17 नगर निगमों में से 13 को जल-प्लस का दर्जा प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है (जहाँ केवल 2 शहरों को जल-प्लस का दर्जा प्राप्त था)
- अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार:
- डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण (सत्यापित): एक वर्ष में 48% से बढ़कर 62%
- कचरा प्रसंस्करण: एक वर्ष में 48% से बढ़कर 85%
- राज्यव्यापी सुधार:
- शहरी स्थानीय निकाय (ULBs): 83 शहरी स्थानीय निकायों ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार किया
- ODF++ ULBs: 337 ULBs को ODF++ (खुले में शौच से मुक्त++) घोषित किया गया, जो पिछले वर्ष (129 ULBs) की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है।
स्वच्छ सर्वेक्षण
- वर्ष 2016 से आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) के तहत दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता और सफाई सर्वेक्षण है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहरों और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को दी जाने वाली वार्षिक रैंकिंग तथा मान्यताएँ हैं।
- इसका उद्देश्य नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना, स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और प्रदर्शन बेंचमार्किंग के माध्यम से प्रतिस्पर्द्धी संघवाद को बढ़ावा देना है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2025:
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 (9वें संस्करण) के संशोधित ढाँचे के तहत, संकेतकों को सरल बनाया गया है और 10 व्यापक खंडों में पुनर्गठित किया गया है।
- वर्ष 2025 के लिये वार्षिक थीम "रिड्यूस, रीयूज़, रीसायकल (3R)" है, जो 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम (मार्च 2025) में अपनाए गए जयपुर घोषणा-पत्र के अनुरूप सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांतों को बढ़ावा देता है।
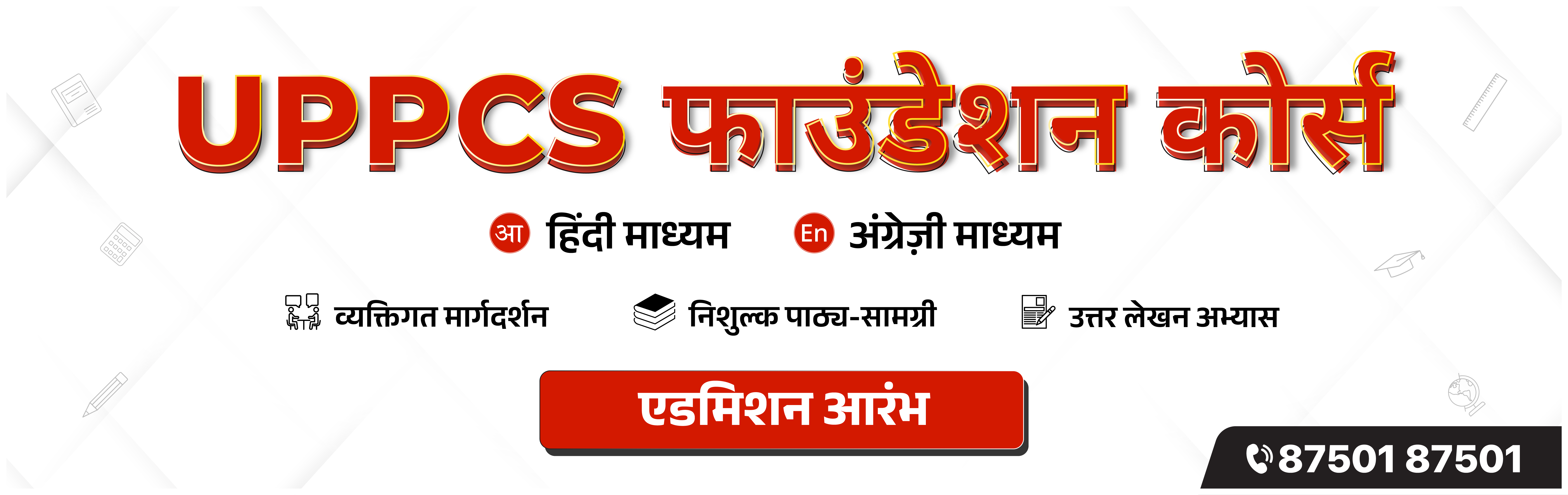
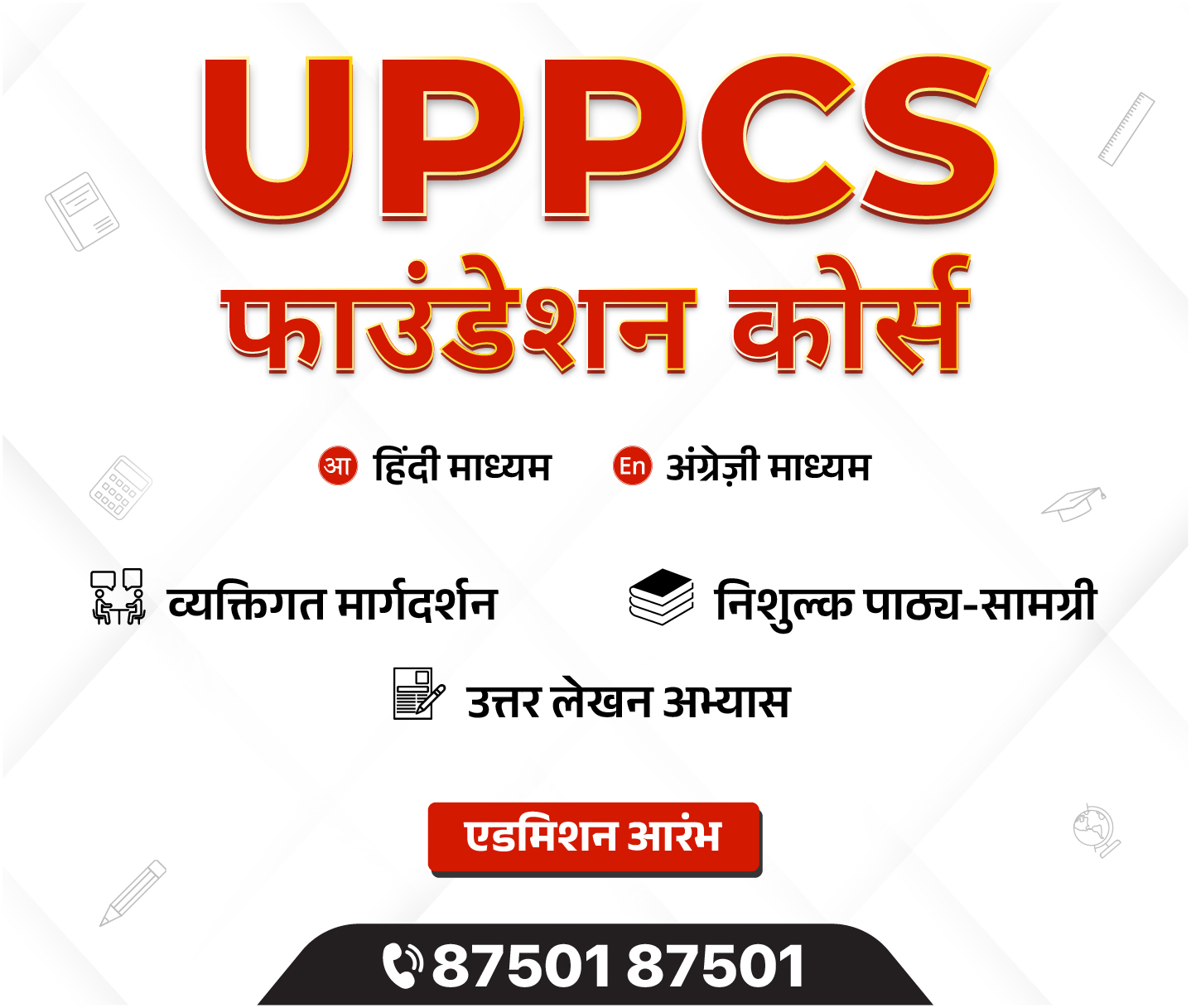

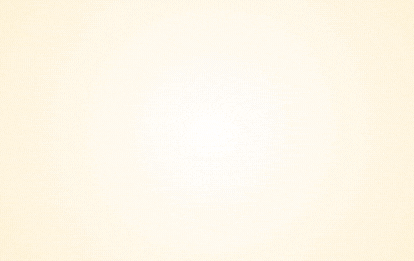



 PCS परीक्षण
PCS परीक्षण


