मध्य प्रदेश Switch to English
मध्य प्रदेश में 'रीवाइल्डिंग' पहल
चर्चा में क्यों?
'टाइगर स्टेट' के नाम से प्रसिद्ध मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में 'रीवाइल्डिंग' नामक एक पहल शुरू की गई है।
मुख्य बिंदु:
- पहल के बारे में:
- 'रीवाइल्डिंग' पहल का उद्देश्य प्रमुख प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में पुनः स्थापित करना है और इसे भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिये एक मॉडल बनाने का लक्ष्य है।
- इसमें ऐसे हिंसक (predator) और शिकार प्रजातियों (prey species) को पुनः स्थापित किया जा रहा है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन वर्तमान में वनों में अनुपस्थित हैं।
- इनकी अनुपस्थिति में खाद्य शृंखला टूट जाती है और प्राकृतिक जीवनचक्र क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है।
- उद्देश्य :
- वन्यजीव पारिस्थितिकी में संतुलन बहाल करना।
- विलुप्त एवं संकटग्रस्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करना।
- जैवविविधता को बढ़ावा देना।
- कार्यान्वयन :
- वन विभाग ने दलदली हिरण और अन्य प्रजातियों को पुनः लाने के लिये एक चरणबद्ध पुनर्वनीकरण योजना बनाई है, जिसमें घास के मैदानों, नदी के दृश्यों और सहायक आवासों सहित पूरे वन पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- इस मिशन को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), वन अनुसंधान संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का समर्थन प्राप्त है।
- जनजातीय और ग्रामीण समुदायों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, ताकि वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ पारिस्थितिकी पर्यटन और आजीविका के अवसर भी सृजित हो सकें।
- महत्त्व:
- रीवाइल्डिंग जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह कार्बन भंडारण को बढ़ाता है, कार्बन उत्सर्जन को कम करता है और जल तथा मृदा जैसे महत्त्वपूर्ण संसाधनों का संरक्षण करता है, जिससे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा होती है।
- पारिस्थितिकी लाभों के अलावा, रीवाइल्डिंग वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करता है और प्राकृतिक चक्रों को मानव हस्तक्षेप से अप्रभावित बनाए रखता है।
राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स Switch to English
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का 8वाँ स्थापना दिवस
चर्चा में क्यों?
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने 1 सितंबर 2025 को अपना 8वाँ स्थापना दिवस मनाया और समावेशी तथा सुलभ बैंकिंग सेवाएँ अंतिम छोर तक पहुँचाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
मुख्य बिंदु
- IPPB के बारे में:
- इसकी स्थापना वर्ष 2018 में डाक विभाग के अधीन एक सरकारी पहल के रूप में की गई थी।
- इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना और डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाना है।
- क्षेत्र
- IPPB के पास 1.64 लाख से अधिक डाकघर तथा 1.90 लाख डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक (GDS) कार्यरत हैं।
- यह 12 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करता है, अरबों डिजिटल लेन-देन संपन्न करता है तथा ग्रामीण, अर्द्ध-शहरी और दूरस्थ क्षेत्रों में घर-घर बैंकिंग उपलब्ध कराता है।
- उद्देश्य
- प्रत्येक भारतीय को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह प्रशस्त करना।
- अंतिम छोर तक बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाना ताकि ग्रामीण एवं वंचित आबादी भी वित्तीय रूप से समावेशित हो सके
- सेवाएँ:
- IPPB ने अपनी सेवाओं का विस्तार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) वितरण, पेंशन भुगतान, ऋण सुविधा, बीमा और निवेश उत्पादों तक किया है, जो विभिन्न संस्थानों के सहयोग से उपलब्ध कराए जाते हैं।
- नई सेवाओं में डिजी स्मार्ट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, प्रीमियम आरोग्य सेविंग्स अकाउंट, आधार-आधारित चेहरा प्रमाणीकरण, रूपे वर्चुअल डेबिट कार्ड, AePS सक्षम भुगतान, अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण और भारत बिल-पे एकीकरण शामिल हैं, जिन्होंने ग्राहकों की सुविधा को तथा बढ़ाया है।
पेमेंट्स बैंक
- परिचय:
- पेमेंट्स बैंक एक विभेदित बैंक (Differentiated Bank) है, जो सीमित बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है।
- डॉ. नचिकेत मोर समिति ने निम्न-आय वर्गों और छोटे व्यवसायों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पेमेंट्स बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी।
- विशेषताएँ:
- यह केवल बचत और चालू खातों में मांग जमा स्वीकार कर सकता है, सावधि जमा नहीं।
- प्रत्येक ग्राहक पेमेंट्स बैंक खाते में अधिकतम 2,00,000 रुपए की शेष राशि रख सकता है।
- पेमेंट्स बैंक अनिवासी भारतीय (Non-Resident Indian-NRI) जमा स्वीकार नहीं कर सकते।
- पेमेंट्स बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवा गतिविधियाँ शुरू करने के लिये सहायक कंपनियाँ स्थापित नहीं कर सकते हैं।
राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स Switch to English
युद्ध अभ्यास 2025
चर्चा में क्यों?
भारतीय सेना का एक दल अमेरिका के अलास्का स्थित फोर्ट वेनराइट के लिये प्रस्थान कर चुका है, जहाँ 1 से 14 सितंबर, 2025 तक भारत-अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘युद्ध अभ्यास’ का 21वाँ संस्करण आयोजित किया जाएगा।
मुख्य बिंदु
- भाग लेने वाली सेनाएँ:
- भारतीय दल में मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन के कार्मिक शामिल हैं, जो भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंटों में से एक है।
- अमेरिकी सेना का प्रतिनिधित्व 11वीं एयरबोर्न डिवीज़न के अंतर्गत आर्कटिक वोल्व्स ब्रिगेड कॉम्बैट टीम की पहली बटालियन, 5वीं इन्फैंट्री रेजीमेंट “बॉबकैट्स” के सैनिकों द्वारा किया जाएगा।
- गतिविधियाँ:
- अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाएँ विविध सामरिक कौशलों का अभ्यास करेंगी, जिनमें हेलिबोर्न ऑपरेशन, निगरानी संसाधनों एवं मानव रहित हवाई प्रणालियों का प्रयोग, रॉकक्राफ्ट, पर्वतीय युद्धकला, हताहतों की निकासी, युद्धक्षेत्र चिकित्सा सहायता तथा तोपखाने, वायुसेना एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों का समन्वित उपयोग शामिल है।
- अभ्यास का समापन:
- यह अभ्यास संयुक्त रूप से नियोजित एवं क्रियान्वित सामरिक अभियानों के साथ संपन्न होगा, जिनमें लाइव-फायर ड्रिल्स से लेकर उच्च पर्वतीय युद्ध परिदृश्यों तक की अभिव्यक्ति होगी।
- उद्देश्य:
- ‘युद्ध अभ्यास 2025’ का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों के लिये परिचालन तत्परता को सुदृढ़ करना है, जिससे शांति अभियानों के प्रभावी प्रबंधन हेतु क्षमता-निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।
- इसके अतिरिक्त, यह अभ्यास बहु-क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने हेतु सेनाओं को तैयार करेगा तथा एकीकृत युद्ध और संयुक्त परिचालन रणनीतियों के महत्त्व पर ज़ोर देगा।
राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स Switch to English
आदि वाणी
चर्चा में क्यों?
जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय गौरव वर्ष (JJGV) समारोह के हिस्से के रूप में जनजातीय भाषाओं के लिये भारत के पहले AI-संचालित अनुवाद मंच ‘आदि वाणी’ का बीटा संस्करण लॉन्च किया है।
मुख्य बिंदु
- आदि वाणी के बारे में
- आदि वाणी को IIT दिल्ली के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय संघ द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें BITS पिलानी, IIIT हैदराबाद, IIIT नवा रायपुर तथा झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का सहयोग शामिल है।
- बीटा संस्करण वर्तमान में संथाली, भीली, मुंडारी और गोंडी भाषाओं का समर्थन करता है, जबकि कुई और गारो जैसी भाषाओं पर विकास कार्य प्रगति पर है।
- प्रमुख विशेषताएँ:
- हिंदी, अंग्रेजी और जनजातीय भाषाओं के बीच वास्तविक समय में पाठ एवं वाक् अनुवाद की सुविधा।
- छात्रों और नव-शिक्षार्थियों के लिये इंटरैक्टिव भाषा शिक्षण मॉड्यूल।
- लोककथाओं एवं मौखिक परंपराओं का डिजिटलीकरण कर सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण।
- जनजातीय भाषाओं में सरकारी परामर्श एवं स्वास्थ्य संबंधी संदेश, उपशीर्षकों सहित उपलब्ध कराना।
जनजातीय गौरव वर्ष (JJGV)
- यह वर्ष भगवान बिरसा मुंडा (धरती आबा) की 150वीं जयंती का स्मरण करता है तथा जनजातीय नायकों की अद्वितीय विरासत को सम्मानित करता है।
- इसे 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव दिवस (2021 में घोषित) के एक साल के विस्तार के रूप में मनाया जा रहा है।
- यह पहल धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान तथा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM JANMAN) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों से जुड़ी हुई है।
उद्देश्य:
- भारत की सांस्कृतिक अस्मिता और स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक योगदान को रेखांकित करना।
- संपूर्ण शासन दृष्टिकोण के माध्यम से जनजातीय कल्याण को प्रोत्साहित करना।
- जनजातीय विकास संबंधी पहलों में जनभागीदारी (लोगों की सक्रिय सहभागिता) को बढ़ावा देना।
- जनजातीय नायकों के प्रति जागरूकता और राष्ट्र-निर्माण में उनकी भूमिका की पहचान को सुदृढ़ करना।
राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स Switch to English
अग्निवीर क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2025
चर्चा में क्यों?
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT के 65वें स्थापना दिवस पर अनेक पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने संस्थान से शिक्षा के प्रति सुधारोन्मुख एवं प्रौद्योगिकी-आधारित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया।
मुख्य बिंदु
शुभारंभ की गई प्रमुख पहलें:
- पीएम ई-विद्या मोबाइल एप्लिकेशन:
- यह पीएम ई-विद्या के अंतर्गत सभी प्रमुख डिजिटल एवं प्रसारण पहलों तक पहुँच हेतु एक केंद्रीकृत पोर्टल है, जिसे BISAG-N के सहयोग से विकसित किया गया है।
- दीक्षा 2.0 :
- इसमें संरचित पाठ, अनुकूली मूल्यांकन, प्रदर्शन फीडबैक, चर्चा मंच और एआई उपकरण जैसे रीड अलाउड, क्लोज्ड कैप्शन तथा 12 भाषाओं में पाठ फाइलों का अनुवाद शामिल है।
- प्रशस्त 2.0:
- यह एक पूर्व-मूल्यांकन समग्र स्क्रीनिंग टूल है जो दिव्यांग बच्चों की शीघ्र पहचान के लिये मोबाइल और वेब प्लेटफॉर्म को उन्नत करता है।
- किताब एक पढ़े अनेक :
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप यह पहल यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ़ लर्निंग (UDL) आधारित सुलभ डिजिटल एवं मुद्रित पाठ्यपुस्तकों के निर्माण पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य समावेशी कक्षाओं की स्थापना करना है, जिससे विशेषकर दिव्यांगजन छात्रों एवं सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों को लाभ मिल सके।
- उत्कल जननींकर सुजोग्य संतान :
- यह पुस्तक ओडिशा के 100 महान व्यक्तित्वों के जीवन और योगदान पर आधारित है, जिन्होंने आधुनिक ओडिशा के विकास में योगदान दिया तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया।
NCERT (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद)
- स्थापना: 1 सितंबर 1961
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- उद्देश्य: भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में , यह विद्यालयी शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सहायता तथा सलाह देता है।
- कार्य: पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण-अधिगम सामग्री और नवीन शैक्षणिक उपकरण विकसित करना, साथ ही अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी संचालित करना।
उत्तर प्रदेश Switch to English
शोध प्रकाशनों को DOI से संबद्ध करना
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) की वैश्विक पहचान और शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देने के लिये राज्य की उच्च शिक्षा विभाग ने सभी शैक्षणिक प्रकाशनों को डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर (DOI) से संबद्ध करने को अनिवार्य कर दिया है।
- इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शोध-पत्र, शोध प्रबंध, सारांश, परियोजना कार्यवाही और अन्य शैक्षणिक उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दृश्यता प्राप्त करें।
- वर्तमान में, समर्थ-CAS पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा प्रकाशित कुल 104,742 शोध प्रकाशनों में से केवल लगभग 8% (8,410 प्रकाशन) ही DOI से संबद्ध किये गए हैं।
मुख्य बिंदु
- डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर (DOI):
- यह एक अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक शृंखला (string) है, जो डिजिटल सामग्री, जैसे शोध-पत्र और शोध प्रबंध, को सौंपी जाती है।
- यह शैक्षणिक कार्य के लिये स्थायी और स्थिर कड़ी के रूप में कार्य करता है तथा समय के साथ इसकी पहुँच, खोज तथा उद्धरण सुनिश्चित करता है।
- DOI का उपयोग वैश्विक स्तर पर शोधकर्त्ता, प्रकाशक और शैक्षणिक डेटाबेस अपने शैक्षणिक कार्यों को कुशलतापूर्वक ट्रैक तथा संबद्ध करने के लिये करते हैं।
- उद्देश्य:
- DOI संबद्धता की ओर यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में उल्लिखित दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो शैक्षणिक संस्थानों की वैश्विक मान्यता और शिक्षा में प्रौद्योगिकी के समावेश पर ज़ोर देता है।
उत्तराखंड Switch to English
अग्निवीर क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2025
चर्चा में क्यों?
उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिये 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्हें आयु सीमा में छूट तथा भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट प्रदान की गई है।
मुख्य बिंदु
- आरक्षण के बारे में:
- उत्तराखंड कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा अग्निवीर क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2025 अधिसूचित कर दी गई है।
- यह कोटा राज्य के स्थायी निवासियों के लिये ग्रुप-सी वर्दीधारी सेवाओं के तहत सीधी भर्ती पर लागू होगा, जिसमें पुलिस, अग्निशमन, वन, जेल, आबकारी और सचिवालय सेवाओं के विभिन्न पद शामिल हैं।
- अग्निपथ योजना
- अग्निपथ योजना जून 2022 में सशस्त्र बलों के लिये अल्पकालिक भर्ती नीति के रूप में प्रारंभ की गई थी।
- इसके अंतर्गत 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को 4 वर्षों के लिये अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाता है, जिनमें से अधिकतम 25% को स्थायी कैडर में सम्मिलित किया जाता है।
- अग्निवीरों को बुनियादी और विशेष सैन्य प्रशिक्षण के साथ-साथ कौशल उन्नयन पाठ्यक्रम भी प्रदान किया जाता है।
- सेवा-समाप्ति पर उन्हें कर-मुक्त सेवा निधि पैकेज मिलता है, जो भविष्य के करियर हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।
- प्रत्येक अग्निवीर को सेवा अवधि के दौरान 48 लाख रुपये की जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है।
मध्य प्रदेश Switch to English
इंदौर को CII ग्रीन सिटी प्रमाणन प्राप्त
चर्चा में क्यों?
इंदौर मध्य प्रदेश का पहला शहर तथा देश के प्रमुख तीन शहरों में से एक बन गया है जिसे CII की इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) द्वारा ‘ग्रीन सिटी प्लैटिनम’ प्रमाणन प्रदान किया गया है।
मुख्य बिंदु
- इंदौर की मान्यता:
- यह मान्यता प्रशासन द्वारा IGBC को प्रस्तुत किये गए एक दर्जन से अधिक मापदंडों पर आधारित विस्तृत आँकड़ों के छह माह तक चले मूल्यांकन के उपरांत प्रदान की गई।
- इस मूल्यांकन में मास्टर प्लानिंग, जल एवं ऊर्जा संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ई-गवर्नेंस, हरित आवरण के विस्तार तथा विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों से संबंधित शहर की पहलों को सम्मिलित किया गया।
- पूर्व प्राप्तकर्त्ता
-
IGBC द्वारा ग्रीन सिटी प्लैटिनम प्रमाणन प्राप्त करने वाले पूर्व शहरों में शामिल हैं:
-
राजकोट स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड (RSCDL)
-
पुणे नगर निगम
-
पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम
-
-
-
IGBC ग्रीन विद्यमान शहर):
- IGBC ग्रीन सिटीज (विद्यमान शहर) रेटिंग प्रणाली एक स्वैच्छिक एवं आम-सहमति आधारित कार्यक्रम है, जिसे IGBC ग्रीन सिटीज कमेटी के सहयोग से विकसित किया गया है।
- यह भारत की अपनी तरह की पहली रेटिंग प्रणाली है, जो विद्यमान शहरों में पर्यावरणीय स्थिरता को संबोधित करती है।
- इस प्रणाली के माध्यम से नगर पालिकाओं, नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों एवं डेवलपर्स को हरित नीति हस्तक्षेप तैयार करने और शहर-स्तर पर हरित पहलों को लागू करने में सहायता मिलती है।
- इसका उद्देश्य पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करना तथा शहरी जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है।
भारतीय हरित भवन परिषद (IGBC)
- यह एक गैर-लाभकारी, सदस्य-संचालित परिषद है, जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा भारत में स्थायी भवन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिये की गई।
- यह परिषद आवासीय, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण-उत्तरदायी निर्माण और डिज़ाइन को प्रोत्साहित करने के लिये हरित भवन रेटिंग प्रणाली, प्रमाणन सेवाएँ एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करती है।

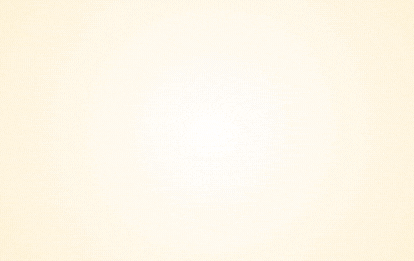



 PCS परीक्षण
PCS परीक्षण

