हरियाणा Switch to English
हरियाणा में उन्नत लिथियम-आयन बैटरी संयंत्र
चर्चा में क्यों?
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के सोहना में TDK कॉर्पोरेशन के उन्नत प्रौद्योगिकी लिथियम-आयन (ली-आयन) बैटरी विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया।
- TDK कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है, जो 30 से अधिक देशों में 250 से अधिक विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास और विक्रय स्थलों का संचालन करती है।
मुख्य बिंदु
- इस संयंत्र में मोबाइल फोन, लैपटॉप, पहनने योग्य उपकरणों (wearables) और सुनने योग्य उपकरणों जैसे घड़ियों, ईयरबड्स और एयरपॉड्स में उपयोग होने वाली ली-आयन बैटरियों का निर्माण किया जाएगा।
- इससे प्रतिवर्ष 20 करोड़ बैटरी पैक का उत्पादन होने की संभावना है, जो भारत की 50 करोड़ पैक की वार्षिक मांग का लगभग 40% पूरा करेगा।
- यह संयंत्र भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC) योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
- इस परियोजना से लगभग 5,000 प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होंगे तथा श्रमिकों को AT बावल संयंत्र में प्रारंभिक प्रशिक्षण पहले ही दिया जा चुका है।
- सोहना संयंत्र भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में वैश्विक केंद्र बनाने, आयात पर निर्भरता घटाने और वैश्विक मूल्य शृंखला में योगदान देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
छत्तीसगढ़ Switch to English
राष्ट्रीय इनक्यूबेटर पुरस्कार
चर्चा में क्यों?
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर की इनोवेशन और उद्यमिता फाउंडेशन (FIE) को 13 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित चौथे भारत उद्यमिता शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय इनक्यूबेटर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
मुख्य बिंदु
- स्थापना:
- NIT रायपुर-FIE की स्थापना मार्च 2021 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के नवाचारों के विकास एवं उपयोग के लिये राष्ट्रीय पहल (NIDHI) कार्यक्रम के तहत एक गैर-लाभकारी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर के रूप में की गई थी।
- पुरस्कार का कारण:
- यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ में 35 से अधिक स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन देने और प्रभावी तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये दिया जा रहा है।
- स्टार्टअप्स में गवर्नेंस, मेडिकल डिवाइस, एनालिटिक्स, डीप-टेक, क्लीन टेक और ICT शामिल हैं।
- आयोजक:
- शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्यमी संघ (EAI) और सरकार द्वारा वित्तपोषित, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इनक्यूबेशन केंद्र, एंटरप्राइजिंग ज़ोन (EZ) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।
- महत्त्व:
- छत्तीसगढ़ में युवाओं को मार्गदर्शन देकर भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करना।
- छत्तीसगढ़ को नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायता।
- उद्यमिता को बढ़ावा देने और तकनीकी आधारित आर्थिक विकास में योगदान।
नवाचारों के विकास एवं उपयोग के लिये राष्ट्रीय पहल (NIDHI)
- परिचय:
- यह एक अभूतपूर्व पहल है जिसे नवाचार को बढ़ावा देने, स्टार्टअप का समर्थन करने और भारत में एक संपन्न उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिये अभिकल्पित किया गया है।
- इसमें विभिन्न घटक शामिल हैं जो देश भर में नवाचार-संचालित उद्यमों को बढ़ावा देने तथा उनमें तेज़ी लाने के लिये एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं
- निधि कार्यक्रम के घटक:
- निधि-प्रयास (युवा और महत्त्वाकांक्षी इनोवेटर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देना और उनमें तेज़ी लाना):
- यह नवीन विचारों को मूर्त प्रोटोटाइप में परिवर्तित करने पर केंद्रित है।
- यह प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट स्तर पर सलाह और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- निधि उद्यमी-इन-रेज़िडेंस (EIR) कार्यक्रम:
- यह उद्यमिता अपनाने वाले छात्रों को फेलोशिप/छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है।
- निधि-प्रयास (युवा और महत्त्वाकांक्षी इनोवेटर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देना और उनमें तेज़ी लाना):
- प्रमुख अभिकर्त्ता और सहयोगी:
- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR):
- NIDHI अत्याधुनिक इनक्यूबेशन सुविधाओं को आकार देने और विकसित करने के लिये CSIR के साथ मिलकर सहयोग करती है।
- यह उन्नत इनक्यूबेशन सुविधाओं की संकल्पना और विकास में सक्रिय भूमिका निभाती है।
- प्रौद्योगिकी और उत्पादों का समर्थन करना जिससे समाज, उद्योग और देश को लाभ होता है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY):
- टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स (TIDE 2.0) योजना में MeitY के साथ NIDHI की साझेदारी तकनीक-संचालित स्टार्टअप को सशक्त बनाती है।
- साथ में वे प्रौद्योगिकी-आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology- DST) की स्थापना 3 मई, 1971 को नेशनल साइंस फाउंडेशन (NSF), USA के मॉडल पर की गई थी।
- यह यह वित्तपोषण तथा नीतिगत सहयोग प्रदान करता है तथा अन्य देशों के साथ वैज्ञानिक कार्यों का समन्वय करता है।
- यह वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक संस्थानों को सशक्त बनाता है तथा स्कूल कॉलेज, पी.एच.डी., पोस्टडॉक छात्रों, युवा वैज्ञानिकों, स्टार्टअप एवं विज्ञान व प्रौद्योगिकी में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हितधारकों के साथ एक उच्च वितरित प्रणाली के तहत भी काम करता है।
उत्तर प्रदेश Switch to English
उत्तर प्रदेश युक्तधारा पोर्टल के साथ एकीकृत
चर्चा में क्यों?
1 अप्रैल 2026 से उत्तर प्रदेश GIS-आधारित भू-स्थानिक योजना प्रणाली युक्तधारा पोर्टल के साथ एकीकृत हो जाएगा, ताकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MNREGS) के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों की वास्तविक समय में निगरानी और योजना बनाई जा सके।
मुख्य बिंदु
- युक्तधारा पोर्टल के बारे में:
- भू-स्थानिक नियोजन तंत्र: पूरे भारत में मनरेगा गतिविधियों की ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजन की सुविधा प्रदान करता है।
- GIS एकीकरण: समग्र ग्रामीण नियोजन को सुगम बनाने करने के लिये ओपन-सोर्स भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) उपकरणों का उपयोग करता है।
- व्यापक अभिलेख: प्रत्येक कार्य की कार्य योजना, स्थान, लागत और प्रगति को दर्ज किया जाता है और उसका मानचित्रण किया जाता है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: यह भुगतान प्रक्रियाओं में विसंगतियों को रोकने और अनियमितताओं को न्यूनतम करने के लिये विकसित किया गया है।
- ग्रामीणों को लाभ
- समय पर रोज़गार और विकास कार्यों के रूप में प्रत्यक्ष लाभ।
- सभी ग्राम-स्तरीय कार्यों पर पारदर्शी एवं सुलभ जानकारी।
- बढ़ी हुई पारदर्शिता के कारण भ्रष्टाचार या अनियमितताओं की संभावना न्यूनतम।
- क्षमता निर्माण पहल:
- राज्य सरकार ने ज़िला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर बैचवार प्रशिक्षण सत्र शुरू किये हैं।
- प्रशिक्षण से यह सुनिश्चित होता है कि अधिकारी और स्थानीय योजनाकार पोर्टल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम हों।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना
- मनरेगा के बारे में:
- यह एक केंद्र प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार की गारंटी प्रदान करना है।
- इसे वर्ष 2005 में अधिनियमित किया गया तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया।
- विस्तार:
- यह योजना पूरे देश में लागू है, केवल 100% शहरी आबादी वाले ज़िले को छोड़कर।
- वित्तीय साझेदारी:
- केंद्र सरकार अकुशल श्रम लागत का 100% तथा सामग्री लागत का 75% वहन करती है, जबकि राज्य सरकारें सामग्री लागत का 25% योगदान करती हैं।
- इस प्रकार, इसके क्रियान्वयन में सहकारी संघवाद की भावना सुनिश्चित होती है।
राजस्थान Switch to English
दुर्लभ कैराकल शावक
चर्चा में क्यों?
विशेषज्ञों ने जैसलमेर के मरुस्थल में दुर्लभ कैराकल (Caracal) शावक की उपस्थिति की पुष्टि की है, जो राजस्थान के लिये एक महत्त्वपूर्ण वन्यजीव खोज है।
- इस खोज के बाद प्रशासन ने जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या सर्वेक्षण प्रारंभ कर दिया है तथा गश्त को और तेज़ कर दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- कैराकल के बारे में:

- कैराकल एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है, जो भारत सहित अफ्रीका, मध्य-पूर्व और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है।
- भारत में इसकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 50 है, जो मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है।
- यह स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक शिकारी के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अपनी विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं तथा उल्लेखनीय शिकार क्षमताओं के लिये जानी जाती है।
- आवास:
- कैराकल सवाना, अर्द्ध-मरुस्थल, शुष्क वन क्षेत्र, चट्टानी पहाड़ियाँ, शुष्क पर्वतीय मैदानों तथा शुष्क पर्वतीय क्षेत्रों के लिये अनुकूल है।
- वर्गीकरण और संबंध:
- कैराकल वास्तविक लिंक्स की तुलना में अफ्रीकी गोल्डन बिल्ली और सर्वल से अधिक निकटता से संबंधित है, हालांकि इसे प्रायः "रेगिस्तानी लिंक्स" कहा जाता है।
- भारत में इसे ‘स्याहगोश’ कहा जाता है, जो फारसी शब्द से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है ‘काले कान’।
- इसका वैज्ञानिक नाम कैराकल कैराकल श्मिट्ज़ी है।
- शारीरिक विशेषताएँ:
- कैराकल का शरीर पतला और पैर लंबे होते हैं तथा यह अफ्रीका की छोटी बिल्लियों में सबसे बड़ी होती है।
- वयस्कों का वज़न 8-18 किलोग्राम तक होता है और इनकी लंबाई लगभग एक मीटर तक पहुँच सकती है। नर सामान्यतः मादाओं से बड़े होते हैं।
- इसका फर छोटा और घना होता है, जिसका रंग हल्के भूरे से लाल-भूरे तक होता है, जबकि नीचे का भाग हल्का रहता है।
- चेहरे पर विशिष्ट रेखाएँ और आँखों के चारों ओर सफेद निशान इसकी पहचान हैं।
- संरक्षण की स्थिति:
- IUCN रेड लिस्ट: कम चिंताजनक
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची 1
- खतरे:
- आवास का क्षरण, शिकार-आधार में कमी तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष।

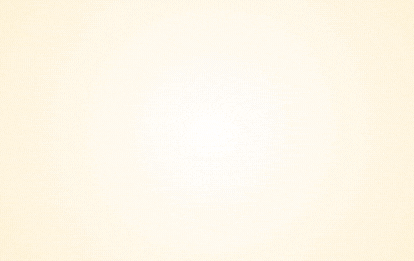



 PCS परीक्षण
PCS परीक्षण

