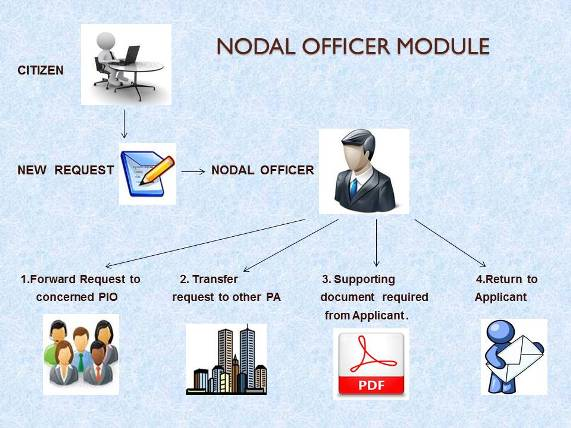भारतीय राजव्यवस्था
RTI अधिनियम, 2005 के 20 वर्ष
- 11 Oct 2025
- 67 min read
प्रिलिम्स के लिये: सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005, शासकीय गुप्त बात अधिनियम (OSA), 1923, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग, RTI संशोधन अधिनियम, 2019, डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In), सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2014, डिजिलॉकर
मेन्स के लिये: RTI अधिनियम, 2005 संबंधी मुख्य तथ्य, इसकी प्रभावशीलता को सीमित करने वाली चुनौतियाँ और इसके कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने की रणनीतियाँ
चर्चा में क्यों?
अक्तूबर 2025 में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर, एक अध्ययन किया गया, जिसमें इसकी कार्य-पद्धति की गंभीर खामियों को उजागर किया है, जो यह दर्शाता है कि पारदर्शिता प्रणाली पर गंभीर दबाव है।
RTI अधिनियम, 2005 संबंधी मुख्य तथ्य क्या हैं?
- परिचय: वर्ष 2005 में अधिनियमित, सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 का उद्देश्य नागरिकों को लोक प्राधिकारियों द्वारा धारित जानकारी तक अबाध पहुँच प्रदान कराना है।
- यह शासकीय कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने, उत्तरदायित्व का सुदृढ़ीकरण करने और लोक संस्थानों में सुशासन के सिद्धांतों में सुधार लाने के लिये अभिकल्पित किया गया था।
- पुणे में शाहिद रज़ा बर्नी द्वारा दायर RTI इस कानून के तहत दायर की गई पहली RTI थी।
- मुख्य घटक: यह अधिनियम केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों सहित सरकार के सभी स्तरों पर प्रवर्तनीय है।
- धारा 8(2) के अंतर्गत लोक हित का शासकीय गुप्त बात से अधिक महत्त्वपूर्ण होने पर इसका प्रकटीकरण किये जाने की अनुमति है और धारा 22 के अंतर्गत RTI अधिनियम, 2005 को अन्य कानूनों के साथ किसी भी विसंगति की दशा में वरीयता दिया जाना सुनिश्चित किया गया है।
- प्रदत्त छूट: RTI अधिनियम, 2005 में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद, नागरिक कोई भी ऐसी सूचना प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों को क्षति पहुँचा सकती हो, अन्य देशों के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकती हो, या इससे किसी अपराध का उद्दीपन हो सकता हो।
- सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019: मूल रूप से RTI अधिनियम, 2005 के तहत, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद ग्रहण करते थे तथा उनका वेतन एवं सेवा की शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समान होती थीं।
- हालाँकि वर्ष 2019 के संशोधन ने इसे बदल दिया, जिससे केंद्र सरकार को उनके कार्यकाल, वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें निर्धारित करने की शक्ति मिल गई।
- RTI अधिनियम, 2005 की उपलब्धियाँ: इससे सार्वजनिक निधि के उपयोग में जवाबदेही बढ़ी है, जिससे नागरिकों को मनरेगा व्यय, PDS रिकॉर्ड और स्थानीय विकास परियोजनाओं तक पहुँच प्राप्त हुई है तथा लीकेज एवं दुरुपयोग में कमी आई है।
- इसने आदर्श सोसायटी, 2G स्पेक्ट्रम और राष्ट्रमंडल खेलों जैसे हाई-प्रोफाइल घोटालों को उज़ागर किया है, साथ ही सरकारी अधिकारियों में जवाबदेही की संस्कृति का निर्माण किया है, तथा उन्हें यह बोध कराया कि उनके कार्य सार्वजनिक जाँच के अधीन हैं।
RTI अधिनियम, 2005 के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?
- अत्यधिक विलंब: अधिकांशतः सूचना आयोगों (IC) में किसी मामले के निपटान में एक वर्ष से ज़्यादा का समय लग जाता है। कुछ राज्यों में तो यह विलंबता बहुत अधिक है, तेलंगाना में यह अनुमानतः 29 वर्ष और 2 माह एवं त्रिपुरा में 23 वर्ष है।
- रिक्त पद: वर्ष 2023 और वर्ष 2024 के बीच, नए आयुक्तों की नियुक्ति न होने के कारण छह सूचना आयोग अलग-अलग अवधि के लिये पूर्णतः निष्क्रिय हो गए।
- वर्तमान में झारखंड और हिमाचल प्रदेश आयोग निष्क्रिय हैं, जबकि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC), छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश आयोग मुख्य सूचना आयुक्त के बिना काम कर रहे हैं।
- विधायी परिवर्तनों के माध्यम से क्षरण: RTI संशोधन अधिनियम, 2019 ने केंद्र सरकार को उनका कार्यकाल और वेतन निर्धारित करने का अधिकार देकर सूचना आयुक्तों की स्वायत्तता को कम कर दिया।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 ने धारा 8(1) में संशोधन किया, जिससे लोक सेवकों सहित सभी व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट मिल गई।
- छूट का विस्तार: सरकारी विभाग अक्सर शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रावधानों का हवाला देते हुए RTI के तहत जानकारी देने से इनकार कर देते हैं। उदाहरण के लिये, RAW, IB और CERT-In जैसी एजेंसियों को RTI अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची के तहत छूट प्राप्त है।
- RTI कार्यकर्त्ताओं को धमकियाँ: RTI कार्यकर्त्ताओं को उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिससे नागरिक भ्रष्टाचार को उज़ागर करने के जोखिम से बचते हैं। विभिन्न कार्यकर्त्ताओं पर हमले हुए हैं या उनकी हत्या कर दी गई है, जबकि व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 के तहत सुरक्षा उपायों का क्रियान्वयन अभी भी शिथिल है।
RTI ढाँचे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये किन सुधारों की आवश्यकता है?
- सूचना आयोग को सुदृढ़ बनाना: पारदर्शी, समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से IC की समय पर नियुक्तियाँ सुनिश्चित करना और आयोगों को पर्याप्त स्टाफ, प्रौद्योगिकी तथा बुनियादी ढाँचा प्रदान करना।
- लंबित मामलों को कुशलतापूर्वक कम करने के लिये प्रत्येक आयुक्त के लिये प्रदर्शन मानक स्थापित करना।
- प्रौद्योगिकी का समेकन: AI चैटबॉट और स्वचालित सहायक नागरिकों को RTI आवेदन तैयार करने में मदद कर सकते हैं, जबकि ब्लॉकचेन डेटा की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है।
- RTI पोर्टलों का डिजिलॉकर और रीयल-टाइम ट्रैकिंग के साथ एकीकरण, आवेदनों तक पहुँच एवं उनकी निगरानी में सुधार ला सकता है।
- कानून का कठोर अनुपालन: RTI अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत अनिवार्य सक्रिय प्रकटीकरण को प्रभावी रूप से लागू किया जाए तथा अनुचित अस्वीकृति या विलंब के मामलों में लोक सूचना अधिकारियों (PIO) पर दंड लगाया जाए, ताकि RTI प्रवर्तन को सशक्त किया जा सके। पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिये यह सुनिश्चित किया जाए कि सूचना आयोग RTI अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अंतर्गत समय पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
- RTI कार्यकर्त्ताओं का संरक्षण: व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, जिसमें गुमनाम शिकायतों और आपातकालीन सुरक्षा उपायों की व्यवस्था हो एवं RTI कार्यकर्त्ताओं पर हमलों के मामलों का निपटारा फास्ट-ट्रैक न्यायालयों द्वारा किया जाए।
- सरकार-सिविल सोसायटी साझेदारी के माध्यम से कार्यकर्त्ताओं की सुरक्षा हेतु ज़िला-स्तरीय हेल्पलाइन, सहायता केंद्र और विधिक सहायता कोष स्थापित किये जाएँ।
- स्वायत्तता की आंशिक बहाली: नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यकारी विवेक पर निर्भर रहने के बजाय संसदीय निगरानी शामिल होनी चाहिये और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा आवधिक समीक्षा स्वतंत्रता को सशक्त कर सकती है।
निष्कर्ष
अपने अधिनियमन के दो दशक बाद, RTI अधिनियम, 2005 को रिक्तियों, अत्यधिक विलंब, कमज़ोर स्वायत्तता और कार्यकर्त्ताओं को खतरों सहित प्रणालीगत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सूचना आयोगों को सशक्त करना, दंड लागू करना, प्रौद्योगिकी का एकीकरण और RTI कार्यकर्त्ताओं की सुरक्षा, कानून की पारदर्शिता, जवाबदेही एवं लोकतांत्रिक शासन उद्देश्यों को पुनर्स्थापित करने के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारतीय लोकतंत्र के लिये एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ, किंतु इसके क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इसके प्रदर्शन को बाधित करने वाली प्रमुख सीमाओं की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये और सुधारात्मक उपाय सुझाइये। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 क्या है?
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास उपलब्ध जानकारी तक पहुँचने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को प्रोत्साहन मिलता है।
2. सूचना आयोगियों पर सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 का प्रभाव कैसे पड़ा?
वर्ष 2019 के संशोधन ने केंद्रीय सरकार को आयोगियों की अवधि, वेतन और सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया, जिससे सूचना आयोगियों की स्वायत्तता कम हो गई।
3. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 का सूचना के अधिकार अधिनियम पर क्या प्रभाव पड़ा?
DPDP अधिनियम ने सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1) में संशोधन किया, जिससे सभी व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट मिल गई, जो सार्वजनिक अधिकारियों के कार्यों की पारदर्शिता को सीमित कर सकता है।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न
मेन्स
प्रश्न. "सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तीकरण के बारे में ही नहीं है, अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनःपरिभाषित करता है।" विवेचना कीजिये। (2018)