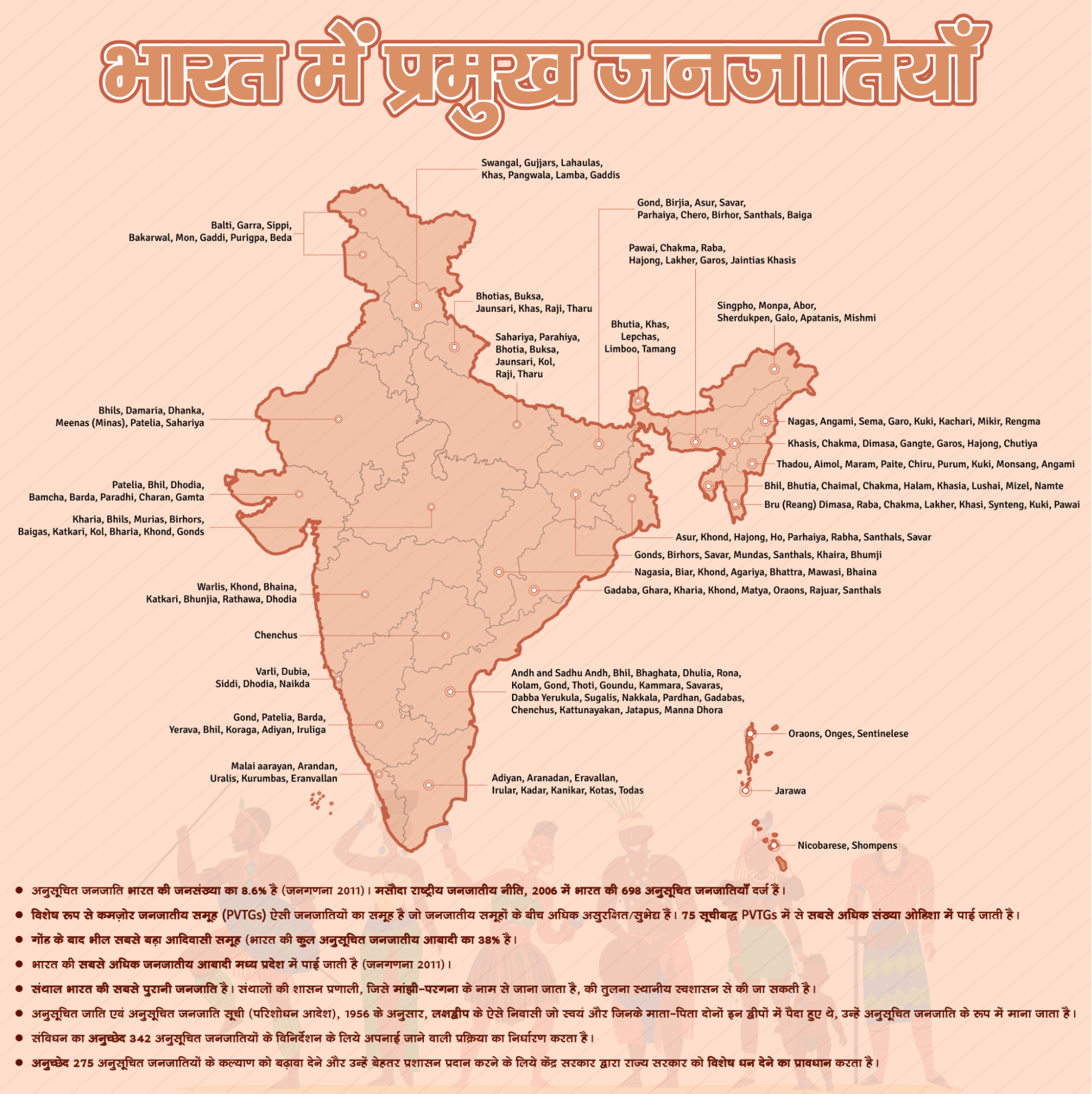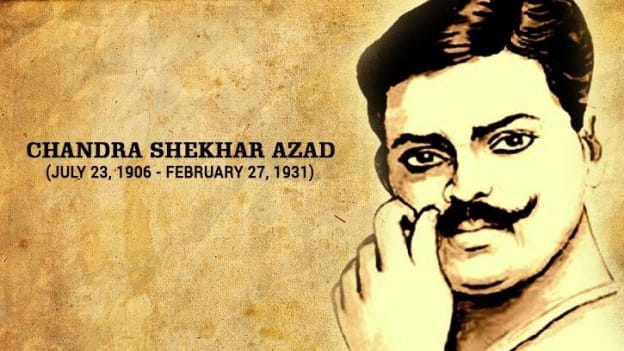मध्य प्रदेश Switch to English
पेसा अधिनियम
चर्चा में क्यों?
मध्य प्रदेश 88 जनजातीय ब्लॉकों में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) को प्रभावी ढंग से लागू करने वाला राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्य बनकर उभरा है, जिससे जनजातीय समुदायों को पारंपरिक चौपालों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विवादों को सुलझाने में सशक्त किया गया है।
- इस सशक्तीकरण पहल ने छोटे-मोटे विवादों के लिये पुलिस थानों पर निर्भरता को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है, जो राज्य की जनजातीय समुदाय के लिये एक वरदान साबित हुआ है।
मुख्य बिंदु
- सांसदों के प्रयासों को राष्ट्रीय मान्यता:
- पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक विशेष पुस्तिका में राज्य की सफलता की कहानियाँ उजागर की गई हैं, जिनमें मध्य प्रदेश की उपलब्धियाँ भी शामिल हैं तथा राष्ट्रीय मानक स्थापित करने में राज्य की भूमिका को मान्यता दी गई है।
- अधिनियम के अंतर्गत विवाद समाधान एवं वित्तीय सशक्तिकरण:
- पारिवारिक एवं भूमि संबंधी मामलों सहित 8,000 से अधिक विवादों का समाधान चौपाल नामक सामुदायिक बैठकों के माध्यम से किया गया है।
- यह अधिनियम न्याय के लिये सहयोगात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है और जनजातीय परंपराओं को बनाए रखते हुए समुदाय की समष्टिगत भलाई सुनिश्चित करता है।
- राज्य के प्रयासों में वित्तीय सशक्तीकरण भी शामिल है, जिसके अंतर्गत जनजातीय समुदायों के लिये सुचारू वित्तीय लेन-देन सुनिश्चित करने हेतु 11,000 से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं।
- अधिनियम के तहत स्थापित समितियाँ:
- PESA अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिये कई समितियाँ कार्यरत हैं, जैसे:
- शांति और विवाद निवारण समिति
- वन संसाधन योजना और नियंत्रण समिति
- सहयोग मातृ समिति (माता सहयोग समिति)
- ये समितियाँ राज्य में अधिनियम और इसके लक्ष्यों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- PESA अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिये कई समितियाँ कार्यरत हैं, जैसे:
पेसा अधिनियम, 1996
- पेसा अधिनियम को 24 दिसंबर, 1996 को उन जनजातीय क्षेत्रों, जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है, में रहने वाले लोगों के लिये पारंपरिक ग्रामसभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने हेतु अधिनियमित किया गया था।
- इस अधिनियम ने पाँचवीं अनुसूची वाले राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में स्व-जनजातीय शासन प्रदान करते हुए पंचायतों के प्रावधानों का विस्तार किया।
- विधान:
- अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्रों को अनुच्छेद 244(1) में उल्लिखित रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम को छोड़कर अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों पर लागू होती है।
- भारत के अनुसूचित क्षेत्र, वे क्षेत्र हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया है, जहाँ मुख्यतः जनजातीय समुदाय निवास करते हैं।
- 10 राज्यों ने पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत क्षेत्रों को अधिसूचित किया है, जो इन राज्यों के कई ज़िलों को (आंशिक या पूर्ण रूप से) कवर करते हैं।
- इनमें शामिल हैं:
- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना।
- महत्त्वपूर्ण प्रावधान:
|
प्रावधान |
विवरण |
|
सामुदायिक भागीदारी के मंच के रूप में कार्य करना तथा विकास योजनाओं की देखरेख करना। |
|
|
ग्राम स्तरीय संस्थाएँ |
स्थानीय सेवाओं के लिये ग्राम पंचायत, ग्रामसभा और पंचायत समिति की स्थापना करना। |
|
शक्तियाँ और कार्य |
संसाधनों का प्रबंधन करने और आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिये महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान करना। |
|
परामर्श |
अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं से पहले ग्रामसभा से परामर्श करना अनिवार्य है। |
|
फंड |
ग्राम पंचायत को धनराशि हस्तांतरण सुनिश्चित करना, ताकि प्रभावी कार्यप्रणाली बनी रहे। |
|
भूमि अधिकार |
जनजातीय भूमि अधिकारों की रक्षा; भूमि अधिग्रहण/हस्तांतरण के लिये सहमति आवश्यक। |
|
सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाएँ |
जनजातीय रीति-रिवाजों की रक्षा करता है और सांस्कृतिक प्रथाओं में हस्तक्षेप को रोकता है। |
मध्य प्रदेश Switch to English
चंद्रशेखर आज़ाद जयंती
चर्चा में क्यों?
प्रधानमंत्री ने चंद्रशेखर आज़ाद को उनकी जयंती (23 जुलाई, 2025) पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
- वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता और क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिये बहादुरीपूर्वक लड़ाई लड़ी।
मुख्य बिंदु
चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में:
- जन्म:
- चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई, 1906 को भाबरा (अब मध्य प्रदेश में) में हुआ था।
- स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका:
- वे जलियांवाला बाग हत्याकांड (1919) से अत्यंत प्रभावित हुए और छोटी उम्र में ही स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए।
- एक छात्र के रूप में वे असहयोग आंदोलन (1921) में शामिल हुए और वर्ष 1922 में गांधीजी द्वारा असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के प्रमुख सदस्य बन गए।
- HRA एक क्रांतिकारी संगठन था, जिसकी स्थापना वर्ष 1924 में कानपुर में सचींद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी द्वारा औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने हेतु की गई थी।
- इसके प्रमुख सदस्य थे- भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी।
- HRA को बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी (HSRA) के रूप में पुनर्गठित किया गया।
- इसकी स्थापना वर्ष 1928 में नई दिल्ली के फिरोज़शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, सुखदेव थापर और जोगेश चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी।
- क्रांतिकारी गतिविधियाँ:
- काकोरी ट्रेन एक्शन (1925)।
- लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने हेतु जे.पी. सॉन्डर्स की हत्या (1928)
- वर्ष 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास।
- विरासत:
- अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में 27 फरवरी, 1931 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार होने से बचने के लिये उन्होंने स्वयं को गोली मारकर बलिदान दे दिया।
राजस्थान Switch to English
खेजड़ी वृक्षों की कटाई
चर्चा में क्यों?
राजस्थान के थार रेगिस्तान, विशेषकर बीकानेर ज़िले में एक गंभीर पर्यावरणीय संघर्ष उभरकर सामने आया है, जहाँ सौर ऊर्जा कंपनियाँ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में सदियों पुराने खेजड़ी वृक्षों की कटाई कर रही हैं।
‘हरियाली’ (पर्यावरण संरक्षण) और ‘हरित ऊर्जा’ (सौर ऊर्जा विकास) के मध्य उत्पन्न इस संघर्ष ने स्थानीय किसानों एवं पर्यावरणविदों के व्यापक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है, जो कठोर वृक्ष संरक्षण कानूनों की माँग कर रहे हैं।
मुख्य बिंदु
खेजड़ी वृक्ष के बारे में:
- खेजड़ी या खेजरी (Prosopis cineraria), जिसे राजस्थान में शमी के नाम से भी जाना जाता है, एक कठोर, सूखा-प्रतिरोधी वृक्ष है, जो रेगिस्तानी पर्यावरण में अस्तित्व के प्रतीक के रूप में जाना जाता है।
- राजस्थान के पश्चिमी ज़िलों के खेतों में सैकड़ों वर्ष पुराने खेजड़ी वृक्ष आसानी से मिल जाते हैं।
- खेजड़ी के पत्ते, जिन्हें स्थानीय रूप से 'लूक' कहा जाता है, ऊँट, बकरी, भेड़ आदि जैसे पालतू पशुओं के लिये पौष्टिक आहार के रूप में उपयोग किये जाते हैं।
- इसके फल सांगरी को राजस्थानी भोजन में विशेष महत्त्व प्राप्त है।
मान्यता:
- खेजड़ी को वर्ष 1983 में आधिकारिक तौर पर राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था।
- इसके साथ ही राज्य सरकार ने इसकी सुरक्षा हेतु प्रतिबंध लगाए, जिनमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1965 तथा राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के तहत खेजड़ी वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध शामिल है।
सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्व:
- वर्ष 1730 ई. में, जोधपुर से लगभग 26 किमी दक्षिण-पूर्व में स्थित एक छोटा-सा गाँव भारत के प्रथम और तीव्र पर्यावरण संरक्षण आंदोलनों में से एक का केंद्र बना।
- इस आंदोलन के 'शहीद' (विशेष रूप से अमृता देवी) बिश्नोई समुदाय के सदस्य थे, जिन्होंने खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी।
- 1970 के दशक में यह बलिदान चिपको आंदोलन की प्रेरणा बना।
संरक्षण के लिये वैकल्पिक रणनीतियाँ:
- पर्यावरणविदों का तर्क है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन ऐसे विकल्पों के माध्यम से भी किया जा सकता है, जिनके लिये वृहद स्तर पर वनों की कटाई आवश्यक नहीं है।
- उदाहरणस्वरूप, सौर पैनलों की स्थापना छतों, सरकारी भवनों अथवा नहरों की सतह पर पर की जा सकती है (जैसे पंजाब में सफलतापूर्वक लागू परियोजनाएँ)।
- हालाँकि ये उपाय महँगे सिद्ध हो सकते हैं, किंतु ये इस क्षेत्र की जैवविविधता संरक्षण में सहायक सिद्ध होंगे।
राजस्थान Switch to English
राजस्थान शहरी गैस वितरण (CGD) नीति 2025
चर्चा में क्यों?
राजस्थान मंत्रिमंडल ने राजस्थान शहरी गैस वितरण (CGD) नीति 2025 को मंज़ूरी दे दी, जिसका उद्देश्य राज्य में गैस-आधारित ऊर्जा ढाँचे को सशक्त करना है।
- CGD नेटवर्क, पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) की आपूर्ति हेतु भूमिगत प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की एक परस्पर जुड़ी प्रणाली है।
मुख्य बिंदु
राजस्थान शहरी गैस वितरण (CGD) नीति 2025
- परिचय:
- इस नीति को जनता को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने हेतु डिज़ाइन किया गया है, साथ ही यह राज्य में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में भी सहायक होगी।
- नीति की समयावधि:
- यह नीति 31 मार्च, 2029 तक अथवा इसके स्थान पर कोई अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी।
- यह पाँच वर्ष की वैधता सरकार को मध्यावधि समीक्षा और आवश्यकता पड़ने पर सुधार हेतु रूपरेखा प्रदान करती है।
- एकल खिड़की प्रणाली:
- कार्यान्वयन तंत्र के एक भाग के रूप में एक समर्पित CGD पोर्टल विकसित किया जाएगा। यह डिजिटल मंच सभी आवेदनों के प्रबंधन, अनुमोदन की स्थिति पर निगरानी तथा हितधारकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु एकल-खिड़की प्रणाली के रूप में कार्य करेगा।
- इस पोर्टल से पारदर्शिता, जवाबदेही और परिचालन गति में सुधार होने, नौकरशाही संबंधी देरी समाप्त होने तथा अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- महत्त्व:
- अवसंरचना निवेश: इस नीति के कार्यान्वयन से CGD अवसंरचना में निवेश वृद्धि होगी, जिससे इस क्षेत्र में सतत् विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
- PNG और CNG नेटवर्क का विस्तार: यह नीति पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) तथा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) नेटवर्क के विस्तार में सहायक सिद्ध होगी, विशेष रूप से छोटे शहरों एवं शहरी क्षेत्रों में, जहाँ वर्तमान में इन सुविधाओं की सीमित पहुँच है।
- सरलीकृत विनियामक प्रक्रियाएँ: नीति में CGD कंपनियों हेतु सरलीकृत और समयबद्ध प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है, जिससे गैस अवसंरचना की स्थापना एवं संचालन के लिये आवश्यक अनुमतियाँ, भूमि आवंटन तथा सरकारी अनुमोदन की प्रक्रिया सुव्यवस्थित की जा सके।
- पर्यावरणीय एवं आर्थिक प्रभाव: यह नीति आवासीय, औद्योगिक एवं परिवहन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है।
- उद्देश्य:
- वर्तमान में वंचित क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की पहुँच बढ़ाकर इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता को प्रोत्साहित करना, जन स्वास्थ्य में सुधार करना तथा ऊर्जा अवसंरचना में आर्थिक निवेश को आकर्षित करना है।

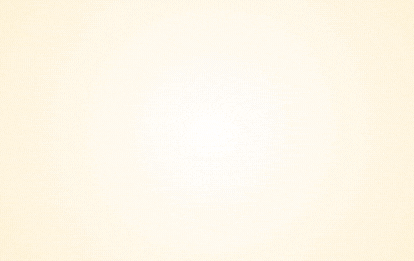



 PCS परीक्षण
PCS परीक्षण