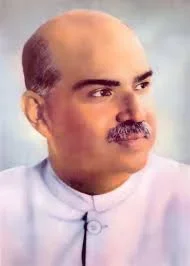मध्य प्रदेश Switch to English
नर्मदा नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ की स्थिति
चर्चा में क्यों?
मध्य प्रदेश में भारी वर्षा के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, जिससे कई ज़िलों, विशेष रूप से शहडोल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
- बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जबलपुर स्थित बरगी बाँध के गेट खोलने पड़े, जिससे आगे बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है।
मुख्य बिंदु
नर्मदा नदी के बारे में:
- नर्मदा मध्य भारत में पश्चिम दिशा में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, जो मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों से होकर प्रवाहित होती है।
- यह नदी 41 सहायक नदियों से पोषित होती है तथा ऐतिहासिक रूप से अरब सागर और गंगा घाटी के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक मार्ग के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है।
नदी का उद्गम और मार्ग:
- नर्मदा नदी का उद्गम पूर्वी मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की सीमा के निकट स्थित मैकल पर्वतमाला से होता है, जो समुद्र तल से लगभग 3,500 फीट (1,080 मीटर) की ऊँचाई पर स्थित है।
- यह नदी मंडला, जबलपुर तथा मार्बल रॉक्स गॉर्ज से होकर बहती हुई विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच स्थित भ्रंश घाटी में प्रवेश करती है।
- इसके पश्चात यह नदी गुजरात में प्रवेश करती है और 21 किमी (13 मील) चौड़े मुहाने से होकर खंभात की खाड़ी में गिरती है।
- नर्मदा सतपुड़ा पर्वतमाला की उत्तरी ढलानों से प्रवाहित होती है तथा जबलपुर के निकट स्थित धुआँधार जलप्रपात सहित विभिन्न भूभागों से होकर बहती है।
जल संसाधन विकास:
- नर्मदा नदी कई राज्यों में जलविद्युत उत्पादन, सिंचाई तथा पेयजल आपूर्ति के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- इस नदी पर निर्मित प्रमुख बाँधों में सरदार सरोवर बाँध (गुजरात), इंदिरा सागर बाँध (पुनासा, मध्य प्रदेश), ओंकारेश्वर बाँध, बरगी बाँध तथा महेश्वर बाँध शामिल हैं।
नर्मदा जल विवाद:
- 1960 के दशक से नर्मदा नदी के जल बँटवारे तथा बाँध निर्माण को लेकर कई राज्यों के बीच विवाद चला आ रहा है।
- वर्ष 1969 में इन विवादों के समाधान हेतु एक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। वर्ष 1980 में गठित नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (NCA), जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं, न्यायाधिकरण के निर्णयों को लागू करने का कार्य करता है।
नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA):
- सरदार सरोवर बाँध को बड़े पैमाने पर विस्थापन के कारण तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा।
- मेधा पाटकर और बाबा आमटे के नेतृत्व में NBA ने प्रभावित समुदायों के लिये उचित पुनर्वास की माँग की।
- उनके सतत् प्रयासों के चलते परियोजना में विलंब हुआ, वर्ष 1993 में विश्व बैंक ने इस परियोजना से अपना समर्थन वापस ले लिया तथा सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा।
- वर्ष 2000 में न्यायालय ने विस्थापित आबादी के पुनर्वास की शर्त पर बाँध निर्माण को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की अनुमति प्रदान की।
भारत में बाढ़ के कारण:
|
बाढ़ का कारण |
विवरण |
|
भारी एवं अनियमित वर्षा |
जून से सितंबर के बीच अत्यधिक मानसून वर्षा अक्सर मिट्टी की अवशोषण क्षमता को पार कर जाती है और जल निकासी तंत्र को बाधित कर देती है। |
|
ग्लेशियरों का पिघलना |
बढ़ते तापमान के कारण हिमालय में हिमनदों और हिमपात के पिघलने की गति तीव्र हो जाती है, जिससे नदियों में नीचे की ओर जलप्रवाह बढ़ जाता है। |
|
चक्रवात और तटीय तूफान |
भीषण चक्रवात भारी वर्षा, तूफानी लहरों और तेज़ हवाओं के साथ तटीय और आसपास के आंतरिक क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बनते हैं। |
|
नदी का अतिप्रवाह |
ऊपरी क्षेत्रों में वर्षा या निचले क्षेत्रों में जल निकासी क्षमता में कमी के कारण नदियाँ अपने किनारों से बाहर बहने लगती हैं। |
|
अनियोजित शहरीकरण |
शहरों और झुग्गी बस्तियों के अनियोजित विस्तार से प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली बाधित होती है, जिससे शहरी बाढ़ की आशंका बढ़ती है। |
|
बाँधों और बैराजों का खराब प्रबंधन |
भारी वर्षा के दौरान बाँधों से अनुचित ढंग से जल छोड़ने या आपातकालीन जल प्रवाह की कमी से निचले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। |
|
जलवायु परिवर्तन का प्रभाव |
ग्लोबल वार्मिंग के कारण अनियमित और अधिक तीव्र वर्षा हो रही है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। |
|
अपर्याप्त जल निकासी अवसंरचना |
खराब रखरखाव या अवरुद्ध नालियों के कारण, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, बारिश के समय गंभीर जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है। |
भारत में बाढ़ प्रबंधन के समाधान:
- नदी इंटरलिंकिंग (ILR) कार्यक्रम:
- ILR कार्यक्रम का उद्देश्य बाढ़-प्रवण नदियों से अतिरिक्त पानी को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करना है, ताकि पानी की उपलब्धता संतुलित हो सके।
- उदाहरण: केन-बेतवा लिंक परियोजना, एक प्रमुख पहल, बुंदेलखंड क्षेत्र में जल सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- जलाशय निर्माण:
- जलाशय भारी वर्षा के दौरान अतिरिक्त जल को संगृहीत करते हैं तथा नीचे की ओर बाढ़ की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिये इसे धीरे-धीरे छोड़ते हैं।
- उदाहरण: सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नांगल बाँध बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन और सिंचाई में मदद करता है।
- तटीय बाढ़ प्रबंधन:
- मैंग्रोव तूफानी लहरों और तटीय बाढ़ के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं, जैसा कि वर्ष 2004 की सुनामी के दौरान देखा गया था।
- केंद्रीय बजट 2023-24 में शुरू की गई MISHTI पहल भारत के तटों पर बड़े पैमाने पर मैंग्रोव वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है।
- बाढ़ पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणाली:
- ये प्रणालियाँ बाढ़ की भविष्यवाणी करने और समय पर चेतावनी जारी करने के लिये मौसम संबंधी और जल विज्ञान संबंधी आँकड़ों का उपयोग करती हैं।
- उदाहरण: केंद्रीय जल आयोग (CWC) देशभर में पूर्वानुमान केंद्रों का नेटवर्क संचालित करता है जो दैनिक बाढ़ बुलेटिन जारी करता है।
- बाढ़ क्षेत्र ज़ोनिंग:
- इसमें बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में भूमि उपयोग को विनियमित करना शामिल है, ताकि संवेदनशीलता को कम किया जा सके और आर्द्रभूमि जैसे प्राकृतिक बाढ़ अवशोषक को संरक्षित किया जा सके।
- उदाहरण: NDMA के बाढ़ क्षेत्र ज़ोनिंग दिशानिर्देश भूमि को चार जोखिम-आधारित क्षेत्रों में वर्गीकृत करते हैं- निषिद्ध, प्रतिबंधित, विनियमित और मुक्त।
- बाढ़ बीमा योजनाएँ:
- बाढ़ बीमा प्रीमियम के बदले में नुकसान की भरपाई प्रदान करता है, जिससे जोखिम न्यूनीकरण को प्रोत्साहन मिलता है।
- उदाहरण: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली फसल हानि को कवर करती है।
बारगी बाँध
परिचय:
- बारगी बाँध, जो जबलपुर में स्थित है, नर्मदा नदी पर बने 30 बाँधों में से एक प्रमुख बाँध है।
- यह जबलपुर शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ:
- बाँध के आधार पर दो बड़ी सिंचाई परियोजनाएँ- बरगी डायवर्ज़न प्रोजेक्ट और रानी अवंतीबाई लोढी सागर प्रोजेक्ट विकसित की गई हैं।
- इन परियोजनाओं ने क्षेत्र में कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया है और जल उपलब्धता में सुधार किया है।
उभरता हुआ पर्यटन स्थल:
- बरगी बाँध जबलपुर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है, जो अपने मनोरम दृश्यों और मनोरंजन की संभावनाओं के लिये पर्यटकों को आकर्षित करता है।
उत्तर प्रदेश Switch to English
उत्तर प्रदेश में नया ईवी पार्क
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश सरकार अपने कानपुर महानगर विकास विज़न 2030 के तहत 700 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पार्क की स्थापना करने जा रही है। 500 एकड़ में फैली इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) द्वारा किया जाएगा।
- नोट: UPSIDA उत्तर प्रदेश में औद्योगिक और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये ज़िम्मेदार प्रमुख सरकारी एजेंसी है।
मुख्य बिंदु
परियोजना के बारे में:
- उद्देश्य: प्रस्तावित ईवी पार्क स्थानीय आपूर्ति शृंखला को बढ़ावा देगा, 'Make in UP' तथा 'Made in UP' पहल के तहत स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगा तथा कानपुर को वैश्विक ईवी परिदृश्य में औद्योगिक नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।
- रणनीतिक स्थान: ईवी पार्क को कानपुर में भीमसेन के पास स्थापित किया जाएगा, जो समर्पित माल ढुलाई गलियारे (DFC) के साथ रणनीतिक रूप से स्थित है।
- यह स्थान प्रमुख रेल तथा सड़क नेटवर्क से जुड़ा होने के कारण लॉजिस्टिक दृष्टि से उपयुक्त है जिससे कच्चे माल तथा तैयार माल का निर्बाध परिवहन सुनिश्चित होता है।
- उत्तर प्रदेश के रक्षा और औद्योगिक गलियारों के साथ एकीकरण: कानपुर, जो पहले से ही उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में एक महत्त्वपूर्ण केंद्र है, अपने औद्योगिक आधार को मज़बूत करके इस पहल से लाभान्वित होगा।
- पार्क की विनिर्माण क्षमताएँ राज्य के बड़े आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करेंगी, जिनमें रक्षा विनिर्माण, नवाचार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना शामिल है।
- कानपुर, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे (UPDIC) के छह केंद्रों में से एक है। अन्य पाँच केंद्र लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट और झाँसी हैं।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल: ईवी पार्क को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र की दक्षता को सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के समर्थन के साथ जोड़ा जाएगा।
- उन्नत विनिर्माण अवसंरचना: पार्क में आवश्यक ईवी घटकों के लिये अत्याधुनिक विनिर्माण इकाइयाँ होंगी, जिनमें शामिल हैं:
- इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त विद्युत मोटर, लिथियम-आयन सेल और कोर इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियाँ।
- समर्पित अनुसंधान एवं विकास केंद्र: पार्क की एक मुख्य विशेषता ईवी प्रौद्योगिकियों में नवाचार पर केंद्रित एक समर्पित अनुसंधान एवं विकास (R&D) केंद्र होगा।
- इससे क्षेत्रीय स्तर पर तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में वैश्विक प्रगति में भी योगदान मिलेगा।
- एकीकृत ईवी घटक क्लस्टर: ईवी घटकों के विनिर्माण को समर्थन देने के लिये पार्क के भीतर एक एकीकृत क्लस्टर विकसित किया जाएगा।
- यह तंत्र लघु और मध्यम उद्यमों (SME), स्टार्टअप और स्थानीय उद्यमियों को सशक्त बनाएगा।
- इस पहल का उद्देश्य ईवी मूल्य शृंखला में स्थानीय भागीदारी को बढ़ाना और उद्यम-संचालित नवाचार को प्रोत्साहित करना है।
- रोजगार सृजन: इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में:
- परिचय: इलेक्ट्रिक वाहन ऐसे वाहन हैं जो पेट्रोल या डीजल से चलने वाले पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (ICE) के बजाय प्रणोदन के लिये एक या एक से अधिक इलेक्ट्रिक मोटरों का उपयोग करते हैं।
- यद्यपि इलेक्ट्रिक वाहनों की अवधारणा लंबे समय से चली आ रही है, ईंधन आधारित वाहनों के बढ़ते कार्बन उत्सर्जन और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों के कारण पिछले दशक में इसमें व्यापक रूप से रुचि बढ़ी है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रकार:
- बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEVs): ये प्रणोदन के लिये पूरी तरह बैटरी शक्ति पर निर्भर होते हैं तथा शून्य टेलपाइप उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं।
- प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (PHEV): इनमें इलेक्ट्रिक मोटर के साथ ही गैसोलीन इंजन मौजूद होता है। इन्हें बाह्य रूप से चार्ज किया जा सकता है और सीमित दूरी तक बैटरी पावर पर चलाया जा सकता है, जबकि लंबी यात्राओं के लिये गैसोलीन इंजन का उपयोग किया जा सकता है।
- हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (HEVs): इनमें इलेक्ट्रिक मोटर और गैसोलीन इंजन दोनों का उपयोग होता है, लेकिन बैटरी को सीधे प्लग-इन कर चार्ज नहीं किया जा सकता।
- बैटरी को गैसोलीन इंजन या पुनर्योजी ब्रेकिंग (regenerative braking) के माध्यम से चार्ज किया जाता है।
भारत में इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी नीतियाँ:
- वर्ष 2010: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा 95 करोड़ रुपए की योजना (जहाँ एक्स-फैक्ट्री कीमतों पर 20% तक के प्रोत्साहन की पेशकश की गई) के माध्यम से भारत ने EVs को प्रोत्साहन प्रदान किया। हालाँकि, मार्च 2012 में यह योजना वापस ले ली गई।
- वर्ष 2013: EVs के अंगीकरण को बढ़ावा देने, ऊर्जा सुरक्षा को संबोधित करने और वाहन प्रदूषण को कम करने के लिये ‘राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (NEMMP) 2020’' का शुभारंभ किया गया। हालाँकि इस योजना का व्यापक क्रियान्वयन नहीं हो सका।
- वर्ष 2015: स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकी कारों को प्रोत्साहित करने के लिये (वर्ष 2020 तक 7 मिलियन EVs के लक्ष्य के साथ) केंद्रीय बजट में 75 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ FAME योजना की घोषणा की गई।
- वर्ष 2017: भारतीय परिवहन मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक कारों का लक्ष्य निर्धारित किया है। उद्योग की चिंताओं के बाद 100% के लक्ष्य को घटाकर 30% कर दिया गया।
- वर्ष 2019: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्रिम खरीद प्रोत्साहन और चार्जिंग अवसंरचना के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण में तेज़ी लाने के लिये 10,000 करोड़ रुपए की FAME-II योजना को मंज़ूरी प्रदान की।
- वर्ष 2023: जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन बाज़ार को बढ़ावा देने के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% और चार्जर या चार्ज स्टेशनों पर 18% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया।
- वर्ष 2025: केंद्र ने घरेलू ईवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (SPMEPCI) के लिये विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये हैं।
छत्तीसगढ़ Switch to English
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती
चर्चा में क्यों?
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
मुख्य बिंदु
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी:
- प्रारंभिक जीवन और उपलब्धियाँ:
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई, 1901 को कलकत्ता में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
- 33 वर्ष की आयु में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने।
- उन्होंने प्रगतिशील सुधार लागू किये और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, भारतीय विज्ञान संस्थान (बंगलूरू) और अंतर-विश्वविद्यालय बोर्ड जैसी शैक्षिक संस्थाओं में सक्रिय योगदान दिया।
- उन्होंने वर्ष 1922 में बंगाली पत्रिका "बंग वाणी" और 1940 के दशकों में द नेशनलिस्ट की शुरुआत की।
- राजनीतिक करियर:
- वह कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए कॉन्ग्रेस उम्मीदवार के रूप में बंगाल विधान परिषद के लिये चुने गए।
- जब कॉन्ग्रेस पार्टी ने विधानमंडल का बहिष्कार करने का निर्णय लिया, तो उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया और बाद में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पुनः सीट जीत ली।
- कृषक प्रजा पार्टी-मुस्लिम लीग गठबंधन सरकार (1937-1941) के दौरान, उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया और मज़बूत राष्ट्रवादी चिंताओं को आवाज़ दी।
स्वतंत्रता के बाद:
- मंत्री की भूमिका:
- वह फज़लुल हक के नेतृत्व वाली प्रगतिशील गठबंधन सरकार में वित्त मंत्री के रूप में शामिल हुए, लेकिन वैचारिक और राजनीतिक मतभेदों के कारण उन्होंने एक वर्ष के भीतर ही इस्तीफा दे दिया।
- बाद में वे बंगाल की राजनीति में एक प्रमुख हिंदू आवाज़ के रूप में उभरे, हिंदू महासभा में शामिल हुए और वर्ष 1944 में इसके अध्यक्ष चुने गए, जो उनकी राजनीतिक यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव था।
- महात्मा गांधी की हत्या के बाद, डॉ. मुखर्जी ने हिंदू महासभा को धार्मिक सीमाओं से परे अपनी भूमिका का विस्तार करने और व्यापक राष्ट्रीय सेवा में संलग्न होने की वकालत की।
- उन्होंने संगठन के अराजनीतिक बने रहने के निर्णय का विरोध किया और परिणामस्वरूप 23 नवंबर, 1948 को हिंदू महासभा से इस्तीफा दे दिया।
- बंगाल विभाजन पर रुख:
- उन्होंने वर्ष 1946 में बंगाल विभाजन का समर्थन किया और बंगाली हिंदुओं की सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए भारत के भीतर एक अलग हिंदू बहुल राज्य, पश्चिम बंगाल बनाने की वकालत की।
- केंद्रीय शासन में भूमिका:
- वे पंडित नेहरू की अंतरिम कैबिनेट में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल हुए और स्वतंत्रता के बाद की प्रारंभिक औद्योगिक नीति में योगदान दिया।
- उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, लियाकत अली खान के साथ दिल्ली समझौते के विरोध में 6 अप्रैल 1950 को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया।
- भारतीय जनसंघ की स्थापना:
- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख गुरु गोलवलकर से परामर्श करने के बाद, उन्होंने 21 अक्तूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आज के समय में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नाम से जानी जाती है।
- वे इसके पहले अध्यक्ष बने। वर्ष 1952 में पार्टी ने तीन लोकसभा सीटें जीतीं, जिनमें उनकी अपनी सीट भी शामिल थी।
- संसद में नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया, हालाँकि इसे आधिकारिक मान्यता नहीं मिली।
- कश्मीर और अनुच्छेद 370 पर रुख:
- उन्होंने अनुच्छेद 370 का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह एक ऐसा कदम है जो भारत के विखंडन का कारण बन सकता है और राष्ट्रीय एकता के लिये खतरा बन सकता है।
- उन्होंने शेख अब्दुल्ला के तीन-राष्ट्र सिद्धांत की आलोचना की और अनुच्छेद 370 को हटाने की मांग के लिये हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के साथ मिलकर सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया।
- 11 मई, 1953 को, बिना परमिट के जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने का प्रयास करते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 23 जून, 1953 को विवादास्पद परिस्थितियों में हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई।
उत्तराखंड Switch to English
कैलाश मानसरोवर यात्रा
चर्चा में क्यों?
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने टनकपुर से पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिये तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
मुख्य बिंदु
- कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में:
- विदेश मंत्रालय (MEA) हर वर्ष जून से सितंबर के बीच इस यात्रा का आयोजन करता है।
- यह तीर्थयात्रा दो आधिकारिक मार्गों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा और सिक्किम में नाथू ला दर्रा से।
- भारत-चीन सीमा विवाद के कारण भारतीय तीर्थ यात्रियों को लगभग दो दशकों तक कैलाश तक पहुँचने से वंचित रखा गया था।
- वर्ष 1981 में विदेश मंत्रालय की निगरानी और चीनी सरकार के सहयोग से यात्रा पुनः शुरू हुई।
- धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व:
- भगवान शिव के निवास के रूप में स्थापित कैलाश पर्वत, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और तिब्बत की बोनपा परंपरा में पवित्र महत्त्व रखता है।
- हिंदू इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र मानते हैं, जैन मानते हैं कि ऋषभदेव ने यहीं निर्वाण प्राप्त किया था; बौद्ध इसे युंगड्रुक गु त्सेग (नौ मंजिला स्वस्तिक पर्वत) कहते हैं।
- भौगोलिक विशेषताएँ:
- कैलाश पर्वत (6,675 मीटर) पश्चिमी तिब्बत में स्थित है, जिसे स्थानीय रूप से कांग रामपोछे या बहुमूल्य रत्न के नाम से जाना जाता है।
- कैलाश के दक्षिण में राकसताल (रावण हृद), मानसरोवर और गुरला मंढाता शिखर (7,683 मीटर) स्थित हैं।
- मानसरोवर झील 4,530 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है, इसकी परिधि 90 किमी, गहराई 90 मीटर तथा क्षेत्रफल 320 वर्ग किमी है।
- राकसताल की परिधि 22 किमी है और यह गंगाछू नामक 6 किमी लंबी नहर के माध्यम से मानसरोवर से जुड़ा हुआ है।
- हिमालय के उत्थान के दौरान, कैलाश के पास चार महान नदियाँ उत्पन्न हुईं: सिंधु (उत्तर), करनाली (दक्षिण), यारलुंग त्संगपो (पूर्व), सतलुज (पश्चिम), जो राकसताल से निकलती हैं।
लिपुलेख दर्रा (उत्तराखंड):
- यह मानसरोवर (सीमा से 50 किमी) जाने का सबसे छोटा मार्ग है, लेकिन उबड़-खाबड़ रास्ते के कारण इसकी यात्रा 200 किमी तक लंबी हो जाती है।
- यह वर्ष 1992 में चीन के साथ व्यापार के लिये खोली गई पहली भारतीय सीमा चौकी थी, इसके बाद शिपकी ला (1994) और नाथू ला (2006) भी खोली गई।
नाथू ला दर्रा (सिक्किम):
- वर्ष 2015 में खोला गया यह 1,500 किमी लंबा पूर्णतः वाहन योग्य मार्ग, दुनिया की सबसे ऊँची वाहन योग्य सड़कों में से एक है तथा तीर्थयात्रियों को बिना चढ़ाई के यात्रा पूरी करने की सुविधा देता है।
- नाथू ला सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (TAR) से जोड़ता है और यह प्राचीन सिल्क रोड का हिस्सा है।
मध्य प्रदेश Switch to English
लाडली बहना योजना के तहत सहायता राशि बढ़ाई
चर्चा में क्यों?
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि दिवाली के बाद, लाडली बहना योजना की 1.27 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को 1,500 रुपए प्रति माह मिलना शुरू हो जाएगा, जो वर्तमान 1,250 रुपए से अधिक है।
मुख्य बिंदु
- लाडली बहना योजना के बारे में:
- इस योजना का शुभारंभ 10 जून 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया था।
- इसके तहत 23 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को शुरू में 1,000 रुपए की सहायता दी गई, जिसे बाद में बढ़ाकर 1,250 रुपए प्रति माह कर दिया गया।
- इसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
- महिलाओं के लिये विशेष बजट आवंटन:
- सरकार ने महिला-केंद्रित योजनाओं के लिये 27,147 करोड़ रुपए का समर्पित बजट निर्धारित किया है, जिसमें से 18,699 करोड़ रुपए लाडली बहना योजना के लिये आवंटित किये गए हैं।
अन्य महिला-केंद्रित योजनाएँ:
- लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में:
- वर्ष 2006 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करके उनका भविष्य सुरक्षित करना है।
- इसका उद्देश्य बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सामाजिक मानसिकता को बढ़ावा देना तथा लैंगिक भेदभाव को कम करना भी है।
- पात्रता मापदंड:
- इस योजना से उन माता-पिता को लाभ मिलता है जिन्होंने दो जीवित बच्चों के बाद परिवार नियोजन अपनाया है, जिससे जनसंख्या नियंत्रण सुनिश्चित होता है।
- इस योजना के लिये पात्र होने के लिये परिवारों को आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत होना चाहिये तथा आयकर दाता नहीं होना चाहिये।
- वित्तीय लाभ:
- राज्य सरकार लड़की के जन्म से लेकर उसके नाम पर प्रतिवर्ष 6,000 रुपए मूल्य के राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र खरीदती है, जब तक कि कुल राशि 30,000 रुपए तक नहीं पहुँच जाती।
- जब लड़की 21 वर्ष की हो जाती है और यदि उसकी शादी 18 वर्ष की आयु से पहले नहीं हुई है, तो उसे योजना के तहत अंतिम लाभ के रूप में 1 लाख रुपए की एकमुश्त राशि मिलती है।
- उषा किरण योजना के बारे में:
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2006 में शुरू की गई उषा किरण योजना घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा और कानूनी सहायता प्रदान करती है।
- यह घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 तथा वर्ष 2006 में अधिसूचित इसके नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करता है।
- मुख्य उद्देश्य:
- इस योजना का उद्देश्य पीड़ितों को शारीरिक, यौन, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार से बचाना है।
- इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं और बच्चों के लिये न्याय, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- लक्षित लाभार्थी:
- यह योजना वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिये बिना सभी आयु वर्ग की महिलाओं को सहायता प्रदान करती है।
- इसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं, जो घरेलू हिंसा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
हरियाणा Switch to English
गंगा यमुना लिंक (GYL) नहर
चर्चा में क्यों?
हरियाणा सरकार गंगा नदी से पानी प्राप्त करने के लिये गंगा यमुना लिंक (GYL) नहर के निर्माण पर विचार कर रही है।
मुख्य बिंदु
- प्रस्तावित नहर का उद्देश्य:
- जीवाईएल नहर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पेयजल और सिंचाई की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- हरियाणा सरकार का लक्ष्य, अनुमोदन और समन्वय के अधीन, नवंबर 2031 तक इस परियोजना को पूरा करना है।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा के दावे का समर्थन किये जाने के बावजूद पंजाब द्वारा सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर का निर्माण पूरा करने से लगातार इंकार करने के कारण राज्य को जल के नए विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं।
- उत्तर प्रदेश से प्रारंभिक समर्थन:
- प्रारंभिक चर्चाओं के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने अनौपचारिक रूप से प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की तथा हरियाणा तक जाने के लिये पाँच संभावित मार्ग सुझाए।
- प्रस्तावित चैनलों में खतौली, बदरुद्दीन नगर, मुरादनगर और यमुनानगर में हिंडन बैरियर के पास के स्थान शामिल हैं।
- समानांतर जल अवसंरचना परियोजनाएँ:
- जीवाईएल नहर के साथ-साथ, हरियाणा हथिनी कुंड बैराज के ऊपर की ओर एक बाँध का निर्माण करके वर्षा जल को एकत्र करने का भी काम कर रहा है।
- इसके अतिरिक्त, जल सुरक्षा को मज़बूत करने के व्यापक प्रयासों के तहत केशाऊ बाँध परियोजना पर कार्य प्रगति पर है।
गंगा नदी
- यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जो 2,510 किमी तक पहाड़ों, घाटियों और मैदानों में बहती है तथा हिंदुओं द्वारा पृथ्वी पर सबसे पवित्र नदी के रूप में मानी जाती है।
- गंगा बेसिन भारत, तिब्बत (चीन), नेपाल और बांग्लादेश में 10,86,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है।
- भारत में, यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली से होकर बहती है, जिसका कुल क्षेत्रफल 8,61,452 वर्ग किमी है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 26% है।
- इसका उद्गम हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है।
- अपने उद्गम पर इस नदी को भागीरथी कहा जाता है। यह देवप्रयाग से नीचे उतरती है, जहाँ एक अन्य धारा अलकनंदा से मिलने के बाद इसे गंगा कहा जाता है।
- दाहिनी ओर से नदी में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना और सोन हैं।
- रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा नदियाँ बायीं ओर से गंगा नदी में मिलती हैं। चंबल और बेतवा दो अन्य महत्त्वपूर्ण उप-सहायक नदियाँ हैं।
- गंगा नदी बेसिन दुनिया के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है और इसका क्षेत्रफल 1,000,000 वर्ग किमी है।
- गंगा नदी डॉल्फिन एक लुप्तप्राय जीव है, जो विशेष रूप से गंगा नदी में निवास करता है।
- गंगा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है और पद्मा या गंगा नाम से आगे बढ़ती है।
- गंगा नदी बांग्लादेश के सुंदरवन दलदल में गंगा डेल्टा के रूप में फैलती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
सतलुज नदी
- उत्पत्ति और प्रवाह-पथ:
- सतलुज नदी सिंधु नदी की पाँच सहायक नदियों में सबसे लंबी है, जो पंजाब क्षेत्र (जिसका अर्थ है "पाँच नदियों की भूमि") को उसका नाम देती है।
- इसका उद्गम दक्षिण-पश्चिमी तिब्बत में हिमालय की उत्तरी ढलान पर 15,000 फीट (4,600 मीटर) की ऊँचाई पर स्थित लांगा झील से होता है।
- यह नदी उत्तर-पश्चिम की ओर बहती है और फिर गहरी हिमालयी घाटियों से होकर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़कर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है।
- यह नदी नांगल के निकट पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है, दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ती है, ब्यास नदी से मिलती है, और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत-पाकिस्तान सीमा पर 65 मील (105 किमी) का विस्तार बनाती है।
- सिंचाई और उपयोग:
- भारत और पाकिस्तान दोनों में सिंचाई के लिये इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।
- प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में भाखड़ा-नांगल परियोजना, सरहिंद नहर और सतलुज घाटी परियोजना शामिल हैं।
- सिंधु जल संधि और जल बँटवारा:
- सतलुज नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल-बँटवारे को लेकर तनाव का स्रोत थी, जब तक कि वर्ष 1960 की सिंधु जल संधि ने इस मुद्दे को हल नहीं कर दिया।
- भारत ने सिंधु जल संधि को तब तक के लिये निलंबित कर दिया है जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता।
यमुना नदी
- उत्पत्ति और प्रवाह-पथ:
- उत्तर भारत की प्रमुख नदियों में से एक यमुना नदी उत्तराखंड में यमुनोत्री के निकट महान हिमालय में बंदरपूंछ पर्वत से निकलती है।
- यह नदी हिमालय की तराई से होकर दक्षिण की ओर बहती है और सिंधु-गंगा के मैदान में प्रवेश करती है तथा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाती है।
- यमुना कई ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण शहरों- दिल्ली, मथुरा, आगरा, फिरोज़ाबाद और इटावा से होकर बहती है।
- प्रयागराज में यह गंगा नदी के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है, जो एक पवित्र हिंदू संगम है।
- धार्मिक महत्त्व:
- यमुना को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है, जो गंगा के बाद दूसरे स्थान पर है।
- प्रयागराज में गंगा के साथ इसका संगम प्रमुख धार्मिक उत्सवों का स्थल है, जिसमें कुंभ मेला भी शामिल है, जिसमें हर 12 वर्ष में लाखों श्रद्धालु आते हैं।
- सहायक नदियाँ:
- इटावा के पास इस नदी में चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियों सहित महत्त्वपूर्ण दक्षिणी सहायक नदियाँ मिलती हैं, जो इसके प्रवाह और जलग्रहण क्षेत्र को समृद्ध करती हैं।
- प्रदूषण एवं संरक्षण प्रयास:
- यमुना नदी मुख्य रूप से अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक उत्सर्जन के कारण गंभीर प्रदूषण से ग्रस्त है।
- 1990 के दशक में, प्रदूषण को कम करने के लिये जापान द्वारा समर्थित यमुना एक्शन प्लान शुरू किया गया था। आंशिक रूप से सफल होने के बावजूद, जनसंख्या वृद्धि और खराब अपशिष्ट प्रबंधन के कारण चुनौतियाँ बनी हुई हैं।


%20(1).gif)
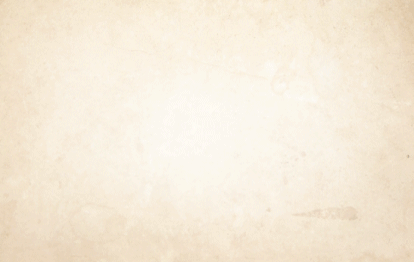

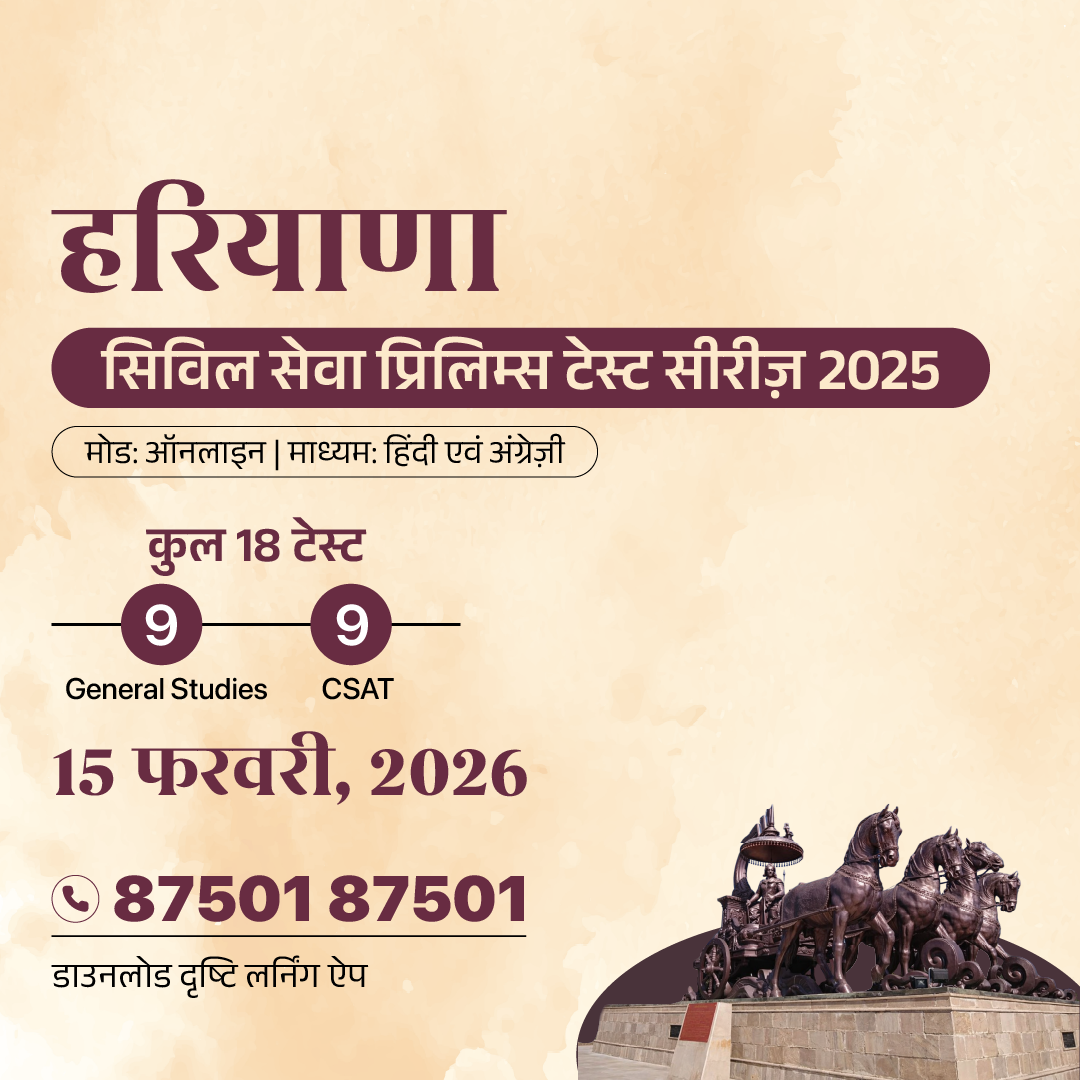
.jpg)
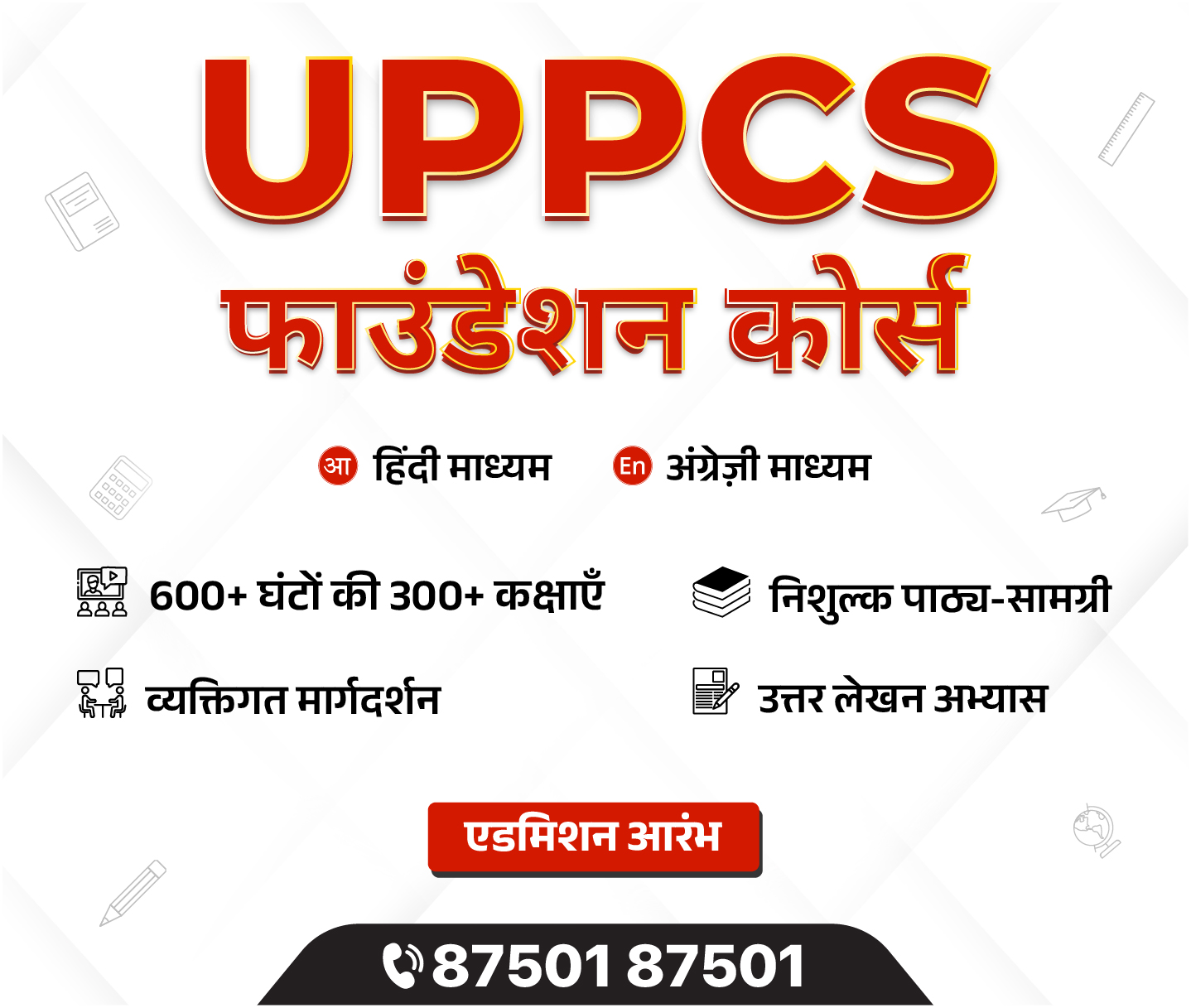
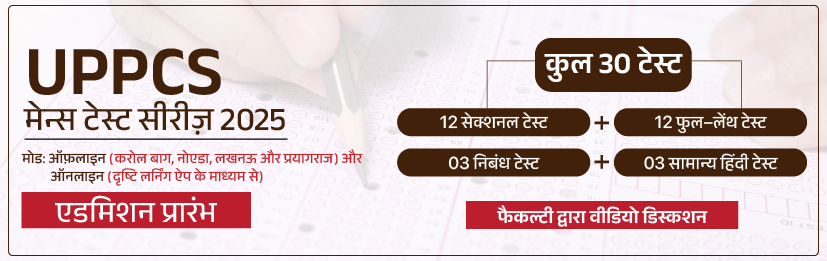
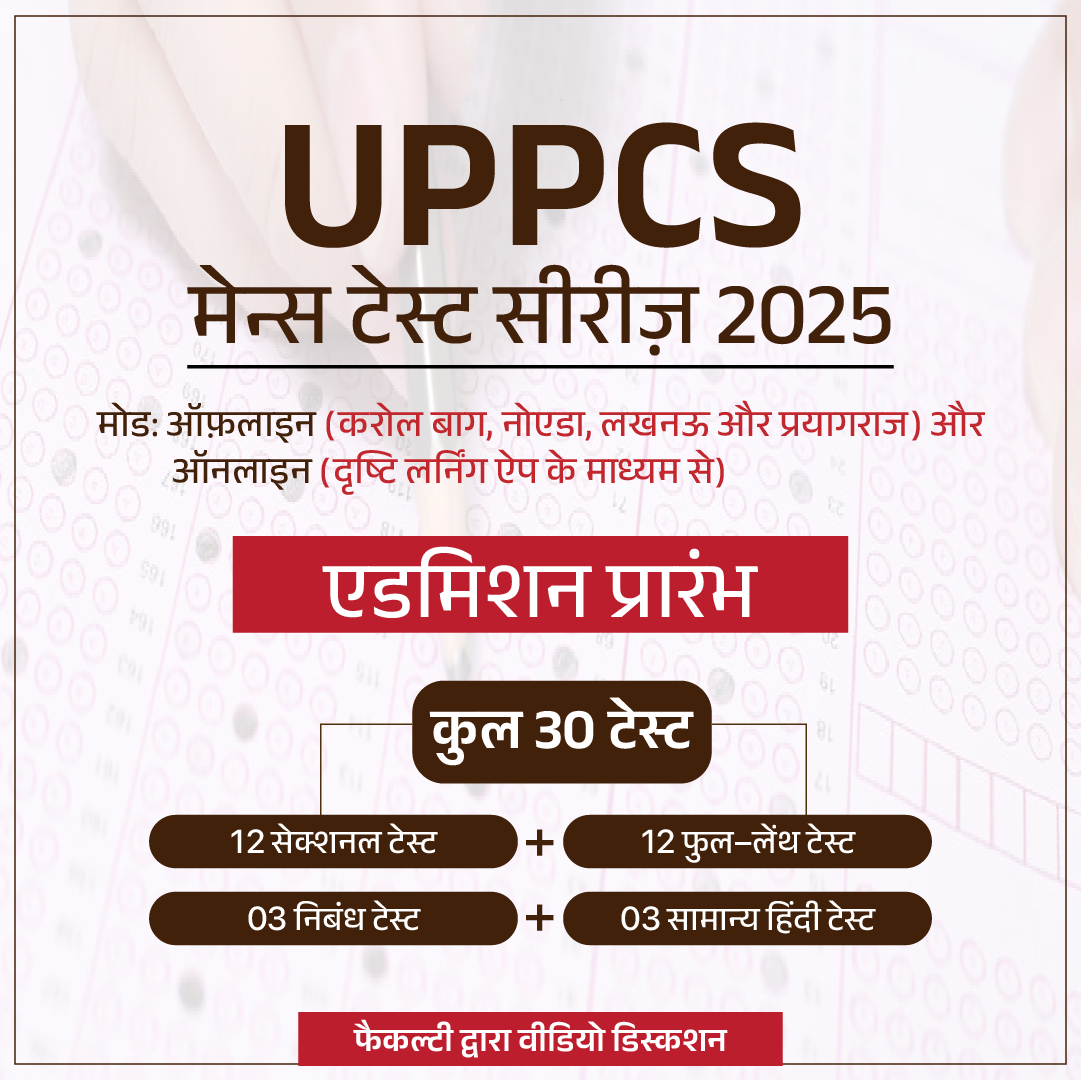

 PCS परीक्षण
PCS परीक्षण