उत्तराखंड Switch to English
विश्व अस्थमा दिवस 2025
चर्चा में क्यों?
अस्थमा की स्थिति तथा इससे उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य खतरों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष मई माह के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है।
मुख्य बिंदु
- विश्व अस्थमा दिवस 2025:
- वर्ष 2025 में यह दिवस मंगलवार, 6 मई को मनाया गया, जिसकी थीम है “श्वसन उपचार को सभी के लिये सुलभ बनाना।”
- इस थीम में रोग प्रबंधन एवं आपातकालीन देखभाल दोनों के लिये श्वास द्वारा दी जाने वाली दवाओं की व्यापक उपलब्धता पर ज़ोर दिया गया है।
- अस्थमा के बारे में:
- अस्थमा एक दीर्घकालिक श्वसन रोग है, जिसमें व्यक्ति के श्वसन नलिकाओं में सूजन और संकुचन हो जाता है, जिससे अधिक बलगम बनता है और साँस लेना कठिन हो जाता है।
- राष्ट्रीय हृदय, फेफड़े और रक्त संस्थान (NHLBI) अस्थमा को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित करता है, जो घरघराहट, साँस फूलना, सीने में जकड़न और खाँसी की बार-बार होने वाली समस्या का कारण बन सकती है।
- वैश्विक स्थिति:
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, दुनिया भर में 250 मिलियन से अधिक लोग अस्थमा से पीड़ित हैं।
- वर्ष 2019 में अस्थमा के कारण विश्व भर में लगभग 4,55,000 लोगों की मृत्यु हुई, जो बेहतर रोग नियंत्रण और उपचार सुविधाओं तक सुलभ पहुँच की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है।
- इतिहास और उत्पत्ति:
- अस्थमा के लिये वैश्विक पहल (GINA) ने वर्ष 1998 में बार्सिलोना, स्पेन में विश्व अस्थमा बैठक के दौरान 35 देशों की भागीदारी के साथ पहला विश्व अस्थमा दिवस मनाया था।
- तब से यह आयोजन वैश्विक स्तर पर फैल चुका है और आज इसे अस्थमा की शिक्षा और जागरूकता के सबसे महत्त्वपूर्ण दिवसों में से एक माना जाता है।
हरियाणा Switch to English
जल संसाधन एटलस 2025
चर्चा में क्यों?
हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण (HWRA) ने हरियाणा जल संसाधन एटलस 2025 लॉन्च किया है, जो एक AI-संचालित भू-स्थानिक मंच है और राज्य में तेज़ी से घटते जल भंडार की निगरानी, प्रबंधन और संरक्षण के लिये उपयोग किया जाता है।
मुख्य बिंदु
- एटलस की मुख्य विशेषताएँ:
- HWRA ने हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (HARSAC) के सहयोग से एटलस विकसित किया है।
- यह मंच सार्वजनिक रूप से सुलभ है और निम्नलिखित विषयों पर वास्तविक समय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है:
- भूजल स्तर और जलभृत
- सतही जल निकाय और नहर प्रणालियाँ
- पुनर्भरण क्षेत्र और जल-प्रधान फसल पैटर्न
- यह इंटरैक्टिव विषयगत मानचित्र और डैशबोर्ड प्रदान करता है।
- यह ज़िला और ब्लॉक स्तर पर जल संकट पर नज़र रखता है तथा अत्यधिक निकासी वाले क्षेत्रों और अनियमित वर्षा वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- पहल के पीछे की तात्कालिकता:
- आंतरिक आकलन से पता चलता है कि हरियाणा के 76 प्रतिशत से अधिक प्रशासनिक ब्लॉक भूजल उपयोग की दृष्टि से या तो “गंभीर” हैं या “अत्यधिक दोहन ” वाले हैं।
- इस मंच का उद्देश्य प्रशासनिक और ज़मीनी स्तर पर डाटा-संचालित हस्तक्षेप को मज़बूत बनाना है।
- डाटा स्कोप और अद्यतन चक्र:
- अधिकांश मुख्य डाटासेट (जैसे भूजल की गहराई और मृदा संरचना) को वार्षिक रूप से संशोधित नहीं किया जाएगा।
- ऐसे मापदंडों को आमतौर पर एक दशक में एक बार अपडेट करने की आवश्यकता होती है, जिससे डाटा नवीनीकरण के मामले में प्लेटफॉर्म का रखरखाव कम हो जाता है।
- एटलस में निम्नलिखित से डाटा एकीकृत किया गया है:
- उपग्रह अवलोकन और जी.पी.एस. सर्वेक्षण
- मौसम संबंधी जानकारी और कृषि रिकॉर्ड
- केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB), भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), सिंचाई विभाग और कृषि विभाग।
- राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियों ने सटीकता और परिचालन प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिये डाटा को मान्य किया है।
केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB)
- जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के तहत CGWB भारत में भूजल संसाधनों के प्रबंधन, अन्वेषण, निगरानी, मूल्याँकन और विनियमन के लिये सर्वोच्च निकाय है।
- वर्ष 1970 में स्थापित, CGWB का गठन आरंभ में अन्वेषणात्मक नलकूप संगठन का नाम बदलकर किया गया था और बाद में वर्ष 1972 में इसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूजल विंग के साथ विलय कर दिया गया।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत गठित केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) भूजल विकास को विनियमित करता है ताकि इसकी स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।
- प्रमुख कार्य और ज़िम्मेदारियाँ: CGWB भूजल प्रबंधन के लिये वैज्ञानिक विशेषज्ञता प्रदान करता है, जिसमें अन्वेषण, निगरानी और जल गुणवत्ता आकलन शामिल हैं।
- यह भूजल स्तर को बढ़ाने के लिये कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन की योजनाओं को भी क्रियान्वित करता है।
- वैज्ञानिक रिपोर्ट: CGWB राज्य और ज़िला जल-भूवैज्ञानिक रिपोर्ट, भूजल वर्ष पुस्तकें और एटलस जारी करता है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग क्या है?
- परिचय:
- IMD की स्थापना 1875 में हुई थी। यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान एवं संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है।
- यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- IMD विश्व मौसम विज्ञान संगठन के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है।
- उद्देश्य:
- कृषि, सिंचाई, नौवहन, विमानन, अपतटीय तेल अन्वेषण आदि जैसी मौसम-संवेदनशील गतिविधियों के इष्टतम संचालन के लिये मौसम संबंधी अवलोकन करना और वर्तमान एवं पूर्वानुमानित मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करना।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवात, नॉर्थवेस्टर, धूल भरी आँधी, भारी बारिश और बर्फ, ठंड तथा ग्रीष्म लहरें आदि जैसी गंभीर मौसम की घटनाओं, जो जीवन एवं संपत्ति के विनाश का कारण बनती हैं, के प्रति चेतावनी देना।
- कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, उद्योगों, तेल की खोज और अन्य राष्ट्र-निर्माण गतिविधियों के लिये आवश्यक मौसम संबंधी आँकड़े प्रदान करना।
- मौसम विज्ञान और संबद्ध विषयों में अनुसंधान का संचालन एवं प्रचार करना।
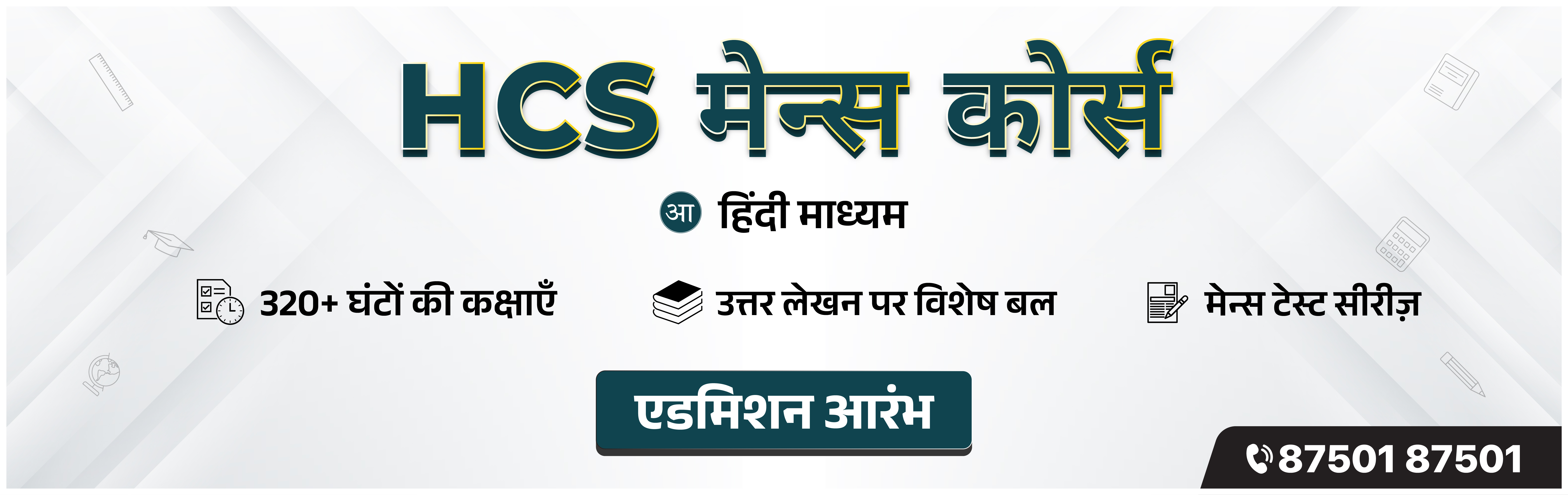

झारखंड Switch to English
भारत का पहला AI-आधारित डाटा पार्क
चर्चा में क्यों?
4 मई, 2025 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडेड डाटा सेंटर पार्क का उद्घाटन किया।
मुख्य बिंदु
- पहल के बारे में:
- भारत में अपनी तरह की इस पहल को 1,000 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित किया जा रहा है, जिसका उपयोग दो वर्षों में किया जाएगा।
- 13.5 एकड़ के इस पार्क में 2.7 हेक्टेयर का विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) शामिल है, जो विशेष रूप से एआई-आधारित सेवाओं के लिये समर्पित है।
- जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना:
- एआई डाटा सेंटर पार्क को छत्तीसगढ़ में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में देखा गया है।
- इसका उद्देश्य कृषि और शिक्षा में एआई-संचालित उन्नत समाधान प्रदान करना है, जिससे छात्रों, किसानों और ग्रामीण आबादी को सीधे लाभ पहुँचे।
- कार्यनीतिक दृष्टि:
- यह छत्तीसगढ़ द्वारा डिजिटल शासन और सार्वजनिक सेवा में रूपांतरण की दिशा में उठाया गया एक का पत्थर सिद्ध होगा।
- सरकार राज्य में सेवा वितरण, संसाधन प्रबंधन और आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने के लिये एआई का उपयोग करने की योजना बना रही है।
- स्कूलों में डाटा एआई क्लबों का निर्माण और शैक्षिक साझेदारी जैसी पूरक पहलों का उद्देश्य डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढाँचें को मज़बूत करना है।
विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है?
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें आर्थिक कानून मौजूद हैं जो देश के घरेलू आर्थिक कानूनों की तुलना में अधिक उदार हैं।
- मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTZ)
- निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ)
- मुक्त क्षेत्र (FZ)
- औद्योगिक संपदा (IE)
- श्रेणी 'SEZ' में अधिक विशिष्ट प्रकारों की एक विस्तृत शृंखला शामिल है, जिनमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं, लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:
- भारत एशिया में निर्यात को बढ़ावा देने में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र मॉडल की प्रभावशीलता को पहचानने वाले पहले देशों में से एक था, एशिया का पहला EPZ वर्ष 1965 में कांडला, गुजरात में स्थापित किया गया था।
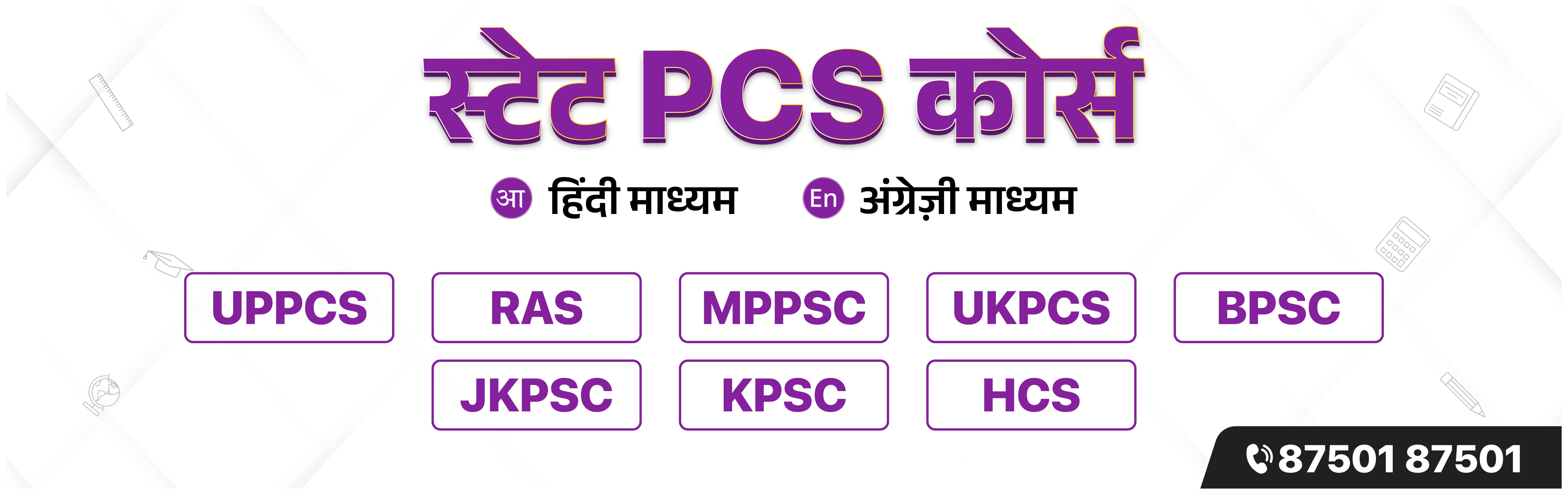
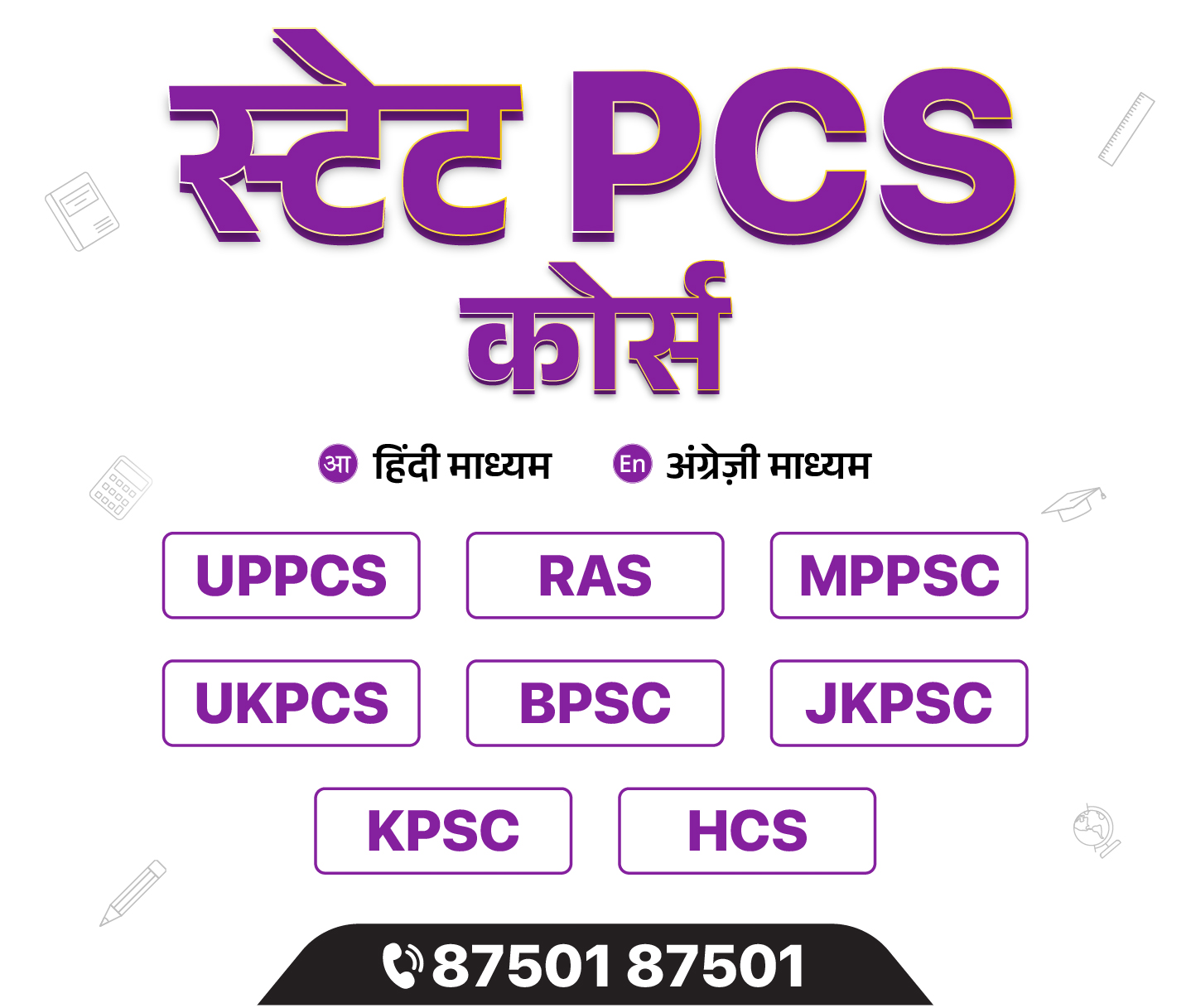
उत्तर प्रदेश Switch to English
उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश के तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आर्यावर्त बैंक, प्रथमा बैंक और बड़ौदा यूपी बैंक का विलय कर दिया गया है। जिसे 'उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक' के नाम से जाना जाएगा।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के बारे में:
- इस बैंक का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन, एकीकृत प्रबंधन और बेहतर ग्राहक सेवाएँ सुनिश्चित करना है।
- यह नया बैंक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के तहत 1 मई 2025 से अस्तित्व में आया।
- इस नवगठित बैंक का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश के 26 ज़िलों तक फैला होगा, जिसमें कुल 22 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संचालन किया जाएगा।
- इस नवगठित बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थापित किया जाएगा और इसका संचालन बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रायोजन में किया जाएगा।
- लाभ
- ऋण वितरण में सुगमता: किसानों, स्वरोज़गार से जुड़े ग्रामीण उद्यमियों को शीघ्र ऋण स्वीकृति।
- डिजिटल सेवाओं का विस्तार: मोबाइल बैंकिंग, UPI, नेट बैंकिंग जैसी सुविधाएँ दूरस्थ गाँवों तक पहुँचेंगी।
- सुविधाओं की निगरानी: नाबार्ड द्वारा एक विशेष समिति गठित की गई है, जो ग्राहकों की सुविधा का आकलन करेगी।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)
- नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिये शीर्ष बैंकिंग संस्थान है।
- इसका मुख्यालय देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में अवस्थित है।
- कृषि के अतिरिक्त यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिये उत्तरदायी है।
- यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के तहत की गई थी।

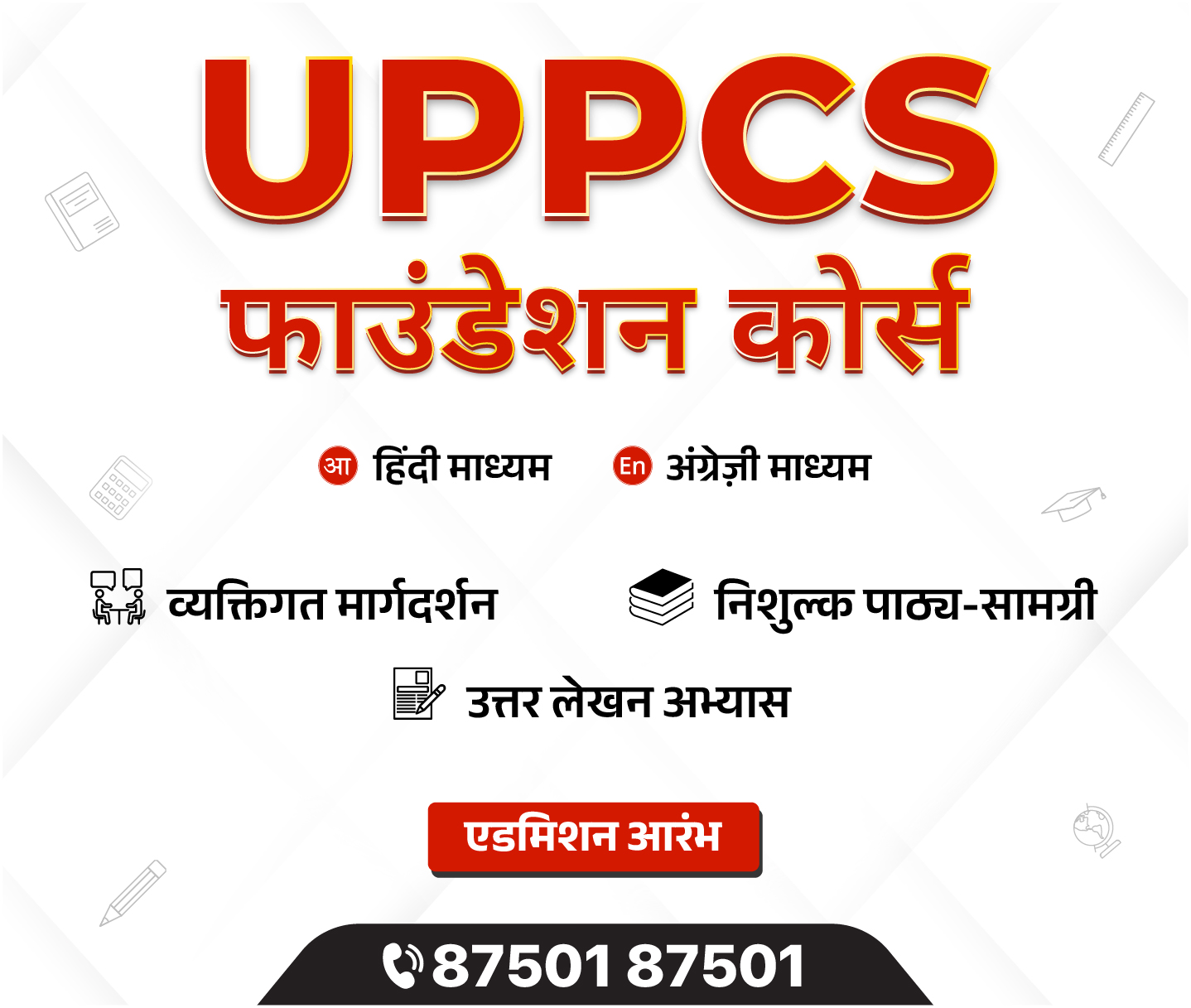
उत्तर प्रदेश Switch to English
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिये विशेष राशन कार्ड
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर नागरिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन कार्ड जारी करने के लिये एक विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की है।
मुख्य बिंदु
- ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति:
- यह कदम उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें समुदाय की उपेक्षा और सरकारी सुविधाओं से वंचित रहने की स्थिति उजागर की गई थी।
- रिपोर्ट के माध्यम से शासन को अवगत कराया गया कि बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर व्यक्ति स्थायी रोज़गार और सरकारी योजनाओं से वंचित हैं।
- सामाजिक भेदभाव के कारण वे खाद्य सुरक्षा, पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं।
- मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप:
- उत्तर पदेश के मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए निर्देश दिये हैं कि:
- राशन कार्ड वितरण प्रक्रिया को सरल, तेज़ और पारदर्शी बनाया जाए।
- यह कार्य राज्य के 'शून्य गरीबी' कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व पूरा किया जाए।
- सभी ज़िलों को निर्देश दिये हैं कि वे राशन कार्ड न रखने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें दस्तावेज़ जारी करें।
- इन लाभार्थियों को ‘पात्र गृहस्थी’ श्रेणी में जोड़ कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत लाया जाए।
- उत्तर पदेश के मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए निर्देश दिये हैं कि:
- महत्त्व
- इससे सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिलेगा तथा ट्रांसजेंडर समुदाय को समान अधिकार और गरिमा मिलेगी।
- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होने से उनकी आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी।
- प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता से कल्याण योजनाओं की पहुँच अधिक प्रभावी होगी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013
- अधिसूचित: 10 सितंबर, 2013
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।
- कवरेज: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत और शहरी आबादी का 50 प्रतिशत।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के 67 प्रतिशत हिस्से को कवर करता है।
- पात्रता
- राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत आने वाले प्राथमिकता वाले घर।
- अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर किये गए घर।
- प्रावधान
- प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपए किलो, गेंहूँ 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो।
- हालाँकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत मौजूदा प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करना जारी रहेगा।
- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम-से-कम 6000 रुपए का मातृत्व लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधानहै।
- 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये भोजन।
- खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता।
- ज़िला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।
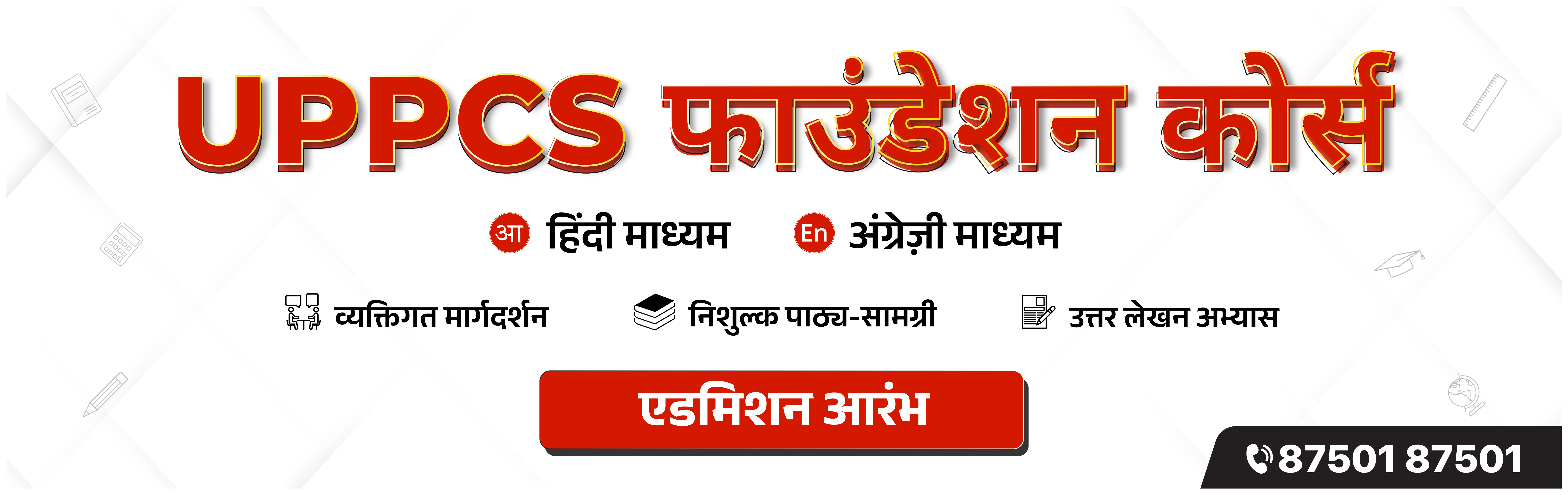
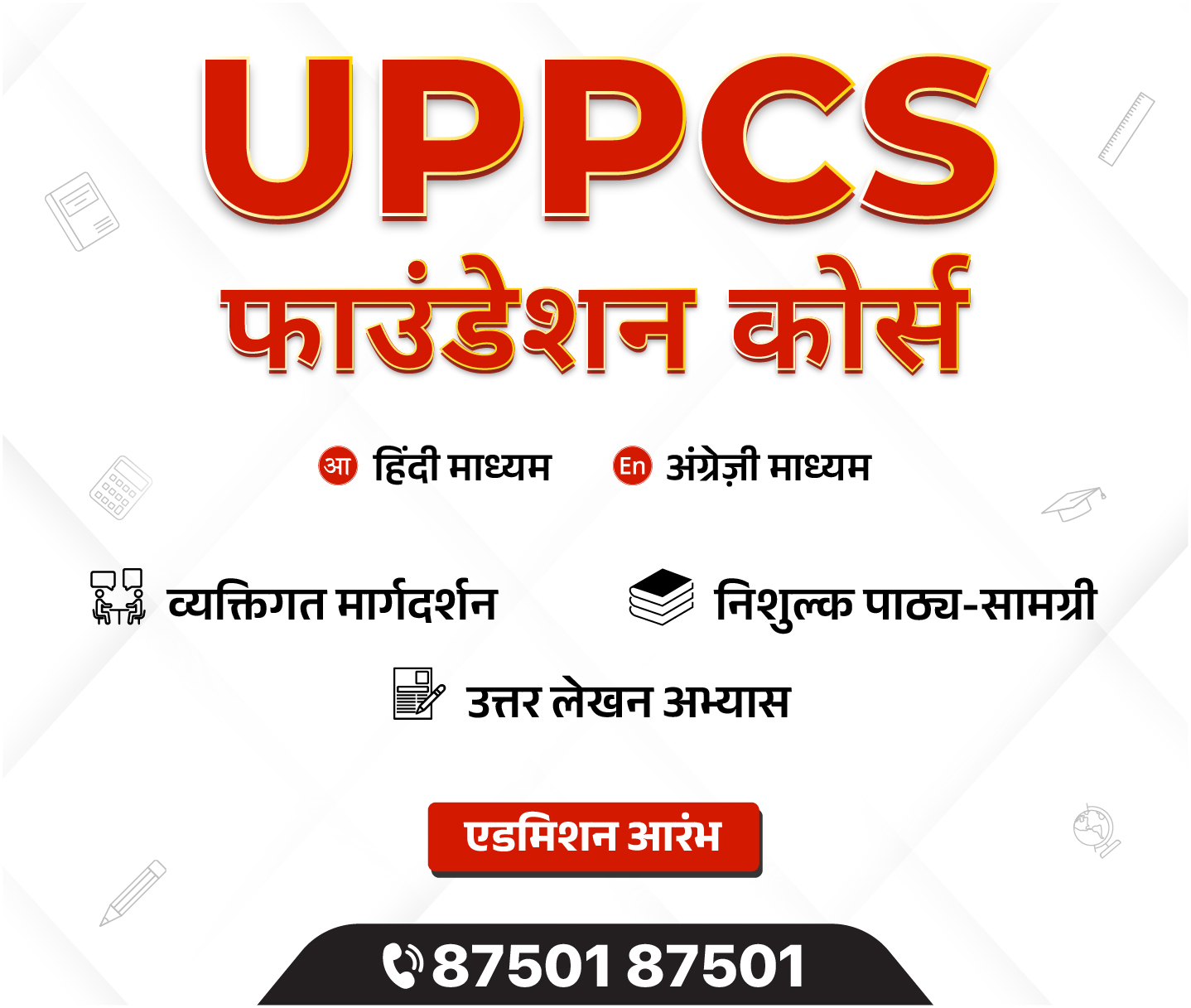
राजस्थान Switch to English
चीता संरक्षण गलियारा
चर्चा में क्यों?
राजस्थान ने मध्य प्रदेश के साथ भारत के पहले अंतर-राज्यीय चीता संरक्षण गलियारे में शामिल होने के लिये सहमति व्यक्त की।
मुख्य बिंदु
- संरक्षित क्षेत्र के बारे में:
- गलियारे का कुल क्षेत्रफल 17,000 वर्ग किमी है, जिसमें से 10,500 वर्ग किमी मध्य प्रदेश में तथा 6,500 वर्ग किमी राजस्थान में फैला है।
- इस गलियारे में मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले में स्थित कुनो राष्ट्रीय उद्यान मुख्य स्थल के रूप में शामिल है, जहाँ चीता पुनःस्थापित परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है।
- गांधी सागर अभयारण्य, जो मंदसौर ज़िले में चंबल नदी के किनारे स्थित है, चीतों के लिये मध्य प्रदेश में दूसरा आवास विकसित करने हेतु चयनित किया गया है।
- इस परियोजना में राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और चित्तौड़गढ़ जैसे ज़िले शामिल किये गए हैं।
- भविष्य में इस गलियारे में उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर के वन क्षेत्रों को भी शामिल किये जाने का प्रस्ताव है।
- संस्थागत सहयोग
- परियोजना को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) का तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त है।
- विशेषज्ञों ने इस परियोजना को एशिया में वन्यजीव संरक्षण का एक अनूठा मॉडल माना है, जो अन्य देशों के लिये उदाहरण बन सकता है।
- कॉरिडोर की विशेषताएँ
- यह गलियारा चीतों को संरक्षित क्षेत्रों के बीच स्वाभाविक और निर्बाध प्रवास की सुविधा प्रदान करेगा।
- यह दो राज्यों के बीच रणनीतिक वन्यजीव संपर्क स्थापित करता है, जो भारत में अपनी तरह की पहली पहल है।
- परियोजना का लक्ष्य चरागाह आधारित पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और संरक्षण है।
- गलियारे की संरचना इस प्रकार की जा रही है कि वह चीतों के अनुकूल, सुरक्षित और प्राकृतिक आवास को एकजुट कर सके।
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)
- परिचय:
- यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है।
- इसकी स्थापना वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की अनुशंसाओं के साथ की गई थी।
- बाघ संरक्षण के सशक्तीकरण के लिये वर्ष 2006 में संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के सक्षम प्रावधानों के तहत इसे गठित किया गया था।
- उद्देश्य:
- प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक अधिकार प्रदान करना ताकि इसके निर्देशों का कानूनी तौर पर अनुपालन हो।
- संघीय ढाँचे के भीतर राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन के लिये आधार प्रदान करके, टाइगर रिज़र्व के प्रबंधन में केंद्र-राज्य की जवाबदेही को बढ़ावा देना।
- संसद द्वारा निगरानी सुनिश्चित करना।
- टाइगर रिज़र्व के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की आजीविका संबंधी हितों को संबोधित करना।


मध्य प्रदेश Switch to English
देश का पहला स्ट्रैटोस्फेरिक एयरशिप
चर्चा में क्यों?
हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित परीक्षण स्थल से स्ट्रैटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया।
मुख्य बिंदु
- एयरशिप के बारे में:
- आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ADRDE) द्वारा विकसित यह एयरशिप प्लेटफॉर्म लगभग 17 किमी. की ऊँचाई पर स्ट्रैटोस्फियर में तैनात किया जा सकता है।
- यह लंबे समय तक एक ही स्थान पर स्थिर रह सकता है और रियल टाइम डाटा भेजने की क्षमता रखता है।
- स्ट्रेटोस्फियर पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जो ट्रॉपोस्फियर के ऊपर और मेसोस्फियर के नीचे स्थित होती है, इसकी ऊँचाई लगभग 10 से 50 किमी तक होती है।
- यह पृथ्वी पर मौसम के परिवर्तनों से अलग एक स्थिर वातावरण प्रदान करता है, जिससे उपग्रहों और अन्य उच्च-ऊँचाई वाले उपकरणों के लिये उपयुक्त क्षेत्र बनती है।
- संरचना:
- यह एयरशिप हल्की और अत्यधिक संवेदनशील तकनीकों से लैस है, जिससे इसे उच्च-ऊँचाई पर संचालन की क्षमता प्राप्त है।
- इसमें ISR (इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉन) कार्यों के लिये अत्याधुनिक पेलोड और सेंसर सिस्टम लगे हैं।
- मिशन के बाद सिस्टम को सुरक्षित रूप से रिकवर किया जा सकता है, जिससे लंबी अवधि तक संचालन संभव होता है।
- रणनीतिक उपयोग:
- यह एयरशिप रडार की पकड़ से बाहर रहकर सुरक्षा बलों की निगरानी क्षमता को मज़बूत करता है।
- कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश जैसे दुर्गम एवं संवेदनशील क्षेत्रों में सैन्य ऑपरेशनों के लिये यह प्लेटफॉर्म बेहद उपयोगी साबित हो सकता है।
- यह तकनीक पारंपरिक निगरानी प्रणालियों की तुलना में कहीं अधिक कुशल और स्थायी है।
- यह व्यापक क्षेत्र को कवर करते हुए दुश्मन की गतिविधियों की सटीक जानकारी दे सकता है।
ADRDE:
- यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की एक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है।
- यह पैराट्रूपर पैराशूट सिस्टम, एयरक्रू पैराशूट सिस्टम, गोला बारूद पैराशूट सिस्टम, ब्रेक पैराशूट, रिकवरी पैराशूट सिस्टम, एरियल डिलीवरी पैराशूट सिस्टम, हैवी ड्रॉप सिस्टम, इन्फ्लेटेबल सिस्टम, एयरशिप टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट अरेस्टर बैरियर सिस्टम के विकास में शामिल है।
- वर्तमान में यह आयुध वितरण पैराशूट, बैलून बैराज व निगरानी प्रणाली, हवाई पोत और संबंधित अनुप्रयोगों एवं अंतरिक्ष पैराशूट जैसी परियोजनाओं में शामिल है।
DRDO
- परिचय:
- DRDO रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान एवं विकास शाखा है जिसका उद्देश्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में सशक्त बनाना है।
- आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास तथा अग्नि और पृथ्वी मिसाइल शृंखला, हल्के लड़ाकू विमान तेजस, मल्टी बैरल रॉकेट लांचर, पिनाका, वायु रक्षा प्रणाली आकाश, रडारों की एक विस्तृत शृंखला और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आदि जैसी सामरिक प्रणालियों एवं प्लेटफॉर्मों के सफल स्वदेशी विकास एवं उत्पादन से भारत की सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई है।
- गठन:
- इसका गठन वर्ष 1958 में भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान (TDEs) और तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय (DTDP) तथा रक्षा विज्ञान संगठन (DSO) के एकीकरण से हुआ था।
- DRDO, 50 से अधिक प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है जो विभिन्न विषयों जैसे वैमानिकी, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग प्रणाली आदि को कवर करते हुए रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में गहनता के साथ संलग्न है।


उत्तर प्रदेश Switch to English
पुलित्ज़र पुरस्कार 2025
चर्चा में क्यों?
पुलित्ज़र पुरस्कार बोर्ड द्वारा पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करते पुलित्ज़र पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई।
मुख्य बिंदु
- पुलित्ज़र पुरस्कार के बारे में:
- पुलित्ज़र पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है।
- इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1917 में की गई थी, जिसे कोलंबिया विश्वविद्यालय और ‘पुलित्ज़र पुरस्कार बोर्ड’ द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- 'पुलित्ज़र पुरस्कार बोर्ड' का निर्माण कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों द्वारा होता है।
- यह पुरस्कार प्रसिद्ध समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्ज़र के सम्मान में दिया जाता है। जोसेफ पुलित्ज़र ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में पत्रकारिता स्कूल को शुरू करने तथा पुरस्कार की शुरुआत करने के लिये अपनी वसीयत से पैसा दिया था।
- पुरस्कार राशि:
- प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रमाण-पत्र और 15,000 डॉलर की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है तथा ‘सार्वजनिक सेवा श्रेणी’ में पुरस्कार विजेता को स्वर्ण पदक दिया जाता है।
- पुलित्ज़र पुरस्कार 2025
- वर्ष 2025 के पुलित्ज़र पुरस्कार कुल 23 श्रेणियों में दिये गए, जिसमें पत्रकारिता की 15 श्रेणियाँ और पुस्तक, नाटक, संगीत आदि की 8 श्रेणियाँ शामिल हैं।
- विजेताओं की सूची
- कथा साहित्य: पर्सीवल एवरेट को 'जेम्स' उपन्यास के लिये पुरस्कार मिला, जो 'हकलबेरी फिन' की कहानी को एक गुलाम की दृष्टि से प्रस्तुत करता है।
- नाटक: ब्रैंडन जैकब्स-जेनकिंस को 'पर्पस' के लिये सम्मानित किया गया, जो एक अमीर अश्वेत परिवार की आंतरिक जटिलताओं पर आधारित है।
- पत्रकारिता: न्यूयॉर्क टाइम्स को 4, न्यू यॉर्कर को 3 और ट्रंप की हत्या के प्रयास की त्वरित रिपोर्टिंग के लिये वाशिंगटन पोस्ट को पुलित्ज़र मिला।
- पब्लिक सर्विस: काविता सुर्णा, लिज़ी प्रेसर, कैसंड्रा जारामिलो और स्टेसी क्रैनिट्ज़ (रिपोर्टिंग पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु के कारण अस्पष्ट गर्भपात कानून अपवाद)।
- जाँचात्मक रिपोर्टिंग: रॉयटर्स स्टाफ (फेंटानाइल संकट पर आपूर्ति शृंखला का खुलासा)।
- स्पष्टीकरण रिपोर्टिंग: आज़म अहमद, क्रिस्टीना गोल्डबॉम और मैथ्यू ऐकिन्स (NYT)।
- स्थानीय रिपोर्टिंग: अलिसा झू, निक थीम और जेसिका गैलाघर (बाल्टिमोर फेंटानाइल संकट)।
- राष्ट्रीय रिपोर्टिंग: वॉल स्ट्रीट जर्नल स्टाफ (एलन मस्क पर रिपोर्टिंग)।
- अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग: डेक्लन वॉल्श और NYT स्टाफ (सूडान संघर्ष पर रिपोर्टिंग)।
- विशेष लेखन: मार्क वॉरेन (एस्क्वायर)।
- टिप्पणी: मोसाब अबू तोहा (द न्यू यॉर्कर)।
- समीक्षा: एलेक्जेंड्रा लैंग (ब्लूमबर्ग सिटीलेब)।
- संपादकीय लेखन: राज मांकड, शेरन स्टाइनमैन, लीसा फाल्केंबर्ग और लीहा बिनकोविट्ज़ (ह्यूस्टन क्रॉनिकल)।
- चित्रित रिपोर्टिंग और टिप्पणी: एन टेल्नेस (वाशिंगटन पोस्ट)।
- ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी: डग मिल्स (NYT)।
- विशेष फोटोग्राफी: मोइसेस समन (द न्यू यॉर्कर)।
- ऑडियो रिपोर्टिंग: द न्यू यॉर्कर स्टाफ।

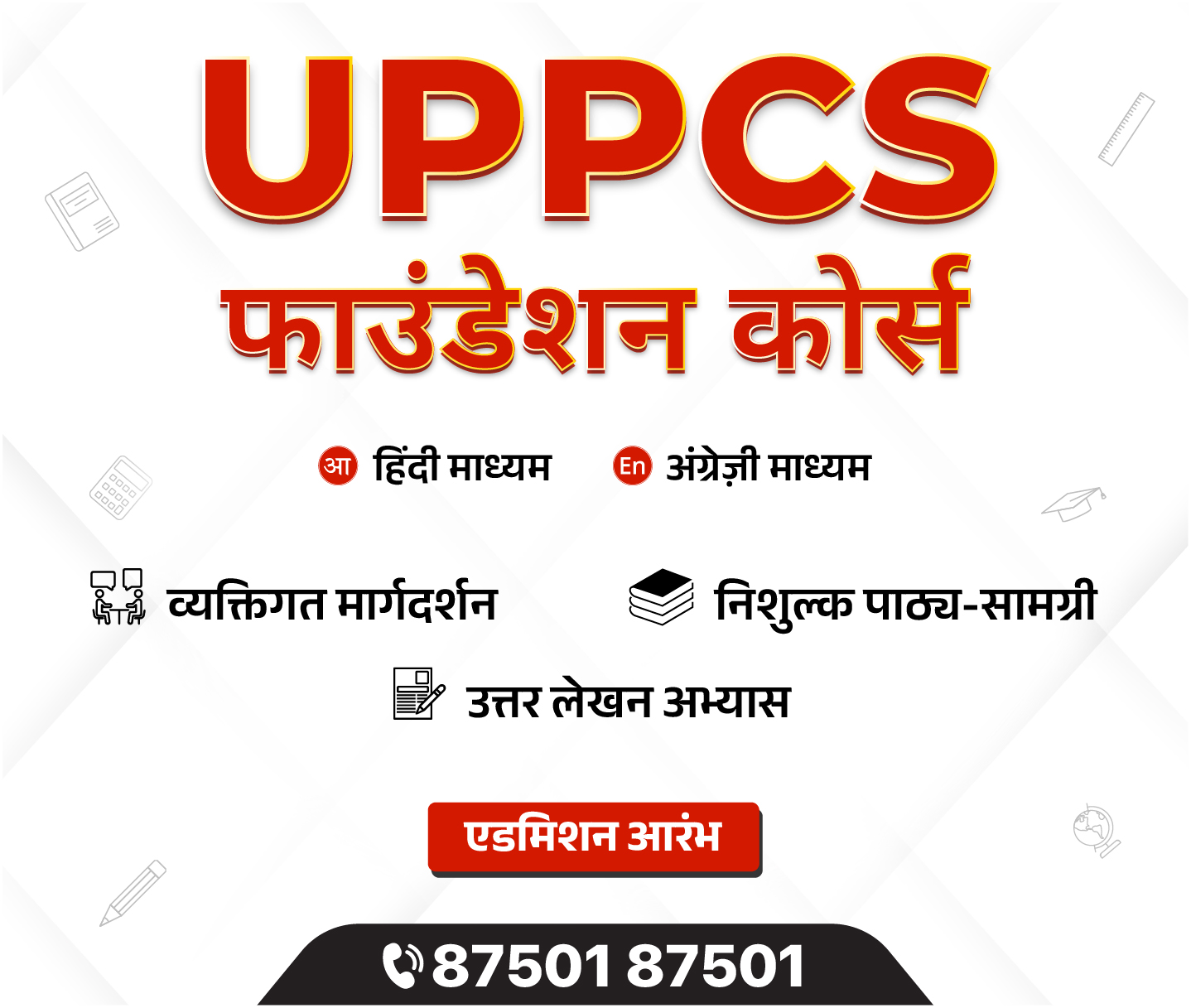

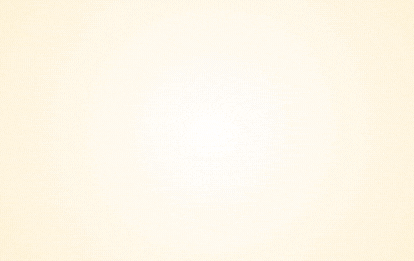



 PCS परीक्षण
PCS परीक्षण


