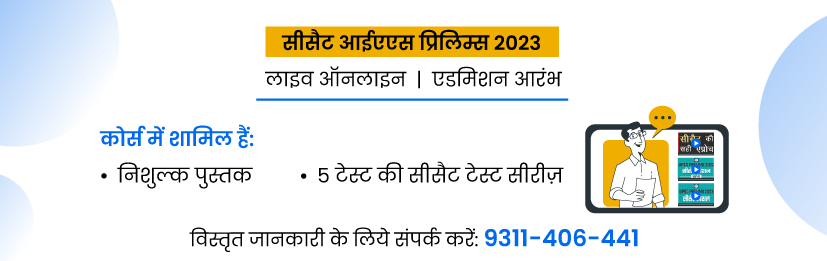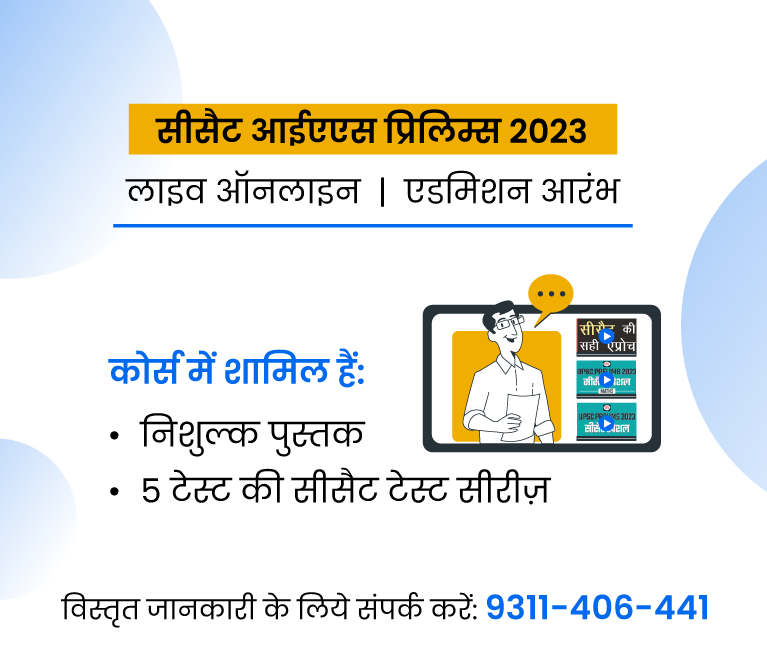जैव विविधता और पर्यावरण
भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023
प्रिलिम्स के लिये:CSE, DTE, वायु प्रदूषण, प्लास्टिक अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, लैंडफिल मेन्स के लिये:भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 |
चर्चा में क्यों?
विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (Centre for Science and Environment- CSE) तथा डाउन टू अर्थ (DTE) पत्रिका ने हाल ही में भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की, जिसमें जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं उद्योग के साथ-साथ जल, प्लास्टिक, वन एवं जैवविविधता सहित विभिन्न विषयों के आकलन की एक विस्तृत शृंखला शामिल है।
- रिपोर्ट का प्रकाशन वार्षिक तौर पर किया जाता है, जो जलवायु परिवर्तन, प्रवासन, स्वास्थ्य एवं खाद्य प्रणालियों पर केंद्रित है। इसमें जैवविविधता, वन एवं वन्य जीवन, ऊर्जा, उद्योग, आवास, प्रदूषण, अपशिष्ट, कृषि और ग्रामीण विकास भी शामिल हैं।
- CSE नई दिल्ली में स्थित एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक हित अनुसंधान संगठन (Advocacy) है।
रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:
- अतिक्रमण:
- देश में 30,000 से अधिक जल निकायों पर अतिक्रमण किया गया है और भारत प्रतिदिन 150,000 टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) उत्पन्न कर रहा है, जिनमें से आधे से अधिक या तो लैंडफिल में फेंक दिया जाता है या अनुपयुक्त पड़ा रहता है।
- वायु प्रदूषण:
- भारत में वायु प्रदूषण के कारण जीवन की औसत अवधि 4 वर्ष और 11 माह कम हो जाती है।
- वायु प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों के कारण शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण भारत में जीवन की औसत अवधि के अधिक वर्ष कम हो रहे हैं।
- ग्रामीण भारत को 35% अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकता है।
- पर्यावरणीय अपराध:
- पर्यावरणीय अपराध बेरोकटोक जारी हैं और लंबित मामलों को निपटाने के लिये न्यायालयों को प्रतिदिन 245 मामलों पर निर्णय देने की आवश्यकता है।
- चरम मौसमी घटनाएँ:
- जनवरी और अक्तूबर 2022 के बीच भारत ने 271 दिनों में चरम मौसमी घटनाओं को देखा।
- इन चरम मौसमी घटनाओं ने 2,900 से अधिक लोगों की जान ले ली।
- सतत् विकास लक्ष्य:
- पिछले पाँच वर्षों में संयुक्त राष्ट्र-अनिवार्य सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals- SDG) को प्राप्त करने में भारत की वर्ष 2022 की वैश्विक रैंकिंग में नौ स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है, जो अब 121वें स्थान पर है।
- भारत चार दक्षिण एशियाई देशों बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और नेपाल से नीचे है।
- भारत सतत् विकास लक्ष्य- 2 (भुखमरी से मुक्ति), सतत् विकास लक्ष्य- 3 (लोगों हेतु स्वास्थ्य और आरोग्यता), सतत् विकास लक्ष्य- 5 (लैंगिक समानता) एवं सतत् विकास लक्ष्य- 11 (संवहनीय शहरी तथा सामुदायिक विकास) सहित 17 सतत् विकास लक्ष्य में से 11 में चुनौतियों का सामना कर रहा है।
- प्लास्टिक अपशिष्ट:
- भले ही प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या का पैमाना अभी भी बहुत बड़ा है, फिर भी कई नीतियाँ और तात्कालिकता सही दिशा में हैं।
- शहर प्लास्टिक के उपयोग को कम कर रहे हैं, स्रोत पर अपशिष्ट को अलग करना और आय का साधन बनाने हेतु अपशिष्ट का पुन: उपयोग एवं पुनर्चक्रण करना सीख रहे हैं।
- कृषि:
- कृषि क्षेत्र में पारंपरिक और पुनर्योजी कृषि पद्धतियों की प्रभावशीलता के प्रमाण देखे जा सकते हैं।
- वनों और जैवविविधता के मुद्दे देखें तो वनों को हो रहा नुकसान एक सर्वविदित सत्य है, लेकिन साथ ही अधिक-से-अधिक समुदाय वनों पर अधिकार की मांग कर रहे हैं और इससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि उन्हें ये अधिकार दिये जा रहे हैं।
सिफारिशें:
- हमें एक सर्वसहमति-आधारित बुनियादी कार्यक्रम की आवश्यकता है जो सभी देशों को दो सबसे महत्त्वपूर्ण वैश्विक समस्याओं से निपटने हेतु एकजुट करता हो, वे समस्याएँ हैं- वर्तमान में हम जिस अस्तित्त्व संबंधी संकट का सामना कर रहे हैं उससे कैसे बचा जाए और एक न्यायसंगत तथा समावेशी विश्व व्यवस्था कैसे बनाई जाए।
- महामारी संधि इस दिशा में एक स्वागत योग्य कदम हो सकता है।
स्रोत: डाउन टू अर्थ
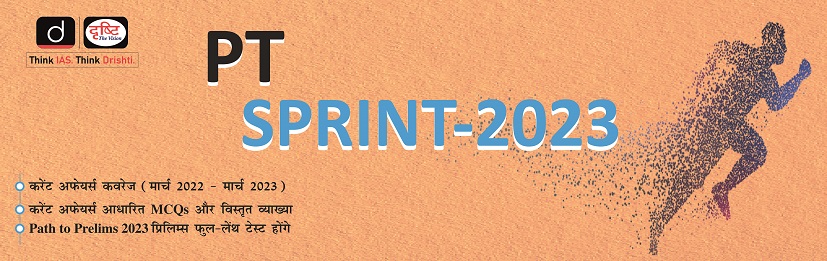

भारतीय अर्थव्यवस्था
IBC सुधार: आय का वितरण
प्रिलिम्स के लिये:गैर-निष्पादित संपत्तियाँ (NPA), लिक्विडेशन वैल्यू, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT), अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCITRAL)। मेन्स के लिये:दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), IBC के तहत लेनदारों के बीच वितरित आय। |
चर्चा में क्यों?
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code- IBC), 2016 में कई बदलावों का प्रस्ताव दिया है।
IBC में सुझाए गए बदलाव:
- मंत्रालय का मानना है कि कुछ लेनदार इस बात से चिंतित हैं कि जब किसी कंपनी के ऋणों का समाधान किया जाता है तो उन्हें धन का उचित हिस्सा नहीं प्राप्त होता है।
- इसे संबोधित करने हेतु यह लेनदारों के बीच धन को वितरित करने के लिये एक निष्पक्ष प्रणाली बनाने का सुझाव देता है।
- इसमें प्रत्येक लेनदार के दावे के आधार पर धन के वितरण हेतु एक विशिष्ट सूत्र का उपयोग करना शामिल है।
- परिसमापन मूल्य से अधिक कोई भी अधिशेष सभी लेनदारों के बीच उनके असंतुष्ट दावे के अनुपात में समानुपातिक होगा।
दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016:
- सरकार ने दिवाला और दिवालियापन से संबंधित सभी कानूनों को समेकित करने और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non-Performing Assets- NPA), जो वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये एक गंभीर समस्या रही है, से निपटने के लिये IBC, 2016 को लागू किया।
- दिवाला एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति या कंपनियाँ अपना बकाया कर्ज़ चुकाने में असमर्थ होती हैं।
- दूसरी ओर दिवालियापन एक ऐसी स्थिति है जिसमें सक्षम क्षेत्राधिकार की न्यायालय किसी व्यक्ति या अन्य संस्था को दिवालिया घोषित करती है और मामले को निपटाने एवं लेनदारों के अधिकारों की रक्षा करने हेतु उचित आदेश जारी करती है। यह एक कानूनी घोषणा है कि संबंधित व्यक्ति या संस्था ऋण चुकाने में असमर्थ है।
- IBC में सभी व्यक्ति, कंपनियाँ, सीमित देयता भागीदारी (Limited Liability Partnerships- LLP) और साझेदारी फर्म शामिल हैं।
- न्यायिक प्राधिकरण:
- कंपनियों और LLP हेतु राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal- NCLT)।
- व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों हेतु ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunal- DRT)।
- न्यायिक प्राधिकरण:
IBC के तहत लेनदारों के बीच आय के वितरण की विधि:
- एक कंपनी के विभिन्न लेनदार होते हैं जैसे- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी ऋणदाता, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, व्यापारिक लेनदार, विक्रेता, काम करने वाले, कर्मचारी, सरकारें आदि।
- यह सहिंता इन लेनदारों को ऋण की प्रकृति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में रखती है।
- बैंक, बॉण्ड जारीकर्त्ता और उधारदाताओं को वित्तीय लेनदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उधारकर्त्ता कंपनी द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा के आधार पर वित्तीय लेनदारों को आगे सुरक्षित एवं असुरक्षित लेनदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इस संहिता की धारा 53 प्राथमिकता के क्रम को निर्धारित करती है जिसमें परिसमापन मूल्य के आधार पर लेनदारों को आय वितरित की जाएगी।
- इस वॉटरफॉल तंत्र के अनुसार, सुरक्षित वित्तीय लेनदार प्राथमिकता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पर हैं। उनके बाद असुरक्षित वित्तीय लेनदार, सरकारी बकाया और अंत में परिचालन लेनदार का स्थान है।
- इस प्रकार जब तक सभी दावों का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक बैंक जैसे वित्तीय लेनदार प्राथमिक होते हैं। वॉटरफॉल तंत्र में वित्तीय लेनदारों के स्तर पर धन समाप्त हो सकता है, इससे अन्य लेनदारों के लिये लगभग कुछ भी नहीं बचता है।
आय वितरण के विषय में न्यायशास्त्र:
- सर्वोच्च न्यायालय ने एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड मामले में लेनदारों को भुगतान करने के तरीके से संबंधित एक मामले पर फैसला सुनाया।
- राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal- NCLAT) ने स्पष्ट किया था कि सभी लेनदारों को समान भुगतान किया जाना चाहिये, भले ही उनके पास प्रतिभूति हो अथवा न हो।
- हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने NCLAT से असहमति जताते हुए कहा कि सुरक्षित लेनदारों को पहले भुगतान किया जाना चाहिये क्योंकि उनके प्रतिभूति ब्याज को संरक्षित करने की आवश्यकता है।
- संहिता की धारा 30(4) के अनुसार, समाधान योजना को अधिकृत करते समय लेनदारों की समिति द्वारा प्रतिभूति ब्याज के मूल्य को ध्यान में रखा जा सकता है।
- दिवाला कानून पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (United Nations Commission on International Trade Law- UNCITRAL) के विधायी गाइड का कहना है कि सुरक्षित लेनदार अपनी सुरक्षा के मूल्य के आधार पर भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, जबकि असुरक्षित और कनिष्ठ (Junior) लेनदारों को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा हाल ही में समाचारों में आए 'दबावयुक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचन पद्धति (स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स/S4A)' का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? (a) यह सरकार द्वारा निरूपित विकासपरक योजनाओं की पारिस्थितिकीय कीमतों पर विचार करने की पद्धति है । उत्तर: (b) |
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
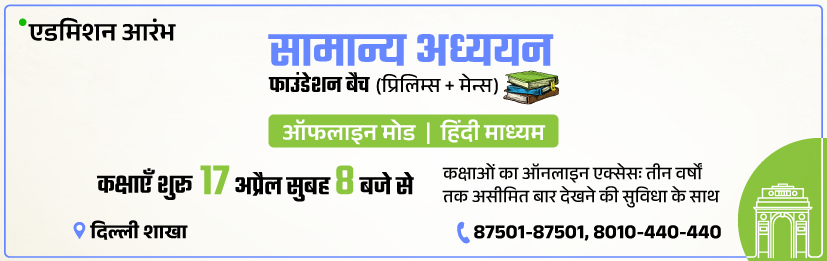
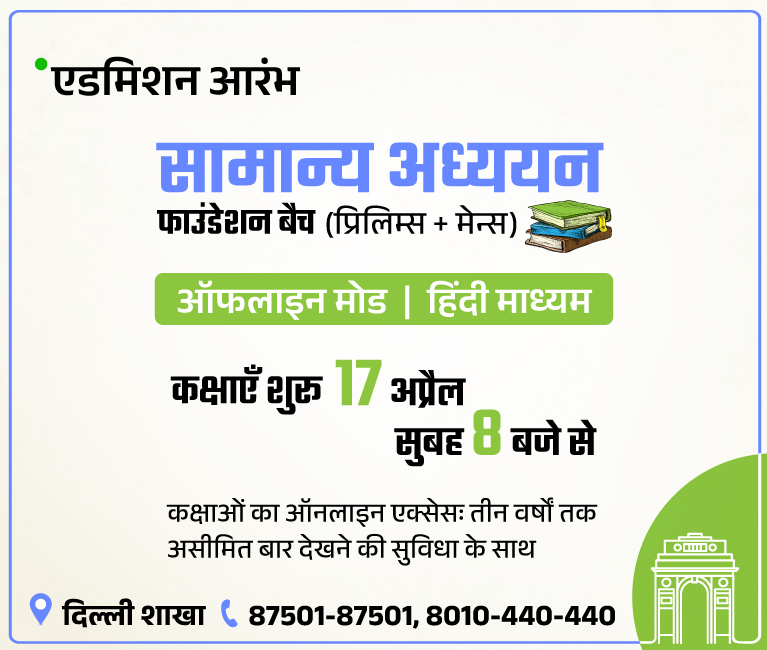
शासन व्यवस्था
विशिष्ट संस्थान योजना
प्रिलिम्स के लिये:यूजीसी, विश्व स्तरीय शिक्षण प्रणाली, उच्च शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और अनुसंधान। मेन्स के लिये:विशिष्ट संस्थान योजना। |
चर्चा में क्यों?
ऐसे कई संस्थान हैं, जिन्हें विशिष्ट संस्थान (Institution Of Eminence- IoE) स्टेटस हेतु चुने जाने के बाद भी तीन वर्ष से अधिक समय से IoE स्टेटस नहीं प्रदान किया गया है।
इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस योजना:
- परिचय:
- केंद्र सरकार ने देश में 20 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु IoE योजना शुरू की है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC) ने वर्ष 2017 में अनिवार्य किया कि IoE योजना अधिसूचना के पाँच वर्ष के भीतर मान्यता प्राप्त कर ले।
- भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को सशक्त बनाने और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक किफायती पहुँच बढ़ाने के लिये विश्व स्तरीय शिक्षण प्रणालियों को लागू करने में मदद के लिए 'विशिष्ट संस्थान' का दर्जा देना शुरू किया गया था।
- इसमें 20 संस्थानों (10 सार्वजनिक और 10 निजी संस्थानों) ने अनुदान प्राप्त किया, और चयनित संस्थानों में से ग्यारह को अप्रैल 2021 में प्रतिष्ठित संस्थानों का दर्जा प्राप्त हुआ।
- उद्देश्य:
- उत्कृष्टता और नवाचार: ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता और नवाचार के लिये उच्च शिक्षा प्रदान करना जिसे स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान डिग्री स्तरों पर उचित माना जा सकता है।
- विशेषज्ञता: विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों में विशिष्ट योगदान देने के लिये विशेषज्ञता के क्षेत्रों में शामिल होना।
- वैश्विक रेटिंग: समय के साथ विश्व के शीर्ष सौ संस्थानों को उनके शिक्षण एवं अनुसंधान के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेटिंग प्रदान करने का लक्ष्य है।
- गुणवत्ता शिक्षण एवं अनुसंधान: उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण एवं अनुसंधान के लिये तथा ज्ञान की उन्नति और इसके प्रसार के लिये प्रदान करना।
- मानदंड:
- वैश्विक/राष्ट्रीय रैंकिंग: केवल वे संस्थान जो किसी भी वैश्विक/राष्ट्रीय रैंक (जैसे, QS, NIRF) में दिखाई देते हैं, उन्हें विशिष्ट संस्थान योजना (IoE) स्थिति के लिये अनुशंसित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (National institutional Ranking Framework- NIRF) में शीर्ष 50।
- दुनिया भर में प्रकाशित प्रतिष्ठित रैंकिंग में शीर्ष 500, जैसे टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी लिस्ट, क्यूएस।
- ग्रीनफील्ड प्रस्ताव: उपरोक्त मानदंड को पूरा करने के बाद ही यदि कोई स्लॉट खाली रहता है, तो अब तक स्थापित (ग्रीनफील्ड) प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
- ग्रीनफील्ड परियोजना शब्द आमतौर पर बिना किसी पूर्व कार्य पर विचार किये किसी परियोजना की शुरुआत को संदर्भित करता है।
- ग्रीनफील्ड संस्थानों को स्थापना और संचालन के लिये 3 वर्ष का समय मिलेगा तथा उसके बाद EEC ऐसे संस्थानों को IoE का दर्जा देने पर विचार करेगा।
- वैश्विक/राष्ट्रीय रैंकिंग: केवल वे संस्थान जो किसी भी वैश्विक/राष्ट्रीय रैंक (जैसे, QS, NIRF) में दिखाई देते हैं, उन्हें विशिष्ट संस्थान योजना (IoE) स्थिति के लिये अनुशंसित किया जाएगा।
- लाभ:
- स्वायत्तता: IoE टैग वाले संस्थानों को फीस, पाठ्यक्रम अवधि और शासन संरचनाओं को तय करने के लिये अधिक स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी।
- अनुदान: IoE टैग के तहत सार्वजनिक संस्थानों को 1,000 करोड़ रुपए का सरकारी अनुदान मिलेगा, जबकि निजी संस्थानों को योजना के तहत कोई धन नहीं मिलेगा।
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
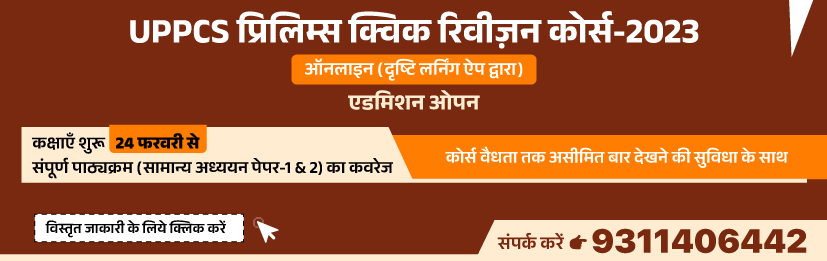
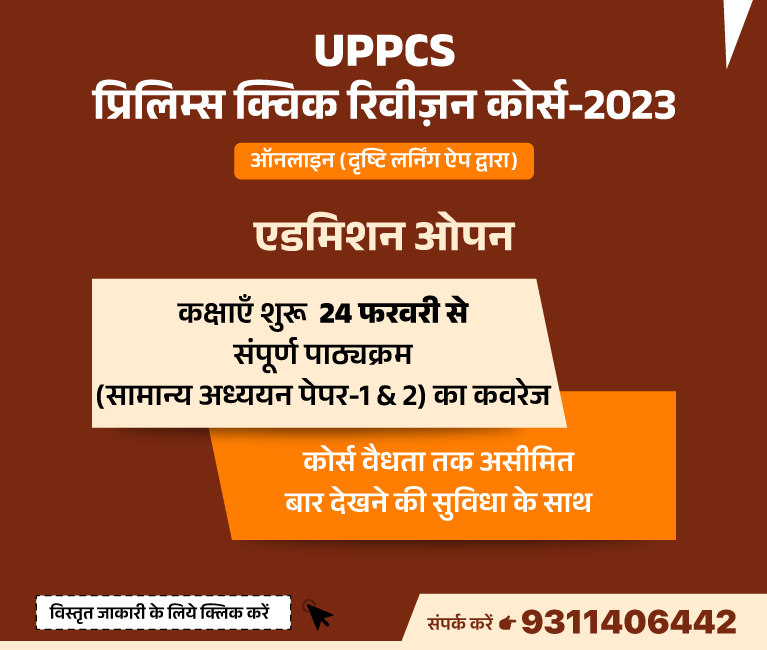
जैव विविधता और पर्यावरण
समुद्री संरक्षित क्षेत्र
प्रिलिम्स के लिये:समुद्री संरक्षित क्षेत्र, अंटार्कटिक, जलवायु परिवर्तन, क्रिल, समुद्री संसाधन, मत्स्यपालन। मेन्स के लिये:समुद्री संरक्षित क्षेत्र। |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार ने घोषणा की है कि भारत समुद्री जीवन और इसकी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की रक्षा के लिये अंटार्कटिक में दो समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (Marine Protected Areas- MPA) की स्थापना का समर्थन करेगा।
समुद्री संरक्षित क्षेत्र:
- परिचय:
- MPA समुद्री संसाधनों, पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं अथवा सांस्कृतिक विरासत के दीर्घकालिक संरक्षण के लिये प्रबंधित एक विशिष्ट क्षेत्र है।
- विशिष्ट संरक्षण, आवास संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र निगरानी अथवा मत्स्य प्रबंधन उद्देश्यों को पूरा करने के लिये इस क्षेत्र के भीतर कुछ गतिविधियाँ सीमित या फिर पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।
- MPA में मत्स्यपालन, अनुसंधान और अन्य मानवीय गतिविधियाँ निश्चित तौर पर प्रतिबंधित नहीं है; वास्तव में कई MPAs अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं।
- अंटार्कटिक में MPAs स्थापित करने की आवश्यकता:
- अंटार्कटिक, जो कि विश्व के महासागरों का 10% है, यहाँ लगभग 10,000 विशिष्ट ध्रुवीय प्रजातियाँ पाई जाती हैं और यह दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है।
- जलवायु परिवर्तन समुद्री बर्फ और हिम स्तर के नीचे समुद्री तल जैसे पर्यावासों को बदल रहा है जो विभिन्न प्रजातियों के आवास हैं।
- व्यावसायिक मत्स्यपालन में क्रिल का उपयोग मछलियों की खुराक और लोगों को पोषक तत्त्व प्रदान करने हेतु किया जाता है।
- क्रिल के बढ़ते मत्स्यन से उन जानवरों को खतरा है जो उन्हें खाते हैं। इनमें मछली, व्हेल, सील, पेंगुइन और अन्य समुद्री पक्षी शामिल हैं।
- वर्ष 2022 के एक अध्ययन में क्रिल मत्स्य डेटा के चालीस से अधिक वर्षों का विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि पश्चिमी अंटार्कटिक प्रायद्वीप के आसपास के क्षेत्रों और दक्षिण ऑर्कनी द्वीपों के पास क्रिल मछली पकड़ने की घटनाएँ सबसे अधिक हुई थीं।
- क्षेत्र के जलवायु परिवर्तन और वाणिज्यिक मत्स्यन को कम करने की आवश्यकता है तथा इसके लिये MPA आवश्यक है।
अंटार्कटिक में MPAs की स्थिति:
- दक्षिणी महासागर में दो MPAs हैं, एक दक्षिण ऑर्कनी द्वीप समूह के दक्षिणी शेल्फ में और दूसरा रॉस सागर में। ये पूरी तरह से समुद्र के केवल 5% की रक्षा करते हैं।
- दक्षिण ऑर्कनी द्वीप MPA के दक्षिणी शेल्फ के भीतर वैज्ञानिक अनुसंधान के अतिरिक्त सभी प्रकार की मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है। मछली पकड़ने के जहाज़ों से निर्वहन और डंपिंग की भी अनुमति नहीं है।
- रॉस MPA में 72% जल क्षेत्र वाणिज्यिक मछली पकड़ने हेतु प्रतिबंधित है।
- वर्ष 2012 से यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने पूर्वी अंटार्कटिक में एक MPA प्रस्तावित किया है। यूरोपीय संघ और नॉर्वे द्वारा वेडेल सागर में तथा चिली एवं अर्जेंटीना द्वारा अंटार्कटिक प्रायद्वीप के आसपास के जल क्षेत्र में एक MPA प्रस्तावित किया गया था।
- वर्ष 2021 में भारत ने पूर्वी अंटार्कटिका और वेडेल सागर को MPA के रूप में नामित करने के लिये अपना समर्थन दिया।
- लेकिन रिपोर्टों के अनुसार, चीन और रूस ने अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण के लिये आयोग (CCAMLR) की 41वीं वार्षिक बैठक में इन प्रयासों को अवरुद्ध कर दिया।
क्रिल:
- क्रिल छोटे, झींगे जैसे क्रस्टेशियन हैं जो विश्व के सभी महासागरों में पाए जाते हैं। वे समुद्री खाद्य शृंखला का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो मछलियों, पक्षियों एवं व्हेल की कई प्रजातियों हेतु प्राथमिक खाद्य स्रोत की भूमिका निभाते हैं।
- क्रिल की लंबाई सामान्यतः 1 से 6 सेंटीमीटर तक होती है और ये अपनी विशिष्ट पहचान हेतु जाने जाते हैं, जिसमें बड़ी आँखें, पारदर्शी शरीर के साथ ही लंबे पंख जैसे एंटीना शामिल हैं।
- क्रिल वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर एवं इसे गहरे समुद्र में जमा करके पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
स्रोत: डाउन टू अर्थ
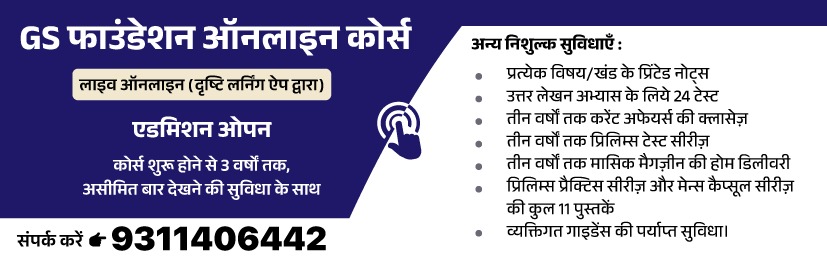
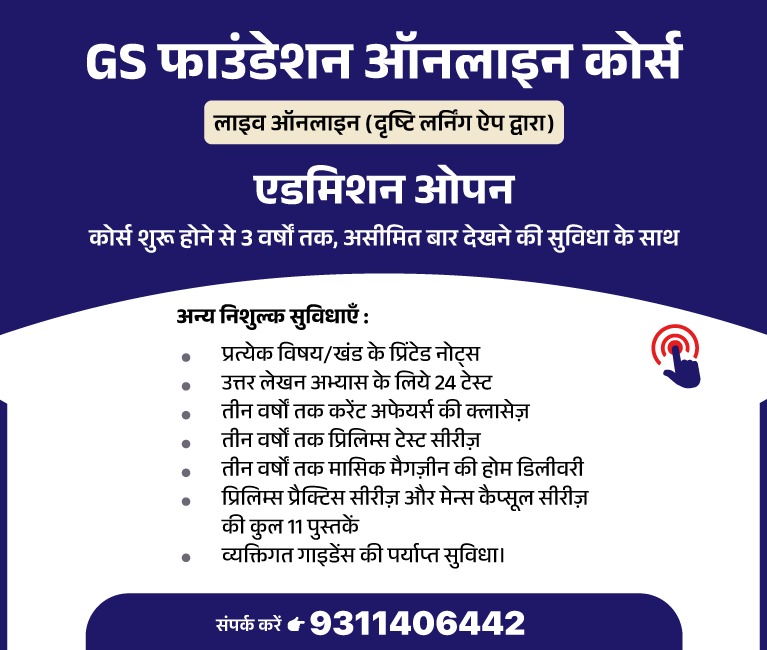
शासन व्यवस्था
सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का PM औपचारिकरण
प्रिलिम्स के लिये:सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP), आकांक्षी ज़िले, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), नाबार्ड की PM औपचारिकरण। मेन्स के लिये:PMFME योजना की विशेषताएँ, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थिति। |
चर्चा में क्यों?
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) भारत में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी एवं व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिये केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme-PMFME) योजना के औपचारिकरण को लागू कर रहा है।
- यह योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान- वोकल फॉर लोकल पहल का एक हिस्सा है।
PMFME योजना की विशेषताएँ:
- परिचय:
- PMFME योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा निजी सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देना है।
- PMFME योजना 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिये लागू है।
- केंद्रित क्षेत्र:
- यह योजना इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं और उत्पादों के विपणन के संबंध में पैमाने का लाभ उठाने के लिये एक ज़िला एक उत्पाद (One District One Product- ODOP) दृष्टिकोण अपनाती है।
- अन्य फोकस क्षेत्रों में वेस्ट टू वेल्थ उत्पाद, लघु वन उत्पाद और आकांक्षी ज़िले शामिल हैं।
- PMFME योजना के तहत उपलब्ध सहायता:
- व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:
- पात्र परियोजना लागत का 35% क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा, जिसमें अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए प्रति यूनिट है।
- सीड कैपिटल के लिये स्वयं सहायता समूहों (SHG) को सहायता:
- कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिये खाद्य प्रसंस्करण में लगे SHG के प्रति सदस्य को 40,000 रुपए तक की सीड कैपिटल के साथ अधिकतम 4 लाख रुपए प्रति SHG की सहायता।
- सामान्य अवसंरचना के लिये समर्थन:
- FPO, SHG, सहकारी समितियों एवं सामान्य बुनियादी ढाँचे की स्थापना के लिये किसी भी सरकारी एजेंसी का समर्थन करने हेतु अधिकतम 3 करोड़ रुपए के साथ 35% की क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी।
- क्षमता निर्माण:
- इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (Entrepreneurship Development Skilling) (EDP+) के लिये प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये संशोधित कार्यक्रम है।
- FSSAI एवं अन्य वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिये ज़िला संसाधन व्यक्तियों (District Resource Persons-DRPs) को नियुक्त किया गया है।
- व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:
भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थिति:
- परिचय:
- खाद्य प्रसंस्करण एक प्रकार का विनिर्माण है जिसमें कच्चे माल को वैज्ञानिक ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मध्यवर्ती खाद्य पदार्थों में संसाधित किया जाता है।
- यह तैयार उत्पाद की भंडारण क्षमता, पोर्टेबिलिटी, स्वाद एवं सुविधा में सुधार करता है।
- महत्त्व:
- वित्त वर्ष-21 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र लगभग 8.3% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है।
- नवीनतम उद्योग वार्षिक सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries- ASI) 2019-20 के अनुसार, पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में 12.2% व्यक्ति खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत थे।
- प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात सहित कृषि-खाद्य निर्यात का मूल्य वर्ष 2021-22 के दौरान भारत के कुल निर्यात का लगभग 10.9% है।
- समस्याएँ:
- अवसंरचना का अभाव: भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष बुनियादी ढाँचे की चुनौतियाँ मौजूद हैं, जिसमें अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज सुविधाएँ, परिवहन सुविधाएँ एवं प्रसंस्करण संयंत्र शामिल हैं।
- वित्त तक सीमित पहुँच: भारत में कई छोटे और मध्यम आकार के खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय अपने संचालन में निवेश करने एवं उत्पादों को बेहतर बनाने हेतु वित्त की प्राप्ति के लिये विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं।
- यह उद्योग क्षेत्र में विस्तार और बड़े अभिकर्त्ताओं के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है।
- अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण: भारत में खाद्य प्रसंस्करण की गुणवत्ता, विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों को लेकर चिंताएँ हैं।
- यह उद्योग हेतु एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यह उपभोक्ता विश्वास को प्रभावित करता है और निर्यात के अवसरों को सीमित करता है।
- सरकारी पहल:
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र हेतु स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment- FDI) की अनुमति दी गई है।
- मेगा फूड पार्कों (Mega Food Parks- MFP) के साथ-साथ MFP में प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में निवेश हेतु किफायती ऋण प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development- NABARD) के साथ 2000 करोड़ रुपए का एक विशेष खाद्य प्रसंस्करण कोष स्थापित किया गया था।
- वर्ष 2019 में व्यक्तिगत निर्माण इकाइयों की स्थापना के साथ-साथ कृषि-प्रसंस्करण समूहों की स्थापना हेतु कोष का दायरा बढ़ाया गया था।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:प्रिलिम्स:प्रश्न. भारत सरकार "मेगा फूड पार्क" की अवधारणा को किन-किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? (2011)
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (b) प्रश्न. लागत प्रभावी छोटी प्रकमण इकाई की अल्प स्वीकारिता के क्या कारण हैं? खाद्य प्रकमण इकाई गरीब किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में किस प्रकार सहायक होगी? (मुख्य परीक्षा- 2017) |
स्रोत: पी.आई.बी.
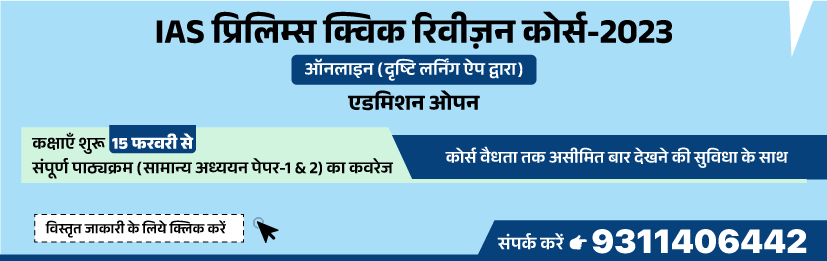
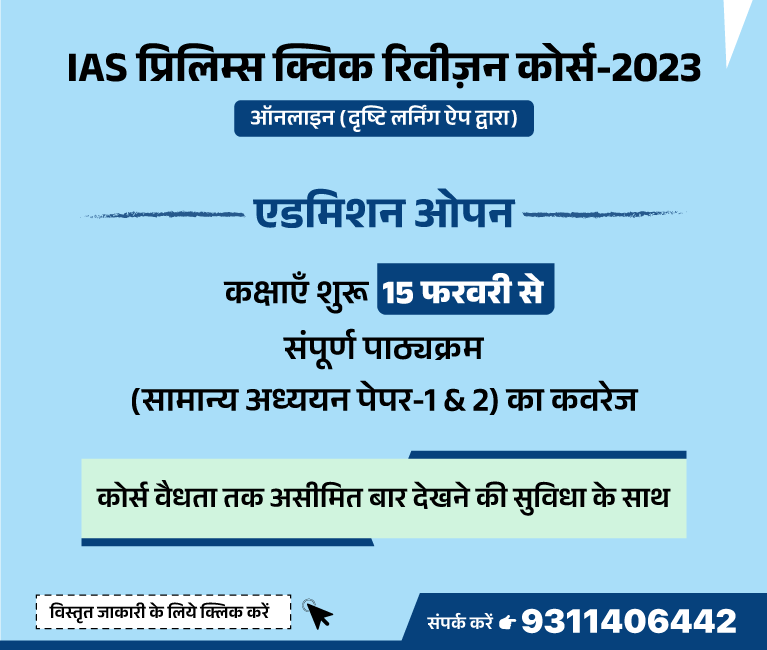
शासन व्यवस्था
मवेशियों का विशृंगीकरण एवं बंध्याकरण
प्रिलिम्स के लिये:मवेशियों का विशृंगीकरण एवं बंध्याकरण, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, पशुपालन, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। मेन्स के लिये:मवेशियों का विशृंगीकरण एवं बंध्याकरण। |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में केंद्र सरकार ने मवेशियों के विशृंगीकरण (सींग निकालने) एवं उनके बंध्याकरण के साथ ही किसी भी जानवर की ब्रांडिंग या नाक में रस्सी बाँधने की प्रक्रिया निर्धारित की है।
मवेशियों का विशृंगीकरण एवं बंध्याकरण:
- विशृंगीकरण मवेशियों के सींगों को हटाने या छोटा करने की प्रक्रिया है, जबकि बंध्याकरण नर मवेशियों के अंडकोष को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित है। दोनों प्रथाओं का उपयोग आमतौर पर विभिन्न कारणों से किया जाता है, जैसे कि हैंडलर्स एवं अन्य जानवरों के लिये सुरक्षा में सुधार करने, जख्म को रोकने, आक्रामकता को कम करने एवं मांस की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु।
- विशृंगीकरण हेतु कई माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है, जिनमें रासायनिक या विद्युत विधियाँ, आरी और विशृंगीकरण आयरन शामिल हैं। कई मामलों में पशुओं के युवा होने पर दर्द एवं असुविधा को कम करने के लिये विशृंगीकरण किया जाता है।
- मौजूदा तरीकों में बैल को ज़मीन पर धकेल कर कैस्ट्रेटर सैन पेनकिलर (Castrator San Painkiller) का उपयोग किया जाना शामिल है।
- बंध्याकरण आमतौर पर नर मवेशियों का किया जाता है जिसका उद्देश्य प्रजनन हेतु नहीं किया जाता अपितु यह आक्रामकता को कम करने एवं मांस की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है।
- बंध्याकरण विधि में रक्त वाहिकाओं, तंत्रिकाओं और वास डेफेरेंस (एक कुंडलित ट्यूब जो वृषण से शुक्राणु को बाहर ले जाती है) को दबा देने से अंडकोष निष्क्रिय हो जाता है।
नए नियम:
- सभी प्रक्रियाओं को लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा पेशेवर की सहायता से किया जाना चाहिये और सामान्य एवं स्थानीय एनेस्थेटिक दोनों का उपयोग किया जाना चाहिये।
- नियम स्वाभाविक रूप से बिना सींग वाले मवेशियों के प्रजनन की मांग करते हैं और नाक की रस्सियों की बजाय फेस हॉल्टर एवं अन्य मानवीय प्रक्रियाओं का उपयोग पर ज़ोर देते हैं, साथ ही जीवित ऊतकों पर ठंडे और गर्म दाहांकन/ब्रांडिंग को प्रतिबंधित करते हैं।
- दर्दनाक मौत को रोकने हेतु नियम बीमार जानवरों के लिये इच्छामृत्यु की पद्धति निर्धारित करते हैं।
- यह समस्या चिंताजनक है क्योंकि अधिकांश डेयरी मालिक और किसान अतिरिक्त खर्च या उन्हें बनाए रखने हेतु आवश्यक प्रयास के कारण अपने बैलों को सड़कों पर छोड़ देते हैं।
संबंधित मौजूदा प्रावधान:
- जानवरों के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 और उप-धारा 3 के तहत सींग निकालने एवं बधिया करने की प्रक्रिया पहले अपरिभाषित थी, जिससे जानवरों के खिलाफ क्रूरता को रोकना मुश्किल हो गया था।
- धारा 11 में उन कृत्यों को परिभाषित किया गया है जो जानवरों के साथ क्रूरता का व्यवहार करते हैं।
- लेकिन उपधारा 3 में पशुपालन प्रक्रियाओं हेतु अपवादों का प्रावधान है, जिसमें एक निर्धारित तरीके से मवेशियों का सींग निकालना और बंध्याकरण, ब्रांडिंग एवं जानवरों की नाक में रस्सी बाँधना शामिल है।
- कानून की धारा 3(c) में "उस समय लागू किसी भी कानून के अधिकार के तहत किसी भी जानवर को भगाने या मारने" हेतु अपवाद का प्रावधान शामिल है।
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960
- इस अधिनियम का उद्देश्य ‘पशुओं को अनावश्यक दर्द पहुँचाने या पीड़ा देने से रोकना’ है, जिसके लिये अधिनियम में पशुओं के प्रति अनावश्यक क्रूरता और पीड़ा पहुँचाने के लिये दंड का प्रावधान किया गया है।
- वर्ष 1962 में इस अधिनियम की धारा 4 के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) की स्थापना की गई थी।
- यह अधिनियम पशुओं और पशुओं के विभिन्न रूपों को परिभाषित करने के साथ ही वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिये पशुओं पर प्रयोग (Experiment) से संबंधित दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
- पहले अपराध के मामले में ज़ुर्माना जो दस रुपए से कम नहीं होगा लेकिन यह पचास रुपए तक हो सकता है।
- पिछले अपराध के तीन वर्ष के भीतर किये गए दूसरे या बाद के अपराध के मामले में ज़ुर्माना पच्चीस रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन यह एक सौ रुपए तक हो सकता है या तीन महीने तक कारावास की सज़ा या दोनों हो सकती है।
- यह वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिये पशुओं पर प्रयोग से संबंधित दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
- यह अधिनियम पशुओं की प्रदर्शनी और पशुओं का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ अपराधों से संबंधित प्रावधान करता है।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2014)
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) व्याख्या:
|
स्रोत: डाउन टू अर्थ