उत्तर प्रदेश Switch to English
एक जनपद एक उत्पाद के तहत नए उत्पाद शामिल
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) योजना के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया।
मुख्य बिंदु
- एक जनपद एक उत्पाद योजना के बारे में:
- यह योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी।
- इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक ज़िले के विशिष्ट और पारंपरिक उत्पादों की पहचान की जाती है तथा उन्हें भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया जाता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वे उत्पाद किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित हैं।
- राज्य सरकार इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में पहचान दिलाने के लिये उद्यमियों को वित्तीय सहायता, सामूहिक विपणन सुविधाएँ तथा अन्य संसाधन प्रदान करती है।
- इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:
- राज्य में रोज़गार के नए अवसरों का सृजन
- राज्य के निर्यात को बढ़ावा देना
- उत्तर प्रदेश को वर्ष 2029 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में योगदान देना
- अब तक इस योजना के अंतर्गत 62 उत्पाद सूचीबद्ध थे, किंतु 12 नए उत्पाद जोड़े जाने के बाद यह संख्या बढ़कर 74 हो गई है।
- 12 नए उत्पाद जो शामिल किये गए हैं:
- बागपत – कृषि यंत्र एवं संबंधित उपकरण
- सहारनपुर – होज़री उत्पाद
- फिरोज़ाबाद – खाद्य प्रसंस्करण
गाज़ियाबाद – मैटल, वस्त्र एवं परिधान - अमरोहा – मेटल एवं वुडन हैंडीक्राफ्ट
- आगरा – पेठा उद्योग और सभी प्रकार के फुटवीयर
- हमीरपुर – मैटल उत्पाद
- बरेली – लकड़ी के उत्पाद
- एटा – चिकोरी उत्पाद
- प्रतापगढ़ – खाद्य प्रसंस्करण
- बिजनौर – ब्रश और संबंधित उत्पाद
- बलिया – सत्तू उत्पाद
भौगोलिक संकेत (GI) टैग
- भौगोलिक संकेत (GI) टैग, एक ऐसा नाम या चिह्न है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं।
- GI टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्त्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति है।
- यह उत्पाद को दूसरों द्वारा नकल या अनुकरण किये जाने से भी बचाता है।
- एक पंजीकृत GI टैग 10 वर्षों के लिये वैध होता है।
- GI पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है।
- विधिक ढाँचा:
- यह बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार-संबंधित पहलुओं (TRIPS) पर WTO समझौते द्वारा विनियमित एवं निर्देशित है।

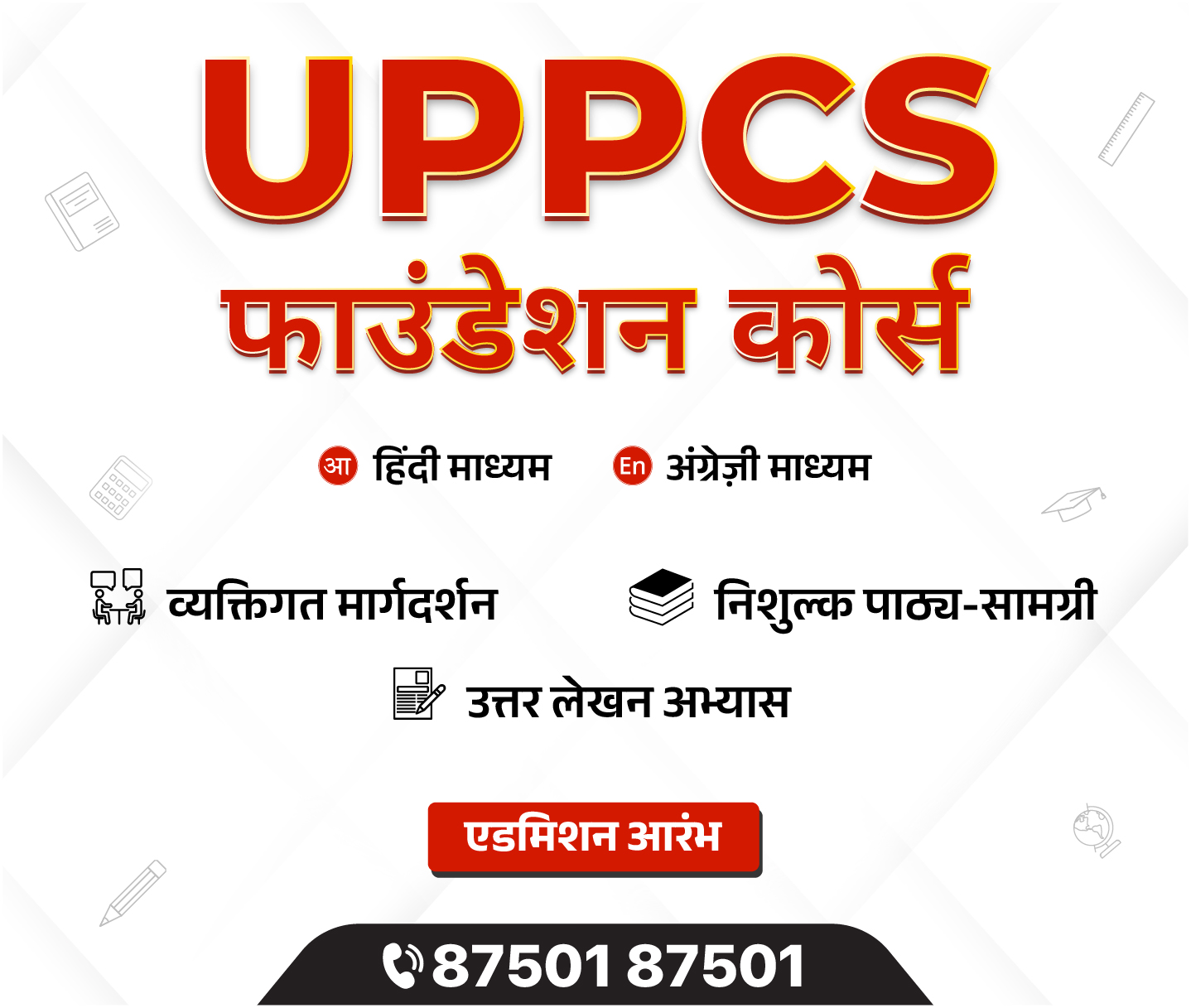
उत्तर प्रदेश Switch to English
भारत का सबसे बड़ा टाइटेनियम और सुपरलॉय सामग्री संयंत्र
चर्चा में क्यों?
केंद्रीय रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपरएलॉय मटेरियल्स प्लांट का उद्घाटन किया।
मुख्य बिंदु
- प्लांट के बारे में:
- यह टाइटेनियम प्लांट PTC इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी एरोलॉय टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा संचालित है।
- यह प्लांट 50 एकड़ क्षेत्र में फैला है और इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 6,000 टन है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल-साइट टाइटेनियम रीमेल्टिंग सुविधा बन गया है।
- इस संयंत्र में उपयोग की जा रही अत्याधुनिक तकनीकों में शामिल हैं:
- वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग (VAR)
- इलेक्ट्रॉन बीम (EB)
- प्लाज्मा आर्क मेल्टिंग (PAM)
- वैक्यूम इंडक्शन मेल्टिंग (VIM)
- इन तकनीकों से aerospace-grade सामग्री का घरेलू उत्पादन संभव हो सकेगा।
- टाइटेनियम प्लांट के साथ-साथ सात अतिरिक्त उन्नत सुविधाओं की आधारशिला भी रखी गई। इनमें प्रमुख हैं:
- एयरोस्पेस प्रिसिजन कास्टिंग प्लांट: जो सिंगल क्रिस्टल कास्टिंग बनाते हैं, जो जेट इंजन के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- एयरोस्पेस फोर्ज शॉप और मिल उत्पाद संयंत्र: बिलेट्स, बार और प्लेट्स जैसे महत्त्वपूर्ण सामग्री के निर्माण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
- एयरोस्पेस प्रिसिजन मशीनिंग शॉप: जो रेडी-टू-असेंबल अल्ट्रा-प्रिसिजन सीएनसी मशीनीकृत घटकों की क्षमता प्रदान करता है।
- यह परियोजना उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत विकसित की जा रही है, जिसका उद्देश्य रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
टाइटेनियम
- यह एक हल्की एवं मज़बूत धातु है। यह इस्पात जैसा मज़बूत, लेकिन उससे बहुत हल्का होता है।
- जलमग्न वस्तु बनाने के लिये टाइटेनियम पसंदीदा पदार्थ है, क्योंकि यह अधिक गहराई में भी पानी के भारी दबाव का सामना कर सकता है और इसमें जंग भी नहीं लगता है।
- टाइटेनियम धातु एल्यूमीनियम, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, लोहा और अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किया जाता है। टाइटेनियम के इन मिश्र धातुओं का उपयोग विमानन उद्योग में किया जाता है।
- टाइटेनियम संयुक्त प्रतिस्थापन भागों का एक घटक है, जिसमें हिप बॉल और सॉकेट शामिल हैं।
- टाइटेनियम का प्रयोग दंत प्रत्यारोपण में भी किया जाता है।
उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा
- यह एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करना है।
- इसमें 6 नोड्स होंगे- अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झाँसी और लखनऊ।
- उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) को राज्य की विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर इस परियोजना को निष्पादित करने के लिये नोडल एजेंसी बनाया गया था।
- इस कॉरिडोर/गलियारे का उद्देश्य राज्य को सबसे बड़े और उन्नत रक्षा विनिर्माण केंद्रों में से एक के रूप में स्थापित करना एवं विश्व मानचित्र पर लाना है।
- रक्षा गलियारा एक मार्ग या पथ को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन के साथ-साथ रक्षा बलों हेतु उपकरण/परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिये किया जाता है।
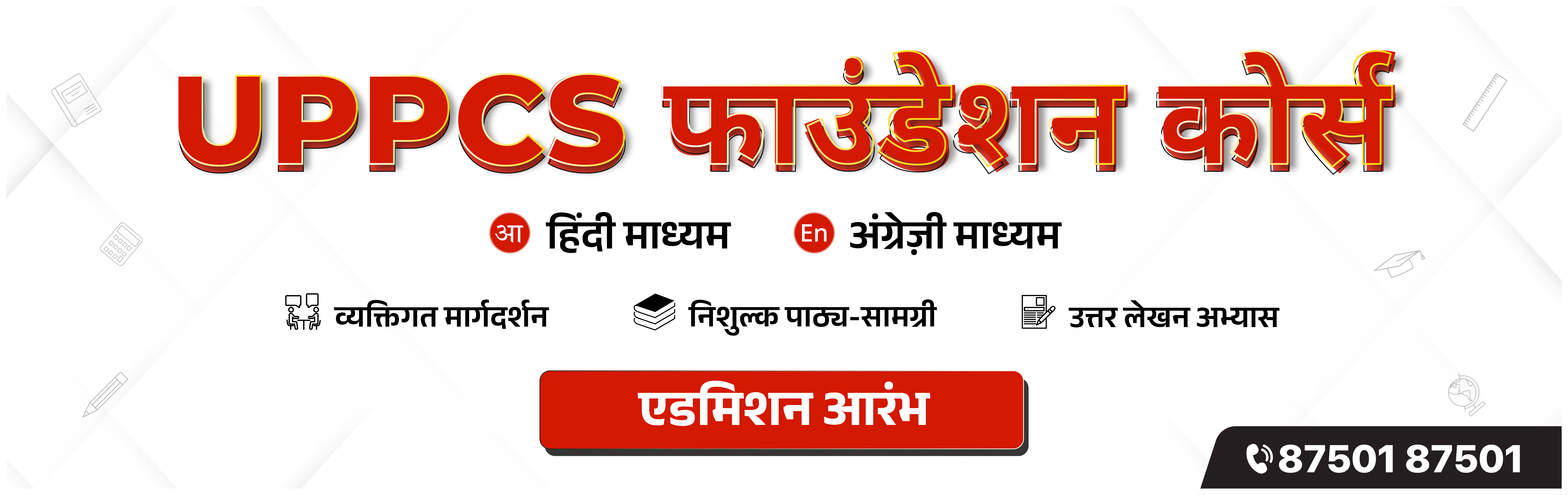
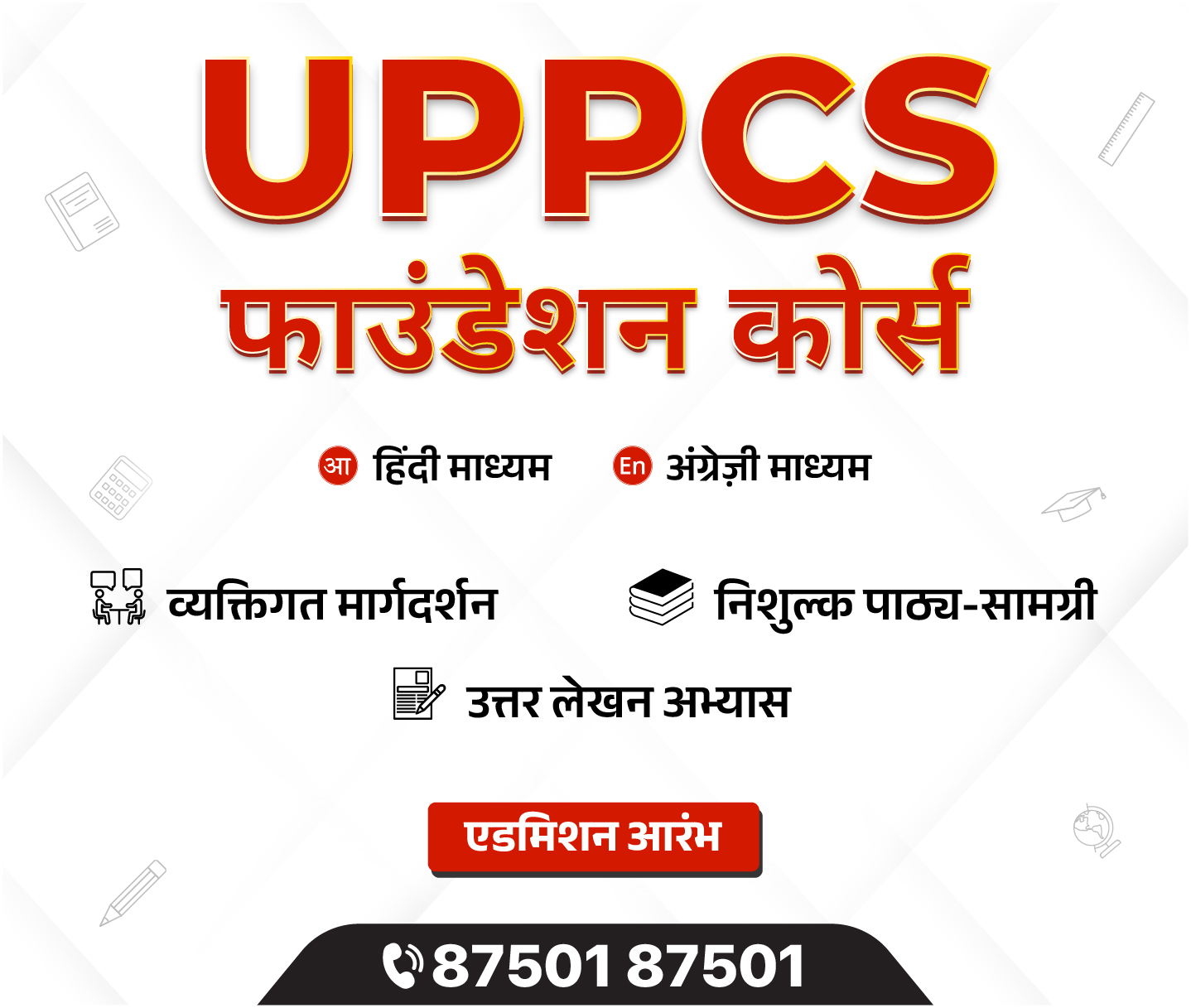
मध्य प्रदेश Switch to English
ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना
चर्चा में क्यों?
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से कार्यान्वित करने के लिये एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं।
मुख्य बिंदु
परियोजना के बारे में:
- यह विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge) योजना है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में सिंचाई हेतु नदी जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करना है।
- इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र संयुक्त रूप से मुलताई, मध्य प्रदेश से निकलने वाली ताप्ती नदी की तीन उपधाराओं का विकास किया जाएगा।
- यह केन-बेतवा लिंक परियोजना (मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) और पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना (मध्य प्रदेश और राजस्थान) के बाद मध्य प्रदेश से जुड़ी तीसरी प्रमुख अंतर-राज्यीय नदी परियोजना है।
प्रमुख विशेषताएँ:
- जल आवंटन: इस परियोजना के अंतर्गत ताप्ती नदी से पूर्वोत्तर महाराष्ट्र में पेयजल आपूर्ति तथा दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश में सिंचाई सहायता हेतु जल स्थानांतरित कर आपूर्ति की जाएगी।
- उपयोग हेतु कुल जल 31.13 हज़ार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) है, जिसमें से 11.76 TMC मध्य प्रदेश को और 19.36 TMC महाराष्ट्र के लिये आवंटित है।
- इस परियोजना में मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र सीमा पर एक डायवर्जन वियर का निर्माण तथा दोनों राज्यों में दाएँ और बाएँ किनारे की नहरों का विकास शामिल है।
- इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की 3,362 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाएगा, जिसके लिये किसी विस्थापन या पुनर्वास की आवश्यकता नहीं होगी।
- लाभार्थी ज़िले: यह परियोजना मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और खंडवा तथा महाराष्ट्र के अकोला, अमरावती और बुलढाणा ज़िलों को कवर करती है, जो पारंपरिक रूप से भूजल संकट और अनियमित वर्षा की समस्या से ग्रस्त रहे हैं।
तापी/ताप्ती नदी:
- पश्चिम की ओर बहने वाली एक अन्य महत्त्वपूर्ण नदी मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है।
- यह नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है।
- इसका बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को कवर करता है।
- ताप्ती नदी की तीन प्रमुख सहायक नदियाँ- पूर्णा, गिरना और पंजरा- महाराष्ट्र राज्य में दक्षिण से बहती हैं।
- उकाई बाँध: तापी नदी पर स्थित एक प्रमुख जलविद्युत परियोजना, जो आसपास के क्षेत्रों को पानी और बिजली प्रदान करती है।


छत्तीसगढ़ Switch to English
करेगुट्टालु पहाड़ी पर माओवादी विरोधी अभियान
चर्चा में क्यों?
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और छत्तीसगढ़ पुलिस ने हाल ही में छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर स्थित करेगुट्टालु पहाड़ी पर 21 दिवसीय गहन माओवादी विरोधी अभियान का समापन किया।
- यह ऑपरेशन वामपंथी उग्रवाद (LWE) को खत्म करने और 31 मार्च, 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने के भारत के चल रहे संघर्ष में एक महत्त्वपूर्ण सफलता है।
मुख्य बिंदु
करेगुट्टालु पहाड़ी का सामरिक महत्त्व
- करेगुट्टालु पहाड़ी लगभग 60 किमी लंबी और 5-20 किमी चौड़ी एक ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र है, जो पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) जैसे प्रमुख माओवादी संगठनों के लिये एक गढ़ और एकीकृत कमान केंद्र बन गया था।
- यह क्षेत्र 300-350 सशस्त्र माओवादी कार्यकर्त्ताओं के लिये शरणस्थली के रूप में कार्य करता था, जिसमें तकनीकी विभाग की हथियार निर्माण इकाइयाँ भी शामिल थीं, जिससे क्षेत्र में लंबे समय तक विद्रोह जारी रहा।
- माओवादी इसे इसकी भौगोलिक स्थिति और दो राज्यों (छत्तीसगढ़ और तेलंगाना) से निकटता के कारण अभेद्य मानते थे, जिससे सुरक्षा बलों के अभियान जटिल हो जाते थे।
ऑपरेशन के उद्देश्य और परिणाम
- इसका प्राथमिक उद्देश्य करेगुट्टालु पहाड़ी पर केंद्रित शीर्ष माओवादी नेतृत्व को विस्थापित करना तथा उनके एकीकृत सैन्य ढाँचे को ध्वस्त करना था।
- इसे छत्तीसगढ़ में अब तक का “सबसे बड़ा व्यापक और समन्वित माओवादी विरोधी अभियान” माना जा रहा है, जो दुर्गम माओवादी गढ़ों पर पुनः कब्ज़ा करने के लिये सुरक्षा बलों की क्षमता और संकल्प को दर्शाता है।
- इस अभियान के दौरान 21 दिनों में 21 मुठभेड़ें हुईं, जिसके परिणामस्वरूप महिला कार्यकर्त्ताओं सहित कई माओवादी मारे गए।
- इस ऑपरेशन में ज़िला रिज़र्व गार्ड, बस्तर फाइटर्स, विशेष कार्य बल, CRPF की कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन (कोबरा) इकाई और राज्य पुलिस जैसी कई इकाइयों के समन्वित प्रयास शामिल थे, जिससे अंतर-एजेंसी तालमेल का प्रदर्शन हुआ।
पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA)
- PLGA का गठन 2 दिसंबर, 2000 को हुआ था।
- यह भारत में प्रतिबंधित राजनीतिक संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की सशस्त्र शाखा के रूप में कार्य करता है।
- यह समूह लंबे समय तक चलने वाले जनयुद्ध के माध्यम से सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
प्रारंभ और विकास:
- CRPF की स्थापना वर्ष 1939 में रियासतों में राजनीतिक उथल-पुथल और अशांति के जवाब में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी।
- वर्ष 1949 में इस बल का नाम बदलकर केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल कर दिया गया।
- तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने CRPF के लिये एक बहुमुखी भूमिका की कल्पना की थी तथा इसके कार्यों को नव स्वतंत्र राष्ट्र की उभरती जरूरतों के साथ संरेखित किया था।
विशेष इकाइयाँ:
- CRPF में कई विशेष इकाइयाँ हैं, जिनमें रैपिड एक्शन फोर्स (RAF), कमांडो बटालियन फॉर रिज़ोल्यूट एक्शन (कोबरा), वीआईपी सुरक्षा विंग और महिला बटालियन शामिल हैं।
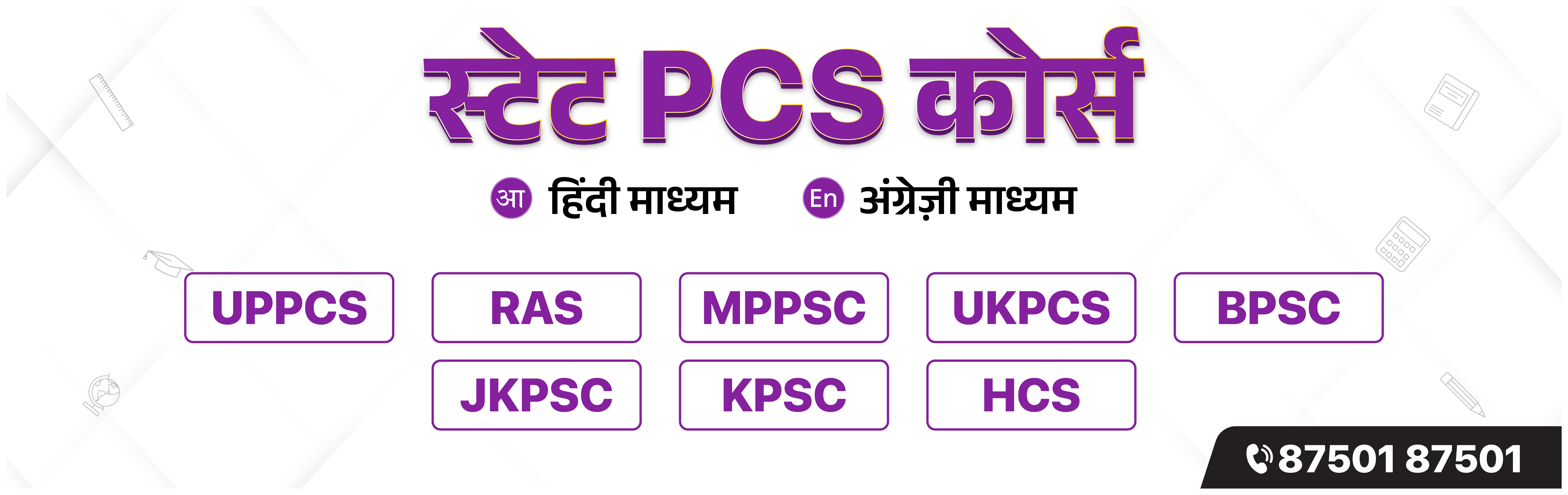
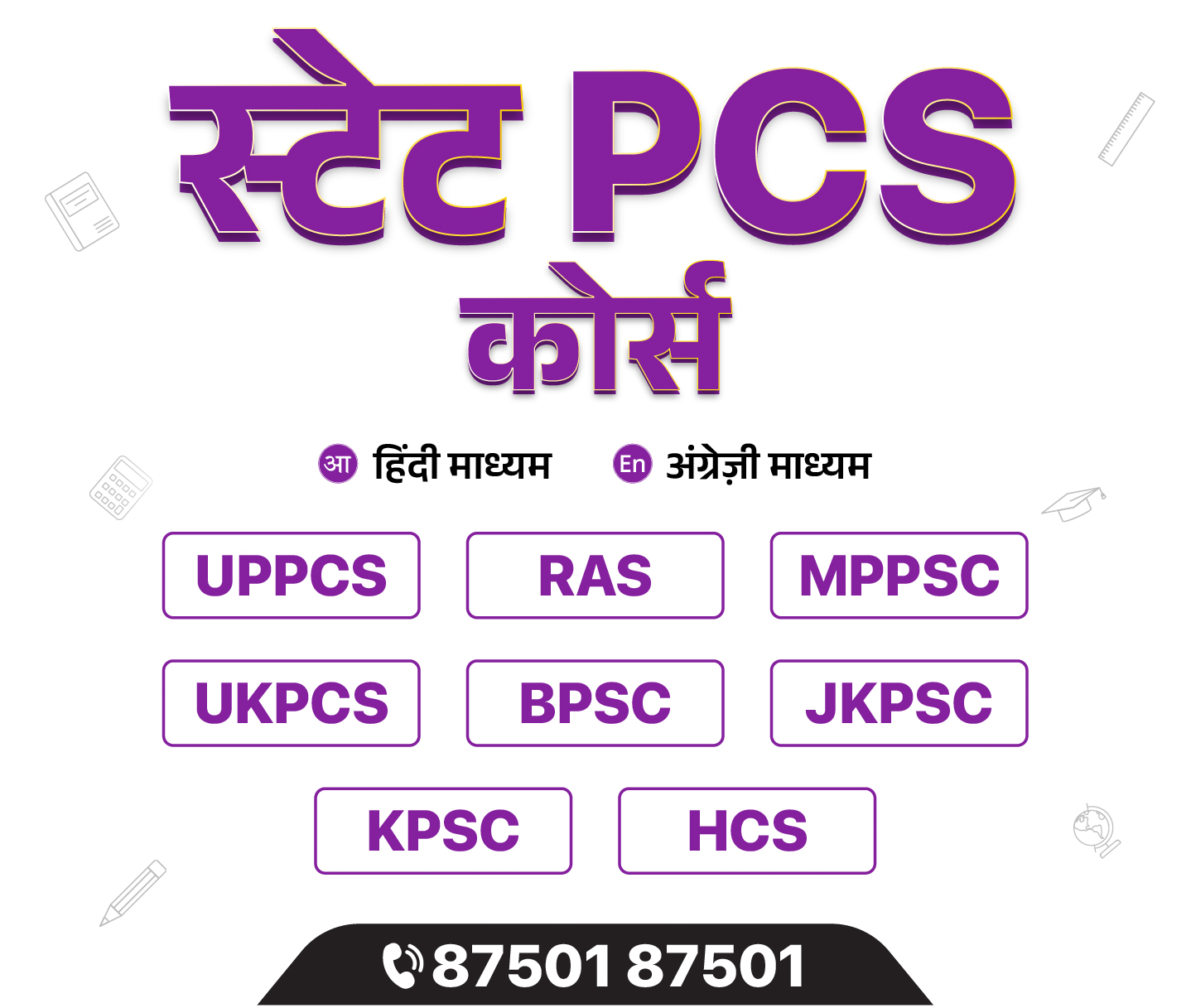
राजस्थान Switch to English
राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2025
चर्चा में क्यों?
राजस्थान सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2025 आयोजित किया गया।
मुख्य बिंदु
मेले के बारे में:
- मेले में विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्यवर्द्धक और परंपरागत मसाले, मिलेट्स अनाज (श्री अन्न) से बने उत्पाद और अन्य सहकारी उत्पादों की प्रदर्शनी की गई।
- इस वर्ष मेले में श्री अन्न से बने उत्पाद विशेष रूप से आकर्षण के केंद्र बने हैं।
- मेले में विभिन्न स्वयं सहायता समूह, सहकारी उपभोक्ता संघ और स्थानीय उत्पादकों ने अपनी विविध उत्पाद शृंखला के साथ भाग लिया।
- यह मेला उपभोक्ताओं को सीधे शुद्ध, गुणवत्तापूर्ण और स्वास्थ्यकर उत्पाद खरीदने का अवसर प्रदान करता है।
- मेले के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोज़गार और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलता है।
मिलेट्स
- यह एक सामूहिक शब्द है, जो अनेक छोटे बीज वाली घासों (small-seeded grasses) को संदर्भित करता है, जिनकी खेती अनाज की फसलों के रूप में की जाती है, मुख्य रूप से समशीतोष्ण, उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शुष्क क्षेत्रों की सीमांत भूमि पर।
- भारत में उपलब्ध कुछ सामान्य मोटे अनाज हैं रागी (फिंगर मिलेट), ज्वार (सोरघम), समा (लिटिल मिलेट), बाजरा (पर्ल मिलेट) और वरिगा (प्रोसो मिलेट)।
- वैश्विक और भारतीय उत्पादन: भारत बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद नाइजर और चीन का स्थान है।
- बाजरा संवर्द्धन: खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मान्यता दी गई।
- भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देती है।


उत्तराखंड Switch to English
नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) सांख्यिकीय रिपोर्ट 2021
चर्चा में क्यों?
भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) सांख्यिकीय रिपोर्ट 2021 के अनुसार, उत्तराखंड वर्ष 2016 से 2021 की अवधि के दौरान जन्म दर में वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र राज्य था।
- यह प्रवृत्ति शहरीकरण, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और महिला शिक्षा जैसे कारकों से प्रेरित उन्नत जनसांख्यिकीय परिवर्तन को इंगित करती है।
मुख्य बिंदु
रिपोर्ट के बारे में:
- SRS भारत का सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है, जिसे जन्म और मृत्यु दर जैसे प्रजनन और मृत्यु दर संकेतकों का वार्षिक अनुमान प्रदान करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- 2021 SRS, दशकीय जनगणना से प्राप्त महत्त्वपूर्ण जनसंख्या प्रवृत्ति अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो 2021 के लिये अभी तक आयोजित नहीं की गई है।
अशोधित जन्म दर:
- अशोधित जन्म दर वर्ष के दौरान होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को दर्शाती है, जिसका अनुमान मध्य वर्ष में प्रति 1,000 जनसंख्या पर लगाया जाता है।
- भारत की अशोधित जन्म दर 2021 में 19.3 थी, जो 2016 से 2021 तक सालाना 1.12% की दर से घट रही है।
- इसी अवधि के दौरान तमिलनाडु, दिल्ली और केरल में क्रमशः 2.35%, 2.23% और 2.05% प्रति वर्ष की दर से तीव्र गिरावट देखी गई।
- जन्म दर में सबसे कम गिरावट राजस्थान (0.48%), बिहार (0.86%), छत्तीसगढ़ (0.98%), झारखंड (0.98%), असम (1.05%), मध्य प्रदेश (1.05%), पश्चिम बंगाल (1.08%) और उत्तर प्रदेश (1.09%) में हुई।
- आंध्र प्रदेश (1.26%), तेलंगाना (1.67%) और कर्नाटक (1.68%) सहित अन्य दक्षिणी राज्यों में भी औसत से अधिक तीव्र गिरावट दर्ज की गई।
- संपूर्ण दक्षिणी क्षेत्र में परिवार का आकार छोटा होता जा रहा है तथा जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो रही है।
कुल प्रजनन दर (TFR) :
- कुल प्रजनन दर (TFR) एक महिला द्वारा अपने प्रजनन वर्षों के दौरान अपेक्षित बच्चों की औसत संख्या को दर्शाती है।
- वर्ष 2021 में, भारत की TFR 2.0 थी, जिसमें बिहार में 3.0 की उच्च TFR, उत्तर प्रदेश में 2.7, मध्य प्रदेश में 2.6 और राजस्थान में 2.4 थी।
सकल प्रजनन दर (GRR):
- भारत के लिये GRR 1 है, जिसका अर्थ है कि औसतन भारत में प्रत्येक महिला की एक बेटी होती है, जो प्रजनन आयु तक जीवित रहती है और उसके अपने बच्चे होते हैं।
- इसके विपरीत, बिहार (1.4), उत्तर प्रदेश (1.3), राजस्थान (1.2) और मध्य प्रदेश (1.2) में उच्च GRR दर्ज की गई।
जन्म पंजीकरण प्रवृत्ति और डाटा अंतर्दृष्टि: नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) 2021 के आंकड़ों से पता चलता है कि जन्म दर में सबसे कम गिरावट वाले राज्यों में पंजीकृत जन्मों में भी वृद्धि दर्ज की गई है, जिनमें शामिल हैं:
- बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, आदि।
- तेलंगाना में 2019 के बाद पंजीकृत जन्मों में तीव्र वृद्धि देखी गई, जिसके बाद 2020 के बाद इसमें गिरावट आई।
उत्तराखंड में महिला कल्याण से संबंधित योजनाएँ
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना: यह योजना महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रथम बार बनी माताओं और उनकी बेटियों को सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान करने के लिये शुरू की गई थी।
- नंदा गौरा योजना: लड़कियों को जन्म से लेकर शादी तक उनकी शिक्षा और सशक्तीकरण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड के पात्र निवासियों के बीच कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह और सामाजिक असमानता को रोकना है।
- मातृत्व लाभ योजना (UKBOCWWB): यह पंजीकृत महिला श्रमिकों को उनकी मातृत्व अवधि के दौरान 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना: यह कुपोषण से निपटने और मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक खाद्य पूरक प्रदान करती है।
भारत के महापंजीयक
- गृह मंत्रालय के अधीन वर्ष 1949 में स्थापित RGI, भारत की दशकीय जनगणना और भारतीय भाषाई सर्वेक्षण सहित जनसंख्या डाटा संग्रह की देखरेख के लिये ज़िम्मेदार है।
- RGI RBD अधिनियम, 1969 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है और निरंतर जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिये CRS का प्रबंधन करता है।
- यह सभी सामान्य निवासियों के जनसांख्यिकीय विवरण दर्ज करने के लिये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) का भी रखरखाव करता है।
- RGI का नेतृत्व एक वरिष्ठ सिविल सेवक करता है, जो आमतौर पर संयुक्त सचिव स्तर का होता है, RGI जनसांख्यिकीय योजना और नीति निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

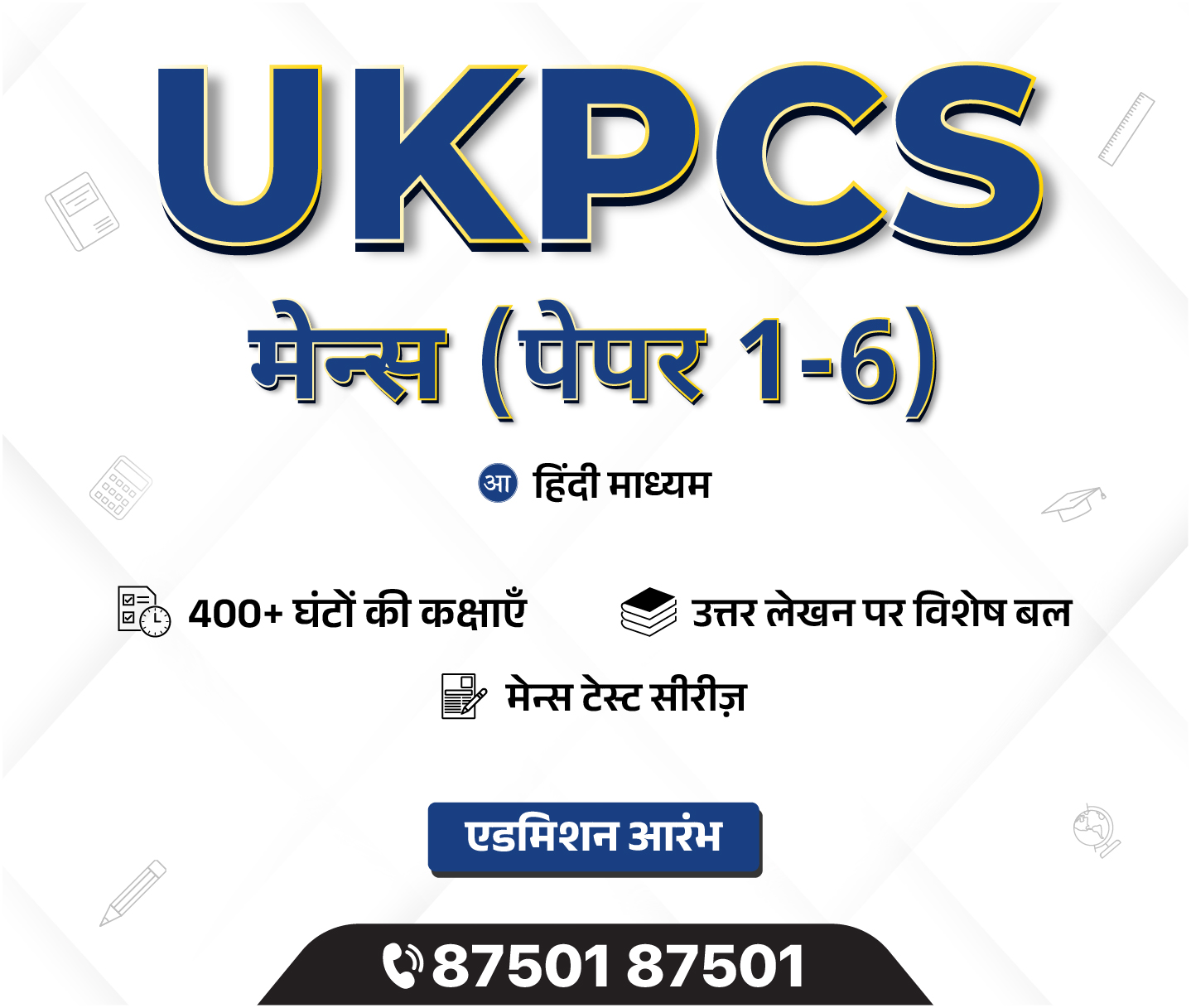
हरियाणा Switch to English
हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के प्रयास
चर्चा में क्यों?
हरियाणा सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने तथा 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत उपायों को मज़बूत करने लिये एक बैठक आयोजित की गई।
मुख्य बिंदु
- ज़िला स्तरीय समितियों का गठन:
- ज़िला स्तरीय स्थायी समितियों का गठन किया गया है, जिनके अध्यक्ष उपायुक्त (DC) हैं तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं।
- ये समितियाँ राज्य के लिंगानुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से कड़ी निगरानी और बेहतर समन्वय के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- नियमित निगरानी और निरीक्षण:
- समितियाँ साप्ताहिक बैठकें आयोजित करेंगी ताकि
- चिकित्सीय गर्भपात (MTP) किटों की बिक्री पर रिपोर्ट की समीक्षा की जा सके।
- अवैध लिंग निर्धारण को रोकने के लिये अल्ट्रासाउंड केंद्रों का निरीक्षण किया जा सके।
- कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिये रणनीति तैयार की जा सके।
- समितियाँ साप्ताहिक बैठकें आयोजित करेंगी ताकि
- कानूनी कार्रवाई और अनुशासनात्मक उपाय:
- लिंग-चयनात्मक गर्भपात में संलिप्त पाए जाने वाले डॉक्टरों पर हरियाणा मेडिकल काउंसिल द्वारा मेडिकल लाइसेंस रद्द करने सहित कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- 12 सप्ताह से अधिक के सभी गर्भपातों की, विशेषकर जब दंपति की पहले से ही बेटियाँ हों, सिविल सर्जनों द्वारा गहन जाँच की जाएगी।
- प्रारंभिक गर्भावस्था पंजीकरण: स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह शीघ्र ट्रैकिंग और सहायता के लिये 10 सप्ताह से पहले प्रत्येक गर्भावस्था का प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) पंजीकरण सुनिश्चित करे।
- 'सहेलियों' के माध्यम से व्यक्तिगत सहायता: एक या एक से अधिक लड़कियों वाली गर्भवती महिलाओं को परामर्श और निगरानी के लिये आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को 'सहेली' के रूप में नियुक्त किया जाता है।
- यदि कोई आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता अवैध गर्भपात में संलिप्त पाई गई तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता:
- ज़िला प्रशासन सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियान का विस्तार करेंगे।
- लैंगिक समानता और बालिकाओं के महत्त्व को बढ़ावा देने के लिये धार्मिक और सामुदायिक नेताओं को शामिल किया जाएगा।
बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना
- इसे लिंग-चयनात्मक गर्भपात से निपटने और घटते बाल लिंग अनुपात (2011 में प्रति 1,000 लड़कों पर 918 लड़कियाँ) में सुधार लाने के लिये जनवरी 2015 में शुरू किया गया था।
- यह योजना महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालयों की संयुक्त पहल है।
- 405 ज़िलों में क्रियान्वित इस योजना का मुख्य उद्देश्य लिंग-पक्षपाती लिंग चयन को रोकना, लड़कियों का अस्तित्व और संरक्षण सुनिश्चित करना, उनकी शिक्षा और भागीदारी को बढ़ावा देना तथा उनके अधिकारों की रक्षा करना है।
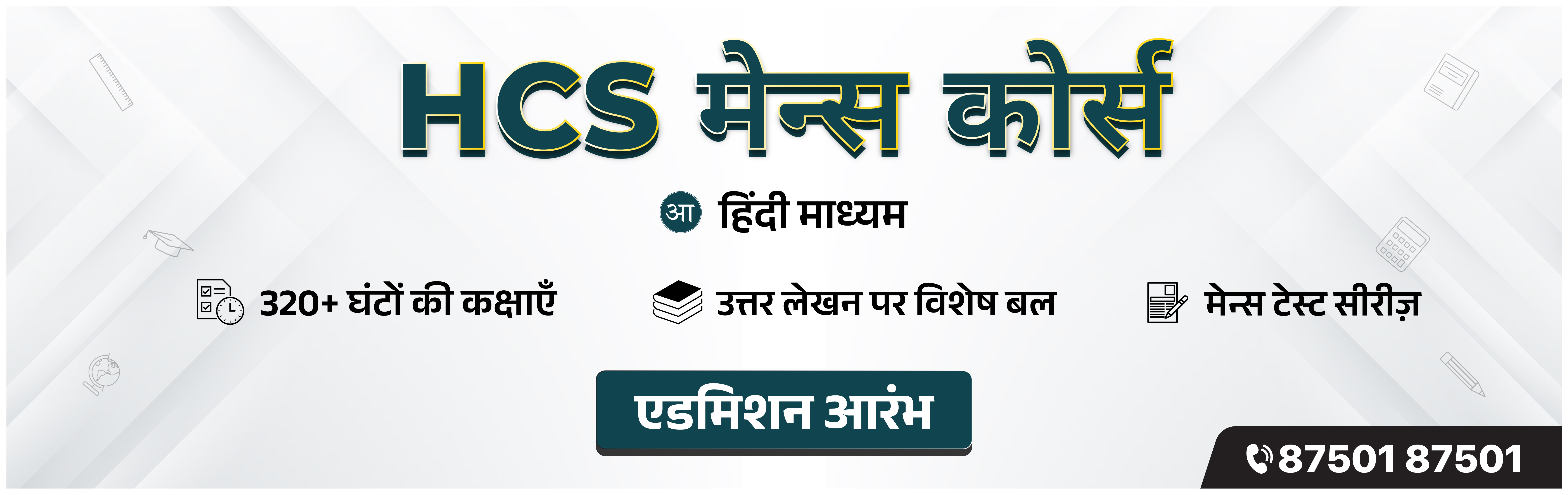


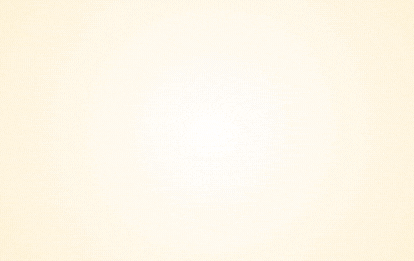



 PCS परीक्षण
PCS परीक्षण



