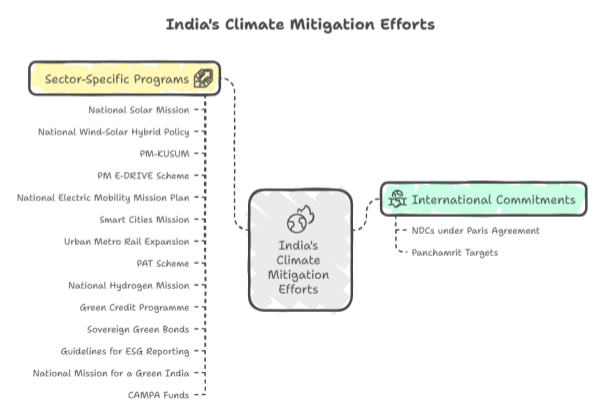जैव विविधता और पर्यावरण
जलवायु-परिवर्तन के प्रति भारत की समुत्थानशक्ति
यह एडिटोरियल 03/08/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “India’s climate challenge” पर आधारित है। इस लेख के तहत भारत के गंभीर होते जलवायु संकट— समुद्र-स्तर में वृद्धि, अनियमित मानसून और निरंतर आपदाओं पर प्रकाश डाला गया है, जो यह दर्शाते हैं कि अब जलवायु-अनुकूलन एवं समुत्थानशील विकास दृष्टिकोण अपनाना अत्यंत आवश्यक हो गया है।
प्रिलिम्स के लिये:सुंदरबन मैंग्रोव, वायनाड भूस्खलन, चक्रवात, हसदेव अरण्य, वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना, ग्रीनवाशिंग, नगरीय ऊष्मा द्वीप मेन्स के लिये:भारत के समक्ष जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रमुख खतरे, भारत के जलवायु शमन प्रयासों की प्रभावशीलता को कमज़ोर करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ। |
भारत एक गंभीर होते जलवायु संकट का सामना कर रहा है। पिछले दो दशकों में जलवायु आपदाओं से 79.5 अरब डॉलर के आर्थिक नुकसान तथा अनियमित मानसून के कारण पूरे क्षेत्र अस्थिर होने के साथ, देश बढ़ते समुद्र तल, चरम मौसमी घटनाओं और कृषि व्यवधान जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। मुंबई, चेन्नई और कोच्चि जैसे तटीय शहरों के वर्ष 2040 तक आंशिक रूप से जलमग्न होने का खतरा है, जबकि सुंदरबन के मैंग्रोव वन वर्ष 2100 तक अपने 80% क्षेत्र को खो सकते हैं, जिससे जैवविविधता और प्राकृतिक आपदाओं के बफर (आपदा-रोधी तंत्र), दोनों को खतरा होगा। उत्तराखंड में हाल ही में आई बाढ़, वायनाड में भूस्खलन और हिंद महासागर में चक्रवातों का तीव्र होना कोई मौसमी दुर्भाग्य नहीं, बल्कि जलवायु संबंधी तत्काल चेतावनी है जो यह मांग करती है कि भारत सतत् विकास के लिये अधिक जलवायु-अनुकूल और समुत्थानशील दृष्टिकोण अपनाए।
भारत के सामने जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रमुख खतरे क्या हैं?
- हीट वेव और बाढ़ का बढ़ता दोहरा संकट: भारत बाढ़ के साथ-साथ लगातार बढ़ती भीषण हीट वेव से जूझ रहा है।
- अत्यधिक गर्मी की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता, विशेष रूप से उत्तरी एवं मध्य भारत में, जन स्वास्थ्य, कृषि व ऊर्जा प्रणालियों के लिये खतरा बन रही है।
- वर्ष 2030 तक मुंबई, दिल्ली और चेन्नई जैसे शहरों में हीट वेव के दिनों की संख्या दोगुनी हो जाएगी।
- दूसरी ओर, हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली जैसे उच्च तुंगता पर बसे गाँवों में बादल फटने से फ्लैश फ्लड (आकस्मिक बाढ़) आ गई।
- गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्य भीषण गर्मी एवं अत्यधिक वर्षा की दोहरी मार झेल रहे हैं तथा वर्ष 2030 तक 80% से अधिक ज़िलों के इससे प्रभावित होने का अनुमान है।
- अत्यधिक गर्मी की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता, विशेष रूप से उत्तरी एवं मध्य भारत में, जन स्वास्थ्य, कृषि व ऊर्जा प्रणालियों के लिये खतरा बन रही है।
- समुद्र-स्तर में वृद्धि और तटीय बाढ़: भारत के तटीय क्षेत्र, जहाँ लगभग 17 करोड़ लोग रहते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र-स्तर में वृद्धि के प्रति अत्यधिक सुभेद्य हैं।
- इसका बुनियादी अवसंरचना, आजीविका और जैव विविधता पर असर पड़ेगा। मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों को आसन्न खतरों का सामना करना पड़ रहा है।
- अध्ययनों के अनुसार, वर्ष 2100 तक, सबसे खराब स्थिति में, मुंबई में समुद्र का स्तर 101.4 सेमी तक बढ़ सकता है, जिससे शहर का 22% हिस्सा जलमग्न हो सकता है।
- जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिछले दो दशकों में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में 110 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव पारिस्थितिकी का ह्रास हुआ है, जिससे तटीय बाढ़ के प्रति भारत की सुभेद्यता और बढ़ गई है।
- जल संकट और भूजल का ह्रास: जलवायु परिवर्तन के कारण भारत का जल संकट गंभीर होता जा रहा है, जहाँ 60 करोड़ से अधिक लोग उच्च-से-चरम जल संकट का सामना कर रहे हैं।
- 1,700 घन मीटर (m3) की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नीचे प्रति व्यक्ति ताजे जल की वार्षिक उपलब्धता के साथ, भारत प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के मामले में विश्व में 132वें स्थान पर है। यह देश को ‘जल संकटग्रस्त’ बनाता है।
- वर्ष 1950 और 2024 के दौरान, देश में प्रति व्यक्ति सतही जल उपलब्धता में 73% की गिरावट आई है।
- भूजल का अत्यधिक दोहन इस संकट को और बढ़ा रहा है। भारत में अनुमानित भूजल ह्रास 122-199 अरब घन मीटर के बीच है।
- 1,700 घन मीटर (m3) की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नीचे प्रति व्यक्ति ताजे जल की वार्षिक उपलब्धता के साथ, भारत प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के मामले में विश्व में 132वें स्थान पर है। यह देश को ‘जल संकटग्रस्त’ बनाता है।
- बढ़ता स्वास्थ्य सेवा बोझ और वेक्टर जनित रोग: जलवायु परिवर्तन से स्वास्थ्य पर बोझ बढ़ रहा है, गर्मी से संबंधित बीमारियों और वेक्टर जनित रोगों के मामलों में वृद्धि हुई है।
- भारत में वर्ष 2000-2004 और 2017-2021 के दौरान चरम गर्मी के कारण होने वाली मौतों में 55% की वृद्धि देखी गई। भारत के 49% कार्यबल के बाहर कार्यरत होने के कारण, यह विशेष रूप से श्रमिकों और वृद्ध जनों जैसे कमज़ोर समूहों के लिये महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करता है।
- इसके अलावा, बढ़ते तापमान मच्छरों जैसे रोगवाहकों के आवास का विस्तार करते हैं, जिससे मलेरिया और डेंगू के प्रकोप बढ़ते हैं।
- भारत में वर्ष 2000-2004 और 2017-2021 के दौरान चरम गर्मी के कारण होने वाली मौतों में 55% की वृद्धि देखी गई। भारत के 49% कार्यबल के बाहर कार्यरत होने के कारण, यह विशेष रूप से श्रमिकों और वृद्ध जनों जैसे कमज़ोर समूहों के लिये महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करता है।
- जलवायु प्रेरित ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियाँ: जलवायु परिवर्तन भारत की ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दों को और जटिल बना रहा है, बढ़ते तापमान के कारण शीतलन की माँग एवं जलविद्युत उत्पादन पर दबाव पड़ रहा है।
- हालाँकि भारत के पास महत्त्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य हैं, फिर भी देश अभी भी कोयले पर बहुत अधिक निर्भर है, जो ऊर्जा उत्पादन का 70% हिस्सा है। हसदेव अरण्य जैसे पर्यावरणीय रूप से सुभेद्य क्षेत्रों सहित कोयला खनन पर ज़ोर, भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को कमज़ोर करने का खतरा उत्पन्न करता है, जिससे एक सतत् ऊर्जा भविष्य की ओर संक्रमण कठिन हो जाता है।
- कृषि में व्यवधान और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव: भारत की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण कृषि क्षेत्र, बदलते मौसम पैटर्न का खामियाज़ा भुगत रहा है।
- अनुकूलन उपायों को न अपनाए जाने की स्थिति में, भारत में वर्षा आधारित चावल की पैदावार वर्ष 2050 में 20% और गेहूँ की पैदावार 1% तक कम होने का अनुमान है।
- इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन से वर्ष 2050 और 2080 के परिदृश्यों में खरीफ मक्का की पैदावार में क्रमशः 18 और 23% की कमी आने का अनुमान है।
- अनुकूलन उपायों को न अपनाए जाने की स्थिति में, भारत में वर्षा आधारित चावल की पैदावार वर्ष 2050 में 20% और गेहूँ की पैदावार 1% तक कम होने का अनुमान है।
- जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभाव: भारत में जलवायु परिवर्तन का आर्थिक प्रभाव गहरा है, व्स्ढ़ 1998 और 2017 के दौरान अनुमानित 79.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को वर्ष 2100 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3-10% वार्षिक नुकसान हो सकता है। जलवायु अनुकूलन पर एक सुसंगत राष्ट्रीय रणनीति का अभाव इन नुकसानों को और बढ़ा देता है।
भारत के जलवायु शमन प्रयासों की प्रभावशीलता को कमज़ोर करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?
- जलवायु नीतियों का कमज़ोर क्रियान्वयन और नियामकीय कमियाँ: व्यापक जलवायु कार्यढाँचों के बावजूद, भारत की जलवायु-परिवर्तन कार्रवाई खंडित क्रियान्वयन, प्रशासन के अतिव्यापन और अपर्याप्त संसाधन वाले नियामकों द्वारा लगातार कमज़ोर होती जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप ‘नीति-व्यवहार’ में लगातार अंतर बना हुआ है।
- नवीकरणीय ऊर्जा के लिये भारत के अथक प्रयास को नवीन कोयला निवेशों और लंबे समय तक निर्भरता (विशेष रूप से बेस-लोड बिजली के लिये) के कारण कमज़ोर किया जा रहा है, जो दीर्घकालिक डीकार्बोनाइज़ेशन लक्ष्यों के विरुद्ध है।
- सरकार ने वर्ष 2032 तक 80 गीगावाट नई कोयला-आधारित क्षमता जोड़ने की योजना को मंज़ूरी दी है और कोयले के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की कोई समय-सीमा नहीं बताई है।
- इसके अलावा, वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 के संशोधनों ने वनों की कटाई के विरुद्ध विधिक सुरक्षा को कमज़ोर कर दिया है, जिससे शमन प्रयासों पर और भी अधिक असर पड़ा है।
- नवीकरणीय ऊर्जा के लिये भारत के अथक प्रयास को नवीन कोयला निवेशों और लंबे समय तक निर्भरता (विशेष रूप से बेस-लोड बिजली के लिये) के कारण कमज़ोर किया जा रहा है, जो दीर्घकालिक डीकार्बोनाइज़ेशन लक्ष्यों के विरुद्ध है।
- आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संधारणीयता के बीच असंगतता: भारत का आर्थिक विकास का लक्ष्य प्रायः जलवायु शमन उद्देश्यों से असंगत होता है। औद्योगीकरण और बुनियादी अवसंरचना के विकास पर सरकार का ध्यान कभी-कभी ऐसी नीतियों की ओर ले जाता है जो पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को कमज़ोर करती हैं।
- उदाहरण के लिये, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को वर्ष 2024 में अपर्याप्त जन सुनवाई और जैवविविधता जोखिमों की रिपोर्टों के बीच मंज़ूरी दी गई, जो EIA प्रक्रिया में प्रणालीगत खामियों को दर्शाती है।
- यह दृष्टिकोण विकासात्मक हितों को जलवायु-परिवर्तन कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता के विरुद्ध खड़ा करता है, जिससे सतत् विकास पर चिंताएँ बढ़ती हैं।
- ग्रीन क्रेडिट स्कीम में ग्रीनवाशिंग के जोखिम: भारत का ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और कार्बन क्रेडिट योजनाएँ, हालाँकि नवीन हैं, पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता के मामले में चुनौतियों का सामना करती हैं।
- ग्रीनवाशिंग का जोखिम, जहाँ कंपनियाँ पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने का झूठा दावा करती हैं, अभी भी उच्च बना हुआ है।
- इसके अलावा, जहाँ सरकार का वनीकरण और वृक्षारोपण पर ध्यान कार्बन सिंक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है, वहीं हालिया रिपोर्टों में पाया गया है कि अधिकांश वन आवरण वृद्धि गैर-वन क्षेत्रों में हुई है, जिससे ऐसी पहलों के वास्तविक पर्यावरणीय प्रभाव पर संदेह उत्पन्न होता है।
- शहरी जलवायु अनुकूलन पर अपर्याप्त ध्यान: भारत के शहरी क्षेत्र, जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों का सामना करने के लिये समुत्थानशीलता का अभाव है।
- सरकार का स्मार्ट सिटी मिशन, महत्त्वाकांक्षी होने के बावजूद, सतत् शहरी नियोजन को पूरी तरह से एकीकृत करने में विफल रहने के लिये आलोचना का शिकार रहा है।
- भारतीय शहर नगरीय ऊष्मा द्वीप, जल की कमी और खराब वायु गुणवत्ता से ग्रस्त हैं तथा शहरीकरण इन कमज़ोरियों को और बढ़ा देता है।
- कुछ प्रगति के बावजूद, विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 6 भारत में हैं, जो अधिक आक्रामक शहरी जलवायु रणनीतियों की आवश्यकता को दर्शाता है।
- जलवायु अनुकूलन का कम मूल्यांकन: जहाँ शमन पर मुख्य ध्यान दिया जाता है, वहीं विशेष रूप से सुभेद्य कृषि और जल-तनावग्रस्त समुदायों के लिये अनुकूलन एवं समुत्थानशक्ति-निर्माण उपायों को कम प्राथमिकता दी जाती है तथा उन्हें पर्याप्त धन नहीं मिलता है।
- अनुकूलन व्यय, हालाँकि वित्त वर्ष 2016 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 5.6% हो गया है, वास्तविक ज़रूरतों (विशेष रूप से कृषि एवं ग्रामीण बुनियादी अवसंरचना के लिये) से काफी कम है।
- नवंबर 2022 में, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC) को बिना कोई कारण बताए या यह बताए बिना कि क्या कोष के उद्देश्य पूरे हुए हैं, एक ‘गैर-योजना’ में बदल दिया गया (डाउन टू अर्थ)।
- आलोचकों का कहना है कि अनुकूलन की तत्काल आवश्यकता के बावजूद, हाल के वर्षों में NAFCC की सक्रिय भूमिका कम हो गई है।
- नवंबर 2022 में, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC) को बिना कोई कारण बताए या यह बताए बिना कि क्या कोष के उद्देश्य पूरे हुए हैं, एक ‘गैर-योजना’ में बदल दिया गया (डाउन टू अर्थ)।
- अनुमान है कि भारत को जलवायु परिवर्तन अनुपालन मानकों को पूरा करने के लिये अपने उद्योगों को अनुकूलित करने हेतु वर्ष 2030 तक लगभग 85.6 ट्रिलियन रुपए (1.05 ट्रिलियन डॉलर) की आवश्यकता होगी।
- अनुकूलन व्यय, हालाँकि वित्त वर्ष 2016 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 5.6% हो गया है, वास्तविक ज़रूरतों (विशेष रूप से कृषि एवं ग्रामीण बुनियादी अवसंरचना के लिये) से काफी कम है।
जलवायु-अनुकूलन और समुत्थानशीलता बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?
- स्थानीयकृत जलवायु जोखिम मानचित्रण और सूक्ष्म-क्षेत्रीकरण: भारत को GIS, उपग्रह डेटा और AI का उपयोग करके ज़िला व उप-ज़िला स्तर पर हाई-रिज़ॉल्यूशन जलवायु भेद्यता मानचित्रण में निवेश करना चाहिये।
- हीटवेव, बाढ़ और सूखे के जोखिम के आधार पर क्षेत्रों का सूक्ष्म-क्षेत्रीकरण लक्षित हस्तक्षेपों को सक्षम करेगा।
- यह विस्तृत दृष्टिकोण राज्य कार्य योजनाओं के तहत विकेंद्रीकृत जलवायु-परिवर्तन हेतु नियोजन को मज़बूत करता है।
- आपदा मोचन कार्यढाँचों के साथ एकीकरण समुदाय-स्तरीय समुत्थानशीलता बढ़ाता है। यह प्रतिक्रियाशील मोचन कार्य की तुलना में सक्रिय, स्थान-विशिष्ट अनुकूलन को बढ़ावा देता है।
- जलवायु-प्रतिक्रियाशील शहरी डिज़ाइन: शहरी स्थानीय निकायों को प्रकृति-आधारित समाधान, पारगम्य सतहों और नीले-हरे बुनियादी अवसंरचना जैसे सिद्धांतों का उपयोग करके जलवायु-एकीकृत मास्टर प्लान अपनाना चाहिये।
- नगरीय ऊष्मा द्वीप शमन तकनीकों, जैसे परावर्तक सामग्री और ऊर्ध्वाधर उद्यानों के साथ शहरों का पुनर्निर्माण, भेद्यता को काफी कम कर सकता है। कम आय वाली बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये, जो प्रायः सबसे अधिक प्रभावित होती हैं।
- भवन संहिताओं और ज़ोनिंग कानूनों में समुत्थानशीलता मानकों को शामिल करने से दीर्घकालिक अनुकूलन सुनिश्चित होगा। यह सतत् शहरों पर SDG11 के अनुरूप है।
- कृषि-पारिस्थितिक संक्रमण क्षेत्र: पुनर्योजी, जलवायु-अनुकूल कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिये संवेदनशील कृषि-जलवायु क्षेत्रों में कृषि-पारिस्थितिक गलियारे स्थापित किये जाने चाहिये। वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि वानिकी, कदन्न-आधारित प्रणालियों एवं मृदा-कार्बन संवर्द्धन को अपनाने से खाद्य सुरक्षा व जलवायु बफर में सुधार होता है।
- ये क्षेत्र अनियमित मानसून और मरुस्थलीकरण के विरुद्ध समुत्थानशील बफर के रूप में कार्य करते हैं। MGNREGA और कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ अभिसरण परिचालन मापनीयता सुनिश्चित करता है। यह आजीविका विविधीकरण का भी समर्थन करता है।
- जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसंरचना ऑडिट: जलवायु-अनुकूल क्षेत्रों में सभी प्रमुख सार्वजनिक बुनियादी अवसंरचना— सड़कों, बिजली लाइनों, रेलवे के लिये अनिवार्य समुत्थानशीलता ऑडिट को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिये।
- जोखिम-आधारित इंजीनियरिंग मानदंडों का उपयोग करके, ये ऑडिट बाढ़, चक्रवातों और तापमान तनाव के जोखिम की पहचान कर उसे कम कर सकते हैं।
- पर्यावरणीय मंज़ूरी तंत्र में इस तरह के ऑडिट को शामिल करने से निवारक क्षमता में वृद्धि होती है। जलवायु-रोधी बुनियादी अवसंरचना के लिये PPP मॉडल का लाभ उठाने से वित्तपोषण में तेज़ी आ सकती है। इससे महत्त्वपूर्ण परिसंपत्तियों का जीवनचक्र समुत्थानशीलता सुनिश्चित होती है।
- विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा क्लस्टर: आपदा-प्रवण और दूरस्थ क्षेत्रों में सतत् ऊर्जा अभिगम सुनिश्चित करने के लिये हाइब्रिड सौर-पवन-जैव प्रणालियों का उपयोग करके समुदाय-प्रबंधित नवीकरणीय ऊर्जा क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- ये प्रणालियाँ व्यवधान के प्रति संवेदनशील केंद्रीकृत ग्रिडों पर निर्भरता कम करती हैं। ऊर्जा सहकारी समितियों के माध्यम से तैनाती स्थानीय शासन और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाती है।
- शीत भंडारण और सिंचाई के साथ संयोजन कृषि में अनुकूलन क्षमता को बढ़ाता है। यह जलवायु-रोधी ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- जल-जलवायु पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ: फ्लैश फ्लड, हिमनद झीलों के विस्फोट और सूखे के लिये पूर्वानुमान विश्लेषण के साथ वास्तविक काल जल-जलवायु चेतावनी प्रणालियों का विस्तार किया जाना चाहिये।
- डिजिटल पूर्वानुमान मॉडलों के साथ स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों का एकीकरण सामुदायिक जवाबदेही को बढ़ाता है।
- राज्य आपदा प्राधिकरणों को मोबाइल अलर्ट, सायरन और सामुदायिक रेडियो के माध्यम से अंतिम-बिंदु संचार स्थापित करना चाहिये। यह सक्रिय जोखिम संचार निष्क्रिय पीड़ितों को सक्रिय प्रतिभागियों में बदल देता है। यह ज़मीनी स्तर पर समुत्थानशीलता को क्रियान्वित करता है।
- एकीकृत तटीय बफर ज़ोन: बहु-कार्यात्मक तटीय बफर बेल्ट को एक स्तरित दृष्टिकोण: मैंग्रोव पुनर्स्थापन, बायोशील्ड, इको-टूरिज्म ज़ोन और लचीले आवास, के साथ विकसित किया जाना चाहिये।
- ज़ोनिंग में मछुआरों और सुभेद्य समुदायों के लिये आजीविका सुरक्षा उपायों को एकीकृत करना चाहिये।
- उपग्रह निगरानी और LIDAR मानचित्रण का उपयोग गतिशील तटीय विनियमन को सक्षम बनाता है। इस रणनीति को स्पष्ट प्रवर्तनीयता के साथ CRZ दिशानिर्देशों में अंतर्निहित किया जाना चाहिये। यह पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक समुत्थानशीलता दोनों को बढ़ाता है।
- जलवायु-संबंधी कौशल विकास मिशन: युवाओं को सौर मरम्मत, जल संचयन, पर्यावरण-निर्माण और जैवविविधता निगरानी जैसे जलवायु-अनुकूल क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने के लिये एक राष्ट्रीय हरित अनुकूलन कौशल मिशन शुरू किया जाना चाहिये।
- जलवायु-सुभेद्य क्षेत्रों को कौशल से जोड़ने से रोज़गार और समुत्थानशीलता दोनों सुनिश्चित होते हैं। ITI और PMKVY जैसे कौशल मंचों में PMKVY पर मॉड्यूल शामिल किये जाने चाहिये। इससे जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिये तैयार भविष्य के लिये तैयार कार्यबल का निर्माण होता है। यह अनुकूली मानव पूंजी का निर्माण करता है।
- विकेंद्रीकृत जलभृत शासन के माध्यम से जल सुरक्षा: जल-भूविज्ञान मानचित्रण पर आधारित जलभृत-स्तरीय प्रबंधन योजनाओं के साथ ग्राम-स्तरीय जल उपयोगकर्त्ता संघों को सशक्त बनाया जाना चाहिये।
- समुदाय-संचालित प्रबंधित जलभृत पुनर्भरण (MAR), स्थानीय वर्षा जल संचयन और जल बजट को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। जल शक्ति अभियान और अटल भूजल योजना के साथ एकीकरण अभिसरण सुनिश्चित कर सकता है। यह कृषि और पेयजल को बनाए रखने वाले समुत्थानशील भूजल पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाता है। यह जल-सामाजिक अनुबंधों में समुत्थानशीलता को आधार प्रदान करता है।
- हरित वित्त और जलवायु निवेश के लिये नीतिगत समर्थन: भारत को कर छूट, ग्रीन बॉण्ड और जलवायु बीमा जैसे वित्तीय साधनों के माध्यम से निम्न-कार्बन, जलवायु-अनुकूल परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करके हरित वित्त के संचालन में तेज़ी लानी चाहिये।
- अनुकूलन और समुत्थानशीलता-निर्माण गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु एक सुदृढ़ कार्यढाँचा विकसित करने से व्यवसायों एवं सरकारों को स्थायी समाधानों में निवेश करने का अधिकार मिलेगा। जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिये एक अनुकूल नीतिगत वातावरण बनाने से वित्तपोषण की कमी को पूरा किया जा सकता है।
- जलवायु शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना: भारत को ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक, समाज के सभी स्तरों पर जलवायु शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों को प्राथमिकता देनी चाहिये, ताकि व्यक्तियों को जलवायु-अनुकूल कार्रवाई करने के लिये ज्ञान से सशक्त बनाया जा सके।
- इसमें स्कूली पाठ्यक्रम में जलवायु परिवर्तन को शामिल करना, सामुदायिक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना और स्थानीय नेताओं एवं नीति निर्माताओं के लिये क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करना शामिल है।
- सामूहिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने और जलवायु-अनुकूल प्रथाओं को व्यापक रूप से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिये एक सुविज्ञ जनता महत्त्वपूर्ण है।
निष्कर्ष:
भारत को अपने विकास पथ को सुरक्षित रखने के लिये जलवायु-अनुकूलन को राष्ट्रीय योजना का एक केंद्रीय आधार बनाने की आवश्यकता है, जिससे पंचामृत लक्ष्यों तथा सतत् विकास लक्ष्यों— SDG2, SDG6, SDG11, SDG13, SDG15 और SDG16 के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके। आपदा के प्रति प्रतिक्रियात्मक रवैये के बजाय अब पूर्वानुमान आधारित और प्रणालीगत अनुकूलन की ओर परिवर्तन आवश्यक है। यदि भारत एकीकृत, समावेशी और नवाचार-आधारित रणनीतियों को अपनाता है, तो यह जलवायु जोखिमों को समुत्थानशीलता में परिवर्तित कर सकता है। ‘जलवायु-स्मार्ट भारत’ का निर्माण केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि सतत् और समतामूलक विकास के लिये एक रणनीतिक अनिवार्यता है।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. “भारत की जलवायु संबंधी सुभेद्यता अब एक दूरगामी पर्यावरणीय चिंता नहीं, बल्कि एक वर्तमान विकासात्मक आपात स्थिति है।” इस संदर्भ में, भारत की जलवायु अनुकूलन रणनीति में प्रमुख संरचनात्मक चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रति समुत्थानशीलता को सुदृढ़ करने के लिये एक बहु-स्तरीय कार्यढाँचे का सुझाव दीजिये। |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs)प्रिलिम्सप्रश्न 1. जलवायु-अनुकूल कृषि (क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये- (2021)
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) प्रश्न 2. 'भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि (ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एलायंस)' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न 1. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं ? (2021) प्रश्न 2. 'जलवायु परिवर्तन' एक वैश्विक समस्या है। भारत जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होगा ? जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत के हिमालयी और समुद्रतटीय राज्य किस प्रकार प्रभावित होंगे ? (2017) |