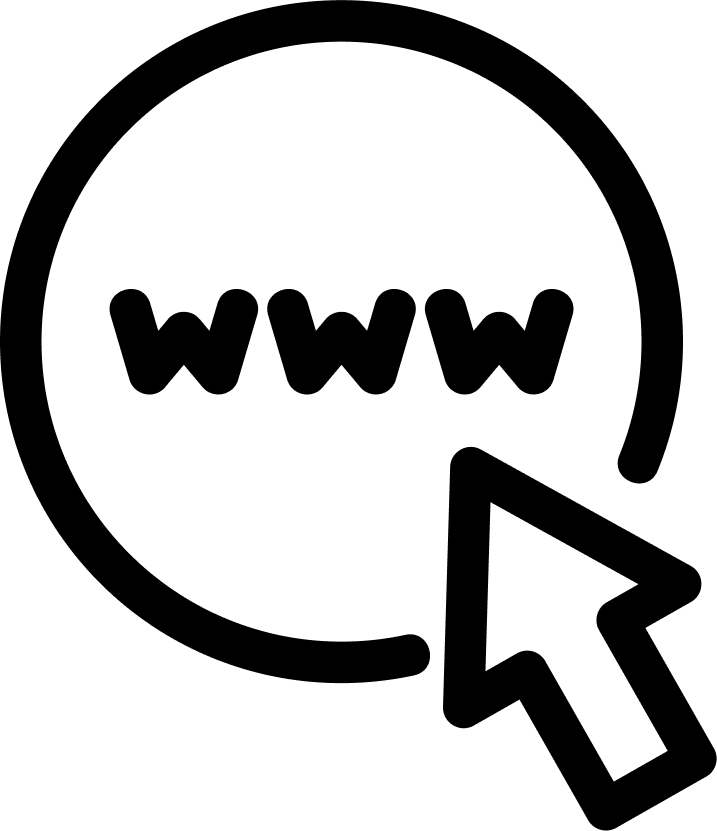भारतीय सिनेमा में साहित्य की उपयोगिता
- 25 Jul, 2023 | नेहा चौधरी

भारतीय सिनेमा और हिन्दी साहित्य दो परस्पर अलग-अलग विधाएँ हैं किंतु दोनों में पारस्परिक संबंध काफी गहरा है। अपनी शैशवावस्था से ही भारतीय सिनेमा भाषा के लिहाज से हिन्दी पर निर्भर रही है। ऐसा इसलिये भी है क्योंकि एक तरफ जहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये अधिकतर कांग्रेसी नेता हिन्दी को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प मान कर इसके जन भाषा के रूप में विकास पर बल दे रहे थे तो दूसरी तरफ साहित्यिक हिन्दी उस समय तक इतनी विकसित हो चुकी थी कि 'गीतांजलि' के लिये नोबेल प्राप्त कर रही थी जबकि इसी समय दादा साहेब फाल्के हिन्दी सिनेमा की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र को पर्दे पर ला रहे थे। हिन्दी की जन भाषा के रूप में बढ़ते रुझान को देखते हुए ही जब आलमआरा बनाई गई होगी तो भाषा के किसी दूसरे विकल्प पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया होगा। एक तथ्य यह भी है कि हिन्दी सिनेमा विश्व स्तर पर भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करती है।
एक-दूसरे से संबंधों की यह शुरुआत साहित्य के कथानक को अपनाने तक तब पहुँची जब आलमआरा के केवल दो ही वर्षों बाद, उस समय तक हिन्दी साहित्य के आसमान में चमकते सितारे के रूप में स्थापित, प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी द्वारा 'मिल मज़दूर' बनाई गई। लेकिन फिल्म के रूप में प्रदर्शित करने हेतु जब कहानी में काफी काट-छाँट करना पड़ा तो प्रेमचंद ने दुखी होकर कहा, "मज़दूर में मैं इतना ज़रा सा आया हूँ कि नहीं के बराबर। फिल्म में डायरेक्टर ही सबकुछ है’। यह साहित्य और सिनेमा के साथ आने की पहली कोशिश थी लेकिन इसमें सफलता हासिल नहीं हुई। 1934 में प्रेमचंद की ही कृतियों पर 'नवजीवन' और 'सेवासदन' बनी। लेकिन जहाँ कहानी और उपन्यास के रूप में दोनों खूब प्रसिद्ध हुई वहीं सिनेमा के रूप में दोनों फ्लॉप हो गईं। आगे 1941 में 'त्रियाचरित्र' पर 'स्वामी' और 'रंगभूमि' पर इसी नाम से आई फिल्मों की भी कमोवेश यही स्थिति रही। इसके बाद हिन्दी साहित्य के कई लेखक फिल्मों में हाथ आजमाने पहुँचे लेकिन ज्यादातर को दर्शकों की सराहना नहीं मिली।
पुस्तकों को फिल्मों में सफलता मिलने का क्रम 1941 में आई भगवतीचरण वर्मा की 'चित्रलेखा' पर आधारित फिल्म से शुरू हुआ किंतु कतिपय कारणों से यह सफलता लंबे समय तक जारी नहीं रह पाई। हालाँकि फणीश्वर नाथ 'रेणु' की कहानी "मारे गए गुलफाम" पर बी आर चोपड़ा द्वारा बनाई गई फिल्म 'तीसरी कसम' को फिल्मी दुनिया में काफी सराहना मिली और आर्ट फिल्मों में एक अलग जगह प्राप्त हुआ लेकिन कमाई के मामले में इसे असफलता का सामना करना पड़ा।
लेकिन इसका यह अर्थ नहीं था कि हिन्दी कहानियाँ या उपन्यास में फिल्म बनने के गुण नहीं मौजूद थे बल्कि, यह कहना अधिक सही होगा कि इसकी वजह कहीं-न-कहीं साहित्य का श्रेष्ठताबोध और फिल्मी दुनिया की सीमाएँ भी रही। जैसे, निर्देशन कौशल, क्योंकि प्रेमचंद की ही कहानी शतरंज की खिलाड़ी पर जब सत्यजीत रे ने फिल्म बनाया तो वो सफल रहा। इसके अलावा तकनीक कौशल की कमी, कहानी के भिन्न आयामों को केवल दो से ढाई घंटे में समेटने में असमर्थता, अभिनेताओं की अक्षमता, वित्त की कमी इत्यादि। यह एक कटु सत्य है कि फिल्म कैसी बनेगी, उसका संदेश जनता में क्या जाएगा ये फैसला वो लोग लेते हैं जो फिल्म में पैसा लगा रहे होते हैं और हिन्दी बिरादरी से उस समय तक ऐसे लोग कम ही हुए थे जो इस दिशा में आगे आएँ यह भी एक वजह रही हिन्दी कहानियों की पर्दे पर असफल रहने की।
इसके अलावा साहित्य लेखन व पठन-पाठन से जुड़ी विधा है जबकी फिल्म में दृश्य महत्त्वपूर्ण है। कई बार पर्दे पर किये गए अभिनय के ज़रिये दर्शकों तक ठीक-ठीक भाव नहीं पहुँच पाते हैं। साथ ही मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में
"केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिये,
उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिये"
साहित्य जहाँकेवल मनोरंजन हेतु नहीं बल्कि एक बृहत उद्देश्य के लिये लिखी जाती है वहीं फिल्म अधिकतर जनता के मनोरंजन के लिये बनते हैं जहाँ बहुत गूढ़ बातों के लिये दर्शक कम ही मिलते हैं। और तो और 35-40 वर्ष पहले तक की बात करें तो थियेटर में नाटक देखना या नाट्य में रामलीला वगैरह देखना तो फिर भी मान्य था लेकिन मध्यवर्गीय परिवारों में सिनेमाघर में जाकर सिनेमा देखने का अर्थ था कि "लड़का हाथ से निकल गया"। क्योंकि फिल्मों को तब तक बहुत हद तक 'बाज़ारू' माना जाता था जहाँ 'बाज़ारू' का अर्थ मनोरंजन के निम्न स्तर से है। तो हिन्दी सिनेमा को मध्यवर्गीय सभ्य परिवारों में इन्हीं कुछ तीन दशकों से मान्यता मिली है।
यह भी सत्य है कि फिल्मों की एक सीमा है-बाज़ार से प्रभावित होना एवं बाज़ार को प्रभावित करना। यह बाज़ार से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य बाज़ार से फिल्म बनने का मूल्य एवं अत्यधिक लाभ हासिल करना है जबकि, साहित्य का मुख्य उद्देश्य जनता की बेहतरी है। फिल्में यदि बाज़ार से लाभ नहीं कमा पाती हैं तो आगे अगली फिल्म का निर्माण बाधित होगा। हालाँकि आजकल पुस्तकों की अधिक बिक्री पर भी लेखकों एवं प्रकाशकों द्वारा जोर दिया जा रहा है जो कि अच्छी बात है फिर भी अभी लेखन में यह स्थिति नहीं आई है कि यदि अच्छा लाभ न मिले तो लेखक आगे लिखेगा ही नहीं। इसका एक कारण यह हो सकता है कि लेखन एक व्यक्तिगत कर्म है जो 'स्वांत सुखाय' के लिये होता है जबकि फिल्म बनाने का प्राथमिक उद्देश्य जनता का मनोरंजन कर लाभ कमाना होता है। फिल्मों से जुड़ी इस तरह की सीमाएँ जब कम होने लगती है तो स्वतः ही साहित्य एवं सिनेमा एक दिशा में आने लगता है। इसका उदाहरण हम सत्तर के दशक एवं उसके बाद बनने वाली फिल्मों जैसे मन्नू भंडारी की कहानी 'यही सच है' पर बनी फिल्म 'रजनीगंधा', शरतचंद्र चटर्जी की 'देवदास' पर इसी नाम से बनी फिल्म है।
वर्तमान दौर की बात करें तो एक तरफ बीते सौ-सवा सौ वर्षों में सिनेमा में जहाँ दर्शकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए, समाज की प्रमुख समस्याओं पर फिल्में बनी हैं जैसे, समलैंगिकों पर 'शुभ मंगल सावधान' और 'अलीगढ़'; धर्म को लेकर पाखंड पर सिर्फ एक बंदा काफी है' इत्यादि, वहीं सिनेमा ने समय के साथ खुद को विषयवस्तु से लेकर प्रस्तुति-विधान तक निरंतर अपडेट किया, जबकि साहित्य अपनी कथित महानता के दंभ में अपनी स्वर्णिम आभा को बैठा है। जिस कारण जहाँ सिनेमा के दर्शकों में निरंतर विस्तार हुआ तो साहित्य के पाठक सिमटते गए जो आज हिन्दी प्रकाशकों की एक बड़ी समस्या है। हालाँकि आजकल एक बार फिर हम फिल्म में हिन्दी साहित्यकारों के सफल प्रवेश को देख सकते हैं। एक तरफ मणी रत्नम ने 'पोन्नियिन सेल्वन' पुस्तक से इसी नाम की फिल्म का दो भाग बनाया और दोनों ने ही बॉक्स ऑफिस पर सफल कमाई की। इसी पोन्नियिन सेल्वन का संवाद 'नई वाली हिन्दी' के लेखक दिव्य प्रकाश दुबे ने लिखा है तो दूसरी तरफ सत्य व्यास की लघु उपन्यास 'चौरासी' पर "ग्रहण" नाम की सीरीज़ तो निखिल सचान की "यूपी 65" पर इसी नाम से सीरीज़ आ चुकी है।
अतः हम कह सकते हैं कि सिनेमा अगर साहित्य की अँगुली पकड़ चले तो न केवल मनोरंजन बल्कि समाज की ज़रूरतों, समस्याओं व विशेषताओं को भी वैश्विक जनता तक पहुँचा सकती है एवं साहित्य यदि सिनेमा हेतु स्वयं को जरा लचीला बनाए तो इसकी बात सीमित क्षेत्र में न रहकर एक बड़े वर्ग तक जा सकती है। इस तरह "जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब" साहित्य तथा "समाज का दर्पण" सिनेमा दोनों अपनी-अपनी सीमाओं का विस्तार कर एक साथ आगे बढ़ने हेतु तैयार होंगे।
 |
नेहा चौधरीनेहा चौधरी, बिहार के मुंगेर ज़िले से हैं। इन्होंने बिज़नेस स्टडीज़ से स्नातक एवं हिंदी से स्नातकोत्तर करने के बाद "दृष्टि आईएएस" के साथ 4 साल से अधिक समय तक कार्य किया। फिलहाल विभिन्न प्लेटफॉर्म से जुड़कर स्वतंत्र रूप से कंटेंट लेखन का कार्य करती हैं। विश्व स्तर पर चल रहे विभिन्न मुद्दों के साथ नारी अधिकारितावाद के लिए मुखर हैं। विश्व-साहित्य एवं मनोविज्ञान में रुचि रखती हैं। |