ऊर्जा की राजनीति: विभाजित विश्व में स्थिर भविष्य की खोज
- 24 Nov, 2025
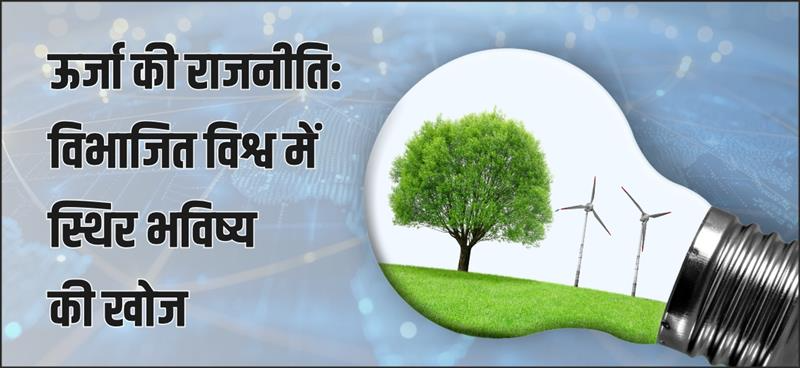
ऊर्जा का महत्त्व केवल तकनीकी या आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी केंद्र बन गया है। ऊर्जा संसाधन, चाहे वह जीवाश्म ईंधन जैसे तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला हों या नवीकरणीय स्रोत जैसे सौर एवं पवन ऊर्जा, हों वे अब किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता, सुरक्षा रणनीतियों तथा पर्यावरणीय नीतियों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसका कारण यह है कि ऊर्जा केवल आर्थिक या भौतिक संसाधन नहीं है, बल्कि यह शक्ति, नियंत्रण और नैतिकता का प्रतीक भी है। फ्रेंकफर्ट विचारकों के अनुसार, ऊर्जा उत्पादन और वितरण पर सामुदायिक नियंत्रण शोषण को कम कर सकता है एवं समानता बढ़ा सकता है। वहीं मिशेल फूको के दृष्टिकोण से यह शक्ति और असमानता के नए जाल को जन्म दे सकता है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, नवीकरणीय ऊर्जा मानवता को आर्थिक और पर्यावरणीय स्वतंत्रता प्रदान कर सकती है तथा इसके लिये वैश्विक सहयोग, नीति समर्थन एवं समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यदि नियंत्रण असमान रूप से हो, तो यह नई प्रकार की दासता और निर्भरता भी उत्पन्न कर सकती है। यह स्पष्ट करता है कि ऊर्जा न केवल मुक्ति का स्रोत हो सकती है, बल्कि यदि नियंत्रण असमान रूप से हो तो नई दासता का कारण भी बन सकती है।
वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य तेज़ी से परिवर्तनशील स्थिति में है। इसमें जीवाश्म ईंधन अभी भी अधिकांश देशों की ऊर्जा ज़रूरतों का मुख्य आधार हैं, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार अभूतपूर्व गति से हो रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा का उदय भू-राजनीतिक संतुलन को बदल रहा है और नए गठबंधनों, प्रतिस्पर्द्धाओं एवं साझेदारियों को उत्पन्न कर रहा है। भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र पर भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ, नीतिगत परिवर्तन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी नई तकनीकों का गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस स्थिति में स्वच्छ ऊर्जा निवेश, ऊर्जा दक्षता और बैटरी भंडारण तकनीक में तेज़ प्रगति अत्यंत आवश्यक है। सतत् और समावेशी ऊर्जा संक्रमण ही आने वाले दशकों में आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता एवं वैश्विक सहयोग की आधारशिला बनेगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक जीवाश्म ईंधन वैश्विक ऊर्जा मिश्रण का 41–55 प्रतिशत हिस्सा बनाए रखेंगे, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा 61–67 प्रतिशत तक हो सकती है। यह स्पष्ट करता है कि ऊर्जा संक्रमण की सफलता केवल तकनीकी और आर्थिक दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि भू-राजनीतिक एवं वैश्विक सहयोग पर भी निर्भर होगी। ऊर्जा सुरक्षा और उत्सर्जन में कमी दोनों ही महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि ऊर्जा, राजनीति वैश्विक शक्ति संतुलन और आर्थिक स्थिरता को परिभाषित करती है। दरअसल स्वच्छ ऊर्जा अब केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं रह गई है, बल्कि यह नए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों, वैश्विक निवेश और आर्थिक रणनीतियों का आधार बन रही है। भविष्य में, नवीकरणीय ऊर्जा न केवल पर्यावरणीय स्थिरता के लिये आवश्यक होगी, बल्कि भू-राजनीतिक और आर्थिक रणनीतियों में भी इसका केंद्र भूमिका होगी।
अगर हम ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की बात करें तो पता चलता है कि वैश्विक ऊर्जा निवेश वर्ष 2025 में लगभग 3.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गया है और इसमें स्वच्छ ऊर्जा में 2.2 ट्रिलियन डॉलर का निवेश हुआ, जबकि जीवाश्म ईंधन में 1.1 ट्रिलियन डॉलर खर्च किये गए। चीन ने वर्ष 2024 में अमेरिका, यूरोप और भारत की तुलना में दोगुनी नवीकरणीय क्षमता जोड़कर इस क्षेत्र में भी अपने वैश्विक को नेतृत्व बनाए रखा। परमाणु ऊर्जा में भी 70 अरब डॉलर से अधिक निवेश हुआ है। ये निवेश खासकर फ्राँस और जापान में किया गया। चीन के पास महत्त्वपूर्ण खनिजों एवं तकनीकी उपकरणों पर नियंत्रण है एवं यह वैश्विक नवीकरणीय उत्पादन शृंखला में प्रभाव डालता है। भारत और ब्राज़ील नवीकरणीय ऊर्जा में तेज़ी से निवेश बढ़ा रहे हैं, जिससे उनकी ऊर्जा स्वतंत्रता एवं वैश्विक भूमिका सशक्त बन रही है। अफ्रीका जैसे विकासशील क्षेत्र निवेश की कमी के कारण पिछड़ रहे हैं, जबकि वैश्विक सहयोग और तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से इन्हें समर्थ बनाना आवश्यक है।
वर्ष 2024 में विश्व की कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दो प्रतिशत अधिक रही है। बिजली की मांग में चार प्रतिशत से अधिक की वृद्धि मापी गई, जिसका मुख्य कारण इलेक्ट्रिफिकेशन, डेटा सेंटरों की बढ़ती संख्या, अत्यधिक तापमान और इमारतों में बिजली उपयोग रहा है। सौर और पवन ऊर्जा में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, इस क्षेत्र में तकनीकी नवाचार जैसे पेरोव्स्काइट सौर सेल, ग्रीन हाइड्रोजन एवं उन्नत बैटरी स्टोरेज ने उत्पादन क्षमता तथा दक्षता में महत्त्वपूर्ण सुधार किया है। अगले पाँच सालों यानी वर्ष 2025 से 2030 के बीच वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 5,500 गीगावाट की वृद्धि होने की उम्मीद है। यह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की कुल बिजली उत्पादन क्षमता के समकक्ष है। साल 2024 में ही स्वच्छ ऊर्जा ने वैश्विक बिजली उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा हासिल कर लिया था और वर्ष 2030 तक यह उत्पादन 17,000 टेरावाट ऑवर तक पहुँच सकता है, जो वर्ष 2023 की तुलना में 90 प्रतिशत अधिक है। इस तेज़ी के पीछे लागत में गिरावट भी प्रमुख भूमिका निभा रही है, क्योंकि 90 प्रतिशत से अधिक नए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ अब जीवाश्म ईंधन से सस्ते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक नवीकरणीय ऊर्जा बिजली उत्पादन का 50 प्रतिशत और कुल ऊर्जा मिश्रण का 61–67 प्रतिशत तक हिस्सा ले सकती है, जबकि जीवाश्म ईंधन 41–55 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखेंगे। वैश्विक स्तर पर बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। साल 2030 तक यह मांग दोगुनी होकर 945 टेरा वॉट घंटा तक पहुँच सकती है, जिससे नवीकरणीय स्रोतों की आवश्यकता और बढ़ जाएगी। इसका एक बड़ा कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटरों की संख्या में नियमित वृद्धि़ को माना जाता है। कुल मिलाकर, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वर्ष 2030 तक 84 प्रतिशत बढ़ सकता है और वर्ष 2050 तक दोगुना हो सकता है, लेकिन वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने के लिये एवं नवीकरणीय उपायों को तेज़ी से अपनाने की आवश्यकता होगी।
ऊर्जा के क्षेत्र के मुख्य वैश्विक खिलाड़ी जैसे अमेरिका, चीन, रूस, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ, ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार एवं संक्रमण पर नियंत्रण के लिये प्रतिद्वंद्विता कर रहे हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध ने तेल और गैस के प्रवाह को प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप रूस ने अपने तेल निर्यात को छूट पर चीन, भारत एवं तुर्की की ओर मोड़ा। वहीं, अमेरिका तरलीकृत प्राकृतिक गैस या एलएनजी का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया, जिससे उसकी वैश्विक ऊर्जा भूमिका का विस्तार हुआ है। अमेरिका में पवन क्षमता लगातार बढ़ रही है और यूरोप ऊर्जा सुरक्षा के लिये नवीकरणीय ऊर्जा एवं दक्षता पर ज़ोर दे रहा है। मध्य पूर्व में ईरान और इज़रायल के बीच तनाव वर्ष 2025 में बढ़ा, लेकिन संघर्ष विराम एवं कूटनीतिक प्रयासों के कारण तेल की कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर रहीं। ओपेक विस्तारित समूह ने जुलाई 2025 में उत्पादन समायोजन किया और संकेत दिया कि बाज़ार में अतिरिक्त बैरल जारी किये जाएंगे, जिससे वैश्विक आपूर्ति पर असर पड़ा। इस तरह, भू-राजनीति और ऊर्जा आपूर्ति आपस में जुड़कर वैश्विक बाज़ार की कीमतों एवं सुरक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं।
यह अनुमान लगाया गया है कि क्षेत्रीय दृष्टि से चीन नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी रहेगा। वह विशेषकर सौर पैनल, बैटरी और इलेक्ट्रोलाइज़र के उत्पादन में अपनी अग्रज भूमिका में बना रहेगा, जबकि भारत इस क्षेत्र में तेज़ी से उभरता हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। भारत ने वर्ष 2030 के 40 प्रतिशत नवीकरणीय लक्ष्य को समय से पहले पूरा कर लिया है और अब ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण में निवेश बढ़ा रहा है। भारत और अन्य विकासशील देशों में भी बिजली मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है। देश की तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या और उच्च आर्थिक विकास दर के कारण ऊर्जा खपत में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2025 में भारत की जनसंख्या 1.4 अरब से अधिक होने का अनुमान है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, भारत वैश्विक ऊर्जा मांग वृद्धि का प्रमुख स्रोत बन चुका है, हालाँकि आयात पर निर्भरता भारत के लिये सुरक्षा चुनौती बनी हुई है। साल 2023–24 में भारत की तेल आयात निर्भरता 89 प्रतिशत, प्राकृतिक गैस 46.6 प्रतिशत और कोयला 25.86 प्रतिशत थी, जबकि वर्ष 2024–25 में कोयले की आयात निर्भरता घटकर 19.6 प्रतिशत हो गई। ग्राउंड माउंटेड सौर क्षमता 97.15 गीगावॉट और रूफटॉप सौर 21.52 गीगावॉट तक पहुँच गई है। वर्ष 2025 की पहली छमाही में 22 गीगावॉट नई नवीकरणीय क्षमता जोड़ी गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 57 प्रतिशत अधिक है। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिये कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन और परमाणु ऊर्जा में निवेश भी तेज़ हुआ है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 17.24 लाख घरों को लाभ मिला और लगभग 9,842 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य रखा है, जिसके लिये अनुमानित निवेश 21 ट्रिलियन डॉलर है।
कुल मिलाकर, भारत और दुनिया दोनों के लिये नवीकरणीय ऊर्जा ही आने वाले दशकों में सतत् विकास, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक प्रगति की कुंजी है। हाल के सुधार, जैसे भारत का स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य समय से पहले हासिल करना, यह दिखाते हैं कि समग्र दृष्टिकोण, निवेश और नीति समर्थन के माध्यम से ऊर्जा मुक्ति एवं स्थिरता संभव है, जबकि चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। भविष्य की चुनौतियों में व्यापार युद्ध, जैसे अमेरिका-चीन टैरिफ विवाद, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डेटा सेंटरों से बढ़ती बिजली मांग शामिल हैं। विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि वर्ष 2030 तक बिजली की मांग लगभग दोगुनी होकर 945 टेरा वॉट ऑवर तक पहुँच सकती है, जिससे नवीकरणीय स्रोतों की ज़रूरत और बढ़ जाएगी। भारत और अन्य देशों के प्रयास यह दिखाते हैं कि सही नीति, निवेश एवं वैश्विक सहयोग से ऊर्जा मुक्ति तथा सतत् विकास संभव है।




