कृत्रिम बुद्धिमत्ता: शक्ति का केंद्रीकरण या अवसरों का लोकतंत्रीकरण?
- 17 Nov, 2025
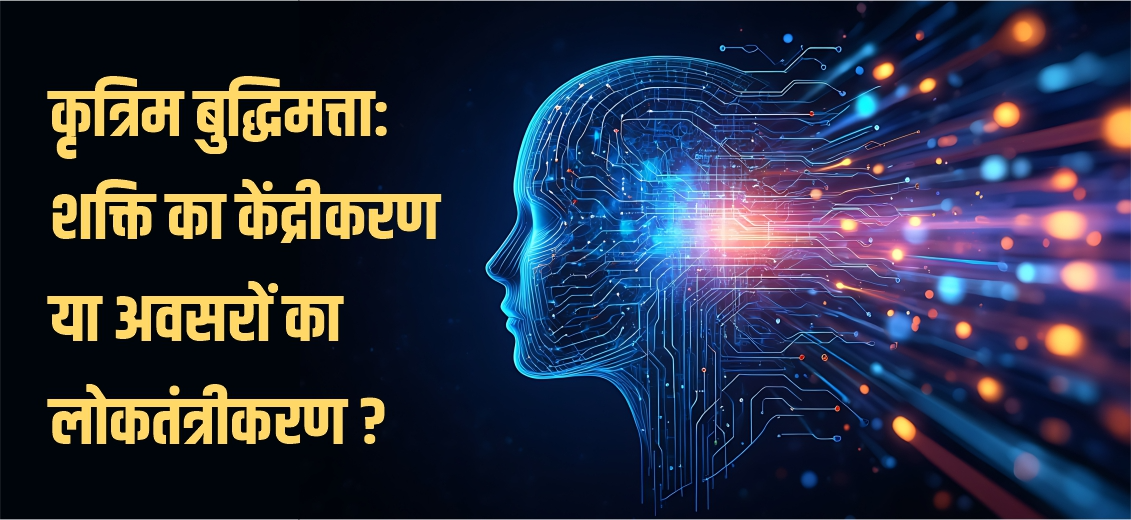
कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव चेतना का ऐसा अंग है, जो तकनीक के माध्यम से हमारी बुद्धि, रचनात्मकता और सीमाओं को प्रतिबिंबित करता है। यह न केवल मशीनों का कौशल है, अपितु मानवता के स्वयं को समझने का एक तरीका भी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव सभ्यता के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ है, जो तकनीकी नवाचार के साथ-साथ गहन दार्शनिक प्रश्नों को जन्म देता है। यह न केवल मशीनों की बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, बल्कि मानव समाज की संरचना, शक्ति और स्वतंत्रता के स्वरूप को पुनर्परिभाषित करने की एक प्रणाली भी है। इनमें एक मूल प्रश्न यह है कि क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शक्ति को कुछ हाथों में केंद्रित कर देगी जिससे नई असमानताएँ और नियंत्रण की प्रणालियाँ उभरेंगी? या यह अवसरों का लोकतंत्रीकरण करेगा, जिससे ज्ञान, रचनात्मकता और सशक्तीकरण हर व्यक्ति तक पहुँचेगा? कृत्रिम बुद्धिमत्ता छायाओं को सत्य बनाने का प्रयास है, पर यहाँ मूल प्रश्न यह है कि क्या यह सत्य हमारा है अथवा मशीन का। यह एक तरफ मानव क्षमता को विस्तार देने वाला उपकरण है, तो दूसरी तरफ हमारे ऊपर नए प्रकार की निगरानी और नियंत्रण स्थापित करने वाली व्यवस्था भी बन सकता है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास 1950 के दशक से शुरू हुआ, जब एलन ट्यूरिंग ने मशीनों की सोचने की क्षमता पर प्रश्न उठाया। सन् 1980 में मशीन लर्निंग, 2000 में डीप लर्निंग और वर्ष 2020 तक जेनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने क्रांति ला दी। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिकित्सा, शिक्षा और ऊर्जा प्रबंधन में अग्रणी है। अगर हम इसे परिभाषित करने का प्रयास करें तो ये कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने और काम करने की क्षमता देती है। यह मशीनों को सीखने, समझने, निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज हमारे जीवन का हिस्सा है—चाहे वह नेटफ्लिक्स की फिल्म सुझाव हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, या चैटबॉट्स। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कई तरह से काम करती है। मशीन लर्निंग से डेटा विश्लेषण करके मौसम की भविष्यवाणी करना, डीप लर्निंग से चेहरों या ध्वनियों को पहचाना आदि। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने चिकित्सा में कैंसर का पता लगाने, शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण और ऊर्जा क्षेत्र में मांग प्रबंधन में सहायता तो की है लेकिन इसके साथ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे गोपनीयता का खतरा एवं नौकरियों पर प्रभाव। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैश्विक ऊर्जा मांग को दोगुना कर रही है, जिससे पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियाँ उभर रही हैं।
मिशेल फूको के दृष्टिकोण से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता शक्ति संरचनाओं का विस्तार है, जो डेटा और एल्गोरिदम की सहायता से समाज को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। यह निगरानी और पूर्वानुमान का ऐसा शक्तियुक्त यंत्र बन सकता है, जो मानवीय स्वतंत्रता को बाधित कर सकता है। दूसरी ओर, इमैनुएल कांट की नैतिकता हमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग में मानव गरिमा को केंद्र में रखने की प्रेरणा देती है। इन दोनों तरह के विचारों को देखें तो यह कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारी रचनात्मकता का विस्तार तो है और साथ ही प्रश्न यह भी सामने आता है कि क्या हम इसे अपनी सोच का, आत्मा का हिस्सा बनाएंगे या इसके परिचारक या गुलाम होंगे। संक्षेप में क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवता की मुक्तिदाता है या मशीन के अधीनस्थ बन जाने का उपागम है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता शक्ति को केंद्रित करने की है, जो इसे कुछ सरकारों, कंपनियों और व्यक्तियों के हाथों में एक शक्तिशाली हथियार बनाती है। मिशेल फूको की शक्ति-संबंधी अवधारणा से देखें, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीक है जो निगरानी, डेटा संग्रह और व्यवहार नियंत्रण के माध्यम से "पैनोप्टिकन" (सर्वदृष्टा) का आधुनिक रूप रचती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता -संचालित निगरानी प्रणालियाँ—चाहे वह चेहरा पहचानने वाली तकनीक हो या सोशल मीडिया विश्लेषण, विश्व भर में सरकारों और कंपनियों द्वारा उपयोग में लाई जा रही हैं। उदाहरण के लिये, कुछ देशों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित सामाजिक क्रेडिट प्रणाली नागरिकों के व्यवहार को देखते हैं, जिससे उनकी स्वतंत्रता सीमित होती है। यह फूको के "अनुशासन और दंड" के उस सिद्धांत को साकार करता है, जहाँ शक्ति सूक्ष्म है लेकिन सर्वव्यापी तरीके से लागू होती है।
कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली का एक नया औजार है, जो शक्ति को पूंजीपतियों और तकनीकी दिग्गजों के हाथों में केंद्रित करता है। वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता बाज़ार का मूल्य 500 अरब डॉलर से अधिक हो गया है, जिसमें कुछ प्रमुख कंपनियाँ जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और चीनी दिग्गज कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी डेटा एवं कंप्यूटिंग संसाधनों पर नियंत्रण रखते हैं। ये डेटा को शक्ति का "नया स्रोत" बनाकर उसका शोषण करते हैं, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ती है।
फ्रेंकफर्ट धारा के विचाराकों के शब्दों में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्पादन के साधनों का हिस्सा है, जिसे पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग पर नियंत्रण के लिये उपयोग करता है। स्वचालन के कारण, विश्व भर में लाखों नौकरियाँ प्रभावित हुई हैं, विशेषकर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में। भारत में, जहाँ सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का 55% हिस्सा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से 15-20% नौकरियों पर जोखिम माना जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ऊर्जा उपभोग भी शक्ति के केंद्रीकरण को दर्शाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा सेंटरों से वैश्विक बिजली मांग 945 टेरावॉट घंटे तक पहुँचने की उम्मीद है। यह वर्ष 2030 तक दोगुनी हो सकती है। यह मांग कुछ देशों और निगमों के नियंत्रण में केंद्रित है, जो ऊर्जा संसाधनों एवं कंप्यूटिंग शक्ति को अपने अधीन रखते हैं। भारत जैसे देशों में, जहाँ ऊर्जा सुरक्षा पहले से ही चुनौती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की यह मांग आयात निर्भरता और लागत को बढ़ा रही है। यह एक नई दासता का रूप है, जहाँ तकनीकी एवं आर्थिक निर्भरता समाज को बाँधती है।
इसके अलावा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास और नियंत्रण कुछ देशों—मुख्य रूप से अमेरिका एवं चीन—के हाथों में है। ये दोनों देश वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पेटेंट्स और निवेश के 70% से अधिक हिस्से के लिये ज़िम्मेदार हैं। भारत, हालाँकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति कर रहा है, फिर भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपूर्ति शृंखला में इन देशों पर निर्भर है। यह तकनीकी साम्राज्यवाद एक नई वैश्विक शक्ति संरचना बनाता है, जहाँ छोटे देश और समुदाय अपने डेटा तथा तकनीकी स्वायत्तता खो रहे हैं।
दूसरी ओर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अवसरों के लोकतंत्रीकरण की अपार संभावनाएँ हैं। यह तकनीक ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रचनात्मकता को हर व्यक्ति तक पहुँचाने का साधन बन सकती है। इमैनुएल कांट की नैतिकता के दृष्टिकोण से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग मानव गरिमा और स्वायत्तता को बढ़ाने के लिये होना चाहिये। कांट का "नैतिक नियम" कहता है कि हमें हर व्यक्ति को साध्य के रूप में देखना चाहिये, न कि साधन के रूप में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अगर ज़िम्मेदारी से उपयोग हो, तो यह मानव क्षमता को मुक्त कर सकता है।
अवसर के लोकतंत्रीकरण का एक महत्त्वपूर्ण आयाम शिक्षा का क्षेत्र है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाया है। भारत में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण ने लाखों छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ शिक्षकों की कमी है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता -संचालित ऐप्स ने शिक्षा को सुलभ बनाया। उदाहरण के लिये, पीएम-ई विद्या पहल ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया और वर्ष 2025 में 17.24 लाख घरों को पीएम सूर्य घर योजना के तहत सौर ऊर्जा से जोड़ा गया, जिससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों के लिये बिजली उपलब्ध हुई। यह तकनीकी और ऊर्जा पहुँच का लोकतंत्रीकरण है, जो सामाजिक समावेशन को बढ़ाता है।
अवसर के लोकतंत्रीकरण का दूसरा महत्त्वपूर्ण आयाम स्वास्थ्य का क्षेत्र है। स्वास्थ्य क्षेत्र में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने कैंसर जैसे रोगों का जल्दी पता लगाने में मदद की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित डायग्नोस्टिक तकनीकों ने भारत के ग्रामीण अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुँच को और अधिक सुगम बनाया है। एक तीसरे आयाम के रूप में यह तकनीक छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप्स को भी सशक्त बना रही है। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप्स की संख्या वर्ष 2025 में 2,000 से अधिक हो गई है, जो कृषि, वित्त और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में नवाचार ला रहे हैं। जेनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैसे कि छायाचित्रों के विविधिकरण और लिखने का काम, करने से रचनात्मकता को लोकतांत्रिक बनाया, जिससे छोटे कलाकार एवं लेखक वैश्विक मंच पर पहुँच रहे हैं।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने ऊर्जा क्षेत्र में भी अवसर खोले हैं। भारत ने 32 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने ग्रिड प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता में योगदान दिया। स्मार्ट ग्रिड और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित लोड पूर्वानुमान ने ऊर्जा वितरण को अधिक समावेशी बनाया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुँची। यह कांट के सिद्धांत को साकार करता है, जहाँ तकनीक मानवता की सेवा में है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यह दोहरा स्वरूप—शक्ति का केंद्रीकरण और अवसरों का लोकतंत्रीकरण—हमें एक और द्वंद्व की ओर ले जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल के उपयोगितावाद से देखें, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मूल्यांकन इसके परिणामों से होना चाहिये। अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकांश लोगों के लिये सुख और अवसर बढ़ाती है, तो यह नैतिक रूप से उचित है। लेकिन अगर यह असमानता और नियंत्रण को बढ़ाता है, तो यह समाज के लिये हानिकारक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने दोनों परिणाम दिये हैं। यह शिक्षा और स्वास्थ्य में अवसर लाया है, लेकिन नौकरियों का नुकसान एवं डेटा गोपनीयता के खतरे ने असमानता को भी बढ़ाया है।
गहराई से विचार करने पर हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सत्य की प्रकृति पर विचार करने को प्रेरित होते हैं। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमें सत्य की ओर ले जाता है, या यह एक नई छाया है जो हमें वास्तविकता से दूर रखती है? डेटा और एल्गोरिदम पर आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाज को एक ऐसी दुनिया दिखा सकता है जो पक्षपाती या हेरफेर से भरी हो। उदाहरण के लिये, सोशल मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कंटेंट सुझाव उपयोगकर्त्ताओं को उनके विचारों के दायरे में बाँधते हैं, जिससे "फिल्टर बबल" बनता है। इसके विपरीत, हाइडेगर की दृष्टि हमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एक उपकरण के रूप में देखने की सलाह देती है, जो मानव के "होने" को प्रकट करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमें अपनी रचनात्मकता और सीमाओं को समझने में मदद कर सकता है, बशर्ते हम इसे अपने मूल्यों के अधीन रखें। भारत जैसे देश में, जहाँ सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ गहरी हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग समावेशी नीतियों के साथ होना चाहिये।
भारत में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास और उपयोग इस द्वंद्व को स्पष्ट करता है। एक ओर, भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया है। राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति और डिजिटल इंडिया मिशन ने तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दिया। दूसरी ओर, डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा के मुद्दे चुनौतियाँ हैं। भारत में डेटा संरक्षण कानून 2023 लागू होने के बावजूद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग की आशंका बनी हुई है। ऊर्जा क्षेत्र में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत किया है, लेकिन इसकी मांग ने आयात निर्भरता को बढ़ाया।
भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभों को लोकतांत्रिक बनाने के लिये शिक्षा, नीति और बुनियादी ढाँचे में निवेश करना होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे नियंत्रित करते हैं। कांत की नैतिकता हमें सिखाती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मानवता की सेवा में होना चाहिये, न कि इसके अधीन। इसके लिये पारदर्शिता, समावेशिता और जवाबदेही ज़रूरी है। वैश्विक स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता नैतिकता पर चर्चा तेज़ हुई है और भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता गवर्नेंस फ्रेमवर्क की दिशा में कदम उठाए हैं।
फ्रेंकफर्ट स्कूल के दृष्टिकोण से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लोकतंत्रीकरण तभी संभव है जब डेटा और कंप्यूटिंग संसाधनों का स्वामित्व सामुदायिक हो। फूको हमें चेतावनी देता है कि बिना सतर्कता के, कृत्रिम बुद्धिमत्ता शक्ति का एक नया उपकरण बन सकता है। हाइडेगर हमें प्रेरित करता है कि हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मानवता के आत्म-प्रकटीकरण के साधन के रूप में देखें।
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता न तो केवल शक्ति का केंद्रीकरण है, न ही केवल अवसरों का लोकतंत्रीकरण। यह दोनों का मिश्रण है और इसका स्वरूप हमारे सामूहिक निर्णयों पर निर्भर करता है। भारत जैसे विशाल सामाजिक-आर्थिक विविधता वाले देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास तभी सार्थक होगा जब वह समावेशी और नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। हालाँकि एआई ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नए अवसर खोले हैं, पर इसके साथ निगरानी, असमानता एवं तकनीकी निर्भरता जैसी चुनौतियाँ भी समान रूप से मौजूद हैं। दार्शनिक रूप से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमें मानवता के मूल प्रश्नों से जूझने को बाध्य करती है: हम क्या बनना चाहते हैं? स्वतंत्र या अधीन? यह प्रश्न तकनीक से बड़ा है—यह हमारी नियति का प्रश्न है।




