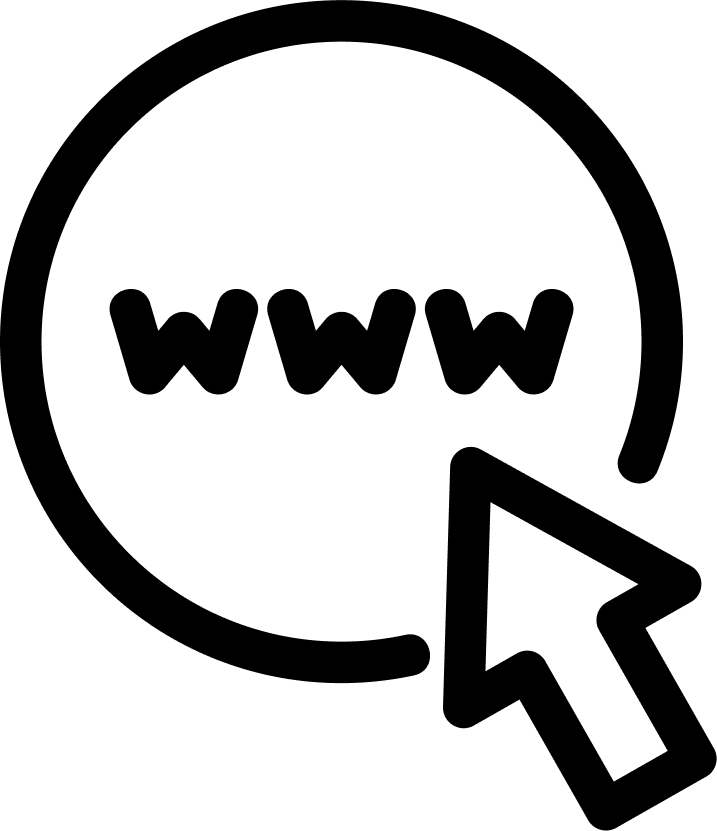सत्यजित रे : साहित्यिक गरिमा की फिल्मों के महान सर्जक
- 02 Aug, 2023 | सुंदरम आनंद

सत्यजित रे पर लिखे अपने एक संस्मरण में हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार कुँवर नारायण ने लिखा है- " उनका( रे ) सिनेमा साहित्य के साथ अंतरंग विनिमय का अनोखा दस्तावेज़ है" । उनके इस कथन की तस्दीक इस बात से की जा सकती है कि 37 फिल्मों की रे की सिने-फ़ेहरिश्त में तकरीबन दो दर्जन फिल्में ऐसी हैं, जिनका मज़मून किसी न किसी साहित्यिक कृति से जुड़ा है। इन फिल्मांतरित कृतियों में उन्होंने ज्यादातर बांग्ला साहित्य की रचनाओं को आधार बनाया है। टैगोर, विभूति भूषण,ताराशंकर बंद्योपाध्याय, सुनील गंगोपाध्याय आदि की रचनाओं का उन्होंने सफल और संजीदा फिल्मांकन किया है।
रे ने केवल दो गैर-बांग्ला फिल्में बनायीं या यूँ कहें कि उन्होंने हिन्दी (हिंदुस्तानी) में दो फिल्में बनायी हैं- 'शतरंज के खिलाड़ी' (1977) और 'सद्गति '(1981)। हिंदी के कथा- सम्राट प्रेमचन्द की इन्हीं नामों से लिखी कहानियों के सिने- रूपांतरण के रूप ये फिल्में बेशक रे की सर्वश्रेष्ठ फिल्में नहीं हैं लेकिन कई मामलों में ये उनकी अन्य कृतियों से अलहदा ज़रूर हैं। इन फिल्मों के बाबत उनकी जीवनी 'सत्यजित रे : द इनर आइ' में एंड्रयू रॉबिंसन ने लिखा है:-
" अद्भुत सेटिंग्स और उनकी फिल्मों के लिहाज से बड़े प्रोडक्शन वैल्यू के साथ इस फिल्म में ब्रिटिश राज का सीधा चित्रण और नामचीन अंग्रेज अभिनेताओं का उपयोग ऐसे गुण हैं जो इस फिल्म (शतरंज के खिलाड़ी) को उनकी अन्य फिल्मों से अलग करते हैं “|
वहीँ ‘सद्गति (1981 ) के बारे में रॉबिन्सन का मानना है :-
“रे ने(प्रेमचंद की ) इस कहानी के फिल्मांतरण में काफी कम बदलाव किये हैं। यह उनकी अपने मूल स्रोत के प्रति सबसे ईमानदार(यथातथ्य ) फिल्म है “|
फिल्मांतरण और रे: कुछ अंतःसूत्र
सत्यजित रे महान फ़िल्मकार तो थे ही,साथ ही वे सिनेमा के व्याकरण और सिद्धांतों को लेकर सजग रहने वाले प्रयोगशील फ़िल्मकार भी थे| शायद इसीलिए उनकी फ़िल्में आजतक गंभीर विमर्शों की माँग करती हैं। तभी तो श्याम बेनेगल जैसे आला फ़िल्मकार भी उनके बारे में कह उठते हैं:-
“मैं कभी उनकी फ़िल्में देखकर नहीं थकता। यदि आप उनके समकालीनों का काम देखें तो आप उनमें पुरानापन महसूस करना शुरू करने लगते हैं। लेकिन रे के काम के साथ पुरानेपन का एहसास नहीं होता “|
उनकी फ़िल्में सिने-प्रेमियों ,फिल्मकारों और अध्येताओं के लिए सिनेमा-अध्ययन की सन्दर्भ सामग्री बनकर सामने आती हैं । बकौल कुँवर नारायण :-
“समग्रता में उनकी (रे ) फिल्मों का संसार एक बड़ी प्रबंध रचना की तरह विविध और विशद है...... वे (उनकी फ़िल्में ) उच्च कोटि के साहित्य के स्तर पर हमारे मन और चिंतन को आंदोलित करती हैं।“
जिन फिल्मों का रे ने फिल्मांतरण किया है वे ‘फिल्मांतरण के विभिन्न सिद्धांतों’ को समझने के सटीक उदाहरण हैं| उनकी फ़िल्मांतरित कृतियों के बारीक़ अध्ययन से हम फिल्मांतरण की तकनीकी प्रक्रिया और उसके सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव के विविध आयामों की समझ विकसित कर सकते हैं। कथा-साहित्य के उनके सिनेमाई रूपांतरण इस बात की नज़ीर हैं कि साहित्य और सिनेमा के बीच के विनिमय का फलक महज लिखे शब्दों का स्क्रीन पर बोलते चित्रों में परिवर्तन भर नहीं है, बल्कि यह दो कलाओं के बीच एक सक्रिय संवाद भी है। इसके ज़रिये कला और संस्कृति के बारे में दो कलाकारों की समझ भी प्रतिध्वनित होती है। रे के सिनेमा में मौजूद इन गुणों के बारे में अमर्त्य सेन ने लिखा है :-
“ सत्यजित रे का काम भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की संस्कृतियों तथा उन संस्कृतियों के बीच चलने वाले उपयोगी विमर्शों के बारे में गहरी समझ पैदा करता है "
टैगोर से लेकर ताराशंकर बंद्योपाध्याय तक या फिर विभूतिभूषण से लेकर सुनील गंगोपाध्याय तक अलग-अलग दौर और शैली के रचनाकारों की कृतियों को अपनी रचनात्मक दृष्टि में ढालकर उन्होंने समकालीन और सार्वभौमिक ‘सिनेमाई पाठ’ बनाकर दुनिया के सामने पेश किया |
प्रेमचंद वाया रे
यूँ तो शुरुआती दिनों से ही सिनेमा पर साहित्य की स्पष्ट छाप रही है। तभी तो आइजेंस्टाइन और ग्रिफिथ के साथ डिकेन्स को भी सिने-कला के प्रमुख सूत्रधारों में गिना जाता है। फिल्मांतरण को लेकर जब दुनिया भर में विमर्श की शुरुआत हुई तो उसमें ‘मूल कृति के प्रति ईमानदारी’ (Fidelity ) को सबसे ज़्यादा तरज़ीह दी गयी | लेकिन जैसे-जैसे एक कला के रूप में सिनेमा को मान्यता मिलनी शुरू हुई, उसके तकनीक, विन्यास और व्याकरण को लेकर नए-नए प्रयोग शुरू हुए तो फिल्मांतरण के प्रति भी समालोचकों की दृष्टि बहुआयामी होने लगी। साहित्यिक कृति में लेखक की केन्द्रीयता के तर्ज़ पर जब सिनेमाई कृति में निर्देशक की केन्द्रीयता को लेकर बहस चली तो इन बहसों ने फिल्मांतरण के प्रति विभिन्न धारणाओं को विकसित करने में अहम भूमिका निभायी। इन बदलावों को रेखांकित करते हुए क्रिस्टोफर ओर्र ने कहा है :-
“आज मुद्दा यह नहीं है कि रूपान्तरित फिल्म अपने मूल स्रोत के प्रति ईमानदार है या नहीं बल्कि चुनी गयी सामग्री के प्रति फ़िल्मकार का अप्रोच और सिनमाई कृति में मूल कृति में निहित भाव की अभिव्यक्ति को देखना ज़्यादा अहम हो गया है "
इसी परिप्रेक्ष्य में अमेरिका के नामचीन स्क्रीनप्ले लेखक डेविट बॉडीन की यह मान्यता भी उल्लेखनीय है कि
“ किसी साहित्यिक कृति का सिनेमा में रूपान्तरण बेशक एक रचनात्मक उपक्रम है, लेकिन यह प्रक्रिया उस कृति के द्वारा स्थापित होने वाले मूड की पुनर्रचना तथा (उस कृति की) एक खास किस्म की चयनात्मक व्याख्या कर पाने की क्षमता की मांग करती है "|
रे ने प्रेमचंद की जिन दोनों कहानियों (‘शतरंज के खिलाड़ी’ और ‘सद्गति) को सिनेमा के परदे पर उकेरा है, उन्हें बेहतर ढंग से समझने में उक्त दोनों उद्धरण माकूल मालूम पड़ते हैं।
शतरंज के खिलाड़ी (1977 ) की अगर बात करें तो यह कई मायनों में रे की नायाब फिल्म है, एक तो यह उनकी पहली हिंदी फिल्म है ही, साथ ही यहाँ वे पहली बार ऐतिहासिक कथावस्तु पर अ-रैखीय कथाविन्यास के साथ अपनी सिने-अभिव्यक्ति करते नज़र आते हैं। इनके अलावा रे यहाँ कहानी के अंशों तथा बिम्बों के ज़रिये पहली बार सेक्सुअलिटी के सवालों को भी सामने लाने की कोशिश करते दिखे हैं। अपने इस सिनेमाई रूपांतरण में रे ने बिना संदेह प्रेमचंद की इस कहानी को सार्थक विस्तार दिया है। जहाँ प्रेमचंद ने अपनी कहानी में बेबाक रूप से लखनऊ और वहां के दो काल्पनिक नवाबों के ज़रिये, किसी ऐतहासिक पात्र या घटना का सहारा लिए बग़ैर (बस कहानी की पहली पंक्ति में उन्होंने यह संकेत भर किया है :- “वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था ") 19 वीं सदी के मध्य के भारत की पतनशील प्रवित्तियों की एक ‘परिस्थिति’ भर चित्रित की है। वहीँ रे ने प्रेमचंद के बरअक्स अपनी फिल्म में उस दौर के भारत की पतनशील सामंतवादी व्यवस्था को ब्रिटिश राज की उभरती हुई औपनिवेशिक व्यवस्था के सामानांतर रखकर प्रस्तुत किया है। उनकी फिल्म में लखनऊ की तहज़ीब और उस दौर के वहाँ के ऐतिहासिक सन्दर्भों को बेहद बारीकी से पिरोया गया है। इस अर्थ में उनकी फिल्म प्रेमचंद की ‘शतरंज के खिलाड़ी ‘ और मौलाना अब्दुल हलीम शरर की ‘गुज़श्त: लखनऊ ‘ के बीच एक संयोजक के मानिंद सामने आती है।
उन्होंने बाकायदा वाजिद अली शाह के किरदार को न केवल अलग से गढ़ा है, बल्कि उस दौर की वास्तविक घटनाओं का सहारा लेकर उसे एक संश्लिष्ट चरित्र बनाने में भी वे सफल हुए हैं। भाषायी स्तर पर कहानी में जहाँ प्रेमचंद ने अपनी चिरपरिचित स्वाभाविक शैली को ही अपनाया है ( हालाँकि ‘ शतरंज की बाज़ी ‘ नाम से प्रकाशित इसी कहानी को उर्दू में लखनऊ के आम भाषायी लहज़े के करीब रखा है), वहीँ रे की फिल्म में लखनऊ की संस्कृति के प्रामाणिक चित्रण में ‘लखनवी ज़बान ‘ने खासी भूमिका निभाई है।
‘शतरंज के खिलाड़ी’ के साहित्यिक और सिनेमाई पाठ में इस जोड़-घटाव के पीछे शायद दो महान सर्जकों के ‘क्रिएटिव विजन ‘में मौलिक अंतर की अहम भूमिका है। इस फ़र्क़ की ओर इशारा करते हुए वहीं कुँवर नारायण ने लिखा है
“राय (रे ) की दृष्टि मूलतः लिरिकल है,जबकि प्रेमचंद अपनी बात बेबाकी और दो टूक ढंग से कहते हैं : उसमें लाग-लपेट नहीं ,ज़िन्दगी की बेतकल्लुफ मौजूदगी है। उनकी कला इस हद तक ज़िन्दगी से घुली-मिली रहती है कि वह अलग से दिखाई नहीं देती। जबकि राय की कला अपने होने को छिपाती नहीं यथार्थ के साथ-साथ अपनी भी एक स्पस्ट पहचान बनाती चलती है“
दूसरी तरफ जब हम ‘सद्गति’(1981 ) का रुख करते हैं तो पाते हैं कि यहाँ रे ने फिल्मांतरण के ‘यथातथ्य प्रस्तुति ‘(Fidelity ) की शास्त्रीय शैली को अपनाया है। शायद इसीलिए इसे रे की ‘प्रेमचंद की तकनीक पर बनी फिल्म’ भी कहा जाता है। ‘शतरंज के खिलाड़ी’ तुलना में यहाँ ‘सिनेमाई पाठ ‘ की अपेक्षा ‘साहित्यिक पाठ ‘ ज़्यादा मुकम्मल और बेलाग रूप में अभिव्यक्त होता नज़र आता है। कहानी में जहाँ प्रेमचंद का स्वर निर्भ्रांत,विक्षुब्ध और नग्न यथार्थ की प्रस्तुति करने वाला वाला है, वहीं फिल्म में रे ने बिम्बों ,प्रतीकों और संकेतों का सहारा अधिक लिया है। जिसकी वजह से शायद कथ्य में मौजूद ‘पॉलिटिकल कंटेंट ‘ की तीक्ष्णता थोड़ी मंद हुई है। ऐसा हो सकता है कि फिल्म की कम अवधि तथा दूरदर्शन से लिए गए आर्थिक सहयोग के कारण भी शायद रे उतनी रचनात्मक आज़ादी न ले पाए हों, जो इस प्रकार के विषयों को खुलकर बरतने के लिए अपेक्षित होती है। इसके बावजूद बिना किसी संदेह के इस फिल्मांतरण में भी रे की इस दृष्टिकोण की पुष्टि होती है कि :-
“ सिनेमा मूलतः एक दृश्य माध्यम है और कथ्य में मौजूद वातावरण की अक्षुण्णता एक अच्छी फिल्म की मौलिक पहचान होती है “
‘सद्गति’ (1981 ) में एक अच्छी फिल्म की यह मौलिक विशेषता निश्चित रूप से मौजूद है।
रे के फिल्मांतरण की प्रासंगिकता
पहले सत्यजित रे मेमोरियल लेक्चर में बोलते हुए जावेद अख्तर ने कहा था “कोई चीज़ तब प्रासंगिक होती है जब उसकी प्रचूर मौजूदगी हो या उसकी भरपूर कमी हो “
जावेद साहब की इस टिप्पणी को सामने रखकर देखें तो दृश्य-ध्वनि,शब्द-संगीत ,भाव-भाषा की काव्यमय जुगलबंदी के साथ रे की फ़िल्में शाश्वत मानवीय मूल्यों को सामने लाती हैं।
फिल्मों के लिए जब भी स्रोत के रूप में उन्होंने साहित्यिक कृतियों की तरफ रुख किया तो कथावस्तु में चित्रात्मकता के साथ उसमें ‘जीवन-रस’ की मौजूदगी विषय चयन की उनकी बुनियादी कसौटी रही है। जिस प्रकार ‘साहित्य का उद्देश्य’ में प्रेमचंद कहते हैं :-
“हम जीवन में जो कुछ देखते हैं या जो कुछ हम पर गुज़रती है, वही अनुभव और चोटें कल्पना में पहुँचकर साहित्य-सृजन की प्रेरणा करती है "
ठीक उसी तर्ज़ पर रे भी यह मानते हैं कि :-
“कला के प्रति हमारी सोच में दरअसल जीवन के प्रति हमारा नजरिया ही सबसे बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित होता है"
कलादृष्टि के स्तर पर समानता के साथ रे के रचना संसार में भी हम छवियों तथा भावों के मामले में ‘प्रेमचन्दीय’ साफगोई और प्रभावशीलता रेखांकित कर सकते हैं। उन्होंने अपनी कृतियों के ज़रिये हमारे आसपास मौजूद जीवन के राग-रंगों को इस तरह नियोजित किया है कि वे बार-बार संदर्भवान होकर सामने आती हैं। कुँवर नारायण ने शायद इसीलिए सत्यजित रे के सिनेमा के बारे में यह लिखा है:-
“राय (रे) की फ़िल्में इसलिए महान नहीं हैं कि वे साहित्य की स्पर्धा में अपनी एक अलग दुनिया रचती हों,वे विशिष्ट हैं क्योंकि वे उच्च कोटि के साहित्य के स्तर पर हमारे मन और चिंतन को आंदोलित करती हैं " |
 |
सुंदरम आनंद(लेखक जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से हिन्दी कथा साहित्य पर बनी फिल्मों पर शोधरत हैं) |