उत्तराखंड Switch to English
उत्तराखंड की पहली योग नीति
चर्चा में क्यों?
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य की पहली योग नीति का शुभारंभ किया।
- साथ ही गढ़वाल और कुमाऊँ क्षेत्रों में 'आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र' (Spiritual Economic Zones) के निर्माण की भी घोषणा की गई।
मुख्य बिंदु
- योग नीति के बारे में:
- इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और कल्याण की वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित करना है।
- यह नीति 'हर घर योग, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य' की अवधारणा को बढ़ावा देती है, जिसमें केंद्र सरकार का सहयोग प्राप्त है।
- वित्तीय प्रावधान:
- इस नीति के तहत योग और ध्यान केंद्रों की स्थापना के लिये अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- कार्यान्वयन लक्ष्य:
- मार्च 2026 तक राज्य के सभी आयुष स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों पर योग सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।
- वर्ष 2030 तक राज्य में पाँच नए योग केंद्र विकसित किये जाएंगे।
- आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र:
- इन क्षेत्रों को आयुर्वेद, योग और आध्यात्मिक पर्यटन के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
- इन क्षेत्रों के माध्यम से राज्य में नए रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।
- यह पहल स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर उपलब्ध कराकर पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन को रोकने में सहायक सिद्ध होगी।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में:
- शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिये योग के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा इसके अभ्यास के माध्यम से वैश्विक सद्भाव और शांति को बढ़ावा देने के लिये पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है।
- उद्गम और संयुक्त राष्ट्र की घोषणा:
- इसका प्रस्ताव भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र (2014) में रखा गया था, जिसके परिणामस्वरूप 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) घोषित किया गया।
- पहला योग दिवस वर्ष 2015 में मनाया गया था, जिसकी थीम थी: "Yoga for Harmony and Peace" (सामंजस्य और शांति के लिये योग)।
- वर्ष 2025 का विषय है “एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिये योग”।
- 21 जून का महत्त्व:
- यह तिथि ग्रीष्म अयनांत (Summer Solstice) के साथ संयोग रखती है, जो उत्तरी गोलार्द्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। योग परंपरा में यह दिन प्रकाश, ऊर्जा तथा आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक माना जाता है।
- वैश्विक मान्यता:
- यूनेस्को ने वर्ष 2016 में योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने योग को मानसिक और शारीरिक कल्याण और गैर-संक्रामक रोगों (NCDs) से निपटने के एक प्रभावी साधन के रूप में मान्यता दी है तथा इसे अपने वैश्विक कार्य योजना (2018–30) में शामिल किया है।
- वर्ष 2015 में भारत के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने योग को एक 'प्राथमिकता' खेल अनुशासन के रूप में वर्गीकृत किया।
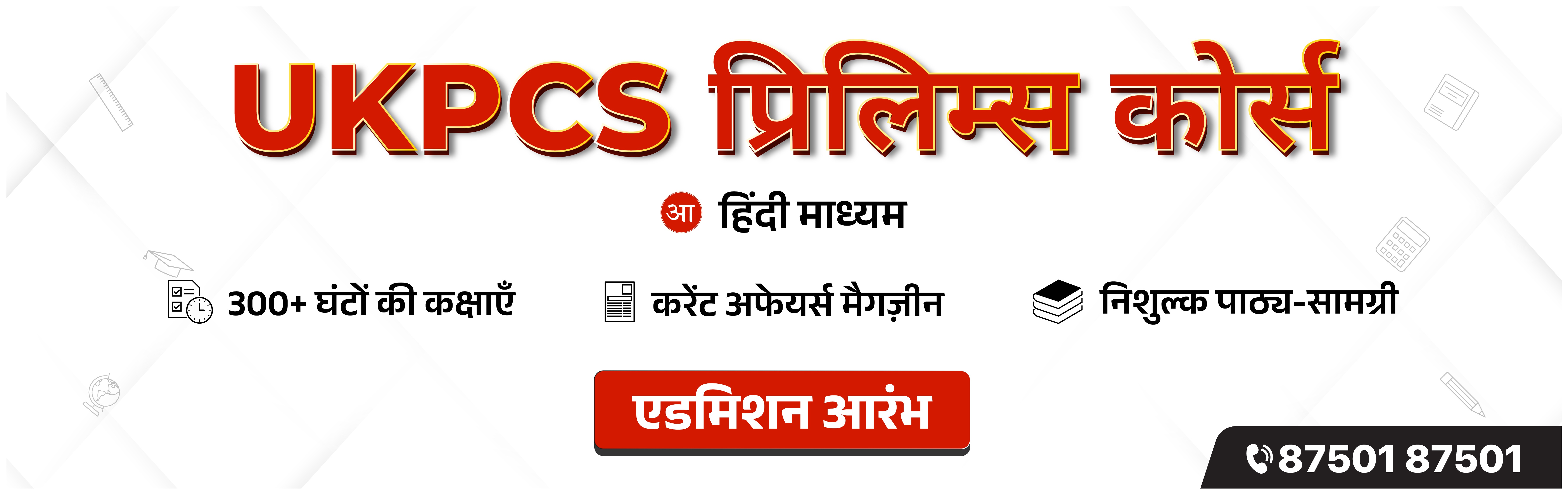

राजस्थान Switch to English
दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण राजस्थान में भारी वर्षा
चर्चा में क्यों?
राजस्थान सक्रिय दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ गया है, जिसके फलस्वरूप राज्य के विभिन्न भागों में विस्तृत एवं तीव्र वर्षा दर्ज की गई है।
- टोंक ज़िले के निवाई में राज्य में सर्वाधिक 165 मिमी वर्षा दर्ज की गई।
मुख्य बिंदु
- राजस्थान में वर्षा वितरण:
- राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा वितरण में उल्लेखनीय भिन्नता देखने को मिलती है।
- पूर्वी राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 64.9 सेमी होती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में यह घटकर 32.7 सेमी रह जाती है।
- राजस्थान के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में काफी अधिक वर्षा होती है तथा राज्य की कुल वार्षिक वर्षा में दक्षिण-पश्चिमी मानसून का योगदान लगभग 91% होता है।
- पश्चिमी राजस्थान मुख्यतः शुष्क और अर्द्ध-शुष्क परिस्थितियों से युक्त है, जिसमें उत्तर-पश्चिमी भाग सर्वाधिक शुष्क है।
- जैसलमेर को राज्य का सबसे शुष्क ज़िला माना जाता है, जहाँ वार्षिक वर्षा 100 मिमी से भी कम होती है।
- दक्षिणी राजस्थान में राज्य की सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है, विशेष रूप से झालावाड़ और बांसवाड़ा जैसे ज़िलों में।
- झालावाड़ राजस्थान के सभी ज़िलों में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है।
- अरावली पर्वतमाला का प्रभाव: अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढलानों, जैसे पाली और जालौर ज़िलों में पश्चिमी राजस्थान के अन्य भागों की तुलना में अधिक वर्षा होती है।
- राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा वितरण में उल्लेखनीय भिन्नता देखने को मिलती है।
- ऋतुओं के अनुसार भिन्नता:
- मानसून ऋतु (जून से सितंबर): कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 90% इसी ऋतु में होता है।
- शीत ऋतु (जनवरी और फरवरी): स्थानीय मौसम की स्थिति के कारण मामूली वर्षा होती है।
- उत्तर-मानसून ऋतु: कुल वार्षिक वर्षा में इसका योगदान बहुत कम होता है।
दक्षिण-पश्चिम मानसून
- दक्षिण-पश्चिम मानसून से प्राप्त वर्षा मौसमी है, जो जून और सितंबर के मध्य होती है।
- मानसून के गठन को प्रभावित करने वाले कारक:
- विभेदक तापन एवं शीतलन: स्थल, जल की अपेक्षा अधिक तेज़ी से गर्म होता है, जिससे भारत के ऊपर निम्न दबाव तथा आस-पास के समुद्री क्षेत्रों पर उच्च दबाव का क्षेत्र निर्मित होता है।
- अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ): यह एक निम्न दबाव पट्टी है, जहाँ उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी व्यापारिक हवाएँ मिलती हैं।
- मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दबाव क्षेत्र: यह उच्च दबाव क्षेत्र हिंद महासागर में लगभग 20° दक्षिण अक्षांश पर स्थित होता है।
- तिब्बती पठार का तापन: ग्रीष्म ऋतु में तीव्र तापन के कारण ऊपर की ओर तीव्र गतिशील हवाएँ चलती हैं, जिससे उच्च ऊँचाई पर निम्न दबाव क्षेत्र बनता है।
- जेट स्ट्रीम: ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम, हिमालय के उत्तर की ओर स्थित हो जाती है।
- दक्षिणी दोलन (SO): यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच वायुदाब का आवधिक उलटाव है, जो मानसून के स्वरूप को प्रभावित करता है।
- दक्षिण-पश्चिम मानसून का तंत्र और प्रारंभ:
- ITCZ की गति: यह सूर्य की गति के साथ उत्तर की ओर स्थानांतरित होता है।
- हवा की दिशा: दक्षिण-पूर्वी व्यापारिक हवाएँ भूमध्य रेखा को पार करती हैं और कोरिओलिस बल के प्रभाव से दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी हवाओं में परिवर्तित हो जाती हैं।
- मानसून गर्त: जुलाई में ITCZ, 20°-25° उत्तर अक्षांश तक पहुँच जाता है, जो सिंधु-गंगा के मैदान पर स्थित होता है।
दो मुख्य शाखाएँ: अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा
- मानसून में अवरोध: मानसून के दौरान वर्षा निरंतर नहीं होती। मानसून गर्त की स्थिति में बदलाव के कारण शुष्क अवधियाँ (अवरोध) उत्पन्न होती हैं।


राजस्थान Switch to English
AI के साथ पढ़ाई
चर्चा में क्यों?
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित शैक्षिक कार्यक्रम “पढ़ाई विद AI” ने राजस्थान के टोंक ज़िले के सरकारी स्कूलों के शैक्षणिक परिणामों में उल्लेखनीय सुधार किया है।
मुख्य बिंदु
- कार्यक्रम के बारे में: इस कार्यक्रम को “पढ़ाई विद AI” कहा जाता है, जिसका अर्थ है “AI के साथ अध्ययन”।
- यह पहल छात्रों की स्वयं-गति से सीखने के लिये डिज़ाइन किये गए एक समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से डिजिटल शिक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत करती है।
- वेब पोर्टल छात्रों को पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को हल करने, समान समस्याओं का अभ्यास करने तथा कमज़ोर क्षेत्रों को निपुण करने में मदद करने के लिये सुधारात्मक अभ्यास, ड्रिल अभ्यास और व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य छात्रों को उन विषयों को समझने और उनका अभ्यास करने में मदद करना है, जो उन्हें कठिन लगते हैं तथा गणित पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- कार्यान्वयन रणनीति:
- गणित में कमज़ोर प्रदर्शन को दूर करने के लिये टोंक कलेक्टर द्वारा शुरू किया गया यह AI-आधारित कार्यक्रम, टोंक ज़िले के 351 स्कूलों में लागू किया गया, जिसमें 2025 सत्र को लक्षित करते हुए कक्षा 10 के लिये तीन महीने की कार्य योजना तैयार की गई।
- प्रभाव और परिणाम:
- टोंक का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत, राज्य औसत से अधिक रहा, जो AI-आधारित शिक्षण कार्यक्रम की सफलता को दर्शाता है।
शिक्षा के लिये राजस्थान की अन्य डिजिटल पहल
- AI-सक्षम मूल्यांकन:
- राजस्थान ने पारंपरिक परीक्षाओं से हटते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप AI-संचालित, योग्यता-आधारित मूल्यांकन की दिशा में कदम बढ़ाया है।
- ध्वनि पहचान तकनीक का उपयोग करके 26 लाख से अधिक छात्रों के लिये मौखिक पठन प्रवाह (ORF) परीक्षण आयोजित किये गए।
- कक्षा 9 से 12 तक के लिये सामान्य मूल्यांकन परीक्षण (CET) को मानकीकृत किया गया है।
- बुनियादी ढाँचा एवं डिजिटल लर्निंग विस्तार:
- विद्यालयी बुनियादी ढाँचे में सुधार हेतु 225 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
- डिजिटल कक्षाओं, स्मार्ट बोर्डों तथा ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- डिजिटल माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण और कैरियर परामर्श का एकीकरण किया जाएगा।
- कौशल विकास एवं कैरियर तैयारी:
- विश्वकर्मा कौशल संस्थान तथा उन्नत कौशल एवं कैरियर परामर्श केंद्र की शुरुआत की गई है।
- 36 ITI संस्थानों का आधुनिकीकरण किया गया तथा नए पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना की गई है।


छत्तीसगढ़ Switch to English
सरकारी नेतृत्व वाली कोल्ड चेन और विकिरण सुविधा
चर्चा में क्यों?
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जनजातीय लोगों की आय बढ़ाने और फसल-उपरांत होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के लिये राज्य की पहली सरकारी एकीकृत कोल्ड चेन और विकिरण सुविधा स्थापित की जाएगी।
मुख्य बिंदु
सुविधा के बारे में:
- स्थान: यह सुविधा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िले के पातररास गाँव में स्थापित की जाएगी।
- एकीकृत अवसंरचना: इसमें शीत भंडारण, गामा विकिरण, प्रसंस्करण तथा रसद घटक शामिल होंगे।
- इस सुविधा को वन एवं बागवानी उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने, नुकसान को कम करने तथा उनकी विपणन क्षमता सुधारने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है।
- अपनी तरह की पहली सुविधा:
- यह प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के अंतर्गत भारत की पहली सरकारी कोल्ड चेन तथा बहु-उत्पाद विकिरण सुविधा होगी।
- कार्यान्वयन एवं वित्तपोषण:
- विकिरण प्रौद्योगिकी हेतु विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं। पूरी परियोजना का वित्तपोषण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा दंतेवाड़ा ज़िले के ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF) द्वारा किया जा रहा है।
- प्रभाव:
- ग्रामीण रोज़गार: यह सुविधा आपूर्ति शृंखला में स्थानीय रोज़गार के अवसर सृजित करेगी।
- आर्थिक सशक्तीकरण: यह क्षेत्र के भीतर मूल्य संवर्द्धन सुनिश्चित करती है ताकि अधिक आय स्थानीय जनजातीय समुदायों के पास ही बनी रहे।
- रणनीतिक संरेखण: यह सुविधा क्षेत्रीय विकास योजनाओं का समर्थन करती है। इसका उद्देश्य बस्तर क्षेत्र में स्थायी आजीविका के अवसरों का विस्तार कर वामपंथी उग्रवाद का सामना करना है।
- लघु वन उपज (MFP) पर ध्यान:
- इस क्षेत्र की प्रमुख लघु वन उपज जैसे– इमली, महुआ, जंगली आम, बाजरा तथा स्थानीय मसाले, अपर्याप्त भंडारण और संरक्षण सुविधाओं के अभाव में अक्सर 10–20% वार्षिक नुकसान झेलते हैं।
- इस सुविधा से भंडारण में सुधार होगा तथा स्थानीय उपज का मूल्यवर्द्धन होगा, जिससे बर्बादी में कमी आएगी और बेहतर बाज़ार मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- इससे वन उपज संग्राहकों और स्थानीय किसानों की आय में प्रत्यक्ष वृद्धि होने की उम्मीद है।
- बाज़ार संबंध: रायपुर, विशाखापत्तनम और अन्य प्रमुख शहरी केंद्रों की पहचान संभावित बाज़ारों के रूप में की गई है।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)
- परिचय:
- कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना (संपदा) को मई 2017 में स्वीकृत किया गया था, जिसे बाद में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) नाम दिया गया।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य खे़त से लेकर खुदरा तक आधुनिक अवसंरचना तथा कुशल आपूर्ति शृंखलाओं का विकास करना है।
- यह खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देती है, किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में सहायक होती है, ग्रामीण रोज़गार सृजित करती है, कृषि बर्बादी को कम करती है, खाद्य प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाती है तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करती है।
- उद्देश्य: कृषि को समर्थन देना, खाद्य प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना तथा कृषि अपशिष्ट को कम करना।
- मुख्य घटक:
- नोडल मंत्रालय: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
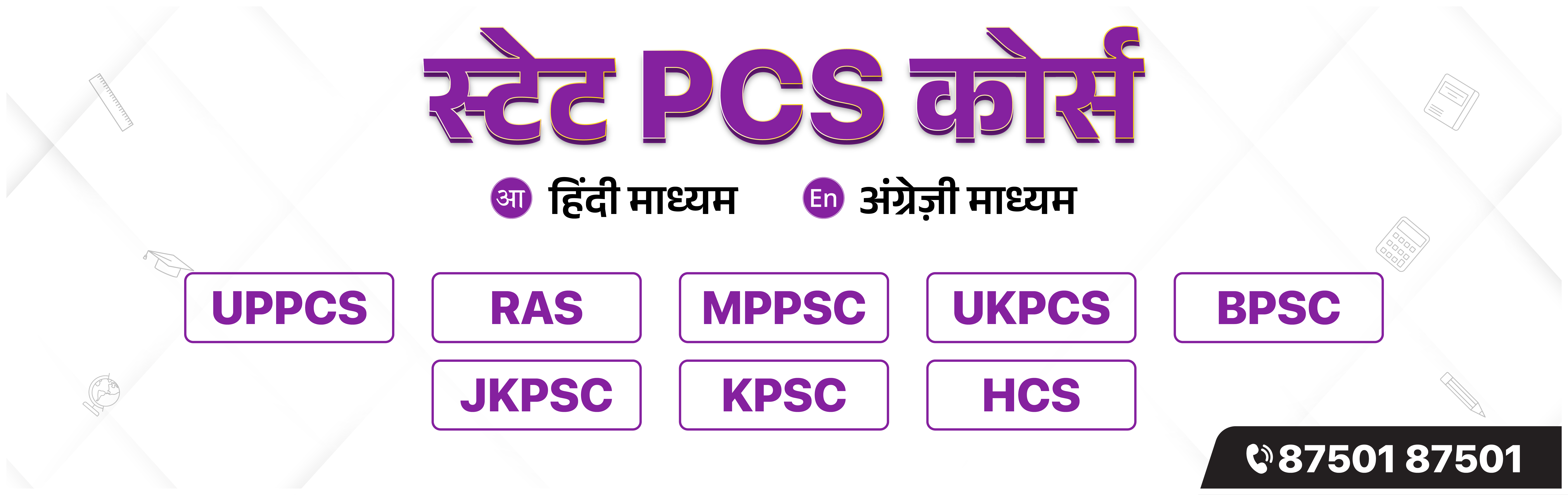
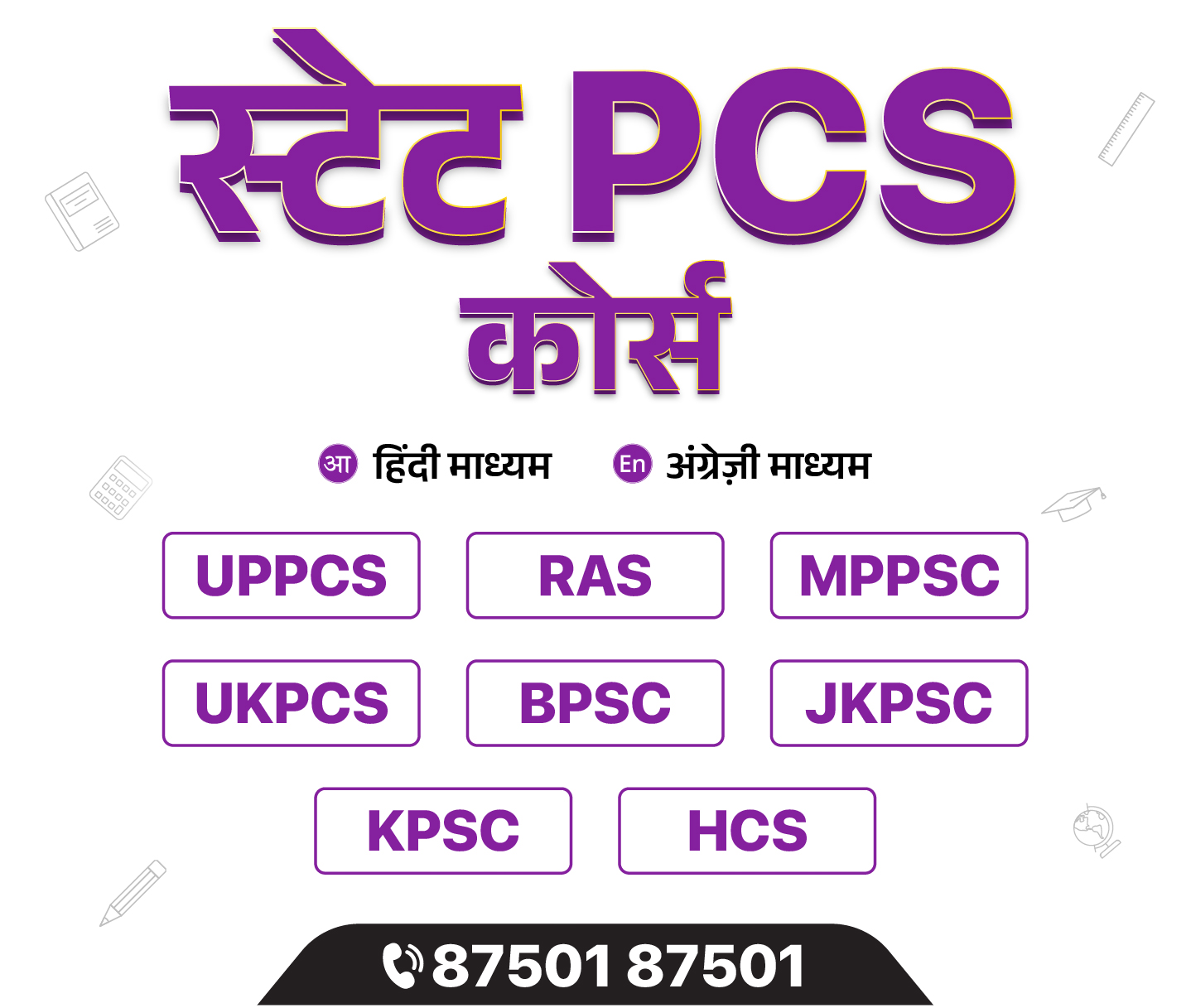


%20(1).gif)
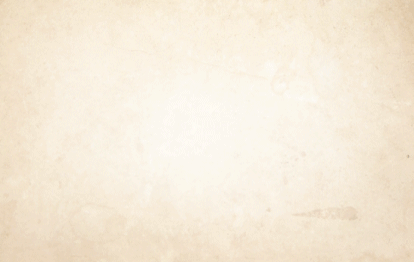

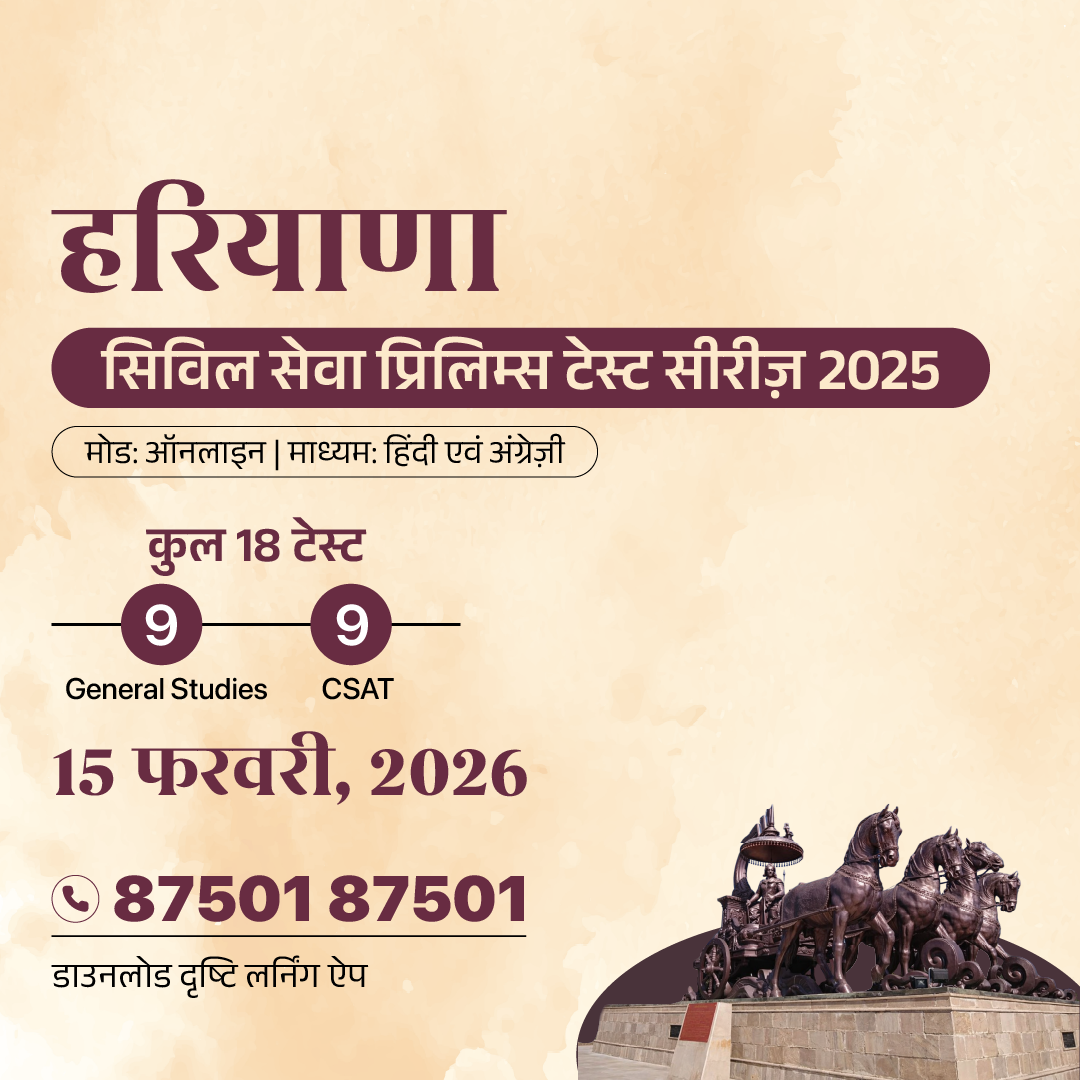
.jpg)
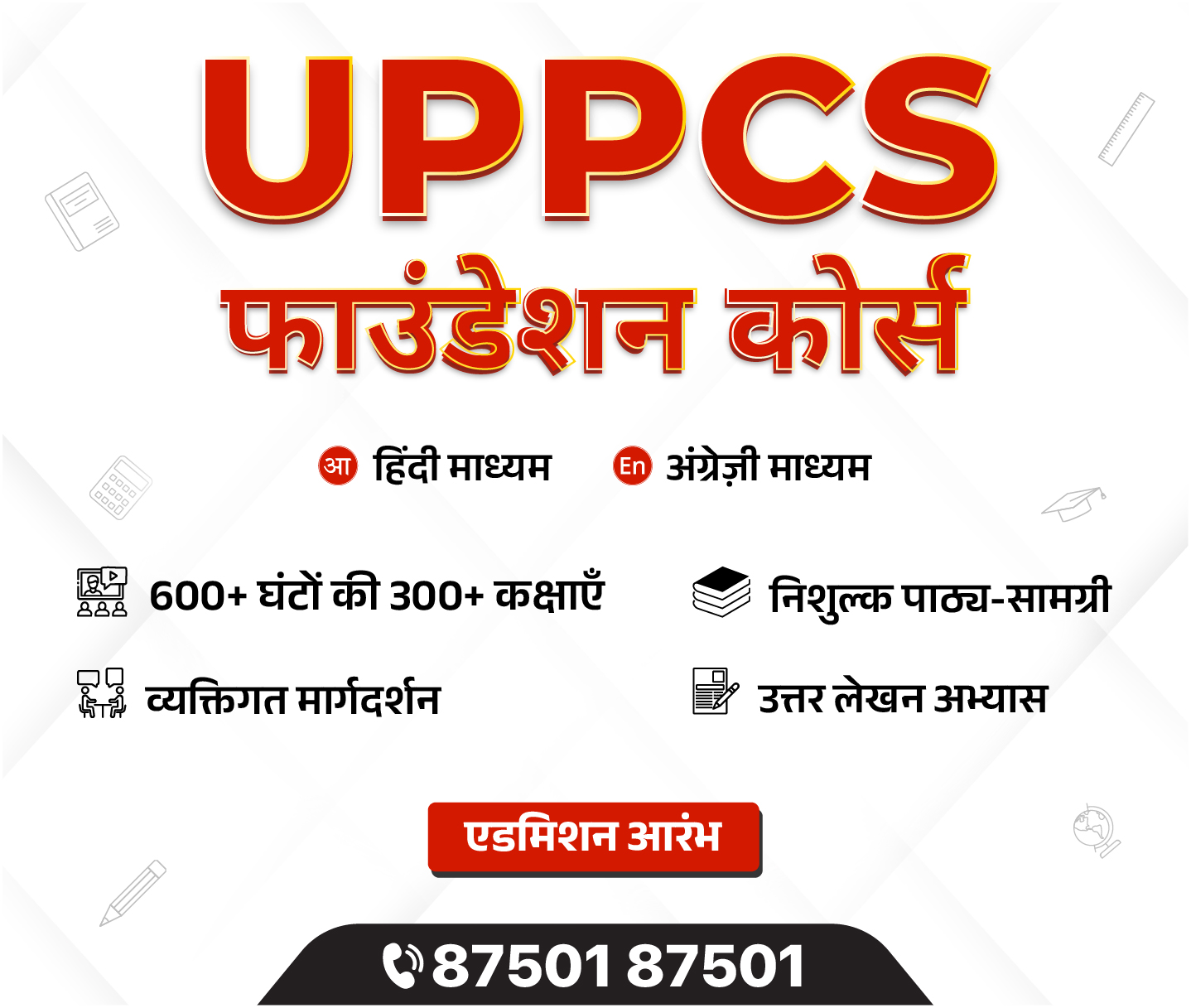
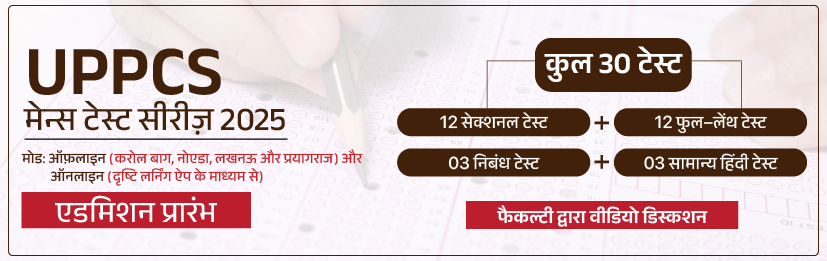
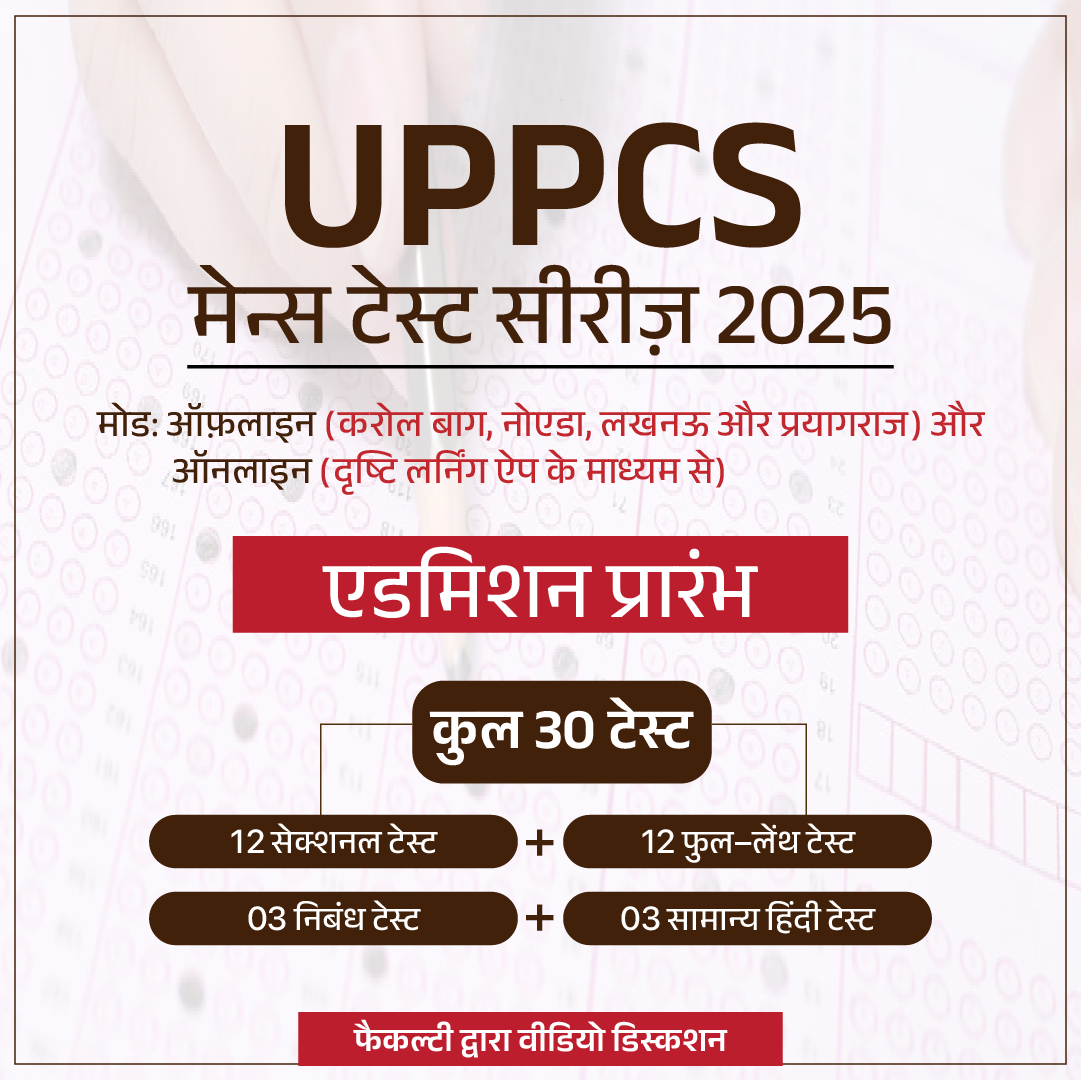

 PCS परीक्षण
PCS परीक्षण

