- फ़िल्टर करें :
- सैद्धांतिक प्रश्न
- केस स्टडीज़
-
प्रश्न :
प्रश्न. "करुणा एक आवश्यकता है, विलासिता नहीं। इसके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती।" नियम-आधारित शासन से समझौता किये बिना लोक सेवक करुणा को संस्थागत किस प्रकार बना सकते हैं? (150 शब्द)
10 Jul, 2025 सामान्य अध्ययन पेपर 4 सैद्धांतिक प्रश्नउत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
- कथन को उचित ठहराने के लिये किसी उद्धरण का हवाला देकर उत्तर की शुरुआत कीजिये
- कथन के लिये मुख्य तर्क दीजिये
- नियम-आधारित शासन से समझौता किये बिना करुणा को संस्थागत बनाने के उपाय सुझाइये
- उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय:
भारतीय दर्शन यह सिखाता है कि सभी प्राणी आपस में जुड़े हुए हैं (वसुधैव कुटुंबकम – "पूरा विश्व एक परिवार है")। इस दृष्टिकोण में, करुणा अर्थात् दूसरों के दुःख को समझने और उसे दूर करने के लिये कार्य करने की नैतिक प्रेरणा कोई विकल्प नहीं, बल्कि नैतिक मानव आचरण के लिये अनिवार्य है।
- लोक प्रशासन के संदर्भ में, इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि शासन में वैधानिकता और मानवता का मिश्रण होना चाहिये।
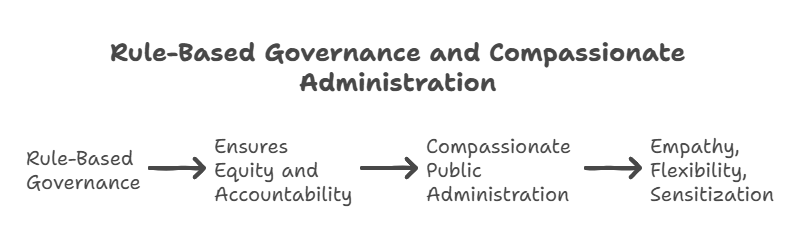
मुख्य भाग:
करुणा: एक आवश्यकता, मानवता के लिये अपरिहार्य:
- करुणा शासन को मानवीय बनाती है: प्रक्रियाओं और मापदंडों द्वारा तेजी से संचालित दुनिया में, करुणा यह सुनिश्चित करती है कि प्रशासन नागरिक-केंद्रित और मानवीय बना रहे।
- यह सद्गुण नैतिकता (अरस्तू) के साथ संरेखित है, जहाँ करुणा एक नैतिक गुण है जो चरित्र विकास के माध्यम से नैतिक आचरण को सक्षम बनाता है।
- करुणा सामाजिक एकजुटता और विश्वास को बढ़ावा देती है: जब नागरिक सार्वजनिक संस्थानों से सहानुभूति और देखभाल का अनुभव करते हैं, तो उनमें विश्वास और सहयोग विकसित होता है, जो लोकतांत्रिक वैधता और सामाजिक स्थिरता के लिए आवश्यक है।
- उपयोगितावादी नैतिकता यह दर्शाते हुए इसका समर्थन करती है कि करुणामय शासन से अधिक खुशी और सामाजिक सद्भाव प्राप्त होता है, जो एक प्रमुख नैतिक परिणाम है।
- नैतिक निर्णय लेने में करुणा आवश्यक है: कानून हर नैतिक दुविधा को कवर नहीं कर सकता; करुणा विवेकाधीन नैतिक निर्णय को सक्षम बनाती है, विशेष रूप से कमज़ोर या हाशिये पर पड़े समूहों से जुड़े मामलों में।
- काण्टीय नैतिकता यह मानती है कि व्यक्तियों को स्वयं में साध्य (साधन नहीं) मानकर उनके साथ व्यवहार करने के लिये करुणामय कार्यों के माध्यम से उनकी गरिमा को मान्यता देना आवश्यक है।
- करुणा मूल सभ्यतागत और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रतिबिम्बित करती है: भारतीय दर्शन में, करुणा धर्म और करुणा की परंपराओं में गहराई से समाहित है। यह कोई भावनात्मक विलासिता नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत कर्त्तव्य है।
- यह गांधीवादी नैतिकता और बौद्ध नैतिक विचारों से मेल खाता है, जो नैतिक और आध्यात्मिक जीवन के केंद्र में करुणा को रखते हैं।
नियम-आधारित शासन से समझौता किये बिना करुणा को संस्थागत बनाना:
- नियमों की करुणामय व्याख्या: न्यायोन्मुखी मानसिकता के साथ नियमों को लागू करना, जहाँ कठोर प्रवर्तन से नुकसान हो सकता है, वहाँ सम्मान और राहत सुनिश्चित करना।
- उदाहरण: लॉकडाउन के दौरान, कई ज़िला मजिस्ट्रेट कार्यालयों ने अपने तात्कालिक अधिदेशों से परे जाकर प्रवासी श्रमिकों के लिये भोजन और आश्रय की व्यवस्था की।
- नीति और कार्यक्रम डिज़ाइन में अंतर्निहित सहानुभूति: नागरिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी कार्यक्रमों को डिज़ाइन (विशेष रूप से हाशिये पर रहने वाले वर्गों के लिये) करना।
- उदाहरण: माताओं के लिये तेलंगाना की केसीआर किट- स्वास्थ्य और भावनात्मक ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील।
- नैतिक प्रशिक्षण और मूल्य सुदृढ़ीकरण: भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नैतिक तर्क को मज़बूत करने के लिये प्रशासनिक अकादमियों में करुणा-केंद्रित प्रशिक्षण की शुरूआत करना।
- अरस्तू की "फ्रोनेसिस" (व्यावहारिक ज्ञान) की अवधारणा के साथ संरेखित।
- गरिमापूर्ण पहुँच के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करना: डिजिटल उपकरण कुशलतापूर्वक तथा सहानुभूतिपूर्वक सेवाएँ प्रदान करने में मदद कर सकते हैं, जिससे उत्पीड़न और विवेकाधिकार में कमी आएगी।
- उदाहरण: पेंशनधारकों के लिये “डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र” वृद्ध नागरिकों पर बोझ को कम करता है।
- कार्रवाई में करुणा के रूप में शिकायत निवारण: नागरिकों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिये सशक्त बनाने से कानूनी समझौता किये बिना उत्तरदायी प्रणाली का निर्माण होता है।
- राजस्थान संपर्क पोर्टल, दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिकों से वास्तविक समय पर राहत और देखभाल प्राप्त की जा सकेगी।
निष्कर्ष:
"एक नियम-आधारित प्रणाली यदि करुणा से रहित हो, तो वह अत्याचार बन जाती है तथा करुणा यदि नियमों के बिना हो, तो अराजकता उत्पन्न करती है।" जनता की सच्ची सेवा तभी संभव है जब लोक प्रशासन में संरचना के साथ संवेदना भी हो। करुणा का संस्थागतकरण का अर्थ यह नहीं है कि नियमों को त्याग दिया जाए बल्कि यह है कि उन्हें संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाए।
To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.
Print




