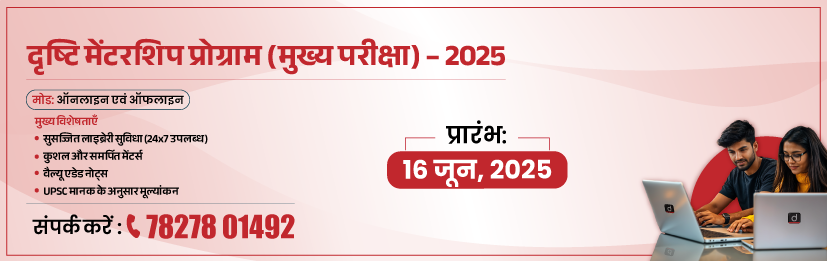शासन व्यवस्था
डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष
प्रिलिम्स के लिये:डिजिटल इंडिया, वित्तीय समावेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्टिकल फाइबर, यूपीआई, आधार, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC), गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM), इंडियाAI मिशन (2024-29), इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, कर्मयोगी भारत, iGOT, डिजीलॉकर, उमंग ऐप, भाषिनी, कॉमन सर्विस सेंटर, भारतनेट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम, 2023, साइबर सुरक्षित भारत, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। मेन्स के लिये:डिजिटल इंडिया का प्रदर्शन, डिजिटल इंडिया से जुड़े प्रमुख मुद्दे और डिजिटल इंडिया को मज़बूत करने के लिये आवश्यक उपाय। |
स्रोत: पी.आई.बी.
चर्चा में क्यों?
प्रधानमंत्री ने 1 जुलाई, 2025 को भारत के डिजिटल इंडिया पहल के सफलतापूर्वक 10 वर्ष पूरे होने की सराहना की, जो डिजिटल विभाजन को कम करने और प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के लिये वर्ष 2015 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल है।
- पिछले दशक (2015-25) में डिजिटल इंडिया ने इंटरनेट पहुँच, शासन, वित्तीय समावेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव किया है, जिससे भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बन गया है।
डिजिटल इंडिया की शुरुआत से अब तक की उपलब्धियाँ क्या हैं?
- डिजिटल अवसंरचना:
- दूरसंचार एवं इंटरनेट वृद्धि: वर्ष 2014 और वर्ष 2025 के बीच, टेलीफोन कनेक्शन 93.3 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ हो गए (टेली-घनत्व 75.23% से बढ़कर 84.49% हो गया), जबकि इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं में 285% की वृद्धि हुई तथा ब्रॉडबैंड कनेक्शन में 1,452% की वृद्धि हुई।
- 5G क्रांति: केवल 22 महीनों में 4.74 लाख 5G टावर स्थापित किये गए, जो 99.6% ज़िलों को कवर करते हैं, जबकि डेटा की लागत 308 रुपए/GB (2014) से घटकर 9.34 रुपए/GB (2022) हो गई।
- ग्रामीण भारत के लिये भारतनेट परियोजना: 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को 6.92 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ा गया है और 4G कनेक्टिविटी अब पूरे भारत में 6,15,836 गाँवों तक पहुँच गई है।
- डिजिटल वित्त:
- एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI): अप्रैल 2025 तक, UPI के माध्यम से 1,867.7 करोड़ लेन-देन संपन्न हुए, जिनका कुल मूल्य 24.77 लाख करोड़ रुपए रहा। यह आँकड़ा वर्ष 2023 के वैश्विक वास्तविक समय लेन-देन का 49% दर्शाता है। वर्तमान में, यह प्रणाली 7 से अधिक देशों में सक्रिय है।
- आधार और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT): अप्रैल 2025 तक, 142 करोड़ आधार आईडी तैयार की गई, जिससे DBT के माध्यम से 44 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किये जा सके तथा इससे 5.87 करोड़ फर्जी राशन कार्ड और 4.23 करोड़ डुप्लिकेट LPG कनेक्शन हटा दिये गए।
- ONDC और GeM: वर्ष 2025 तक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) से लाखों विक्रेता जुड़ चुके होंगे, जबकि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) में 22.5 लाख से अधिक विक्रेता और 1.6 लाख सरकारी खरीदार शामिल हैं।
- AI और सेमीकंडक्टर: इंडियाAI मिशन (2024-29) ने AI नवाचार, कंप्यूटिंग क्षमता, स्टार्टअप और नैतिक AI ढाँचे को बढ़ावा देने के लिये मई 2025 तक 34,000 से अधिक GPU तैनात किये हैं, जो इंडियाAI इनोवेशन सेंटर, AIकोश, फ्यूचर स्किल्स तथा सुरक्षित एवं विश्वसनीय AI जैसे स्तंभों पर आधारित हैं।
- भारत सेमीकंडक्टर मिशन 50% पूंजी सहायता के साथ चिप और डिस्प्ले विनिर्माण को समर्थन देता है, 1.55 लाख करोड़ रुपए की 6 परियोजनाओं को मंज़ूरी (5 निर्माणाधीन हैं) दी गई है।
- नागरिक सशक्तीकरण: कर्मयोगी भारत और iGOT ने 1.21 करोड़ अधिकारियों को शामिल किया है और 3.24 करोड़ शिक्षण प्रमाण-पत्र जारी किये हैं, जबकि डिजिलॉकर (53.92 करोड़ उपयोगकर्त्ताओं के साथ) तथा उमंग ऐप ( 8.34 करोड़ उपयोगकर्त्ताओं के साथ 23 भाषाओं में 2,300 से अधिक सेवाएँ प्रदान करना ) जैसे प्लेटफार्मों ने डिजिटल पहुँच और अधिकार को बढ़ाया है।
डिजिटल इंडिया पहल क्या है?
- परिचय: डिजिटल बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने, सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी सुनिश्चित करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिये 1 जुलाई, 2015 को डिजिटल इंडिया पहल शुरू की गई थी।
- उद्देश्य:
- डिजिटल विभाजन को कम करना: डिजिटल इंडिया का उद्देश्य डिजिटल रूप से सशक्त नागरिकों और प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच वाले लोगों के बीच की खाई को कम करना है।
- समावेशी डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करना: यह डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में समान भागीदारी को बढ़ावा देता है, जिससे सभी के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सरकारी सेवाओं तक पहुँच सक्षम होती है।
- आर्थिक विकास को बढ़ावा देना: प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाकर, यह पहल राष्ट्रव्यापी आर्थिक विकास का समर्थन करती है।
- जीवन की गुणवत्ता में सुधार: इसका उद्देश्य दैनिक जीवन के प्रमुख क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है।
- डिजिटल इंडिया पहल के नौ स्तंभ:
- ब्रॉडबैंड हाईवे: इसका उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी के लिये देश भर में हाई-स्पीड इंटरनेट का विस्तार करना है।
- मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुँच: यह डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिये दूर-दराज़ के क्षेत्रों में मोबाइल कवरेज सुनिश्चित करता है।
- पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम: यह वहनीय पहुँच और डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिये वंचित क्षेत्रों में सामान्य सेवा केंद्र स्थापित करता है ।
- ई-गवर्नेंस: यह बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता के लिये सरकारी सेवाओं को सुव्यवस्थित करता है।
- ई-क्रांति: यह MyGov.in जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन वितरित करता है, जिससे पहुँच में वृद्धि होती है।
- सभी के लिये सूचना: यह अभिलेखों के डिजिटलीकरण और नवाचार के लिये खुले डेटा को बढ़ावा देता है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण: यह स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देता है, आयात को कम करता है और रोज़गार सृजन करता है ।
- नौकरियों के लिये IT: यह डिजिटल साक्षरता और कौशल भारत जैसे मिशनों के माध्यम से युवाओं में IT कौशल का निर्माण करता है।
- अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम: यह ऑनलाइन प्रमाण-पत्र, डिजिटल उपस्थिति और सार्वजनिक वाई-फाई जैसी तत्काल डिजिटल आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- प्रमुख उपलब्धियाँ:
- डिजिटल इंडिया पहल: आधार (अद्वितीय 12-अंकीय बायोमेट्रिक ID), भारतनेट (ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड), डिजिटल लॉकर (दस्तावेज़ों का सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज), भीम UPI (सुरक्षित डिजिटल भुगतान), eSign ( डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके ऑनलाइन दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर), MyGov (शासन में नागरिक भागीदारी) आदि।
डिजिटल इंडिया पहल से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?
- डिजिटल डिवाइड: भारत का डिजिटल विकास असमान बना हुआ है, ग्रामीण इंटरनेट पहुँच और डिजिटल साक्षरता केवल 37% (2023) है, जो क्षेत्रों तथा सामाजिक-आर्थिक समूहों में भारी अंतर को उजागर करता है।
- साइबर सुरक्षा खतरे: बढ़ते डिजिटल उपयोग के कारण 13.91 लाख साइबर सुरक्षा घटनाएँ (2022) हुई हैं, लेकिन भारत को 8 लाख साइबर सुरक्षा पेशेवरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो कमज़ोर साइबर सुरक्षा को उजागर करता है।
- डेटा गोपनीयता: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के बावजूद, प्रवर्तन और डेटा दुरुपयोग को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं, जिसमें 61% कंपनियाँ कथित तौर पर सहमति मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं।
- बुनियादी ढाँचे की बाधाएँ: कम ब्रॉडबैंड स्पीड, अनियमित 5G और खराब फाइबर-ऑप्टिक कवरेज, विशेष रूप से दूर-दराज़ के क्षेत्रों में, डिजिटल पहुँच को सीमित करते हैं, मोबाइल इंटरनेट स्पीड (2024) में भारत 25वें स्थान पर था।
- विनियामक चुनौतियाँ: बार-बार नीतिगत बदलाव, क्षेत्राधिकारों का ओवरलैप होना और स्पेक्ट्रम नीलामी में देरी से 5G रोलआउट में बाधा आती है तथा डेटा स्थानीयकरण लागत के साथ व्यवसायों पर बोझ पड़ता है।
- सार्वजनिक डिजिटल प्रणाली के मुद्दे: CoWIN और आधार जैसे प्लेटफॉर्म को विशेष रूप से गैर-शहरी क्षेत्रों में मापनीयता, सटीकता एवं धोखाधड़ी की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- पर्यावरणीय प्रभाव: डिजिटल विकास ने ई-अपशिष्ट को 1.01 मीट्रिक टन (2019-20) से बढ़ाकर 1.751 मीट्रिक टन (2023-24) कर दिया है, जिससे कमज़ोर ई-अपशिष्ट प्रबंधन तथा डेटा केंद्रों में उच्च ऊर्जा उपयोग के कारण स्थिति और खराब हो गई है।
डिजिटल इंडिया पहल को और मज़बूत करने हेतु क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?
- डिजिटल डिवाइड को पाटना: भारतनेट परियोजना और पीएम-वाणी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढाँचे का विस्तार करना, उपकरणों पर सब्सिडी देना और पहुँच बढ़ाने के लिये क्षेत्रीय भाषा की सामग्री को बढ़ावा देना।
- सहायक तकनीक को अनिवार्य बनाना, किफायती इंटरनेट का समर्थन करना तथा हाशिये पर पड़े समूहों के लिये सुगम्य भारत को डिजिटल इंडिया के साथ एकीकृत करना।
- साइबर सुरक्षा को बढ़ाना: एक व्यापक रणनीति विकसित करना, साइबर सुरक्षित भारत का विस्तार करना कौशल भारत के तहत पेशेवरों को प्रशिक्षित करना और पीएलआई योजनाओं के माध्यम से स्वदेशी साइबर सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करना।
- डेटा गोपनीयता को मज़बूत करना: DPDP अधिनियम, 2023 को प्रभावी ढंग से लागू करना, क्षेत्रीय डेटा संरक्षण कार्यालय स्थापित करना और डेटा स्थानीयकरण दिशा-निर्देशों को स्पष्ट करना।
- डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना: साइबर जागरूकता और डिजिटल कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिये, आउटरीच में सामुदायिक चैंपियनों की भागीदारी के साथ PMGDISHA कार्यक्रम का विस्तार किया जाना।
- ई-कचरा प्रबंधन: स्वच्छ भारत को ई-अपशिष्ट संग्रहण से जोड़ने के लिये एक राष्ट्रीय ढाँचा बनाना, हरित स्टार्टअप का समर्थन करना और पीएलआई को पर्यावरण अनुकूल तकनीक तक विस्तारित करना।
- डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का एकीकरण: सेवा वितरण में सुधार और नौकरशाही देरी को कम करने के लिये आधार, यूपीआई तथा डिजीलॉकर जैसे प्लेटफार्मों को जोड़ें।
निष्कर्ष
अपनी 10 वर्ष की यात्रा में डिजिटल इंडिया ने सेवा वितरण, आर्थिक सशक्तीकरण और नागरिक भागीदारी में क्रांतिकारी बदलाव किया है। हालाँकि डिजिटल डिवाइड, साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। रणनीतिक सुधारों, समावेशी बुनियादी ढाँचे और मज़बूत विनियमन के साथ, डिजिटल इंडिया विकसित भारत की आधारशिला बन सकता है, जिससे न्यायसंगत और सतत् डिजिटल विकास संभव हो सकेगा।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: डिजिटल इंडिया ने तकनीकी अंतर को पाट दिया है, लेकिन अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत के डिजिटल परिवर्तन (2015-2025) के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न: निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2022)
उपर्युक्त में से कौन-से ओपन-सोर्स डिजिटल प्लेटफाॅर्म पर बनाए गए हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत सरकार के ‘डिजिटल इंडिया’ योजना का/के उद्देश्य है/हैं? (2018)
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) प्रश्न: कभी-कभी समाचारों में दिखने वाले 'डिजीलॉकर' के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न. "चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के प्रादुर्भाव ने ई-गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की"। चर्चा कीजिये। (2020) प्रश्न. 'डिजिटल भारत' कार्यक्रम कृषि उत्पादकता और आय को बढ़ाने में किसानों की किस प्रकार सहायता कर सकता है? सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं? (2015) |