उत्तराखंड Switch to English
गढ़वाल राइफल्स के नए कर्नल ऑफ द रेजिमेंट
चर्चा में क्यों?
अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने उत्तराखंड के लैंसडाउन स्थित गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित एक समारोह में गढ़वाल राइफल्स के 23वें 'कर्नल ऑफ द रेजिमेंट' के रूप में आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण किया है। वे लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि का स्थान लेंगे।
मुख्य बिंदु
- गढ़वाल राइफल्स:
- गढ़वाल राइफल्स भारतीय सेना की एक प्रतिष्ठित पैदल सेना रेजिमेंट है, जिसकी स्थापना वर्ष 1887 में बंगाल सेना की 39वीं (गढ़वाल) रेजिमेंट के रूप में की गई थी।
- यह रेजिमेंट आगे चलकर ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा बनी तथा भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इसे भारतीय सेना में समाहित कर लिया गया।
- इस रेजिमेंट के सैनिक मुख्यतः उत्तराखंड के सात गढ़वाली ज़िलों— उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल तथा हरिद्वार से आते हैं। गढ़वाल स्काउट्स, जो जोशीमठ में तैनात हैं, को "हिम तेंदुआ" उपनाम दिया गया है।
- इस रेजिमेंट की पहचान वीरता, साहस तथा राष्ट्र सेवा की सशक्त विरासत से है, जो गढ़वाली योद्धाओं की गौरवशाली परंपरा को दर्शाती है। इसने दोनों विश्व युद्धों तथा स्वतंत्रता के पश्चात हुए अनेक सैन्य संघर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
- इसने वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध तथा वर्ष 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्धों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- यह रेजिमेंट श्रीलंका में ऑपरेशन पवन जैसे शांति अभियानों में अपनी प्रभावी भूमिका के लिये भी जानी जाती है।
- रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है– "युद्धाय कृत निश्चय" अर्थात् "दृढ़ संकल्प के साथ लड़ो"।
- इसका प्रतीक चिह्न माल्टीज़ क्रॉस है, जो अब समाप्त हो चुकी राइफल ब्रिगेड (प्रिंस कंसोर्ट्स ओन) से प्रेरित है।
- गढ़वाल राइफल्स ने अब तक कई प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान प्राप्त किये हैं, जिनमें तीन विक्टोरिया क्रॉस तथा एक अशोक चक्र शामिल हैं।
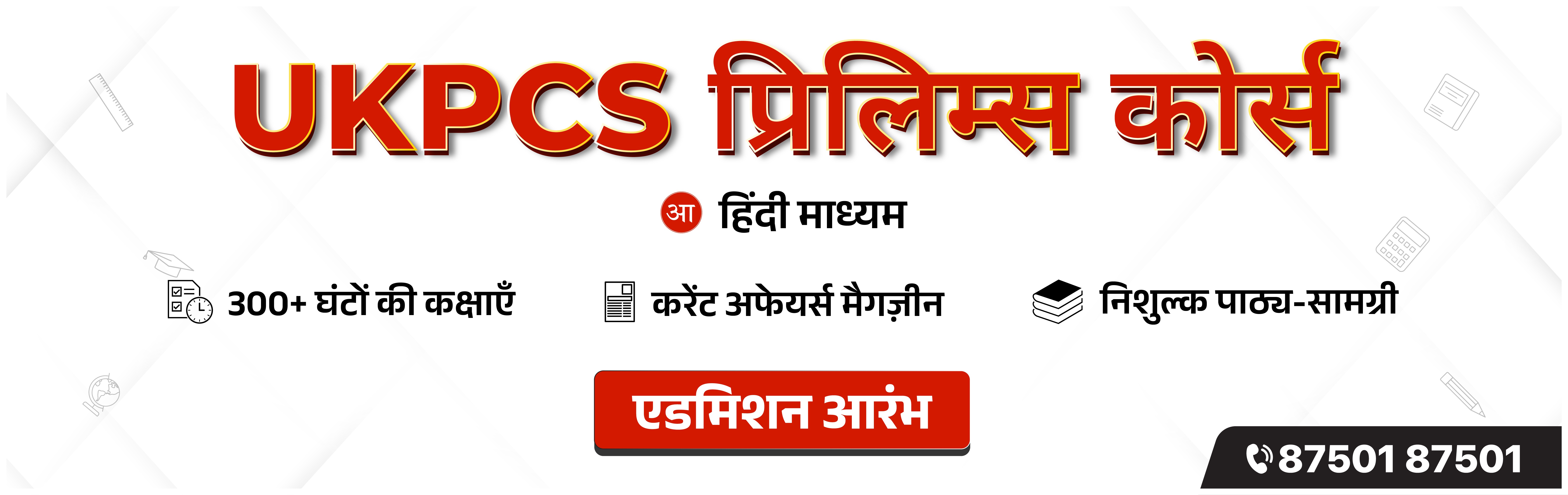
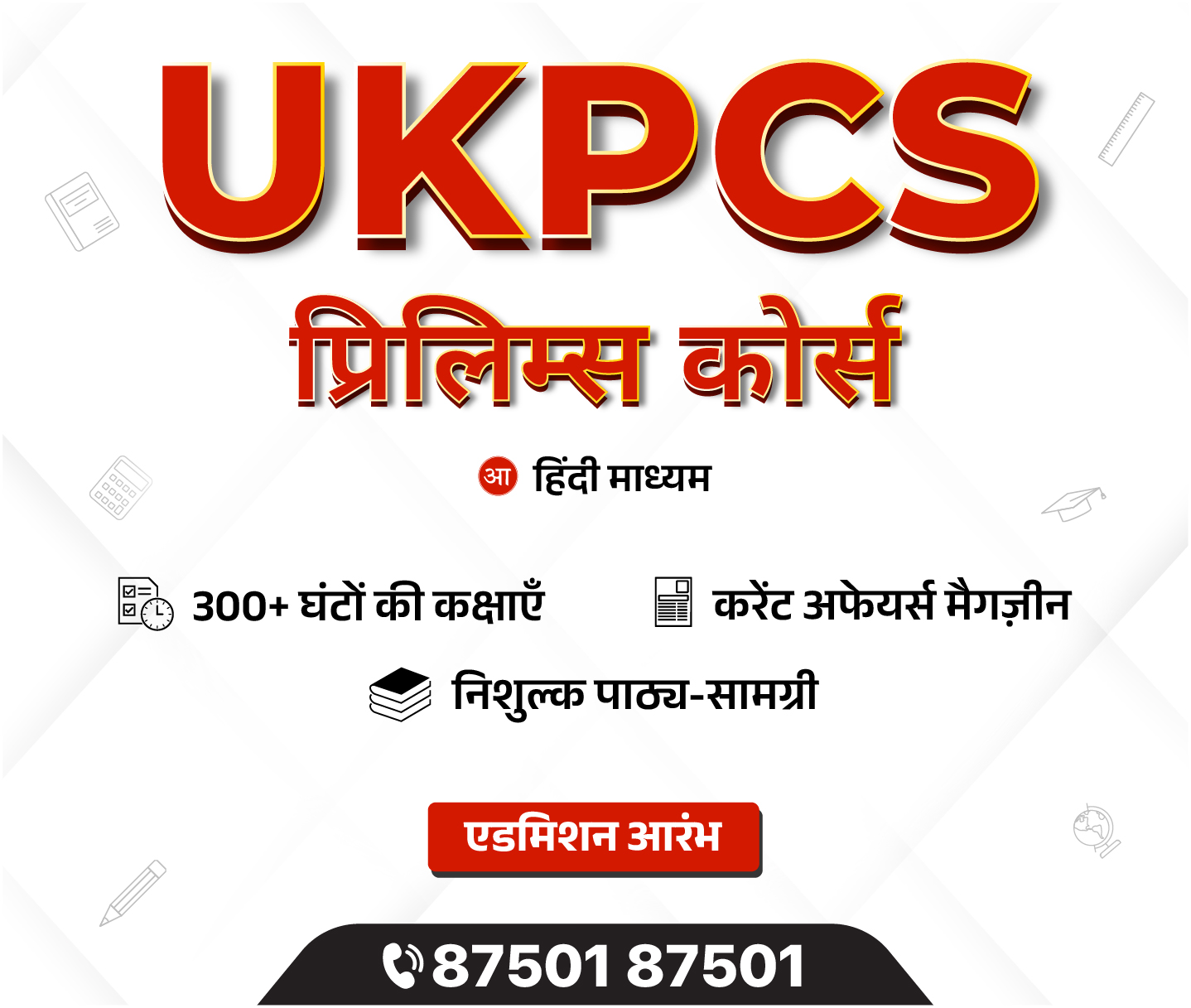
हरियाणा Switch to English
अरावली वनों में कचरा डंपिंग
चर्चा में क्यों?
हरियाणा वन विभाग ने नूंह के अरावली वन क्षेत्र में निर्माण मलबा तथा औद्योगिक कचरा अवैध रूप से फेंकने के लिये तीन फर्मों पर जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
- इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223(B) और धारा 324(3) के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत विधिक कार्रवाई आरंभ की गई है।
मुख्य बिंदु
- अरावली के बारे में:
- अरावली विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, इसकी आयु लगभग तीन अरब वर्ष आंकी गई है।
- यह पर्वतमाला गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है (राजस्थान और हरियाणा होते हुए)।
- इसकी सबसे ऊँची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है।
- जलवायु पर प्रभाव:
- अरावली पर्वतमाला उत्तर-पश्चिम भारत और उससे आगे के क्षेत्रों की जलवायु पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालती है।
- मानसून के दौरान, पर्वत शृंखला मानसून के बादलों को धीरे-धीरे शिमला और नैनीताल की दिशा में अग्रसर करती है, जिससे उप-हिमालयी नदियों को पोषण मिलता है और उत्तर भारतीय मैदानों की सिंचाई संभव होती है।
- सर्दियों के महीनों में यह उपजाऊ जलोढ़ नदी घाटियों (सिंधु और गंगा) को मध्य एशिया से ठंडी पश्चिमी हवाओं के हमले से बचाती है।
- अरावली पर्वतमाला की पारिस्थितिक भूमिका:
- अरावली पर्वतमाला थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोककर मरुस्थलीकरण के विरुद्ध एक प्राकृतिक ढाल का कार्य करती है।
- यह दिल्ली, जयपुर और गुरुग्राम जैसे प्रमुख शहरों को मरुस्थली अतिक्रमण और बढ़ती शुष्कता से संरक्षित रखती है।
- नदियाँ:
- यह शृंखला चंबल, साबरमती और लूनी सहित कई महत्त्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है।
- ये नदियाँ उत्तर-पश्चिमी भारत में कृषि, पेयजल और क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- जैव विविधता हॉटस्पॉट:
- अरावली के वन, घास के मैदान तथा आर्द्रभूमि कई लुप्तप्राय पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लिये आश्रय स्थल हैं, जिससे यह एक महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी आवास बन गया है।
- अरावली पारिस्थितिकी तंत्र के लिये खतरे:
- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2009 में हरियाणा के फरीदाबाद, गुणगाँव (अब गुरुग्राम) और नूँह ज़िलों की अरावली रेंज में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।
- अवैध खनन, अत्यधिक चारण और मानव अधिवास पूरे क्षेत्र में भूमि क्षरण को तेज़ कर रही हैं।
- ये गतिविधियाँ भूमिगत जलभृतों को क्षति पहुँचा रही हैं, झीलों को शुष्क बना रही हैं तथा वन्यजीवों और जैवविविधता को सहारा देने की पर्वत शृंखला की क्षमता को कमज़ोर कर रही हैं।
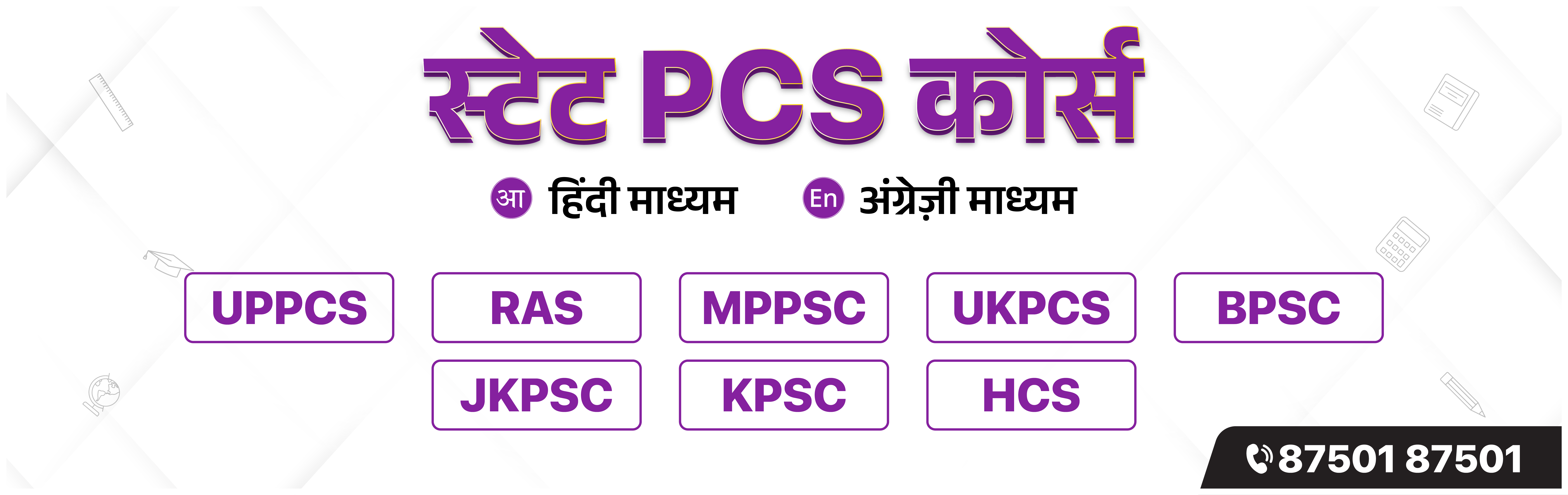
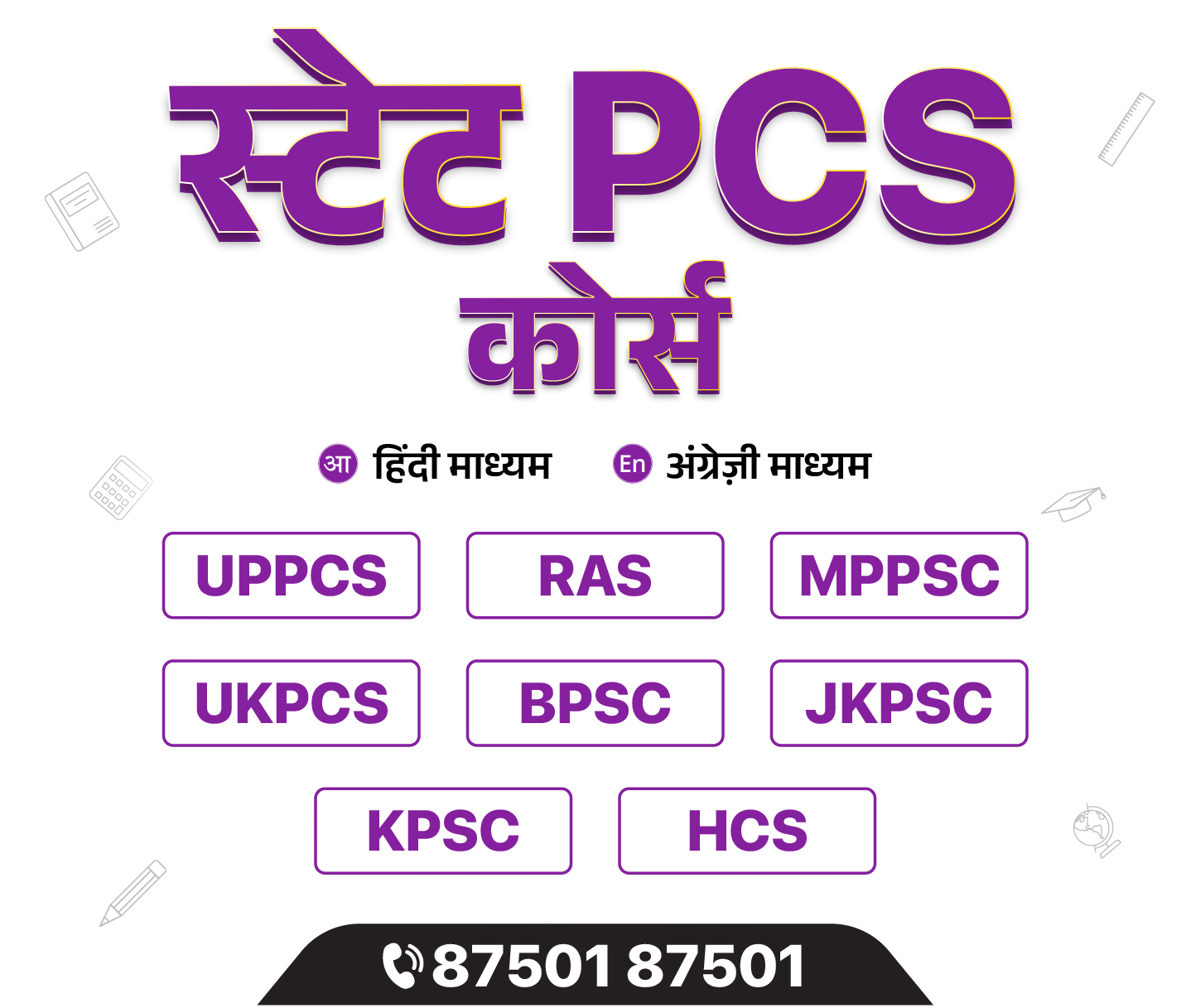
उत्तराखंड Switch to English
उत्तराखंड में बादल फटने की घटना
चर्चा में क्यों?
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से भूस्खलन हुआ, प्रमुख तीर्थयात्रा मार्ग बाधित हुए तथा कई श्रमिक लापता हो गए।
- बाढ़ और भूस्खलन की आशंका वाले ज़िलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
मुख्य बिंदु
- बादल फटना (Cloudburst):
- बादल फटना एक अचानक और तीव्र वर्षा की घटना होती है, जिसमें लगभग 10 वर्ग किमी क्षेत्र में एक घंटे से भी कम समय में 10 सेमी से अधिक वर्षा हो जाती है।
- यह ओलावृष्टि और गरज के साथ भी हो सकती है। बादल फटना विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में सामान्य घटना है।
- स्थानीय प्रकृति के कारण इसकी पहले से भविष्यवाणी करना या पता लगाना कठिन होता है, लेकिन इससे अचानक विनाशकारी वर्षा हो सकती है, जिससे अचानक बाढ़ और भूस्खलन की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।
- भूस्खलन (Landslide):
- परिभाषा: भूस्खलन वह प्रक्रिया है, जिसमें चट्टानों, मिट्टी या मलबे का ढलान की दिशा में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे की ओर खिसकना होता है।
- यह द्रव्यमान क्षरण (mass wasting) का एक रूप है, जिसमें पृथ्वी की सामग्री ढलान पर नीचे की ओर सरकती है।
- कारण: भारी वर्षा, भूकंप तथा जल रिसाव जैसे प्राकृतिक कारक ढलानों को कमज़ोर करते हैं, जबकि वनों की कटाई और निर्माण कार्यों जैसी मानव गतिविधियाँ इस जोखिम को बढ़ाती हैं।
- मिट्टी की संरचना और भू-आकृति जैसे भौगोलिक कारक भी ढलान की स्थिरता को प्रभावित करते हैं और भूस्खलन का कारण बन सकते हैं।
- आकस्मिक बाढ़ (Flash Floods):
- परिभाषा:
- आकस्मिक बाढ़ वह स्थिति होती है, जब तीव्र वर्षा के दौरान या तुरंत बाद जल स्तर में तीव्र वृद्धि होती है।
- ये अत्यधिक स्थानीयकृत और अल्पकालिक घटनाएँ हैं, जो आमतौर पर वर्षा के 6 घंटे के भीतर घटित होती हैं।
- कारण:
- आकस्मिक बाढ़ मुख्यतः तीव्र वर्षा के कारण होती है, जो मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता और जल निकासी प्रणालियों को प्रभावित करती है।
- भारी वर्षा के अतिरिक्त, तापमान में अचानक वृद्धि से होनेवाली शीघ्र हिम पिघलन, बाँध या तटबंध का टूटना, बर्फ या मलबे की रुकावट तथा ग्लेशियर झील का अचानक फटना भी इसके कारण हो सकते हैं।
- इसके अलावा, शहरीकरण के चलते सड़कों और इमारतों जैसी अवशोषण-रहित सतहों से जल का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी में जल समावेशन कम होकर बाढ़ का खतरा और बढ़ जाता है।
- परिभाषा:

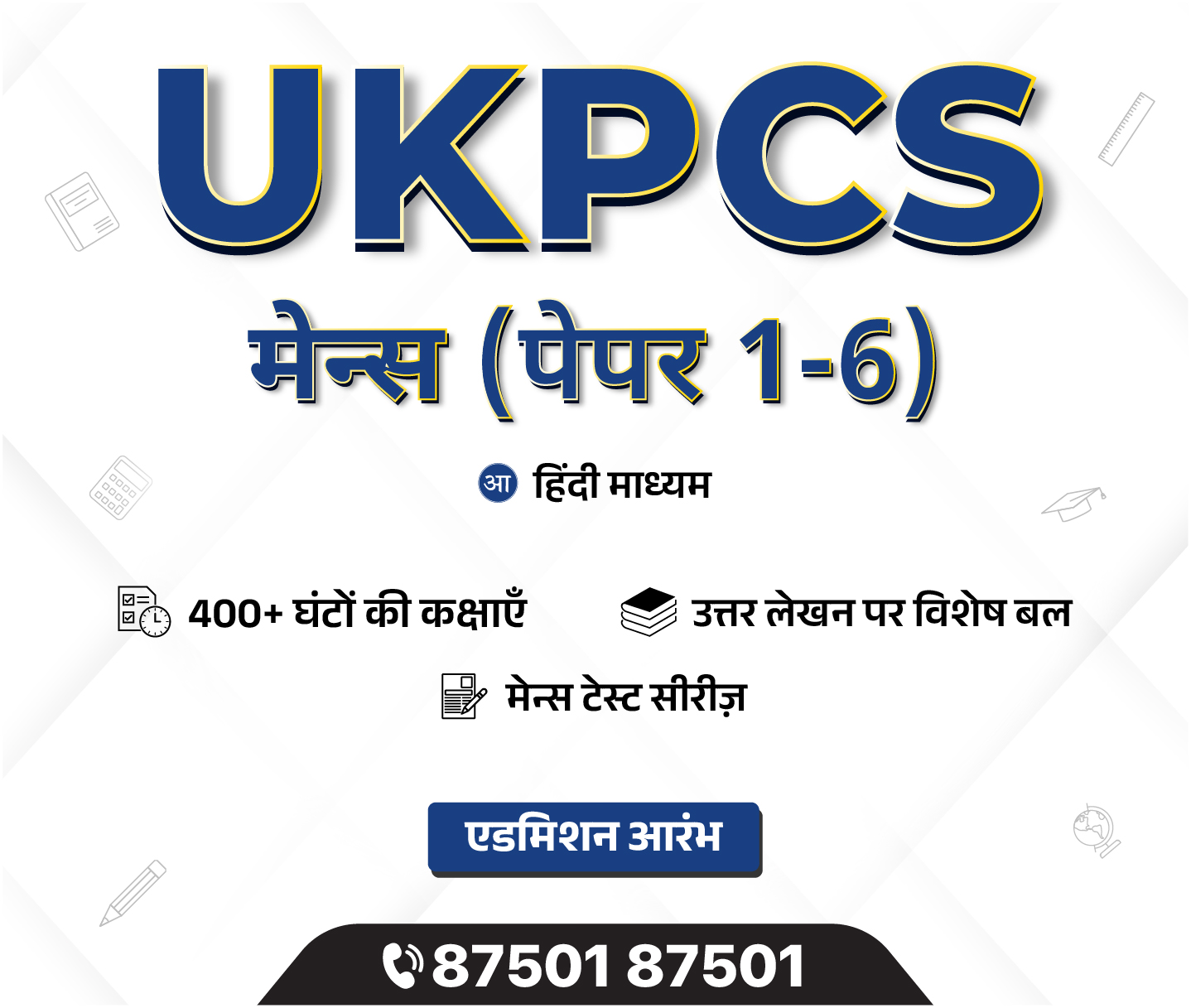
झारखंड Switch to English
हुल दिवस 2025
चर्चा में क्यों?
हुल दिवस (30 जून, 2025) पर प्रधानमंत्री ने भारत के आदिवासी समुदायों के साहस को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले संथाल हुल आदिवासी शहीदों की विरासत को सम्मानित किया।
मुख्य बिंदु
- 1855 के संथाल हुल के बारे में:
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 1855 का संथाल हुल भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सबसे शुरुआती किसान विद्रोहों में से एक था। चार भाइयों- सिद्धो, कान्हो, चाँद और भैरव मुर्मू तथा बहनों फूलो और झानो के नेतृत्व में, विद्रोह 30 जून 1855 को शुरू हुआ।
- विद्रोह का लक्ष्य न केवल अंग्रेज़ थे, बल्कि उच्च जातियाँ, ज़मींदार, दरोगा और साहूकार भी थे, जिन्हें सामूहिक रूप से 'दिकू' कहा जाता था।
- इसका उद्देश्य संथाल समुदाय के आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना था।
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 1855 का संथाल हुल भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सबसे शुरुआती किसान विद्रोहों में से एक था। चार भाइयों- सिद्धो, कान्हो, चाँद और भैरव मुर्मू तथा बहनों फूलो और झानो के नेतृत्व में, विद्रोह 30 जून 1855 को शुरू हुआ।
- विद्रोह की उत्पत्ति:
- वर्ष 1832 में कुछ क्षेत्रों को ‘संथाल परगना’ या ‘दामिन-ए-कोह’ नाम दिया गया, जिसमें वर्तमान झारखंड में साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, पाकुड़ और जामताड़ा के कुछ हिस्से शामिल हैं।
- यह क्षेत्र संथालों को दिया गया था, जो बंगाल प्रेसीडेंसी के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से विस्थापित हुए थे।
- संथाल क्षेत्र में बँधुआ मज़दूरी की दो प्रणालियाँ उभरीं, जिन्हें कामियोती और हरवाही के नाम से जाना जाता है।
- संथालों को दामिन-ए-कोह में बसने और कृषि करने का वादा किया गया था, लेकिन इसके बदले उन्हें दमनकारी भूमि हड़पने तथा बेगारी (बँधुआ मज़दूरी) का सामना करना पड़ा।
- कामियोती के तहत, ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता के लिये काम करना पड़ता था, जबकि हरवाही के तहत, ऋणदाता को व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान करनी पड़ती थीं और आवश्यकतानुसार ऋणदाता के खेत की जुताई करनी पड़ती थी। बॉन्ड की शर्तें इतनी सख्त थीं कि संथाल के लिये अपने जीवनकाल में ऋण चुकाना लगभग असंभव था।
- वर्ष 1832 में कुछ क्षेत्रों को ‘संथाल परगना’ या ‘दामिन-ए-कोह’ नाम दिया गया, जिसमें वर्तमान झारखंड में साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, पाकुड़ और जामताड़ा के कुछ हिस्से शामिल हैं।
- गुरिल्ला युद्ध एवं दमन:
- मुर्मू बँधुओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में लगभग 60,000 संथालों का नेतृत्व किया। छह महीने तक चले भयंकर प्रतिरोध के बावजूद, जनवरी 1856 में भारी जनहानि और तबाही के साथ विद्रोह का दमन दिया गया।
- 15,000 से ज़्यादा संथालों ने अपनी जान गँवाई और 10,000 से अधिक गाँवों का विनाश हुआ।
- हुल ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ़ शुरुआती प्रतिरोध को उजागर किया और यह आदिवासी लचीलेपन का प्रतीक बना हुआ है।
- प्रभाव: इस विद्रोह के परिणामस्वरूप ही संथाल परगना काश्तकारी (Santhal Pargana Tenancy- SPT) अधिनियम, 1876 पारित किया गया जो आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित करने को प्रतिबंधित करता है, केवल समुदाय के भीतर ही भूमि उत्तराधिकार की स्वीकृति देता है तथा संथालों को अपनी भूमि पर स्वयं शासन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
संथाल जनजाति
- जनसांख्यिकीय वितरण:
- संथाल भारत के सबसे बड़े जनजातीय समुदायों में से एक हैं, जो मुख्यतः झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा में केंद्रित हैं।
- भाषा:
- संथाल समुदाय की भाषा संथाली है, जो खेरवाड़ी बोली के अंतर्गत आती है तथा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की मुंडा शाखा से संबंधित है।
- व्यवसाय और आजीविका:
- कई संथाल लोग आसनसोल (पश्चिम बंगाल) के पास कोयला खदानों तथा जमशेदपुर (झारखंड) के इस्पात कारखानों में कार्यरत हैं।
- इसके अतिरिक्त, कुछ लोग मौसमी कृषि मजदूर के रूप में भी काम करते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में चावल की खेती उनकी आर्थिक गतिविधि का मुख्य आधार है।
- ग्राम प्रशासन:
- प्रत्येक संथाल गाँव का नेतृत्व एक वंशानुगत मुखिया करता है, जिसे बुजुर्गों की परिषद का सहयोग प्राप्त होता है। यह मुखिया न केवल प्रशासनिक बल्कि धार्मिक और औपचारिक कर्त्तव्यों का भी निर्वहन करता है।
- गाँवों का एक समूह मिलकर एक परगना बनाता है, जिसका नेतृत्व एक अन्य वंशानुगत मुखिया करता है।
- गोत्र और सामाजिक संरचना:
- संथाल समुदाय में 12 वंश (गोत्र) होते हैं, जो आगे पितृवंशीय उपविभागों में विभाजित हैं।
- गोत्रीय बहिर्विवाह प्रथा का सख्ती से पालन किया जाता है अर्थात् एक ही गोत्र के व्यक्ति आपस में विवाह नहीं कर सकते।
- प्रत्येक कबीले और उप-कबीले की सदस्यता के साथ पहनावे, भोजन, आवास तथा अनुष्ठानों के विशिष्ट नियम जुड़े होते हैं।
- संथालों में एकल विवाह प्रथा सामान्य है; यद्यपि बहुविवाह की अनुमति है, लेकिन यह दुर्लभ है।
- धर्म और विश्वास:
- संथाल पारंपरिक रूप से आत्माओं की पूजा करते हैं और अपने पैतृक पंथों, विशेष रूप से कबीले के मुखियाओं से संबंधित पंथों को विशेष महत्त्व देते हैं।
- उनकी आध्यात्मिक प्रथाएँ और धार्मिक अनुष्ठान, उनकी सांस्कृतिक पहचान का केंद्रीय हिस्सा हैं।
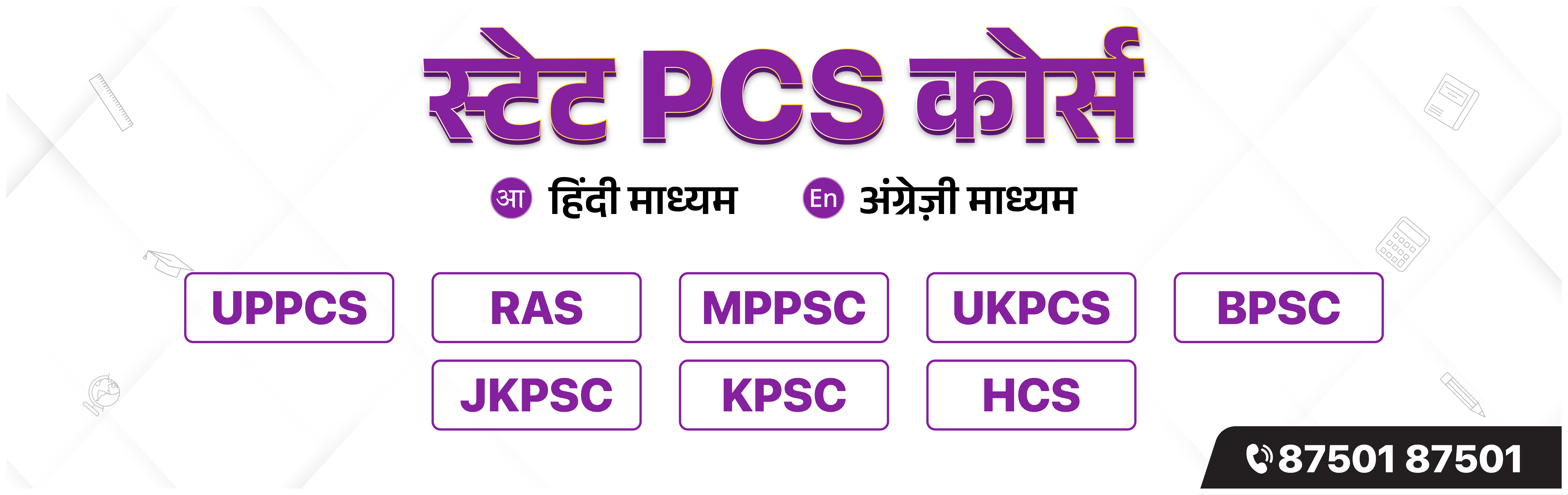
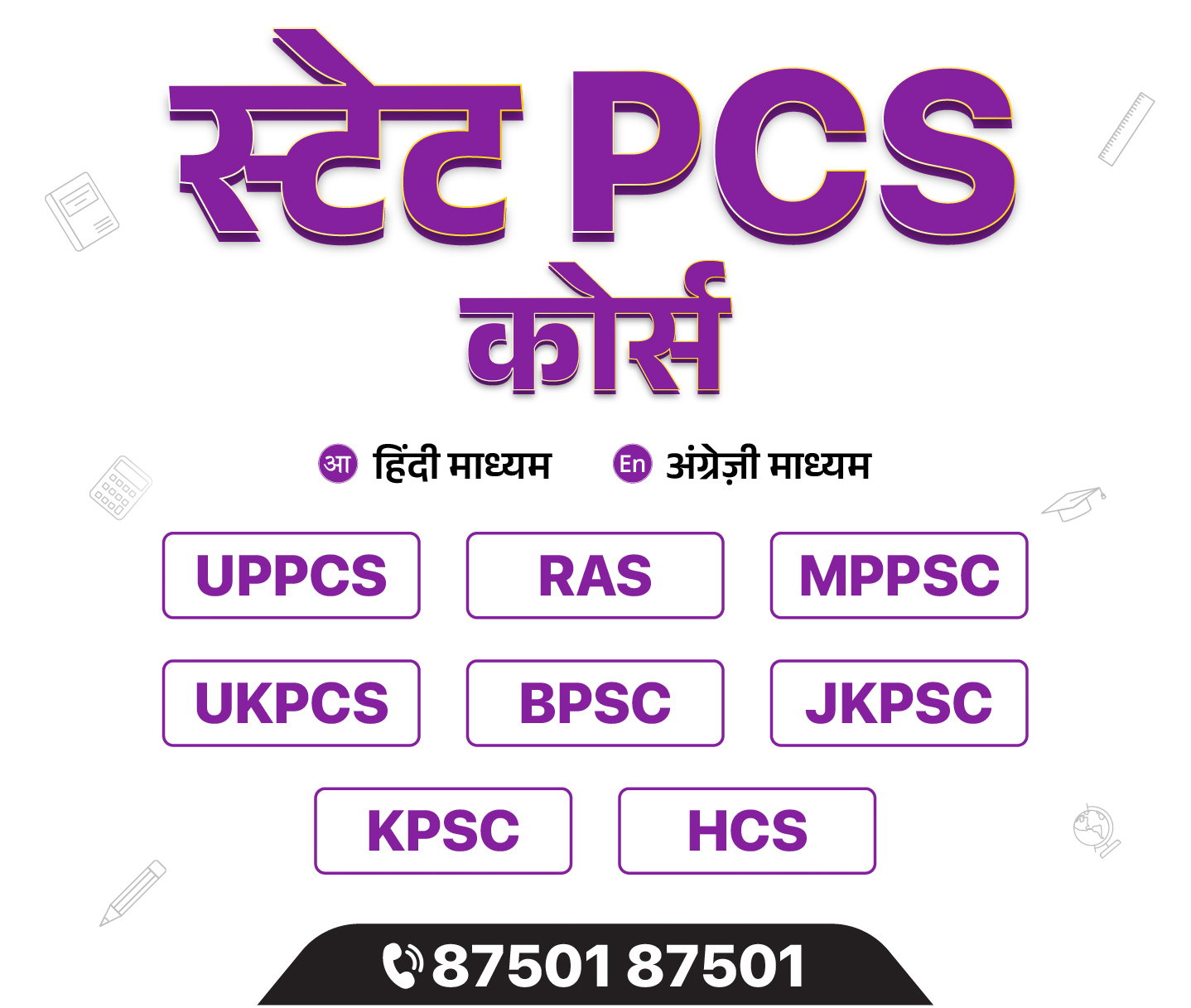


%20(1).gif)
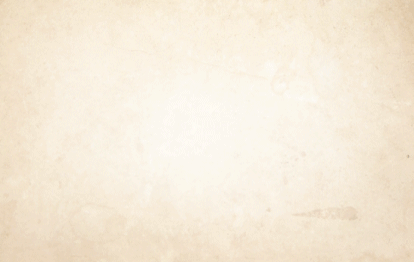

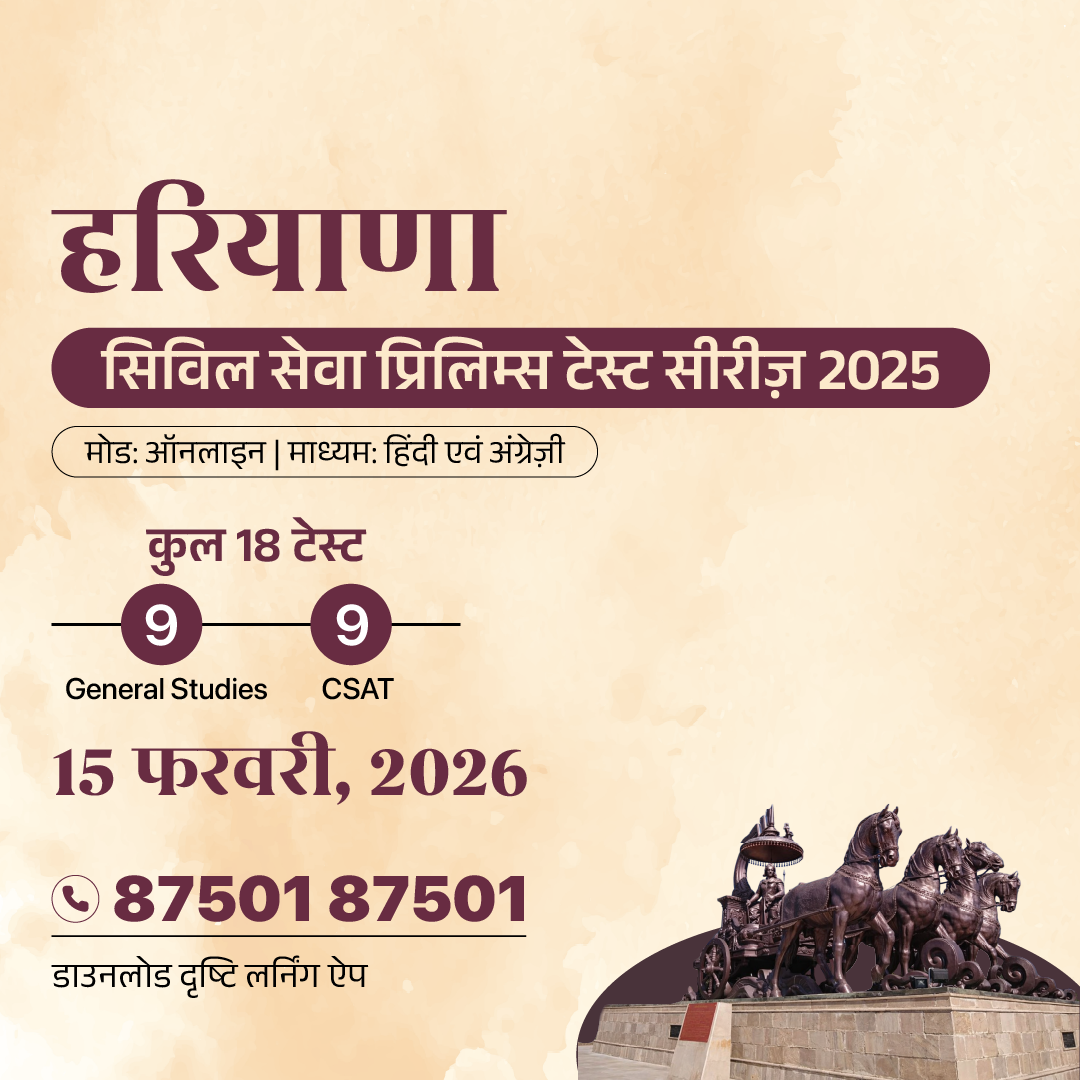
.jpg)
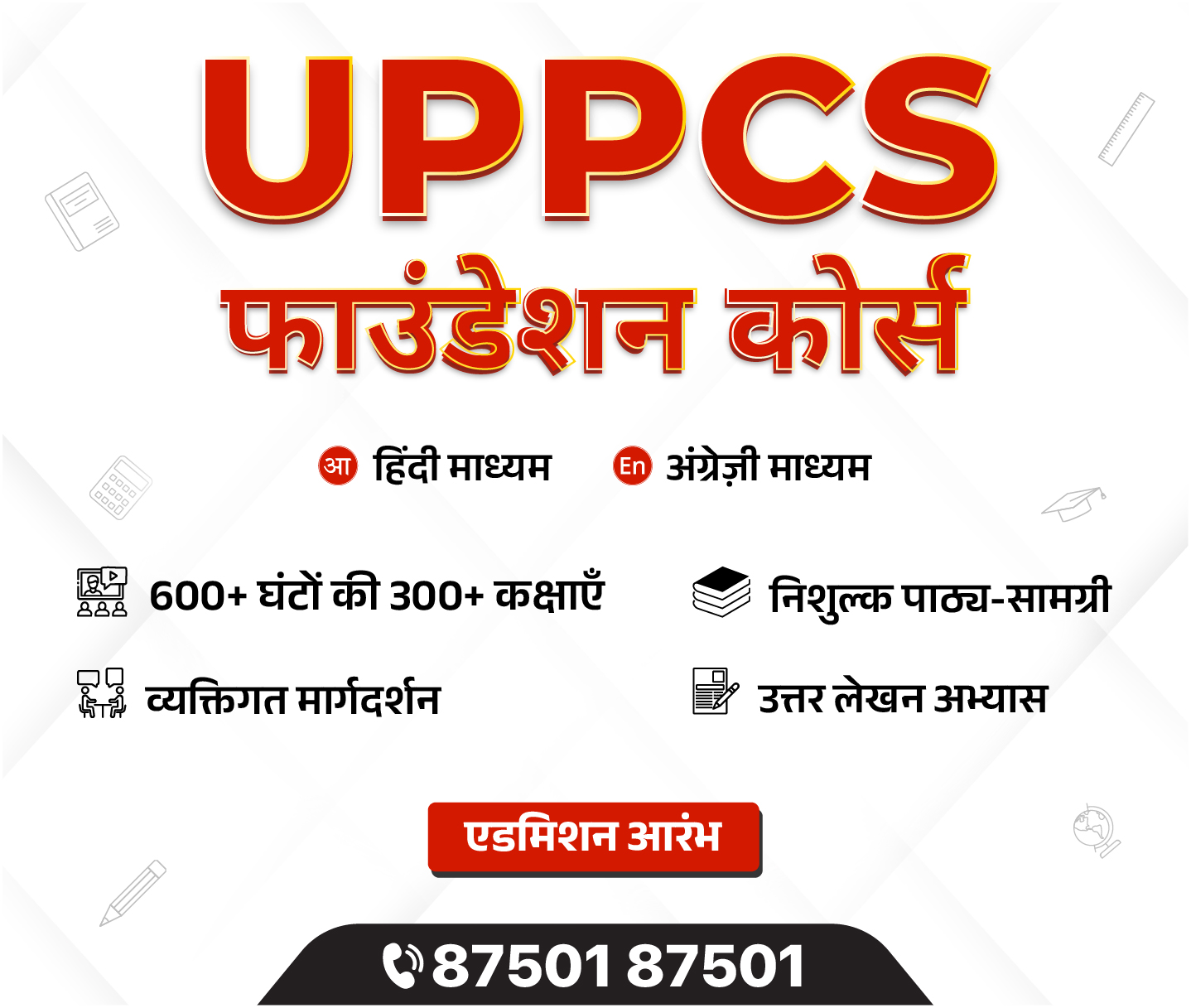
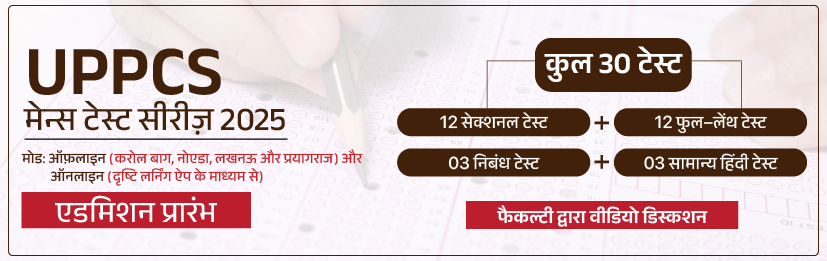
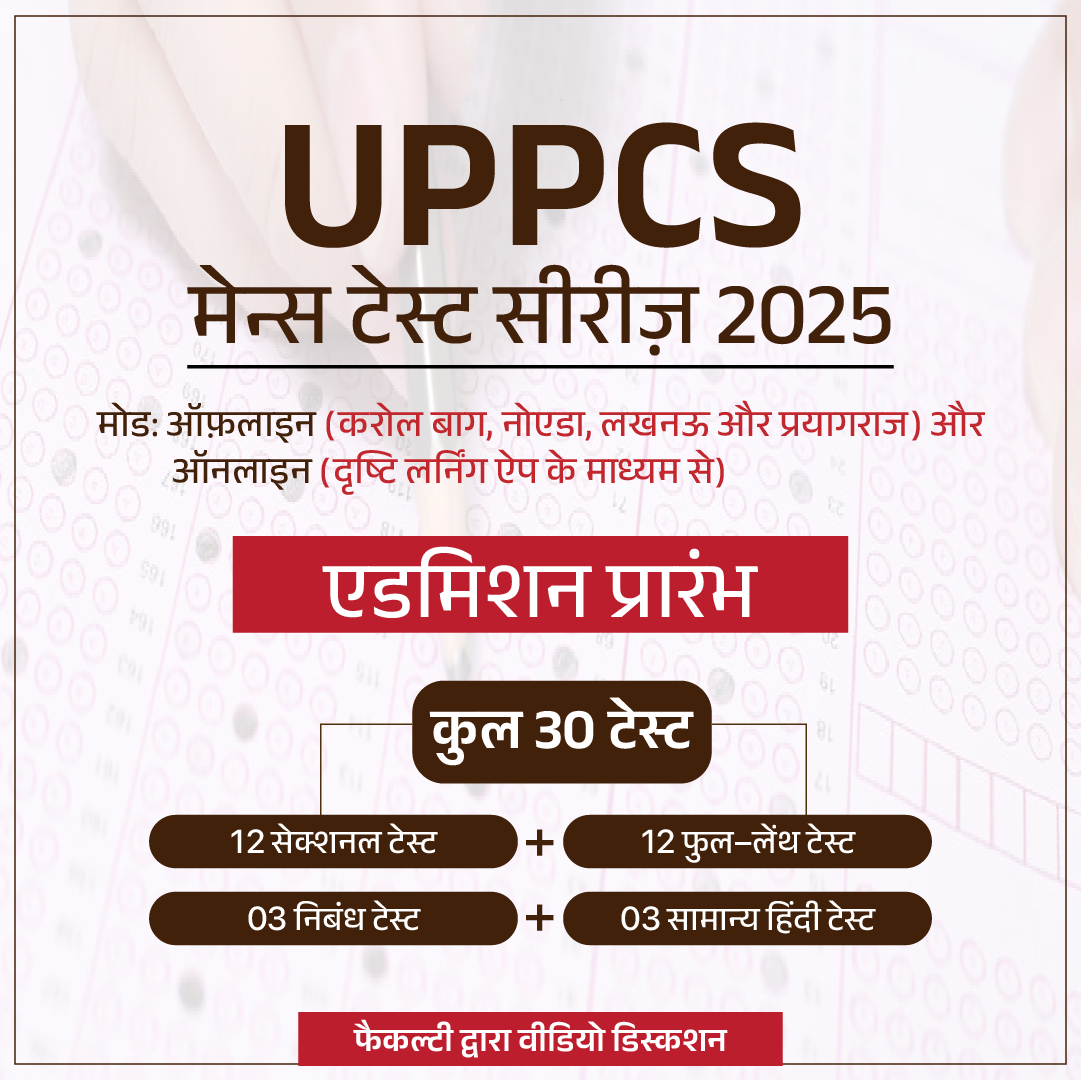

 PCS परीक्षण
PCS परीक्षण

