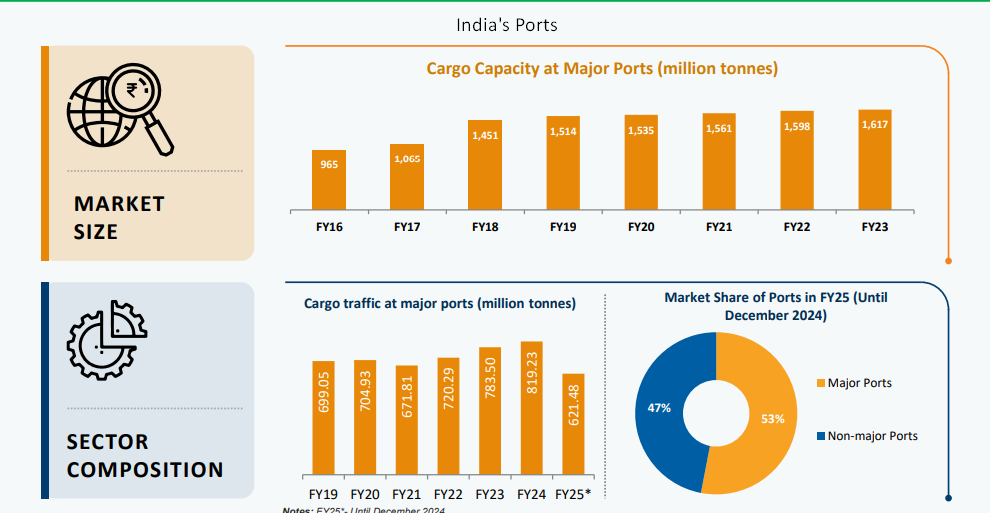शासन व्यवस्था
वैश्विक शिपिंग का डीकार्बोनाइज़ेशन
- 17 Jul 2025
- 85 min read
प्रिलिम्स के लिये:ग्रीनहाउस गैस, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, ग्रीन मेथनॉल, हरित अमोनिया, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, मेन्स के लिये:भारत का हरित बंदरगाह और शिपिंग अवसंरचना विकास, समुद्री उत्सर्जन में कमी लाने में भारत की भूमिका, हरित सागर हरित पत्तन दिशा-निर्देश |
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
वैश्विक नौवहन अब वर्ष 2040-2050 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में भारी कटौती करने की राह पर है। यह बदलाव बढ़ते जलवायु दबावों और वैश्विक डीकार्बोनाइज़ेशन लक्ष्यों से प्रेरित है।
- यह कदम भारत के लिये हरित ईंधन की आपूर्ति तथा इस परिवर्तन हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचे के निर्माण में एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है।
नोट: वैश्विक शिपिंग उद्योग कुल ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में लगभग 3% का योगदान देता है, जो मुख्य रूप से बहुत कम सल्फर ईंधन तेल (VLSFO), डीजल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) के उपयोग से होता है।
- अगर वैश्विक शिपिंग उद्योग एक देश होता तो वह छठा सबसे बड़ा उत्सर्जक होता। बिना हस्तक्षेप के, वर्ष 2050 तक उत्सर्जन 250% तक वृद्धि हो सकती है।
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने वर्ष 2030 तक कार्बन तीव्रता में 40% की कटौती, वर्ष 2040 तक 70% (2008 के स्तर की तुलना में) तथा वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है।
शिपिंग को कार्बन मुक्त करने हेतु कौन से हरित ईंधन का उपयोग किया जाता है?
- ग्रीन मेथनॉल: यह हरित हाइड्रोजन (नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पन्न) और औद्योगिक प्रक्रियाओं से प्राप्त CO₂ से प्राप्त होता है।
- लाभ: इसका उपयोग मौजूदा इंजनों के लिये ड्रॉप-इन ईंधन के रूप में किया जा सकता है, जिससे पारंपरिक ईंधन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन में 90-95% की कमी आती है।
- चुनौतियाँ: नवीकरणीय बिजली की कीमतों और इलेक्ट्रोलाइजर अवसंरचना के कारण हरित मेथनॉल की उत्पादन लागत अधिक होती है।
- हरित अमोनिया: यह वायु से नाइट्रोजन के साथ हरित हाइड्रोजन के संयोजन से उत्पन्न होता है।
- लाभ: पूरी तरह से कार्बन-तटस्थ, जिससे यह शिपिंग के लिये दीर्घकालिक समाधान बन जाता है।
- चुनौतियाँ: हरित अमोनिया अत्यधिक अस्थिर प्रकृति का होता है, जिसके लिये विशेष भंडारण टैंक और इंजन प्रौद्योगिकी में संशोधन की आवश्यकता होती है।
- जैव ईंधन: कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त जैव ईंधन कम कार्बन उत्सर्जन का विकल्प प्रदान कर सकते हैं, लेकिन मेथनॉल या अमोनिया की तरह इनका उपयोग नहीं किया जा सकता।
- लाभ: न्यूनतम संशोधनों के साथ मौजूदा इंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- चुनौतियाँ: भूमि और फीडस्टॉक की कमी के कारण सीमित मापनीयता, कुछ मामलों में जैव ईंधन उत्पादन को खाद्य उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ती है।
शिपिंग उद्योग में हरित ईंधन अपनाने में क्या चुनौतियाँ हैं?
- लागत पर विचार: मेथनॉल जैसे हरित ईंधन के उत्पादन के लिये इलेक्ट्रोलाइजर और बड़ी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और दोनों ही पूंजी-प्रधान हैं।
- एक टन हरित मेथनॉल के उत्पादन हेतु 10-11 मेगावाट घंटे नवीकरणीय बिजली की आवश्यकता होती है, जिसकी लागत लगभग 1,950 अमेरिकी डॉलर प्रति टन है, जबकि VLSFO के लिये यह 560 अमेरिकी डॉलर है, जिससे यह काफी महॅंगा हो जाता है।
- ग्रीन मेथनॉल की मांग वर्ष 2028 तक 14 मिलियन टन से अधिक होने की संभावना है, जबकि आपूर्ति केवल 11 मिलियन टन तक सीमित रह सकती है, जिससे इसकी कीमतों पर दबाव बढ़ेगा।
- प्रौद्योगिकीय और बुनियादी अवसंरचना संबंधी बाधाएँ: ग्रीन ईंधनों को अपनाने के लिये जहाज़ों और बंदरगाह सुविधाओं दोनों में बड़े पैमाने पर बदलाव की आवश्यकता होती है। इसमें इंजनों को फिर से अनुकूल बनाना (रेट्रोफिटिंग) और वैश्विक बंदरगाहों पर बंकरिंग (ईंधन भराई) के लिये अवसंरचना तैयार करना शामिल है।
- अमोनिया इंजन अभी भी प्रायोगिक स्तर पर हैं तथा कई शिपिंग कंपनियाँ ग्रीन मेथनॉल को प्राथमिकता देती हैं, जो अधिक सुरक्षित और अनुकूल है। समुद्री क्षेत्र परंपरागत रूप से सतर्क रहता है और नई तकनीकों को धीरे-धीरे अपनाता है तथा ग्रीन ईंधनों के लिये वैश्विक मानकों का अब भी अभाव है।
- नियामकीय और प्रमाणन संबंधी मुद्दे: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के नियम लगातार विकसित हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सभी देशों द्वारा समान रूप से अपनाया नहीं गया है। ग्रीन ईंधनों के लिये प्रमाणन तंत्र की कमी बाज़ार के भरोसे को प्रभावित करती है।
- भंडारण और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: हालाँकि हाइड्रोजन एक संभावित ईंधन है, लेकिन इसका भंडारण और परिवहन कठिन होने के कारण इसे सीधे शिपिंग में उपयोग करना व्यावहारिक नहीं माना जाता। इसलिये ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मिथेनॉल को अधिक व्यावहारिक विकल्प माना जा रहा है।
- भूराजनीतिक समीकरण: IMO में हुई चर्चाएँ भूराजनीतिक तनावों से काफी प्रभावित रहीं। सऊदी अरब जैसे तेल-निर्यातक देशों ने अपने जीवाश्म ईंधन बाज़ारों की सुरक्षा के लिये बड़े परिवर्तनों का विरोध किया। चीन ने वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता बनाए रखने के लिये न्यूनतम करों का समर्थन किया।
- छोटे राष्ट्रों, विशेषकर छोटे द्वीपीय देशों ने ग्रीन विकास पहलों के लिये वित्त पोषण हेतु अधिक कार्बन कर लगाने का समर्थन किया।
- भारत ने सिंगापुर के साथ मिलकर एक समझौता समाधान का संचालन किया, जिसमें पर्यावरणीय प्रभावशीलता और आर्थिक निष्पक्षता दोनों को एकीकृत किया गया।
वैश्विक शिपिंग डीकार्बोनाइज़ेशन में भारत की भूमिका क्या है?
- नीति नेतृत्व और वैश्विक सहयोग: भारत ने वैश्विक शिपिंग से उत्सर्जन को कम करने हेतु "मार्केट-बेस्ड मेज़र (MBM)" फ्रेमवर्क को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई, जिसे IMO की 83वीं समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति (MEPC) की बैठक में अपनाया गया।
- MBM ढाँचे के तहत भारत ने एक 'ब्रिजिंग मैकेनिज्म' का सुझाव दिया, जिसमें प्रदूषण फैलाने वालों पर दंड और ज़ीरो या नियर-ज़ीरो (ZNZ) ईंधन अपनाने वालों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है।
- भारत ने वर्ष 2025 में मुंबई में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव की मेज़बानी की, जिससे वैश्विक डीकार्बनाइजेशन फ्रेमवर्क के निर्माण में उसकी अग्रणी भूमिका को रेखांकित किया गया।
- स्वच्छ ईंधन उत्पादन: भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखता है, जो कि शिपिंग क्षेत्र के लिये आवश्यक ग्रीन अमोनिया और मेथनॉल जैसे ईंधनों के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- भारत के पास विशाल सौर ऊर्जा क्षमता है और वह वर्ष 2030 तक 280 गीगावॉट सौर ऊर्जा तथा कुल 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य लेकर चल रहा है। यह भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का आदर्श केंद्र बनाता है और वैश्विक शिपिंग डीकार्बोनाइज़ेशन का समर्थन करता है।
- समुद्री बुनियादी अवसंरचना और हरित बंदरगाह: भारत ग्रीन बंकरिंग सुविधाओं को बढ़ावा दे रहा है और हरित सागर ग्रीन पोर्ट दिशानिर्देश तथा ग्रीन टग ट्रांजिशन कार्यक्रम जैसी पहलों के माध्यम से हरित बंदरगाहों में निवेश कर रहा है।
- भारत हरित ईंधन उत्पादन पर केंद्रित है और तूतीकोरिन वी.ओ. चिदंबरनार तथा कांडला जैसे स्थानों पर ग्रीन फ्यूल बंकरिंग पोर्ट विकसित करने की महत्त्वाकांक्षी योजनाएँ बना रहा है।
- हरित समुद्री परिवहन हेतु वित्तीय प्रतिबद्धता: वित्त वर्ष 2025-26 के लिये घोषित ₹25,000 करोड़ के समुद्री विकास कोष (Maritime Development Fund) से हरित बुनियादी अवसंरचना, जहाज़ बेड़े के आधुनिकीकरण और वैकल्पिक ईंधनों में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे IMO के उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
- मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 जैसी नीतियाँ वैश्विक डीकार्बोनाइज़ेशन लक्ष्यों के अनुरूप हैं।
भारत शिपिंग डीकार्बोनाइज़ेशन में किस प्रकार अग्रणी हो सकता है?
- हरित ईंधन अवसंरचना विकास: भारत को अपने प्रचुर सौर ऊर्जा संसाधनों द्वारा संचालित हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्रों के विकास में निवेश करना चाहिये।
- औद्योगिक CO₂ से हरित मेथनॉल के उत्पादन को सुगम बनाने के लिये कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- नीतिगत और वित्तीय प्रोत्साहन: सरकार को हरित ईंधन निवेश के जोखिम को कम करने और हरित मेथनॉल उत्पादन को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिये संप्रभु गारंटी की पेशकश जारी रखना चाहिये।
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PIL) योजनाएँ इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण को समर्थन दे सकती हैं तथा एक मज़बूत हरित ईंधन आपूर्ति शृंखला बनाने में मदद कर सकती हैं।
- जहाज़ निर्माण और रेट्रोफिटिंग: भारत सरकार भारतीय शिपयार्डों में हरित ईंधन-तैयार जहाज़ निर्माण के लिये प्रोत्साहन प्रदान करके अपनी समुद्री क्षमताओं को बढ़ा सकती है।
- भारत ने 110 से अधिक जहाज़ों की खरीद के लिये 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है, जिनमें से 10-20% हरित ईंधन-संगत होंगे, इससे बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था बनाने और वैश्विक जहाज़ निर्माताओं को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
- निर्यात क्षमता: राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत भारतीय हरित हाइड्रोजन की ग्रीनहाउस गैस (GHG) तीव्रता अधिकतम 2 किलोग्राम CO₂e प्रति किलोग्राम या 16.7 ग्राम CO₂ प्रति मेगाजूल (MJ) होनी चाहिये, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन सीमा के भीतर है, जो कि 2034 तक 19.0 ग्राम CO₂e/MJ और उसके बाद 14.0 ग्राम CO₂e/MJ निर्धारित की गई है।
- यह सामंजस्य भारत के लिये हरित ईंधनों के वैश्विक निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय प्रोत्साहनों का लाभ उठाने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।
- यह न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करता है, बल्कि समुद्री लक्ष्यों के अनुरूप भी है तथा वर्ष 2030 तक 40% कार्बन तीव्रता में कटौती तथा वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है।
- अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियाँ और तकनीकी सहयोग: भारत को हरित जहाज़रानी प्रौद्योगिकी (Green Shipping Technology) के हस्तांतरण के लिये दक्षिण कोरिया और जापान के साथ साझेदारी करनी चाहिये तथा सिंगापुर जैसे देशों के साथ गठबंधन बनाकर हरित ईंधन निर्यात को बढ़ावा देना चाहिये।
निष्कर्ष
नीतिगत नेतृत्व, हरित प्रौद्योगिकियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भारत वैश्विक नौवहन डीकार्बोनाइज़ेशन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हरित हाइड्रोजन, स्वच्छ ईंधन उत्पादन और सतत् बंदरगाह विकास पर ध्यान केंद्रित करके भारत का लक्ष्य अपने समुद्री क्षेत्र को वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ जोड़ना, साथ ही दीर्घकालिक आर्थिक लाभ भी प्राप्त करना है।
|
दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति में समुद्री डीकार्बनाइज़ेशन (Maritime Decarbonisation) का क्या महत्त्व है? इस संक्रमण (परिवर्तन) में भारत की क्या भूमिका है? |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रिलिम्स:प्रश्न: हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद (सिम्पोज़ियम) (IONS) के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिये:
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) प्रश्न: 'क्षेत्रीय सहयोग के लिये हिंद महासागर रिम संघ [इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (IOR-ARC)]' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) |