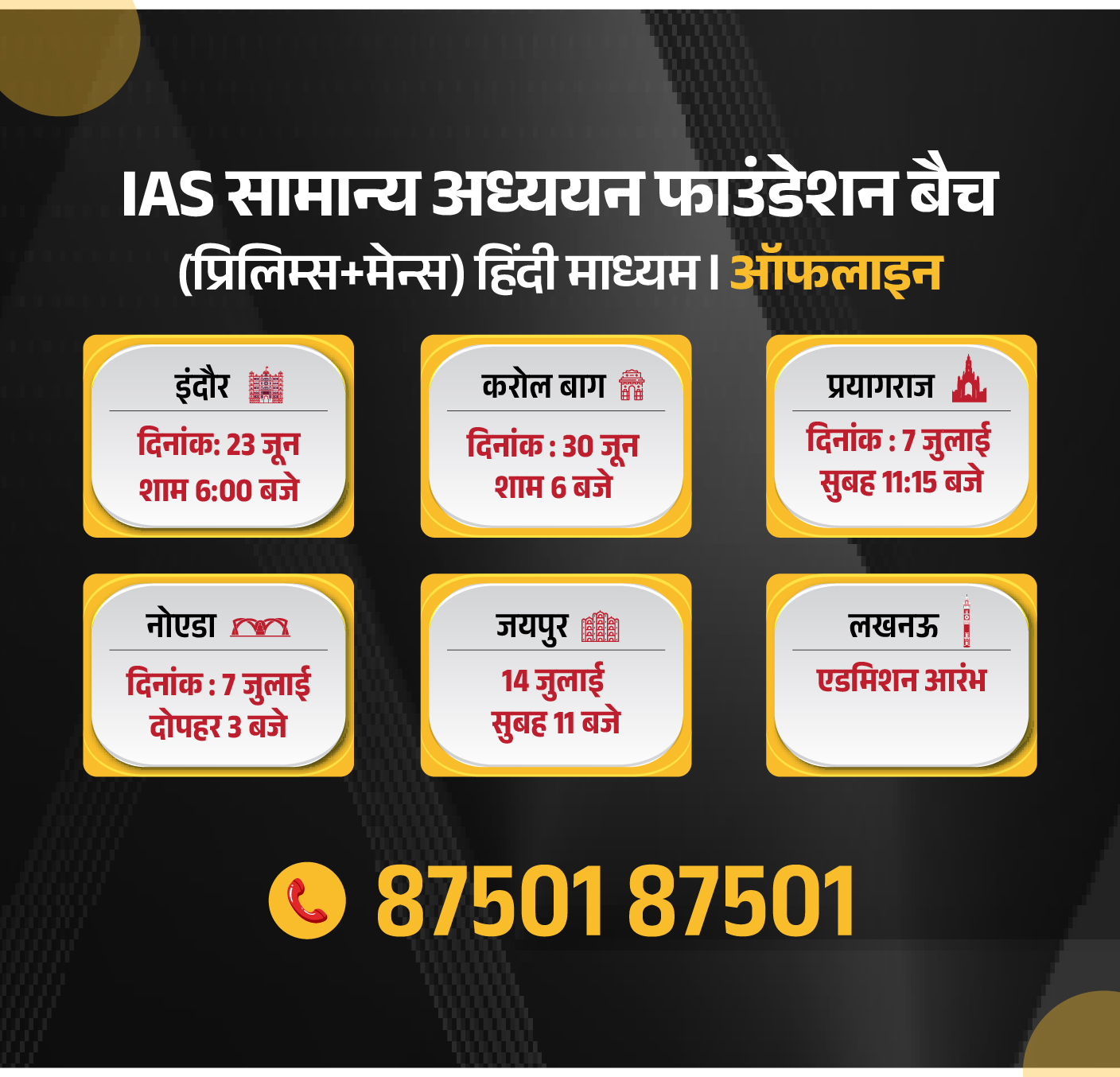भारतीय अर्थव्यवस्था
भारत के विकास के उत्प्रेरक के रूप में शहरी केंद्र
प्रिलिम्स के लिये:सकल घरेलू उत्पाद, एशियाई विकास बैंक, बायोमास, सतत् विकास लक्ष्य मेन्स के लिये:भारत में शहरीकरण और उससे जुड़ी चुनौतियाँ, भारत के आर्थिक विकास में शहरों की भूमिका |
स्रोत: बीएल
चर्चा में क्यों?
भारत तेज़ी से शहरीकरण के दौर से गुज़र रहा है, जहाँ वर्ष 2035 तक शहरी जनसंख्या 67.5 करोड़ तक पहुँचने की उम्मीद है तथा वर्ष 2045 तक इसमें 7 करोड़ लोग और जुड़ सकते हैं। यह तेज़ी से होती शहरीकरण की प्रक्रिया आने वाले दशकों तक भारत की आर्थिक और सामाजिक दिशा को आकार प्रदान करेगी।
- हालाँकि भारतीय शहरों में मौजूद शहरी चुनौतियाँ इस परिवर्तन की पूरी संभावनाओं को प्राप्त करने में अब भी बाधा बनी हुई हैं।
भारत के आर्थिक भविष्य के लिये शहर केंद्र पर क्यों हैं?
- आर्थिक इंजन: शहर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 60% योगदान देते हैं, जबकि वे केवल 3% भू-भाग पर स्थित हैं। यह उन्हें उत्पादकता और नवाचार के केंद्र के रूप में दर्शाता है।
- मुंबई, दिल्ली, बंगलूरू, चेन्नई और हैदराबाद सहित केवल 15 शहर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 30% का योगदान करते हैं। इन शहरों से वर्ष 2047 तक GDP वृद्धि में अतिरिक्त 1.5% योगदान की उम्मीद है।
- समूहन के लाभ: शहरी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व से अधिक आर्थिक उत्पादन, बेहतर रोज़गार सृजन और उद्योगों एवं सेवाओं के समूहों के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा मिलता है।
- भारत की बढ़ती शहरी आबादी से हर साल अतिरिक्त 1.5% आर्थिक उत्पादकता वृद्धि की उम्मीद है, जो राष्ट्रीय उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि को संभव बनाएगी।
- वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता: सुव्यवस्थित शहर व्यापार सुगमता में सुधार करते हैं, विदेशी निवेश को आकर्षित करते हैं तथा भारत को वर्ष 2026 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तथा वर्ष 2047 तक 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सहयोग करते हैं।
- आवश्यक ढाँचागत कुशलता: शहरी क्षेत्रों में परिवहन, आवास, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स की प्रभावी व्यवस्थाएँ ऑपरेशनल लागत को कम करती हैं तथा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करती हैं।
- नवप्रवर्तन केंद्र: शहर स्टार्टअप्स, अनुसंधान एवं विकास (R&D) और प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देते हैं, जिससे वे डिजिटल तथा सेवा क्षेत्रीय परिवर्तन के प्रमुख केंद्र बनते हैं।
- सामाजिक अवसर: शहरीकरण गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच के लिये मार्ग प्रदान करता है तथा आर्थिक विकास को बेहतर मानव विकास परिणामों से जोड़ता है।
शहरी भारत के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?
- भीड़भाड़ और यातायात प्रबंधन: शहरी निवासियों को प्रतिदिन औसतन 1.5 से 2 घंटे ट्रैफिक जाम में फँसे रहना पड़ता है। यह भीड़भाड़ न केवल प्रदूषण बढ़ाती है, बल्कि समय की बर्बादी और उत्पादकता में कमी का कारण भी बनती है।
- भारत के अधिकांश शहरों में समग्र, कुशल और एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की कमी है, जिसके कारण निजी वाहनों पर अत्यधिक निर्भरता रहती है तथा ट्रैफिक की समस्या और बढ़ जाती है।
- उदाहरण के लिये, झारखंड की राजधानी राँची में 1.46 मिलियन की आबादी के लिये केवल 41 बसें हैं।
- एशियाई विकास बैंक के अनुसार, शहरी परिवहन की अकुशलता, रसद में देरी और खराब बुनियादी ढाँचे के कारण भारत को प्रतिवर्ष 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान होता है।
- भारत के अधिकांश शहरों में समग्र, कुशल और एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की कमी है, जिसके कारण निजी वाहनों पर अत्यधिक निर्भरता रहती है तथा ट्रैफिक की समस्या और बढ़ जाती है।
- वायु प्रदूषण: वर्ष 2023 में, विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 42 भारत के हैं, जबकि वर्ष 2022 में यह संख्या 39 थी। खराब वायु गुणवत्ता के प्राथमिक कारणों में वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, निर्माण कार्य से उत्पन्न धूलकण और बायोमास का जलना शामिल हैं।
- इससे श्वसन रोगों का खतरा बढ़ता है, जिससे दिल्ली, मुंबई और बंगलूरू जैसे शहरों में लाखों लोग प्रभावित होते हैं।
- जल संकट: भारत की लगभग आधी नदियाँ प्रदूषित हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ जल की उपलब्धता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। अपर्याप्त जलशोधन तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन से जल संसाधनों पर और दबाव पड़ता है।
- इसके अतिरिक्त, पुराने पाइपलाइन सिस्टम के कारण शहरी क्षेत्रों में 40-50% पानी का नुकसान हो जाता है।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: भारतीय शहरों में प्रतिदिन 1,50,000 टन से ज़्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, लेकिन इसका केवल एक छोटा-सा हिस्सा ही स्थायी रूप से संसाधित किया जाता है। कई शहरों में प्रभावी अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण प्रणालियों का अभाव है।
- खराब अपशिष्ट प्रबंधन से प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी खतरे और अस्वच्छ शहरी वातावरण में योगदान होता है, जिससे शहर रहने लायक नहीं रह जाते।
- स्वच्छता की कमी: कई शहरी क्षेत्रों, विशेषकर अनौपचारिक बस्तियों में उचित स्वच्छता सुविधाओं की कमी है ।
- कई शहरों में अपर्याप्त सीवेज प्रणालियाँ और जल निकायों में सीवेज रिसाव एक चुनौती बनी हुई है।
- किफायती आवास की कमी: भारत में 10 मिलियन किफायती घरों की कमी है और यह संख्या वर्ष 2030 तक तीन गुनी होने की उम्मीद है। शहरी गरीब लोग अक्सर अनौपचारिक बस्तियों या मलिन बस्तियों में रहते हैं, जहाँ स्वच्छ पानी, स्वच्छता और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है।
- इस बढ़ती कमी के कारण न केवल भीड़भाड़ वाली झुग्गियाँ बनती हैं, बल्कि शहरी बस्तियाँ भी बनती हैं, जिससे सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ती हैं तथा सांप्रदायिक या धार्मिक हिंसा की संभावना बढ़ जाती है।
- इसके अतिरिक्त, शहरी स्थान की बढ़ती मांग के कारण संपत्ति की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे किफायती आवास कई लोगों के लिये दुर्गम हो जाता है।
- शहरी बाढ़: कई शहरों में अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था, वर्षा जल निकासी नालियों पर अतिक्रमण और तेज़ी से शहरीकरण के कारण शहरी बाढ़ का सामना करना पड़ता है।
- केरल में वर्ष 2018 की बाढ़ और चेन्नई में वर्ष 2015 की बाढ़ इस बात के प्रमुख उदाहरण हैं कि शहरी बुनियादी ढाँचा चरम मौसम की घटनाओं से निपटने के लिये किस तरह संघर्ष करता है।
- कमज़ोर नगरपालिका वित्त: भारतीय शहर स्थानीय करों और नगर निगम बॉण्डों के माध्यम से पर्याप्त राजस्व जुटाने में विफल रहते हैं। अधिकांश नगरपालिकाएँ केंद्रीय सरकार के फंड पर निर्भर रहती हैं, जो अक्सर अपर्याप्त या अक्षम रूप से उपयोग किये जाते हैं।
- कई शहर शहरी विकास परियोजनाओं के लिये केंद्र सरकार के वित्तपोषण पर निर्भर रहते हैं, लेकिन आवंटित धनराशि अक्सर अपर्याप्त होती है या उसका अकुशल उपयोग किया जाता है।
- डिजिटल अवसंरचना की कमी: सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग और सियोल जैसे देशों के शहरों की तुलना में भारत में इंटरनेट स्पीड बहुत कम है।
- इससे डिजिटल व्यवसायों की वृद्धि बाधित होती है और समग्र आर्थिक विकास धीमा हो जाता है।
- शहरी ऊष्मा द्वीप: उच्च तापमान के कारण एयर कंडीशनर का अत्यधिक उपयोग होता है, जिससे बिजली की मांग बढ़ती है और कार्बन उत्सर्जन में इजाफा होता है।
- इससे स्वास्थ्य जोखिम, हरित आवरण में कमी, जैवविविधता पर प्रभाव, जल संसाधनों पर दबाव, बाढ़ का खतरा और शहरी संरचना पर प्रभाव जैसे कई गंभीर परिणाम सामने आते हैं।
शहरी क्षेत्र में विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये भारत की कौन-सी पहल हैं?
भारत के शहरी भविष्य के लिये किन सुधारों की आवश्यकता है?
- शहरी बुनियादी ढाँचे को मुख्य राष्ट्रीय बुनियादी ढाँचे के रूप में समझना: शहरी बुनियादी ढाँचे जैसे गतिशीलता, जल, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को राजमार्गों, बंदरगाहों तथा ऊर्जा ग्रिड के समान दर्जा दिया जाना चाहिये।
- स्मार्ट शहरों और लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को “रणनीतिक अवसंरचना” के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये ताकि दीर्घकालिक पूंजी निवेश और नीतिगत समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके।
- औद्योगिक गलियारों के साथ शहरी विस्तार को समन्वित करना: आवास, वाणिज्य और परिवहन के बीच के अंतर को कम करने के लिये ट्रांज़िट-ओरिएंटेड डिवेलपमेंट को बढ़ावा देना आवश्यक है। परिवहन, ज़ोनिंग और आर्थिक योजना का स्थानिक एकीकरण कर के संवहनीय, रहने योग्य और उत्पादक शहरी-औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा सकते हैं।
- एकीकृत, तकनीक-सक्षम शहरी शासकीय निकायों का निर्माण करना: शहरी नियोजन और अनुमोदनों को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है। शहरी शासन निकायों को निजी क्षेत्र के नेतृत्व को शामिल करना चाहिये तथा जवाबदेही में सुधार के लिये सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिये।
- रियल-टाइम प्रदर्शन डैशबोर्ड और अर्बन डिजिटल ट्विन्स (शहर का एक गतिशील डिजिटल संस्करण जो उन्नत तकनीकों से डेटा अंतर्दृष्टि प्रदान करता है) शहरी प्रणालियों के उत्तरदायी और पारदर्शी प्रबंधन को सुनिश्चित कर सकते हैं।
- स्वच्छता और अवशिष्ट प्रबंधन को राष्ट्रीय आर्थिक प्राथमिकता बनाना: स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन आर्थिक मुद्दे हैं।
- जैसे तिरुपुर जल PPP परियोजना ने BOOT मॉडल के माध्यम से उद्योगों और नागरिकों को जल आपूर्ति सफलतापूर्वक प्रदान की, वैसे ही उद्योग-प्रेरित मॉडल को अवशिष्ट प्रबंधन, परिपथीय अर्थव्यवस्था और विकेंद्रीकृत स्वच्छता में भी अपनाया जा सकता है।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का पुनर्पूंजीकरण: वर्तमान शहरी परिप्रेक्ष्य में PPP को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है, ताकि लंबी अवधि की निजी पूंजी को मौजूदा (ब्राउनफील्ड) ढाँचागत परियोजनाओं और नई (ग्रीनफील्ड) परियोजनाओं दोनों में आकर्षित किया जा सके।
- जोखिम-न्यूनन उपाय जैसे व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (Viability Gap Funding) और शहरी चुनौती निधि (Urban Challenge Fund) इस तरह के निवेश को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- आधुनिक शहरों की डिजिटल अवसंरचना का सह-निर्माण करना: उद्योगों को सरकार के साथ मिलकर शहरों की डिजिटल संरचना विकसित करनी चाहिये, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित अवसंरचना नियोजन और स्वचालित निर्माण स्वीकृति प्रणाली जैसी सुविधाएँ शामिल हों।
- यह डिजिटल अवसंरचना दक्षता, पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा दे सकती है तथा शहरी विकास की गति को तीव्र कर सकती है।
- शहरों में जलवायु सहनशीलता को सुदृढ़ करना: शहरी नियोजन में जलवायु सहनशीलता को एकीकृत किया जाना चाहिये, जिसके अंतर्गत बाढ़-रोधी अवसंरचनाएँ और ऊष्मा-प्रतिरोधी संरचनाएँ जैसी अनुकूलनशील अधोसंरचनाओं का निर्माण शामिल है। ग्रीन रूफ्स (हरी छतें), शहरी वानिकी और हरित स्थान जैसे उपायों से हीट आइलैंड प्रभाव को कम किया जा सकता है तथा शहरी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है।
- शहरी सुधार में समाज की भूमिका: शहरी सुधार केवल व्यवस्थाओं के सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की सक्रिय भागीदारी से भी जुड़ा हुआ है। सुधारों को नागरिकों और उद्योगों के साथ मिलकर सह-निर्मित किया जाना चाहिये।
- ऐसे भागीदारी आधारित ढाँचे, जो नीति, जनता और निजी पूंजी को एक साथ जोड़ते हैं, शहरों की सहनशीलता तथा वैधता सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हैं। इस प्रकार के सहयोग शहरों को स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सशक्त बनाती हैं, साथ ही वे राष्ट्रीय प्रगति में भी योगदान देती हैं।
निष्कर्ष
भारतीय शहर क्षेत्रीय विकास के महत्त्वपूर्ण प्रेरक हैं, लेकिन इन्हें अवसंरचना, स्थिरता और शासन संबंधी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सतत् शहरी नियोजन, बेहतर सार्वजनिक परिवहन और संसाधनों के कुशल प्रबंधन जैसे- उपाय सतत् विकास लक्ष्य (SDG) 11 (सतत् शहर), SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) तथा SDG 10 (असमानताओं को कम करना) को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक हैं, जिससे समान एवं समावेशी शहरी विकास सुनिश्चित हो सके।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: शहरीकरण भारत के लिये एक अवसर और चुनौती दोनों है। चर्चा कीजिये। |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)मेन्सप्रश्न. कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि पर प्रकाश डालिये। (2016) प्रश्न. क्या कमज़ोर और पिछड़े समुदायों के लिये आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नति के लिये सरकारी योजनाएँ, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहिष्कृत कर देती हैं? (2014) |
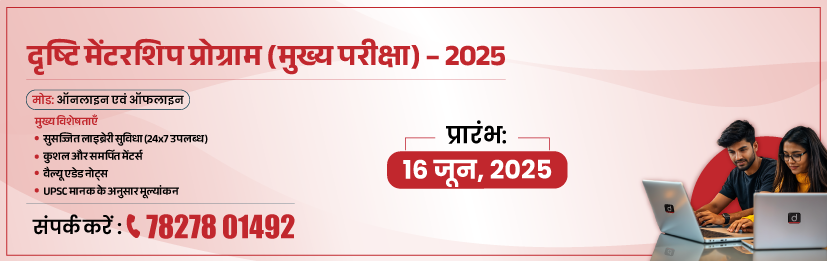

अंतर्राष्ट्रीय संबंध
भारत-नामीबिया संबंध और अफ्रीका
प्रिलिम्स के लिये:नामीबिया, अफ्रीका, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI), वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (ITEC), अधिमान्य व्यापार समझौता (PTA), दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (SACU), नेकलेस ऑफ डायमंड्स रणनीति, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अफ्रीकी संघ, G20, WTO बौद्धिक संपदा, प्रवासी भारतीय दिवस, IIT मद्रास ज़ांज़ीबार। मेन्स के लिये:भारत-नामीबिया संबंधों की मुख्य विशेषताएँ, भारत के लिये अफ्रीका का सामरिक महत्त्व, प्रभावी भारत-अफ्रीका सहयोग में प्रमुख बाधाएँ। |
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
भारत के प्रधानमंत्री ने नामीबिया की राजकीय यात्रा की (जो कि 27 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी), नामीबियाई संसद को संबोधित किया और इस बात की पुनः पुष्टि की कि भारत तथा अफ्रीका की साझेदारी वर्चस्व पर नहीं, बल्कि संवाद पर आधारित है।
- उन्हें नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान "ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनशिएंट वेल्वित्चिया मिराबिलिस" भी प्रदान किया गया, जिससे वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अभिकर्त्ता बन गए।
- नामीबिया ने आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने के लिये स्वीकृति-पत्र सौंपे तथा वह UPI तकनीक को अपनाने के लिये लाइसेंसिंग समझौता करने वाला विश्व का पहला देश बन गया।
नामिबिया
- भौगोलिक स्थिति: नामीबिया एक दक्षिणी अफ्रीकी देश है, जिसकी पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर से बनती है।
- इसकी उत्तरी सीमा अंगोला और ज़ाम्बिया से लगती है, जबकि पूर्व में बोत्सवाना स्थित है और पूर्व तथा दक्षिण दोनों दिशाओं में दक्षिण अफ्रीका इसकी सीमा से जुड़ा हुआ है।
- जलवायु: नामीबिया को उप-सहारा अफ्रीका का सबसे शुष्क राष्ट्र माना जाता है। यहाँ कई प्रमुख रेगिस्तानों हैं, जिनमें नामीब, कालाहारी, सक्युलेंट करू और नामा करू शामिल हैं।
- औपनिवेशिक इतिहास: वर्ष 1884 में जर्मन साम्राज्य ने इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर औपनिवेशिक शासन स्थापित किया और इसका नाम जर्मन दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका रखा।
- प्रमुख नदियाँ: ज़ाम्बेज़ी, ओकावांगो और कुनेने नामीबिया की प्रमुख नदियाँ हैं।
वेल्वित्चिया मिराबिलिस
- परिचय: वेल्वित्चिया मिराबिलिस (नामीबिया का राष्ट्रीय पौधा) एक दुर्लभ और प्राचीन पौधा है, जो मुख्यतः नामीब रेगिस्तान (नामीबिया और दक्षिणी अंगोला) में पाया जाता है। इसे इसकी अद्भुत दीर्घायु और अनोखी विशेषताओं के कारण प्रायः ‘जीवित जीवाश्म’ (Living Fossil) कहा जाता है।
- नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनशिएंट वेल्वित्चिया मिराबिलिस का नाम इसी पौधे के नाम पर रखा गया है।
- स्वरूप: इस पौधे में केवल दो चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, जो निरंतर बढ़ती रहती हैं। ये पत्तियाँ समय के साथ जीर्ण-शीर्ण हो जाती हैं, लेकिन कभी गिरती नहीं हैं। इसका एक काष्ठीय तना (लकड़ी जैसा तना) और गहरी मुख्य जड़ (टैपरूट) इसे शुष्क परिस्थितियों को सहन करने में सहायता करती है।
- दीर्घकालिकता: इसके कुछ नमूने 1,500 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं, जिससे यह विश्व के सबसे पुराने पौधों में शामिल होता है।
- पर्यावास: यह केवल नामीब रेगिस्तान में पाया जाता है और वर्षा की अत्यधिक कमी के कारण नमी के लिये मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर से आने वाली धुँध (कोहरा) पर निर्भर रहता है।
- रेगिस्तान में रहने वाले कई जानवर, जैसे कि ज़ेब्रा, ओरिक्स और ब्लैक राइनोसेरस, वेल्वित्चिया की पत्तियों को जल के एक आवश्यक स्रोत के रूप में खाते हैं।
भारत-नामीबिया संबंधों की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
- ऐतिहासिक और राजनीतिक संबंध: भारत वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र में नामीबिया की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाने वाले पहले देशों में से एक था, जिसने दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पीपुल्स ऑर्गनाइज़ेशन (SWAPO ने नामीबिया के मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया) को भौतिक और राजनयिक समर्थन दिया।
- भारत और नामीबिया के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध वर्ष 1990 में स्थापित हुए तथा नामीबिया ने मार्च 1994 में नई दिल्ली में अपना दूतावास (स्थायी मिशन) शुरू किया।
- चीता स्थानांतरण परियोजना: वर्ष 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया गया, जो कि किसी प्रमुख मांसाहारी प्रजाति का विश्व का पहला अंतर-महाद्वीपीय स्थानांतरण था।
- क्षमता निर्माण एवं रक्षा सहयोग: भारत, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (ITEC) के तहत नामीबियाई नागरिकों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है, साथ ही उन्हें प्रतिवर्ष रक्षा प्रशिक्षण के अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं।
- वर्ष 1996 से, भारतीय वायु सेना (IAF) की एक तकनीकी टीम नामीबियाई वायु सेना के हेलीकॉप्टर पायलटों को प्रशिक्षण दे रही है और भारत ने 2 चेतक तथा 2 चीता हेलीकॉप्टर भी नामीबिया को प्रदान किये हैं।
- विकास सहायता: विकास सहायता: भारत ने नामीबिया को 30,000 कोविशील्ड खुराकें प्रदान कीं और वहाँ भारत-नामीबिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (INCEIT) तथा यूनिवर्सिटी ऑफ नामीबिया में ‘इंडिया विंग’ की स्थापना की।
- आर्थिक संबंध: वर्ष 2024–25 में द्विपक्षीय व्यापार 568.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। प्रमुख क्षेत्रों में खनन, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य और व्यापार शामिल हैं।
- भारत और दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (SACU) के बीच अधिमान्य व्यापार समझौता (PTA) पर बातचीत जारी है, जिसमें नामीबिया समन्वयक की भूमिका निभा रहा है।
- नामीबिया में भारतीय समुदाय: नामीबिया में लगभग 450 भारतीय/अनिवासी भारतीय (NRI)/भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) रहते हैं। इंडिया-नामीबिया चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (INCCI) और इंडिया-नामीबिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन (INFA) जो क्रमशः वर्ष 2016 तथा 2020 में स्थापित हुए व्यापार व समुदाय से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।
अफ्रीका भारत के लिये रणनीतिक रूप से क्यों महत्त्वपूर्ण है?
- भू-राजनीतिक और समुद्री सुरक्षा: अफ्रीका की भौगोलिक स्थिति हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के चौराहे पर है, जो भारत के समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा तथा नौसेना प्रभाव बढ़ाने के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- भारत का पहला विदेशी नौसेना अड्डा (2024) मॉरीशस में नेकलेस ऑफ डायमंड्स रणनीति के तहत स्थापित किया गया, जो समुद्री मार्गों की रक्षा और समुद्री डकैती व आतंकवाद का मुकाबला करने के प्रयासों को दर्शाता है।
- उभरती आर्थिक शक्ति: वर्ष 2022–23 में भारत-अफ्रीका द्विपक्षीय व्यापार 98 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें से 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर खनन और खनिज क्षेत्रों से जुड़े हैं।
- अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया (AfCFTA), जो वर्ष 2021 से कार्यान्वित है, 1.4 अरब लोगों के एकल बाज़ार का निर्माण करता है, जिससे भारतीय निर्यात और निवेश की संभावनाएँ बढ़ती हैं।
- महत्त्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षा: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य विश्व के 70% से अधिक कोबाल्ट की आपूर्ति करता है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों और नवीकरणीय ऊर्जा के लिये आवश्यक है।
- नाइजीरिया और अंगोला, भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करते हैं और वैश्विक आपूर्ति अस्थिरता के बीच भारत के कच्चे तेल आयात में अफ्रीका की हिस्सेदारी बढ़ रही है।
- राजनयिक प्रभाव: भारत ने वर्ष 2023 में अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने में अहम भूमिका निभाई, जो एक राजनयिक उपलब्धि रही और अफ्रीका की वैश्विक आर्थिक भूमिका को मज़बूत किया।
- विश्व व्यापार संगठन में कोविड-19 वैक्सीन और कृषि के लिये बौद्धिक संपदा छूट पर संयुक्त प्रयास, न्यायसंगत वैश्विक शासन के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं तथा भारत की ग्लोबल साउथ में नेतृत्व भूमिका को भी सुदृढ़ करते हैं।
- भूराजनैतिक सहयोगी: अफ्रीका के 54 देश, वैश्विक मंचों पर एक शक्तिशाली समूह बनाते हैं और भारत के लिये एक प्रमुख भूराजनैतिक साझेदार के रूप में उभर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में प्रतिनिधित्व को लेकर भारत और अफ्रीका एक-दूसरे का समर्थन करते हैं।
- जैसे-जैसे वैश्विक शक्ति बदल रही है, भारत-अफ्रीका की मज़बूत साझेदारी चीन जैसी क्षेत्रीय शक्तियों को संतुलित करने का कार्य कर रही है।
- सशक्त प्रवासी समुदाय: 3 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोग अफ्रीका में रहते हैं, जो दोनों क्षेत्रों के बीच सेतु का कार्य करते हैं और ऐतिहासिक रूप से अफ्रीकी अर्थव्यवस्था में योगदान देते आए हैं।
- भारत इस संबंध को प्रवासी भारतीय दिवस जैसी पहलों के माध्यम से मज़बूत कर रहा है। वर्ष 2019 के प्रवासी भारतीय दिवस में अफ्रीकी प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिल सके।
भारत-अफ्रीका संबंधों को गहरा करने में प्रमुख बाधाएँ क्या हैं?
- धीमी निवेश गतिविधि: बढ़ते संबंधों के बावजूद, जोखिम की धारणा, सीमित बाज़ार ज्ञान और भारत के आर्थिक प्रभाव को सीमित करने वाली कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के कारण अफ्रीका में भारतीय निवेश चीन और पश्चिम से पीछे है।
- भारतीय निर्यातों पर विश्वसनीयता की समस्या: कुछ अफ्रीकी बाज़ारों में यह धारणा बनी हुई है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता पश्चिमी या चीनी उत्पादों की तुलना में कम है, जिसका प्रभाव औषधि और मशीनरी जैसे क्षेत्रों पर पड़ता है।
- गाम्बिया में वर्ष 2022 में दूषित सिरप की घटना, जिसके कारण 60 से अधिक बच्चों की मृत्यु हो गई, ने भारत की प्रतिष्ठा और बाज़ार हिस्सेदारी को और अधिक नुकसान पहुँचाया।
- राजनयिक असंतुलन: भारत की अफ्रीका नीति की आलोचना होती है कि यह पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका पर अधिक केंद्रित है, जबकि पश्चिमी अफ्रीका जैसे अन्य क्षेत्रों को नज़रअंदाज़ किया गया है।
- उदाहरण के लिये, वर्ष 2022–23 में दक्षिण अफ्रीका का निर्यात 8.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जबकि पश्चिमी अफ्रीका, जिसकी आर्थिक क्षमता काफी है, अब भी कम जुड़ाव वाला क्षेत्र बना हुआ है।
- जटिल सुरक्षा परिदृश्य: वर्ष 2020–2023 के बीच 9 सैन्य तख्तापलट और सशस्त्र संघर्षों, कमज़ोर शासन प्रणाली और कट्टरपंथ के बढ़ते प्रभाव के चलते अफ्रीका में भारत के साथ सुरक्षा तथा आर्थिक साझेदारी बाधित होती है।
- संसाधन प्रतिस्पर्द्धा: अफ्रीकी तेल और गैस को लेकर भारत-चीन प्रतिस्पर्द्धा ने तनाव बढ़ा दिया है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं तथा राजनयिक दबाव बनता है, क्योंकि अफ्रीकी देश दोनों एशियाई शक्तियों के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं।
- उदाहरण: वर्ष 2006 में भारत को अंगोला में तेल परिसंपत्तियों की बोली में चीन से हार का सामना करना पड़ा था।
अफ्रीका के साथ संबंध मज़बूत करने के लिये भारत को क्या कदम उठाने चाहिये?
- व्यापार ढाँचों का पुनर्गठन: भारत को अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA) के साथ आर्थिक साझेदारियाँ बनानी चाहिये, जिसके तहत कॉफी, कोको और दुर्लभ खनिजों को वरीयता प्राप्त पहुँच (भारतीय दवाओं और आईटी सेवाओं के लिये बढ़े हुए बाज़ार की पहुँच के बदले में) दी जा सकती है।
- रणनीतिक वार्ता रूपरेखा: भारत को संयुक्त एजेंडा निर्धारित करने तथा खाद्य सुरक्षा और जलवायु समुत्थानशील जैसी चुनौतियों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिये वार्षिक भारत-अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी मंच की स्थापना करनी चाहिये।
- नव-उपनिवेशवाद का सामना: भारत आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर अफ्रीकी देशों को नव-उपनिवेशवाद का मुकाबला करने में मदद कर सकता है, उदाहरण के लिये, स्थानीय स्तर पर मुद्रा छापने के लिये तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- दक्षिण सूडान, तंजानिया और मॉरिटानिया जैसे 40 से अधिक अफ्रीकी देश ब्रिटेन, फ्राँस और जर्मनी में अपनी मुद्रा छापना जारी रखे हुए हैं।
- नवाचार-संचालित क्षमता निर्माण: भारत को प्रमुख अफ्रीकी देशों में नवाचार केंद्र (Innovation Hubs) और अनुसंधान एवं विकास केंद्र (R&D Centers) स्थापित करने चाहिये, जिनका ध्यान कृषि प्रौद्योगिकी (Agri-tech), नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल प्रशासन और स्वास्थ्य सेवा पर हो। यह कार्य IIT मद्रास ज़ांज़ीबार (2023) मॉडल को आधार बनाकर किया जा सकता है।
- सुरक्षा साझेदारी को गहरा करना: भारत को नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करके, खुफिया जानकारी साझा करने और साइबर सुरक्षा सहयोग का विस्तार करके अफ्रीकी संघ सुरक्षा ढाँचे के साथ जुड़ाव को गहरा करना चाहिये।
- अवसंरचना को प्रोत्साहन: भारत को सौर ऊर्जा, जल उपचार और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं को स्पष्ट समयसीमा और जवाबदेही के साथ तेजी से आगे बढ़ाने के लिये भारत-अफ्रीका अवसंरचना आयोग की स्थापना करनी चाहिये।
निष्कर्ष:
भारत-नामीबिया और भारत-अफ्रीका संबंध ऐतिहासिक एकजुटता, रणनीतिक सहयोग और साझा विकास लक्ष्यों की मज़बूत नींव को दर्शाते हैं। हालाँकि भारत की व्यापक अफ्रीका नीति आशाजनक है, लेकिन इसमें निवेश की कमी, क्षेत्रीय असंतुलन और बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा जैसी चुनौतियों से निपटने के लिये रणनीतिक पुनर्समीक्षा की आवश्यकता है। मज़बूत संवाद, नवाचार-आधारित क्षमता निर्माण और समावेशी व्यापार ढाँचे भारत-अफ्रीका संबंधों को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकते हैं।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों को मज़बूत करने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं ? (2020) (a) अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न. ‘उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत द्वारा प्राप्त नव-भूमिका के कारण उत्पीड़ित एवं उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में दीर्घकाल से संपोषित भारत की पहचान लुप्त हो गई है’। विस्तार से समझाइये। (2019) |


चर्चित स्थान
सिएरा लियोन
स्रोत: द हिंदू
सिएरा लियोन के कई द्वीप बढ़ते समुद्री स्तर के कारण डूबने की कगार पर हैं, जो पश्चिमी अफ्रीका में जलवायु-प्रेरित विस्थापन के सबसे गंभीर मामलों में से एक है।
सिएरा लियोन:
- स्थान: सिएरा लियोन पश्चिम अफ्रीका के दक्षिण-पश्चिमी तट पर स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है, जिसकी सीमा गिनी (उत्तर और पूर्व), लाइबेरिया (दक्षिण) और अटलांटिक महासागर (पश्चिम) से लगती है।
- इसमें बनाना और टर्टल द्वीप समूह शामिल हैं, जो पर्यटन और सांस्कृतिक महत्त्व के लिये जाने जाते हैं।
- इसकी राजधानी फ्रीटाउन विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है।
- इतिहास: सिएरा लियोन को वर्ष 1787 में इंग्लैंड से आए पूर्व गुलाम लोगों द्वारा उपनिवेशित किया गया था, इसके बाद वर्ष 1792 में नोवा स्कोटिया और वर्ष 1800 में जमैका से आए लोग यहाँ निवास करने लगे।
- प्रारंभ में सिएरा लियोन कंपनी द्वारा प्रबंधित, यह वर्ष 1808 में ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बन गया तथा वर्ष 1961 में इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई।
- भूगोल और पारिस्थितिकी: इस द्वीप में मैंग्रोव दलदलों से युक्त तटीय क्षेत्र, जंगलों से ढके पहाड़ी इलाके, ऊँचा पठारी क्षेत्र तथा पूर्वी हिस्से में पर्वत शृंखलाएँ पाई जाती हैं।
यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय (tropical) है।- इसकी सबसे ऊँची पर्वत चोटी माउंट बिंटुमानी (लोमा मंसा) तथा प्रमुख नदियाँ रोकल, ताइआ, मोआ और सेवा हैं।
- अर्थव्यवस्था: मुख्यतः कृषि प्रधान, जहाँ निर्वाह खेती ही मुख्य आजीविका है। यह हीरे, सोना, बॉक्साइट और रूटाइल (टाइटेनियम डाइऑक्साइड) जैसे खनिज संसाधनों से भी समृद्ध है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता:
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का सदस्य
- भारत उन पहले देशों में से एक था जिसने संयुक्त राष्ट्र सिएरा लियोन मिशन (UNAMSIL) में योगदान दिया। वर्ष 2000–2001 में भारत ने वहाँ 4,000 सैनिकों की सैन्य टुकड़ी तैनात की थी।
और पढ़ें: सिएरा लियोन में तख्तापलट का प्रयास