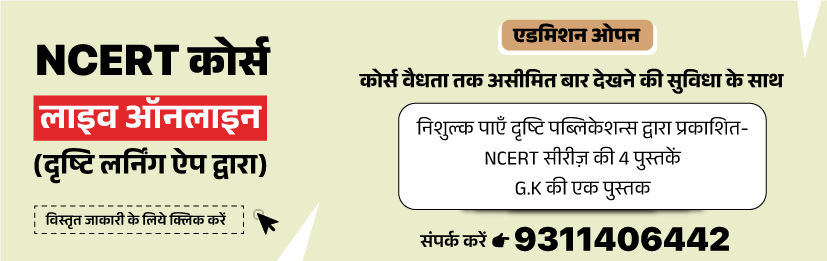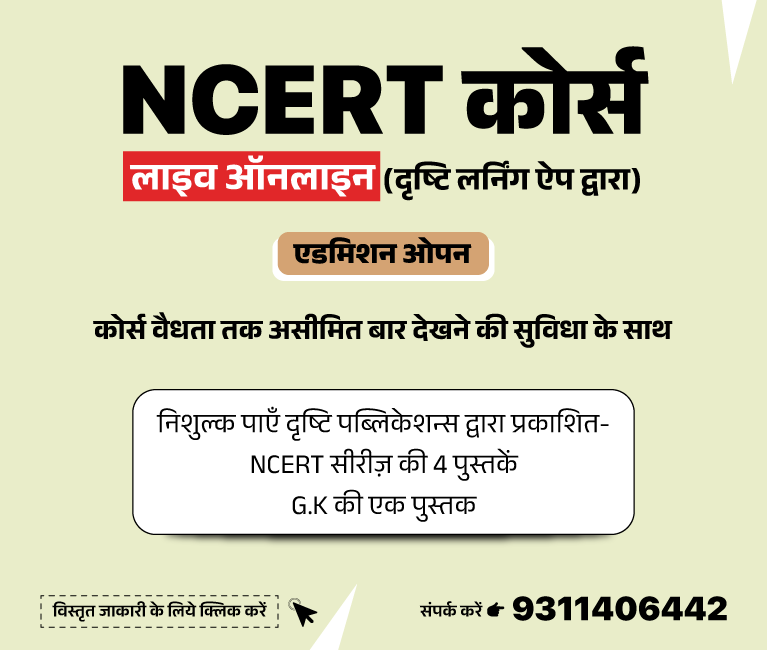विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
मेघा-ट्रॉपिक्स-1 उपग्रह
प्रिलिम्स के लिये:मेघा-ट्रॉपिक्स-1 उपग्रह, इसरो, उपग्रह का पुन: प्रवेश, सीएनईएस, भू प्रेक्षण उपग्रह। मेन्स के लिये:मेघा-ट्रॉपिक्स-1 उपग्रह। |
चर्चा में क्यों?
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा हाल ही में सेवामुक्त किये गए मेघा-ट्रॉपिक्स-1 (MT-1) उपग्रह के नियंत्रित पुन: प्रवेश परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- 5°S और 14°S अक्षांश तथा 119°W और 100°W देशांतर के बीच प्रशांत महासागर के बीच एक निर्जन क्षेत्र को MT-1 के इच्छित पुन: प्रवेश क्षेत्र के रूप में चुना गया था।
नियंत्रित पुनः प्रवेश:
- लक्षित सुरक्षित क्षेत्र के भीतरी प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिये नियंत्रित पुन: प्रवेश में बहुत कम ऊँचाई पर डी-ऑर्बिटिंग की आवश्यकता होती है।
- आमतौर पर बड़े उपग्रहों या रॉकेट निकायों, जिनकी पुन: प्रवेश पर एयरो-थर्मल विखंडन से बचने की संभावना होती है, को ग्राउंड कैज़ुअल्टी रिस्क को सीमित करने के लिये नियंत्रित री-एंट्री से गुज़रना पड़ता है।
- एयरो-थर्मल विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उच्च गति से पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से यात्रा करने वाली कोई वस्तु अत्यधिक गर्मी और दबाव का अनुभव करती है, जिससे वह अलग हो जाती है या खंडित हो जाती है।
- हालाँकि ऐसे सभी उपग्रहों को विशेष रूप से उनके जीवन के अंत में नियंत्रित पुन: प्रवेश प्रक्रिया से गुज़रने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
MT-1 उपग्रह के प्रमुख बिंदु क्या हैं?
- परिचय:
- यह एक इंडो-फ्रेंच अर्थ ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट है, जिसे उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिये अक्तूबर 2011 में लॉन्च किया गया था।
- इस मिशन का मुख्य उद्देश्य संवहन प्रणालियों के जीवन चक्र को समझना है जो उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के वातावरण में ऊर्जा तथा नमी बजट में उनकी भूमिका को समझने में मदद करते हैं।
- इसकी वृत्ताकार कक्षा भूमध्य रेखा से 20 डिग्री झुकी हुई है, यह जलवायु अनुसंधान हेतु एक तरह का उपग्रह है जिसने पूर्वानुमान मॉडल (Prediction Models) को परिष्कृत करने में वैज्ञानिकों की सहायता की है।
- पेलोड:
- माइक्रोवेव एनालिसिस एंड डिटेक्शन ऑफ रेन एंड एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर्स (MADRAS), एक इमेजिंग रेडियोमीटर जिसे सेंटर नेशनल डी'एट्यूड्स स्पैटियालेस (CNES), फ्राँस और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- CNES से साउंडर फॉर प्रोबिंग वर्टिकल्स प्रोफाइल्स ऑफ ह्यूमिडिटी (SAPHIR)
- CNES से स्कैनर फॉर रेडिएशन बजट (ScaRaB)
- इटली से खरीदे गए रेडियो ऑक्यूलेशन सेंसर फॉर वर्टिकल प्रोफाइलिंग ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी (ROSA)
स्रोत: द हिंदू


सामाजिक न्याय
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: सशस्त्र बलों में महिलाएँ
प्रीलिम्स के लिये:भारत की महिला श्रम बल भागीदारी, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाएँ ILO, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। मेन्स के लिये:सशस्त्र बलों में महिलाओं की स्थिति, भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी। |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्रुप कैप्टन शालिज़ा धामी का चयन पश्चिमी क्षेत्र (पाकिस्तान का सामना करने वाली) में एक फ्रंटलाइन लड़ाकू इकाई की कमान संभालने के लिये किया गया है।
- वह पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालने वाली भारतीय वायु सेना की पहली महिला अधिकारी होंगी।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस:
- परिचय: यह प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इसमें शामिल है:
- महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न
- महिलाओं की समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाना
- त्वरित लैंगिक समानता के लिये लॉबिंग
- महिला-केंद्रित अनुदान आदि के लिये धन उगाहना।
- संक्षिप्त इतिहास:
- महिला दिवस पहली बार वर्ष 1911 में क्लारा ज़ेटकिन द्वारा मनाया गया था, जो एक जर्मन महिला थीं। इस उत्सव की शुरुआत पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में श्रमिक आंदोलन के दौरान हुई थी।
- हालाँकि पहली बार वर्ष 1913 में यह समारोह 8 मार्च को मनाया गया था और तब से इसी दिन मनाया जाता है।
- वर्ष 1975 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।
- दिसंबर 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी ऐतिहासिक और राष्ट्रीय परंपराओं के अनुसार सदस्य देशों द्वारा वर्ष के किसी भी दिन मनाए जाने वाले महिला अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिये संयुक्त राष्ट्र दिवस की घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया।
- महिला दिवस पहली बार वर्ष 1911 में क्लारा ज़ेटकिन द्वारा मनाया गया था, जो एक जर्मन महिला थीं। इस उत्सव की शुरुआत पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में श्रमिक आंदोलन के दौरान हुई थी।
- थीम:
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2023 की थीम "डिजिटऑल: लैंगिक समानता के लिये नवाचार और प्रौद्योगिकी" है और इसका उद्देश्य लैंगिक मुद्दों को प्रकाश में लाने में प्रौद्योगिकी के महत्त्व पर ज़ोर देना है।
सशस्त्र बलों में महिलाओं की स्थिति:
- पृष्ठभूमि:
- भारतीय वायु सेना में वर्ष 2016 में महिला फाइटर पायलटों को शामिल किया गया। पहले बैच में तीन महिला फाइटर पायलट शामिल थीं, जो वर्तमान में मिग-21, Su-30MKI और राफेल उड़ाती हैं।
- महिला अधिकारियों ने इंजीनियरिंग, सिग्नल, आर्मी एयर डिफेंस, इंटेलिजेंस कॉर्प्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डनेंस कॉर्प्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सहित हथियारों और सेवाओं में विभिन्न सेना इकाइयों की कमान संभालनी शुरू कर दी है।
- वर्तमान सांख्यिकी:
- सशस्त्र बलों में 10,493 महिला अधिकारी कार्यरत हैं, जिनमें अधिकांश चिकित्सा सेवाओं में हैं।
- भारतीय थल सेना तीनों सेवाओं में सबसे बड़ी होने के साथ ही इसमें 1,705 महिला अधिकारी (सबसे अधिक संख्या में) हैं, इसके बाद भारतीय वायु सेना में 1,640 महिला अधिकारी और भारतीय नौसेना में 559 महिला अधिकारी हैं।
- जनवरी 2023 में सेना ने पहली बार सियाचिन ग्लेशियर पर एक महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान को तैनात किया है।
- फरवरी 2023 में सेना ने पहली बार महिला अधिकारियों को चिकित्सा क्षेत्र से बाहर कमांड भूमिकाएँ सौंपना शुरू किया है।
- उनमें से लगभग 50 को उत्तरी और पूर्वी कमान के तहत परिचालन क्षेत्रों में कमांड इकाइयों हेतु नियुक्त किया गया है, जो चीन के साथ भारत की सीमाओं की रखवाली करेंगी।
- नौसेना ने महिला अधिकारियों को फ्रंटलाइन जहाज़ों पर भी शामिल करना शुरू कर दिया है, जो पहले महिला अधिकारियों हेतु नो-गो ज़ोन था।
- इनमें से कई को सेना की संवेदनशील उत्तरी और पूर्वी कमान में तैनात किया गया है।
लैंगिक समानता से संबंधित चिंताएँ:
- वैश्विक:
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अनुसार, लैंगिक समानता एक दूर का सपना बनता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) का अनुमान है कि अगर स्थिति ऐसी ही बनी रहीं तो 300 वर्ष का और अधिक समय लगेगा।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, कानूनी बाधाओं ने 2.7 बिलियन महिलाओं को पुरुषों के समान नौकरी के अवसर प्राप्त करने से रोका है।
- 2019 तक सांसद महिलाएँ 25% से कम थीं।
- तीन में से एक महिला लिंग आधारित हिंसा का अनुभव करती है।
- भारत के संदर्भ में:
- सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के आँकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2021 तक पुरुष श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 67.4% थी, जबकि महिला LFPR 9.4% था।
- यहाँ तक कि अगर कोई विश्व बैंक से डेटा प्राप्त करता है, तो भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर लगभग 25% है, जबकि वैश्विक औसत 47% है।
- वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक (जो लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को मापता है) में भारत वर्ष 2022 में 135वें स्थान पर खिसक गया।
- हालाँकि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने अपनी भविष्य की रिपोर्ट में देशों को रैंक प्रदान करने के लिये पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के मानदंड में बदलाव करने पर सहमति व्यक्त की है। इससे वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति बेहतर होगी।
- अंतर-संसदीय संघ (IPU), जिसमें भारत एक सदस्य है, द्वारा संकलित आँकड़ों के अनुसार लोकसभा के कुल सदस्यों में से महिलाएँ केवल 14.44% का प्रतिनिधित्त्व करती हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा 2018 में किये गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत की 95% से अधिक कामकाज़ी महिलाएँ अनौपचारिक श्रमिक हैं, जो बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के गहन श्रम, न्यूनतम-वेतन, अत्यधिक अनिश्चित रोज़गार/परिस्थितियों में काम करती हैं।
सशस्त्र बलों में महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ:
- सामाजिक चुनौतियाँ:
- पुरुष अधिकारियों वाली संरचना, मुख्य रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि के प्रचलित सामाजिक मानदंडों के साथ इकाइयों की कमान में महिला अधिकारियों को स्वीकार करने के लिये सैनिकों को अभी तक मानसिक रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया है।
- शत्रु देश द्वारा युद्ध बंदी की स्थिति में पकड़ी गई महिला अधिकारी के प्रति समाज की कम स्वीकार्यता है।
- शारीरिक चुनौतियाँ:
- मातृत्त्व, बच्चों का पालन-पोषण और मनोवैज्ञानिक बाधाएँ महत्त्वपूर्ण कारक हैं जो सेना में महिला अधिकारियों की भर्ती को प्रभावित करते हैं।
- गर्भावस्था, मातृत्त्व और विस्तारित घरेलू जिम्मेदारियों के कारण महिलाओं के लिये इन सेवा संबंधी जोखिमों को संभालना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब पति और पत्नी दोनों सैन्यकर्मी हों।
- पारिवारिक मुद्दे:
- सशस्त्र बलों के सेवा कर्मियों को पारिवारिक कर्तव्य के निर्वहन से परे बलिदान और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, जिसमें बार-बार स्थानांतरण जैसी परिस्थितियाँ शामिल हैं, जो बच्चों की शिक्षा और जीवनसाथी की नौकरी को प्रभावित करती है।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न:प्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा समूह विश्व के देशों को उनके "ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स" के अनुसार रैंक प्रदान करता है? (2017) (a) वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. समय और स्थान के संदर्भ में भारतीय महिलाओं को किन संघर्षों का सामना करना पड़ता है? (2019) प्रश्न. विविधता, निष्पक्षता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिये उच्च न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्त्व की वांछनीयता पर चर्चा कीजिये। (2021) |
स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस
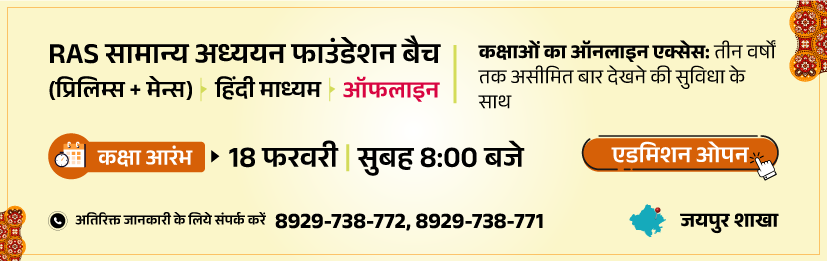
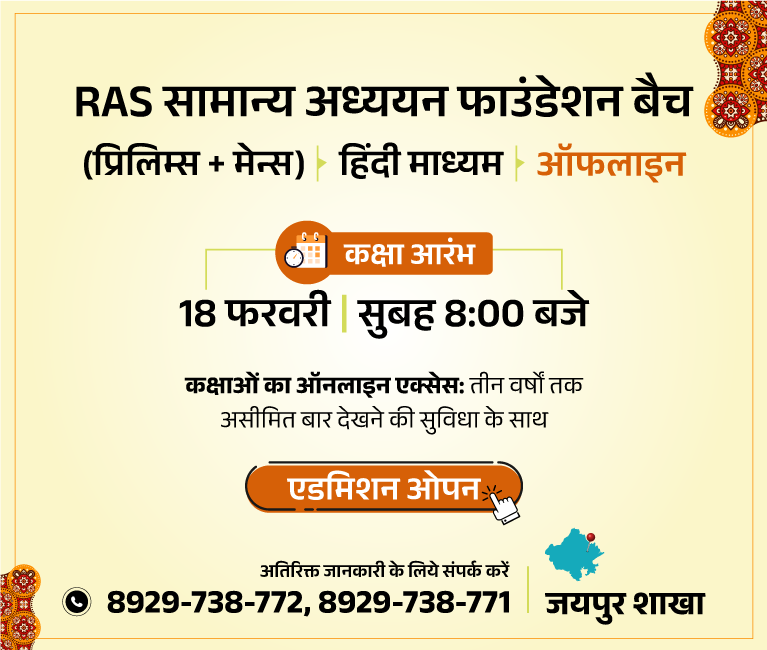
शासन व्यवस्था
राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC)
प्रिलिम्स के लिये:राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), परामर्श, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE), 2020-2021। मेन्स के लिये:भारत में वर्तमान प्रत्यायन मानदंड, भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित चुनौतियाँ। |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (National Assessment and Accreditation Council- NAAC) पर अनियमित रूप से कार्य संचालन का आरोप लगाया गया है।
राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद:
- परिचय:
- यह भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करने हेतु ज़िम्मेदार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC) के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी।
- NAAC के कार्य:
- एक बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से, जैसे- पाठ्यक्रम, संकाय, बुनियादी ढाँचे, अनुसंधान और वित्तीय कल्याण आदि मापदंडों के आधार पर A++ से लेकर C तक के ग्रेड प्रदान करता है।
- आरोप:
- NAAC की कार्यकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष ने यह आरोप लगाने के बाद इस्तीफा दे दिया कि कदाचार के कारण कुछ संस्थानों को संदिग्ध ग्रेड दिया जा रहा है।
- एक जाँच आयोग ने IT प्रणाली और मूल्यांकनकर्त्ताओं के आवंटन में अनियमितताएँ पाईं।
- जाँच में यह भी बताया गया है कि लगभग 4,000 मूल्यांकनकर्त्ताओं के पूल से लगभग 70% विशेषज्ञों को साइट का दौरा करने का कोई अवसर नहीं मिला है।
- जनवरी 2023 तक उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) 2020-2021 में 1,113 विश्वविद्यालयों और 43,796 कॉलेजों में से केवल 418 विश्वविद्यालय तथा 9,062 कॉलेज NAAC से मान्यता प्राप्त थे।
भारत में वर्तमान प्रत्यायन मानदंड क्या हैं?
- मानदंड:
- वर्तमान में केवल वही संस्थान जो कम-से-कम 6 वर्ष पुराने हैं या जहाँ से छात्रों के कम-से-कम दो बैच स्नातक हैं, मान्यता हेतु आवेदन कर सकते हैं, जो 5 वर्षों के लिये वैध है।
- प्रत्यायन अधिदेश:
- NAAC द्वारा प्रत्यायन स्वैच्छिक है, हालाँकि UGC द्वारा कई परिपत्र जारी किये गए हैं जिनमें संस्थानों से मूल्यांकन कराने का आग्रह किया गया है।
- मान्यता में तेज़ी लाने के प्रयास:
- UGC ने मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक संस्थानों को सलाह देने के लिये वर्ष 2019 में 'परामर्श' नाम से एक योजना शुरू की।
- NAAC ने एक पुराने संस्थानों को प्रोविजनल एक्रिडिटेशन फॉर कॉलेजेज़ (PAC) जारी करने की संभावना तलाशी।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) ने अगले 15 वर्षों में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को उच्चतम स्तर की मान्यता प्राप्त करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में अन्य चुनौतियाँ क्या हैं?
- सीमित पहुँच: उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद सीमांत समुदायों के कई छात्र अभी भी प्रवेश की बाधाओं का सामना करते हैं, जिसमें वित्तीय बाधाएँ और शैक्षिक अवसरों की कमी शामिल है।
- विशेष रूप से दिव्यांग श्रेणी के छात्रों की संख्या 2019-20 के 92,831 से घटकर 2020-21 में 79,035 हो गई।
- लैंगिक असमानता: महिलाओं को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों एवं समर्थन प्रणालियों की कमी सहित अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
- उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE), 2020-21 में उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में महिला नामांकन कुल नामांकन का 49% था।
- रोज़गार के मुद्दे: बड़ी संख्या में स्नातक होने के बावजूद भारत में कई छात्र व्यावहारिक कौशल और उद्योग-संबंधित शिक्षा की कमी के कारण रोज़गार पाने के लिये संघर्ष करते हैं।
- इसके अतिरिक्त भारतीय अनुसंधान उत्पादन के मामले में कई अन्य देशों से पीछे है, एवं कई उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान संस्कृति का अभाव है।
आगे की राह
- डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन: डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग शिक्षा को अधिक कुशल, किफायती और सुलभ बना सकता है।
- संस्थानों को डिजिटल की बुनियादी संरचनाओं में निवेश करना चाहिये और नई तकनीकों के अनुकूल छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिये।
- प्रत्यायन में वृद्धि: प्रत्यायन की प्रक्रिया को अत्यधिक पारदर्शी और सुलभ बनाया जाना चाहिये ताकि संस्थानों को प्रत्यायन प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।
- इसके अतिरिक्त सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि मान्यता प्रक्रिया निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त हो।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भारत में शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकता है।
- सूचना, कौशल और सामग्री के आदान-प्रदान के लिये संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग करना चाहिये।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न:प्रिलिम्स:प्रश्न.'उन्नत भारत अभियान' कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? (2017) (a) स्वैच्छिक संगठनों एवं सरकार की शिक्षा प्रणाली तथा स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर 100% साक्षरता हासिल करना। उत्तर: (b) |
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
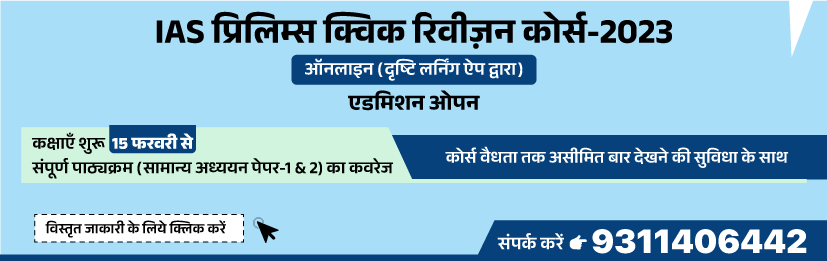
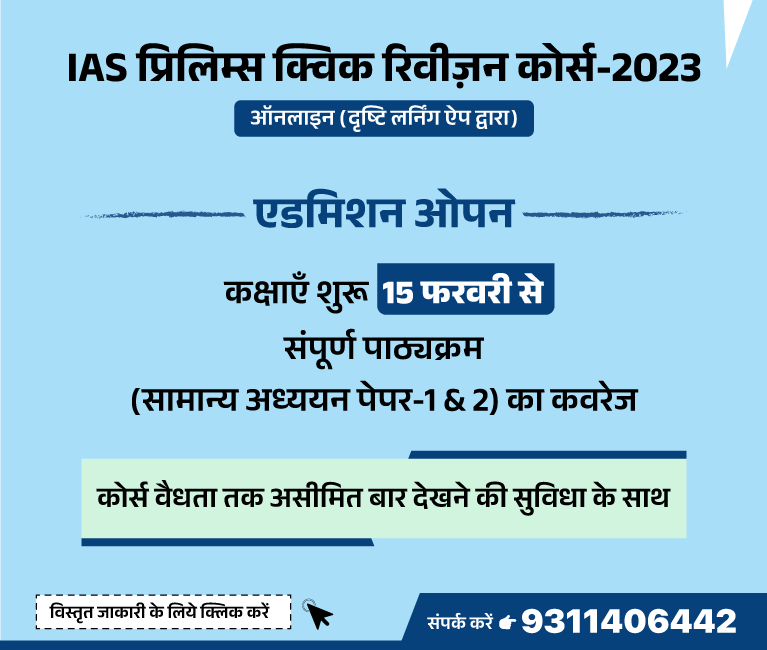
अंतर्राष्ट्रीय संबंध
अफगानिस्तान पर भारत-मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह (JWG)
प्रिलिम्स के लिये:अफगानिस्तान पर भारत-मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह (JWG), ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन मेन्स के लिये:वैश्विक समूह, भारत और उसके पड़ोस, भारत के लिये मध्य एशिया का महत्त्व, क्षेत्र की भू-राजनीतिक गतिशीलता। |
चर्चा में क्यों?
भारत चाबहार बंदरगाह के माध्यम से तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान को सहायता के रूप में गेहूँ की अपनी अगली खेप भेजेगा। दिल्ली में अफगानिस्तान पर भारत-मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह (JWG) की पहली बैठक में इस निर्णय की घोषणा की गई।
- भूमि मार्ग से गेहूँ के भेजने हेतु पाकिस्तान के साथ समझौते की समाप्ति के बाद इस व्यवस्था को नवीनीकृत करने के प्रयास असफल रहे।
संयुक्त कार्य समूह से संबंधित प्रमुख बिंदु:
- JWG की बैठक जनवरी 2022 में भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के एक वर्ष बाद हुई, जहाँ अफगानिस्तान पर एक विशेष संपर्क समूह गठित करने के निर्णय की घोषणा की गई थी।
- मादक पदार्थों के मुद्दे, आतंकवाद और कट्टरता का प्रसार और शरणार्थी समस्या मध्य एशिया में पड़ोसी देशों के लिये चिंता का विषय रहे हैं।
- UNODC की रिपोर्ट के अनुसार, तालिबान द्वारा काबुल पर नियंत्रण करने के बाद पिछले एक साल में अफीम का उत्पादन लगभग एक-तिहाई बढ़ गया है।
- विश्व का 80% से अधिक अफीम और हेरोइन की तस्करी अफगानिस्तान से की जाती है, जो कि गोल्डन क्रिसेंट का एक हिस्सा है।
- अनुमानित 30 लाख लोग या अफगानिस्तान की आबादी का लगभग दसवाँ हिस्सा अफीम का आदी है।
- UNODC की रिपोर्ट के अनुसार, तालिबान द्वारा काबुल पर नियंत्रण करने के बाद पिछले एक साल में अफीम का उत्पादन लगभग एक-तिहाई बढ़ गया है।
- JWG ने "वास्तव में समावेशी और प्रतिनिधि राजनीतिक संरचना के गठन के महत्त्व पर बल दिया जो अल्पसंख्यकों, महिलाओं, लड़कियों सहित सभी अफगानों के लिये समान अधिकारों का विस्तार करता है।
JWG बैठक के प्रमुख परिणाम:
- संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों सहित किसी भी आतंकी संगठन को शरण नहीं दी जानी चाहिये या अफगानिस्तान के क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
- भारत की सहमति:
- UNODC (संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय) के अधिकारियों और हितधारकों के लिये अनुकूलित क्षमता निर्माण।
- नशीली दवाओं की तस्करी का मुकाबला करने और अफगान ड्रग उपयोगकर्त्ताओं, विशेष रूप से महिलाओं के लिये पुनर्वास प्रयासों की पहल पर सहयोग।
अफगानिस्तान के लिये भारत के सहायता उपाय:
- अनाज:
- वर्ष 2022 में भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूँ के वितरण के लिये संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसे मानवीय सहायता के रूप में अफगानिस्तान भेजने के लिये भारत प्रतिबद्ध है।
- भारत ने कोविड-19 वैश्विक महामारी और खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिये वर्ष 2020 में अफगानिस्तान को 75,000 मीट्रिक टन गेहूँ देने की प्रतिबद्धता जताई।
- भारत ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने, विशेषकर सूखे के समय बच्चों के लिये वर्ष 2018 में अफगानिस्तान को 2000 टन दाल भेजी।
- चिकित्सा आपूर्ति:
- वर्ष 2020 में भारत ने अफगानिस्तान सरकार को सर्जिकल दस्ताने के 50,000 जोड़े, पेरासिटामोल की 1 लाख टैबलेट्स और हाइड्रॉक्सी-क्लोरोक्विनोन की 5 लाख टैबलेट्स प्रदान कीं।
- भारत ने वर्ष 2015 में काबुल में एक मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना की, जो अफगानी बच्चों को नवीनतम नैदानिक सुविधाएँ प्रदान करता है और भारत के लिये सद्भावना पैदा करता है।
- आधारभूत संरचना:
- भारत द्वारा वर्ष 2001 से अफगानिस्तान के पुनर्वास प्रयासों के लिये 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:प्रिलिम्स:प्रश्न . भारत के चाबहार बंदरगाह के निर्माण का क्या महत्त्व है? (2017) (a) अफ्रीकी देशों के साथ भारत के व्यापार में भारी वृद्धि होगी। उत्तर: (c) व्याख्या:
मेन्सप्रश्न. संसार के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक राज्यों से भारत की निकटता ने उसकी आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार एवं बंदूक बेचने, गुपचुप धन विदेश भेजने और मानव तस्करी जैसे अवैध गतिविधियों के बीच की कड़ियों को स्पष्ट कीजिये। इन गतिविधियों को रोकने के लिये क्या-क्या उपाय किये जाने चाहिये? (मुख्य परीक्षा, 2018) |
स्रोत: द हिंदू