हमारे लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हम क्या बनने जा रहे हैं
- 26 May, 2025
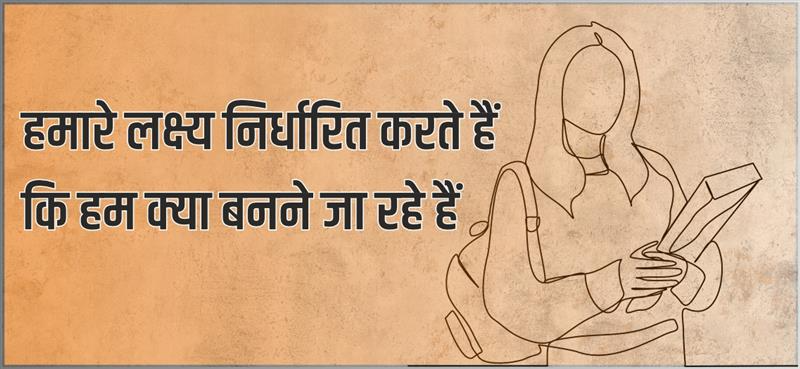
लक्ष्य, ऐसी आकांक्षाएँ हैं जिन्हें एक निश्चित समय सीमा में पूरा करने या हासिल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की जाती है। लक्ष्य में विशिष्ट उद्देश्य, समयबद्धता और संकल्प जैसे तत्त्वों का प्रमुख रूप से समावेश होता है एवं ये प्रत्येक व्यक्ति या समुदाय की अपनी अभिरुचि के अनुसार होते हैं। इनमें त्याग और रणनीति के तत्त्व भी महत्त्वपूर्ण होते हैं। किसी भी प्रकार का लक्ष्य बिना त्याग एवं रणनीति के प्राप्त करना असंभव है। लक्ष्य तय करना स्वयं की जवाबदेही का एक तरीका है, भले ही असफलता हाथ लगे।
लक्ष्य तय करने से हमें अपने जीवन को सरल बनाने और अपनी रुचि के अनुसार जीने में सहायता मिलती है। लक्ष्य हमें अनुसरण करने के लिये एक मार्ग सुझाते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिये काम करना हमें बताता है कि हम जीवन में वास्तव में क्या चाहते हैं। इससे हमें चीज़ों की प्राथमिकताएं तय करने में भी मदद मिलती है। यदि हम बिना किसी लक्ष्य के जीवन में भटकना चुनते हैं तो भी यह निश्चित रूप से हमारी ही पसंद है। लक्ष्य निर्धारित करने से हमें वैसा जीवन जीने में मदद मिलती है, जैसा कि हम वास्तव में जीना चाहते हैं। इस तरह से लक्ष्य यह तय करते हैं कि हम भविष्य में क्या बनने जा रहे हैं।
इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिये, "मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होना चाहता हूँ", यह एक लक्ष्य है। इसके लिये "मैं इस महीने से अपने अध्ययन की अवधि को बढ़ाकर दस घंटे कर दूँगा", यह संकल्प है। संकल्प लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। "मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करना चाहता हूँ"। यह भी एक लक्ष्य है और इसके लिये मेरा संकल्प है कि मैं रोजाना 20 किलोमीटर साइकिल चलाऊंगा | यह समझना होगा कि लक्ष्य हासिल करने के साधन अनेक हो सकते हैं पर संकल्प लेना सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण साधन है। हासिल किये जाने वाला लक्ष्य स्थाई होता है और यह निरंतर प्रगति की मांग करता है। संकल्प की प्रकृति में परिवर्तन आ सकता है पर लक्ष्य वही रहता है। इसका एक प्रमुख प्रभाव यह पड़ता है कि जिन लोगों ने स्पष्ट रूप से लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, वे अपने खाली समय का आनंद उन लोगों की तुलना में अधिक ले सकते हैं, जिन्होंने लक्ष्य निर्धारित नहीं किये हैं। वे अपनी योजना के अनुसार काम करके संतुष्ट बने रह सकते हैं।
लक्ष्य को पाने में संकल्प के बाद त्याग की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना त्याग के संकल्प पूरा नहीं किया जा सकता। यह सही है कि हमें अपने जीवन के प्रत्येक पल को योजनाबद्ध तरीके से जीने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम सभी को ऐसे दिनों का सामना करना पड़ सकता है, जब संकल्प पूरा नहीं किया जा सकता । हालाँकि, असली चुनौती यह तय करना नहीं है कि हम परिणाम चाहते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक त्याग किया जा सकता है। जीवन के लक्ष्य केवल हँसते-खेलते-गाते हासिल नहीं होते। लक्ष्य हासिल करने का रास्ता अति ऊबाऊ भी हो सकता है। यह सोचना आसान है कि हम क्या कर सकते हैं या हम क्या करना चाहते हैं। किंतु अपने लक्ष्यों के साथ आने वाले समझौतों को स्वीकार करना पूरी तरह से अलग बात है। जैसे हर खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतना चाहता है, किंतु बहुत कम लोग ओलंपियन की तरह प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। यह बात भलीभांति समझनी होगी कि लक्ष्य निर्धारण का अर्थ केवल उन पुरस्कारों एवं प्रतिष्ठा को चुनना भर नहीं है जिनका आनंद लेना है, बल्कि उन लागतों को चुनना भी है जिन्हें चुकाने के लिये तैयार होना होता है। यदि हममें कीमत चुकाने की तत्परता नहीं है तो हम क्या बनेंगे, यह हम नहीं बल्कि हमारे हालात तय कर देंगे।
विचारकों ने लक्ष्यों के सात सामान्य प्रकारों की चर्चा की है। इनमें पहला है अल्पकालिक लक्ष्य। इस प्रकार के लक्ष्य आमतौर पर अपेक्षाकृत जल्दी प्राप्त होते हैं। उनको मासिक, साप्ताहिक या दैनिक लक्ष्यों में विभाजित कर सकते हैं। दूसरा प्रकार है दीर्घकालिक लक्ष्य। दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिये, आमतौर पर अधिक विस्तारित अवधि की आवश्यकता होती है, जैसे कि कई महीने अथवा साल। तीसरा है व्यक्तिगत लक्ष्य। इस प्रकार के लक्ष्य निजी जीवन से संबंधित होते हैं, जैसे स्वास्थ्य, रिश्ते और अभिरुचि। चौथा प्रकार है व्यावसायिक लक्ष्य। ये लक्ष्य कैरियर की सफलता से संबंधित होते हैं और नौकरी के प्रदर्शन, पदोन्नति और कौशल विकास पर केंद्रित हो सकते हैं। पाँचवाँ प्रकार वित्तीय लक्ष्य है, जोकि धन के अर्जन से संबंधित होते हैं, जैसे कि मकान खरीदने के लिये बचत करना, ऋण चुकाना या सेवानिवृत्ति के लिए निवेश करना। छठा प्रकार है शैक्षणिक लक्ष्य। शिक्षा में परिणाम प्राप्त करने के लिये ये लक्ष्य निर्धारित होते हैं, जैसे डिग्री लेना, ग्रेड में सुधार या कोई नया कौशल सीखना। सातवाँ और अंतिम प्रकार का लक्ष्य सामाजिक लक्ष्य कहा गया है। सामाजिक लक्ष्य सामाजिक कार्यों से संबंधित हैं और इसमें नए दोस्त बनाना, अपने संचार कौशल में सुधार करना या सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। यह आवश्यक नहीं कि केवल एक लक्ष्य ही एक समय में लिया जाए, एक साथ दो या दो से अधिक लक्ष्य भी निर्धारित किये जा सकते हैं।
इन सातों में किसी भी प्रकार के लक्ष्य या लक्ष्यों का निर्धारण ही वह भविष्यवाणी है जो हमें यह बताती है कि हम क्या बनने जा रहे हैं। लक्ष्य का निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी चीज़ की पहचान की जाती है और उसे पाने की मनोकामना होती है। मनचाही चीज़, पद या प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन, प्रस्थिति, अच्छे अंक, प्रशंसा आदि। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये हमें कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती हैं। इस प्रक्रिया में दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य बनाना शामिल हो सकता है जो अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने, लक्ष्य पाने और अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करने में सहायता करते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने से आत्मविश्वास बढ़ सकता है, प्रेरणा बढ़ सकती है और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा मिल सकता है। कोई भी व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित कर सकता है, लेकिन उसे सफलतापूर्वक प्राप्त करना लक्ष्य निर्धारण के लिये उपयोग किये जाने वाले मापदंडों पर निर्भर करता है, इसलिये यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना महत्त्वपूर्ण है। अगर आप अपनी जीवन योजना खुद नहीं बनाते हैं तो संभावना है कि आप किसी और की योजना में फँस जाएंगे तब सोचना होगा कि क्या उन्होंने आपके लिये योजना बनाई थी, निश्चित तौर पर नहीं। जिन लोगों ने महान कार्य किये हैं, उन्होंने अपनी दृष्टि एक ऐसे लक्ष्य पर केंद्रित की, जो ऊँचा था, जो कभी-कभी असंभव प्रतीत होता था, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत से उसे हासिल किया।
लक्ष्य निर्धारण दुनिया में हर जगह है पर जिस चीज़ के बारे में हम पर्याप्त नहीं सोचते, वह यह है कि अपने लक्ष्यों को कैसे पूरा किया जाए, उसे पूरा करने का विज्ञान और रणनीति क्या है। हम क्या बनने जा रहे हैं, इसके बारे में पर्याप्त विचार नहीं किया जाता । इसलिये जब लक्ष्य निर्धारण की बात आती है तो स्पष्टता महत्त्वपूर्ण होती है। स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य तय करने से वह भ्रम दूर होता है जो तब होता है, जब लक्ष्य को अधिक सामान्य तरीके से निर्धारित किया जाता है। चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिमाग को आगे बढ़ाते हैं और बड़ा सोचने के लिये प्रेरित करते हैं। याद रखना होगा कि रातोरात गंतव्य को नहीं बदल सकते, लेकिन रणनीति से रातोरात दिशा अवश्य बदल सकते हैं। कुछ बनने के लिये लक्ष्य को अधिक प्रभावी और सार्थक बनाने के लिये यह पहचानना महत्त्वपूर्ण है कि कौन से लक्ष्य व्यक्तिगत मूल्यों और प्राथमिकताओं के साथ संरेखित हैं। हम जिस सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं, उसके सबसे नीचे रहना, उस सीढ़ी के शीर्ष पर रहने से बेहतर है, जिस पर चढ़ना ही नहीं था। अगर लक्ष्य निर्धारित करने के तरीके के बारे में सोच-समझकर काम किया जाए तो लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जब यह संरेखण नहीं होता तो तय लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता या फिर ऐसा हो सकता है कि दूसरी प्राथमिकताएँ सामने आ गई हों या काम पूरा होने में उम्मीद से ज़्यादा समय लग गया हो।
जो हम बनना चाहते हैं, उस लक्ष्य को लिखना एक महत्त्वपूर्ण कदम है। लक्ष्य को लिखने से वे अधिक मूर्त और ठोस बन जाते हैं। जो लोग अपना लक्ष्य लिखते हैं, उनके पास उन लोगों की तुलना में सफलता प्राप्त करने की बेहतर संभावना होती है, जो अपने लक्ष्य नहीं लिखते। जो बनना है उस बात को दूसरों के साथ साझा करने से स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ता है, जिससे सफलता की संभावना बढ़ती है। जब कोई और प्रगति को देख रहा होता है तो प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिये अधिक प्रेरणा मिलती है, ताकि वे असफल होते न देखें।
कुछ बनने के लक्ष्य अक्सर दीर्घकालिक और अमूर्त प्रकृति के होते हैं, इसलिये उन्हें छोटे एवं सरल चरणों में तोड़ना सहायक हो सकता है। इन लक्ष्यों के लिये समय-सीमा तय करने से ध्यान केंद्रित करने, योजना बनाने और प्रगति को समझने में मदद मिलती है। सफलता के लिये लक्ष्य निर्धारित करते समय यह महत्त्वपूर्ण है कि समय-सीमा यथार्थवादी हो। लक्ष्य निर्धारण में यथार्थवादी होने का आशय यह है कि उन चुनौतियों का भी ध्यान रखना चाहिये जिनका सामना करना पड़ेगा। ये बाधाएँ संसाधनों की कमी, अप्रत्याशित घटनाओं या दूसरों के कार्यों के कारण हो सकती हैं। संभावित बाधाओं की एक सूची बनाकर उन तरीकों पर विचार करना चाहिये, जिससे वे कम हो सकें। संभावित बाधाओं के बारे में जागरूक होने से सफलता के मार्ग में कम रोड़े आएंगे और वह बन सकेंगे,जो हम स्वयं के बारे में सोचते हैं।
जब हम यह तय कर लेते हैं कि हमें क्या बनना है तो तीन बुनियादी रणनीतियों का उपयोग करना चाहिये। इनमें पहली है कि अपने विभिन्न लक्ष्यों को कम करें। इसे “लक्ष्य प्रतिस्पर्द्धा” कहा गया है। इसके अनुसार बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा दूसरे छोटे लक्ष्य हैं। यानी सभी लक्ष्य आपस में ही प्रतिस्पर्द्धा करते हैं। जब भी कोई नए लक्ष्य तय किये जाते हैं तो दूसरे कामों से ध्यान और ऊर्जा खींचनी पड़ती है। इसलिये प्रगति करने का सबसे सही तरीका यही है कि कम महत्त्वपूर्ण चीज़ों पर विराम लगाया जाए और एक समय में एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया जाए। सरल शब्दों में प्राथमिकताओं को थोड़ा सा पुनर्गठित करना आना चाहिये। जो अक्सर लक्ष्य निर्धारण की समस्या की तरह दिखता है, वह वास्तव में लक्ष्य चयन की समस्या है। हमें वास्तव में बड़े लक्ष्यों की नहीं, बल्कि बेहतर फोकस की आवश्यकता है। इस बात को एक उदाहरण से समझना होगा। हमारा जीवन गुलाब के पौधे की तरह है। जैसे-जैसे गुलाब का पौधा बढ़ता है, उसमें क्षमता से ज़्यादा कलियाँ बनती हैं। इसलिये गुलाब के पौधे को सुंदर दिखाने के लिये काटना-छाँटना ज़रूरी है। दूसरे शब्दों में, फूल ढंग से खिलने के जरूरी है कि कुछ कलियाँ कटें, ताकि फूल पूरी तरह से खिल सकें। हमारे बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिये छोटे लक्ष्यों में लगातार काँट-छाँट करने की ज़रूरत होती है। हमारे जीवन में नए लक्ष्य आना और नए अवसरों के बारे में उत्साहित होना स्वाभाविक है पर अगर हम अपने कुछ लक्ष्यों को काटने का साहस जुटा पाते हैं तो हम बाकी लक्ष्यों को पूरी तरह से खिलने के लिये ज़रूरी जगह बना लेते हैं। संक्षेप में जीवन में कुछ बनने के लिये छोटे लक्ष्यों की छँटाई की ज़रूरत होती है।
जब भी कोई नया लक्ष्य निर्धारित होता है तो सबसे महत्त्वपूर्ण बात होती है कि उस पर खरा उतरा जाए। शुरुआत में खरे उतरना सफल होने से भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि अगर खरे उतरने की आदत नहीं बनती है तो भविष्य में सुधारने के लिये कुछ भी नहीं होगा। एक अन्य बात यह भी समझनी होगी कि प्रभावी लक्ष्य निर्धारण के लिये आस-पास की व्यवस्था पर विचार करना चाहिये। अक्सर हम गलत व्यवस्था के अंदर सही लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। अगर हम लंबे समय तक प्रगति करना चाहते हैं तो माहौल को अपनी महत्त्वाकांक्षाओं के साथ जोड़ना होगा। हालाँकि हममें से अधिकांश लोगों को किसी भी समय कई तरह के विकल्प चुनने की आज़ादी होती है, लेकिन हम अक्सर अपने आस-पास के माहौल के हिसाब से फ़ैसले लेते हैं। जब लक्ष्य प्राप्त करने की बात आती है तो इसका महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दीर्घावधि में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं या नहीं, इसका बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अल्पावधि में आसपास किस प्रकार के प्रभाव हैं।
निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि हमारे निर्णय और कार्य ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं क्या। कुछ न करना भी एक निर्णय है और उसका परिणाम हमारे भविष्य के जीवन पर प्रभाव डालता है। हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सावधानीपूर्वक योजना और प्रक्रिया की आवश्यकता होती है,अन्यथा आगे चल कर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ हासिल करने में संकल्प, प्रतिबद्धता की अहम भूमिका होती है, साथ ही कई प्रकार के त्याग भी करने पड़ते हैं। इससे ही हमारा भविष्य उज्ज्वल और सुंदर बन सकता है।




