सामाजिक विभेदीकरण बनाम पदानुक्रम
- 22 May, 2025
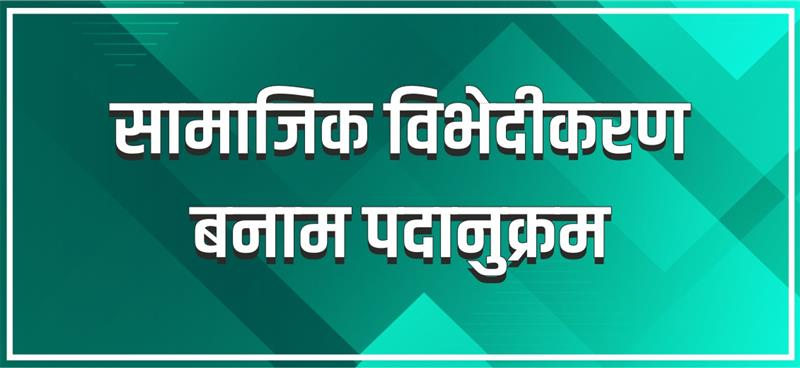
मानव समाज में ऐसा कोई युग नहीं रहा है जिसमें सभी लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति समान रही हो। प्रत्येक युग में समाज की संरचना इन्हीं दो संज्ञाओं से परिभाषित होती रही है। यही सामाजिक और आर्थिक स्थिति, समाज में दो विशेष स्थितियों को जन्म देती है। इनको सामाजिक विभेदीकरण और पदानुक्रम कहा जाता है। इस तरह से किसी समाज को समझने में सामाजिक विभेदीकरण तथा पदानुक्रम दो प्रमुख अवधारणाएँ हैं। ये दोनों किसी समाज की सामाजिक संरचना एवं मानव समूहों के संगठन के प्रारुप का पता लगाने के लिये महत्त्वपूर्ण उपागम हैं। ये अवधारणाएँ सामाजिक असमानता और समाज के संगठन के विभिन्न समान पहलुओं को दर्शाती हैं, लेकिन इनके बीच मूलभूत अंतर भी हैं।
सामाजिक विभेदीकरण सामाजिक संरचना में विभिन्न समूहों या व्यक्तियों के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। यह अंतर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या अन्य आधारों पर उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया समाज में विभिन्न भूमिकाओं, व्यवसायों और स्थिति को जन्म देती है। उदाहरण के लिये एक समाज में शिक्षक, डॉक्टर, किसान तथा व्यापारी जैसे विभिन्न व्यवसायों के आधार पर लोग अलग-अलग भूमिकाएँ निभाते हैं। यह विभेदीकरण समाज को कार्यात्मक रूप से संगठित करने में सहायता करता है, क्योंकि विभिन्न कार्यों के लिये विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। यह ध्यान रखना होगा कि सामाजिक विभेदीकरण हमेशा असमानता से संबंधित नहीं होता; यह केवल अंतर को दर्शाता है। जैसे- एक समाज में लिंग, आयु या जातीयता के आधार पर लोग अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि यह असमानता को दर्शाए, हाँ विभेद करने में सहायक अवश्य हो सकते हैं।
वहीं दूसरी ओर सामाजिक पदानुक्रम सामाजिक संरचना में शक्ति, संसाधनों और स्थिति के आधार पर असमानता की व्यवस्था को संदर्भित करता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्ति या समूह ऊँच-नीच के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। उदाहरण के लिये धन संपत्ति की मात्रा के आधार पर बने समाजों में अमीर और गरीब या जाति-आधारित समाजों में उच्च तथा निम्न जातियों के बीच पदानुक्रम देखा जा सकता है। पदानुक्रम सामाजिक शक्ति, अवसरों और संसाधनों के असमान वितरण को दर्शाता है। यह सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है तथा समाज में विशेषाधिकारों एवं वंचन की स्थिति उत्पन्न करता है। सामाजिक पदानुक्रम को सामाजिक स्तरीकरण भी कहा जाता है। यह सभी समाजों में किसी न किसी रूप में सार्वभौमिक रूप में देखा जा सकता है। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों को आय, संपत्ति, व्यवसाय, जाति, पद आदि के आधार पर उच्च और निम्न श्रेणियों के स्तरों में विभाजित करता है। इनमें से प्रत्येक विभाजन एक परत के समान होता है और जब इन सभी परतों को उच्च तथा निम्न के क्रम में रखा जाता है, तो इसे “सामाजिक स्तरीकरण या पदानुक्रम या पदों का अनुक्रम” कहा जाता है। जैसे ज़मीन के भीतर मिट्टी की परतें होती हैं वैसे ही समाज भी कई परतों या स्तरों में विभाजित होता है। इस प्रकार समाज के विभिन्न स्तरों के समूहों एवं सदस्यों में अर्थात् प्रत्येक समाज में ऐसी स्थितियाँ मिलती हैं जिनमें श्रेष्ठता एवं हीनता की भावना पाई जाती है। इसलिये सामाजिक स्तरीकरण या पदानुक्रम एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समाज को विभिन्न ऊपरी और निचले वर्गों में विभाजित किया जाता है तथा तद्नुसार सामाजिक संरचना में लोगों की प्रस्थिति एवं भूमिका को निर्धारित किया जाता है। सामाजिक स्तरीकरण एक ऐसी व्यापक प्रणाली है जो केवल सामाजिक प्रतिष्ठा, पद या हैसियत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सामाजिक अधिकारों, शक्ति, सत्ता और असमानताओं का भी वितरण करती है। सरल समाज में स्तरीकरण का सरल रूप देखने को मिलता है जबकि जटिल और आधुनिक समाजों में अनेक सामाजिक स्तर पाए जाते हैं।
इस आधार पर संक्षेप में कहा जा सकता है कि सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य समाज में व्यक्तियों को उच्च और निम्न श्रेणियों में क्रमबद्ध रूप से विभाजित करने से है। इसमें समाज का विभिन्न स्थायी श्रेणियों और समूहों में विभाजन किया जाता है तथा उच्चतर एवं अधीनता वाले परस्पर संबंध होते हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्तियों और समूहों को थोड़ी बहुत स्थायी प्रस्थितियों के उच्चतम तथा निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है। सरल रूप में स्तरीकरण या पदानुक्रम उच्च तथा निम्न सामाजिक इकाइयों में समाज का समानांतर विभाजन है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामाजिक स्तरीकरण या पदानुक्रम के द्वारा समाज को विभिन्न उच्च और निम्न समूहों में विभाजित तथा संगठित किया जाता है जहाँ ये समूह एक-दूसरे से जुड़े होते हैं तथा सामाजिक एकता व स्थिरता बनाए रखते हैं।
सामाजिक स्तरीकरण की अनिवार्यता के पक्ष की बात करें तो यह कहा जाता है कि यह समाज की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो लगभग हर समाज में पाई जाती है। सामाजिक स्तरीकरण का मूल कारण सामाजिक विभेदीकरण है, जो समाज में लोगों के बीच सामाजिक अंतर उत्पन्न करता है और उन्हें विभिन्न भागों में वर्गीकृत करता है। सामाजिक स्तरीकरण में व्यक्तियों को उनकी योग्यता तथा कार्य के अनुसार विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है, ताकि समाज की सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। इसमें समाज में विभिन्न श्रेणियों का विकास होता है, जिनकी सामाजिक स्वीकृति होती है और जो अपेक्षाकृत स्थिर होती हैं। यह ऐसी प्रक्रिया है जो समाज में निरंतर गति से चलती रहती है। जैसे-जैसे व्यक्ति के कार्य एवं क्षमताएँ बदलती और विकसित होती हैं, वे समान रूपों में स्तरीकृत हो जाते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के कारण दो भिन्न वर्गों में भेद होता है, परंतु एक वर्ग के लोगों में एक सामूहिक चेतना पाई जाती है, जिसे वर्ग चेतना कहते हैं। इसमें समाज का विभिन्न इकाइयों में विभाजन इसलिये होता है ताकि सभी इकाइयों को उच्च और निम्न स्थान दिया जा सके। यानी सामाजिक स्तरीकरण में कहीं भी कोई खुला या बंद वर्ग नहीं होता है। यानी लोगों का आवागमन उच्च से निम्न स्तर में या निम्न स्तर से उच्च स्तर में हो सकता है। भारत में इस स्तरीकरण को लेकर विशेष परिस्थिति है। इसका कारण यहाँ जाति व्यवस्था का होना है। जाति व्यवस्था वास्तव में एक प्रकार की पदानुक्रमिक व्यवस्था ही है, लेकिन इसे विशेष इसलिये माना जाता है क्योंकि जाति एक बंद वर्ग के रूप में कार्य करती है। यानी जाति परिवर्तित नहीं होती, बदली नहीं जा सकती। यह जन्म आधारित होती है इसलिये जिस जाति में जन्म होता है आजीवन उसी जाति का सदस्य व्यक्ति बना रहता है। कुछ विचारकों के अनुसार जाति न तो पूरी तरह से बंद वर्ग है और न ही खुली श्रेणी है। कुछ विशेष परिस्थितियों में जाति की स्थिति पदानुक्रम में आगे पीछे भी हो जाती है।
सामाजिक विभेदीकरण और पदानुक्रम के बीच मुख्य भेद उनके उद्देश्य तथा प्रभाव का होता है। विभेदीकरण समाज में विविधता तथा कार्यात्मक विशेषीकरण को बढ़ावा देता है, जबकि पदानुक्रम असमानता तथा शक्ति के असंतुलन को रेखांकित करता है। उदाहरण के लिये एक अस्पताल में चिकित्सक, लेखाकार, दवा विक्रेता और नर्स के बीच विभेदीकरण कार्यात्मक है, क्योंकि चारों की भूमिकाएँ अलग हैं, लेकिन यदि चिकित्सक को शेष से अधिक शक्ति और संसाधन दिये जाएँ, फिर नर्स को, उसके बाद लेखाकार को तथा अंत में दवा विक्रेता को तो यह एक पदानुक्रम का रूप ले लेता है जिसके शीर्ष पर चिकित्सक सर्वाधिक शक्ति युक्त और अंत में सबसे कम शक्तिमान दवा विक्रेता है। इस तरह से विभेदीकरण, पदानुक्रम में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि सामाजिक विभेदीकरण समाज को संगठित और कार्यात्मक बनाता है, लेकिन जब यह पदानुक्रम में बदल जाता है, तो यह सामाजिक तनाव तथा असमानता को भी जन्म दे सकता है। उदाहरण के लिये कुछ विचारक मानते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था शुरू में व्यावसायिक विभेदीकरण पर आधारित थी, लेकिन समय के साथ यह कठोर पदानुक्रम में बदल गई, जिसने सामाजिक असमानता को बढ़ावा दिया। इस तरह से विभेदीकरण समाज में विविधता और कार्यक्षमता को बढ़ावा देता है, जबकि पदानुक्रम असमानता तथा शक्ति के वितरण को दर्शाता है। एक समतामूलक समाज के लिये यह आवश्यक है कि विभेदीकरण को कार्यात्मक बनाए रखा जाए और पदानुक्रम से उत्पन्न होने वाली असमानताओं को कम किया जाए।
समकालीन भारत में सामाजिक विभेदीकरण और पदानुक्रम को समझने हेतु कई सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य दिये गए हैं। संरचनात्मक-कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार, सामाजिक विभेदीकरण समाज को कार्यात्मक रूप से संगठित करता है। विभिन्न सामाजिक भूमिकाएँ और व्यवसाय समाज की स्थिरता तथा प्रगति हेतु आवश्यक हैं। हालाँकि यह परिप्रेक्ष्य पदानुक्रम से उत्पन्न होने वाली असमानताओं को कम आँकता है। उदाहरण के लिये जाति व्यवस्था को कभी कार्यात्मक माना गया था, लेकिन इसने सामाजिक अन्याय को जन्म दिया। संघर्ष सिद्धांत का परिप्रेक्ष्य पदानुक्रम को शक्ति और संसाधनों के असमान वितरण का परिणाम मानता है। भारत में, वर्ग और जाति आधारित संघर्ष इस परिप्रेक्ष्य को सही ठहराते हैं। उदाहरण के लिये भूमि सुधार तथा आरक्षण नीतियों के खिलाफ उच्च वर्गों एवं जातियों का विरोध शक्ति के लिये संघर्ष को दर्शाता है। नवनारीवादी परिप्रेक्ष्य लैंगिक पदानुक्रम पर ध्यान केंद्रित करता है और पितृसत्तात्मक संरचनाओं को चुनौती देता है। भारत में #मी-टू आंदोलन और लैंगिक समानता के लिये विधिक सुधार इस परिप्रेक्ष्य को मज़बूत करते हैं। कम चर्चित किंतु महत्त्वपूर्ण उत्तर-आधुनिक परिप्रेक्ष्य सामाजिक विभेदीकरण को पहचान और जीवनशैली के आधार पर देखता है। समकालीन भारत में, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने नई सामाजिक पहचानों को जन्म दिया है, जैसे कि इन्फ्लुएंसर एवं डिजिटल नोमैड्स। यह परिप्रेक्ष्य पारंपरिक पदानुक्रम को कम महत्त्व देता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है।
आधुनिक भारत में सामाजिक विभेदीकरण एवं पदानुक्रम, ये दोनों अवधारणाएँ आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव के संदर्भ में तेज़ी से परिवर्तित हो रही हैं। इन परिवर्तनों में आर्थिक, शैक्षिक, तकनीक कारकों की पर्याप्त भूमिका है। सामाजिक विभेदीकरण भारत में ऐतिहासिक रूप से जाति, धर्म तथा व्यवसाय जैसे कारकों पर आधारित रहा है। समकालीन भारत में यह प्रक्रिया और अधिक जटिल हो गई है, क्योंकि वैश्वीकरण, नगरीकरण एवं तकनीकी प्रगति ने नए सामाजिक समूहों, अस्मिताओं व पहचानों को जन्म दिया है। भारत की क्षेत्रीय और भाषायी विविधता सामाजिक विभेदीकरण का एक प्रमुख कारक है। विभिन्न राज्यों तथा क्षेत्रों में सांस्कृतिक प्रथाएँ, भाषाएँ और परंपराएँ सामाजिक समूहों को अलग करती हैं।
भारत की अर्थव्यवस्था में तेज़ी से आए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप नए व्यवसाय और कार्यक्षेत्र विकसित हुए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और सेवा क्षेत्र के विस्तार ने पारंपरिक व्यवसायों के साथ-साथ नए सामाजिक समूहों को जन्म दिया है। उदाहरण के लिये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डिजिटल मार्केटर, यूटयूबर, सोशल मीडिया हैंडलर, फाइनेंस एडवाइजर तथा फ्रीलांसर जैसे कार्यक्षेत्र आज नई सामाजिक पहचानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह विभेदीकरण समाज को कार्यात्मक रूप से संगठित करता है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। नगरीकरण ने इस सामाजिक विभेदीकरण को और बढ़ाया है। नगरों में लोग न केवल व्यवसाय, बल्कि जीवनशैली, सांस्कृतिक प्राथमिकताओं और सामाजिक संजाल के आधार पर अलग-अलग समूहों में बँटे हुए हैं। नगरीकरण के कारण मध्यम वर्ग का उदय हुआ और इसने उपभोक्तावाद के नए सामाजिक स्तरों को जन्म दिया है। शैक्षिक प्रसार और समानता के प्रत्यय की बढ़ती समझ के कारण समाज में लिंग आधारित भूमिकाएँ भी बदल रही हैं। महिलाओं की शिक्षा तथा कार्यबल में बढ़ती भागीदारी ने लैंगिक विभेदीकरण को नया आयाम दिया है। साथ ही, एलजीबीटी समुदाय की बढ़ती स्वीकार्यता ने पहचान आधारित विभेदीकरण को और जटिल बनाया है। ये परिवर्तन सामाजिक विभेदीकरण को बढ़ा रहे हैं।
भारत में पदानुक्रम ऐतिहासिक रूप से जाति, वर्ग और लिंग जैसे कारकों पर आधारित रहा है। समकालीन भारत में, ये पारंपरिक पदानुक्रम बदल रहे हैं, लेकिन नई असमानताएँ भी उभर रही हैं। जाति व्यवस्था भारत में पदानुक्रम का सबसे प्रमुख उदाहरण रही है। हालाँकि संवैधानिक प्रावधानों और सामाजिक सुधारों ने जातिगत भेदभाव को कम करने की कोशिश की है, फिर भी यह ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रभावी है। आरक्षण नीतियों ने दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को सामाजिक गतिशीलता के अवसर प्रदान किये हैं, लेकिन उच्च जातियों के बीच विशेषाधिकार तथा निम्न जातियों के बीच वंचन की स्थिति बनी हुई है। उदाहरण के लिये उच्च शिक्षा और नौकरियों में अभी भी कुछ समूहों का प्रभुत्व है। वहीं आर्थिक स्तर पर उदारीकरण के बाद धन तथा संसाधनों का असमान वितरण बढ़ा है। एक ओर, अरबपतियों और उच्च मध्यम वर्ग की संख्या बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर, गरीबी और बेरोज़गारी की समस्या बनी हुई है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 1% सबसे अमीर लोग देश की 50% से अधिक संपत्ति नियंत्रित करते हैं। यह आर्थिक पदानुक्रम सामाजिक तनाव को बढ़ाता है और अवसरों तक पहुँच को सीमित करता है। एक तीसरा एवं महत्त्वपूर्ण लैंगिक पदानुक्रम भारत में गहरे रूप से अभी भी समाया हुआ है। महिलाओं को शिक्षा और रोज़गार में अवसर मिल रहे हैं, लेकिन पितृसत्तात्मक संरचनाएँ अभी भी प्रभावी हैं। कार्यस्थल पर लैंगिक वेतन अंतर और यौन उत्पीड़न की घटनाएँ सामाजिक असमानता को दर्शाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं की स्थिति और भी कमज़ोर है, जहाँ शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुँच सीमित है। डिजिटल युग ने एक नए पदानुक्रम को जन्म दिया है। इंटरनेट और स्मार्टफोन तक पहुँच ने कुछ वर्गों को सूचना तथा अवसरों तक बेहतर पहुँच प्रदान की है, जबकि ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर समुदाय डिजिटल अंतर के कारण पिछड़ गए हैं। यह डिजिटल असमानता शिक्षा, रोज़गार एवं सामाजिक सहभागिता के क्षेत्रों में नए प्रकार की विषमताएँ उत्पन्न कर रही है।
समकालीन भारत में सामाजिक विभेदीकरण और पदानुक्रम से संबंधित कई चुनौतियाँ हैं। जिनके हल के लिये हमें प्रयास करने होंगे। सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के लिये शिक्षा और रोज़गार के अवसरों का समान तथा संतुलित वितरण आवश्यक है। जाति एवं लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिये सामाजिक सुधार और जागरूकता अभियान महत्त्वपूर्ण हैं। डिजिटल असमानता को कम करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी पहुँच बढ़ानी होगी। भविष्य में, भारत को एक ऐसी सामाजिक संरचना की दिशा में अग्रसर होना चाहिये जो विभेदीकरण को उपयोगी बनाए रखते हुए, पदानुक्रम से उत्पन्न होने वाली असमानताओं को प्रभावी रूप से कम कर सके। शिक्षा, समावेशी नीतियाँ और सामाजिक संवाद इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। विभिन्न सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य इन प्रवृत्तियों को समझने में मदद करते हैं, लेकिन एक समतामूलक समाज हेतु सामाजिक सुधार और नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हैं। भारत की सामाजिक संरचना को समावेशी और न्यायपूर्ण बनाने के लिये विभेदीकरण तथा पदानुक्रम के बीच संतुलन बनाना होगा।




