राजस्थान Switch to English
राजस्थान में स्थायी लोक अदालतों का अक्रियाशील होना
चर्चा में क्यों?
राजस्थान सरकार द्वारा पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने में विलंब के कारण राज्य के 16 ज़िलों में स्थायी लोक अदालतें (PLAs) स्थगित कर दी गई हैं, जिससे हज़ारों लंबित मामलों के समाधान में विलंब हो रहा है।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 3 मई 2025 को स्पष्ट किया था कि जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, वे विवाद समाधान में भाग नहीं ले सकेंगे।
नोट: अकेले जोधपुर में 972 से अधिक मामले लंबित हैं, जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय ने अनुसार ज़िलों में कुल लंबित मामलों की संख्या 10,000 से अधिक हो सकती है।
मुख्य बिंदु
न्यायिक प्रतिक्रिया
- राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और न्याय तक पहुँच तथा निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार (अनुच्छेद 21) पर इसके गंभीर प्रभाव पर चिंता व्यक्त की।
- उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ (2012) में सर्वोच्च न्यायालय केनिर्णय का हवाला दिया, जो मनमाना या दुर्भावनापूर्ण पाए जाने पर नीतिगत निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की अनुमति देता है।
- मामले की कार्यवाही में सहायता के लिये उच्च न्यायालय ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायमित्र नियुक्त किया है।
- एमिकस क्यूरी (शाब्दिक अर्थ, "न्यायालय का मित्र" ) वह व्यक्ति होता है, जो किसी मामले में पक्षकार नहीं होता है और उसे किसी पक्षकार द्वारा निवेदन किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। इसका कार्य न्यायालय को सूचना, विशेषज्ञता या किसी मुद्दे पर महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान कर सहायता करना होता है।
स्थायी लोक अदालतें (PLAs)
- परिचय:
- PLAs विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-B के तहत कार्य करती हैं।
- यह एक वैधानिक निकाय है, जिसे मुख्यतः पूर्व-विवाद सुलह और समझौते को सुनिश्चित करने के लिये स्थापित किया गया है, विशेष रूप से उन मामलों में जो लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित हों।
- PLAs पक्षकारों को मुकदमा दायर करने से पहले सुलह का प्रयास करने हेतु एक अनिवार्य मंच प्रदान करता है।
- हालाँकि, लोक अदालतों को लंबित मामलों के साथ-साथ मुकदमा-पूर्व मामलों पर भी क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
- PLAs आपराधिक अपराधों से संबंधित मामलों का निर्णय नहीं कर सकते।
- संघटन:
- प्रत्येक स्थायी लोक अदालत में शामिल होते हैं:
- एक अध्यक्ष (आमतौर पर सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी) और
- सार्वजनिक सेवा या कानून में अनुभव वाले दो अन्य सदस्य।
- प्रत्येक स्थायी लोक अदालत में शामिल होते हैं:
- बाध्यकारी प्रकृति:
- स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है।
- यदि दोनों पक्ष आपसी समझौते पर पहुँचने में असफल रहते हैं, तो PLAs को मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार है।
- इस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, जिससे त्वरित एवं निर्णायक समाधान सुनिश्चित होता है।
PLAs के गैर-कार्यशील होने के निहितार्थ
- न्याय तक पहुँच: लोक अदालतें वहनीय और त्वरित न्याय के लिये एक महत्त्वपूर्ण तंत्र हैं, विशेष रूप से कमज़ोर वर्गों के लिये।
- लंबित मामले: इस स्थगन से वर्तमान लंबित मामलों में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे विवाद समाधान और भी अधिक विलंबित हो जाएगा।
- वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) ढाँचे में व्यवधान : इस स्थगन वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को कमज़ोर करता है, जिससे अधिक मामले नियमित अदालतों में वापस चले जाते हैं।
- वादियों की अनिश्चितता: अधिकारियों के कार्यकाल समाप्त होने के कारण लंबित निर्णयों के कारण वादी को लंबे समय तक अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, जिससे कानूनी प्रणाली में विश्वास कम होता है।
लोक अदालत
- लोक अदालत या जन अदालत: न्यायालय में लंबित या मुकदमे-पूर्व विवादों को समझौते या सौहार्दपूर्ण समाधान के माध्यम से निपटान हेतु एक वैकल्पिक मंच है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा है कि लोक अदालत न्यायनिर्णयन की एक प्राचीन भारतीय प्रणाली है जो आज भी प्रासंगिक है और गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है।
- यह वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR ) प्रणाली का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लंभित मामले के संदर्भ में भारतीय न्यायालयों को राहत प्रदान करना है।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य नियमित न्यायालयों में होने वाली लंबी और महँगी प्रक्रियाओं के बिना त्वरित न्याय प्रदान करना है।
- लोक अदालत में किसी की हार या जीत नहीं होती है, इसमें विवाद समाधान हेतु एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाता है।
- कानूनी ढाँचा: प्रारंभ में कानूनी प्राधिकार के बिना एक स्वैच्छिक संस्था के रूप में कार्य करते हुए, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 द्वारा लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
- इस अधिनियम द्वारा संस्था को न्यायालय के आदेश के समान प्रभाव वाले अधिकार प्रदान किये गए।


बिहार Switch to English
अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक 2025
चर्चा में क्यों?
बिहार सरकार ने पटना में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक (IBSM) 2025 में अपनी कृषि-खाद्य क्षमता पर प्रकाश डाला। यह कार्यक्रम राज्य सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) और भारतीय व्यापार संवर्द्धन परिषद (TPCI) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।
मुख्य बिंदु
- बैठक का महत्त्व:
- अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक 2025 भारत के कृषि-निर्यात में राज्य की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच है, जिसमें साझेदारी को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिये बिजनेस-टू-बिजनेस बैठकें, तकनीकी सत्र और प्रदर्शनियाँ शामिल हैं।
- इस बैठक में संयुक्त अरब अमीरात, जापान और जर्मनी सहित वैश्विक कंपनियों ने रुचि दिखाई तथा बिहार के चावल, मसालों, मखाना और फलों की बड़े पैमाने पर खरीद की मांग की।
- इस आयोजन का उद्देश्य नए बाज़ार संबंध बनाना, स्थानीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के लिये खरीद बढ़ाना और बिहार की कृषि क्षमता को निर्यात वृद्धि में बदलना है।
- इस आयोजन को ग्रामीण आर्थिक विकास के लिये एक मील का पत्थर माना जाता है और यह सरकार के 'विकसित भारत @2047' के दृष्टिकोण की पुष्टि करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक 2025 भारत के कृषि-निर्यात में राज्य की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच है, जिसमें साझेदारी को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिये बिजनेस-टू-बिजनेस बैठकें, तकनीकी सत्र और प्रदर्शनियाँ शामिल हैं।
- PMFME योजना और भविष्य की संभावनाएँ:
- वित्त वर्ष 2024-25 में, पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PMFME) के तहत 624.42 करोड़ रुपए के 10,270 ऋण स्वीकृत किये गए- जो भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है।
- बिहार में स्थापित होने वाला NIFTEM (राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान) संस्थान, खाद्य प्रौद्योगिकी में नवाचार का भावी केंद्र होगा।
- मखाना निर्यात पर ध्यान:
- इस कार्यक्रम में “भारत के मखाना निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीतियाँ” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बिहार के अपने अद्वितीय जीआई-टैग उत्पाद में नेतृत्व को रेखांकित किया गया।
- वर्ष 2024 तक बिहार में 15 उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ। इनमें शाही लीची, भागलपुरी जरदालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, मखाना (फॉक्स नट), मधुबनी पेंटिंग, सिक्की घास उत्पाद और सुजिनी कढ़ाई आदि शामिल हैं।
- इस कार्यक्रम में “भारत के मखाना निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीतियाँ” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बिहार के अपने अद्वितीय जीआई-टैग उत्पाद में नेतृत्व को रेखांकित किया गया।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PMFME)
- परिचय:
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत PMFME योजना शुरू की है।
- इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा निजी सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देना है।
- यह योजना 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिये लागू है।
- केंद्रित क्षेत्र:
- यह योजना कच्चे माल की खरीद, सामान्य सेवाओं और उत्पादों के विपणन के संबंध में व्यापकता का लाभ उठाने के लिये एक ज़िला एक उत्पाद (One District One Product- ODOP) दृष्टिकोण अपनाती है।
- अन्य फोकस क्षेत्रों में वेस्ट टू वेल्थ उत्पाद, लघु वन उत्पाद और आकांक्षी ज़िले शामिल हैं।
- यह योजना कच्चे माल की खरीद, सामान्य सेवाओं और उत्पादों के विपणन के संबंध में व्यापकता का लाभ उठाने के लिये एक ज़िला एक उत्पाद (One District One Product- ODOP) दृष्टिकोण अपनाती है।
- मखाना
- मिथिला मखाना या माखन (वानस्पतिक नाम: यूरीले फेरोक्स सालिस्ब.) बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में उगाई जाने वाली जलीय मखाना की एक विशेष किस्म है।
- मखाना, पान और मछली के साथ मिथिला की तीन प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचानों में से एक है।
- मिथिला मखाना को वर्ष 2022 में भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त हुआ, जिसमें बिहार भारत के कुल मखाना उत्पादन में 80% का योगदान देता है।
- मखाना में प्रोटीन और फाइबर के साथ-साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस जैसे सूक्ष्म पोषक तत्त्व भी होते हैं।
- मई 2023 में, केंद्र सरकार ने मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा को "राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा" में अपग्रेड किया और मछली जैसी अन्य जलीय फसलों को शामिल करने के लिये इसके कार्य-क्षेत्र का विस्तार किया।
- केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित, बिहार में प्रस्तावित मखाना बोर्ड का उद्देश्य खेती के तरीकों को सुव्यवस्थित करना, तकनीकी सहायता प्रदान करना, मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना, विपणन बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना एवं निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना है।
- मिथिला मखाना या माखन (वानस्पतिक नाम: यूरीले फेरोक्स सालिस्ब.) बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में उगाई जाने वाली जलीय मखाना की एक विशेष किस्म है।


उत्तर प्रदेश Switch to English
भारत के 86 वें ग्रैंडमास्टर
चर्चा में क्यों?
तमिलनाडु के श्रीहरि LR संयुक्त अरब अमीरात के अल ऐन में एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 में भारत के 86वें ग्रैंडमास्टर (GM) बने।
मुख्य बिंदु
- श्रीहरि LR के बारे में:
- श्रीहरि ने अपना पहला GM नॉर्म वर्ष 2023 में कतर मास्टर्स में और दूसरा वर्ष 2024 में चेन्नई GM ओपन में अर्जित किया।
- उन्होंने अगस्त 2024 में 2500 एलो रेटिंग पार कर ली, लेकिन अंतिम मानदंड प्राप्त करने में उन्हें लगभग 10 महीने लग गए।
- एलो रेटिंग प्रणाली कुछ खेलों, जैसे शतरंज, में अन्य खिलाड़ियों की तुलना में किसी खिलाड़ी की सापेक्षिक शक्ति को मापती है।
- भारत के ग्रैंडमास्टर्स:
- पहले भारतीय ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद थे, जिन्होंने वर्ष 1988 में यह खिताब जीता था।
- पहली भारतीय महिला ग्रैंडमास्टर कोनेरू हंपी थीं, जिन्होंने वर्ष 2002 में 15 वर्ष की आयु में यह खिताब जीता था। उस समय वह दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंडमास्टर बनी थीं।
- वर्तमान में भारत में तीन महिला ग्रैंडमास्टर हैं: कोनेरू हंपी, द्रोणावल्ली हरिका और आर. वैशाली।
- प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर मैनुअल एरॉन वर्ष 1961 में बने थे तथा अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जयश्री खादिकर वर्ष 1979 में बनी थीं।
अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE)
- परिचय:
- FIDE शतरंज के खेल के लिये एक वैश्विक नियामक संस्था है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1924 में पेरिस, फ्राँस में हुई थी।
- इसका मुख्यालय लॉज़ेन, स्विटज़रलैंड में है।
- यह सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं की देखरेख और उनको विनियमित करता है।
- एक गैर-सरकारी संस्था के रूप में स्थापित, FIDE को वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा आधिकारिक तौर पर वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी।
- FIDE का आदर्श वाक्य:
- "जेन्स ऊना सुमस"- लैटिन में इसका अर्थ है "हम एक परिवार हैं ", जो वैश्विक शतरंज समुदाय में एकता पर ज़ोर देता है।
- FIDE की मुख्य गतिविधियाँ:
- शीर्ष 10 समग्र खिलाड़ियों और शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की औसत रेटिंग के आधार पर देश की रैंकिंग जारी करता है।
- सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंटों के नियमों, मानदंडों और आचरण को नियंत्रित करता है।
- यह विश्व के राष्ट्रीय शतरंज महासंघों को जोड़ने वाले एक केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करता है।

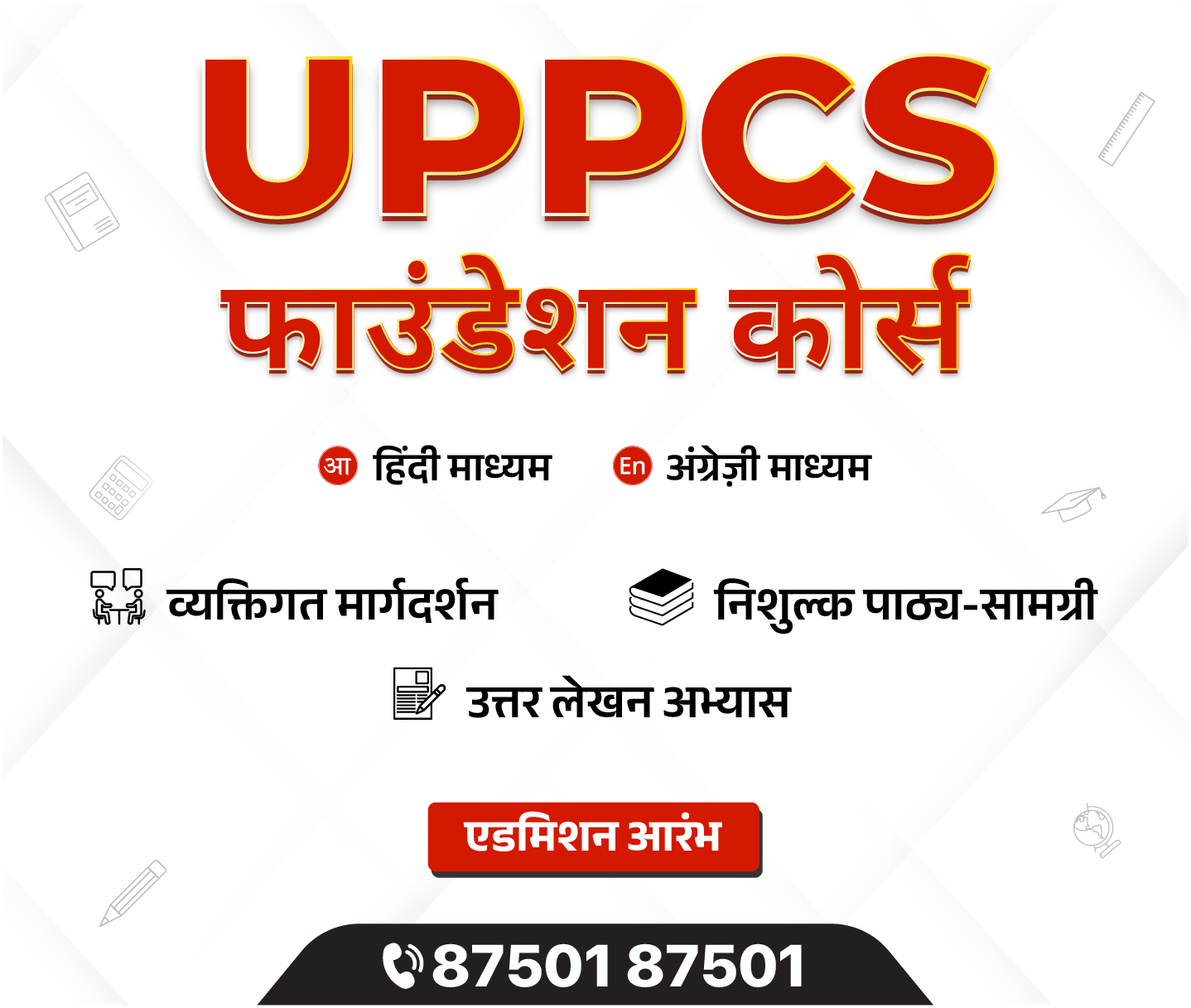
राजस्थान Switch to English
कोटा में प्रधानमंत्री दिव्यशा केंद्र (PMDK)
चर्चा में क्यों?
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिये कोटा, राजस्थान में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र (PMDK) का उद्घाटन किया और उन्हें सहायक उपकरण वितरित किये।
मुख्य बिंदु
- PMDK पहल के बारे में:
- PMDK पहल का नेतृत्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO) द्वारा किया जाता है।
- इसका प्राथमिक लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को उच्च गुणवत्ता वाले, वहनीय सहायक उपकरण उपलब्ध कराना है।
- वर्तमान में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 45 PMDK केंद्र कार्यरत हैं।
- सरकार का लक्ष्य जून 2025 तक इस नेटवर्क को 100 केंद्रों तक विस्तारित करना है।
- लक्ष्य:
- नवनिर्मित PMDK में दृष्टिबाधित व्यक्तियों पर विशेष ज़ोर दिया गया है।
- यह सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:
- प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स
- ब्रेल उपकरण
- गतिशीलता सहायता
- उन्नत पुनर्वास प्रौद्योगिकियाँ
- कौशल विकास और सशक्तीकरण:
- इसका उद्देश्य लाभार्थियों में कौशल निर्माण के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना है।
- इन कार्यक्रमों का उद्देश्य रोज़गार और उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाना है।
दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिये पहल


उत्तर प्रदेश Switch to English
शाही जामा मस्जिद विवाद एवं पूजा स्थल अधिनियम 1991
चर्चा में क्यों?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिये एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा।
मुख्य बिंदु
शाही जामा मस्जिद विवाद
- पृष्ठभूमि: यह मामला स्थानीय निवासियों द्वारा संभल अदालत में दायर याचिका से उत्पन्न हुआ, जिसमें दावा किया गया कि यह स्थल मूलतः श्री हरिहर मंदिर था, जिसे कथित तौर पर मुगल सम्राट बाबर ने वर्ष 1529 में ध्वस्त कर दिया था।
- कानूनी स्थिति: शाही जामा मस्जिद प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत एक संरक्षित स्मारक है। इसे भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- शाही जामा मस्जिद और उपासना स्थल अधिनियम, 1991: उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 इस विवाद के केंद्र में है।
- अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि उपासना स्थलों का धार्मिक स्वरूप, जैसा कि वे 15 अगस्त 1947 को थे, संरक्षित किया जाना चाहिये तथा ऐसे स्थानों की धार्मिक पहचान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर रोक लगाई गई है।
- शाही जामा मस्जिद विवाद में मस्जिद के धार्मिक स्वरूप को परिवर्तित करने की मांग करके अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती दी गई है।
उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991
- परिचय: उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 का उद्देश्य उपासना स्थलों की धार्मिक स्थिति को संरक्षित रखना तथा विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच या एक ही संप्रदाय के भीतर धर्मांतरण को रोकना है।
- इस अधिनियम का उद्देश्य इन स्थानों के धार्मिक चरित्र को स्थिर रखते हुए तथा ऐसे धर्मांतरण से उत्पन्न विवादों को रोककर सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना है।
- अधिनियम के प्रमुख प्रावधान
- धारा 3: किसी भी उपासना स्थल को, पूर्णतः या आंशिक रूप से, एक धार्मिक संप्रदाय से दूसरे धार्मिक संप्रदाय में परिवर्तित करने पर रोक लगाती है।
- धारा 4(1): यह अनिवार्य करता है कि उपासना स्थल की धार्मिक पहचान 15 अगस्त 1947 की स्थिति से अपरिवर्तित रहनी चाहिये। धार्मिक चरित्र को बदलने का कोई भी प्रयास निषिद्ध है।
- धारा 4(2): यह विधेयक 15 अगस्त 1947 से पहले किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन से संबंधित सभी चल रही कानूनी कार्यवाहियों को समाप्त करता है तथा ऐसे स्थानों की धार्मिक स्थिति को चुनौती देने वाले नए मामलों को शुरू करने पर रोक लगाता है।
- धारा 5 (अपवाद): अयोध्या विवाद (बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि), जिसे अधिनियम से छूट दी गई।
- अयोध्या विवाद के अलावा, अधिनियम में निम्नलिखित को भी छूट दी गई है: कोई भी उपासना स्थल जो प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है, या प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत आने वाला कोई पुरातात्त्विक स्थल है।
- ऐसे मामले जो पहले ही आपसी समझौते से सुलझा लिये गए हों या निपटा दिये गए हों।
- अधिनियम के लागू होने से पहले हुए धर्मांतरण।
- धारा 6 (दंड): अधिनियम में उल्लंघन के लिये कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें तीन वर्ष तक का कारावास और उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने का प्रयास करने पर ज़ुर्माना शामिल है।
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI)
- ASI केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। यह देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्त्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिये प्रमुख संगठन है।
- यह प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्त्व स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 के तहत देश के भीतर सभी पुरातात्त्विक उपक्रमों की देख-रेख करता है।
- यह 3,650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्त्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्त्व के अवशेषों का प्रबंधन करता है।
- इसकी गतिविधियों में पुरातात्त्विक अवशेषों का सर्वेक्षण करना, पुरातात्त्विक स्थलों की खोज और उत्खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण तथा रखरखाव आदि शामिल हैं।
- इसकी स्थापना वर्ष 1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को “भारतीय पुरातत्त्व का जनक” भी कहा जाता है।

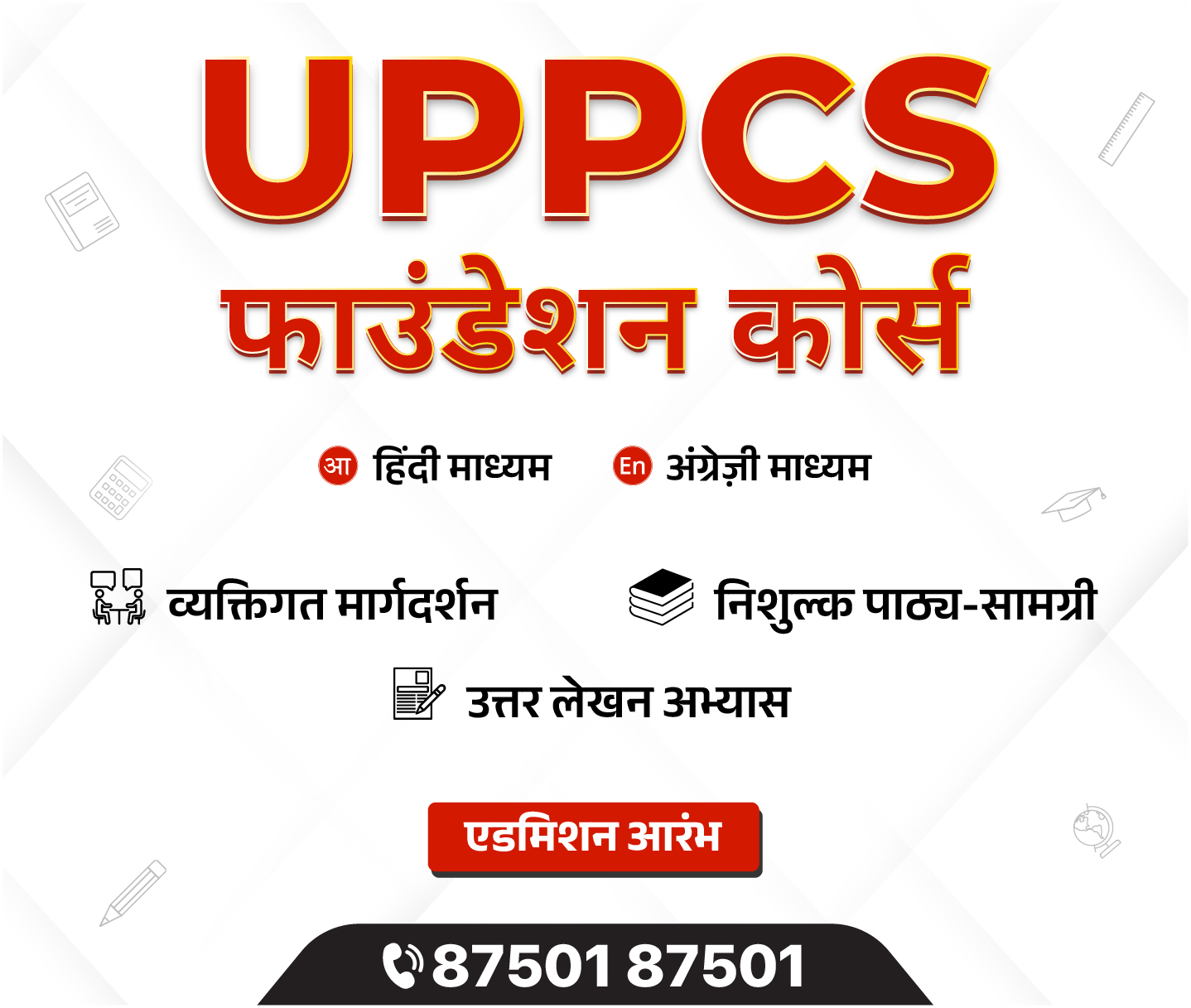

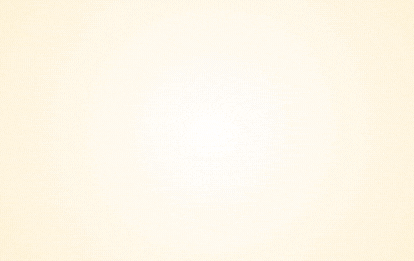



 PCS परीक्षण
PCS परीक्षण

