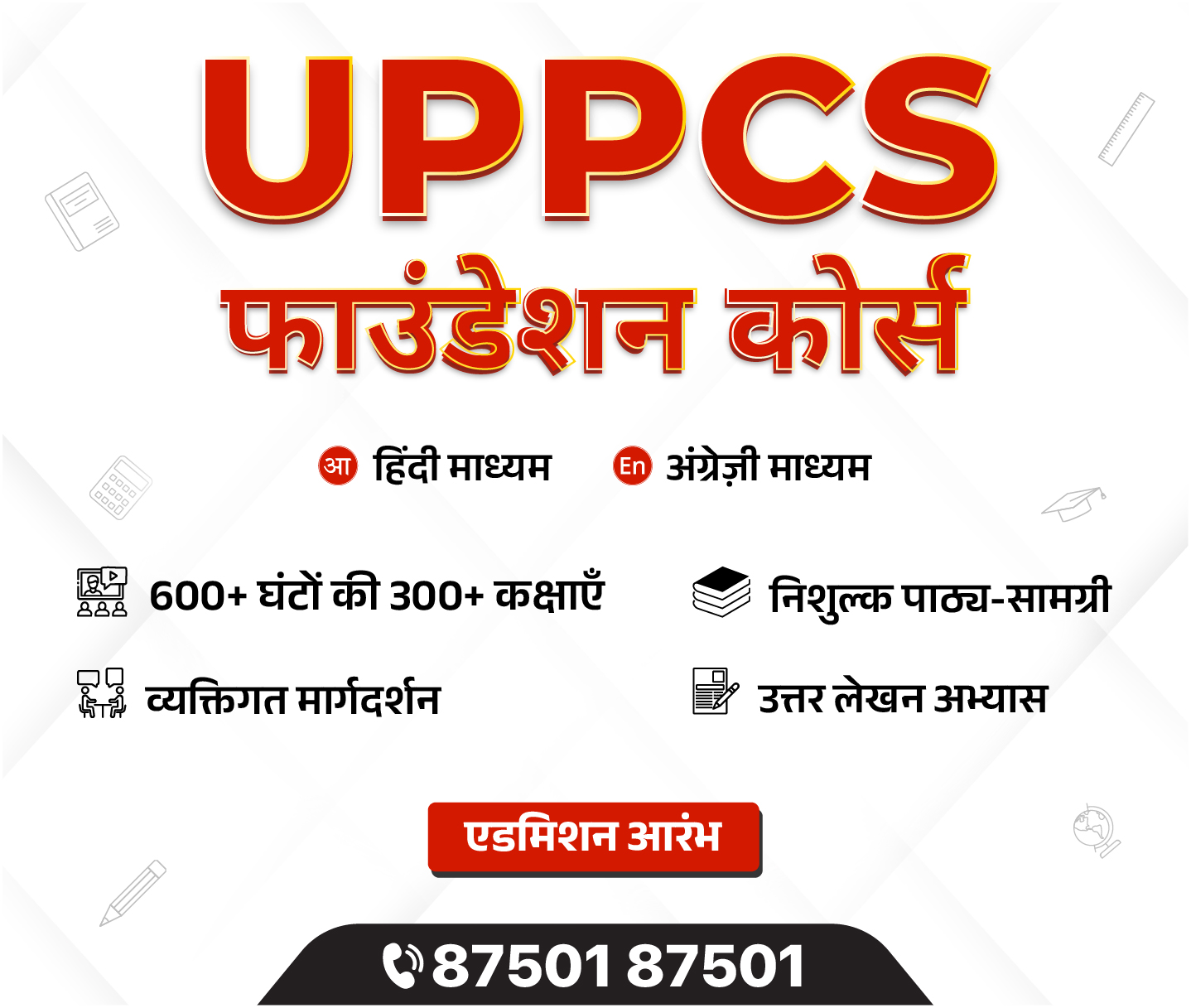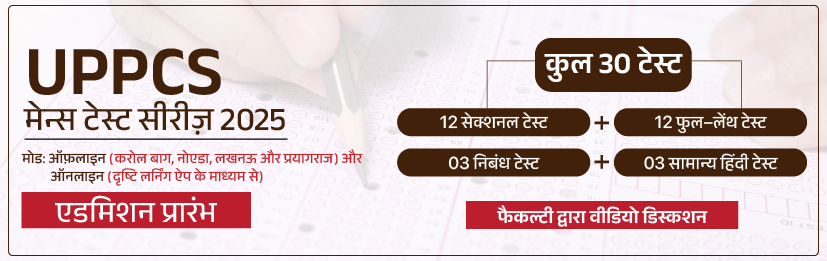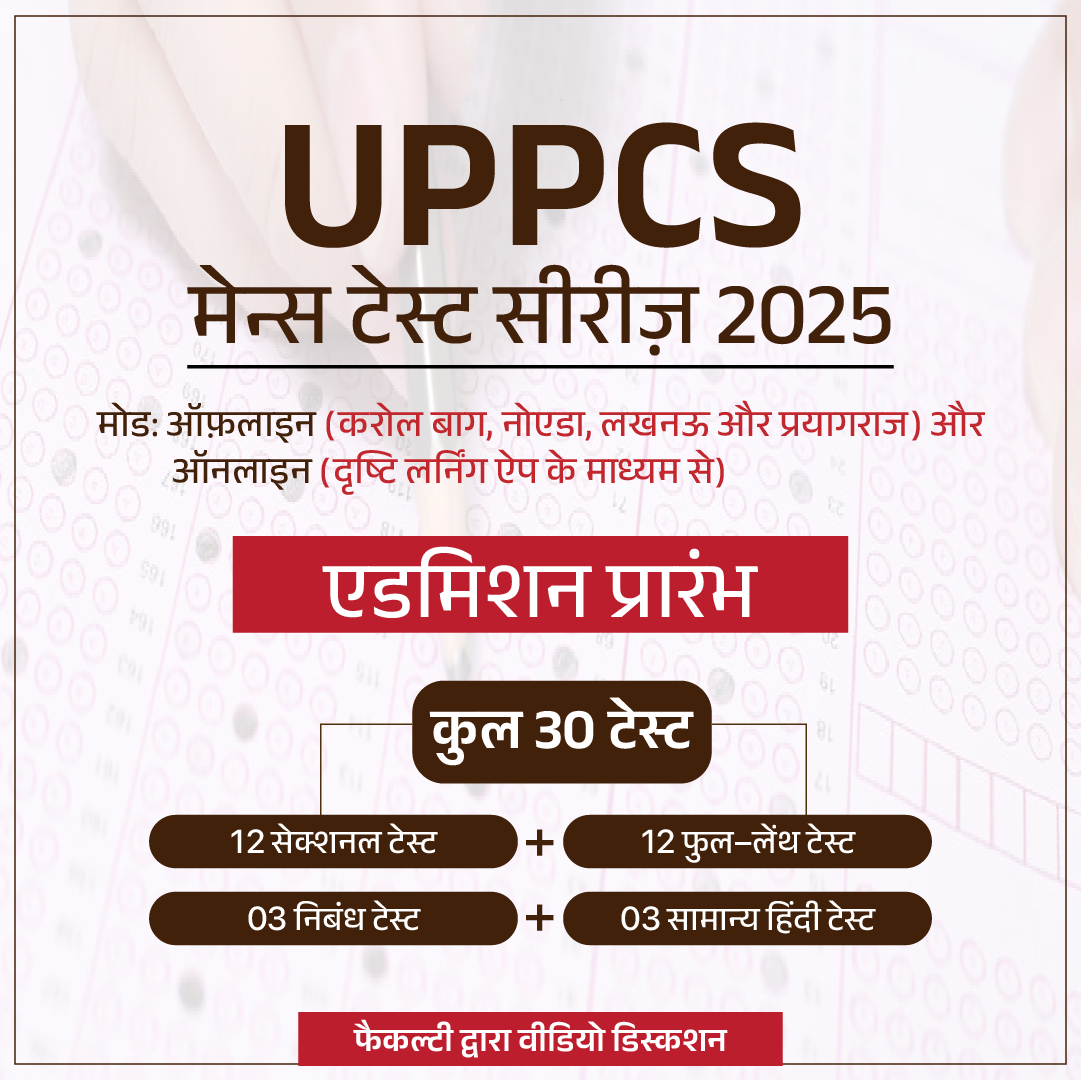राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स Switch to English
गुजरात ने ‘पोषण उड़ान 2026’ शुरू किया
चर्चा में क्यों?
गुजरात ने मकर संक्रांति उत्सव के दौरान ‘पोषण उड़ान 2026’ की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक उत्सवों और सामुदायिक सहभागिता का उपयोग करते हुए पूरे राज्य में पोषण तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है।
मुख्य बिंदु:
- पहल: ‘पोषण उड़ान 2026’ पूरे राज्य में जन-जागरूकता बढ़ाने के लिये पतंग उत्सव की लोकप्रियता का उपयोग करता है, जिसमें पोषण और स्वास्थ्य संदेशों वाली पतंगें उड़ाई जाती हैं।
- इसका उद्देश्य बच्चों, किशोरियों और माताओं के लिये संतुलित आहार तथा स्वास्थ्य के महत्त्व को रेखांकित करना है।
- एकीकरण: यह कार्यक्रम आँगनवाड़ी केंद्रों पर ICDS (एकीकृत बाल विकास सेवाओं) के अंतर्गत संचालित किया जाता है।
- कार्यान्वयन: यह राज्यव्यापी पोषण जागरूकता अभियान गुजरात के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है।
- फोकस: पहल का मुख्य ज़ोर आहार विविधता, जंक फूड के सेवन को घटाने, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता प्रथाओं पर है ताकि पोषण संबंधी परिणामों में सुधार हो सके।
- लक्षित समूह: जागरूकता अभियान में स्कूल के बच्चे, किशोरियाँ, गर्भवती और धात्री महिलाएँ तथा स्थानीय समुदाय के अभिकर्त्ता शामिल होते हैं।
- स्वास्थ्य हस्तक्षेप: माताओं और बच्चों के लिये हीमोग्लोबिन परीक्षण, आयरन एवं फोलिक एसिड (IFA) टैबलेट वितरण, BMI (शरीर द्रव्यमान सूचकांक) जाँच तथा व्यक्तिगत पोषण परामर्श जैसी गतिविधियाँ संचालित की गईं।
|
और पढ़ें: मकर संक्रांति उत्सव, पोषण अभियान, ICDS, BMI |

.png)

%20(1).gif)
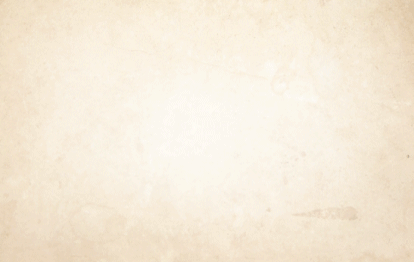
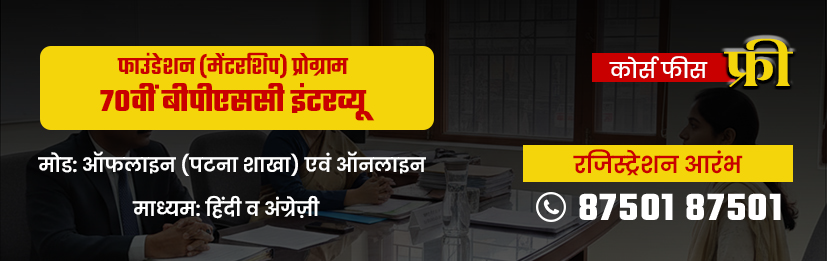
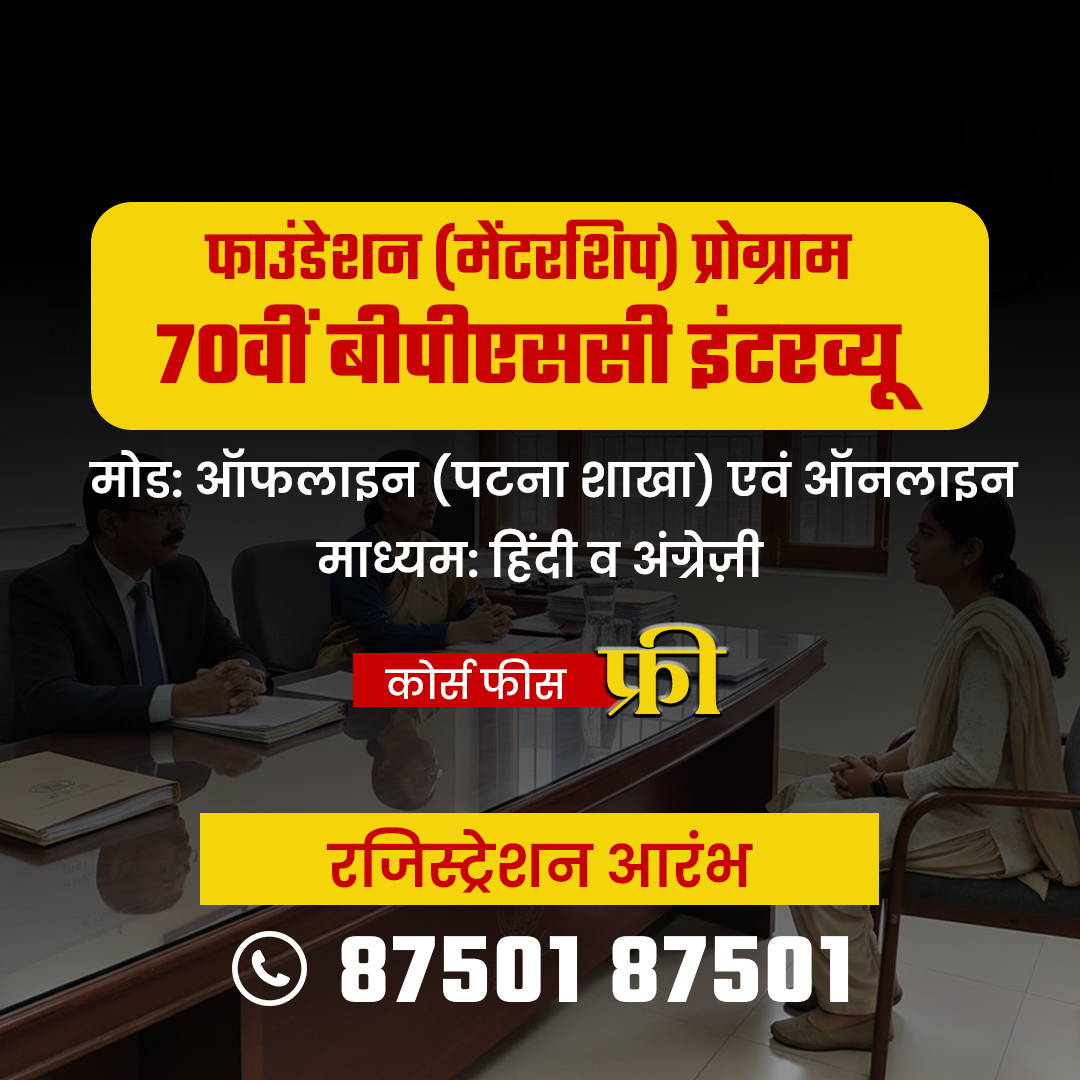
.jpg)