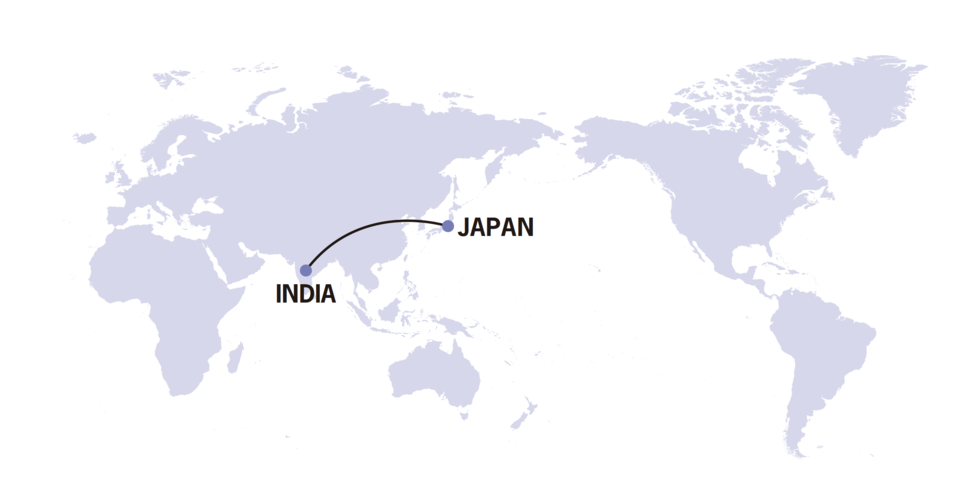अंतर्राष्ट्रीय संबंध
भारत-जापान अभिसरण: क्षेत्रीय शक्ति संतुलन
- 01 Sep 2025
- 132 min read
यह एडिटोरियल 01/09/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “Renewed focus: On India-Japan ties” पर आधारित है। यह लेख भारतीय प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में 68 अरब डॉलर के निवेश लक्ष्य तथा सेमीकंडक्टर, हरित प्रौद्योगिकी और आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर बल दिया गया है। यह साझेदारी क्षेत्रीय शक्ति-संघर्षों के बीच स्थिरता प्रदान करने वाली एक महत्त्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है।
प्रिलिम्स के लिये: भारत-जापान संबंध, मालाबार, धर्म गार्जियन, JIMEX, GIFT सिटी, चाइना प्लस वन रणनीति, शिंकानसेन तकनीक, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण (LUPEX) मिशन, US-2 एम्फिबियन एयरक्राफ्ट डील
मेन्स के लिये: भारत और जापान के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र, भारत और जापान के बीच मतभेद के प्रमुख क्षेत्र।
हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान आयोजित 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन ने यह दर्शाया कि वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच भारत-जापान रणनीतिक साझेदारी और गहरी हो रही है। इस दौरान दोनों देशों ने दर्जनभर से अधिक समझौते किये, जिनका ‘Next-Gen (अगली पीढ़ी)’ पर केंद्रित दृष्टिकोण था। इसमें भारत में 68 अरब डॉलर के जापानी निवेश का लक्ष्य, अर्द्धचालक (सेमीकंडक्टर), हरित प्रौद्योगिकी और आर्थिक सुरक्षा में सहयोग शामिल है। समग्र रूप से, यह शिखर सम्मेलन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि भारत-जापान संबंध महाशक्तियों (जैसे: अमेरिका, चीन, रूस) के बीच प्रतिस्पर्द्धा से प्रभावित अस्थिर क्षेत्रीय व्यवस्था में एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं।
भारत और जापान के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं?
- सामरिक और रक्षा सहयोग: भारत और जापान ने क्षेत्रीय अस्थिरता (विशेष रूप से चीन की हठधर्मिता और अमेरिकी नीति में अनिश्चितता के बीच) को संतुलित करने के लिये अपनी सामरिक साझेदारी को उन्नत किया है।
- नियमित सैन्य अभ्यास, खुफिया जानकारी साझाकरण और संस्थागत संवाद गहन रक्षा अभिसरण को दर्शाते हैं।
- भारत और जापान के बीच अगस्त वर्ष 2025 में 'सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा' पर हस्ताक्षर, वर्ष 2008 के समझौते से कहीं अधिक व्यापक और गहन स्तर का उन्नयन है।
- यह सुरक्षा सहयोग के लिये एक व्यापक कार्यढाँचा प्रदान करता है, जिसमें मालाबार, धर्म गार्जियन और JIMEX जैसे द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय अभ्यासों में वृद्धि शामिल है।
- इस समझौते में रक्षा उपकरणों के सह-विकास की भी संभावनाएँ हैं, जिसमें UNICORN (यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना) नौसैनिक मस्तूल जापान और भारत के बीच सह-विकास का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
- आर्थिक साझेदारी और निवेश: भारत और जापान अगली पीढ़ी के निवेश और लघु एवं मध्यम उद्यम (SME) सहयोग के माध्यम से आर्थिक एकीकरण को गहन कर रहे हैं।
- चाइना प्लस वन रणनीति के तहत, जापान भारत को एक विनिर्माण केंद्र और एक बढ़ते बाज़ार के रूप में देखता है।
- व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की समीक्षा और GIFT सिटी को बढ़ावा देने का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार एवं वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
- जापान ने वर्ष 2035 तक 68 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है, जो भारत के विकास में दीर्घकालिक विश्वास को दर्शाता है।
- आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य योजना आपूर्ति शृंखलाओं को सुदृढ़ करने तथा आर्थिक लचीलापन सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।
- ये सभी कदम भारत-जापान आर्थिक संबंधों में एक परिवर्तनकारी चरण का प्रतीक हैं।
- बुनियादी अवसंरचना और संपर्क: बुनियादी अवसंरचनाओं का विकास लंबे समय से सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है, जहाँ जापान भारत की प्रमुख परियोजनाओं को महत्त्वपूर्ण वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- यह सहयोग भारत की आर्थिक क्षमता और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- इसका एक प्रमुख उदाहरण मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना है, जिसमें जापान की ‘शिंकानसेन’ तकनीक का उपयोग किया गया है।
- हालाँकि प्रगति में विलंब हुआ है, फिर भी दोनों देशों ने अपनी साझेदारी के प्रतीक के रूप में इसके महत्त्व की पुष्टि की है और वर्ष 2030 के दशक की शुरुआत में शिंकानसेन की नवीनतम E10 शृंखला शुरू करने तथा इसके शीघ्रातिशीघ्र संचालन की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की है।
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पहल: दोनों देश हरित परिवर्तन के लिये प्रतिबद्ध हैं तथा अपने-अपने शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये स्वच्छ ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी विभिन्न पहलों पर सहयोग कर रहे हैं।
- यह साझेदारी जापान की तकनीकी क्षमता और भारत के बढ़ते स्वच्छ ऊर्जा बाज़ार का लाभ उठाती है।
- भारत-जापान स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत संयुक्त ऋण तंत्र इस क्षेत्र में प्रमुख साधन हैं।
- वर्ष 2030 तक भारत का 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का भारत का लक्ष्य सौर सेल तथा हरित हाइड्रोजन क्षेत्रों में जापानी निवेश एवं प्रौद्योगिकी के लिये अपार अवसर प्रदान करता है।
- नवाचार और मानव संसाधन विकास: भारत और जापान कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में अपनी साझेदारी का विस्तार कर रहे हैं, साथ ही भविष्योन्मुखी संबंधों को बढ़ावा देने के लिये लोगों के बीच आदान-प्रदान को भी बढ़ावा दे रहे हैं।
- यह सहयोग भारत के टैलेंट पूल और जापान की तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाता है।
- जापान-भारत AI सहयोग पहल (JAI) और चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण (LUPEX) मिशन इस गहन सहयोग के प्रमुख उदाहरण हैं।
- भारत-जापान मानव संसाधन आदान-प्रदान की नई कार्य योजना के तहत, दोनों देशों ने आगामी पाँच वर्षों में 500,000 से अधिक कर्मियों का आदान-प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें भारत से जापान में 50,000 कुशल श्रमिक शामिल हैं, ताकि जापान की जनांकिकीय चुनौतियों का समाधान किया जा सके और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।
- स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा: दोनों देश स्वास्थ्य सेवा नवाचार पर सहयोग कर रहे हैं, जो बढ़ती उम्र की आबादी और उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों पर केंद्रित है। यह साझेदारी चिकित्सा प्रौद्योगिकी और वृद्धावस्था देखभाल में जापान की विशेषज्ञता को भारत के बड़े पैमाने पर औषधि निर्माण एवं डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी अवसंरचना के साथ जोड़ने का प्रयास करती है।
- एक प्रमुख विकास वृद्धावस्था चिकित्सा और डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों पर संयुक्त अनुसंधान है।
- इसके अलावा, साझेदारी में अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग और विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल प्रबंधन पर एक समझौता ज्ञापन शामिल है, जो स्थायी सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी अवसंरचना का समर्थन करता है।
- सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध: भारत-जापान संबंधों को उनकी साझा बौद्ध विरासत से मज़बूती मिलती है, जो एक गहरे सभ्यतागत बंधन का निर्माण करती है।
- सांस्कृतिक कूटनीति दोनों देशों के बीच सद्भावना और विश्वास को मज़बूत करती रही है।
- भाषा शिक्षा, पर्यटन और शैक्षणिक आदान-प्रदान की पहल, धारणाओं को जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- इसका एक प्रतीकात्मक उदाहरण वर्ष 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री को भेंट की गई दारुमा गुड़िया है, जो सांस्कृतिक निरंतरता एवं समुत्थानशक्ति का प्रतीक है।
- जापान ने जापानी भाषा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये भारतीय संस्थानों में अपने ‘NIHONGO पार्टनर्स’ कार्यक्रम का भी विस्तार किया है।
भारत और जापान के बीच असहमति के प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं?
- निरंतर व्यापार असंतुलन: व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के बावजूद, भारत और जापान के बीच व्यापार की मात्रा अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है तथा जापान के पक्ष में एक महत्त्वपूर्ण एवं बढ़ता हुआ व्यापार असंतुलन है।
- यह असहमति का एक स्रोत है क्योंकि भारत अपने निर्यात बाज़ार का विस्तार करना चाहता है।
- वित्त वर्ष 2024 में, जापान का भारत को निर्यात 17.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि भारत का जापान को निर्यात 5.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो एक बहुत बड़े व्यापार असंतुलन को दर्शाता है।
- यह असंतुलन आंशिक रूप से जापान द्वारा सख्त गैर-टैरिफ अवरोधों और आयात मानकों (विशेष रूप से भारतीय कृषि एवं वस्त्र उत्पादों के लिये) के कारण है।
- इन अवरोधों को दूर करने में प्रगति की कमी ने भारतीय व्यवसायों को CEPA का पूर्ण उपयोग करने से अवरुद्ध कर दिया है।
- रुकी हुई बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएँ और रक्षा खरीद: द्विपक्षीय सहयोग की प्रतीक, प्रमुख मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) परियोजना को लंबे समय से विलंब और लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भारत में बड़े पैमाने पर जटिल परियोजनाओं के क्रियान्वयन की कठिनाइयाँ उजागर होती हैं।
- मूल रूप से वर्ष 2022 में पूरा होने वाली इस परियोजना के अब वर्ष 2028 तक चरणों में पूरा होने की उम्मीद है।
- मुख्य मुद्दे धीमी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया, विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में, और नियामक जटिलताएँ हैं।
- इसके अलावा, उदाहरण के लिये, प्रस्तावित US-2 एम्फिबियन एयरक्राफ्ट डील, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मूल्य निर्धारण विवादों के लिये एक स्पष्ट कार्यढाँचे के अभाव के कारण वर्षों से रुका हुआ है।
- मूल रूप से वर्ष 2022 में पूरा होने वाली इस परियोजना के अब वर्ष 2028 तक चरणों में पूरा होने की उम्मीद है।
- भिन्न रणनीतिक दर्शन: हालाँकि दोनों देश चीन के बारे में समान चिंताएँ रखते हैं, लेकिन उनके मूलभूत रणनीतिक दृष्टिकोण भिन्न हैं, जिससे एक सूक्ष्म, अंतर्निहित असहमति उत्पन्न होता है।
- जापान अमेरिका का एक औपचारिक सहयोगी है, जबकि भारत रणनीतिक स्वायत्तता की नीति का पालन करता है।
- रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के साथ जापान का तालमेल भारत की आर्थिक व्यावहारिकता के विपरीत है, जिससे व्यापक रणनीतिक मंचों पर नीतिगत असहमति उत्पन्न हो रहा है।
- इस तरह का विचलन समन्वित भू-राजनीतिक संदेश और ऊर्जा एकजुटता की कमज़ोरियों को उजागर करता है।
- तृतीय-पक्ष बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा: जैसे-जैसे दोनों देश हिंद-प्रशांत और अफ्रीका में अपनी आर्थिक उपस्थिति बढ़ा रहे हैं, वे प्रभाव और परियोजनाओं के लिये प्रतिस्पर्द्धा में हैं। यह विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ उनके जुड़ाव में स्पष्ट है।
- वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों में जापान की स्थापित उपस्थिति एवं गहरी वित्तीय प्रतिबद्धताएँ कभी-कभी भारत के अपने प्रभाव का निर्माण करने के प्रयासों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करती हैं।
- डिजिटल व्यापार और डेटा प्रशासन का बेमेल: डेटा स्थानीयकरण पर भारत का सुरक्षात्मक रुख कुछ हद तक वैश्विक डिजिटल व्यापार मानदंडों पर जापान के दबाव से अलग है।
- यह CEPA के तहत द्विपक्षीय डिजिटल अर्थव्यवस्था सहयोग और मानकों को संरेखित करने में असहमति उत्पन्न करता है।
- उदाहरण के लिये, वर्ष 2019 के G20 ओसाका शिखर सम्मेलन में, भारत ने जापान की ‘ओसाका ट्रैक’ पहल से बाहर निकलने का विकल्प चुना, जो ‘Data Free Flow with Trust (विश्वास के साथ डेटा मुक्त प्रवाह)’ का आह्वान करता है, जो डेटा गवर्नेंस पर तीव्र नियामक विचलन का संकेत देता है।
जापान के साथ अपने संबंधों को मज़बूत करने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?
- संतुलित विकास के लिये व्यापार ढाँचे का पुनर्निर्धारण: भारत को लक्षित मार्केट-एक्सेस प्रोटोकॉल के साथ, विशेष रूप से कृषि, दवा और वस्त्र निर्यात के लिये, CEPA 2.0 पर वार्ता करनी चाहिये।
- एक संयुक्त ‘गैर-टैरिफ बाधा समीक्षा समिति’ जापान के कड़े मानकों को कम करने के लिये वार्ता को संस्थागत रूप दे सकती है।
- भारत को मूल्य-संवर्द्धन क्षेत्रों में जापानी निवेश का भी लाभ उठाना चाहिये जो भारतीय निर्यात को जापानी आपूर्ति शृंखलाओं में एकीकृत करते हैं।
- व्यापार संवर्द्धन परिषदों को प्रसंस्कृत खाद्य, आयुर्वेद और नवीकरणीय तकनीक जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- यह संतुलित दृष्टिकोण आर्थिक पूरकता को सुदृढ़ करते हुए विषमता को कम करेगा।
- लचीली आपूर्ति शृंखलाओं का सह-निर्माण: भारत दुर्लभ मृदा प्रसंस्करण, अर्द्धचालक निर्माण और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिये संयुक्त केंद्र स्थापित करने के लिये जापान के साथ साझेदारी कर सकता है।
- जापानी फर्मों को भारतीय औद्योगिक गलियारों में शामिल करके, दोनों पक्ष विश्वसनीय, जोखिम-मुक्त आपूर्ति नेटवर्क बना सकते हैं।
- यह चीन पर अत्यधिक निर्भरता के प्रतिकार के रूप में काम करेगा तथा साथ ही भारतीय उद्योग को वैश्विक मूल्य शृंखला में एक भूमिका प्रदान करेगा।
- ‘विश्वसनीय आर्थिक गलियारे’ के तहत इन पहलों की सह-ब्रांडिंग रणनीतिक पूरकता को मज़बूत करेगी।
- ऐसे सहयोगी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र रोज़गार और नवाचार के तालमेल को भी बढ़ावा देंगे।
- समुद्री और हिंद-प्रशांत सहयोग को मज़बूत करना: भारत को जापान के साथ नौसैनिक अंतर-संचालन को अभ्यासों से आगे बढ़ाकर समन्वित गश्त, HADR मिशन और समुद्री क्षेत्र जागरूकता तक विस्तारित करना चाहिये।
- निगरानी में जापान की तकनीकी दक्षता और भारत के रणनीतिक भूगोल का लाभ उठाकर एक मज़बूत हिंद-प्रशांत सुरक्षा ढाँचा बनाया जा सकता है।
- ऐसा सहयोग ASEAN देशों को आश्वस्त करेगा और विवादित जलक्षेत्रों में चीनी आक्रामकता को संतुलित करेगा।
- यह एक व्यापक सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की स्थिति को मज़बूत करेगा, साथ ही जापान को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में मज़बूत करेगा।
- डिजिटल और फिनटेक एकीकरण को गहरा करना: भारत को जापान में अपने UPI मॉडल और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी अवसंरचना को अपनाने में तीव्रता लानी चाहिये, साथ ही अगली पीढ़ी के फिनटेक प्लेटफॉर्म का संयुक्त रूप से विकास करना चाहिये।
- साइबर सुरक्षा और हार्डवेयर में जापान की सटीकता के साथ भारत के डिजिटल पैमाने को जोड़कर, दोनों देश डिजिटल गवर्नेंस में वैश्विक मानकों का नेतृत्व कर सकते हैं।
- एक द्विपक्षीय डिजिटल साझेदारी चार्टर डेटा फ्लो, AI एथिक्स और फिनटेक विनियमों को समन्वित कर सकता है।
- यह साझेदारी को केवल लेन-देन की बजाय भविष्योन्मुखी बनाएगा। यह पूरे एशिया के लिये व्यापक रूप से अनुकरण योग्य एक सॉफ्ट-पावर ब्रिज के रूप में भी काम करेगा।
- लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना: भारत कुशल पेशेवरों, छात्रों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिये जापान में संरचित गतिशीलता मार्गों का विस्तार कर सकता है।
- भारत-जापान सांस्कृतिक केंद्र, भाषा संस्थान और नवाचार फेलोशिप स्थापित करने से सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ दूर होंगी।
- मज़बूत श्रम गतिशीलता समझौते जापान की जनांकिकीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और साथ ही भारतीय युवाओं के लिये अवसर भी खोल सकते हैं। ऐसी जन-केंद्रित कूटनीति, शासन कला से परे, स्थायी सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देती है। इस प्रकार, मानवीय संपर्क दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास का आधार बन जाएगा।
- सतत् विकास कूटनीति को बढ़ावा देना: भारत को जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसंरचना, संधारणीय शहरीकरण और हरित वित्त पर जापान के साथ तालमेल बिठाना चाहिये।
- स्मार्ट शहरों, नवीकरणीय ग्रिड और जल प्रबंधन में संयुक्त परियोजनाएँ दोनों देशों को एशिया में स्थिरता के क्षेत्र में अग्रणी बना सकती हैं।
- द्विपक्षीय निवेश में ESG सिद्धांतों को शामिल करने से वैश्विक पूंजी और विश्वसनीयता आकर्षित होगी।
- इससे साझेदारी द्विपक्षीय सहयोग से बढ़कर क्षेत्रीय मानदंड-निर्धारण तक पहुँच जाएगी। इसे ‘हरित रणनीतिक अभिसरण’ के रूप में परिभाषित करने से यह वैश्विक जलवायु आख्यानों में कूटनीतिक रूप से स्थापित हो सकता है।
- बहुपक्षीय तालमेल मंचों का लाभ उठाना: भारत वैश्विक शासन पर जापान के साथ तालमेल बिठाने के लिये क्वाड, SCO और G20 जैसे मंचों का पूरक क्षेत्रों के रूप में उपयोग कर सकता है।
- विभाजन करने के बजाय, भारत को जहाँ तक संभव हो, कूटनीतिक एकजुटता को सुदृढ़ करने के लिये अपनी स्थिति में समन्वय स्थापित करना चाहिये।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) जैसे बहुपक्षीय संस्थानों के सुधारों का सह-समर्थन संयुक्त नेतृत्व का संकेत होगा।
- यह बहुपक्षीय तालमेल मतभेदों को कम करेगा और दोनों देशों की सामूहिक आवाज़ को सशक्त करेगा। ऐसी कूटनीति वैश्विक मंच पर साझेदारी की ताकत को प्रदर्शित करती है।
- रक्षा औद्योगिक सह-उत्पादन का विस्तार: भारत को जापान के साथ रक्षा प्लेटफॉर्मों की खरीद से हटकर सह-डिज़ाइन और सह-निर्माण की ओर रुख करना चाहिये।
- UAV, नौसैनिक प्रणालियों और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स का संयुक्त रूप से विकास करके, दोनों देश रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ावा दे सकते हैं।
- इससे पश्चिमी आपूर्तिकर्त्ताओं पर निर्भरता कम होगी और संवेदनशील क्षेत्रों में विश्वास बढ़ेगा।
निष्कर्ष:
भारत–जापान संबंध आज साझा मूल्यों, आर्थिक परस्परता और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों को लेकर समान चिंताओं पर आधारित रणनीतिक सहयोग का उदाहरण हैं। जैसे भारत एक वैश्विक विकास इंजन के रूप में उभर रहा है और जापान एक सक्रिय साझेदार की भूमिका को फिर से परिभाषित कर रहा है, वैसे ही दोनों देशों की साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता एवं वैश्विक शासन को आकार देने में महत्त्वपूर्ण होगी। इसी भाव को व्यक्त करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जापान को भारत के विकास, रूपांतरण और इंडो-पैसिफिक में शांति, समृद्धि एवं स्थिरता की सामूहिक खोज का ‘स्वाभाविक साझेदार’ बताया है।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. उभरते हिंद-प्रशांत सुरक्षा कार्यढाँचे को आकार देने में भारत-जापान संबंधों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। उनके भिन्न रणनीतिक दृष्टिकोण किस प्रकार एक चुनौती और अवसर दोनों के रूप में कार्य करते हैं? |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)
मेन्स
प्रश्न 1. 'चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद (क्वाड)' वर्तमान समय में स्वयं को सैनिक गठबंधन से एक व्यापारिक गुट में रूपांतरित कर रहा है— विवेचना कीजिये। (2020)