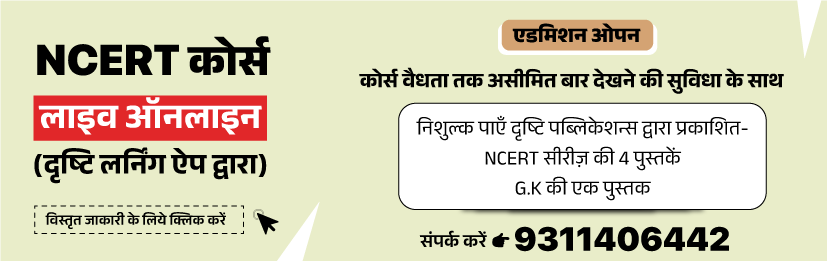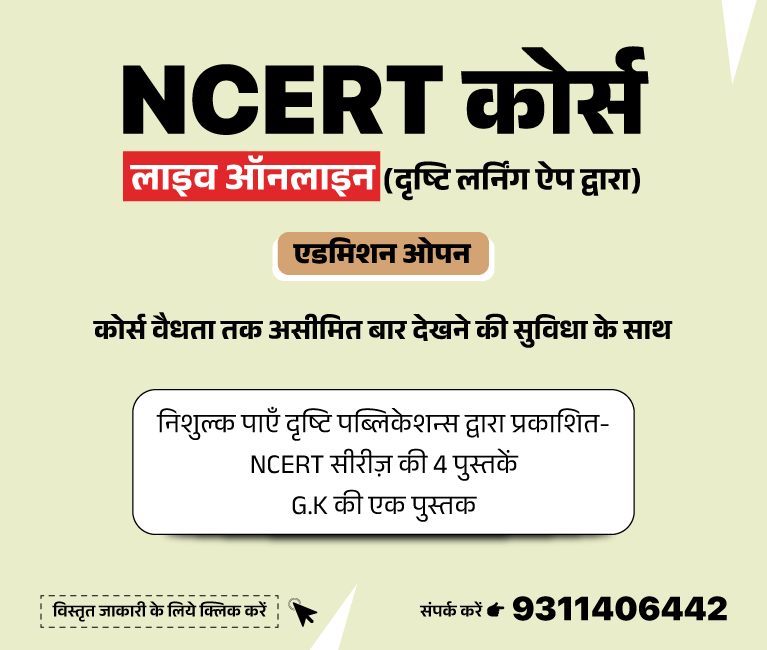भारतीय राजव्यवस्था
विशेष न्यायालय
प्रिलिम्स के लिये:विशेष न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 मेन्स के लिये:विशेष न्यायालय |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विधायकों की त्वरित जाँच के लिये विशेष न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य-विशिष्ट दृष्टिकोण का सुझाव दिया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "वन-साइज़-फिट्स-ऑल" दृष्टिकोण सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की लंबित समस्या को हल नहीं कर सकता है क्योंकि प्रत्येक राज्य में वादों की संख्या अलग-अलग है।
पृष्ठभूमि:
- वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि सांसदों के लंबे समय से लंबित मुकदमों को तेज़ी से ट्रैक करने के लिये देश भर में विशेष अदालतें स्थापित की जाएँ।
- इसके बाद 11 राज्यों में विशेष रूप से मौजूदा सांसदों और विधायकों की सुनवाई के लिये 12 विशेष न्यायालय स्थापित किये गए।
- सितंबर 2020 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी (न्यायालय का मित्र) ने अपनी दो रिपोर्टों में इस बात पर प्रकाश डाला कि विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिये न्यायालय द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन करने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मौजूदा 2,556 संसद (सांसद) और विधान सभाओं के (विधायक) सदस्यों से जुड़े 4,442 आपराधिक मामले लंबित हैं।
- इन मामलों की संख्या अब 5,000 का आँकड़ा पार कर चुकी है, जिनमें से 400 जघन्य अपराधों से संबंधित हैं।
विशेष न्यायालय:
- परिचय:
- विशेष न्यायालय एक सीमित क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय है जो किसी विशेष क्षेत्रीय वार्ड के बजाय कानून के एक निश्चित क्षेत्र से संबंधित होता है। भारत में इन न्यायालयों की स्थापना विशेष न्यायालय अधिनियम, 1979 के तहत की गई है।
- भारत में विशिष्ट प्रकार के मामलों से निपटने हेतु विभिन्न विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। ये न्यायालय त्वरित न्याय प्रदान करने और कुछ प्रकार के मामलों से जुड़ी अद्वितीय कानूनी चुनौतियों का समाधान करने के लिये स्थापित किये गए हैं।
- क्षेत्राधिकार:
- विशेष क्षेत्राधिकार कुछ प्रकार के मामलों पर न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है, जैसे दिवालियापन, सरकार के खिलाफ दावे, प्रमाणित वसीयत, पारिवारिक मामले, आप्रवासन और सीमा शुल्क या अधिकतम राशि या मूल्य वाले मामलों में न्यायालयों के अधिकार पर सीमाएँ। विशेष क्षेत्राधिकार को सीमित क्षेत्राधिकार के रूप में भी जाना जाता है।
- विशेष न्यायालय बहुत ही सीमित क्षेत्राधिकार के तहत मामलों की सुनवाई करता है और इसके न्यायाधीश एक विशिष्ट अवधि के लिये ही कार्य करते हैं, जबकि संवैधानिक न्यायालय का मुख्य अधिकार यह तय करना है कि जिन कानूनों को चुनौती दी गई है, क्या वे असंवैधानिक हैं, उदाहरण के लिये संवैधानिक अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ विरोधाभाषी हैं।
- विशेष क्षेत्राधिकार कुछ प्रकार के मामलों पर न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है, जैसे दिवालियापन, सरकार के खिलाफ दावे, प्रमाणित वसीयत, पारिवारिक मामले, आप्रवासन और सीमा शुल्क या अधिकतम राशि या मूल्य वाले मामलों में न्यायालयों के अधिकार पर सीमाएँ। विशेष क्षेत्राधिकार को सीमित क्षेत्राधिकार के रूप में भी जाना जाता है।
अन्य संबंधित पहलें:
- POCSO मामलों के लिये विशेष न्यायालय
- फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिये योजना
- ई-न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना
आगे की राह
- चूँकि राजनीति नौकरशाही पर हावी है और व्यापार, नागरिक समाज और मीडिया पर लगाम लगाती है, इसलिये देश को ऐसे शासन की आवश्यकता है जो "आपराधिक" वायरस से मुक्त हो।
- जनता के दबाव से अभियोजन सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। यदि एक राजनीतिक दल को बड़ी संख्या में दागी उम्मीदवारों को टिकट देने के मामले में दोषी ठहराया जाता है, तो यह सकारात्मक कदम हो सकता है।
स्रोत: द हिंदू
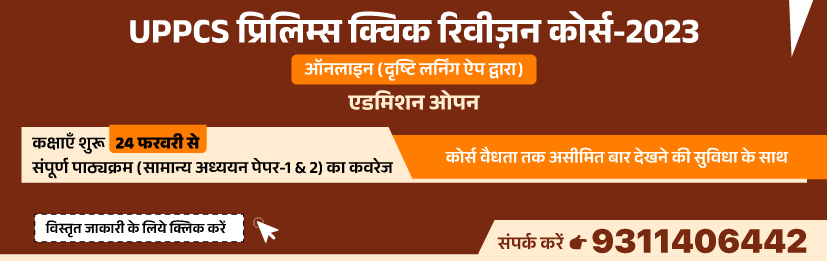
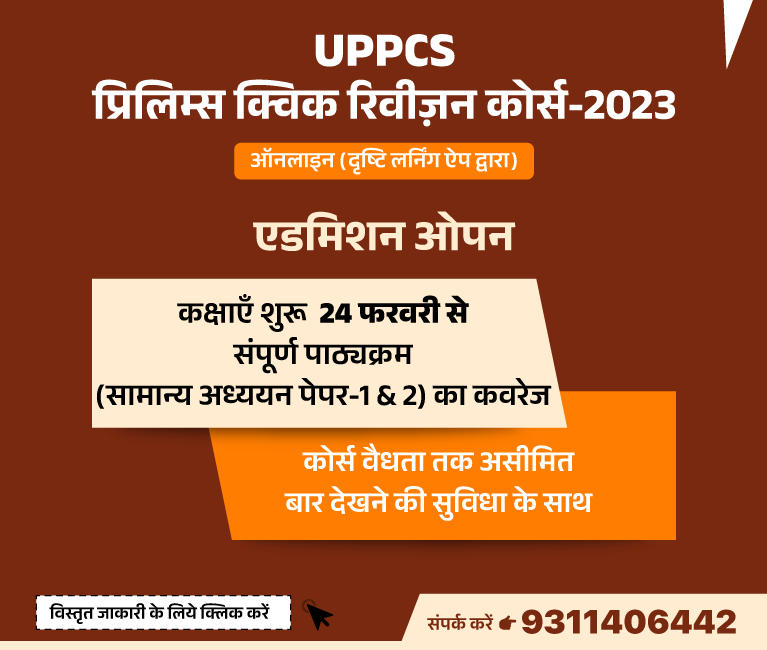
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
निर्देशित ऊर्जा व हाइपरसोनिक हथियार
प्रिलिम्स के लिये:निर्देशित ऊर्जा हथियार (DEWs) और हाइपरसोनिक हथियार की विशेषताएँ मेन्स के लिये:निर्देशित ऊर्जा व हाइपरसोनिक हथियार का महत्त्व |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में भारत के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने वांछित रेंज तथा सटीकता प्राप्त करने के लिये निर्देशित ऊर्जा हथियारों (Directed Energy Weapons- DEWs) और हाइपरसोनिक हथियारों के विकास को बढ़ावा देने तथा उन्हें अपने हवाई प्रणालियों में एकीकृत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
निर्देशित ऊर्जा व हाइपरसोनिक हथियार:
- परिचय:
- आम भाषा में निर्देशित-ऊर्जा हथियार लेज़र, माइक्रोवेव अथवा कण बीम के माध्यम से केंद्रित ऊर्जा का उपयोग करके अपने लक्ष्य को नष्ट करता है।
- उदाहरण- माइक्रोवेव हथियार, लेज़र हथियार, ड्रोन रक्षा प्रणाली आदि।
- हाइपरसोनिक हथियार वह होता है जो ध्वनि की गति से पाँच से दस गुना (मैक 5 से मैक 10 तक) गति से अपने लक्ष्य पर वार कर सकता है।
- आम भाषा में निर्देशित-ऊर्जा हथियार लेज़र, माइक्रोवेव अथवा कण बीम के माध्यम से केंद्रित ऊर्जा का उपयोग करके अपने लक्ष्य को नष्ट करता है।
- पारंपरिक गोला-बारूद की तुलना में DEWs के लाभ:
- DEWs में (विशेष रूप से लेज़र में) उच्च परिशुद्धता, प्रति भेदन कम लागत, लॉजिस्टिक लाभ और ट्रैक न किये जाने (Stealth Capacity) की अधिक क्षमता होती है।
- यह प्रकाश की गति से घातक बल (लगभग 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड) संचारित करता है।
- वायुमंडलीय कर्षण और गुरुत्वाकर्षण के संकुचित प्रभाव का इसके वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- लक्ष्यों के विरुद्ध उपयोग की गई ऊर्जा के प्रकार और तीव्रता को अलग-अलग करके उनके प्रभावों को अनुकूलित किया जा सकता है।
- कमियाँ:
- सीमित मारक क्षमता: अधिकांश DEWs की सीमित मारक क्षमता होती है और लक्ष्य एवं हथियार के बीच की दूरी बढ़ने पर उनकी प्रभावशीलता तेज़ी से घट जाती है
- उच्च लागत: DEWs और हाइपरसोनिक हथियारों का विकास एवं निर्माण महँगा हो सकता है, साथ ही कुछ स्थितियों में उनकी प्रभावशीलता की तुलना में लागत को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
- प्रत्युपाय: DEWs को चिंतनशील सामग्रियों या अन्य प्रत्युपायों (Countermeasures) का उपयोग करके प्रत्युत्तर दिया जा सकता है, जो उनकी प्रभावशीलता को कम कर सकते हैं।
- हथियारों की प्रतिस्पर्द्धा: एक देश द्वारा हाइपरसोनिक हथियारों और DEWs के विकास से हथियारों की प्रतिस्पर्द्धा शुरू हो सकती है, क्योंकि अन्य देश प्रतिक्रिया में अपने स्वयं के हाइपरसोनिक हथियार विकसित करना चाहते हैं। इससे तनाव एवं अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- भारत के लिये महत्त्व:
- एयरोस्पेस उद्योग में इन प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग युद्ध लड़ने के तरीके को बदल सकता है जिससे भारत को भविष्य के युद्ध लड़ने और जीतने के लिये आवश्यक अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म, हथियारों, सेंसर और नेटवर्क का उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकता है।
- DEWs और हाइपरसोनिक हथियार भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाकर चीन, पाकिस्तान जैसे शत्रु राष्ट्रों के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- DEWs वाले अन्य देश:
- रूस, फ्राँस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इज़रायल और चीन उन देशों में से हैं जिन्होंने DEWs या लेज़र निर्देशित ऊर्जा हथियार विकसित करने का कार्यक्रम बनाया है और कई देशों की सेनाओं ने भी उन्हें नियोजित किया है।
- इससे पहले अमेरिका ने क्यूबा पर सोनिक हमले (हवाना सिंड्रोम) का आरोप लगाया था।
भारत की DEWs और हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ:
- 1KW लेज़र हथियार: DRDO ने 1KW लेज़र हथियार का परीक्षण किया है, जो 250 मीटर दूर लक्ष्य को भेद सकता है।
- दिशात्मक रूप से अप्रतिबंधित रे-गन ऐरे (DURGA) II: DRDO ने एक परियोजना DURGA II शुरू की है, जो 100 किलोवाट का हल्का DEW है।
- हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी विकास: भारत में हाइपरसोनिक तकनीक का विकास और परीक्षण DRDO एवं ISRO दोनों द्वारा किया गया है।
- वर्ष 2021 में DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल (HSTDV) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो ध्वनि की गति से 6 गुना अधिक गति से यात्रा करने में सक्षम था।
- भारत अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के हिस्से के रूप में एक स्वदेशी, दोहरी सक्षमता (पारंपरिक और साथ ही परमाणु) वाला हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल भी विकसित कर रहा है।
आगे की राह
- रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की अवधारणा के लिये भारतीय रक्षा प्रोद्योगिकी का उपयोग कर स्वदेशी डिज़ाइन एवं विकास क्षमताओं को विकसित करना शामिल होना चाहिये।
- हमारी रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिये रक्षा अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है।
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
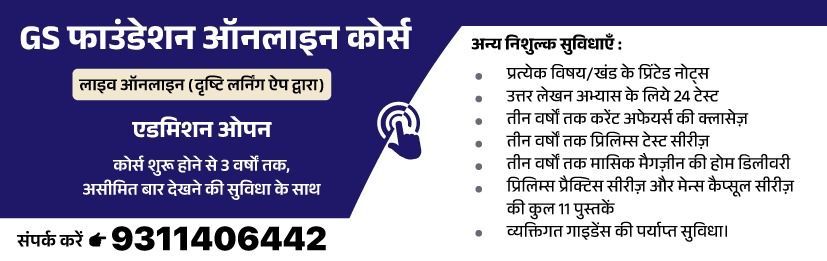
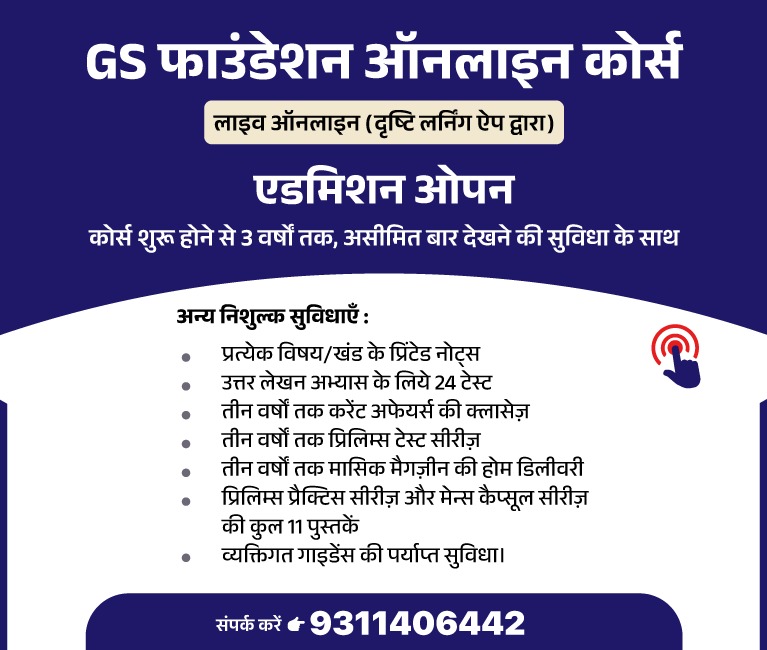
शासन व्यवस्था
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
प्रिलिम्स के लिये:दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (DSPE) अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति मेन्स के लिये:CBI और सिफारिशों से संबंधित मुद्दे |
चर्चा में क्यों?
कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी संसदीय समिति ने कई राज्यों द्वारा CBI जाँच हेतु सामान्य सहमति वापस लिये जाने के मद्देनज़र कहा है कि CBI को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानून की 'कई सीमाएँ' हैं और इसकी स्थिति, कार्यों एवं शक्तियों को परिभाषित करने के लिये इसे एक नए कानून के साथ बदलने की आवश्यकता है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI):
- परिचय:
- CBI की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी और यह दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (Delhi Special Police Establishment- DSPE) अधिनियम द्वारा शासित है।
- इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति (1962-1964) के सुझावों पर की गई थी।
- वर्तमान में CBI भारत सरकार के कार्मिक विभाग, कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।
- CBI की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी और यह दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (Delhi Special Police Establishment- DSPE) अधिनियम द्वारा शासित है।
- कार्य:
- भारतीय अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों और भारत सरकार के स्वामित्त्व या नियंत्रण वाले निकायों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी तथा दुर्व्यवहार के मामलों की जाँच करना।
- राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जाँच करना, अर्थात् निर्यात एवं आयात नियंत्रण, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर विदेशी मुद्रा नियमों से संबंधित कानूनों का उल्लंघन।
- उदाहरण: नकली भारतीय करेंसी नोट, बैंक धोखाधड़ी, आयात-निर्यात और विदेशी मुद्रा उल्लंघन आदि।
- मुद्दे:
- CBI बनाम राज्य पुलिस:
- किसी विशेष राज्य में CBI जाँच राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के अधीन है।
- एक राज्य में सत्तारूढ़ दल कभी-कभी वास्तविक रूप से और कई बार कमज़ोर आधार पर CBI को मामलों की जाँच करने की अनुमति देने से इनकार कर देता है, जिससे जाँच की सीमा सीमित हो जाती है।
- ओवरलैपिंग/दोहराव:
- राज्य पुलिस बलों के साथ विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (CBI का एक प्रभाग) को उन अपराधों के लिये जाँच और अभियोजन की समवर्ती शक्तियाँ प्राप्त हैं जो कभी-कभी मामलों के दोहराव एवं ओवरलैपिंग का कारण बनते हैं।
- CBI बनाम राज्य पुलिस:
- राजनीतिक हस्तक्षेप:
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने CBI के कामकाज़ में अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप की आलोचना की है तथा इसे "अपने मालिक की आवाज़ में बोलने वाला पिंजरे में बंद तोता" कहा है।
संसदीय समिति के निष्कर्ष और सिफारिशें:
- निष्कर्ष:
- सामान्य सहमति की वापसी:
- 9 राज्यों ने CBI द्वारा किसी भी जाँच के लिये आवश्यक सामान्य सहमति को वापस ले लिया है, जिससे CBI को नियंत्रित करने वाला मौजूदा कानून अप्रभावी हो गया है।
- रिक्त पद:
- CBI में रिक्तियों को आवश्यक गति से नहीं भरा जा रहा है, जिससे जाँच की गुणवत्ता में बाधा आ रही है जिससे अंततः एजेंसी की प्रभावशीलता एवं दक्षता प्रभावित हो रही है।
- CBI में स्वीकृत 7,295 पदों के मुकाबले कुल 1,709 पद खाली हैं।
- उच्च पदों, कानूनी अधिकारियों एवं तकनीकी अधिकारियों के संवर्गों में ये रिक्तियाँ निर्विवाद रूप से मामलों की लंबितता को बढ़ाएगी, जाँच की गुणवत्ता को बाधित करेगी जो अंततः एजेंसी की प्रभावशीलता एवं दक्षता को प्रभावित करेगी।
- सामान्य सहमति की वापसी:
- अनुशंसा:
- CBI की स्थिति को पुनः परिभाषित करना:
- समिति CBI की स्थिति, कार्यों और शक्तियों को परिभाषित करने तथा इसके कामकाज़ में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये सुरक्षा उपाय निर्धारित करने हेतु एक नया कानून बनाने की सिफारिश करती है।
- रिक्तियों को तिमाही आधार पर भरना:
- समिति CBI निदेशक से सिफारिश करती है कि वह तिमाही आधार पर रिक्तियों को भरने में हुई प्रगति की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक उपाय करें कि संगठन में पर्याप्त स्टाफ है।
- प्रतिनियुक्ति पर निर्भरता को कम करना:
- CBI को प्रतिनियुक्ति पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहिये एवं पुलिस निरीक्षक तथा पुलिस उपाधीक्षक के पद पर स्थायी कर्मचारियों की भर्ती करने का प्रयास करना चाहिये।
- वाद प्रबंधन प्रणाली: CBI को एक वाद प्रबंधन प्रणाली (Case Management System) निर्मित करनी चाहिये जो एक केंद्रीकृत डेटाबेस होगा, जिसमें इसके पास दर्ज शिकायतों एवं उनके निपटारे में हुई प्रगति का विवरण होगा।
- पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये मामलों के आँकड़े तथा वार्षिक रिपोर्ट भी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी चाहिये।
- CBI के पास दर्ज मामलों का विवरण, उनकी जाँच में हुई प्रगति और अंतिम परिणाम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
- CBI की स्थिति को पुनः परिभाषित करना:
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:प्रश्न. एक राज्य-विशेष के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने और जाँच करने के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र पर कई राज्यों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। हालाँकि सी.बी.आई. जाँच के लिये राज्यों द्वारा दी गई सहमति रोके रखने की शक्ति आत्यंतिक नहीं है। भारत के संघीय ढाँचे के विशेष संदर्भ में व्याख्या कीजिये। (2021) |
स्रोत: द हिंदू