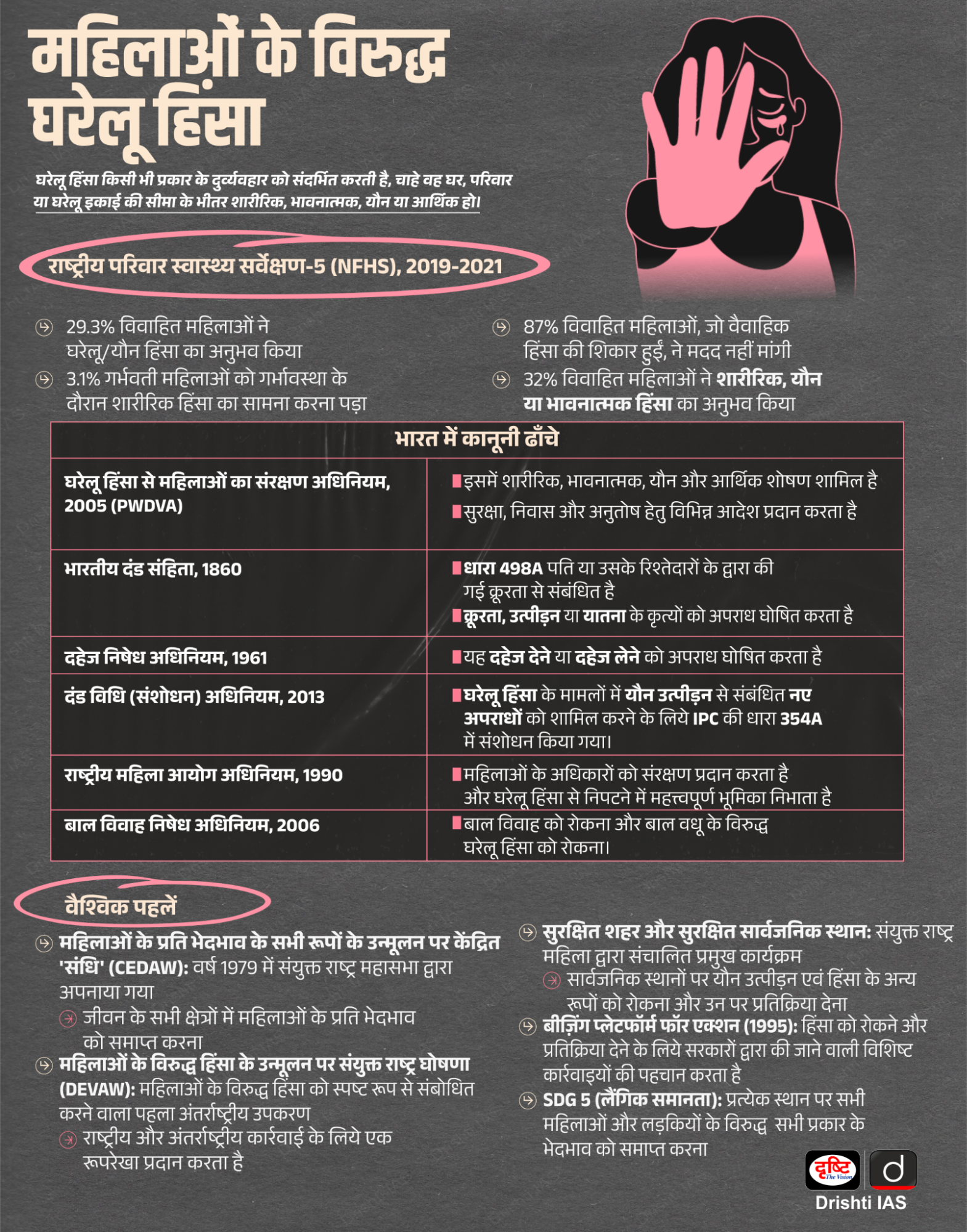भारतीय राजव्यवस्था
वैवाहिक विवाद में अंतिम विकल्प के रूप में पुलिस
प्रिलिम्स के लिये:सर्वोच्च न्यायालय, विश्व आर्थिक मंच, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) मेन्स के लिये:वैवाहिक विवाद में अंतिम विकल्प के रूप में पुलिस, घरेलू हिंसा में योगदान देने वाले कारक, वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) |
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक समस्याओं का सामना कर रहे परिवारों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा है कि पुलिस के पास जाना उनके लिये "अंतिम विकल्प" होना चाहिये।
सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या हैं?
- परिचय:
- सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध पति द्वारा दायर याचिका पर निर्णय सुनाते हुए कुछ टिप्पणियाँ कीं, जिसमें उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय केवल "क्रूरता और उत्पीड़न के वास्तविक मामलों" में पुलिस के हस्तक्षेप का उपयोग करने में सावधानी बरतने की सलाह देता है।
- टिप्पणियाँ:
- यह निर्णय भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (घरेलू क्रूरता) के यांत्रिक अनुप्रयोग के विरुद्ध चेतावनी देता है।
- एक "पूर्ण" घरेलू हिंसा के मामले में आपराधिक धमकी या मामूली परेशानियों से परे क्षति पहुँचाने जैसे तत्त्वों की आवश्यकता होती है।
- न्यायालय ने संसद से भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85 और 86 (3 वर्ष तक की सज़ा) (IPC की धारा 498A के समान) की समीक्षा करने का आग्रह किया।
- तलाक को बच्चे के पालन-पोषण के लिये हानिकारक माना जाता है, विशेष रूप से जब कानूनी प्रक्रियाओं के कारण जल्दबाज़ी की जाती है।
- यह निर्णय उच्च न्यायालयों को वैवाहिक मुद्दों से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका पर निर्णय लेने से पूर्व सभी पहलुओं और परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
नोट:
- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध को IPC की धारा 377 के तहत "बलात्कार" नहीं माना जाएगा क्योंकि ऐसे मामले में पत्नी की सहमति महत्त्वहीन हो जाती है क्योंकि वह उससे विवाहित थी।
- एक पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए दर्ज़ कराई गई FIR को न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया।
- हालाँकि वैवाहिक बलात्कार IPC में अपराध नहीं है, फिर भी केरल उच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 में फैसला सुनाया कि वैवाहिक बलात्कार पति द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता है और क्रूरता के दायरे में यह तलाक का आधार है।
वैवाहिक विवादों को हल करने हेतु अन्य मौजूदा उपाय क्या हैं?
- वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution- ADR) के तहत विभिन्न तंत्र वैवाहिक विवादों के यथाशीघ्र समाधान में सहायता कर सकते हैं:
- मध्यस्थता: एक तटस्थ तृतीय पक्ष वैवाहिक और पारिवारिक विवादों के संबंध में पारस्परिक रूप से सहमत समाधान तक पहुँचने के लिये पति-पत्नी के बीच बातचीत एवं समझौते की सुविधा प्रदान करता है।
- के. श्रीनिवास राव बनाम डी.ए. दीपा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवादों में मध्यस्थता पर ज़ोर दिया।
- सुलह: मध्यस्थता के समान, सुलहकर्त्ता भी समाधान प्रस्तावित कर सकता है और युग्म को एक समझौते की ओर मार्गदर्शित कर सकता है।
- माध्यस्थम्: यहाँ दोनों पक्षों द्वारा चुना गया एक निजी मध्यस्थ तर्क सुनता है और विवाद से संबंधित बाध्यकारी निर्णय देता है।
- मध्यस्थता: एक तटस्थ तृतीय पक्ष वैवाहिक और पारिवारिक विवादों के संबंध में पारस्परिक रूप से सहमत समाधान तक पहुँचने के लिये पति-पत्नी के बीच बातचीत एवं समझौते की सुविधा प्रदान करता है।
- इसके अतिरिक्त विभिन्न कानूनी संस्थान विवाह की अवधारणा में भावनाओं और सामाजिक वर्जनाओं जैसे कारकों की भागीदारी के कारण न्याय प्रदान करने के अधिक प्रभावी तरीके के रूप में वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution- ADR) प्रदान करते हैं।
- 1984 के परिवार न्यायालय अधिनियम द्वारा स्थापित परिवार न्यायालय विवाह और पारिवारिक मामलों तथा उससे संबंधित विवादों के सुलह एवं त्वरित निपटान को बढ़ावा देते हैं।
- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत स्थापित ग्राम न्यायालय भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वैवाहिक विवादों तक त्वरित और सीधी पहुँच प्रदान करते हैं।
- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 भी पारिवारिक विवादों में सुलह को प्रोत्साहित करते हैं।
आगे की राह
- संसद को भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 86 की समीक्षा पर विचार करना चाहिये ताकि भविष्य इसके दुरुपयोग या फर्ज़ी मामलों को रोका जा सके।
- वैवाहिक विवादों से संबंधित मामलों में पुलिस के हस्तक्षेप को कम करने के लिये कानूनी कार्रवाई से पूर्व सुलह के प्रयासों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये।
- संवेदनशील वैवाहिक मुद्दों को संभालने में मध्यस्थों और सुलहकर्त्ताओं के उचित प्रशिक्षण द्वारा ADR तंत्र को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
- खाप पंचायतों (जाति या सामुदायिक समूहों) जैसे स्थानीय एवं अनियमित ADR तंत्र को विनियमित और सुधारने की आवश्यकता है, जो अर्द्ध-न्यायिक निकायों के रूप में कार्य करते हैं तथा संवेदनशील वैवाहिक मुद्दों में भी सदियों पुराने रीति-रिवाज़ों के आधार पर कठोर दंड देते हैं।
- शांतिपूर्ण विवाद समाधान के लिये कानूनी अधिकारों और ADR विकल्पों के बारे में जन जागरूकता पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
- वैवाहिक कलह का सामना कर रहे जोड़ों को सुलभ मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने, संचार और संघर्ष समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिये उचित तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये।
निष्कर्ष:
सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी वैवाहिक विवादों के प्रति सूक्ष्म दृष्टिकोण पर आधारित है। यह जोड़ों को तत्काल पुलिस हस्तक्षेप या आपराधिक कार्यवाही पर सुलह करने और सहनशीलता को प्राथमिकता देने के लिये प्रोत्साहित करता है। क्रूरता के वास्तविक मामलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय का उद्देश्य कानूनों के दुरुपयोग को रोकना तथा पति-पत्नी और बच्चों दोनों की भलाई की रक्षा करना है।
|
दृष्टि मुख्य प्रश्न: प्रश्न. वैवाहिक मामलों में पुलिस की भागीदारी पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर चर्चा कीजिये। इसके अलावा भारत में वैवाहिक विवादों को सुलझाने के अन्य मौजूदा तरीकों का भी उल्लेख कीजिये। |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, गत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. प्रायः समाचारों में देखी जाने वाली 'बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच (बीजिंग डिक्लरेशन ऐंड प्लैटफॉर्म फॉर ऐक्शन)' निम्नलिखित में से क्या है? (2015) (a) क्षेत्रीय आतंकवाद से निपटने की एक कार्यनीति (स्ट्रैटजी), शंघाई सहयोग संगठन (शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन) की बैठक का एक परिणाम उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. हमें देश में महिलाओं के प्रति यौन-उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कुकृत्य के विरुद्ध विद्यमान विधिक उपबंधों के होते हुए भी, ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संकट से निपटने के लिये कुछ नवाचारी उपाय सुझाइए। (2014) प्रश्न. भारत में एक मध्यम-वर्गीय कामकाज़ी महिला की अवस्थिति को पितृतंत्र (पेट्रिआर्की) किस प्रकार प्रभावित करता है? (2014) |
एथिक्स
केरल सर्जिकल घटना में नैतिक और प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ
प्रिलिम्स के लिये:चिकित्सीय नैतिकता के सिद्धांत, भारतीय दंड संहिता (IPC) मेन्स के लिये:चिकित्सीय लापरवाही के नैतिक निहितार्थ, मानव कार्रवाई में नैतिकता के निर्धारक और परिणाम |
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
चर्चा में क्यों?
हाल ही में केरल के एक चिकित्सक को एक बच्चे की अतिरिक्त अँगुली हटाने के बजाय त्रुटिवश जीभ की सर्जरी करने के लिये निलंबित कर दिया गया।
- यह कोझिकोड के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुआ। जीवन को खतरे में डालने के लिये चिकित्सक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 336 और 337 के तहत कानूनी कार्रवाई की गई।
- यह घटना चिकित्सा प्रोटोकॉल और नैतिकता के सख्ती से पालन करने की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
नैतिकता चिकित्सा पद्धति को किस प्रकार निर्देशित करती है?
- नैतिक सिद्धांत चिकित्सा पद्धति में मूलभूत होते हैं, जो अक्सर कानूनी आवश्यकताओं से अधिक कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। उन चार प्राथमिक सिद्धांतों में शामिल हैं:
- स्वायत्तता: उचित सूचित सहमति प्राप्त करके अपने उपचार के बारे में सूचित निर्णय लेने के रोगी के अधिकार का सम्मान करना।
- बच्चे के माता-पिता द्वारा प्रदान की गई सहमति अँगुली की सर्जरी के लिये थी, जीभ की सर्जरी के लिये नहीं, जिससे बच्चे की स्वायत्तता का उल्लंघन हुआ।
- उपकार: संपूर्ण सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान रोगी के स्वास्थ्य और कल्याण के सर्वोत्तम हित में कार्य करना।
- गलत तरीके से सर्जरी करना रोगी की आवश्यकताओं या उसके सर्वोत्तम हितों के अनुरूप नहीं है।
- गैर-दोषपूर्ण: रोगी को खतरों से सुरक्षित रखना, एक चिकित्सा पेशेवर जो अस्थायी या स्थायी रूप से पंजीकृत है, वह जानबूझकर लापरवाह व्यवहार में संलग्न नहीं हो सकता है जो रोगी को आवश्यक चिकित्सा उपचार तक पहुँच से वंचित कर सकता है।
- इस घटना में बच्चे की जीभ पर एक अनावश्यक और हानिकारक प्रक्रिया की गई, जो इस सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है।
- न्याय: धर्म, राष्ट्रीयता, नस्ल या सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे कारकों के आधार पर भेदभाव किये बिना, सभी रोगियों के साथ निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार करना।
- यह स्थिति इस प्रश्न को जन्म देती है कि क्या बच्चे के साथ उचित व्यवहार किया गया, विशेषकर चिकित्सा क्षेत्र में अपेक्षित मानकों के आलोक में।
- स्वायत्तता: उचित सूचित सहमति प्राप्त करके अपने उपचार के बारे में सूचित निर्णय लेने के रोगी के अधिकार का सम्मान करना।
- मिथ्यापूर्ण शपथ: यह नए चिकित्सा स्नातकों के लिये एक आधारशिला है और दीक्षांत समारोहों के दौरान इसका पाठ किया जाता है, जो उन्हें नैतिकता का पालन करने के लिये बाध्य करती है। भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 में उल्लिखित सिद्धांत मानवता की सेवा, चिकित्सा कानूनों का पालन, जीवन के प्रति सम्मान, रोगी कल्याण प्राथमिकता, गोपनीयता, शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता और सामूहिक सम्मान के प्रति प्रतिबद्धता का वचन देते हैं।
- यह शपथ एक नैतिक दिशासूचक के रूप में कार्य करती है, जो चिकित्सकों का चिकित्सा पेशे की सम्मानित परंपराओं और नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिये मार्गदर्शन करती है।
केरल सर्जिकल घटना में कौन-से नैतिक सिद्धांत शामिल हैं?
- सत्यनिष्ठा और वस्तुनिष्ठताः चिकित्सक के कार्य में सत्यनिष्ठा और वस्तुनिष्ठता का अभाव था, जो किसी भी सेवा, विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित, अपेक्षित मूलभूत मूल्य हैं।
- लोक सेवा के प्रति समर्पण: रोगी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। सर्जिकल त्रुटि इस प्रतिबद्धता के खंडित होने का संकेत देती है।
- चिकित्सकों से चिकित्सा पद्धति और देखभाल के उच्च मानक बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। सर्जिकल (चिकित्सा संबंधी) त्रुटि इन कर्त्तव्यों और ज़िम्मेदारियों को निभाने में विफलता का संकेत देती है।
- रोगी की विश्वसनीयता और गोपनीयता: विश्वसनीयता चिकित्सक-रोगी संबंध का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
- ऐसी घटनाएँ न केवल रोगी और चिकित्सक के बीच बल्कि व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में भी लोगों के विश्वास को कम कर सकती हैं।
- जवाबदेही और नैतिक शासन: चिकित्सक द्वारा किया गया कार्य संबंधित अस्पताल के प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल उठाता है।
- यह घटना स्वास्थ्य देखभाल में आने वाली नैतिक दुविधाओं को उजागर करती है तथा नैतिक दिशानिर्देशों के सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर बल देती है।
आगे की राह
- संरचनात्मक संचार प्रोटोकॉल: स्थिति-पृष्ठभूमि-आकलन-अनुशंसा (Situation Background Assessment Recommendation- SBAR) तकनीक जैसे संरचित संचार प्रोटोकॉल को लागू करने से स्पष्टता में सुधार हो सकता है और त्रुटियाँ कम हो सकती हैं।
- सूचित सहमति सुनिश्चित करने में समझ के सत्यापन के साथ-साथ प्रक्रिया, जोखिम, लाभ और विकल्पों की विस्तृत व्याख्या शामिल हैI
- पूर्वकारी सत्यापन को मज़बूत करना: सर्जरी से तुरंत पहले एक अनिवार्य "टाइम-आउट" प्रक्रिया को अपनाना ताकि रोगी की पहचान, सर्जिकल साइट और पूरी सर्जिकल टीम की उपस्थिति में नियोजित प्रक्रिया की पुष्टि की जा सके।
- पारदर्शी जाँच प्रक्रिया: यह सुनिश्चित करना कि घटनाओं की जाँच पारदर्शी तरीके से हो और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में विश्वास बहाल करने के लिये निष्कर्षों को जनता के साथ साझा किया जाए।
- मुआवज़ा: पीड़ितों को हुई हानि के कारण उन्हें उचित मुआवज़ा प्राप्त करने का अधिकार है। यह मुआवज़ा चिकित्सा बिलों के तत्काल वित्तीय बोझ से अलग होना चाहिये। इसमें वास्तविक और अमूर्त दोनों प्रकार की हानियाँ शामिल होनी चाहिये।
- नैतिक जागरूकता की संस्कृति को बढ़ावा देना: स्वास्थ्य पेशेवरों को नैतिक सिद्धांतों और चिकित्सा पद्धति में उनके अनुप्रयोग के संबंध में शिक्षित करने के लिये व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाएँ आयोजित करना।
- नैतिक दुविधाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिये स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के भीतर स्पष्ट बातचीत एवं पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा देना।
- कानूनी और नैतिक आचार संहिता: कानूनी रूप से निहित आचार संहिता के कार्यान्वयन हेतु समर्थन करना, जो स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिये स्पष्ट नैतिक अपेक्षाओं को रेखांकित करता है।
- चिकित्सा पद्धति में सत्यनिष्ठा, करुणा और व्यावसायिकता को बढ़ावा देने वाले सामाजिक रूप से लागू आचार संहिता के महत्त्व पर ज़ोर देना।
- एक सहायक और सहयोगात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देना जो नैतिक आचरण, व्यावसायिकता तथा रोगी-केंद्रित देखभाल को महत्त्व देता हो।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. "विश्वास चिकित्सक और रोगी के संबंध की नींव होता है तथा चिकित्सीय लापरवाही की घटनाएँ इस विश्वास को समाप्त कर सकती हैं।" इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में जनता का विश्वास बहाल करने के उपाय सुझाइए। |