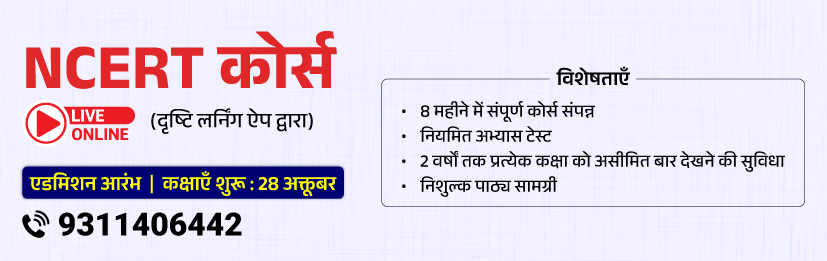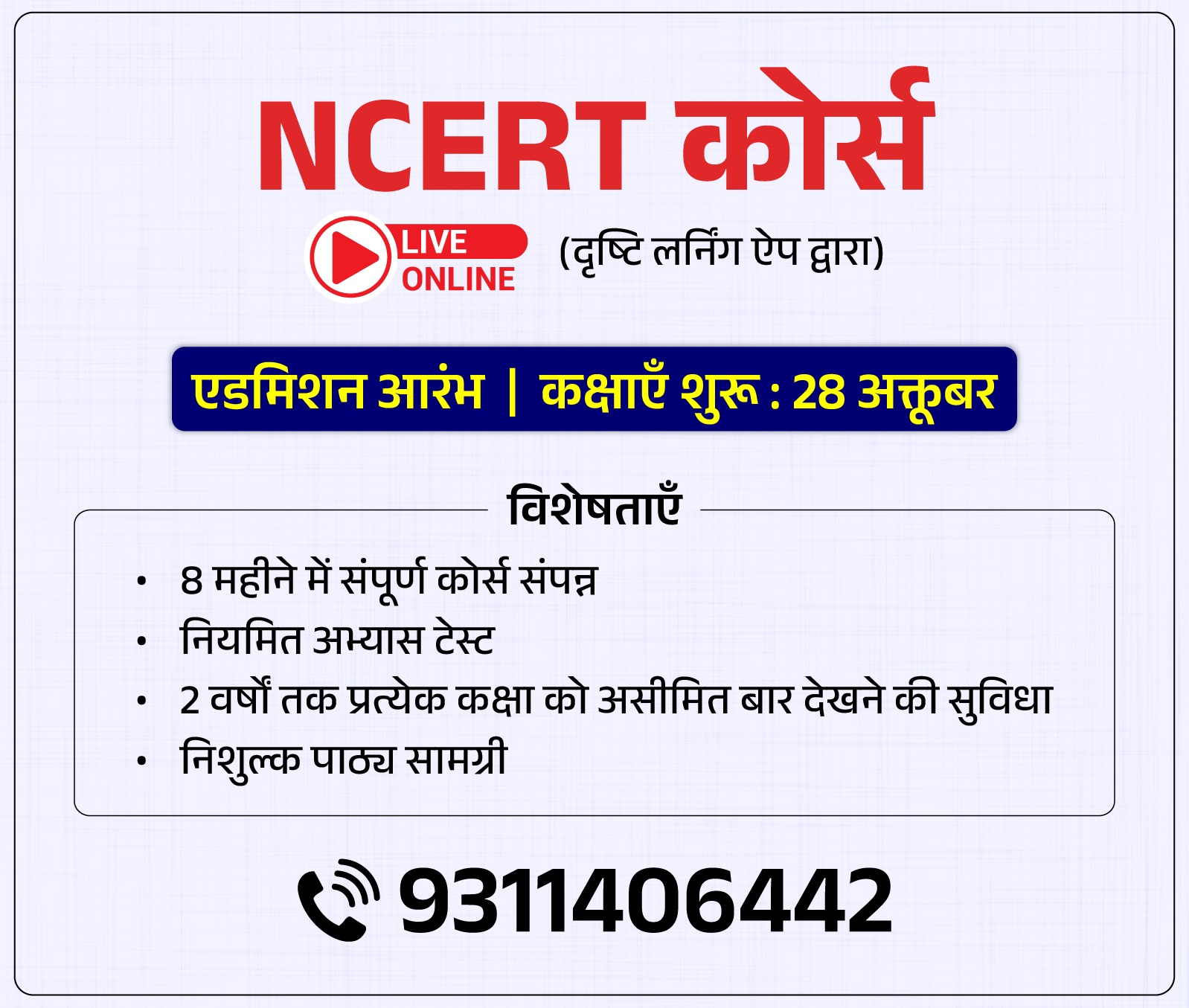भारतीय इतिहास
कुम्हरार और मौर्य स्थापत्य कला का 80 स्तंभ वाला सभागार
प्रिलिम्स के लिये:भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, मौर्य साम्राज्य, सम्राट अशोक, बौद्ध धर्म, केंद्रीय भूजल बोर्ड, साँची स्तूप, आजीवक संप्रदाय मेन्स के लिये:मौर्य साम्राज्य और प्राचीन भारत में महत्त्व, मौर्य वास्तुकला |
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
चर्चा में क्यों?
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) ने पटना के कुम्हरार स्थित मौर्यकालीन पुरातात्त्विक स्थल पर 80 स्तंभों वाले सभा भवन के अवशेषों के सर्वेक्षण के प्रयास शुरू किये हैं।
- इस पहल से मौर्य साम्राज्य और वास्तुकला में उनके योगदान के प्रति वर्तमान रूचि पर प्रकाश पड़ता है
कुम्हरार के 80 स्तंभों वाले सभा भवन के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?
- ऐतिहासिक महत्त्व: कुम्हरार का 80 स्तंभों वाला सभा भवन, मौर्य साम्राज्य (321-185 ईसा पूर्व) से संबंधित है, जो प्राचीन भारत के महानतम राजवंशों में से एक था।
- ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक (268-232 ईसा पूर्व) ने इस हॉल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, जिसका उद्देश्य खंडित बौद्ध संघ को एकीकृत करने के साथ और धम्म (बौद्ध शिक्षाओं) का प्रचार करना था।
- यह घटना बौद्ध धर्म को वैश्विक धर्म के रूप में स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण थी।
- यह स्थल मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र (मौर्य राजधानी) की भूमिका की पुष्टि करता है।
- ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक (268-232 ईसा पूर्व) ने इस हॉल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, जिसका उद्देश्य खंडित बौद्ध संघ को एकीकृत करने के साथ और धम्म (बौद्ध शिक्षाओं) का प्रचार करना था।
- वास्तुशिल्पीय महत्त्व: इस हॉल में 80 बलुआ पत्थर के खंभे हैं जो इसकी छत का आधार हैं।
- बलुआ पत्थर और लकड़ी जैसी सामग्रियों का परिवहन सोन -गंगा नदी मार्ग से किया जाता था, जो मौर्य काल के दौरान योजना और संसाधन प्रबंधन को दर्शाता है।
- पुरातात्त्विक खोजें:
- प्रथम उत्खनन (1912-1915): एक अक्षुण्ण स्तंभ, अन्य स्तंभों के स्थान को चिह्नित करने वाले 80 गड्ढे, तथा पत्थर के टुकड़े मिले।
- राख की मोटी परतों के साक्ष्य से पता चलता है कि विनाश आग से हुआ था, संभवतः इंडो-यूनानी आक्रमण के दौरान या बाद में हूणों के आक्रमण के दौरान।
- दूसरा उत्खनन (1961-1965): चार अतिरिक्त स्तंभ मिले।
- प्रथम उत्खनन (1912-1915): एक अक्षुण्ण स्तंभ, अन्य स्तंभों के स्थान को चिह्नित करने वाले 80 गड्ढे, तथा पत्थर के टुकड़े मिले।
- संरक्षण चुनौतियाँ: जल स्तर बढ़ने के कारण यह स्थल आंशिक रूप से जलमग्न हो गया, जिसके कारण ASI को संरक्षण उपाय के रूप में वर्ष 2004-2005 में इसे मृदा से ढकना पड़ा।
- असेंबली हॉल की रीओपनिंग: पटना में घटते भूजल स्तर और मौर्यकालीन विरासत में बढ़ती रुचि के कारण ASI द्वारा इस स्थल की रीओपनिंग की जा रही है।
- प्रारंभ में, केंद्रीय भूजल बोर्ड के सहयोग से, आर्द्रता और भूजल प्रभावों का अध्ययन करने के लिये 6-7 स्तंभों को उज़ागर किया जाएगा।
- इसके पश्चात् एक विशेषज्ञ समिति 80 स्तंभों को पूर्ण रूप से पुनः खोलने पर निर्णय लेगी, जिसमें संरक्षण और सार्वजनिक पहुँच के बीच संतुलन बनाया जाएगा।
मौर्यकला और स्थापत्य की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
- स्थापत्य के प्रकार: मौर्य स्थापत्य को दरबारी कला (राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों हेतु सुरचित) और लोकप्रिय कला (व्यापक रूप से सुलभ और स्थानीय परंपराओं से प्रभावित) में वर्गीकृत किया गया है ।
मौर्य दरबार कला:
- महल: यूनानी इतिहासकार मेगस्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के महलों की प्रशंसा करते हुए उन्हें उल्लेखनीय रचना बताया, जबकि चीनी यात्री फाह्यान ने इन्हें ईश्वर प्रदत्त स्मारक कहा।
- चंद्रगुप्त मौर्य का महल पर्सेपोलिस (अकेमेनिड साम्राज्य की राजधानी) के अकेमेनिड महलों से प्रभावित था।
- निर्माण में प्रयुक्त होने वाली प्राथमिक सामग्री लकड़ी थी।
- उदाहरण: कुम्हरार में अशोक का महल और चंद्रगुप्त का महल।
- स्तम्भ: मौर्य स्तंभ ऊँचे, स्वतंत्र, अखंड हैं तथा चुनार से प्राप्त बलुआ पत्थर से निर्मित हैं।
- इसमें चमकदार पॉलिश है, ये अकेमेनियन स्तंभों से प्रभावित हैं।
- मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, जो नक्काशी के कौशल को दर्शाते हैं, जबकि अकेमेनियाई स्तंभों का निर्माण टुकड़ों में किया गया था।
- उत्तर भारत में पाए जाने वाले अशोक के स्तंभों में प्रायः शेर और बैल जैसी पशु आकृतियाँ होती हैं, जो राजकीय प्रतीक हैं।
- इन्हें बौद्ध शिक्षाओं और दरबारी आदेशों के प्रसार के लिये बनवाया गया था, जिन पर पाली, प्राकृत, ग्रीक और आरमेइक भाषा में शिलालेख अंकित थे।
- मौर्य स्तंभों की संरचना में चार भाग हैं: जिसमें एकाश्म शाफ्ट, एक कमल या घंटी के आकार का शीर्ष, एक स्तंभ और एक शीर्ष आकृति शामिल है।
- अकेमेनियन स्तंभों के साथ समानताओं में पॉलिश किये गए पत्थर और कमल जैसी आकृतियाँ, साथ ही उद्घोष अंकित करने की प्रथा शामिल है।
- इसमें चमकदार पॉलिश है, ये अकेमेनियन स्तंभों से प्रभावित हैं।
- स्तूप: सामान्यतः स्तूपों में एक बेलनाकार ड्रम, एक अर्द्धगोलाकार टीला (अंडाकार), एक हर्मिका (वर्गनुमा रेलिंग), और एक छत्र (तीन छतरी के आकार को सहारा देने वाला केंद्रीय स्तंभ) होता है, जो बौद्ध सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है।
- स्तूप का मुख्य भाग कच्ची ईंटों से निर्मित था, जबकि बाह्य सतह पर पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था, जिसे प्लास्टर से ढका गया था तथा लकड़ी की मूर्तियों से सजाया गया था।
- साँची स्तूप (मध्य प्रदेश), सबसे प्रसिद्ध अशोक स्तूप। पिपरहवा स्तूप (उत्तर प्रदेश) सबसे प्राचीन।
- बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् के अन्य स्तूप: राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लकप्पा, रामग्राम, वेथापिडा, पावा, कुशीनगर, पिप्पलिवन।
मौर्य लोकप्रिय कला:
- गुफा स्थापत्य: मौर्य काल के दौरान, जैन और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा गुफाओं का उपयोग विहार के रूप में किया जाता था। अत्यधिक नक्काशीयुक्त अंदरूनी भाग और सजावटी प्रवेश द्वार इनकी विशेषता है।
- उदाहरण: बिहार में बराबर गुफाएँ (4 गुफाएँ), अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिये निर्मित (मक्खलिपुत्त गोशाल द्वारा स्थापित, इस बात पर बल दिया गया कि ब्रह्मांड नियति (भाग्य) द्वारा शासित था)।
- मूर्तियाँ: यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियों की पूजा जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में की जाती थी।
- उदाहरण: लोहानीपुर यक्ष (नग्न पुरुष आकृति का धड़), और दीदारगंज यक्षिणी, पटना आदि।
- मृद्भांड: उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद्भाण्ड (NBPW) के रूप में पहचाने जाने वाले मौर्यकालीन मृद्भांडो पर काला रंग और चमकदार सतह होती थी, जिसका उपयोग प्रायः विलासिता की वस्तुओं के लिये किया जाता था।
मौर्य साम्राज्य
- चन्द्रगुप्त मौर्य (321-297 ईसा पूर्व): मौर्य साम्राज्य के संस्थापक ने नंद वंश को समाप्त कर हिंदू कुश जैसे क्षेत्रों पर कब्जा करके साम्राज्य का विस्तार किया।
- 305-303 ईसा पूर्व में, उन्होंने सेल्यूकस निकेटर के साथ एक संधि की, जिससे उन्हें अतिरिक्त क्षेत्र प्राप्त हुए। बाद में चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी बन गए।
- चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य (322 ईसा पूर्व - 297 ईसा पूर्व) और उनके उत्तराधिकारी बिंदुसार के शासनकाल के दौरान प्रधानमंत्री थे। साम्राज्य की सफलता में चाणक्य ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- बिंदुसार (298-272 ई.पू.): साम्राज्य का विस्तार दक्कन तक किया, जिसे "अमित्रघात" (शत्रुओं का नाश करने वाला) के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार ने आजीविक संप्रदाय को अपनाया। डेमेकस उनके दरबार में एक यूनानी राजदूत था।
- अशोक (272-232 ईसा पूर्व): कलिंग युद्ध के बाद, जिसमें भारी जनहानि हुई, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया तथा अपने धम्म (नैतिक कानून) के माध्यम से शांति को बढ़ावा दिया। उन्होंने तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किया और बौद्ध धर्म को विश्व स्तर पर फैलाया।
- दशरथ (232-224 ई.पू.): शाही शिलालेख जारी करने वाले अंतिम मौर्य शासक दशरथ थे, जिन्हें क्षेत्रीय संघर्ष का सामना करना पड़ा।
- सम्प्रति (224-215 ईसा पूर्व): विघटित क्षेत्रों पर मौर्य नियंत्रण पुनः स्थापित किया और जैन धर्म को बढ़ावा दिया।
- शालिशुक (215-202 ईसा पूर्व): नकारात्मक प्रतिष्ठा के रूप में एक आक्रमणकारी शासक के रूप में जाना जाता था।
- देववर्मन (202-195 ईसा पूर्व): संक्षिप्त शासनकाल, पुराणों में उल्लेखित।
- शतधन्वन (195-187 ईसा पूर्व): बाहरी आक्रमणों के कारण कई क्षेत्रो का विघटन।
- बृहद्रथ (187-185 ईसा पूर्व): अंतिम मौर्य सम्राट, पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या, मौर्य वंश के पतन का प्रतीक।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)
- केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत ASI, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 तथा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958. (AMASR अधिनियम) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा और रखरखाव करता है।
- ASI पुरातात्विक स्थलों और संरक्षित स्मारकों का सर्वेक्षण, उत्खनन और संरक्षण कार्य करता है।
- ASI की स्थापना वर्ष 1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। उन्हें "भारतीय पुरातत्व का जनक" माना जाता है।
|
दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत की सांस्कृतिक विरासत में मौर्य वास्तुकला के योगदान पर चर्चा कीजिये। |
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रारंभिकप्रश्न. निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया ? "कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा-मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निन्दा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुँचाता है।" (2020) (a) अशोक उत्तर: (a) प्रश्न. निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्तिशिल्प (रिलीफ स्कल्प्चर) शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ ‘राण्यो अशोक’ (राजा अशोक) उल्लिखित है? (2019) (a) कंगनहल्ली उत्तर: (a) प्रश्न: निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था? (2016) (a) जॉर्ज बुहलर उत्तर: (B) |
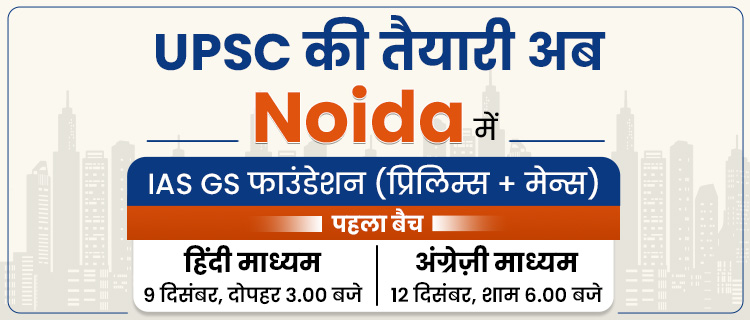
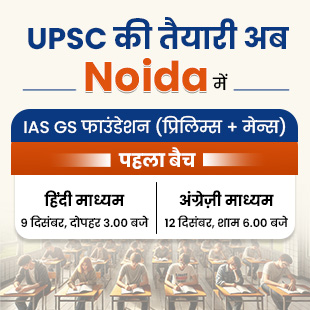
भारतीय इतिहास
अकाल तख्त
प्रिलिम्स के लिये:अकाल तख्त, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, गुरु हरगोबिंद, गुरु गोबिंद सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, गुरु ग्रंथ साहिब मेन्स के लिये:धार्मिक संस्थाओं का शासन और स्वायत्तता, भारत में धर्म और राजनीति के बीच अंतर्संबंध, सिख धर्म |
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
चर्चा में क्यों?
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) द्वारा शासित सिख समुदाय की सर्वोच्च लौकिक और आध्यात्मिक संस्था अकाल तख्त ने शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर धार्मिक दंड (तन्खा) लगाया है।
- यह कार्रवाई पंजाब में SAD के कार्यकाल (वर्ष 2007-2017) के दौरान कथित कुशासन के लिये सज़ा के रूप में की गई है।
- इससे अकाल तख्त के अधिकार तथा शिरोमणि अकाली दल और SGPC के साथ उसके संबंधों पर चर्चा आरंभ हो गई है।
अकाल तख्त क्या है?
- ऐतिहासिक महत्त्व: अकाल तख्त की स्थापना वर्ष 1606 में गुरु हरगोबिंद, 6 वें सिख गुरु द्वारा, उनके पिता, गुरु अर्जन देव (सिखों के 5 वें गुरु) को मुगलों द्वारा फाँसी दिये जाने के परिणामस्वरूप की गई थी।
- तख्त एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है "शाही सिंहासन"। अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर परिसर में हरमंदिर साहिब के सामने स्थित है।
- मुगल उत्पीड़न के प्रत्युत्तर में निर्मित अकाल तख्त सिख संप्रभुता का प्रतीक बन गया, जो शासन एवं न्याय के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता था।
- प्रतीकात्मकता: गुरु ने दो तलवारों को चिह्नित किया, जो मीरी (लौकिक शक्ति) और पीरी (आध्यात्मिकता) का प्रतीक थीं, जिसमें मीरी तलवार छोटी थी, जो आध्यात्मिक अधिकार की प्रधानता को दर्शाती थी।
- अकाल तख्त में एक ऊँचा सिंहासन है, जो मुगल संप्रभुता द्वारा स्वीकृत अधिकतम ऊँचाई से तीन गुना ऊँचा है।
- इसकी ऊँचाई दिल्ली के लाल किले में मुगल सिंहासन की बालकनी से भी अधिक है, जो मुगल शासन के खिलाफ अवज्ञा और सिख संप्रभुता का प्रतीक है।
- आध्यात्मिक और लौकिक प्राधिकार: अकाल तख्त सिख धर्म के पाँच तख्तों (शक्ति के आसन) में से एक है, लेकिन अपने दोहरे प्राधिकार (लौकिक शासन के साथ आध्यात्मिक मार्गदर्शन) के कारण सर्वोच्च स्थान रखता है।
- हुक्मनामा (फरमान) जारी करने की परंपरा यहीं से आरंभ हुई, जो सिख समुदाय के मार्गदर्शन में इसकी सर्वोच्च भूमिका का प्रतीक है।
- 10वें गुरु के बाद की भूमिका: गुरु गोबिंद सिंह (10 वें और अंतिम गुरु) के निधन के पश्चात् अकाल तख्त सिखों के लिये एक महत्त्वपूर्ण केंद्र बन गया।
- अशांत समय के दौरान, जैसे कि 18 वीं शताब्दी में सिखों पर अत्याचार के दौरान, अकाल तख्त सरबत खालसा (सिखों की आम सभा) के लिये महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने का केंद्र बन गया।
- महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने लगभग चार दशकों (1801-39) तक पंजाब पर शासन किया, ने वर्ष 1805 में अंतिम सरबत खालसा का आयोजन किया।
- अकाल तख्त जत्थेदार की भूमिका: अकाल तख्त के जत्थेदार (प्रमुख) को नैतिक और आध्यात्मिक जवाबदेही के लिये सिखों को बुलाने और विनम्रता एवं अनुशासन पैदा करने के लिये दंड (तन्खा) निर्धारित करने का अधिकार है, यह अधिकार केवल उन लोगों पर लागू होता है जो सिख के रूप में पहचान रखते हैं।
- जत्थेदार के लिये नैतिक रूप से ईमानदार होना, बपतिस्मा लेना और सिख ग्रंथों में शिक्षित होना ज़रूरी है। शुरुआत में सरबत खालसा द्वारा नियुक्त जत्थेदार की नियुक्ति ब्रिटिश प्रभाव के तहत दरबार साहिब समिति को सौंप दी गई। वर्ष 1925 के बाद, SGPC ने जत्थेदार की नियुक्ति की।
अन्य 4 सिख तख्त
- तख्त श्री केशगढ़ साहिब: हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की तलहटी में स्थित तख्त श्री केशगढ़ साहिब खालसा और गुरु गोबिंद सिंह से जुड़ा एक ऐतिहासिक स्थल है।
- तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब: बिहार के पटना में स्थित, यह गुरु गोबिंद सिंह का जन्मस्थान है।
- तखत सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब: महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित, यह वर्ष 1708 में गुरु गोबिंद सिंह के दाह संस्कार का स्थान है।
- तख्त श्री दमदमा साहिब: पंजाब के तलवंडी साबो में स्थित, यह वह स्थान है जहाँ गुरु गोबिंद सिंह ने सिख धर्मग्रंथ (गुरु ग्रंथ साहिब) को अंतिम रूप प्रदान किया था।
सिख धर्म के दस गुरु
|
गुरु नानक देव (1469-1539) |
|
|
गुरु अंगद (1504-1552) |
|
|
गुरु अमर दास (1479-1574) |
|
|
गुरु राम दास (1534-1581) |
|
|
गुरु अर्जुन देव (1563-1606) |
|
|
गुरु हरगोबिंद (1594-1644) |
|
|
गुरु हर राय (1630-1661) |
|
|
गुरु हरकिशन (1656-1664) |
|
|
गुरु तेग बहादुर (1621-1675) |
|
|
गुरु गोबिंद सिंह (1666-1708) |
|
अकाल तख्त, SGPC और शिरोमणि अकाली दल के बीच क्या संबंध है?
- सिख शासन में SGPC की भूमिका: वर्ष 1920 में गठित SGPC को सिख गुरुद्वारों का प्रबंधन और धार्मिक सिद्धांतों को बनाए रखने का कार्य सौंपा गया था। वर्ष 1925 के सिख गुरुद्वारा अधिनियम के तहत, इसे अकाल तख्त के जत्थेदार को नियुक्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ।
- SGPC पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में प्रमुख सिख तीर्थस्थलों के वित्त और प्रशासन को नियंत्रित करती है।
- शिरोमणि अकाली दल: गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के दौरान सिखों को संगठित करने के लिये प्रारंभ में SGPC की राजनीतिक शाखा के रूप में गठित शिरोमणि अकाली दल ने SGPC के साथ मिलकर कार्य किया।
- अंतर्संबंधित: SGPC पर नियंत्रण से शिरोमणि अकाली दल को अकाल तख्त पर नियुक्तियों और निर्णयों को प्रभावित करने की अनुमति मिलती है।
- आलोचकों का तर्क है कि यह संबंध अकाल तख्त की नैतिक सत्ता की स्वतंत्रता को कमज़ोर करता है, जिससे यह राजनीतिक हस्तक्षेप के प्रति संवेदनशील हो जाता है।
गुरुद्वारा सुधार आंदोलन
- गुरुद्वारा सुधार आंदोलन या अकाली आंदोलन वर्ष 1920 में अमृतसर, पंजाब में आरंभ हुआ, जिसका नेतृत्व सिखों ने किया, जिनका उद्देश्य ब्रिटिश नियंत्रण और गुरुद्वारों को चलाने वाले भ्रष्ट महंतों (पुजारियों) का विरोध करना था।
- इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश समर्थित महंतों से गुरुद्वारों को वापस लेना था, जिसके परिणामस्वरूप नवंबर,1920 में SGPC का गठन हुआ।
- अकाली आंदोलन औपनिवेशिक भारत में धार्मिक सुधार के बड़े आंदोलन का हिस्सा था।
- इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1925 का सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ, जिसने सिख समुदाय को अपने गुरुद्वारों पर कानूनी नियंत्रण प्रदान किया तथा महंतों का वंशानुगत नियंत्रण समाप्त कर दिया।
अकाल तख्त और SGPC के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?
- स्वायत्तता का क्षरण: अकाल तख्त के निर्णयों में राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों ने सिख समुदाय के भीतर इसकी नैतिक स्थिति को कमज़ोर कर दिया है।
- SGPC चुनावों में देरी से भाई-भतीजावाद और पारदर्शिता की कमी की धारणा को बढ़ावा मिला है।
- सिख नेतृत्व का विखंडन: SGPC के भीतर और सिख समुदाय के विभिन्न गुटों के बीच विवाद इन संस्थाओं की प्रभावशीलता एवं एकता को कमज़ोर करते हैं।
- विशेष रूप से प्रवासी सिखों की ओर से SGPC और अकाल तख्त के भीतर सुधार और लोकतंत्रीकरण की मांग ज़ोर पकड़ रही है।
- एक बदलते विश्व में प्रासंगिकता: अकाल तख्त को वैश्विक सिख समुदाय के भीतर अपने अधिकार को स्थापित करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसमें बढ़ती नशीली दवाओं की लत और बढ़ती आर्थिक असमानताओं जैसे सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना शामिल है, साथ ही न्याय, विनम्रता और एकता के अपने मूल सिद्धांतों को कायम रखना भी शामिल है।
आगे की राह
- जत्थेदारों की स्वतंत्र नियुक्ति: SGPC-नियंत्रित नियुक्तियों से व्यापक, समुदाय-संचालित प्रक्रिया में परिवर्तन जिसमें वैश्विक सिख प्रतिनिधित्व शामिल है।
- सामूहिक निर्णय लेने को सुनिश्चित करने और राजनीतिक संस्थाओं द्वारा एकतरफा कार्यवाही को न्यूनतम करने के लिये सरबत खालसा सभाओं की प्रथा को बहाल करना।
- SGPC का लोकतांत्रिक चुनाव: किसी भी राजनीतिक दल द्वारा सत्ता पर दीर्घकालिक एकाधिकार को रोकने के लिये समय पर और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना।
- शक्तियों का पृथक्करण: SGPC के प्रशासनिक कार्यों और अकाल तख्त की आध्यात्मिक और लौकिक अधिकारों के बीच स्पष्ट सीमाएँ स्थापित करना।
- सिख प्रवासियों के साथ सहभागिता: सिख शासन की समावेशिता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये वैश्विक सिख समुदाय के संसाधनों और दृष्टिकोणों का लाभ उठाना।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: सिख शासन में अकाल तख्त के महत्त्व और समुदाय को आकार देने में इसकी भूमिका की जाँच कीजिये और आधुनिक समय में इसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइये। |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिये: (2013)
इनमे से कौन उस समय उपदेश देता था/देते थे जब जब लोदी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारुढ़ हुआ? (a) 1 और 3 उत्तर: (b) |

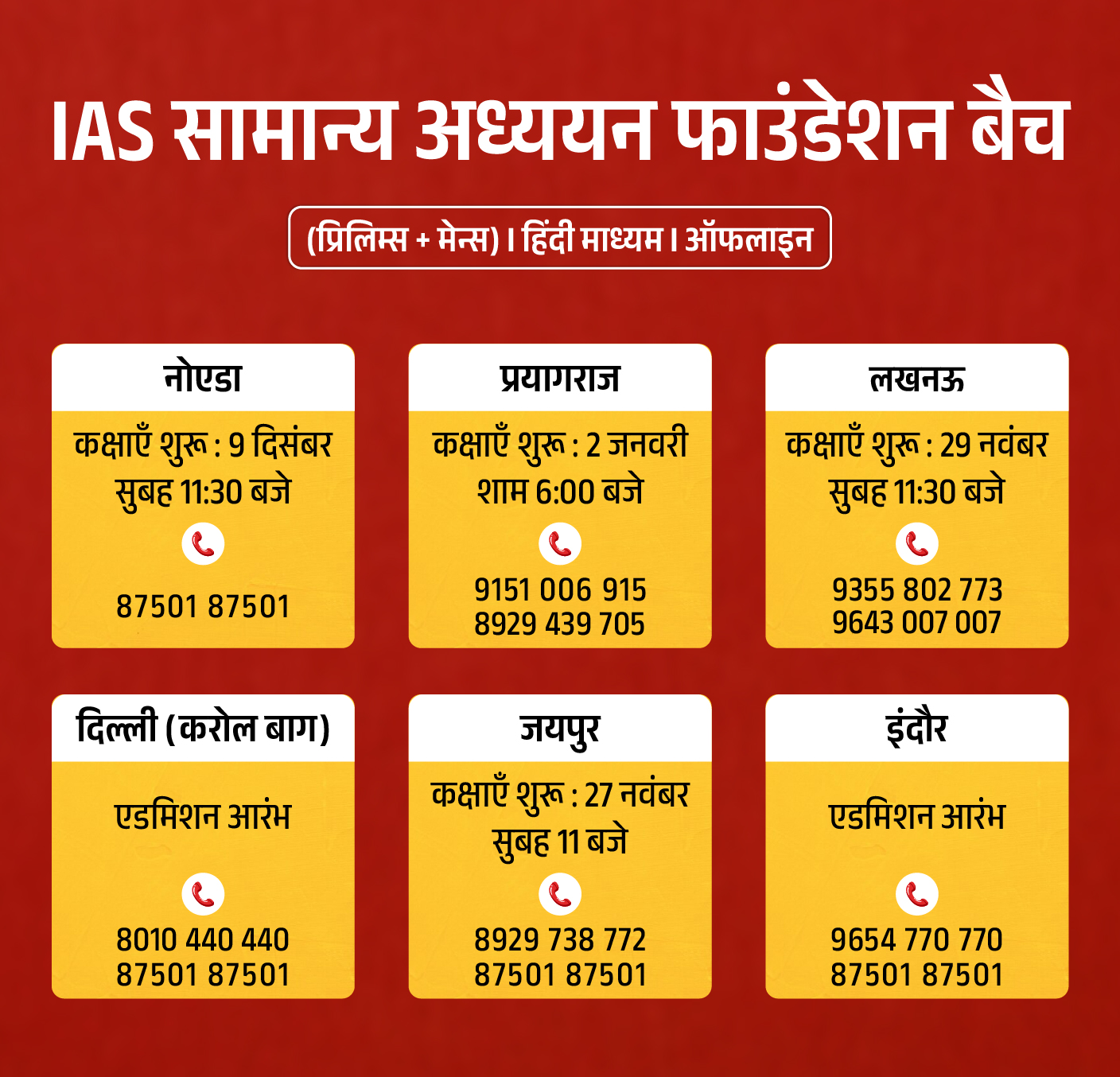
भारतीय इतिहास
डॉ. अंबेडकर का 69वाँ महापरिनिर्वाण दिवस
प्रिलिम्स के लिये:डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर, भारतीय संविधान, भगवान बौद्ध, सामाजिक समानता, सकारात्मक कार्रवाई, पूना समझौता, भारतीय वित्त आयोग, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बाँध, रोज़गार कार्यालय, प्रारूप समिति, विधि के समक्ष समानता, सर्वोच्च न्यायालय, नीति निदेशक सिद्धांत। मेन्स के लिये:कल्याणकारी राज्य, जाति-आधारित भेदभाव, सामाजिक न्याय में डॉ. अंबेडकर का योगदान, संविधान निर्माण और राष्ट्र निर्माण के प्रयास। |
स्रोत: पी.आई.बी
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और सामाजिक न्याय के अग्रदूत भारत रत्न डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 6 दिसंबर को 69वाँ महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया।
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस सामाजिक सुधार, न्याय और समानता पर उनके परिवर्तनकारी प्रभाव पर ज़ोर देते हुए उनकी विरासत का सम्मान करता है।
- "महापरिनिर्वाण" शब्द बौद्ध दर्शन से निकला है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है तथा बौद्ध कैलेंडर में सबसे पवित्र दिन है।
डॉ. अंबेडकर ने किस प्रकार सामाजिक न्याय का समर्थन किया?
- शोषितों के समर्थक: डॉ. अंबेडकर दलितों, महिलाओं और मज़दूरों के लिये आशा की किरण बनकर उभरे। उन्होंने जाति आधारित भेदभाव को मिटाने और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिये अपना जीवन समर्पित कर दिया।
- उनका समर्थन प्रणालीगत बाधाओं को समाप्त करने और हाशिये पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने तक फैला हुआ था।
- सशक्तीकरण पहल: डॉ. अंबेडकर ने हाशिये पर पड़े समूहों के उत्थान के लिये सकारात्मक कार्रवाई का समर्थन किया, ताकि हाशिये पर पड़े समूहों द्वारा सामना किये गए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिये शिक्षा, रोज़गार और राजनीति में आरक्षण जैसी नीतियों का प्रावधान किया जा सके।
- अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 334 के तहत आरक्षण शिक्षा, सार्वजनिक रोज़गार, विधायी निकायों और चुनावों में हाशिये के समूहों के लिये प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।
- शिक्षा को बढ़ावा देने, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने और बहिष्कृत समुदायों को सशक्त बनाने के लिये बहिष्कृत हितकारिणी सभा (1923) की स्थापना की।
- दलितों की आवाज़: दलितों को मंच प्रदान करने और सामाजिक असमानताओं को चुनौती देने के लिये मूकनायक (मूक नेता) समाचार पत्र की स्थापना की।
- अग्रणी आंदोलन: सार्वजनिक जल संसाधनों तक समान पहुँच का समर्थन करते हुए महाड़ सत्याग्रह (1927) सहित ऐतिहासिक आंदोलनों का नेतृत्व किया।
- वर्ष 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन (नासिक सत्याग्रह) का नेतृत्व किया, ताकि पूजा स्थलों पर जाति आधारित प्रतिबंधों को तोड़ा जा सके, जो अस्पृश्यता के खिलाफ एक व्यापक लड़ाई का प्रतीक है।
- पूना समझौता (1932): पूना समझौता पर बातचीत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने दलितों के लिये पृथक निर्वाचिका मंडलों के स्थान पर आरक्षित सीटें स्थापित कीं, जिससे उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त हुआ।
संविधान निर्माण में डॉ. अंबेडकर का क्या योगदान था?
- प्रारूप समिति के अध्यक्ष: वर्ष 1947 में नियुक्त प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, डॉ. अंबेडकर ने विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान को तैयार करने की सावधानीपूर्वक प्रक्रिया का निरीक्षण किया।
- विविध विचारों और चुनौतियों के बावजूद, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वर्ष 1949 में सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधानों के साथ संविधान को अपनाया जाए।
- मौलिक अधिकार: डॉ. अंबेडकर ने संविधान के भाग III का मसौदा तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो विधि के समक्ष समानता, भेदभाव के खिलाफ संरक्षण (अनुच्छेद 15, 17) और अल्पसंख्यकों के लिये सुरक्षा जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।
- शिक्षा और रोज़गार में आरक्षण के प्रावधान (अनुच्छेद 15[4], 16[4]) का उद्देश्य हाशिये पर पड़े समुदायों का उत्थान करना और समानता सुनिश्चित करना है, जो सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की रीढ़ है।
- अनुच्छेद 32: "संविधान की आत्मा" कहे जाने वाले अनुच्छेद 32 में नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार दिया गया है।
- उन्होंने संवैधानिक गारंटियों की रक्षा में इसकी केंद्रीय भूमिका पर बल दिया।
- संसदीय लोकतंत्र: उन्होंने सरकार के संसदीय स्वरूप की वकालत की, जिसके बारे में उनका मानना था कि इससे जवाबदेही, पारदर्शिता और सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है।
- इस प्रणाली को समतावादी सिद्धांतों को बनाए रखने और राष्ट्र की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये डिज़ाइन किया गया था।
- संघीय संरचना: इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को संतुलित करते हुए दोहरी राजनीति की संकल्पना की गई।
- यह ढाँचा भारत की अद्वितीय सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता के अनुकूल बनाया गया था, जिससे एकता और लचीलापन दोनों सुनिश्चित हो सके।
- राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत: निदेशक सिद्धांतों को कल्याणकारी राज्य बनाने, सामाजिक सुरक्षा, लैंगिक समानता और बेहतर जीवन स्तर जैसे लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में देखा गया ।
- यद्यपि ये सिद्धांत न्यायोचित नहीं हैं, फिर भी ये भारत में नीति-निर्माण का अभिन्न अंग बने हुए हैं।
राष्ट्र निर्माण में डॉ. अंबेडकर का क्या योगदान था?
- आर्थिक ढाँचा: डॉ. अंबेडकर के शैक्षणिक योगदान ने कई आर्थिक संस्थाओं की नींव रखी।
- उनकी डॉक्टरेट थीसिस ने भारत के वित्त आयोग के निर्माण और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 के नीति ढाँचे को प्रभावित किया ।
- अवसंरचना विजन: दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बाँध और सोन नदी परियोजना जैसी बड़े पैमाने की अवसंरचना परियोजनाओं की परिकल्पना की गई और उन्हें बढ़ावा दिया गया, ताकि स्थायी संसाधन प्रबंधन और राष्ट्रीय विकास सुनिश्चित हो सके।
- राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड प्रणाली की संकल्पना की, ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास में दूरदर्शिता का प्रदर्शन किया।
- रोज़गार सुधार: देश भर में व्यवस्थित रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये नौकरी नियुक्ति प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने हेतु रोज़गार कार्यालयों की स्थापना की गई।
- सामाजिक और आर्थिक न्याय: समावेशी नीतियों के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को पाटने की वकालत की और हाशिये पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने के लिये शासन संरचनाओं में सामाजिक न्याय को एकीकृत करने का समर्थन किया।
डॉ. बी.आर. अंबेडकर को सरकार की श्रद्धांजलि
- भारत रत्न पुरस्कार: डॉ. अंबेडकर को वर्ष 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित किया।
- अंबेडकर सर्किट: अंबेडकर के जीवन से संबंधित पाँच स्थानों को तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया गया (पंचतीर्थ विकास):
- जन्मस्थान महू
- लंदन में स्मारक (शिक्षा भूमि)
- नागपुर में दीक्षा भूमि
- मुंबई में चैत्य भूमि
- दिल्ली में महापरिनिर्वाण भूमि
- भीम ऐप: डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिये इनके सम्मान में एक डिजिटल भुगतान ऐप लॉन्च किया गया, जो वित्तीय समावेशन और सशक्तीकरण का प्रतीक है।
- डॉ. अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र (DACE): 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरंभ किये गए ये केंद्र अनुसूचित जाति के छात्रों को सिविल सेवा परीक्षाओं के लिये मुफ्त कोचिंग प्रदान करते हैं।
- अंबेडकर सामाजिक नवप्रवर्तन और उद्भवन मिशन (ASIIM): अनुसूचित जाति के युवाओं को स्टार्टअप विचारों के लिये वित्तपोषण द्वारा सहायता प्रदान करता है।
- स्मारक टिकट और सिक्के: डॉ. अंबेडकर की विरासत को सम्मानित करने के लिये 10 रुपए और 125 रुपए मूल्यवर्ग के सिक्के और एक स्मारक डाक टिकट जारी किये गए।
- राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक: संकल्प भूमि बरगद परिसर (वडोदरा) और सतारा में अंबेडकर स्कूल जैसे स्थलों को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में प्रस्तावित किया गया।
- संविधान दिवस समारोह: वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में अंबेडकर की भूमिका को याद दिलाता है।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: डॉ. अंबेडकर ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढाँचे, सामाजिक न्याय और भारतीय संविधान को आकार देने में अपनी भूमिका के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में कैसे योगदान दिया? |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस दल की स्थापित की थी? (2012)
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. अपसारी उपागमों और रणनीतियों के होने के बावज़ूद महात्मा गांधी और डॉ. बी.आर. अंबेडकर का दलितों की बेहतरी का एकसमान लक्ष्य था। स्पष्ट कीजिये।(2015) |