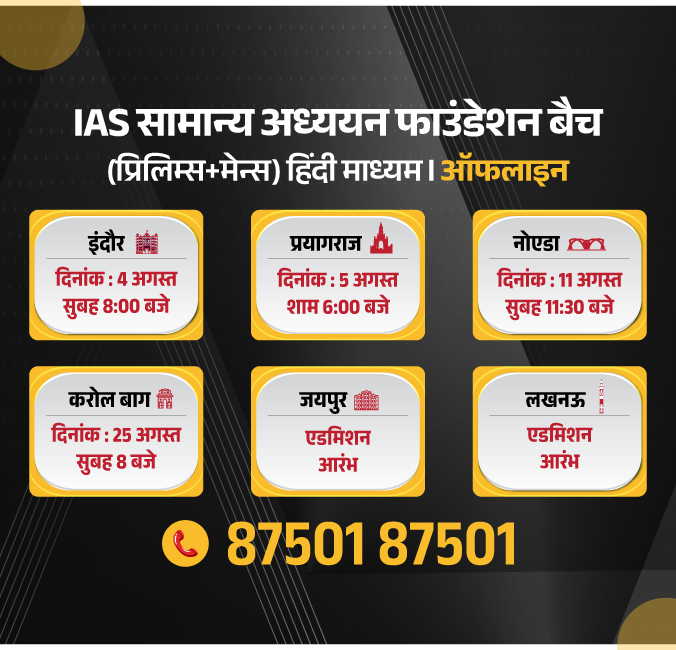बिहार Switch to English
सतीश प्रसाद सिंह: बिहार के सबसे अल्पकालिक मुख्यमंत्री
चर्चा में क्यों?
जैसे-जैसे बिहार 2025 के विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रहा है, राज्य के राजनीतिक इतिहास पर पुनः चर्चा हो रही है, विशेष रूप से इसके प्रमुख नेताओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- इन्हीं में से एक सतीश प्रसाद सिंह, जो बिहार के छठवें मुख्यमंत्री थे, अपने सबसे कम कार्यकाल के लिये प्रसिद्ध हैं। उन्होंने केवल 4 दिन तक मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाला था।
मुख्य बिंदु
- मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल:
- सतीश प्रसाद सिंह ने मात्र चार दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर कार्य कर इतिहास रच दिया। उन्होंने 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक यह पद संभाला।
- उनका कार्यकाल राजनीतिक अस्थिरता से चिह्नित रहा और उन्हें बी.पी. मंडल के उदय से पूर्व अंतरिम मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था।
- राजनीतिक शुरुआत:
- खगड़िया में जन्मे सतीश प्रसाद सिंह कम उम्र से ही समाजवादी विचारधाराओं से अत्यधिक प्रभावित थे।
- उनका राजनीतिक जीवन सामाजिक न्याय और किसानों के हितों के प्रति समर्पण से प्रेरित रहा।
सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री
- नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। वर्ष 2025 तक उनका कुल कार्यकाल 18 वर्ष से अधिक का हो चुका है।
- उन्होंने श्रीकृष्ण सिंह का पूर्व रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 17 वर्ष एवं 52 दिन तक मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया था।
- सबसे लंबा निरंतर कार्यकाल:
- इस श्रेणी में रिकॉर्ड अब भी श्रीकृष्ण सिंह के नाम है, जिन्होंने लगातार 14 वर्ष एवं 314 दिन तक मुख्यमंत्री पद पर सेवा दी।
- नीतीश कुमार का सबसे लंबा सतत् कार्यकाल 8 वर्ष एवं 239 दिन (2005–2014; बीच में जीतन राम माँझी द्वारा संक्षिप्त कार्यकाल) रहा है।
- अधिकतम शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री:
- नीतीश कुमार ने अब तक बिहार के मुख्यमंत्री पद की 9 बार शपथ ली है, जो किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया सर्वाधिक शपथ ग्रहण है।
- राष्ट्रपति शासन
- बिहार में राज्य के गठन के बाद से अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है।
- कुल मिलाकर राज्य में अब तक 37 कार्यकाल हो चुके हैं, जिनमें ये 8 राष्ट्रपति शासन अवधि शामिल हैं।
नोट:
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में प्रांतीय सरकारों के प्रमुखों को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री या प्रीमियर कहा जाता था।
- मोहम्मद युनुस (1 अप्रैल 1937 – 19 जुलाई 1937) बिहार प्रांत के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 109 दिन तक मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के तहत यह पद संभाला।
- उल्लेखनीय है कि वे पूरे ब्रिटिश भारत में इस पद की शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति थे।
बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची (1947-2025)
|
क्र. सं. |
नाम |
कार्यकाल |
राजनीतिक दल/गठबंधन |
|
1 |
श्री कृष्ण सिन्हा |
15 अगस्त 1947– 31 जनवरी 1961 |
भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |
|
2 |
दीप नारायण सिंह |
1 फरवरी 1961 – 18 फरवरी 1961 |
भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |
|
3 |
बिनोदानंद झा |
18 फरवरी 1961 – 2 अक्तूबर 1963 |
भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |
|
4 |
कृष्ण बल्लभ सहाय |
2 अक्तूबर 1963 – 5 मार्च 1967 |
भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |
|
5 |
महामाया प्रसाद सिन्हा |
5 मार्च 1967 – 28 जनवरी 1968 |
जन क्रांति दल |
|
6 |
सतीश प्रसाद सिंह |
28 जनवरी 1968 – 1 फरवरी 1968 |
शोषित दल |
|
7 |
बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल (बीपी मंडल) |
1 फरवरी 1968 – 22 मार्च 1968 |
शोषित दल |
|
— |
राष्ट्रपति शासन |
29 जून 1968 – 26 फरवरी 1969 |
— |
|
8 |
हरिहर सिंह |
26 फरवरी 1969 – 22 जून 1969 |
भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |
|
9 |
भोला पासवान शास्त्री |
22 जून 1969 – 4 जुलाई 1969 |
भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |
|
— |
राष्ट्रपति शासन |
4 जुलाई 1969 – 16 फरवरी 1970 |
— |
|
10 |
दरोगा प्रसाद राय |
16 फरवरी 1970 – 22 दिसंबर 1970 |
भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |
|
11 |
कर्पूरी ठाकुर |
22 दिसंबर 1970 – 2 जून 1971 |
संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी |
|
12 |
भोला पासवान शास्त्री |
2 जून 1971 – 9 जनवरी 1972 |
भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |
|
— |
राष्ट्रपति शासन |
9 जनवरी 1972 – 19 मार्च 1972 |
— |
|
13 |
केदार पांडे |
19 मार्च 1972 – 2 जुलाई 1973 |
भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |
|
14 |
अब्दुल गफूर |
2 जुलाई 1973 – 11 अप्रैल 1975 |
भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |
|
15 |
जगन्नाथ मिश्रा |
11 अप्रैल 1975 – 30 अप्रैल 1977 |
भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |
|
— |
राष्ट्रपति शासन |
30 अप्रैल 1977 – 24 जून 1977 |
— |
|
16 |
कर्पूरी ठाकुर |
24 जून 1977 – 21 अप्रैल 1979 |
जनता पार्टी |
|
17 |
राम सुंदर दास |
21 अप्रैल 1979 – 17 फरवरी 1980 |
जनता पार्टी (सेक्युलर) |
|
— |
राष्ट्रपति शासन |
17 फरवरी 1980 – 8 जून 1980 |
— |
|
18 |
जगन्नाथ मिश्रा |
8 जून 1980 – 14 अगस्त 1983 |
भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |
|
19 |
चंद्रशेखर सिंह |
14 अगस्त 1983 – 12 मार्च 1985 |
भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |
|
20 |
बिंदेश्वरी दुबे |
12 मार्च 1985 – 13 फरवरी 1988 |
भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |
|
21 |
भागवत झा आज़ाद |
14 फरवरी 1988 – 10 मार्च 1989 |
भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |
|
22 |
सत्येंद्र नारायण सिन्हा |
11 मार्च 1989 – 6 दिसंबर 1989 |
भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |
|
23 |
जगन्नाथ मिश्रा |
6 दिसंबर 1989 – 10 मार्च 1990 |
भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस |
|
24 |
लालू प्रसाद यादव |
10 मार्च 1990 – 28 मार्च 1995 |
जनता दल |
|
— |
राष्ट्रपति शासन |
28 मार्च 1995 – 5 अप्रैल 1995 |
— |
|
25 |
लालू प्रसाद यादव |
5 अप्रैल 1995 – 25 जुलाई 1997 |
जनता दल/राष्ट्रीय जनता दल |
|
26 |
राबड़ी देवी |
25 जुलाई 1997 – 11 फरवरी 1999 |
राष्ट्रीय जनता दल |
|
— |
राष्ट्रपति शासन |
11 फरवरी 1999 – 9 मार्च 1999 |
— |
|
27 |
राबड़ी देवी |
9 मार्च 1999 – 2 मार्च 2000 |
राष्ट्रीय जनता दल |
|
28 |
नीतीश कुमार |
3 मार्च 2000 – 10 मार्च 2000 |
समता पार्टी |
|
29 |
राबड़ी देवी |
11 मार्च 2000 – 6 मार्च 2005 |
राष्ट्रीय जनता दल |
|
— |
राष्ट्रपति शासन |
7 मार्च 2005 – 24 नवंबर 2005 |
— |
|
30 |
नीतीश कुमार |
24 नवंबर 2005 – 17 मई 2014 |
जनता दल (यूनाइटेड) |
|
31 |
जीतन राम मांझी |
20 मई 2014 – 22 फरवरी 2015 |
जनता दल (यूनाइटेड) |
|
32 |
नीतीश कुमार |
22 फरवरी 2015 – 20 नवंबर 2015 |
जनता दल (यूनाइटेड) |
|
33 |
नीतीश कुमार |
20 नवंबर 2015 – 26 जुलाई 2017 |
जनता दल (यूनाइटेड)-महागठबंधन |
|
34 |
नीतीश कुमार |
27 जुलाई 2017 – 16 नवंबर 2020 |
जनता दल (यूनाइटेड) - NDA |
|
35 |
नीतीश कुमार |
16 नवंबर 2020 – 9 अगस्त 2022 |
जनता दल (यूनाइटेड) - NDA |
|
36 |
नीतीश कुमार |
10 अगस्त 2022 – 28 जनवरी 2024 |
जनता दल (यूनाइटेड)-महागठबंधन |
|
37 |
नीतीश कुमार |
28 जनवरी 2024 – वर्तमान |
जनता दल (यूनाइटेड) - NDA |


बिहार Switch to English
पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त
चर्चा में क्यों?
बिहार के राज्यपाल ने न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली को पटना के राजभवन में पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई।
- उन्होंने न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन का स्थान लिया, जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था। इससे पहले, न्यायमूर्ति विपुल पंचोली ने गुजरात उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में तथा गुजरात उच्च न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय दोनों में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था।
मुख्य बिंदु
पटना उच्च न्यायालय के बारे में
- निर्माण:
- पटना उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1912 में भारत के गवर्नर-जनरल द्वारा जारी एक घोषणा के तहत की गई थी, जिसने बिहार और उड़ीसा को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया।
- इस उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला 1 दिसंबर 1913 को भारत के वायसराय और गवर्नर-जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वारा रखी गई थी।
- इस उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैंप्स चैमियर थे, जिन्होंने मार्च 1916 से अक्तूबर 1917 तक कार्य किया।
- स्वतंत्रता के बाद:
- वर्ष 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद, पटना उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया, जिससे उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की अनुमति मिल गई।
- स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर क्लिफोर्ड मोनमोहन अग्रवाल थे, जिन्होंने जनवरी 1948 से जनवरी 1950 तक कार्य किया।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संरचना और नियुक्ति
- संरचना:
- प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य न्यायाधीश होते हैं।
- राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के कार्यभार के आधार पर उसके सदस्यों की संख्या निर्धारित करते हैं।
- नियुक्ति:
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है।
- न्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है।
- दो या अधिक राज्यों के लिये एक ही उच्च न्यायालय होने की स्थिति में, राष्ट्रपति द्वारा सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों से परामर्श किया जाता है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ उस राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है।
- योग्यताएँ:
-
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिये:
- वह भारत का नागरिक होना चाहिये।
- उसे भारत के क्षेत्र में दस वर्षों तक न्यायिक पद पर कार्य करना चाहिये, या
- उसे दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय (या लगातार उच्च न्यायालयों) में अधिवक्ता होना चाहिये।
-
- न्यूनतम आयु:
- संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है।
- न्यायाधीशों का कार्यकाल:
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रह सकते हैं।
भारत में उच्च न्यायालय
- स्थिति:
- भारत की न्यायिक प्रणाली में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से नीचे तथा अधीनस्थ न्यायालयों से ऊपर कार्य करता है।
- उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। (भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं)।
- संवैधानिक प्रावधान:
- प्रत्येक राज्य के लिये उच्च न्यायालय:
- भारत का संविधान, प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है (अनुच्छेद 214)।
- संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान:
- अनुच्छेद 231 में प्रावधान है कि संसद, कानून द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिये अथवा दो या अधिक राज्यों और एक केंद्रशासित क्षेत्र के लिये एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है।
- क्षेत्राधिकार:
- प्रादेशिक क्षेत्राधिकार राज्य के क्षेत्राधिकार के साथ सह-समाप्त होता है (या एक सामान्य उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संबंधित राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार के साथ सह-समाप्त होता है)।
- अनुच्छेद 214 से 231:
- ये अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।
- प्रत्येक राज्य के लिये उच्च न्यायालय:



.gif)
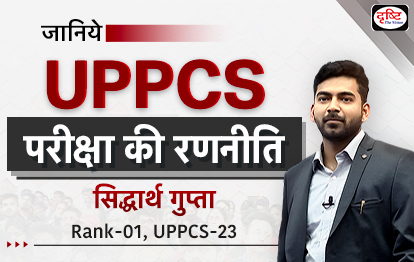
%20(1).gif)
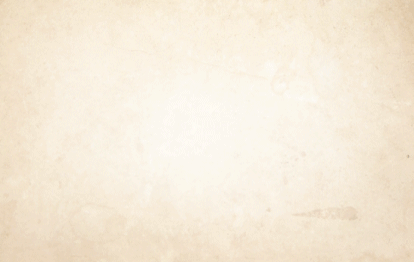


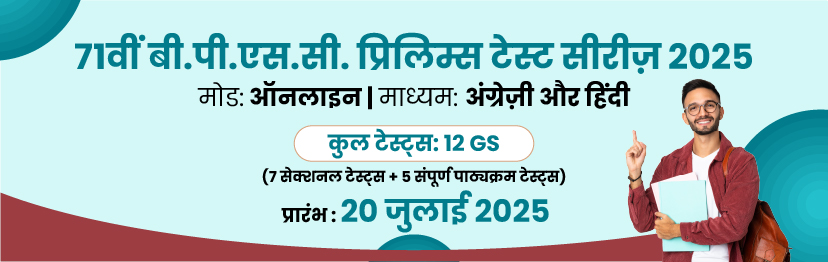
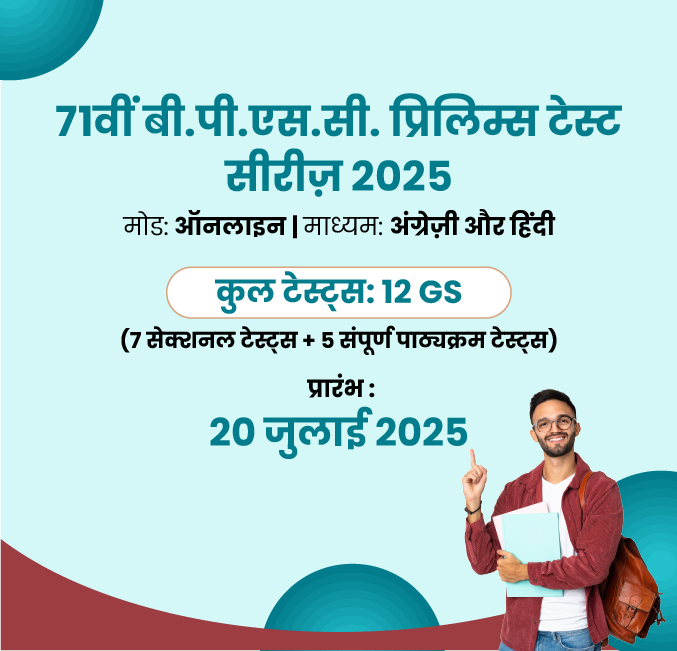


-UPPCS-Hindi%20(web).png)
-UPPCS-Hindi(mobile).png)
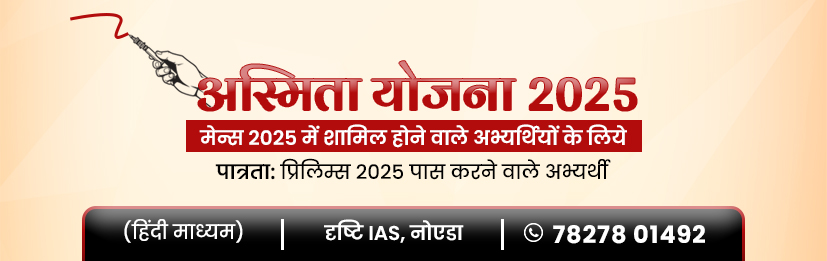

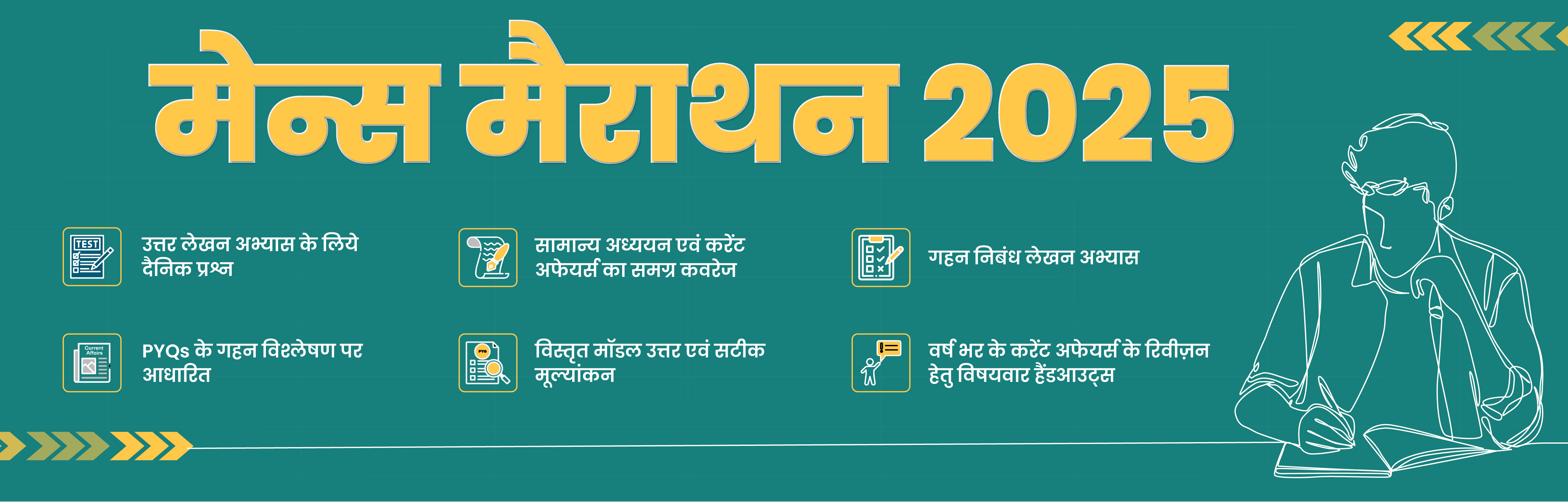
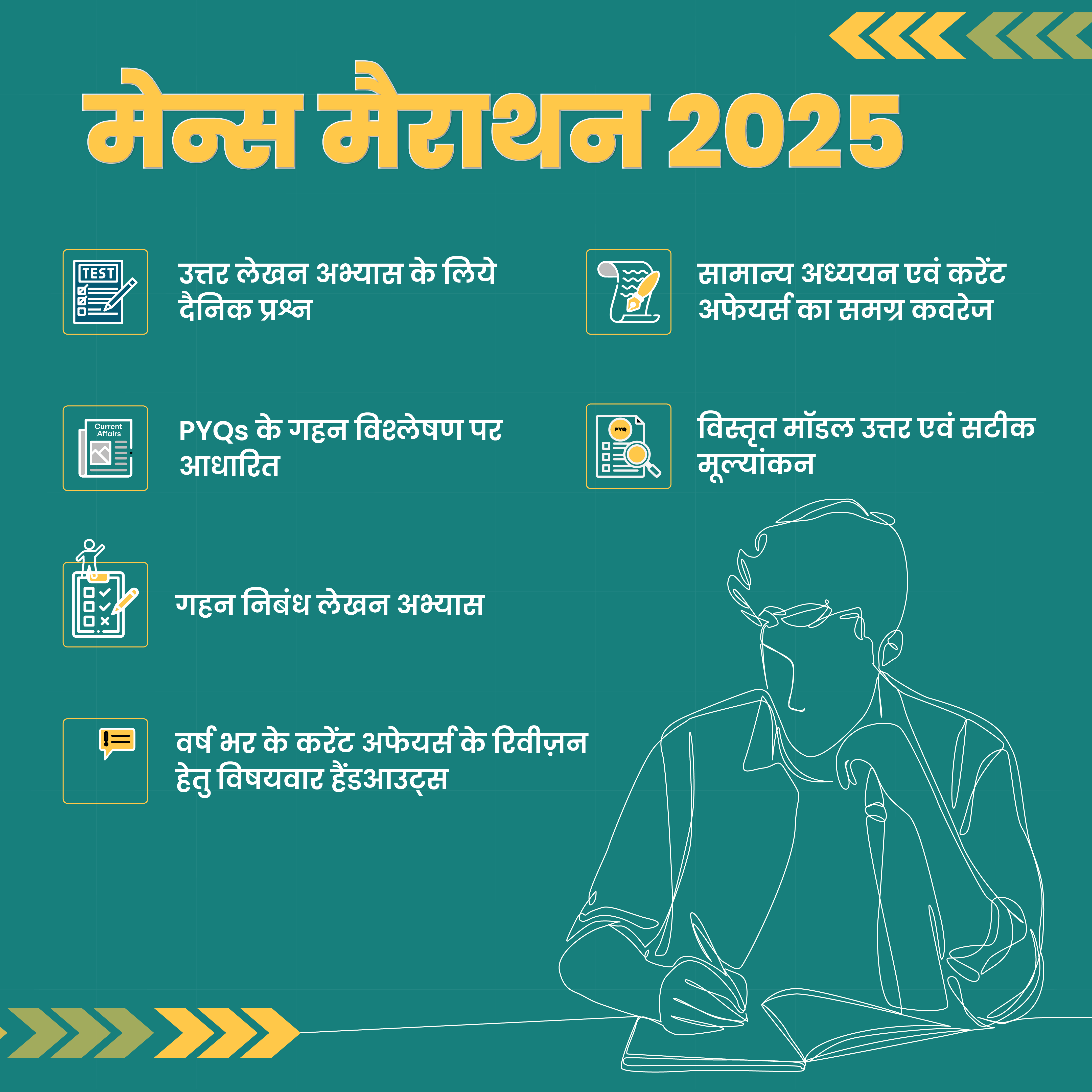
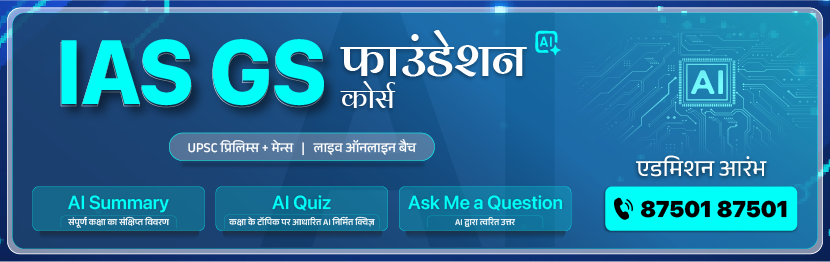
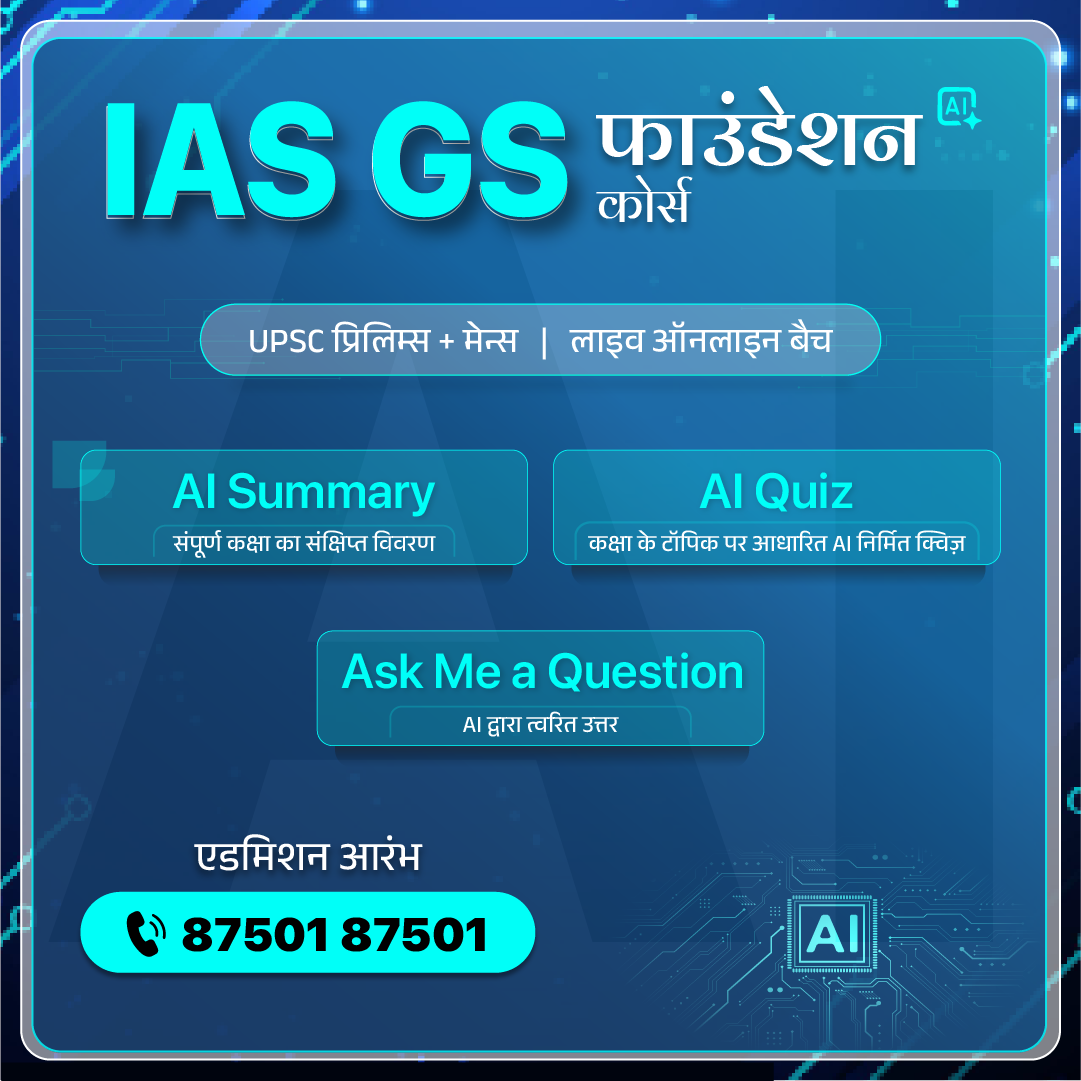

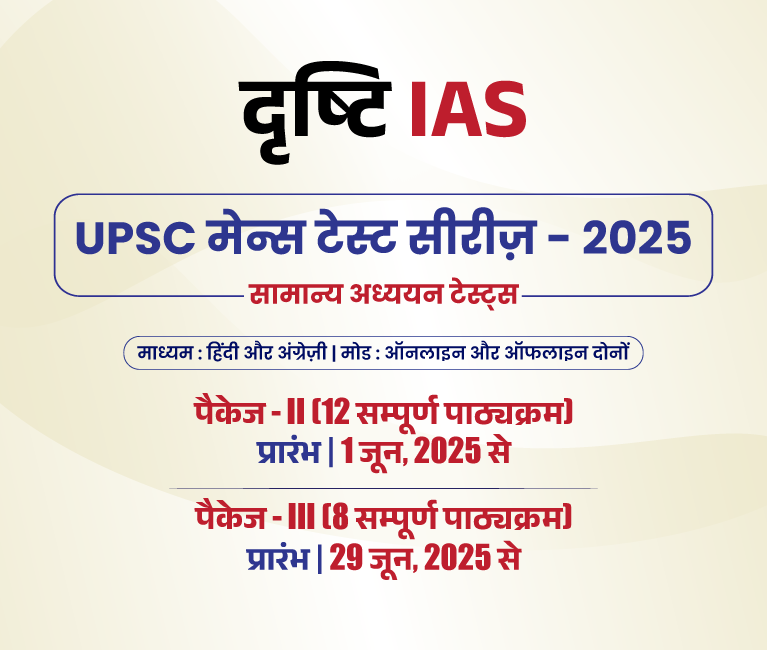
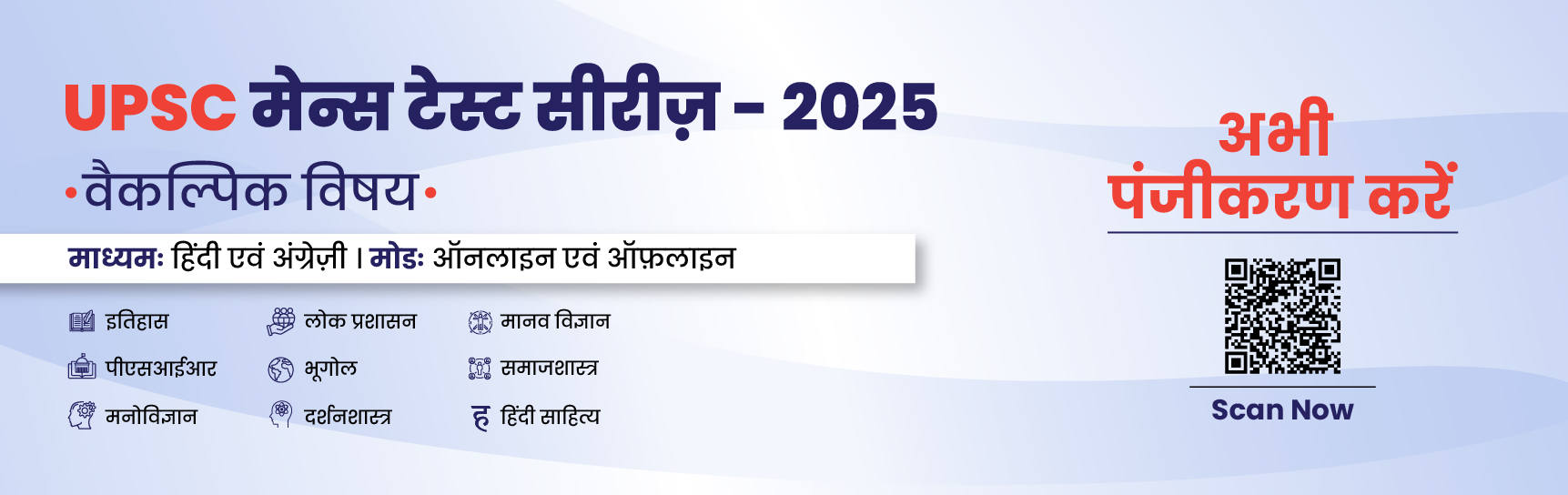
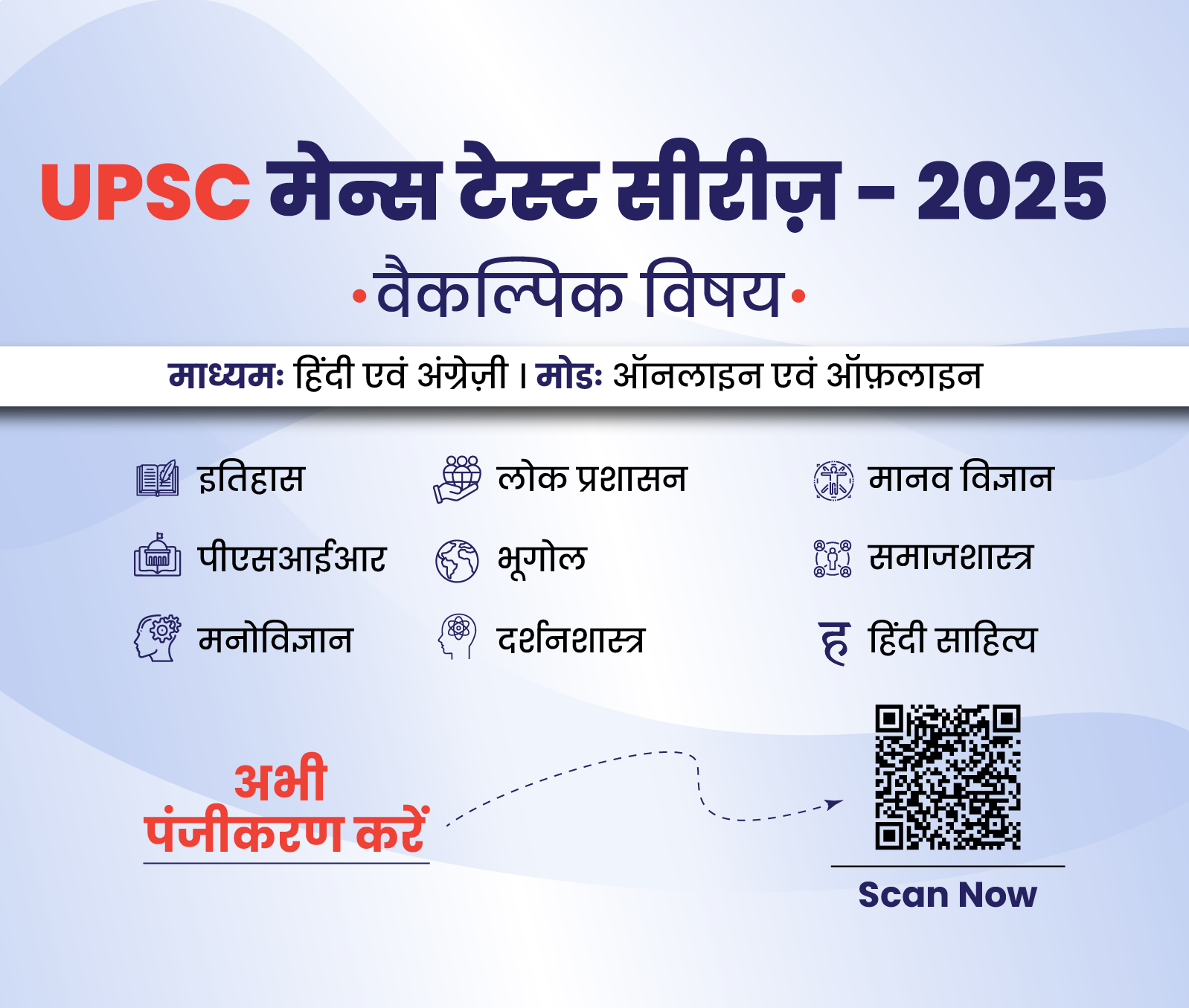
.png)