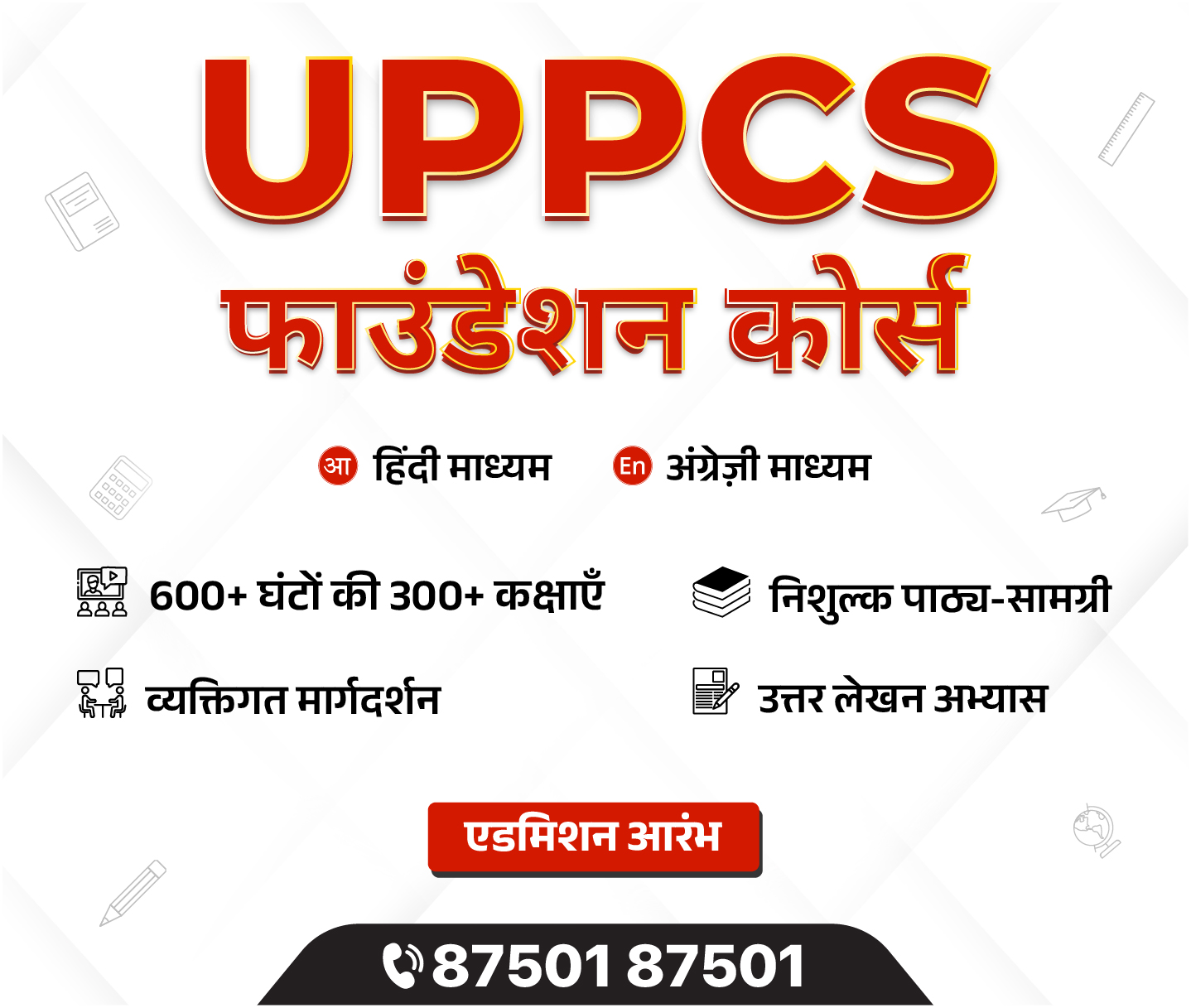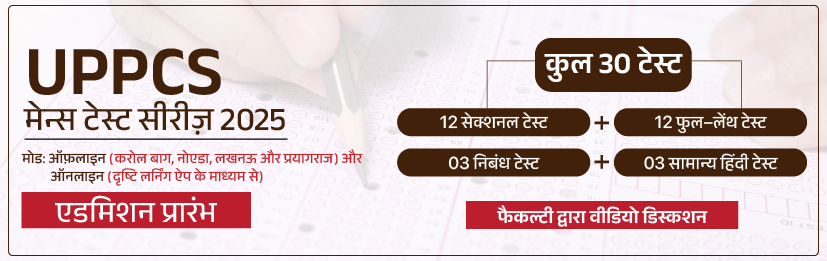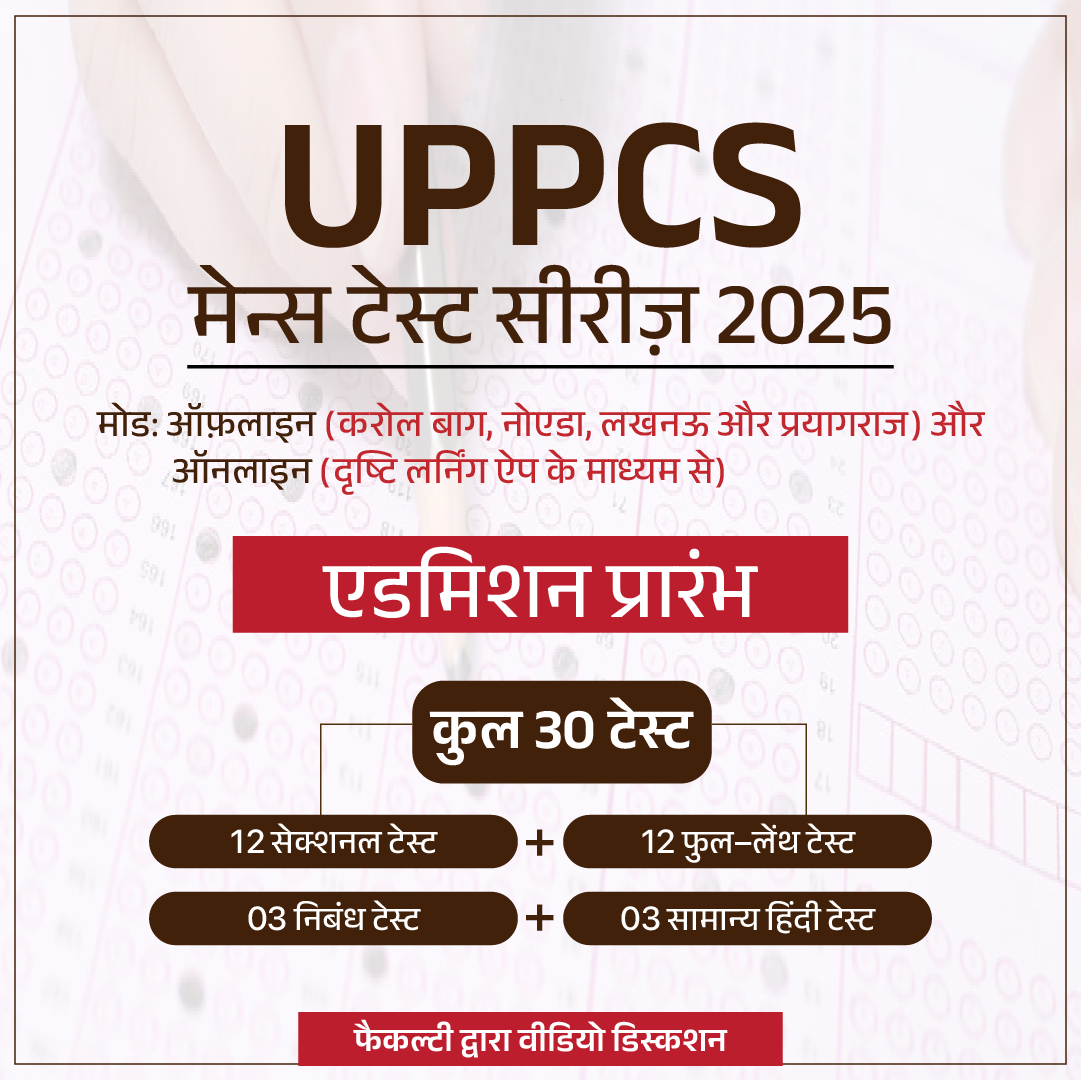राजस्थान Switch to English
विकसित राजस्थान @2047 विज़न डॉक्यूमेंट का अनावरण किया
चर्चा में क्यों?
राजस्थान सरकार ने जयपुर में विकसित राजस्थान @2047 विज़न डॉक्यूमेंट का अनावरण किया।
मुख्य बिंदु
- परिचय: अगस्त, 2025 में राज्य मंत्रि परिषद द्वारा स्वीकृत, यह विज़न डॉक्यूमेंट राजस्थान को वर्ष 2047 तक एक विकसित राज्य में बदलने के लिये एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करता है, जो राष्ट्रीय लक्ष्य विकसित भारत @2047 के अनुरूप है।
- यह समावेशी और सतत् विकास पर ज़ोर देता है, जिसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों तथा वंचित वर्ग को प्राथमिकता प्रदान की गई है।
- लक्ष्य 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, जिसमें कृषि, उद्योग, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास के मुख्य स्तंभ होंगे।
- थीम्स और फोकस क्षेत्र: विज़न डॉक्यूमेंट चार प्रमुख थीमों के चारों ओर संरचित है, जो तेरह महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करती हैं:
- सार्वजनिक कल्याण और सामाजिक सशक्तीकरण: कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित, ताकि मानव विकास को बढ़ावा दिया जा सके तथा सामाजिक समानता सुनिश्चित हो।
- तीव्र विकास, समृद्धि और रोज़गार: उद्योग, खनन, पर्यटन और सांस्कृतिक विकास पर ज़ोर, ताकि व्यापक स्तर पर रोज़गार सृजित किया जा सके तथा समावेशी समृद्धि सुनिश्चित हो।
- बुनियादी ढाँचा और सतत् विकास: जल सुरक्षा, पर्यावरणीय सततता और जलवायु लचीलापन को प्राथमिकता, ताकि पर्यावरण-मैत्रीपूर्ण तथा जलवायु-सहनीयता (Climate Resilience) बुनियादी ढाँचे का प्रारूप तैयार किया जा सके।
- नीति, वित्त और प्रशासन: ग्रामीण-शहरी विकास, वित्तीय प्रबंधन और सुशासन को एकीकृत करना, ताकि संस्थागत क्षमता, पारदर्शिता एवं प्रशासनिक दक्षता को प्रबल किया जा सके।
- कार्यान्वयन ढाँचा:
- विभागीय कार्य योजनाएँ: प्रत्येक विभाग विज़न लक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट योजनाएँ तैयार करेगा।
- वार्षिक मूल्यांकन: परिणामों को ट्रैक करने के लिये वित्तीय और प्रदर्शन समीक्षा की जाएगी।
- निरंतर निगरानी: जवाबदेही और समय पर सुधार सुनिश्चित करने के लिये मूल्यांकन ढाँचे अपनाए जाएंगे।
- महत्त्वपूर्ण वर्ष: वर्ष 2030, 2035 और 2040 के लक्ष्य अनुसार प्रगति के मानक निर्धारित किये गए हैं।
वर्ष 2047 तक प्रमुख लक्ष्य |
|
|
क्षेत्र |
लक्ष्य |
|
निर्माण उद्योग |
सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन (GSVA) में हिस्सा 20% तक बढ़ाना |
|
स्वास्थ्य |
जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष तक बढ़ाना |
|
बाल स्वास्थ्य |
शिशु मृत्यु दर को 1,000 जीवित जन्मों पर 10 से कम करना |
|
शिक्षा |
100% स्कूल नामांकन प्राप्त करना; सभी स्कूलों को स्मार्ट और कंप्यूटर-सक्षम संस्थानों में उन्नत करना |
|
महिला सशक्तीकरण |
महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को 60% से अधिक बढ़ाना |
|
पर्यटन |
घरेलू पर्यटकों में राजस्थान का हिस्सा 15% तक बढ़ाना |
राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स Switch to English
नीरज चोपड़ा को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की गई
चर्चा में क्यों?
दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को राष्ट्र के प्रति उनके उत्कृष्ट योगदान और उपलब्धियों के सम्मान में प्रादेशिक सेना (Territorial Army) में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की गई है।
- पिपिंग समारोह नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में आयोजित किया गया, जहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी की उपस्थिति में औपचारिक रूप से यह रैंक प्रतीक/चिह्न (Rank Insignia) प्रदान किया।
मुख्य बिंदु
- परिचय: 24 दिसंबर, 1997 को हरियाणा के पानीपत ज़िले के खंडरा गाँव में जन्मे नीरज चोपड़ा एक कृषक परिवार से संबंध रखते हैं और भारत के सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में से एक बन चुके हैं।
- भारतीय सेना में यात्रा:
- नीरज चोपड़ा अगस्त, 2016 में भारतीय सेना में राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में नायब सूबेदार (Naib Subedar) के रूप में शामिल हुए थे तथा वर्ष 2021 में उन्हें एथलेटिक्स में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिये सूबेदार (Subedar) के पद पर पदोन्नत किया गया।
- वर्ष 2022 में, ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें सूबेदार मेजर (Subedar Major) पद पर पदोन्नत किया गया और भारतीय सेना के सर्वोच्च शांतिकालीन सम्मान ‘परम विशिष्ट सेवा पदक’ से सम्मानित किया गया।
- अप्रैल, 2025 में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रसेवा और उत्कृष्ट खेल उपलब्धियों की मान्यता में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल (Honorary Lieutenant Colonel) की उपाधि प्रदान की।
- खेल में प्राप्त उपलब्धियाँ:
- टोक्यो ओलंपिक 2020: ट्रैक एंड फील्ड में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रचा।
- विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023: स्वर्ण पदक जीता, जिससे वैश्विक एथलेटिक्स में भारत की उपस्थिति और दृढ़ हुई।
- पेरिस ओलंपिक 2024: रजत पदक प्राप्त किया, जिससे उनका निरंतर उच्च प्रदर्शन स्तर बना रहा।
- एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल: कई स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाला फेंक स्पर्द्धा में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की।
- डायमंड लीग एवं अन्य प्रतियोगिताएँ: लगातार शीर्ष स्थान प्राप्त किया तथा वर्ष 2025 में 90.23 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो (Personal Best Throw) कर भारतीय एथलेटिक्स में एक नया रिकॉर्ड बनाया।
- पुरस्कार एवं सम्मान:
- विशिष्ट सेवा पदक (2023)
- परम विशिष्ट सेवा पदक (2022)
- पद्मश्री (2022)
- मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार (2021)
- अर्जुन पुरस्कार (2018)
राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स Switch to English
पिंकी आनंद को बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया
चर्चा में क्यों?
डॉ. पिंकी आनंद, वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, को बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय (BICC) में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि वर्ष 2024 में पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय किशन कौल की उसी न्यायालय में नियुक्ति के बाद हुआ है।
डॉ. पिंकी आनंद
- पृष्ठभूमि: हार्वर्ड लॉ स्कूल की स्नातक और इन्लैक्स स्कॉलर, डॉ. पिंकी आनंद के पास 40 वर्षों से अधिक का विधिक अनुभव है। उन्होंने भारत में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (2014-2020) के रूप में कार्य किया और उन्हें संवैधानिक कानून, सिविल मध्यस्थता तथा आपराधिक कानून में विशेषज्ञता प्राप्त है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व: उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किया है, जिनमें ब्रिक्स (BRICS) शामिल हैं; ब्रिक्स लीगल फोरम की संस्थापक सदस्य भी हैं।
- सम्मान: उन्हें फ्राँस के राष्ट्रपति द्वारा फ्रेंच नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया।
बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय (BICC)
- बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय (Bahrain International Commercial Court- BICC) की स्थापना जटिल सीमा पार वाणिज्यिक विवादों को निपटाने के लिये की गई है। यह न्यायालय 5 नवंबर, 2025 को न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण समारोह के साथ अपना कार्य आरंभ करेगा, जिसमें बहरीन के राजपरिवार और प्रधानमंत्री की उपस्थिति होगी।
- BICC की अध्यक्षता प्रसिद्ध मध्यस्थता विशेषज्ञ जान पॉल्सन कर रहे हैं और इसमें 17 न्यायाधीश शामिल हैं- जिनमें 7 महिलाएँ एवं 10 पुरुष हैं, जो विश्व के विभिन्न न्यायिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- यह न्यायालय मार्च, 2024 में बहरीन और सिंगापुर के बीच हुई एक संधि के तहत स्थापित किया गया है तथा इसका ढाँचा सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय (Singapore International Commercial Court- SICC) के मॉडल पर आधारित है ताकि वाणिज्यिक विवाद समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जा सके।


%20(1).gif)
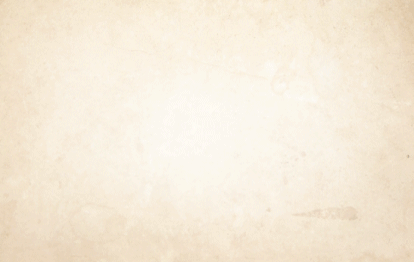

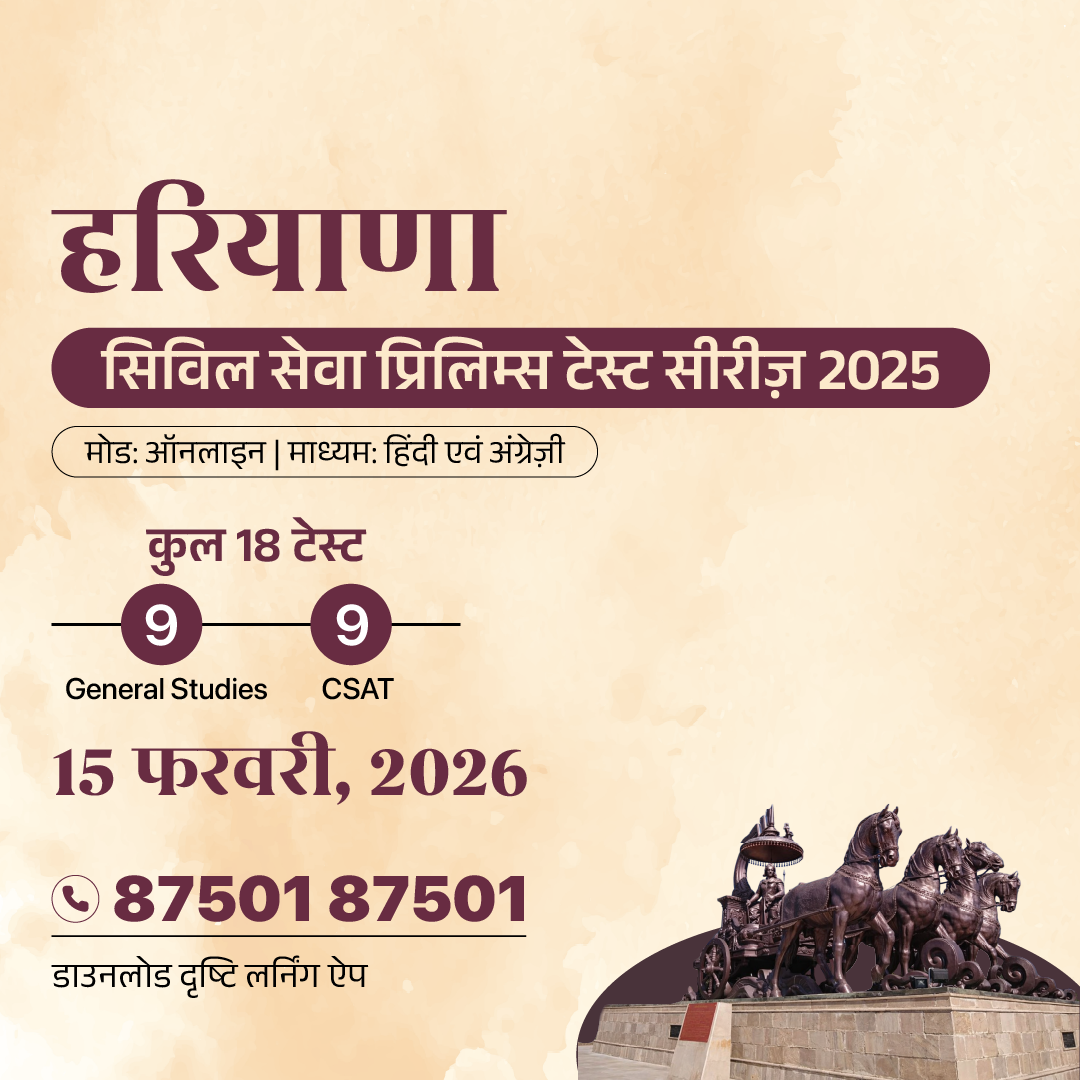
.jpg)