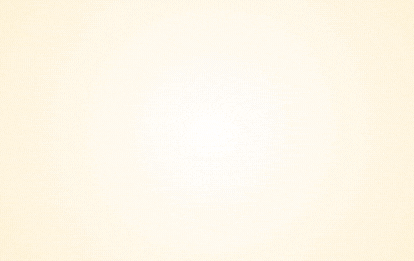राजस्थान Switch to English
राजस्थान में स्थायी लोक अदालतों का अक्रियाशील होना
चर्चा में क्यों?
राजस्थान सरकार द्वारा पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने में विलंब के कारण राज्य के 16 ज़िलों में स्थायी लोक अदालतें (PLAs) स्थगित कर दी गई हैं, जिससे हज़ारों लंबित मामलों के समाधान में विलंब हो रहा है।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 3 मई 2025 को स्पष्ट किया था कि जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, वे विवाद समाधान में भाग नहीं ले सकेंगे।
नोट: अकेले जोधपुर में 972 से अधिक मामले लंबित हैं, जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय ने अनुसार ज़िलों में कुल लंबित मामलों की संख्या 10,000 से अधिक हो सकती है।
मुख्य बिंदु
न्यायिक प्रतिक्रिया
- राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और न्याय तक पहुँच तथा निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार (अनुच्छेद 21) पर इसके गंभीर प्रभाव पर चिंता व्यक्त की।
- उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ (2012) में सर्वोच्च न्यायालय केनिर्णय का हवाला दिया, जो मनमाना या दुर्भावनापूर्ण पाए जाने पर नीतिगत निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की अनुमति देता है।
- मामले की कार्यवाही में सहायता के लिये उच्च न्यायालय ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायमित्र नियुक्त किया है।
- एमिकस क्यूरी (शाब्दिक अर्थ, "न्यायालय का मित्र" ) वह व्यक्ति होता है, जो किसी मामले में पक्षकार नहीं होता है और उसे किसी पक्षकार द्वारा निवेदन किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। इसका कार्य न्यायालय को सूचना, विशेषज्ञता या किसी मुद्दे पर महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान कर सहायता करना होता है।
स्थायी लोक अदालतें (PLAs)
- परिचय:
- PLAs विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-B के तहत कार्य करती हैं।
- यह एक वैधानिक निकाय है, जिसे मुख्यतः पूर्व-विवाद सुलह और समझौते को सुनिश्चित करने के लिये स्थापित किया गया है, विशेष रूप से उन मामलों में जो लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित हों।
- PLAs पक्षकारों को मुकदमा दायर करने से पहले सुलह का प्रयास करने हेतु एक अनिवार्य मंच प्रदान करता है।
- हालाँकि, लोक अदालतों को लंबित मामलों के साथ-साथ मुकदमा-पूर्व मामलों पर भी क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
- PLAs आपराधिक अपराधों से संबंधित मामलों का निर्णय नहीं कर सकते।
- संघटन:
- प्रत्येक स्थायी लोक अदालत में शामिल होते हैं:
- एक अध्यक्ष (आमतौर पर सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी) और
- सार्वजनिक सेवा या कानून में अनुभव वाले दो अन्य सदस्य।
- प्रत्येक स्थायी लोक अदालत में शामिल होते हैं:
- बाध्यकारी प्रकृति:
- स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है।
- यदि दोनों पक्ष आपसी समझौते पर पहुँचने में असफल रहते हैं, तो PLAs को मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार है।
- इस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, जिससे त्वरित एवं निर्णायक समाधान सुनिश्चित होता है।
PLAs के गैर-कार्यशील होने के निहितार्थ
- न्याय तक पहुँच: लोक अदालतें वहनीय और त्वरित न्याय के लिये एक महत्त्वपूर्ण तंत्र हैं, विशेष रूप से कमज़ोर वर्गों के लिये।
- लंबित मामले: इस स्थगन से वर्तमान लंबित मामलों में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे विवाद समाधान और भी अधिक विलंबित हो जाएगा।
- वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) ढाँचे में व्यवधान : इस स्थगन वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को कमज़ोर करता है, जिससे अधिक मामले नियमित अदालतों में वापस चले जाते हैं।
- वादियों की अनिश्चितता: अधिकारियों के कार्यकाल समाप्त होने के कारण लंबित निर्णयों के कारण वादी को लंबे समय तक अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, जिससे कानूनी प्रणाली में विश्वास कम होता है।
लोक अदालत
- लोक अदालत या जन अदालत: न्यायालय में लंबित या मुकदमे-पूर्व विवादों को समझौते या सौहार्दपूर्ण समाधान के माध्यम से निपटान हेतु एक वैकल्पिक मंच है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा है कि लोक अदालत न्यायनिर्णयन की एक प्राचीन भारतीय प्रणाली है जो आज भी प्रासंगिक है और गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है।
- यह वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR ) प्रणाली का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लंभित मामले के संदर्भ में भारतीय न्यायालयों को राहत प्रदान करना है।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य नियमित न्यायालयों में होने वाली लंबी और महँगी प्रक्रियाओं के बिना त्वरित न्याय प्रदान करना है।
- लोक अदालत में किसी की हार या जीत नहीं होती है, इसमें विवाद समाधान हेतु एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाता है।
- कानूनी ढाँचा: प्रारंभ में कानूनी प्राधिकार के बिना एक स्वैच्छिक संस्था के रूप में कार्य करते हुए, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 द्वारा लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
- इस अधिनियम द्वारा संस्था को न्यायालय के आदेश के समान प्रभाव वाले अधिकार प्रदान किये गए।


राजस्थान Switch to English
कोटा में प्रधानमंत्री दिव्यशा केंद्र (PMDK)
चर्चा में क्यों?
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिये कोटा, राजस्थान में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र (PMDK) का उद्घाटन किया और उन्हें सहायक उपकरण वितरित किये।
मुख्य बिंदु
- PMDK पहल के बारे में:
- PMDK पहल का नेतृत्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO) द्वारा किया जाता है।
- इसका प्राथमिक लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को उच्च गुणवत्ता वाले, वहनीय सहायक उपकरण उपलब्ध कराना है।
- वर्तमान में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 45 PMDK केंद्र कार्यरत हैं।
- सरकार का लक्ष्य जून 2025 तक इस नेटवर्क को 100 केंद्रों तक विस्तारित करना है।
- लक्ष्य:
- नवनिर्मित PMDK में दृष्टिबाधित व्यक्तियों पर विशेष ज़ोर दिया गया है।
- यह सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:
- प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स
- ब्रेल उपकरण
- गतिशीलता सहायता
- उन्नत पुनर्वास प्रौद्योगिकियाँ
- कौशल विकास और सशक्तीकरण:
- इसका उद्देश्य लाभार्थियों में कौशल निर्माण के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना है।
- इन कार्यक्रमों का उद्देश्य रोज़गार और उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाना है।
दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिये पहल