वन्यजीव संरक्षण: पारिस्थितिकी संतुलन का आधार
- 05 May, 2025
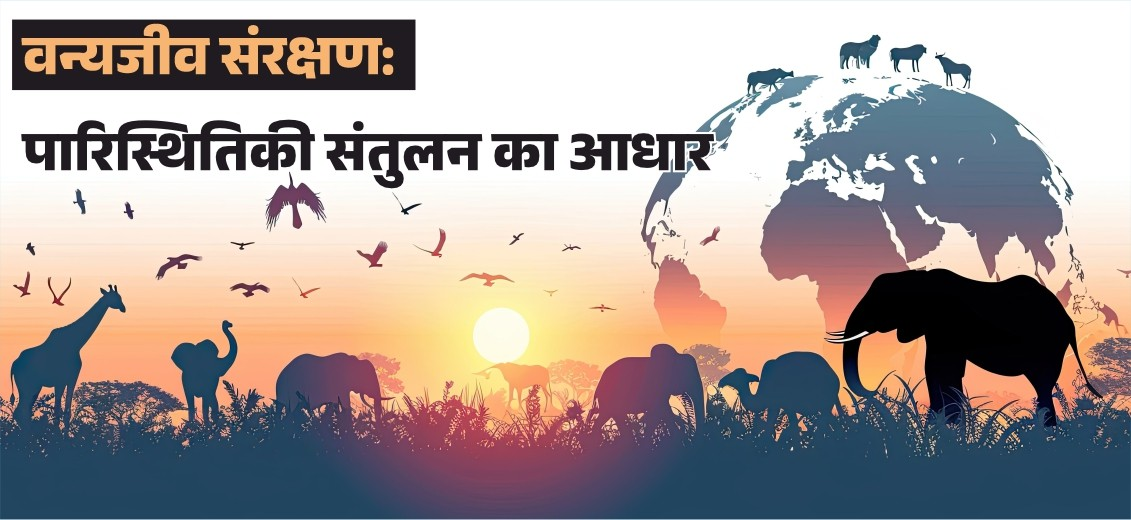
वन्य शब्द का अर्थ जंगली या जंगल में जीवन से है और वन्यजीव के आशय में प्राकृतिक आवास में रहने वाले ऐसे सभी जीव (पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव) शामिल हैं जिनकी न तो खेती की जाती है एवं न ही पालतू बनाए जाते हैं। इन वन्यजीवों का संरक्षण करने का अभिप्राय ऐसे कार्यों के संयोजन से है जिसका उद्देश्य लुप्तप्राय और संकटग्रस्त पशु प्रजातियों की रक्षा करना, उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करना और संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इस प्रकार के संरक्षण में ऐसी सभी तरह की रणनीतियाँ शामिल हैं, जो जैव विविधता को बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों का सामना करने के लिये पारिस्थितिक तंत्र को लचीला बनाने के उपायों का समर्थन करती हैं।
वन्यजीव संरक्षण की महत्ता पृथ्वी पर जैव विविधता की रक्षा करने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में है। इसमें हर प्रजाति के मूल्य को पहचानना शामिल है, चाहे उसका आकार कितना भी सूक्ष्म या दीर्घ हो अथवा उसकी मनुष्यों के लिये उपयोगिता कुछ भी हो। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने एवं जैव विविधता की रक्षा करके हम पारिस्थितिक तंत्र के अस्तित्व, उनके महत्त्वपूर्ण कार्यों और पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता को सुनिश्चित करते हैं। वन्यजीवों का संरक्षण करके हम यह तय करते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ हमारे प्राकृतिक संसार एवं उसमें रहने वाली अविश्वसनीय, अनूठी प्रजातियों का आनंद ले सकें। इसके लिये हमें यह समझना होगा कि प्रजातियाँ पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिये कैसे परस्पर क्रिया करती हैं और साथ ही वे दूसरी तरफ पर्यावरण और मानवीय प्रभावों से कितना और किस प्रकार प्रभावित होती हैं।
इस संदर्भ में यहाँ पहला प्रश्न यह उठता है कि वन्यजीव संरक्षण आखिरकार क्यों महत्त्वपूर्ण है? हमें वन्यजीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? इसका साधारण उत्तर यही है कि पृथ्वी पर हमारे जीवन की सुरक्षा के लिये स्थिर एवं संतुलित पारिस्थितिक तंत्र का होना अनिवार्य है। बिना पारिस्थितिक संतुलन के मनुष्य जीवन ही खतरे में आ जाएगा और उसकी क्षमताओं पर गहरा असर पड़ेगा। सूर्य धरा पर अपनी प्रकाश ऊर्जा का विकिरण करता है। पौधे इस प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से शर्करा में परिवर्तित करते हैं और अन्य वन्यजीवों के लिये ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ये वन्यजीव किसी अन्य के लिये भोजन बनते हैं और कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है। यही शृंखला पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से अपना रास्ता बनाती है। यह रास्ता ही वह खाद्य जाल है जो यह बताता है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में सभी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आपस में कैसे परस्पर क्रिया करते हैं और प्रजातियों के बीच ऊर्जा कैसे स्थानांतरित होती है।
वास्तव में पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा जटिल संजाल है जिसमें प्रत्येक प्रजाति एक विशिष्ट भूमिका निभाती है। एक भी प्रजाति के नष्ट होने से इस संजाल पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, खाद्य शृंखलाओं में व्यवधान आ सकता है, पोषक चक्रों में बदलाव आ सकता है और संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र अस्थिर हो सकता है। वन्यजीवों का संरक्षण करके हम इस पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा, लचीलापन और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। इन्हीं बातों से इस प्रणाली में संतुलन बना रहता है और सभी प्राणियों के लिये जीवन संभव हो पाता है।
वन्यजीव संरक्षण का विचार धरती पर उपस्थित सभी जीवों के जीवन के अधिकार का समर्थन करता है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की बात करता है। संपन्न पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक कार्य करके इस संसार को लाभ पहुँचाते हैं और हमें यह लाभ स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, उपजाऊ मिट्टी, छाया और कार्बन पृथक्करण आदि के रूप में मिलता है। जैसे-जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जमा होती है और ग्रीनहाउस प्रभाव में योगदान देती है, वैसे-वैसे हमारी धरती गर्म होती है और जलवायु परिवर्तन होता है। लेकिन पौधे, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, हवा से कार्बन को अवशोषित करते हैं। पेड़-पौधों को जीवित रहने के लिये इसकी आवश्यकता होती है। वे इसे समस्त जीवों की प्राणवायु ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस प्रकार से वन्य जीव संरक्षण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को धीमा करने और पारिस्थितिक संतुलन का एक खास हिस्सा है, क्योंकि वन हर साल सभी मानव कार्बन उत्सर्जन का लगभग एक-चौथाई हिस्सा अवशोषित करते हैं। साथ ही हमारे महासागर, जंगल और दलदली भूमि भी कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। कई जंतु भी यही भूमिका निभाते हैं और वे एक तरह से पारिस्थितिक तंत्र इंजीनियर के रूप में कार्य करते हैं। वे अपने प्राकृतिक व्यवहार के माध्यम से अपने आस-पास के वातावरण को बदलते हैं और पारिस्थितिक तंत्र को पनपने और उसमें संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं, जैसे– हाथियों को पारिस्थितिक तंत्र इंजीनियर के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे अपने आस-पास की भूमि और अपने साथ रहने वाले अन्य जानवरों का जीवन सरल बनाते हैं। इसी तरह व्हेल न केवल अपने विशाल शरीर में लगभग 33 टन कार्बन जमा करती है, बल्कि अपने मल के माध्यम से फ़ाइटोप्लांकटन को भी उगाती है। ये फ़ाइटोप्लांकटन छोटे समुद्री शैवाल होते हैं जो दुनिया की आधे से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं।
पारिस्थितिक संतुलन में प्राकृतिक गड़बड़ी को ऐसी घटना के रूप में देखा जाता है जो पारिस्थितिक तंत्र की वर्तमान स्थिति में व्यवधान पैदा करती है। प्राकृतिक गड़बड़ी मौसम, भूविज्ञान और जैविक उतार-चढ़ाव सहित प्रकृति की शक्तियों के कारण होती है। इसमें आग, बाढ़, भूकंप, रोग और सूखा जैसी चीज़ें हो सकती हैं। पर सभी व्यवधान प्राकृतिक नहीं होते। मानवीय क्रियाकलापों ने पारिस्थितिक तंत्र में देखी जाने वाली कई गड़बड़ियों में योगदान दिया है। प्राकृतिक व्यवधान कभी-कभी होते हैं, पर सतत् मानवीय व्यवधान पारिस्थितिक तंत्र पर लगातार दबाव डालकर प्रजातियों को प्रभावित कर रहे हैं। जिस क्षण पारिस्थितिक तंत्र एक तनाव के साथ तालमेल बिठाना शुरू करता है, तो दूसरा तनाव सामने आता है। जिन पारिस्थितिक तंत्रों पर हम निर्भर हैं, उनमें से कई को नई परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिये पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। व्यवधानों का वृद्धि, क्षय और वृद्धि का प्राकृतिक चक्र होता है। पर सतत् तनावों के कारण यह चक्र ठीक से काम नहीं कर पा रहा है।
मानवजनित प्रदूषकों का व्यवधान पारिस्थितिक तंत्र पर खासा दबाव डाल रहा है। जब जानवर अपने शिकार को खाते हैं, तो वे उसमें मौजूद सभी रसायनों और पोषक तत्त्वों को भी सोख लेते हैं। कभी-कभी जानवर प्रदूषक भी खा लेते हैं जो उनके शरीर में जमा हो सकते हैं। मानवजन्य प्रदूषण के कारण पर्यावरण में भारी धातुएँ, तेल और औद्योगिक उत्पाद और दवा एवं रसायन मिल गए हैं। पौधे, मछलियाँ और दूसरी प्रजातियाँ इन विषाक्त पदार्थों को सोख लेती हैं और जब वे मनुष्य या दूसरे पशुओं द्वारा खाए जाते हैं, तो विषाक्त पदार्थ उनके शरीर में अवशोषित हो जाते हैं। जैसे-जैसे यह खाद्य जाल आगे बढ़ता है, विषाक्त पदार्थ का संक्रेंद्रण भी अधिक होता चला जाता है। इस तथ्य को एक उदाहरण के माध्यम से समझा जाना चाहिये। गिद्ध पक्षी लावारिस मानव एवं पशुओं को खाकर उनका निपटारा करते हैं। साल 1994 में किसानों ने मवेशियों को दर्द निवारक दवा डिक्लोफेनाक देना शुरू किया, लेकिन यह दवा उन मृत पशुओं को खाने वाले गिद्धों के लिये गहरी समस्या साबित हुई क्योंकि इससे गिद्धों के गुर्दे खराब हो जाते थे। इससे केवल एक दशक में भारतीय गिद्धों की आबादी में भारी गिरावट आई और यह संख्या पाँच करोड़ से घटकर मात्र कुछ हज़ार रह गई।
यहाँ पर यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि अगर वन्यजीव संरक्षण अवैज्ञानिक और अतार्किक होगा तो वन्यजीव संरक्षण की दिशा और वैज्ञानिक प्रक्रिया बाधित हो सकती है तथा मानव और वन्य प्राणियों के बीच संतुलित संबंध नष्ट हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में वैचारिक भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। वैज्ञानिक वन्यजीव संरक्षण की अवधारणा की कुंजी समग्रता के आधार पर वन्यजीवों के संरक्षण और उपयोग के बीच के संबंध को समझना है। इसके अनुसार पारिस्थितिक प्रणाली एक जैविक संपूर्ण है और इसके प्रत्येक भाग को अलग से नहीं समझा जा सकता है। एक अंतर को यहाँ समझना उचित होगा कि वन्यजीव कल्याण और वन्यजीव अधिकार समानार्थी नहीं अपितु ये वन्यजीव संरक्षण के दो अलग-अलग पहलू हैं। वन्यजीव अधिकारों का समर्थन करने वाले लोग तर्क देते हैं कि जानवरों में विचार, इच्छाएँ, चेतना और स्मृतियाँ होती हैं और वे मनुष्यों की तरह ही भावना और दर्द महसूस करते हैं। उन्हें चोट से बचने या शोषण न किये जाने का अधिकार है। यह हमारा दायित्व है कि हम अनुसंधान या व्यापारिक खेती में जंतुओं का उपयोग न करें। वन्यजीव भी जीवन का विषय हैं और मनुष्यों की तरह उनके पास दिल व मनोविज्ञान दोनों होते हैं, इसलिये वे अधिकारों के हकदार हैं। जबकि पशु कल्याण कानूनों के माध्यम से किया जाता है,जैसे– पशु कल्याण सुनिश्चित करने के लिये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 बनाया गया है।
यह देखना होगा कि वन्यजीव संरक्षण में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के काम में अल्पकालिक हस्तक्षेप और दीर्घकालिक स्थिरता दोनों प्रकार के लक्ष्य शामिल हैं। वन्यजीव अहम प्राकृतिक संसाधन रहे हैं और पशुपालन ने दीर्घकालिक मानव विकास के लिये आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की है। वन्यजीवों ने कपड़ों, चिकित्सा सामग्री, प्रायोगिक मॉडल, पर्यटन और वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास में खासी भूमिका निभाई है। वन्यजीवों का संरक्षण और उपयोग समग्रता के दृष्टिकोण से एकीकृत है, परस्पर विरोधी नहीं। मनुष्य और वन्यजीव संस्कृति, पारंपरिक चिकित्सा, भोजन और पारिस्थितिक पर्यटन के मामले में आपस में बहुत निकट से जुड़े हुए हैं। अपने आंतरिक मूल्य से परे, वन्यजीव और उनके आवास मानव समाज को ठोस आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। वे स्वस्थ पारिस्थितिक संतुलित तंत्र परागण, जल-शोधन और कार्बन पृथक्करण जैसे आवश्यक कार्यों का समर्थन करते हैं। संक्षेप में संरक्षण के प्रयास न केवल वन्यजीवों की रक्षा करते हैं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिये इन आर्थिक लाभों को भी बनाए रखते हैं। इस कारण से वन्यजीवों को मनुष्य से अलग करके देखना आसान और उचित नहीं है। इसलिये यह सामाजिक और वैज्ञानिक दोनों रूपों से अहम है कि वन्यजीवों की सुरक्षा की जाए ताकि असंतुलन न पनप सके।
इस पक्ष के अलावा वन्यजीव संरक्षण को मनुष्य की नैतिक अनिवार्यता के रूप में देखा जाना चाहिये। पृथ्वी पर सभी जीवों की विविधता की रक्षा और संरक्षण करना मनुष्य मात्र की नैतिक ज़िम्मेदारी है। प्रत्येक प्रजाति को अस्तित्व बनाए रखने का अपना अधिकार है और उनका यह अधिकार मनुष्यों के लिये उनकी उपयोगिता से स्वतंत्र होता है। कोई भी वन्यजीव यदि मनुष्य के लिये उपयोगी न भी हो तो भी उसे यह अधिकार है कि उसे नुकसान नहीं पहुँचाया जाए। वन्यजीव संरक्षण करुणा और सम्मान के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए सभी जीवित प्राणियों के होने के अंतर्निहित मूल्य का सम्मान करता है। अगर इस मूल्य का सम्मान न हो तो जैव विविधता में गिरावट आ जाएगी और परिणामस्वरूप पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाएगा। पर्याप्त जैव विविधता के बिना जीवन अस्थिर बनेगा क्योंकि मनुष्य अपने लगभग सभी संसाधनों के लिये किसी न किसी तरह से प्राकृतिक दुनिया पर निर्भर है।
निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि वन्यजीवों का संरक्षण नहीं करना मनुष्यों और प्रकृति के बीच संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिये तर्कसंगत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह ध्यान रखना होगा कि वन्यजीवों का संरक्षण चार प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है। पहला, प्रत्येक वन्यजीव को मनुष्यों के समान जीवन का अधिकार दिया जाना चाहिये, दूसरा, प्रत्येक वन्यजीव को मानव द्वारा उत्पन्न दर्द और पीड़ा से मुक्त रहना चाहिये, तीसरा, उनका किसी भी मानवीय उद्देश्य के लिये शोषण नहीं किया जाना चाहिये और चौथा, प्रत्येक वन्यजीव को दुर्लभता की परवाह किये बिना समान दर्जा दिया जाना चाहिये चाहे वह प्रजाति देशी, विदेशी, आक्रामक या जंगली हो या नहीं। वन्यजीवों को मनुष्यों के समान सभी प्रकार की आचरण एवं विधिक सुरक्षा दी जानी चाहिये ताकि पारिस्थितिक संतुलन बना रहे क्योंकि यह धरा सबके लिये है न कि केवल मनुष्य, उसके जीवन एवं आनंद के लिये। सभी जीवों को जीवित रहने का अधिकार मनुष्य मात्र के समान है, उससे कम नहीं।




