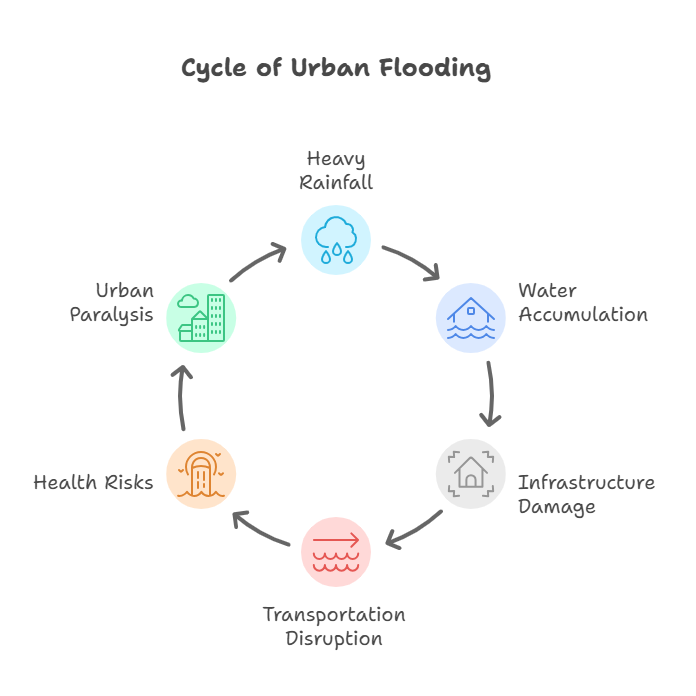- फ़िल्टर करें :
- अर्थव्यवस्था
- विज्ञान-प्रौद्योगिकी
- पर्यावरण
- आंतरिक सुरक्षा
- आपदा प्रबंधन
-
प्रश्न :
प्रश्न. भारतीय शहरों द्वारा अपनाई गई वर्तमान बाढ़ प्रबंधन रणनीतियों पर चर्चा कीजिये। शहरी बाढ़ को कम करने में ये रणनीतियाँ कितनी प्रभावी हैं तथा बाढ़ जोखिम प्रबंधन एवं आपदा शमन में क्या सुधार किये जा सकते हैं? (250 शब्द)
18 Jun, 2025 सामान्य अध्ययन पेपर 3 आपदा प्रबंधनउत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
- शहरी बाढ़ प्रबंधन की वर्तमान प्रवृत्तियों तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा शहरी बाढ़ पर प्रस्तुत आँकड़ों का संक्षिप्त विवरण दीजिये।
- भारतीय नगरों में वर्तमान बाढ़ प्रबंधन रणनीतियों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- इन रणनीतियों की प्रभावशीलता को रेखांकित कीजिये।
- प्रभावी बाढ़ जोखिम प्रबंधन हेतु संभावित सुधारों का सुझाव दीजिये।
- समापन में शहरी बाढ़ प्रबंधन पर केंद्रीय जल आयोग द्वारा प्रस्तुत दिशा-निर्देशों का उल्लेख कीजिये।
परिचय:
मुंबई जैसे शहरों में भंडारण जलाशयों जैसी परियोजनाओं के बावजूद भारत शहरी बाढ़ की दृष्टि से अत्यधिक सुभेद्य बना हुआ है। देश के कुल 329 मिलियन हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र बाढ़-प्रवण (NDMA के अनुसार) है। यह स्थिति लक्षित, प्रभावी बाढ़ जोखिम प्रबंधन और सतत् शहरी नियोजन की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
मुख्य भाग:
भारतीय नगरों में वर्तमान बाढ़ प्रबंधन रणनीतियाँ:
- वर्षा जल निकासी प्रणालियों का विस्तार: कई नगरों में भारी वर्षा के समय जलभराव की समस्या से निपटने के लिये वर्षाजल निकासी प्रणाली के विस्तार और सुधार पर ध्यान दिया जा रहा है।
- मुंबई और बेंगलुरु जैसे नगरों में बढ़ती वर्षाजल की मात्रा को सँभालने के लिये जलनिकासी क्षमता को सुदृढ़ किया जा रहा है।
- दिल्ली और कोलकाता जैसे नगरों में मौजूदा जलनिकासी प्रणालियों की नियमित रूप से सिल्ट निकासी की जा रही है ताकि उनकी वहन क्षमता में वृद्धि हो।
- बाढ़ पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ: शहर वास्तविक काल वर्षण डेटा, नदी के जल स्तर और तूफानी जल की स्थिति एकत्र करने के लिये उन्नत बाढ़ पूर्वानुमान उपकरण एवं सेंसर अपना रहे हैं।
- उदाहरण के लिये, चेन्नई ने जल निकायों में सेंसर नेटवर्क स्थापित किये हैं जो बेहतर बाढ़ पूर्वानुमान के लिये लाइव डेटा प्रदान करते हैं।
- नदी और झील पुनरुद्धार परियोजनाएँ: बैंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों में अतिप्रवाह और बाढ़ को रोकने के लिये नदी पुनरुद्धार परियोजनाएँ शुरू की जा रही हैं।
- इन पहलों का उद्देश्य नदियों और झीलों के जलमार्गों को पुनः व्यवस्थित करके जल प्रवाह का प्रबंधन करना तथा शहरी बाढ़ को कम करना है।
- बाढ़ क्षेत्र निर्धारण (फ्लडप्लेन ज़ोनिंग) और भूमि उपयोग नियोजन: मुंबई, अहमदाबाद और पुणे जैसे शहरों में फ्लडप्लेन ज़ोनिंग का बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में कोई नया निर्माण न किया जाए।
- तटीय बाढ़ अवरोधक: चेन्नई और मुंबई जैसे तटीय नगरों में समुद्री तूफानों एवं उच्च ज्वार से बचाव हेतु समुद्री दीवारों व ज्वारीय द्वारों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि मानसून के समय बाढ़ की स्थिति और अधिक विकराल न हो।
इन रणनीतियों की प्रभावशीलता:
बाढ़ की रोकथाम/न्यूनीकरण के लिये अनेक रणनीतियों तथा बुनियादी अवसंरचना के आधुनिकीकरण के प्रयासों के बावजूद, मौजूदा प्रणालियाँ प्रायः वर्षा की बढ़ती तीव्रता को प्रबंधित करने में विफल हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारी वर्षा के दौरान बड़े पैमाने पर जलभराव और शहरी क्षेत्र में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि:
- अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना और बोझ से दबी प्रणालियाँ: मौजूदा अवसंरचना वर्तमान वर्षा-प्रवृत्तियों की तीव्रता को सँभालने में अक्षम है। इसका परिणाम व्यापक शहरी बाढ़, आर्थिक क्षति और जनजीवन के बाधित होने के रूप में सामने आता है।
- उदाहरण: दिल्ली की जलनिकासी प्रणाली, जिसे 1970 के दशक में डिज़ाइन किया गया था, शहर की बढ़ती जनसंख्या और परिवर्तित वर्षा-प्रवृत्तियों के अनुकूल नहीं है। इसी कारण वर्ष 2023 में भारी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई।
- प्राकृतिक जल निकायों की हानि: शहरी क्षेत्रों में वेटलैंड्स, झीलों और बाढ़ मैदानों पर अनियंत्रित अतिक्रमण ने वर्षा जल को सोखने तथा बाढ़ को नियंत्रित करने की शहरों की क्षमता को कम कर दिया है।
- उदाहरण: बेंगलुरु ने अपनी 79% झीलें खो दी हैं, जिससे उसकी बाढ़-रोधी क्षमता में भारी गिरावट आई है, जबकि पूर्व में ये झीलें प्राकृतिक बाढ़ अवरोधक के रूप में कार्य करती थीं।
- अकुशल अपशिष्ट प्रबंधन: नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट का पर्याप्त रूप से प्रबंधन न किये जाने के कारण नालियाँ जाम हो जाती हैं और जल प्रवाह क्षमता कम हो जाती है।
- उदाहरण: वर्ष 2020 की मुंबई बाढ़ के दौरान, जल निकासी प्रणाली में अपशिष्ट संचय ने गंभीर जलभराव में योगदान दिया।
- समग्र एवं पूर्व-निवारक उपायों का अभाव: वर्तमान रणनीतियाँ प्रायः पूर्व-निवारक उपायों के बजाय बाढ़ के बाद राहत पर केंद्रित होती हैं।
- बाढ़ की समस्या का प्रायः तभी हल किया जाता है जब वह घटित होती है, जबकि दीर्घकालिक योजना या नगरीय डिज़ाइन में संरचनात्मक दृढ़ता का अभाव रहता है।
- उदाहरण: चेन्नई (वर्ष 2015) में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद, पुनर्निर्माण के प्रयास मुख्य रूप से बाढ़-प्रतिरोधी बुनियादी अवसंरचना के पुनर्निर्माण के बजाय अल्पकालिक राहत पर केंद्रित थे।
प्रभावी बाढ़ जोखिम प्रबंधन के लिये सुधार:
- ‘स्पॉन्ज सिटी’ अवधारणा को लागू करना: स्पॉन्ज सिटी दृष्टिकोण का उद्देश्य ऐसे सतहों का निर्माण करना है जो जल को सोख सकें, शहरी आर्द्रभूमियों का पुनर्भरण करना तथा हरित क्षेत्रों का निर्माण करना है, जो वर्षा जल को अवशोषित और संग्रहित कर सकें। यह सतही बहाव और जलभराव की समस्या को उल्लेखनीय रूप से कम कर सकता है।
- बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों ने इस मॉडल को अपनाकर सकारात्मक परिणाम प्राप्त किये हैं। विशेष रूप से मुंबई जैसे भारतीय शहरों को अपनी शहरी योजनाओं में इस प्रकार की विधियों को सम्मिलित करना चाहिये।
- स्मार्ट स्टॉर्मवॉटर प्रबंधन प्रणाली अपनाना: इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आधारित सेंसरों और रीयल-टाइम डेटा विश्लेषण का प्रयोग करके बाढ़ के जोखिमों की बेहतर पूर्वानुमान और प्रबंधन किया जा सकता है।
- सिंगापुर की स्मार्ट वॉटर असेसमेंट नेटवर्क (SWAN) प्रणाली वास्तविक समय में डेटा प्रदान कर बाढ़ प्रबंधन को सुदृढ़ बनाती है।
- दिल्ली जैसे भारतीय शहर ऐसी तकनीकें अपनाकर अपनी प्रतिक्रिया की गति तथा बाढ़-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं।
- सिंगापुर की स्मार्ट वॉटर असेसमेंट नेटवर्क (SWAN) प्रणाली वास्तविक समय में डेटा प्रदान कर बाढ़ प्रबंधन को सुदृढ़ बनाती है।
- शहरी आर्द्रभूमि और झीलों का पुनरुद्धार: शहरी आर्द्रभूमियों और झीलों की रक्षा तथा पुनर्भरण बाढ़ से निपटने की क्षमता को बढ़ाने के लिये आवश्यक है।
- उदाहरणस्वरूप, कोलकाता की 'ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स' बाढ़ नियंत्रण तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अन्य शहरों को भी अपनी आर्द्रभूमियों और झीलों की पूर्व क्षमता को पुनः स्थापित करने के प्रयास करने चाहिये।
- ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्टिकल गार्डन: शहरी विकास में हरित आधारभूत संरचना को सम्मिलित किया जाना चाहिये। वर्टिकल गार्डन, ग्रीन रूफ्स और पारगम्य पक्की सतहों से वर्षा जल को अवशोषित कर जलनिकासी प्रणाली पर बोझ को कम किया जा सकता है।
- मिलान का 'बॉस्को वर्टीकाले' (वर्टिकल फॉरेस्ट) एक अभिनव उदाहरण है जहाँ भवनों के माध्यम से जल बहाव को नियंत्रित किया जाता है और वायु गुणवत्ता को भी सुधारा जाता है। इस प्रकार की योजनाएँ बाढ़-प्रवण भारतीय शहरों के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं।
- क्षेत्र निर्धारण कानूनों को मज़बूत करना तथा पारिस्थितिक संरक्षण: बाढ़ संभावित क्षेत्रों और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिये क्षेत्र निर्धारण कानूनों का सख़्ती से अनुपालन आवश्यक है।
- साथ ही, प्रतिपूरक वनीकरण और पारिस्थितिक संरक्षण को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ताकि शहरी बाढ़ की समस्याओं को कम किया जा सके।
- समुदाय-आधारित बाढ़ प्रबंधन: स्थानीय समुदायों को बाढ़ प्रबंधन की प्रक्रिया में सम्मिलित कर एक अधिक सशक्त और टिकाऊ शहरी वातावरण निर्मित किया जा सकता है।
- महाराष्ट्र का 'नगदरवाड़ी' गाँव, जहाँ समुदाय-आधारित वर्षा जल संचयन की पहलों से जलाभाव की समस्या का समाधान हुआ, एक प्रेरणास्पद उदाहरण है। इस प्रकार की जमीनी पहल को अन्य भारतीय शहरों में भी अपनाया जा सकता है।
- जन जागरूकता और आपदा तैयारी में सुधार: बाढ़ से सुरक्षा, अपशिष्ट प्रबंधन और जल संरक्षण विषयों पर जन-जागरूकता अभियान चलाकर शहरी बुनियादी ढाँचे पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सकता है।
- रॉटरडैम के ‘वॉटर स्क्वेयर’ न केवल अत्यधिक वर्षा के समय जल संचयन करते हैं, बल्कि बाढ़ प्रबंधन के लिये शैक्षिक केंद्र के रूप में भी कार्य करते हैं। भारत में भी इस प्रकार की योजनाओं से जन-जागरूकता बढ़ाई जा सकती है तथा स्थानीय स्तर पर बाढ़ से निपटने की क्षमता को सुदृढ़ किया जा सकता है।
निष्कर्ष:
भारत में शहरी बाढ़ की समस्या तात्कालिक तथा निरंतर प्रयासों की माँग करती है, क्योंकि वर्तमान उपाय आवश्यक होते हुए भी इस समस्या की व्यापकता से निपटने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। शहरी बाढ़ प्रबंधन पर केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश नगरों को शहरी नियोजन में बाढ़ जोखिम प्रबंधन को समाहित करने का एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, जिसमें सतत् जल निकासी प्रणाली, बाढ़ क्षेत्र निर्धारण और जलवायु-सहनशीलता पर विशेष बल दिया गया है।
To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.
Print