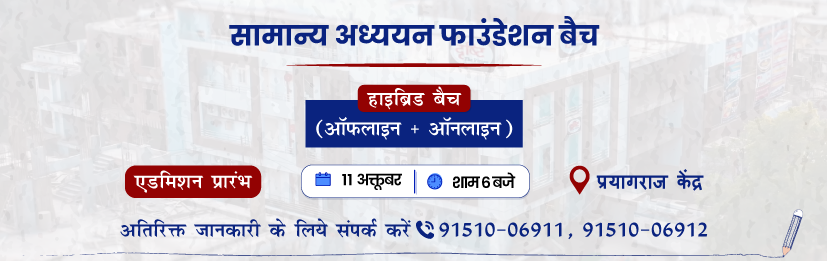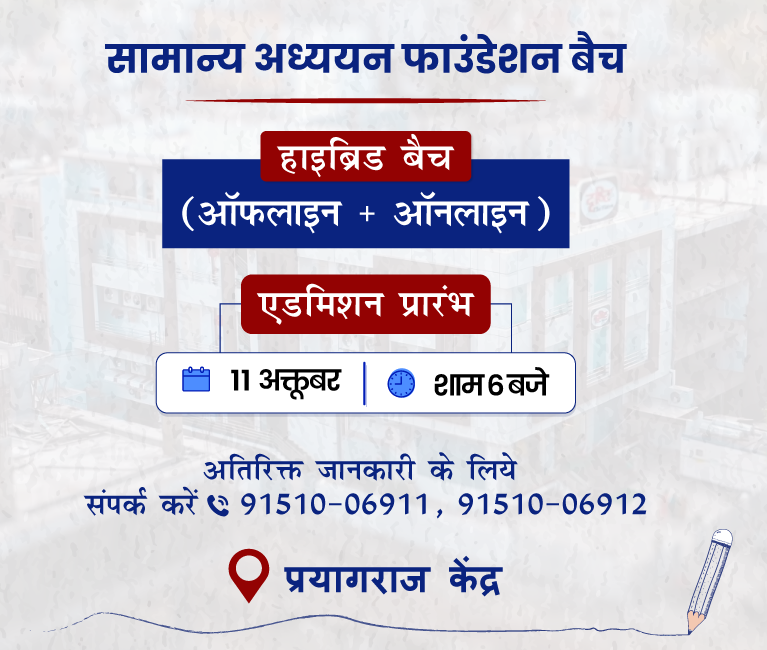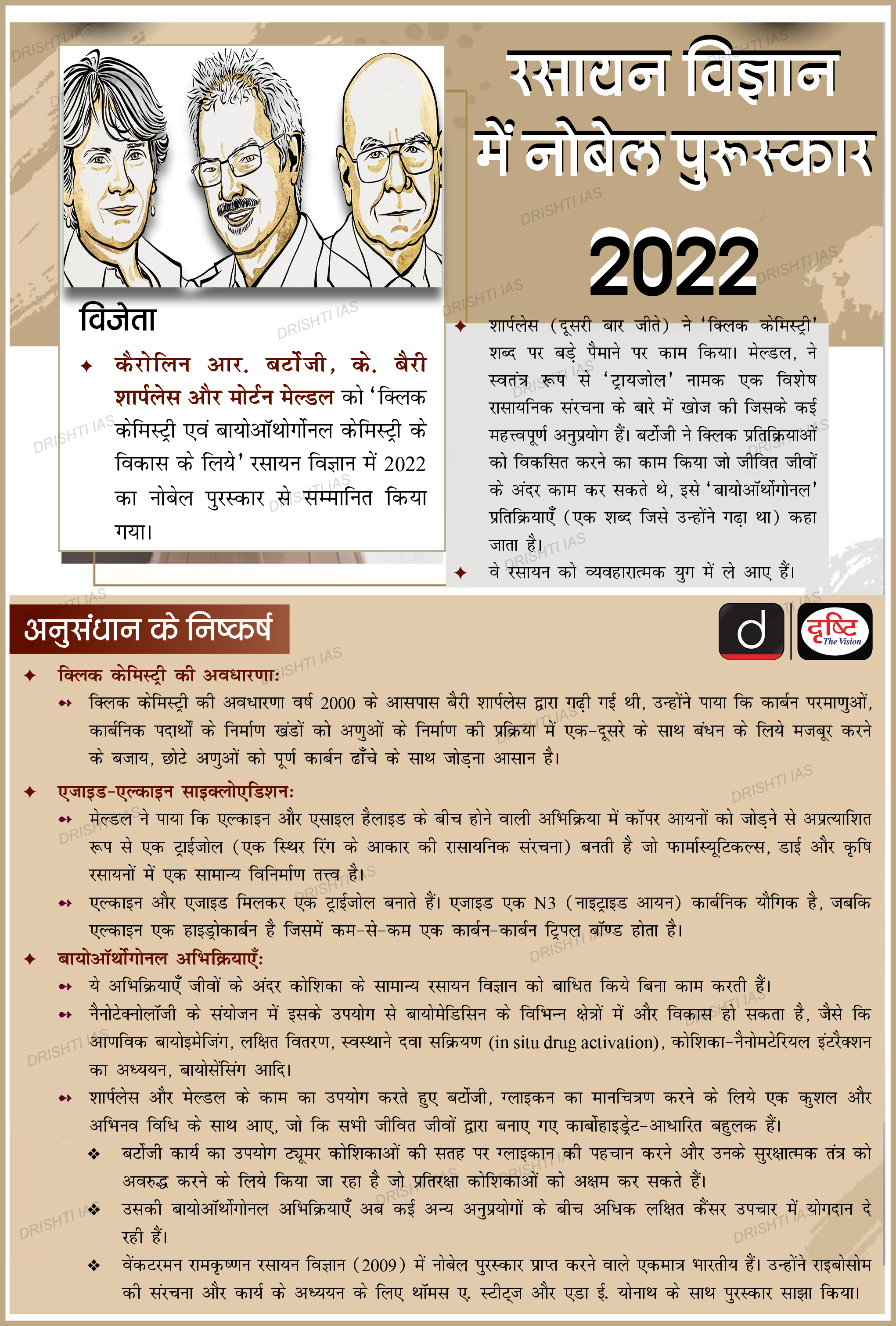इन्फोग्राफिक्स
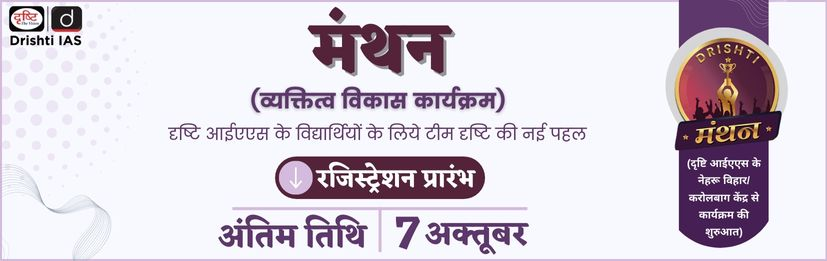
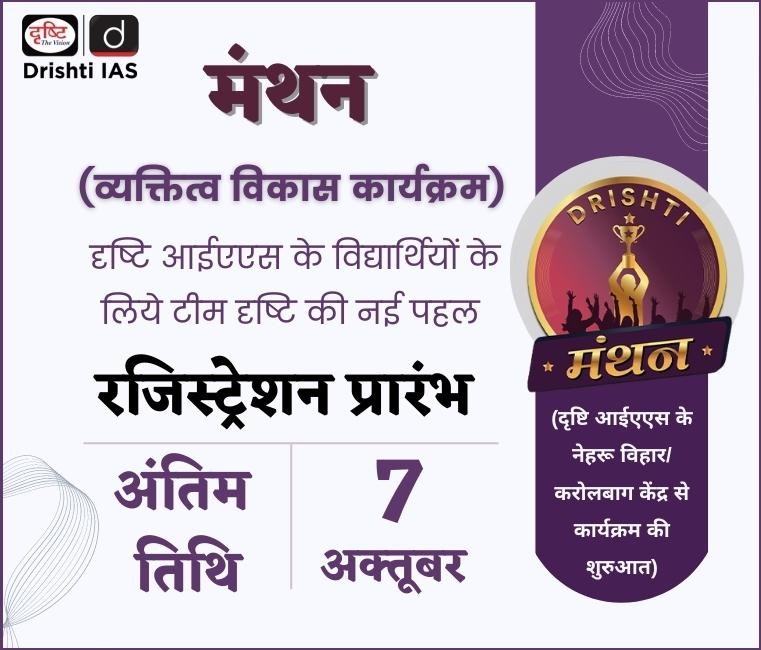
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
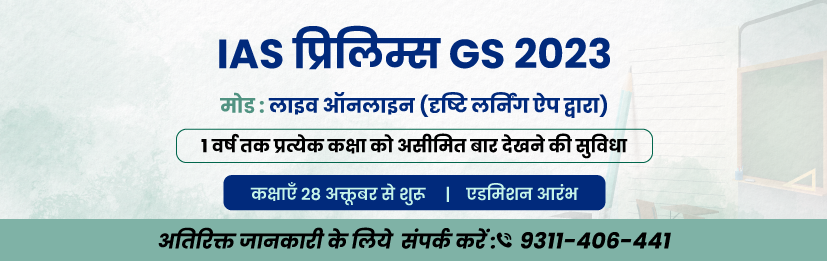
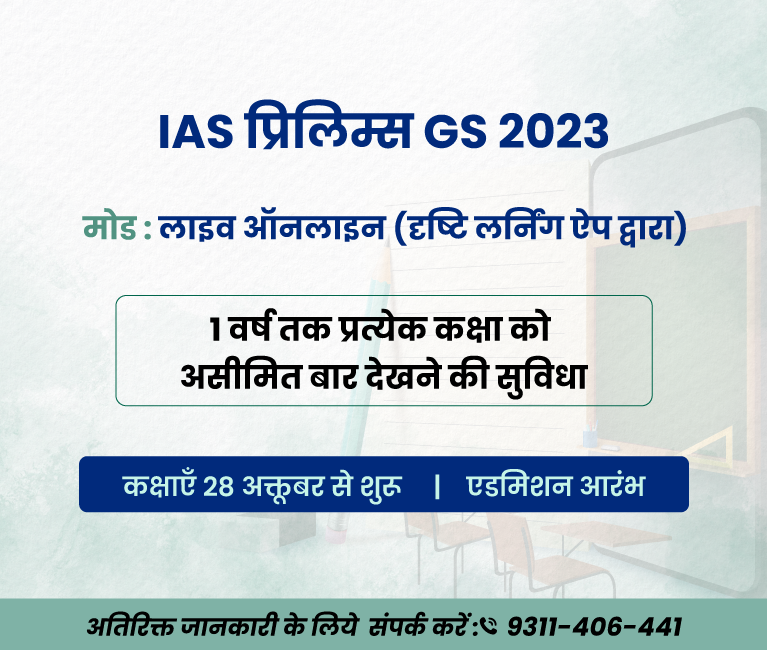
जैव विविधता और पर्यावरण
बायोमास को-फायरिंग लक्ष्य में भारत का पिछड़ापन
प्रिलिम्स के लिये:बायोमास और इसके लाभ, डीकार्बोनाइज़ेशन, ग्रीन हाउस गैस। मेन्स के लिये:बायोमास को-फायरिंग, महत्त्व और चुनौतियाँ। |
चर्चा में क्यों?
विद्युत मंत्रालय उन संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में कटौती करने पर विचार कर रहा है जो बायोमास को-फायरिंग मानदंडों का पालन नहीं करते हैं।
- विद्युत मंत्रालय ने अक्तूबर 2021 में सभी ताप विद्युत संयंत्रों को अक्तूबर 2022 तक 5% को-फायरिंग अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया था।
- 2020-21 में केवल आठ बिजली संयंत्रों ने बायोमास सह को-फायरिंग (co-fired biomass pellets) को अपनाया और यह संख्या हाल ही में बढ़कर 39 हो गई है।
बायोमास को-फायरिंग:
- परिचय:
- बायोमास को-फायरिंग कोयला थर्मल संयंत्रों में बायोमास के साथ ईंधन के एक हिस्से को प्रतिस्थापित करने की विधि है।
- कोयले को जलाने के लिये डिज़ाइन किये गए बॉयलरों में कोयले और बायोमास का एक साथ दहन किया जाता है। इस उद्देश्य हेतु मौजूदा कोयला विद्युत संयंत्रों का आंशिक रूप से पुनर्निर्माण और पुनर्संयोजित किया जाना है।
- को-फायरिंग एक कुशल और स्वच्छ तरीके से बायोमास को बिजली में बदलने एवं बिजली संयंत्रों से होने वाले ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने का एक विकल्प है।
- बायोमास को-फायरिंग कोयले को डीकार्बोनाइज़ करने के लिये विश्व स्तर पर स्वीकृत एक लागत प्रभावी तरीका है।
- भारत एक ऐसा देश है जहांँ आमतौर पर बायोमास को खेतों में जला दिया जाता है, जो आसानी से उपलब्ध एक बहुत ही सरल समाधान का उपयोग करके स्वच्छ कोयले की समस्या को हल करने के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।
- बायोमास को-फायरिंग कोयला थर्मल संयंत्रों में बायोमास के साथ ईंधन के एक हिस्से को प्रतिस्थापित करने की विधि है।
- महत्त्व:
- बायोमास को-फायरिंग फसल अवशेषों को खुले में जलाने से होने वाले उत्सर्जन को रोकने का एक प्रभावी तरीका है; यह कोयले का उपयोग करके बिजली उत्पादन की प्रक्रिया को भी डीकार्बोनाइज़ करता है।
- कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में 5-7% कोयले को बायोमास से प्रतिस्थापित करने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 38 मिलियन टन की कमी आ सकती है।
- यह जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्सर्जन में कटौती करने में मदद कर सकता है, कुछ हद तक कृषि पराली जलाने की भारत की बढ़ती समस्या का समाधान कर सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार पैदा करते हुए कचरे के बोझ को कम कर सकता है।
- भारत में अधिक बायोमास उपलब्धता के साथ-साथ कोयला संचालित क्षमता में तेज़ी से वृद्धि हुई है।
- बायोमास को-फायरिंग फसल अवशेषों को खुले में जलाने से होने वाले उत्सर्जन को रोकने का एक प्रभावी तरीका है; यह कोयले का उपयोग करके बिजली उत्पादन की प्रक्रिया को भी डीकार्बोनाइज़ करता है।
- चुनौतियाँ:
- कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में बायोमास के साथ 5-7% कोयले को प्रतिस्थापित करने से 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की कमी हो सकती है, लेकिन मौजूदा बुनियादी ढांँचा इसे वास्तविकता में बदलने के लिये पर्याप्त रूप से मज़बूत नहीं है।
- को-फायरिंग के लिये प्रतिदिन लगभग 95,000-96,000 टन बायोमास पैलेट की आवश्यकता होती है, लेकिन देश में 228 मिलियन टन अतिरिक्त कृषि अवशेष उपलब्ध होने के बावजूद भारत की पैलेट निर्माण क्षमता वर्तमान में 7,000 टन प्रतिदिन है।
- यह बड़ा अंतर उपयोगिता को मौसमी उपलब्धता और बायोमास पैलेट की अविश्वसनीय आपूर्ति के कारण है।
- बायोमास पैलेट को संयंत्र स्थलों पर लंबे समय तक संग्रहीत करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वे वायु से नमी को जल्दी अवशोषित करते हैं, जिससे वे को-फायरिंग के लिये अनुपयुक्त हो जाते हैं।
- कोयले के साथ दहन के लिये केवल 14% नमी वाले पैलेट का उपयोग किया जा सकता है।
बायोमास:
- परिचय:
- बायोमास पौधे या पशु अपशिष्ट है जिसे विद्युत या ऊष्मा उत्पन्न करने के लिये ईधन के रूप में जलाया जाता है। उदाहरण लकड़ी, फसलें और जंगलों, यार्डों या खेतों से निकलने वाले अपशिष्ट।
- बायोमास हमेशा से देश के लिये महत्त्वपूर्ण एवं लाभदायक ऊर्जा स्रोत रहा है।
- लाभ:
- यह नवीकरणीय, व्यापक रूप से उपलब्ध, कार्बन-तटस्थ है और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण रोज़गार प्रदान करने की क्षमता है।
- यह दृढ़ रूप से ऊर्जा प्रदान करने में भी सक्षम है। देश में कुल प्राथमिक ऊर्जा उपयोग का लगभग 32% अभी भी बायोमास से ही प्राप्त होता है तथा देश की 70% से अधिक आबादी अपनी ऊर्जा आवश्यता हेतु इस पर निर्भर है।
- बायोमास विद्युत और सह उत्पादन कार्यक्रम:
- परिचय:
- इस कार्यक्रम को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
- कार्यक्रम के तहत बायोमास के कुशल उपयोग के लिये चीनी मिलों में खोई आधारित सह उत्पादन और बायोमास विद्युत उत्पादन शुरू किया गया है।
- विद्युत उत्पादन के लिये उपयोग की जाने वाली बायोमास सामग्री में चावल की भूसी, पुआल, कपास के डंठल, नारियल के अवशेष, सोया भूसी, डी-ऑयल केक, कॉफी अपशिष्ट, जूट अपशिष्ट, मूंँगफली के छिलके आदि शामिल हैं।
- उद्देश्य:
- ग्रिड विद्युत उत्पादन हेतु देश के बायोमास संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिये प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
- परिचय:
संबद्ध पहलें:
आगे की राह
- बिजली संयंत्रों में पैलेट निर्माण और को-फायरिंग के इस व्यवसाय मॉडल में किसानों की आंतरिक भूमिका सुनिश्चित करने के लिये प्लेटफॉर्मों की स्थापना करने की आवश्यकता है।
- प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बिना को-फायरिंग क्षमता का दोहन करने के लिये उभरती अर्थव्यवस्थाओं को प्रौद्योगिकी और नीति तैयार करने की आवश्यकता है।
- मिट्टी और जल संसाधनों की सुरक्षा, जैवविविधता, भूमि आवंटन एवं कार्यकाल, खाद्य कीमतों सहित जैव ऊर्जा के लिये स्थिरता संकेतकों को नीतिगत उपायों में एकीकृत करने की आवश्यकता है।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2019) 1. कार्बन मोनोऑक्साइड फसल/बायोमास अवशेषों के जलने से उपर्युक्त में से कौन-से वातावरण में उत्सर्जित होते है? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d)
अतः विकल्प (d) सही है। |
स्रोत: द हिंदू
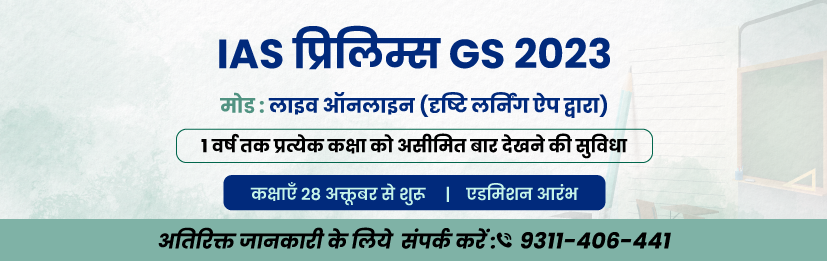
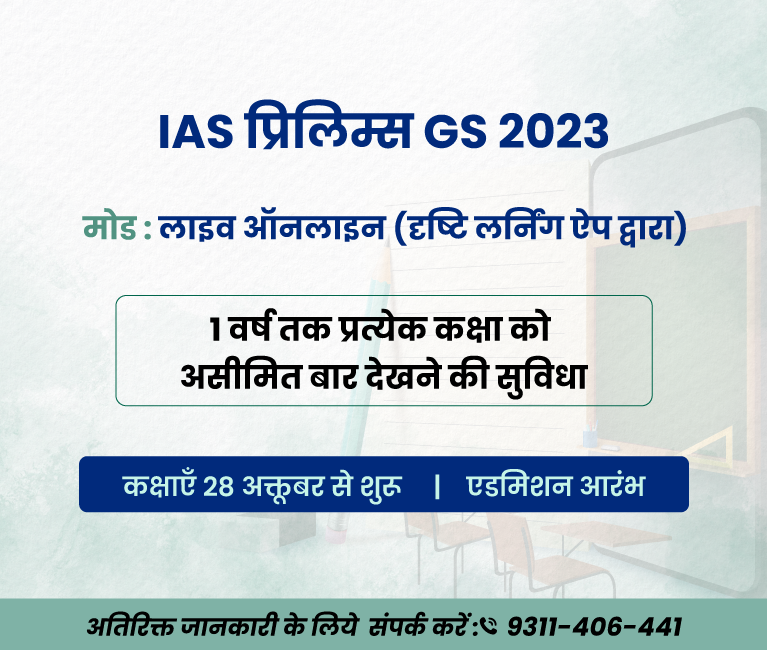
शासन व्यवस्था
अनुसूचित जाति की मान्यता हेतु मानदंड
प्रिलिम्स के लिये:SC दर्ज़ा के लिये मानदंड, 1950 का संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, भारत का महापंजीयक। मेन्स के लिये:SC दर्ज़ा पाने के लिये मानदंड और दलित ईसाइयों और मुसलमानों के समावेश के पक्ष और विपक्ष में तर्क। |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में,सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1950 के संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार की स्थिति की जानकारी मांगी है, जो केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्मों के सदस्यों को SC के रूप में मान्यता देने की अनुमति देता है।
याचिका में क्या है?
- दलित ईसाइयों और मुसलमानों को शामिल करने के लिये तर्क देने वाली याचिकाओं में कई स्वतंत्र आयोग की रिपोर्टों का हवाला दिया गया है, जिसमें भारतीय ईसाइयों और भारतीय मुसलमानों के बीच जाति एवं जाति असमानताओं के अस्तित्त्व का दस्तावेज़ीकरण किया गया है।
- याचिकाओं से पता चलता है कि SC के सदस्य धर्मांतरण के बाद भी उन्हीं सामाजिक बाधाओं का अनुभव करते हैं।
- याचिकाओं में इस प्रस्ताव के खिलाफ तर्क दिया गया है कि धर्मांतरण जाति की पहचान खो देती है, यह देखते हुए कि सिख धर्म और बौद्ध धर्म में भी जातिवाद मौजूद नहीं है और फिर भी उन्हें SC के रूप में शामिल किया गया है।
- विभिन्न रिपोर्टों और आयोग का हवाला देते हुए याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि धर्मांतरण के बाद भी जाति-आधारित भेदभाव जारी है, इसलिये इन समुदायों को SC का दर्जा दिया गया है।
1950 के संविधान आदेश में किसे शामिल किया गया है?
- अधिनियमित होने पर, वर्ष 1950 के संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश ने शुरू में अस्पृश्यता की प्रथा से उत्पन्न सामाजिक विकलांगता को संबोधित करने के लिये केवल हिंदुओं को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता देने का प्रावधान किया था।
- वर्ष 1956 में इस आदेश में संशोधन किया गया था ताकि सिख धर्म अपनाने वाले दलितों को शामिल किया जा सके और वर्ष 1990 में एक बार फिर बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलितों को शामिल किया जा सके। दोनों संशोधनों को वर्ष 1955 में काका कालेलकर आयोग और वर्ष 1983 में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर उच्चाधिकार प्राप्त पैनल (हप्प) की रिपोर्टों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी।
- केंद्र सरकार ने वर्ष 1936 की तत्कालीन औपनिवेशिक सरकार के 1936 के इंपीरियल ऑर्डर द्वारा बहिष्कार का हवाला देते हुए वर्ष 2019 में दलित ईसाइयों को अनुसूचित जातियों के सदस्यों के रूप में शामिल करने की संभावना को खारिज कर दिया था जिसने पहले दलित वर्गों की एक सूची को वर्गीकृत किया था और विशेष रूप से "भारतीय ईसाइयों" को इससे बाहर रखा था।
दलित ईसाइयों को बाहर रखने का कारण:
- भारत के महापंजीयक कार्यालय (RGI) ने सरकार को आगाह किया था कि अनुसूचित जाति का दर्जा अस्पृश्यता की प्रथा से उत्पन्न होने वाली सामाजिक अक्षमताओं से पीड़ित समुदायों के लिये है, जो कि हिंदू और सिख समुदायों में प्रचलित थी।
- इसने यह भी नोट किया कि इस तरह के कदम से देश भर में अनुसूचित जाति की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- वर्ष 2001 में RGI ने वर्ष 1978 के नोट का जिक्र किया और कहा कि दलित बौद्धों की तरह जो दलित इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए वे विभिन्न जाति समूहों के थे, न कि केवल एक जाति के, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें "एकल जातीय समूह" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। जिसे शामिल करने के लिये अनुच्छेद 341 के खंड (2) का पालन करना आवश्यक है।
- इसके अलावा RGI ने कहा कि चूँकि "अस्पृश्यता" की प्रथा हिंदू धर्म और उसकी शाखाओं की एक विशेषता थी, इसलिये दलित मुसलमानों एवं दलित ईसाइयों को SC के रूप में शामिल करने की अनुमति देने से "अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत समझा जा सकता है कि भारत ईसाइयों व मुसलमानों पर अपनी जाति व्यवस्था थोपने" की कोशिश कर रहा है।
- वर्ष 2001 के नोट में यह भी कहा गया है कि दलित मूल के ईसाई और मुस्लिम धर्मांतरण के कारण अपनी जातिगत पहचान खो चुके हैं एवं उनके नए धार्मिक समुदाय में अस्पृश्यता की प्रथा प्रचलित नहीं है।
धर्म-तटस्थ आरक्षण के पक्ष में तर्क:
- धर्म परिवर्तन से सामाजिक पहचान नहीं बदलती है।
- सामाजिक पदानुक्रम और विशेष रूप से जाति पदानुक्रम ईसाई धर्म व मुसलमानों के भीतर बना हुआ है, भले ही धर्म इसे मना करता है।
- उपरोक्त परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आरक्षण को धर्म से अलग करने की आवश्यकता है।
सरकार का इस मुद्दे पर विचार:
- वर्ष 1996 में सरकार सबसे पहले संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश में संशोधन के लिये एक विधेयक लाई जिसे पारित नहीं किया जा सका।
- सरकार ने कुछ ही दिनों में दलित ईसाइयों को अध्यादेश के माध्यम से अनुसूचित जाति के रूप में शामिल करने का प्रयास किया, जिसे भारत के राष्ट्रपति को भेजा गया था, लेकिन तब इसे प्रख्यापित नहीं किया जा सका।
- वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने RGI एवं तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की राय मांगी थी कि क्या दलित ईसाइयों को शामिल किया जा सकता है। दोनों ने प्रस्ताव के खिलाफ सिफारिश की थी।
- इसके अलावा समय-समय पर कई प्रयास किये गए लेकिन सभी विफल रहे।
अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु अन्य संवैधानिक प्रावधान:
- अनुच्छेद 15 (4) अनुसूचित जाति की उन्नति हेतु विशेष प्रावधानों को संदर्भित करता है।
- अनुच्छेद 16 (4A) के अनुसार, यदि राज्य के तहत प्रदत्त सेवाओं में अनुसूचित जाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो पदोन्नति के मामले में यह किसी भी वर्ग या पदों हेतु आरक्षण का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है।
- अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा समाज के कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहन तथा सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 335 यह प्रावधान करता है कि संघ और राज्यों के मामलों में सेवाओं एवं पदों पर नियुक्तियों हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावे को लगातार प्रशासनिक दक्षता के साथ ध्यान में रखा जाएगा।
- संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 क्रमशः लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों को आरक्षित करते हैं।
- पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX और नगर पालिकाओं से संबंधित भाग IXA में SC तथा ST के सदस्यों हेतु आरक्षण की परिकल्पना की गई है जो कि SC और ST को प्राप्त है।
स्रोत: द हिंदू
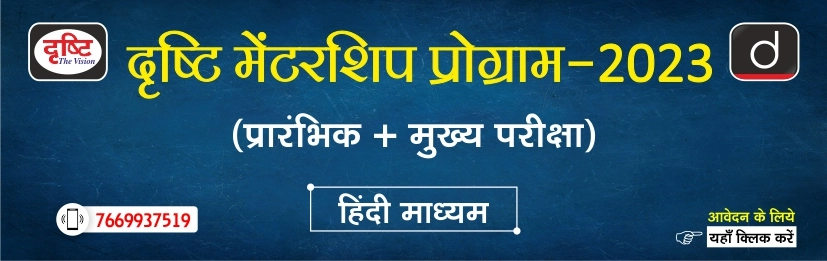
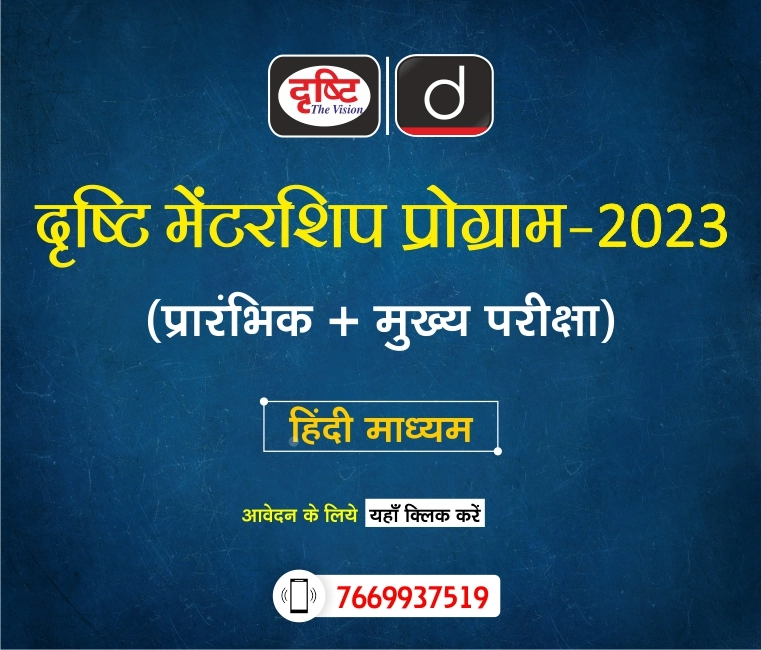
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
पर्यावरणीय मुद्दों को सुलझाने में नैनोमैटेरियल्स की भूमिका
प्रिलिम्स के लिये:नैनोमैटेरियल्स, कार्बन डॉट्स, नैनो टेक्नोलॉजी मेन्स के लिये:वैज्ञानिक नवाचार और खोज, नैनो टेक्नोलॉजी |
चर्चा में क्यों?
नैनोमैटेरियल्स या कार्बन डॉट्स (CD) जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग जल प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान में मदद कर सकता है।
- शहरी विकास ने जल निकायों में हानिकारक और ज़हरीले प्रदूषकों की शुरुआत के परिणामस्वरूप जलीय पर्यावरण की आधुनिक समाज की अखंडता को नष्ट कर दिया है।
- नैनो टेक्नोलॉजी जैसे आदर्श तकनीकी विकास टिकाऊ और कुशल पर्यावरणीय स्वच्छता के लिये अभिनव समाधान प्रदान करते हैं।
नैनो टेक्नोलॉजी/नैनो तकनीक:
- परिचय:
- नैनो टेक्नोलॉजी भौतिक घटनाओं का अध्ययन करने और 1 से 100 नैनोमीटर (NM) तक भौतिक आकार सीमा में नई सामग्री एवं उपकरणों की संरचना विकसित करने के लिये तकनीकों का उपयोग तथा विकास है।
- नैनो टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती है, जिसमें विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, पर्यावरण एवं ऊर्जा भंडारण, रासायनिक तथा जैविक प्रौद्योगिकियाँ और कृषि शामिल है।
- भारत में नैनो टेक्नोलॉजी:
- भारत में नैनोटेक्नोलॉजी के उद्भव ने अभिकर्त्ताओं के विविध समूह की भागीदारी देखी है, जिनमें से प्रत्येक का अपना एजेंडा और भूमिका है।
- वर्तमान में भारत में नैनो तकनीक ज़्यादातर सरकार के नेतृत्व वाली पहल है। उद्योग की भागीदारी हाल ही में शुरू हुई है।
- कुछ अपवादों को छोड़कर नैनो प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास बड़े पैमाने पर सार्वजनिक वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के साथ-साथ अनुसंधान संस्थानों में किया जा रहा है।
कार्बन डॉट्स:
- परिचय:
- CDs कार्बन नैनोमटेरियल समूह के सबसे नया सदस्यों में से एक हैं।
- इसे वर्ष 2004 में खोजा गया था और इसका औसत व्यास 10 नैनोमीटर से कम है।
- CD में उल्लेखनीय ऑप्टिकल गुण होते हैं, जो संश्लेषण के लिये उपयोग किये जाने वाले अग्रदूत के आधार पर विशिष्ट रूप से भिन्न होते हैं।
- यह अपने अच्छे इलेक्ट्रॉनदाताओं और ग्राह्यता के कारण सेंसिंग एवं बायोइमेजिंग जैसे अनुप्रयोगों में अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं।
- बायोइमेजिंग उन तरीकों से संबंधित है जो वास्तविक समय में जैविक प्रक्रियाओं की कल्पना करते हैं।
- इसके अलावा CDs सस्ती, अत्यधिक जैव-संगत और पर्यावरण के अनुकूल हैं।
- पर्यावरणीय मुद्दों के प्रबंधन में CDs की भूमिका:
- प्रदूषक संवेदन:
- CDs प्रतिदीप्ति (fluorescence) और वर्णमिति (colourimetric) पर्यावरण प्रदूषकों का पता लगाने के लिये एक उत्कृष्ट संभावना प्रदान करते हैं।
- ये अपने उच्च प्रतिदीप्ति उत्सर्जन के कारण प्रदूषक का पता लगाने के लिये एक फ्लोरोसेंट नैनोप्रोब के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किये जाते हैं।
- ये वर्णमिति (colourimetric) विधि द्वारा रंग परिवर्तन के साथ प्रदूषकों का पता लगाने में भी सक्षम बनाते हैं।
- प्रदूषक ग्राही (Contaminant Adsorption):
- यह प्रौद्योगिकी इनके छोटे आकार और बड़े विशिष्ट सतह क्षेत्र के कारण सतह पर प्रदूषक ग्राही की सुविधा दे सकती है।
- जल उपचार:
- CDs, जल उपचार के लिये भी उपयोगी हो सकते हैं क्योंकि इनसे पतली-फिल्म नैनोकम्पोज़िट झिल्ली के निर्माण द्वारा यह अन्य यौगिकों के साथ रासायनिक बंधन बना सकते हैं।
- जलकुंभी अपशिष्ट से CDs का उत्पादन किया गया है, जो UV प्रकाश के तहत हरी प्रतिदीप्ति प्रदर्शित करते हैं। जलीय निकायों के लिये नुकसानदायक वनस्पतियों का पता लगाने के लिये ये फ्लोरोसेंट सेंसर भी साबित हुए हैं ।
- प्रदूषक पदार्थों में गिरावट:
- यह प्रौद्योगिकी अगली पीढ़ी के फोटोकैटलिसिस के लिये अत्याधुनिक दृष्टिकोण प्रदान करके प्रदूषक निराकरण के लिये भी उपयोगी हो सकती है।
- फोटोकैटलिसिस में प्रकाश और अर्धचालक का उपयोग करके होने वाली प्रतिक्रियाएँ शामिल हैं।
- प्रदूषित पानी में कार्बनिक प्रदूषक इलेक्ट्रॉन और होल (hole) स्थानांतरित करने वाले एजेंटों के रूप में कार्य कर सकते हैं, जबकि कार्बन डॉट्स फोटोसेंसिटाइज़र के रूप में कार्य करते हैं।
- यह प्रौद्योगिकी अगली पीढ़ी के फोटोकैटलिसिस के लिये अत्याधुनिक दृष्टिकोण प्रदान करके प्रदूषक निराकरण के लिये भी उपयोगी हो सकती है।
- रोगाणुरोधी:
- CDs के रोगाणुरोधी तंत्र में मुख्य रूप से- भौतिक / यांत्रिक विनाश, ऑक्सीडेटिव तनाव, फोटोकैटालिटिक प्रभाव और जीवाणु चयापचय का निषेध आदि शामिल हैं।
- दृश्य या प्राकृतिक प्रकाश के तहत बैक्टीरिया सेल के संपर्क में CDs कुशलतापूर्वक प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियाँ उत्पन्न कर सकते हैं।
- यह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (डीएनए) या राइबोन्यूक्लिक एसिड (आरएनए) को नुकसान पहुँचा सकता है, जिससे बैक्टीरिया की मृत्यु हो सकती है।
- प्रदूषक संवेदन:
कार्बन डॉट्स के ग्रीन संश्लेषण का वर्गीकरण:
- आम तौर पर कार्बन डॉट्स के संश्लेषण को "टॉप-डाउन" और "बॉटम-अप" विधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- टॉप-डाउन विधि लेज़र पृथक्करण, चाप निर्वहन और रासायनिक या विद्युत रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा बड़े कार्बन संरचनाओं को क्वांटम आकार के कार्बन डॉट्स में परिवर्तित करती है।
- बॉटम-अप विधि में सीडी पायरोलिसिस, कार्बोनाइज़ेशन, हाइड्रोथर्मल प्रक्रियाओं या माइक्रोवेव-असिस्टेड संश्लेषण द्वारा छोटे अणु अग्रदूतों को कार्बोनाइज़ करने से उत्पन्न होती है।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रश्न. स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो तकनीक के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2015)
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: c व्याख्या:
प्रश्न: नैनो तकनीक से आप क्या समझते हैं और यह स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे मदद कर रही है? (मुख्य परीक्षा, 2020) |
स्रोत: डाउन टू अर्थ