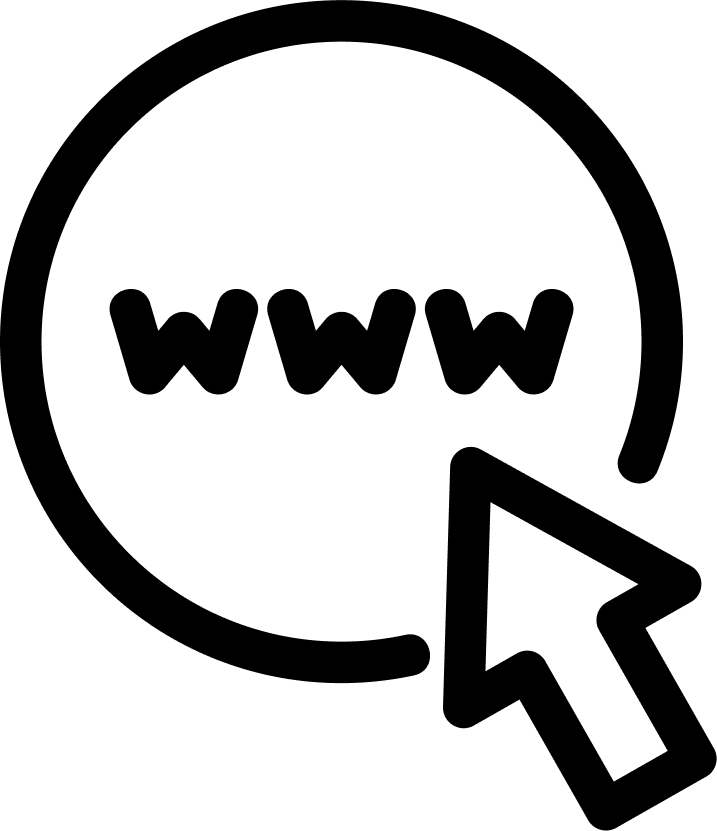हिंदी भाषा और ज्ञान-विज्ञान की यात्रा
- 10 Sep, 2021 | प्रवीण झा

हाल में एक विद्यार्थी का संदेश मिला कि यूरोप पर और खास कर रोमन सभ्यता पर हिंदी में एक अच्छी किताब बता दूँ। समस्या यह है कि मैं स्वयं इतिहास की किताबों के लिये अंग्रेज़ी किताबों का ही रुख करता हूँ। जो लिखता हूँ, वह उनसे बने आधार पर और कुछ अपनी समझ से लिखता हूँ। इसका अर्थ यह नहीं कि हिंदी में कुछ लिखा नहीं गया। मैंने उन्हें लालबहादुर वर्मा जी की लिखी यूरोप और आधुनिक विश्व का इतिहास सुझा दी, और कहा कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे मित्रों से संपर्क कर लें। और भी किताबें होंगी। इस मध्य मैं स्वयं रोमन सभ्यता पर किताबें जुटा रहा था, तो सोचा कम से कम एक हिंदी में लिखी किताब भी पढ़ लूँ। अनूदित नहीं, मूल रूप से हिंदी में लिखी। अब डिजिटल युग है तो बड़ी सुविधा से एक ‘रोम का इतिहास’ नामक पुस्तक मिल गयी, जो 1928 ई. में प्राणनाथ विद्यालंकार जी ने लिखी थी।
इस पुस्तक में लगभग दो सौ पृष्ठ थे और एक रुपया दाम था। यह काशी नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से प्रयाग के इंडियन प्रेस से छपी थी। यह किताब पढ़ कर लगा कि इतनी सहज हिंदी में इतने कम पृष्ठों में पूरे रोमन इतिहास को समेटना दुष्कर कार्य रहा होगा। इसके लिये एक नहीं, दर्जनों किताबें पढ़ी गई होंगी। मैंने काशी नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से प्रकाशित मनोरंजन पुस्तकमाला की अन्य किताबें ढूँढनी शुरू की, तो पचास से अधिक किताबें मिल गईं। जर्मनी- चीन विषयक से लेकर भौतिक विज्ञान, तर्कशास्त्र, कृषि विज्ञान, धर्म, जीवनियाँ, भूगोल, गणित इत्यादि विषयों पर किताबें मिलीं। ताज्जुब यह कि कथा या कविताएँ नहीं मिली, या मेरी नज़र में नहीं आई। इस पर आश्चर्य इस कारण हुआ क्योंकि आज हिंदी साहित्य उपन्यासों और कविताओं से समृद्ध है। हर साल दर्जनों किताबें बड़े प्रकाशनों से छपती हैं। किंतु भूगोल या गणित या तकनीकी पर कितनी किताबें छपती होंगी? आखिर उन्नीसवीं सदी में या बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा कि पूरा ध्यान ज्ञान-विज्ञान पर हो गया? उस समय तो पश्चिम में भी विज्ञान उन्नत नहीं था, फिर इतनी सरदर्दी क्यों ली गई?
यह भारत का नवजागरण काल था, जब भारतीयों पर यह हीन-भावना थोपी जा रही थी कि भारतीय भाषों में कुछ भी ज्ञान-विज्ञान विषयक नहीं है। इस कारण अंग्रेज़ी भाषा की किताबें पढ़नी ही होगी। यह आरोप पूरी तरह ग़लत नहीं था क्योंकि विज्ञान की भाषा वाकई अंग्रेज़ी ही होती जा रही थी। उत्तर भारत के प्रमुख क्षेत्रों में कचहरी की भाषा फ़ारसी थी। मिला-जुला कर नागरी लिपि का प्रयोग सीमित था, और इसे सीखने की प्रतिबद्धता नहीं थी।
उन्हीं दिनों बनारस के क्वींस कॉलेज के कुछ विद्यार्थी छात्रावास में मिले कि नागरी लिपि के लिये कुछ किया जाए। ये लोग नौवीं से इंटरमीडिएट कक्षा के विद्यार्थी रहे होंगे। 9 जुलाई, 1893 को बाबू हरिदास बुआसाव के घर पर बाबू श्यामसुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिवकुमार सिंह जमा हुए। उस समय तक दयानंद सरस्वती के आर्यसमाजी भी हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार कर रहे थे। बैठक में एक खाका बना कि नागरी लिपि को कचहरी में शामिल किया जाए, और इस लिपि में यथासंभव ज्ञान-विज्ञान लिखा जाए। ऐसी चीजें लिखी जाएँ, जिसके लिये लोग अंग्रेज़ी का रुख करते हैं।
उस समय ब्रिटिश सरकार यह विचार कर रही थी कि कचहरी की भाषा फ़ारसी से बदल कर रोमन लिपि में कर दी जाए। इससे हिंदू और मुसलमान, दोनों ही शंकित हुए। उन्होंने अर्जियाँ लगायी कि उर्दू और नागरी को बिहार से लेकर उत्तर-पश्चिम प्रांत की कचहरियों में शामिल किया जाए। इसी तरह बंगाली, मराठी आदि भाषाओं ने भी मुहिम चलाई। कथित रूप से बाबू राधाकृष्ण दास ने सौगंध खाई-
“अगर हिंदी भाषा का कचहरियों और स्कूलों में प्रसार हो गया तो मैं प्रयाग के संगम में नहा कर दूध चढ़ाऊँगा”
आखिर 1900 ई. में प्रांत के गवर्नर एंटोनी मकडॉनेल ने कचहरी में नागरी और फारसी के प्रयोग पर मुहर लगा दी। लेकिन, अधिकांश मुंशी फ़ारसी या अंग्रेज़ी ही जानते थे, नागरी उनके लिये सहज नहीं थी। न ही नागरी में कोई तकनीकी शब्दकोश उपलब्ध था। पत्र-पत्रिकाएँ भी कम थीं। उसी वर्ष (1900 ई.) एक ‘सरस्वती’ नामक पत्रिका छपनी शुरू हुई, और दो वर्ष बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने।
वहीं, रामचंद्र शुक्ल और अमीर सिंह जैसे विद्वतजन हिंदी का शब्दकोश (हिंदी शब्दसागर) निर्माण करने लगे। एक दशक से अधिक के बाद 1913-14 में ही एक 96 पृष्ठ का पतला शब्दकोश छप सका। आज की हिंदी में भले ही लाखों शब्दों की दुहाई दी जाती है, लेकिन इसके बनने की प्रक्रिया का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। कई शब्द गढ़े जा रहे थे। संस्कृत, फ़ारसी और स्थानीय भाषाओं से लिये जा रहे थे। अंग्रेज़ी के तकनीकी शब्दों के नए अनुवाद के साथ कोष्ठक में मूल शब्द सहूलियत के लिये लिखा होता।
राजा शिवप्रसाद ‘सितारा-ए-हिंद’ ने विज्ञान पर आधारित एक सरल पुस्तक लिखी- ‘विद्यांकुर’। उन्होंने ही भूगोल पर आधारित ‘भूगोल हस्तामलक’ भी लिखी। ऐसा नहीं कि ये इनके विशेषज्ञ थे, किंतु इन्होंने विशद अध्ययन कर ये कुंजियाँ तैयार की। विद्यार्थियों को भी ये किताबें अंग्रेज़ी के बनिस्बत सुलभ लगी और एक-एक किताब की तीन हज़ार से अधिक प्रतियाँ बिक गईं। उनके अतिरिक्त ओंकार भट्ट, बालकृष्ण शास्त्री और अम्बिका प्रसाद जैसे लोगों ने भी विज्ञान पर किताबें लिखी। अमीर सिंह ने रसखान और घनानंद के जीवन पर आधारित पुस्तक लिखी। तमाम इतिहास लिखे जाने शुरू हुए। संस्कृत, फ़ारसी और अंग्रेज़ी किताबों के अनुवाद शुरू हुए। महज दो दशकों में हिंदी के ज्ञान-विज्ञान की किताबों का जखीरा बन गया।
अगर इसी गति और इतने ही शोध से हिंदी में किताबें लिखी जातीं, तो लोग ढूँढ कर डायनासोर विषय में पढ़ने के लिये हिंदी किताबें जोहते। मगर न जाने कब यह धारा साहित्य और कुछ समाजशास्त्र पुस्तकों तक सिमटती चली गई। तकनीकी, चिकित्सकीय और भूगोल आदि की किताबें घटने लगीं। बड़े प्रकाशकों की यह शिकायत भी रही कि इन विषयों की पांडुलिपियाँ कम आती हैं। कथा खूब गढ़े जाते हैं, शोध कर उपन्यास लिखे जाते हैं; लेकिन भारतीय इतिहास पढ़ने के लिये भी इंतजार करना पड़ता है कि रामचंद्र गुहा की पुस्तक का अनुवाद आ जाए। जब तक हिंदी में युद्ध स्तर पर, सहज भाषा में, और ज्ञान-विज्ञान विषयक लेखन नहीं होगा, तब तक यह घरेलू भाषा ही रह जाएगी। कामकाजी भाषा नहीं बनेगी। जब तक कामकाजी भाषा नहीं बनेगी, पूंजी और नौकरियाँ इनसे नहीं जुड़ पाएगी। न ही बनारस के छात्रावास में बैठे उन छात्रों का स्वप्न पूरा होगा जो उन्होंने एक सदी पूर्व देखा था।
 |
प्रवीण झा (लेखक नॉर्वे में डॉक्टर हैं तथा लोकप्रिय पुस्तक 'कुली लाइन्स' के लेखक हैं) |