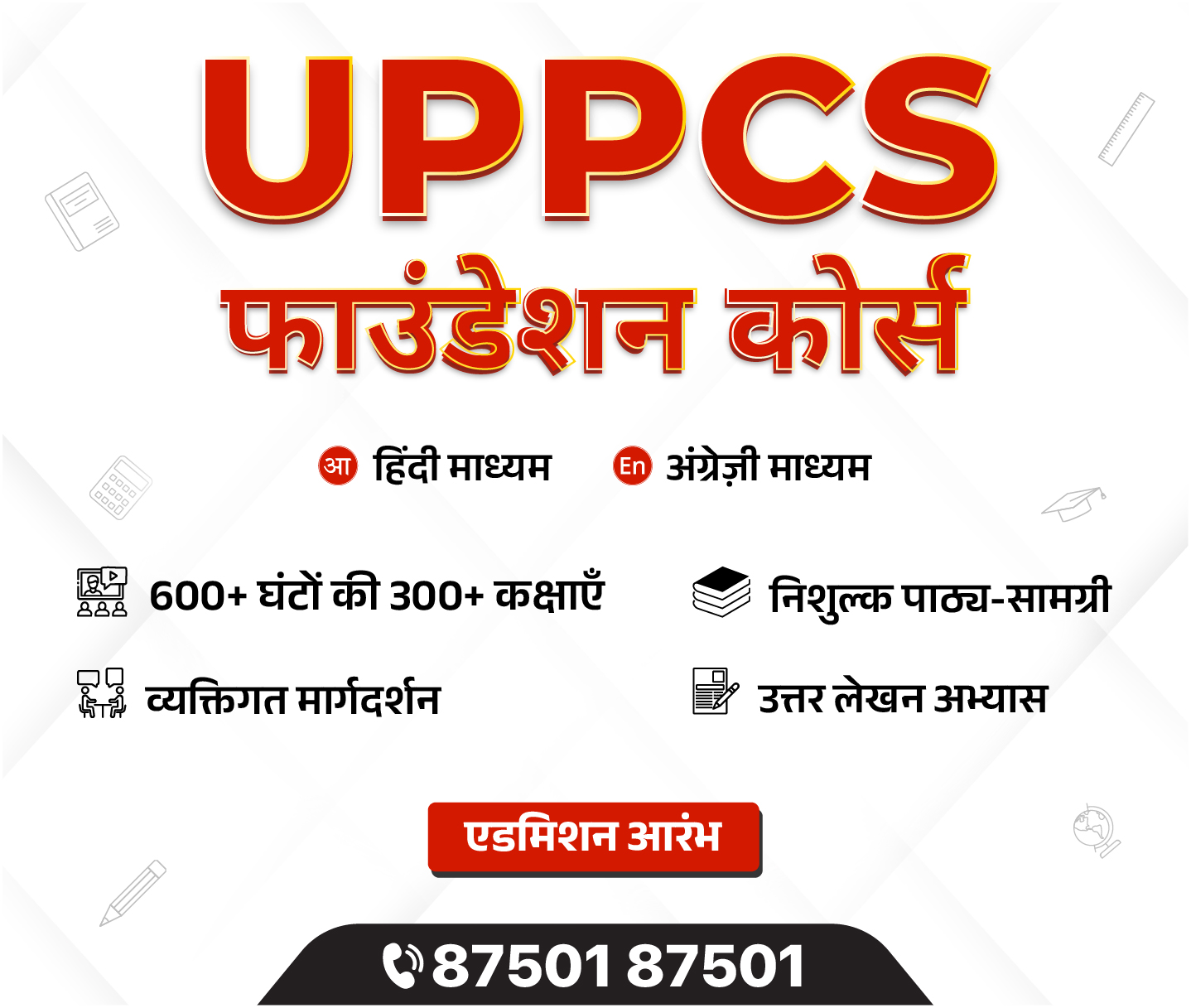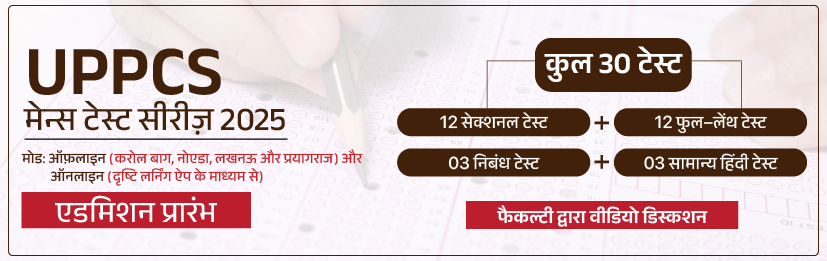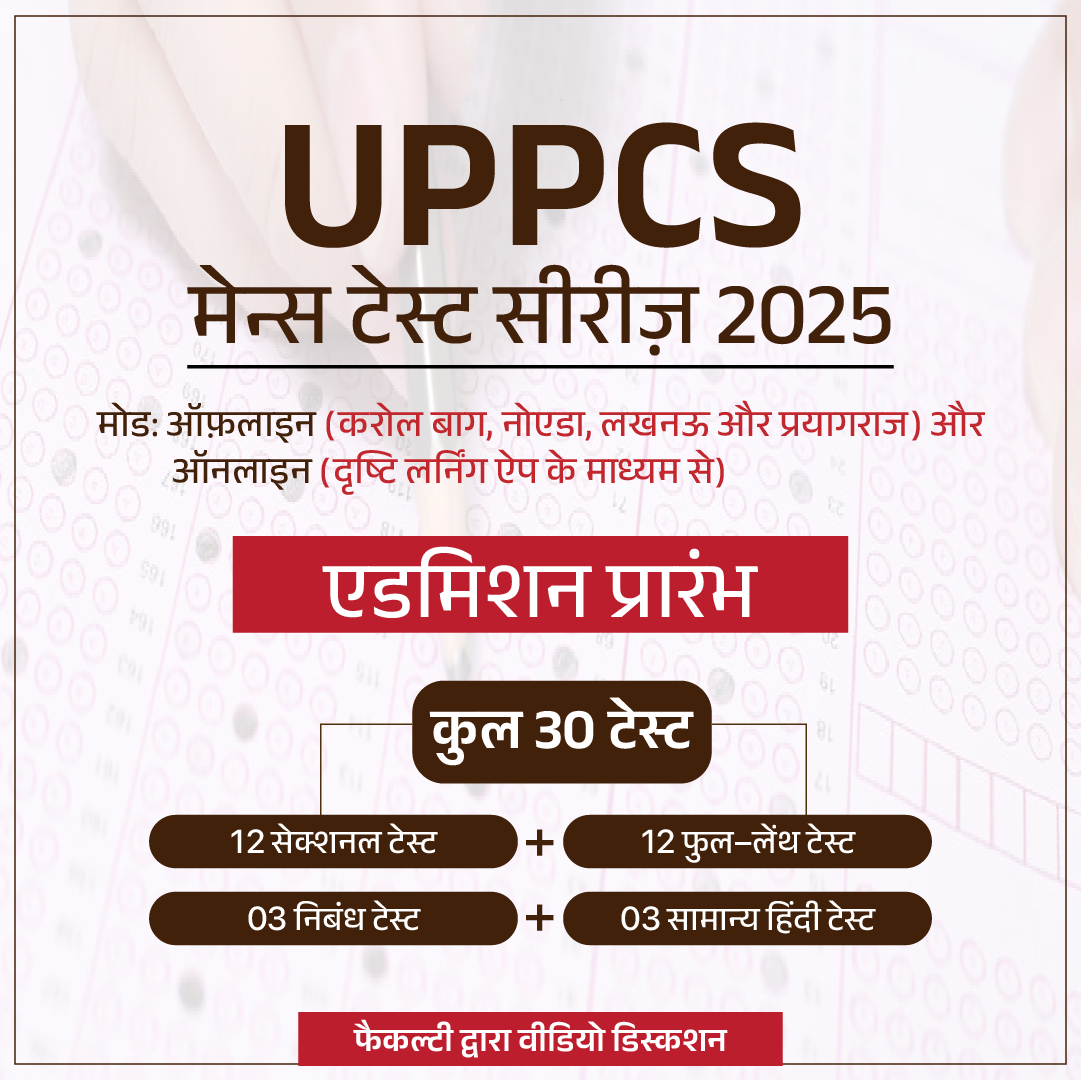उत्तर प्रदेश Switch to English
उत्तर प्रदेश बजट 2026-27
चर्चा में क्यों?
11 फरवरी, 2026 को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये उत्तर प्रदेश राज्य बजट प्रस्तुत किया। यह बजट वर्ष 2029 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने के लिये एक रणनीतिक रोडमैप के रूप में कार्य करता है।
मुख्य बिंदु:
- वर्ष 2026–27 के लिये कुल बजट अनुमान: ₹9,12,696.35 करोड़, जो पिछले वर्ष के बजट की तुलना में लगभग 12.2–12.9% अधिक है।
- पूंजीगत व्यय: परिसंपत्ति निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय बदलाव देखा गया है। कुल परिव्यय का 19.5% (लगभग ₹1.78 लाख करोड़) दीर्घकालिक आर्थिक विकास को मज़बूत करने हेतु निर्धारित किया गया है।
- राजस्व व्यय: मुख्यतः प्रशासनिक व्यय, वेतन और ब्याज भुगतान को शामिल करता है।
- वर्ष 2026–27 के लिये इसका अनुमान लगभग ₹5.83 लाख करोड़ है।
- राजकोषीय घाटे की सीमा: GSDP का 3%, जो 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है और वर्ष 2030–31 तक प्रभावी रहेगा।
- ऋण–GSDP लक्ष्य: राज्य वित्तीय स्थिरता पर ज़ोर देते हुए वित्त वर्ष के अंत तक ऋण अनुपात को घटाकर लगभग 23.1% करने का लक्ष्य रखता है।
- GSDP: ₹30.25 लाख करोड़ आँकी गई है, जिसमें 13.4% की वृद्धि अनुमानित है।
- प्रति व्यक्ति आय: ₹54,564 (2016-17) से बढ़कर ₹1,09,844 हो गया, वर्ष 2025-26 में ~₹1,20,000 तक पहुँचने की उम्मीद है।
- गरीबी एवं रोज़गार: लगभग 6 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाले गए और बेरोज़गारी दर 2.24% है।
- ये आँकड़े राज्य के तीव्र आर्थिक विस्तार और विकास पथ को दर्शाते हैं।
- अवसंरचना (कुल परिव्यय का 25%):
- नॉर्थईस्ट कॉरिडोर: गोरखपुर से सहारनपुर को जोड़ने वाले उच्च-गति कॉरिडोर के लिये ₹34,000 करोड़।
- जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा: वैश्विक संपर्क बढ़ाने हेतु पाँच रनवे तक विस्तार।
- एक्सप्रेसवे: पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ने के लिये गंगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हेतु निरंतर वित्तपोषण।
- शिक्षा एवं युवा सशक्तीकरण (12.4%):
- स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना: 5 मिलियन टैबलेट/स्मार्टफोन का वितरण।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना: युवा उद्यमियों को ₹5 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण।
- नए विश्वविद्यालय: तीन नए विश्वविद्यालय और 16 नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा।
- कृषि एवं किसान समृद्धि (9–12%):
- सिंचाई: निजी नलकूपों के लिये मुफ्त विद्युत की व्यवस्था जारी।
- गन्ना: वर्ष 2025–26 के लिये गन्ना मूल्य में ₹30 प्रति क्विंटल की वृद्धि, जिससे किसानों की आय में ₹3,000 करोड़ की बढ़ोतरी।
- महिला कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा:
- कन्या सुमंगला योजना: 26.81 लाख से अधिक बालिकाएँ लाभान्वित; बेटी के विवाह हेतु अनुदान ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख।
- सेफ सिटी परियोजनाएँ: CCTV नेटवर्क और एंटी-रोमियो स्क्वॉड का विस्तार।
- छात्राओं एवं कामकाजी महिलाओं की गतिशीलता बढ़ाने के लिये विशेष स्कूटी योजना हेतु ₹400 करोड़ का प्रावधान।
- महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिये विशेष कौशल विकास केंद्रों की स्थापना।
- परिवारों एवं अल्पसंख्यकों को समर्थन:
- गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह सहायता हेतु ₹150 करोड़ का प्रावधान (सामाजिक सुरक्षा तंत्र का हिस्सा)।
- समावेशी विकास लक्ष्यों के अनुरूप सामाजिक कल्याण पर विशेष ज़ोर।
- औद्योगिक एवं तकनीकी नेतृत्व:
- विनिर्माण केंद्र: उत्तर प्रदेश अब भारत के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65% करता है और देश की 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयाँ यहाँ स्थित हैं।
- रोज़गार मिशन: 10 लाख युवाओं के लिये घरेलू और विदेशी रोज़गार अवसर बढ़ाने हेतु उत्तर प्रदेश रोज़गार मिशन की स्थापना।
- ऊर्जा संक्रमण: स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 2,815 मेगावाट तक पहुँची और वर्ष 2016 से तापीय क्षमता में 55% से अधिक की वृद्धि।

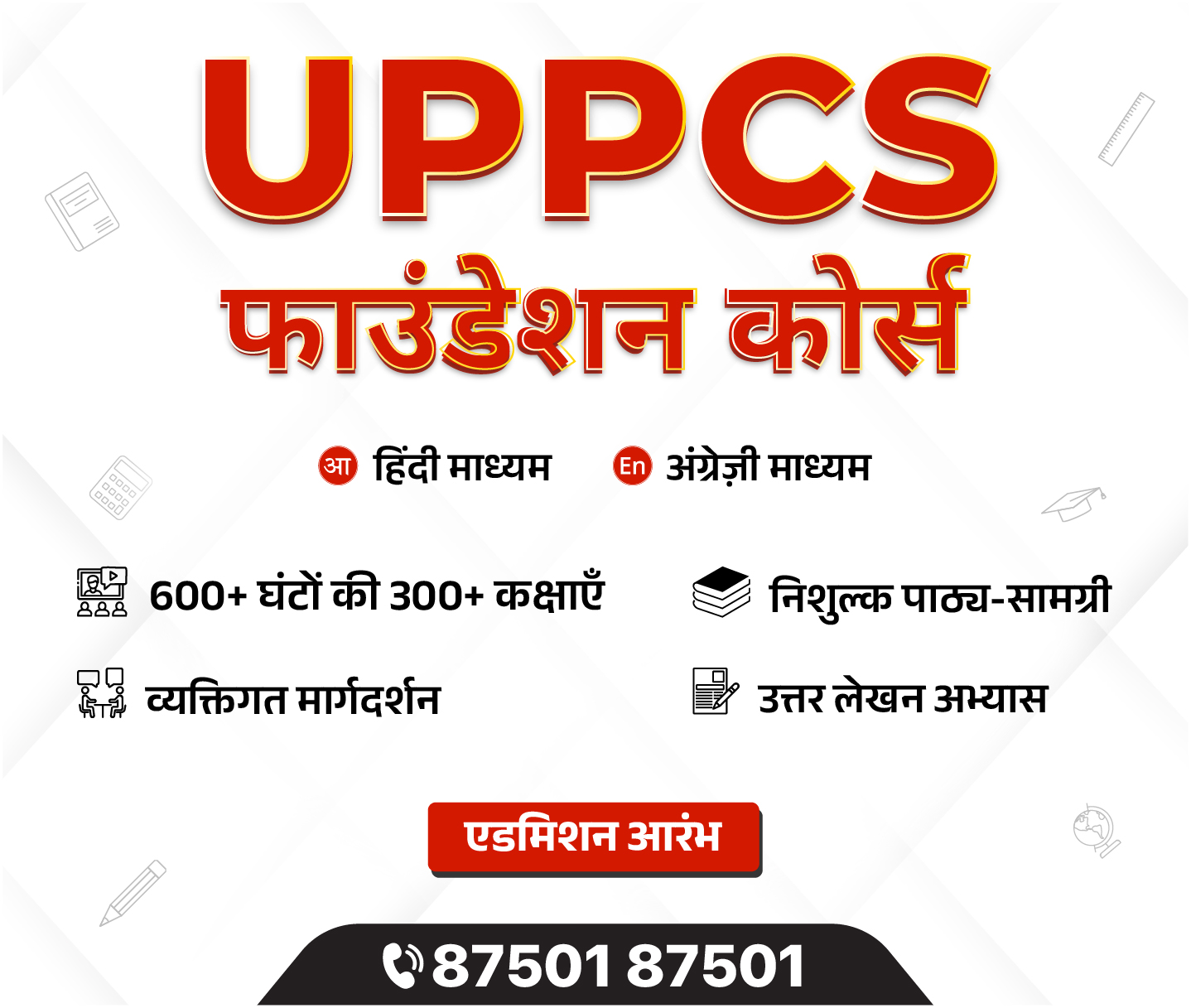
राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स Switch to English
जर्मनी में BIOFACH 2026 में भारत को ‘कंट्री ऑफ द ईयर’ चुना गया
चर्चा में क्यों?
भारत को फरवरी 2026 में जर्मनी के नूर्नबर्ग में आयोजित होने वाले जैविक उत्पादों के विश्व के अग्रणी व्यापार मेले BIOFACH 2026 में ‘कंट्री ऑफ द ईयर’ (Country of the Year) का प्रतिष्ठित खिताब प्रदान किया गया है।
मुख्य बिंदु:
- कार्यक्रम: BIOFACH 2026 जर्मनी में आयोजित होने वाला जैविक उत्पादों का विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है।
- भारत को वैश्विक मंच पर अपनी जैविक कृषि की ताकत और निर्यात क्षमता को मान्यता देते हुए आधिकारिक रूप से ‘कंट्री ऑफ द ईयर’ घोषित किया गया है।
- आयोजन प्राधिकरण: भारत की भागीदारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा आयोजित की जा रही है।
- पैन-इंडिया प्रतिनिधित्व: 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रदर्शक भाग ले रहे हैं, जो भारत की कृषि तथा क्षेत्रीय विविधता को प्रदर्शित करते हैं।
- उत्पाद: यहाँ चावल, तिलहन, दलहन, मसाले, जड़ी-बूटियाँ, काजू, अदरक, हल्दी, बड़ी इलायची, दालचीनी, आम प्यूरी, आवश्यक तेल तथा अन्य मूल्यवर्द्धित जैविक उत्पादों की विस्तृत शृंखला प्रदर्शित की जा रही है।
- निर्यात प्रोत्साहन: यह आयोजन भारतीय जैविक निर्यातकों को वैश्विक खरीदारों से जुड़ने, बाज़ार तक पहुँच बढ़ाने और वैश्विक जैविक बाज़ार में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है।
- महत्त्व: BIOFACH में ‘कंट्री ऑफ द ईयर’ के रूप में भारत की पहचान उसकी जैविक कृषि में नेतृत्व भूमिका, बढ़ते निर्यात प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संधारणीय कृषि पद्धतियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
|
और पढ़ें: APEDA, कृषि, संधारणीय कृषि पद्धतियाँ |
राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स Switch to English
विशाखापत्तनम में ऐतिहासिक समुद्री संगम
चर्चा में क्यों?
पहली बार भारत एक साथ तीन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री आयोजनों—अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा (International Fleet Review–IFR) 2026, अभ्यास मिलन 2026 और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) के नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
मुख्य बिंदु:
- स्थल: विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश — भारत की पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय और एक रणनीतिक समुद्री प्रवेश द्वार।
- मुख्य आयोजन: यह पहली बार होगा जब भारत इन तीनों प्रमुख समुद्री आयोजनों की मेज़बानी एक साथ कर रहा है।
- IFR 2026: 18 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू युद्धपोतों के एक विशाल बेड़े की समीक्षा करेंगी, जिसमें INS विक्रांत जैसे पोतों के साथ भारत की ‘बिल्डर नेवी’ को प्रदर्शित किया जाएगा।
- अभ्यास मिलन 2026: मिलन भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें पेशेवर आदान-प्रदान, सामरिक अभ्यास और संयुक्त समुद्री अभियानों को शामिल किया जाता है।
- IONS सम्मेलन: भारत वर्ष 2025–2027 की अवधि के लिये अध्यक्षता सॅंभाल रहा है और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिये 25 से अधिक देशों की मेज़बानी कर रहा है।
- भागीदारी: 50-70 से अधिक देशों के युद्धपोतों और विमानों के भाग लेने की उम्मीद है, जो प्रमुख समुद्री शक्तियों तथा क्षेत्रीय साझेदारों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- वैश्विक उपस्थिति: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, श्रीलंका, ईरान, यूनाइटेड किंगडम, यूएई, दक्षिण अफ्रीका सहित कई देश इसमें भाग लेंगे, जो व्यापक कूटनीतिक सहभागिता को दर्शाता है।
|
और पढ़ें: अभ्यास मिलन, हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी |


%20(1).gif)
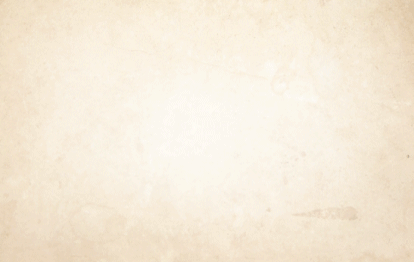

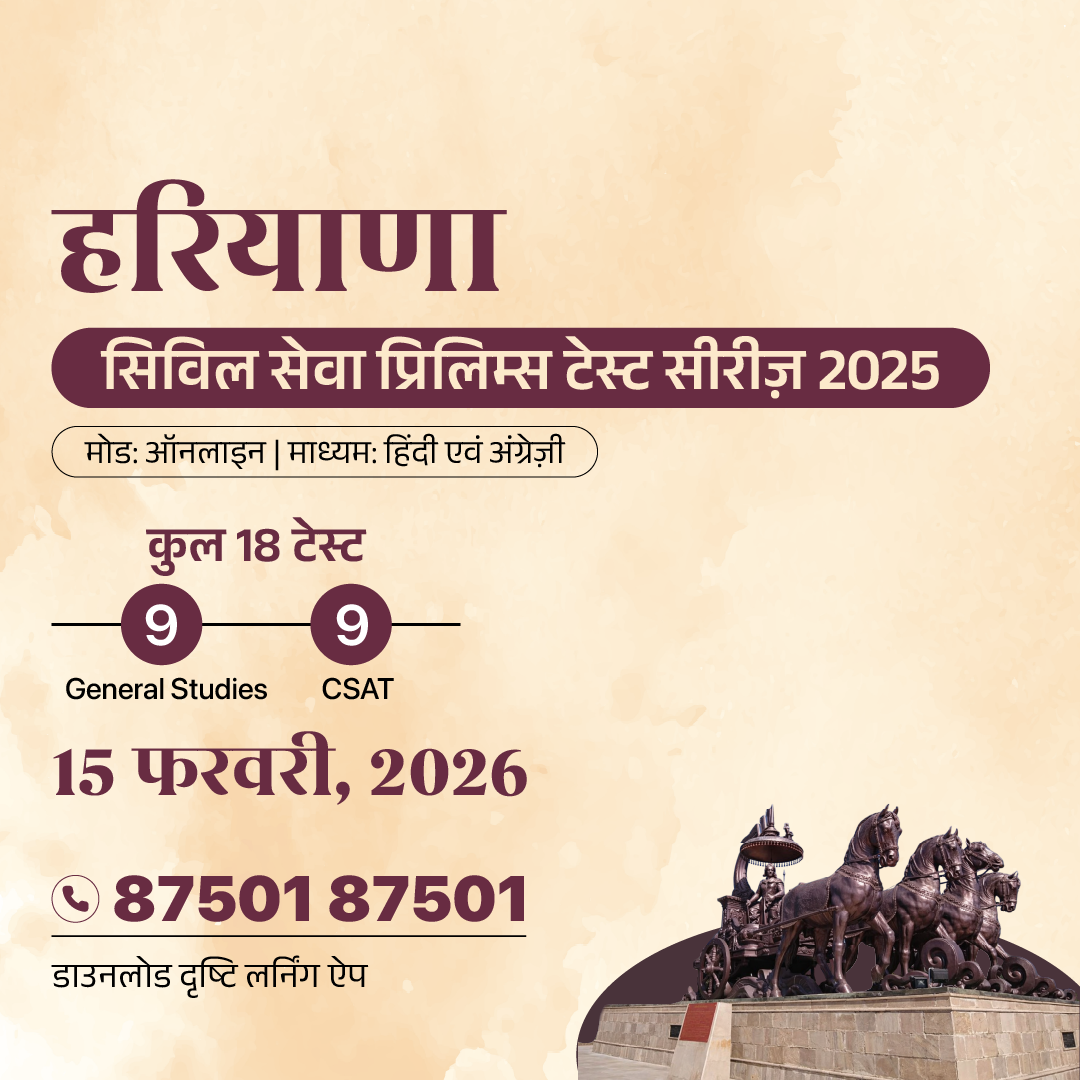
.jpg)