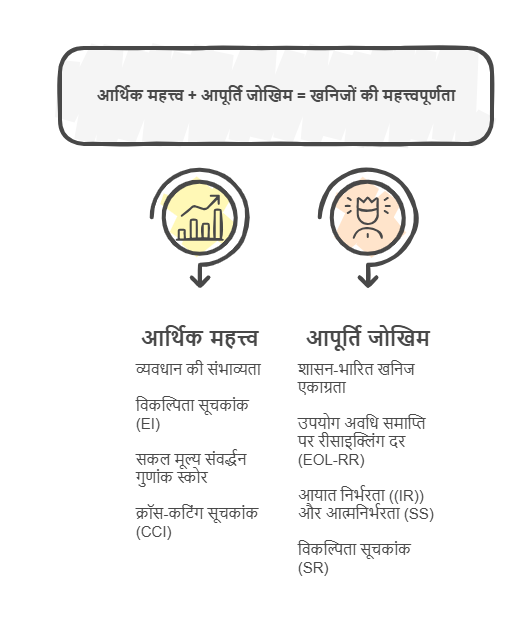भारतीय अर्थव्यवस्था
भारत के महत्त्वपूर्ण खनिज का भविष्य सुरक्षित करना
- 09 Sep 2025
- 156 min read
यह संपादकीय “ए क्रिटिकल मिशन: रीसाइक्लिंग क्रिटिकल मिनरल्स कैन ऑफर नियर-टर्म कुशन” पर आधारित है, जो 09/09/2025 को द बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित हुआ था। इस लेख में केंद्र सरकार की ₹1,500 करोड़ की योजना (2025-31) को सामने लाया गया है, जिसका उद्देश्य लिथियम, कोबाल्ट, निकल एवं रेयर अर्थ जैसे महत्त्वपूर्ण खनिजों की रीसाइक्लिंग क्षमता विकसित करना है, ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके और ई-वेस्ट का प्रबंधन किया जा सके।
प्रिलिम्स के लिये: महत्त्वपूर्ण खनिज, राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2025 (MMDR अधिनियम), ओडिशा की नीयामगिरि पहाड़ियाँ
मेन्स के लिये: भारत द्वारा अपने महत्त्वपूर्ण खनिज पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु उठाए गए कदम, भारत के महत्त्वपूर्ण खनिज पारिस्थितिकी तंत्र से सबंधित प्रमुख समस्याएँ
भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) की रीसाइक्लिंग क्षमता विकसित करने हेतु ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंज़ूरी दी है, जो सत्र 2025-26 से सत्र 2030-31 तक चलेगी। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और उन्नत विनिर्माण के लिये आवश्यक लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर-अर्थ तत्त्वों पर भारत की भारी आयात निर्भरता को कम करना है। जहाँ खनन परियोजनाओं को परिणाम देने में वर्षों लगते हैं, वहीं रीसाइक्लिंग आपूर्ति शृंखलाओं को तुरंत प्रबलता प्रदान करने के साथ-साथ बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी अपशिष्ट के प्रबंधन का एक तरीका प्रदान करती है। यह रीसाइक्लिंग पहल भारत की खनिज सुरक्षा के लिये बहुआयामी रणनीति का महत्त्वपूर्ण स्तंभ है, जो घरेलू खोज, विदेशी अधिग्रहण और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने के व्यापक लक्ष्य को भी सुदृढ़ता प्रदान करती है।
भारत ने अपने महत्त्वपूर्ण खनिज पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु कौन-से कदम उठाए हैं?
- घरेलू अन्वेषण और खनन: भविष्य की आपूर्ति सुनिश्चित करना: भारत आयात पर निर्भरता कम करने के लिये अपने घरेलू अन्वेषण प्रयासों का आक्रामक रूप से विस्तार कर रहा है।
- सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (NCMM) के अंतर्गत वर्ष 2030 तक 1,200 महत्त्वपूर्ण खनिज भंडारों की पहचान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
- यह प्रयास भारत की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूर्ण करता है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा और EV उत्पादन के लिये आवश्यक लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ जैसे खनिज शामिल हैं।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने वर्ष 2024-25 में पहले ही 195 अन्वेषण परियोजनाएँ शुरू की हैं, जिनका फोकस राजस्थान जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रेयर अर्थ तत्त्वों पर है।
- भारत वर्ष 2031 तक 100 से अधिक महत्त्वपूर्ण खनिज खंडों की नीलामी करने की उम्मीद कर रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश में कोबाल्ट और जम्मू-कश्मीर में लिथियम जैसे अब तक अप्रयुक्त भंडारों पर रणनीतिक फोकस होगा।
- सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (NCMM) के अंतर्गत वर्ष 2030 तक 1,200 महत्त्वपूर्ण खनिज भंडारों की पहचान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
- रीसाइक्लिंग और अर्बन माइनिंग: महत्त्वपूर्ण खनिजों का रीसाइक्लिंग, विशेषकर ई-वेस्ट और उपयोग हो चुकी बैटरियों से, भारत की रणनीति का केंद्रीय हिस्सा बन गया है।
- NCMM के तहत ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य 270 किलोटन रीसाइक्लिंग क्षमता स्थापित करना है, जिससे प्रतिवर्ष 40 किलोटन महत्त्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति हो सके।
- यह पहल केवल नई खनन पर निर्भरता को कम नहीं करती बल्कि बढ़ती हुई ई-वेस्ट की समस्या से भी निपटती है।
- इस योजना से 70,000 नौकरियाँ सृजित होंगी और ₹8,000 करोड़ के निवेश आकर्षित होंगे, जो भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकॉनमी) की ओर बढ़ते कदम को प्रदर्शित करता है।
- साथ ही वित्त वर्ष 2028 तक सभी नए गैर-लौह/अलौह उत्पादों में 5% रीसाइक्लिंग सामग्री शामिल किये जाने की भारत की योजना, सरकार के रीसाइक्लिंग क्षमता बढ़ाने के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती है।
- NCMM के तहत ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य 270 किलोटन रीसाइक्लिंग क्षमता स्थापित करना है, जिससे प्रतिवर्ष 40 किलोटन महत्त्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति हो सके।
- अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियाँ: भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से महत्त्वपूर्ण खनिजों तक दीर्घकालिक अभिगम्यता सुनिश्चित कर रहा है, जिससे भू-राजनीतिक व्यवधानों के जोखिम को कम किया जा सके।
- खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) के माध्यम से, भारत ने लिथियम और कोबाल्ट अन्वेषण अधिकारों के लिये अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ समझौते किये हैं।
- जनवरी 2024 में, KABIL ने अर्जेंटीना के साथ पाँच लिथियम-समृद्ध खंडों का अन्वेषण करने के लिये एक समझौता किया।
- यह साझेदारी भारत को लिथियम की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता करेगी, जिससे घरेलू उत्पादन में अंतर को पूरा किया जा सके और लिथियम प्रसंस्करण में प्रभुत्व रखने वाले चीन पर निर्भरता कम हो।
- प्रौद्योगिकीय नवाचार और अनुसंधान एवं विकास: भारत महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये निष्कर्षण, प्रसंस्करण एवं रीसाइक्लिंग तकनीकों में सुधार हेतु अनुसंधान और विकास में भारी निवेश कर रहा है।
- NCMM का लक्ष्य वर्ष 2030 तक महत्त्वपूर्ण खनिज तकनीकों में 1,000 पेटेंट दर्ज करना है, जिससे पूरे मूल्य शृंखला में नवाचार को प्रोत्साहन प्राप्त हो।
- उदाहरण के लिये, भारत ने पहले ही नई निष्कर्षण तकनीकों के लिये पेटेंट प्रदान किये हैं, जो आयात पर निर्भरता कम कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, 7 उत्कृष्टता केंद्रों (CoE) का निर्माण खनिज प्रसंस्करण और उन्नत सामग्री विज्ञान में नवाचार को बढ़ावा देगा।
- नीति और नियामक सुधार: भारत ने महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण नीति सुधार किये हैं, जिससे सार्वजनिक और निजी दोनों भागीदारों के लिये अन्वेषण एवं खनन गतिविधियों में भागीदारी आसान हो गई है।
- खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2025 (MMDR अधिनियम) में संशोधन किया गया ताकि केंद्र सरकार को 24 महत्त्वपूर्ण खनिजों की नीलामी करने का विशेष अधिकार प्राप्त हो, जिससे घरेलू खनिज संसाधनों पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित हो सके।
- सरकार महत्त्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया को भी तीव्र कर रही है, जिससे प्रशासनिक-प्रक्रिया संबंधी विलंब कम हो रहा है।
- नई अन्वेषण अनुज्ञप्ति (Exploration Licence- EL) के परिचय से निजी क्षेत्र की भागीदारी को और प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे भारत की खनिज अन्वेषण गतिविधियाँ तेज़ होंगी तथा इसकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
- रणनीतिक भंडारण: भारत वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान और भू-राजनीतिक तनाव से सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण खनिजों का रणनीतिक भंडार तैयार कर रहा है।
- NCMM के तहत, सरकार कम से कम 5 महत्त्वपूर्ण खनिजों का राष्ट्रीय भंडार बनाने की योजना बना रही है, जिससे संकट के समय भी निरंतर अभिगम्यता सुनिश्चित हो सके।
- रणनीतिक भंडार एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा, आपूर्ति शृंखला के जोखिमों को कम करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बाज़ार में उतार-चढ़ाव या भू-राजनीतिक तनाव से प्रभावित न हों।
- NCMM के तहत, सरकार कम से कम 5 महत्त्वपूर्ण खनिजों का राष्ट्रीय भंडार बनाने की योजना बना रही है, जिससे संकट के समय भी निरंतर अभिगम्यता सुनिश्चित हो सके।
भारत के महत्त्वपूर्ण खनिज पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित मुख्य समस्याएँ क्या हैं?
- आयात पर भारी निर्भरता: भारत का लिथियम, कोबाल्ट और ग्रेफाइट जैसे महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये आयात पर निर्भर होना उसके ऊर्जा संक्रमण और तकनीकी महत्वाकांक्षाओं के लिये एक गंभीर कमज़ोरियों का कारण बनता है।
- जैसे-जैसे भारत EV (इलेक्ट्रिक वाहन) अंगीकरण और सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, इन खनिजों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
- भारत लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों के लिये पूरी तरह आयात पर निर्भर है और चीन प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता है, जो वैश्विक लिथियम उत्पादन का 70% से अधिक नियंत्रित करता है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में, भारत ने महत्त्वपूर्ण खनिजों के आयात पर ₹34,000 करोड़ से अधिक व्यय किये, जो इस निर्भरता से जुड़ी आर्थिक दबाव और भू-राजनीतिक जोखिम को उजागर करता है।
- उन्नत निष्कर्षण तकनीकों की कमी: भारत उन्नत खनन और खनिज निष्कर्षण तकनीकों में महत्त्वपूर्ण अंतर का सामना कर रहा है, जिससे घरेलू संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना कठिन हो जाता है।
- हालाँकि सरकार इस क्षेत्र में अनुसंधान में निवेश कर रही है, फिर भी नवाचार की गति धीमी बनी हुई है, जिससे भारत अपने खनिज संभावनाओं का अधिकतम उपयोग नहीं कर पा रहा है।
- हाल ही में गहरे खनिज ब्लॉकों (जैसे: जम्मू-कश्मीर में लिथियम) की नीलामी के बावजूद वाणिज्यिक निष्कर्षण में बहुत कम प्रगति हुई है; लाइसेंसिंग, भौगोलिक डेटा की सटीकता और खनन तकनीक सभी प्रमुख बाधाएँ हैं।
- हाल ही में भारतीय सरकार ने कमज़ोर प्रतिक्रिया के कारण कर्नाटक में एक दुर्लभ मृदा तत्त्व (rare earth element- REE) ब्लॉक सहित 5 महत्त्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी रद्द कर दी।
- पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताएँ: खनन और निष्कर्षण प्रक्रियाओं के पर्यावरण और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जिनसे भारत को महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिये निपटना आवश्यक है।
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास संबंधी समस्याएँ और खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय क्षरण प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
- मध्य भारत (मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़) के तीन कोयला खानों पर किये गए एक अध्ययन में पाया गया कि वर्ष 1994 से 2022 के दौरान खनन गतिविधियों ने स्थानीय भूमि आवरण का 35% हिस्सा क्षतिग्रस्त कर दिया।
- झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में, बिना उपचारित खदान के जल निष्कर्षण से नदियाँ और भूजल भारी धातुओं एवं विषाक्त पदार्थों से प्रदूषित होते हैं, जिससे जल पीने व कृषि के लिये असुरक्षित हो जाता है।
- सामाजिक चिंताओं के संदर्भ में, ओडिशा के नियामगिरी पहाड़ियों में बॉक्साइट खनन को लेकर दशकों तक चल रहा संघर्ष सामाजिक प्रतिरोध का एक प्रमुख उदाहरण है।
- बाज़ार अस्थिरता और मूल्य में उतार-चढ़ाव: महत्त्वपूर्ण खनिज के वैश्विक बाज़ार में अत्यधिक अस्थिरता है, जहाँ आपूर्ति शृंखला में व्यवधान, भू-राजनीतिक तनाव और बदलती मांग के पैटर्न के आधार पर कीमतें बदलती रहती हैं।
- भारत की वैश्विक बाज़ारों पर निर्भरता इसे मूल्य वृद्धि के प्रति सुभेद्य बनाती है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की लागत प्रभावित होती है।
- उदाहरण के लिये, वर्ष 2022 की एक मैकिंसे रिपोर्ट में बताया गया कि ईवी की बढ़ती मांग के कारण लिथियम की कीमतें एक वर्ष में लगभग 550% बढ़ गईं।
- हालाँकि, आपूर्ति अधिक होने के कारण 2025 में लिथियम की कीमतें कई वर्षों के निचले स्तर पर पहुँच गई हैं।
- अपर्याप्त कार्यबल और कौशल विकास: भारत के महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में ऐसा कुशल कार्यबल नहीं है जो जटिल निष्कर्षण, प्रसंस्करण और तकनीकी उन्नतियों का समर्थन कर सके।
- हालाँकि नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (NCMM) ने 2025 में प्रमुख IIT और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये हैं, फिर भी अधिकांश नए खनन परियोजनाएँ विशेष रूप से दुर्लभ मृदा तत्त्व एवं लिथियम के लिये परियोजना डिज़ाइन और सतत् विशेषज्ञता के लिये अभी भी विदेशी सलाहकारों पर निर्भर हैं।
- यदि कुशल कार्यबल उपलब्ध नहीं है, तो भारत के लिये महत्त्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं में नवाचार करना और उन्हें कुशलतापूर्वक संचालित करना कठिन हो सकता है, जिससे विदेशी विशेषज्ञता एवं तकनीक पर निर्भरता और बढ़ जाएगी।
- डाउनस्ट्रीम उद्योगों का धीमा विकास: महत्त्वपूर्ण खनिज केवल खनन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इन्हें ईवी बैटरी, सेमीकंडक्टर और रक्षा जैसे डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में एकीकृत करना भी महत्त्वपूर्ण है।
- भारत का बैटरी निर्माण इकोसिस्टम (जैसे नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी स्टोरेज) अभी भी विकासशील है, जिससे खनिज उपलब्धता और औद्योगिक उपयोग के बीच असंगति उत्पन्न हो रही है।
- खनिज नीति और औद्योगिक नीति के बीच स्पष्ट संबंध की कमी कुशल उपयोग को रोकती है।
भारत अपनी महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखला को बेहतर बनाने के लिये कौन-से उपाय अपना सकता है?
- गहन खनिज निष्कर्षण तकनीकों का विकास: क्रिटिकल मिनरल्स की विशाल अप्रयुक्त संभावनाओं को उजागर करने के लिये, भारत को गहन और कठिन-उपलब्ध खनिज भंडारों के लिये उन्नत निष्कर्षण तकनीकों के विकास में निवेश करना चाहिये।
- इससे यह सुनिश्चित होगा कि चुनौतीपूर्ण भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाए जाने वाले कोबाल्ट और लिथियम जैसे मूल्यवान संसाधनों को पर्यावरणीय मानकों को बनाए रखते हुए कुशलतापूर्वक खनन किया जा सके।
- खनिज निष्कर्षण में नवाचार पर ध्यान केंद्रित करके, भारत विदेशी तकनीकों पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है तथा खनन में घरेलू क्षमताओं को बढ़ावा दे सकता है।
- खनिज अन्वेषण के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी: मज़बूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित करने से भारत में क्रिटिकल मिनरल भंडारों के तेज़ अन्वेषण और विकास में सहायता मिल सकती है।
- सरकारी प्रोत्साहनों को निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और निवेश के साथ जोड़कर, ये भागीदारी खनिज भंडारों के अन्वेषण एवं उपयोग की प्रक्रिया को तेज़ कर सकती हैं।
- सरकार खनन कंपनियों के साथ सहयोगी परियोजनाएँ स्थापित कर सकती है, जो जोखिम साझा करने के ढाँचे प्रदान करें, जिससे अन्वेषण गतिविधियाँ तेज़ी से और लागत-कुशल तरीके से आगे बढ़ सकें।
- शीघ्र अनुमोदनों के लिये नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना: भारत के खनिज क्षेत्र में प्रायः नियामक अनुमोदनों में विलंब होता है, जो अन्वेषण और उत्पादन की गति को प्रभावित करती है।
- महत्त्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं के लिये फास्ट-ट्रैक अनुमोदन तंत्र स्थापित करके, भारत अपने महत्त्वपूर्ण खनिज भंडारों के विकास को तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है।
- इसमें पर्यावरणीय मंज़ूरी को सरल बनाना और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को तेज़ करना शामिल हो सकता है, ताकि प्रशासनिक बाधाओं को कम किया जा सके तथा परियोजनाओं का समय पर निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।
- पारदर्शी खनिज आपूर्ति शृंखला के लिये ब्लॉकचेन का उपयोग: भारत की खनिज आपूर्ति शृंखला में ब्लॉकचेन तकनीक को शामिल करने से पारदर्शिता (Transparency), पता लगाने की क्षमता (Traceability) और कार्यकुशलता (Efficiency) बढ़ सकती है।
- ब्लॉकचेन खनिजों की निष्कर्षण से लेकर प्रसंस्करण तक की यात्रा की निगरानी में सहायता कर सकता है, जिससे सप्लाई चेन सुरक्षित रहे और अवैध खनन या संघर्ष से जुड़े स्रोत जैसी अनैतिक प्रथाओं से मुक्त रहे।
- यह तकनीक इन्वेंटरी लेवल, मांग के अनुमान और कीमत के संबंध में रियल-टाइम डेटा भी दे सकती है, जिससे बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है।
- शहरी खनन और ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना: भारत ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण के लिये अवसंरचना में सुधार करके शहरी खनन का उपयोग कर सकता है, जो कोबाल्ट, निकल और दुर्लभ मृदा तत्त्व जैसे महत्त्वपूर्ण खनिज का एक प्रमुख स्रोत है।
- पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरियों और अन्य उपभोक्ता उत्पादों से मूल्यवान खनिज निष्कर्षण के लिये अत्याधुनिक पुनर्चक्रण संयंत्र स्थापित करने से नए खनन संसाधनों पर निर्भरता में काफी कमी आ सकती है।
- इसके अतिरिक्त, अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाने और पुनर्चक्रण में भागीदारी के लिये प्रोत्साहित करने से संग्रह की दक्षता एवं खनिज पुनर्प्राप्ति दर बढ़ेगी।
- द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संसाधन अधिग्रहण समझौते: अपने खनिज आपूर्ति शृंखला की सुरक्षा के लिये, भारत को खनिज समृद्ध देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी और समझौतों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता का विस्तार करना चाहिये।
- महत्त्वपूर्ण खनिज संसाधनों और प्रसंस्करण सुविधाओं तक पहुँच के लिये द्विपक्षीय समझौतों पर वार्ता करके, भारत दीर्घकालिक आपूर्ति प्रतिबद्धताएँ सुनिश्चित कर सकता है तथा कुछ ही देशों पर अत्यधिक निर्भरता से अपने स्रोतों को विविधित कर सकता है।
- इन साझेदारियों में संयुक्त उद्यम, प्राथमिकता वाले व्यापार समझौते और विदेशी खनन संचालन में इक्विटी हिस्सेदारी शामिल हो सकते हैं।
- घरेलू खनिज प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाना: भारत को अपने महत्त्वपूर्ण खनिज के घरेलू प्रसंस्करण क्षमता को काफी हद तक बढ़ाना चाहिये, विशेष रूप से लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्त्वों जैसे खनिजों के लिये, जिनमें वर्तमान में यह विदेशी रिफाइनरों पर निर्भर है।
- विश्व स्तरीय प्रसंस्करण संयंत्रों का निर्माण करके और अत्याधुनिक रिफाइनिंग तकनीकों में निवेश करके, भारत मूल्य शृंखला में ऊपर बढ़ सकता है, जिससे यह केवल कच्चे खनिजों का निर्यात ही नहीं करेगा, बल्कि बैटरी निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों जैसे डाउनस्ट्रीम उद्योगों से भी लाभ प्राप्त कर सकेगा।
- वैकल्पिक सामग्रियों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना: दुर्लभ महत्त्वपूर्ण खनिज पर निर्भरता कम करने के लिये, भारत को वैकल्पिक सामग्रियों और तकनीकों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना चाहिये।
- बैटरियों, सोलर पैनलों और इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम, कोबाल्ट एवं दुर्लभ मृदा तत्त्वों के लिये विकल्पी सामग्रियों पर अनुसंधान आपूर्ति जोखिम को कम करने में सहायता कर सकता है।
- सरकारी वित्तपोषण, शैक्षणिक साझेदारियाँ और उद्योग सहयोग सामग्री विज्ञान में नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे भारत को ऐसे विकल्प मिलें जो अधिक सतत् और कम लागत में उपलब्ध हो सकें।
- क्षेत्रीय खनिज प्रसंस्करण हब स्थापित करना: प्रमुख खनिज-समृद्ध राज्यों में उन्नत अवसंरचना और सुविधाओं के साथ समर्पित खनिज प्रसंस्करण हब बनाना, प्रसंस्करण और रिफाइनिंग में पैमाने की अर्थव्यवस्था (Economies of Scale) प्रदान कर सकता है।
- इन हब्स को औद्योगिक पार्कों के मॉडल पर तैयार किया जा सकता है, जो खनन, बेनिफिशिएशन, स्मेल्टिंग और पुनर्चक्रण/रीसाइक्लिंग के लिये एकीकृत सुविधाएँ प्रदान करें।
- यह दृष्टिकोण न केवल संचालन को सुचारू बनाएगा, बल्कि रोज़गार के अवसरण का सृजन करेगा और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, साथ ही खनिज मूल्य शृंखला पर अधिक नियंत्रण सुनिश्चित करेगा।
- सर्कुलर इकोनॉमी (चक्रीय अर्थव्यवस्था) दृष्टिकोण अपनाना: भारत अपने क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को इस दृष्टिकोण के माध्यम से मज़बूत कर सकता है, जिसमें खनिजों का जीवनचक्र समाप्त होने पर पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण किया जाता है।
- सामग्रियों के सर्कुलर उपयोग को प्रोत्साहित करने वाली राष्ट्रीय नीति, साथ ही व्यवसायों को पुनर्चक्रण योग्य उत्पाद डिज़ाइन करने के लिये प्रोत्साहन देने से, संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।
- इससे खनिज संसाधनों का संरक्षण होगा, अपशिष्ट में कमी आएगी और आपूर्ति शृंखला में चक्र बंद करने के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों में प्रभावशाली योगदान मिलेगा।
निष्कर्ष:
भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, आत्मनिर्भरता और सतत् औद्योगिक विकास के लिये एक सुदृढ़ महत्त्वपूर्ण खनिज पारिस्थितिकी तंत्र अनिवार्य है। घरेलू अन्वेषण, पुनर्चक्रण और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को सुदृढ़ करके, भारत अपनी कमज़ोरियों को कम कर सकता है तथा अपनी समुत्थानशीलता बढ़ा सकता है। ऐसे उपाय सीधे तौर पर सतत् विकास लक्ष्यों: SDG 7 (सस्ती और प्रदूषण-मुक्त ऊर्जा), SDG 9 (उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएँ) और SDG 12 (उत्तरदायित्वपूर्ण खपत और उत्पादन) को आगे बढ़ाते हैं। समय पर सुधार और नवाचार के माध्यम से भारत खनिज सुरक्षा को अपने व्यापक दृष्टिकोण — आत्मनिर्भर भारत और नेट-ज़ीरो 2070 लक्ष्यों के साथ संरेखित कर सकता है।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में क्रिटिकल मिनरल्स के महत्त्व की विवेचना कीजिये। पारंपरिक खनन के पूरक मार्ग के रूप में पुनर्चक्रण किस प्रकार कार्य कर सकता है? |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)
प्रिलिम्स
प्रश्न 1. भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)
- इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक ‘गौण खनिज’ है।
- गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हैं।
- गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिये नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (a)
प्रश्न 2. भारत में 'ज़िला खनिज प्रतिष्ठान (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन्स)' का/के उद्देश्य क्या है/हैं? (2016)
- खनिज-संपन्न ज़िलों में खनिज-खोज संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना
- खनिज-कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना
- राज्य सरकारों को खनिज-खोज के लिये लाइसेंस निर्गत करने के लिये अधिकृत करना
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (b)
मेन्स
प्रश्न 1. गोंडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं। विवेचना कीजिये। (2021)
प्रश्न 2. “प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद, कोयला खनन विकास के लिये अभी भी अपरिहार्य है।” विवेचना कीजिये। (2017)