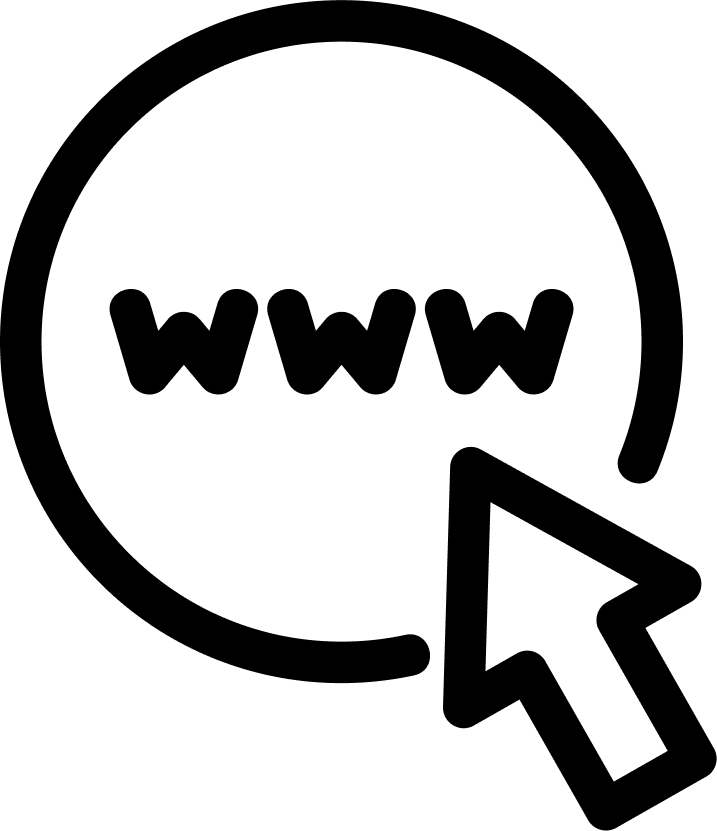हिंदी साहित्य और सिनेमा का संबंध
- 10 Jan, 2022 | पीयूष द्विवेदी
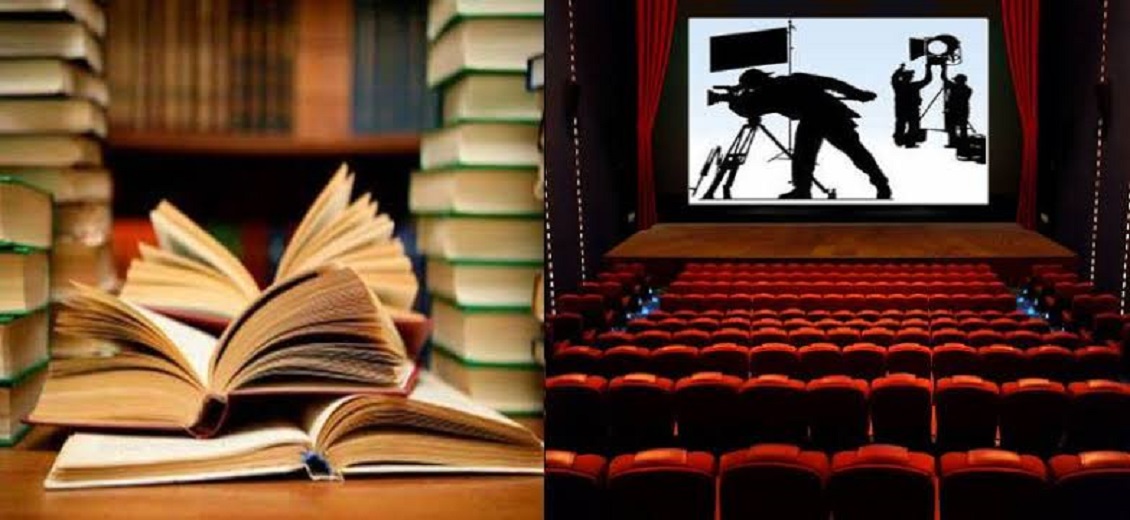
सन 1913 भारतीय सिनेमा और भारतीय साहित्य के लिए एक उल्लेखनीय वर्ष है। इस वर्ष जहॉं एक तरफ गुरुदेव रविन्द्र नाथ टैगोर को उनकी महान कृति ‘गीतांजलि’ के लिए साहित्य का नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ दादा साहब फाल्के द्वारा अपनी फिल्म ‘राजा हरिश्चंद्र’ के जरिये भारतीय सिनेमा की नींव रखी गई थी। यानी जब भारतीय साहित्य विश्व पटल पर प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा था, तब सिनेमा देश में अपने लिए जमीन तलाशने की कोशिश में लगा था। लेकिन आज उक्त दोनों घटनाओं को सौ वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद यह स्थिति बनी है कि भारतीय सिनेमा, विशेषकर हिंदी सिनेमा, जहॉं अपना वैश्विक विस्तार कर चुका है, वहीं हिंदी साहित्य बहुधा पुरस्कारों की राजनीति में उलझा, पाठकों से विपन्न होकर, अपने द्वारा ही बनाए गए एक संकुचित दायरे में सिकुड़कर रह गया है। हिंदी साहित्य ने प्रतिष्ठा और पाठक दोनों गंवाएं हैं। इस स्थिति के कारणों में उतरने पर विषयांतर हो जाएगा अतः सार संक्षेप में इतना ही कहना ठीक होगा कि बीते सौ वर्षों में सिनेमा ने जहाँ दर्शकों की अभिरुचि को पकड़ते हुए समय के साथ खुद को विषयवस्तु से लेकर प्रस्तुति-विधान तक निरंतर अद्यतित (अपडेट) किया, वहीं साहित्य अपनी कथित महानता के दंभ में पुरानी लकीर ही पीटता रह गया। परिणामतः सिनेमा के दर्शकों में निरंतर विस्तार हुआ, तो वहीं साहित्य के पाठक सिमटते गए।
हिंदी साहित्य और सिनेमा के संबंधों पर आएँ तो स्थिति बड़ी जटिल नजर आती है। शुरुआती दौर में सिनेमा ने सफल साहित्यिक कृतियों के फिल्मांकन पर ध्यान लगाया था, लेकिन जब ऐसी फ़िल्में बड़े परदे पर असर छोड़ने में कामयाब नहीं हुईं तो धीरे-धीरे साहित्य से सिनेमा जगत का लगाव कम होता गया। इस लगाव के कम होने का संभवतः एक कारण यह भी है कि हिंदी के बहुधा साहित्यकार एक तरफ तो यह इच्छा रखते हैं कि उनकी रचना पर फिल्म बने और दूसरी तरफ सिनेमा को दोयम दर्जे का माध्यम भी मानते आए हैं। प्रेमचंद से होकर उनके उत्तरवर्ती तमाम साहित्यकारों में यह समस्या बनी रही और एक हद तक आज भी है।
प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी ने ‘मिल मजदूर’ नामक फिल्म बनाई थी। लेकिन प्रेमचंद को कहानी में बदलाव के साथ फिल्म बनाना पसंद नहीं आया। एक पत्र में इस फिल्म का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि, ‘मजदूर में मैं इतना ज़रा सा आया हूँ कि नहीं के बराबर। फिल्म में डायरेक्टर ही सबकुछ है’। आगे भी विभिन्न फिल्म कंपनियों और निर्माता-निर्देशकों द्वारा प्रेमचंद की सेवासदन, रंगभूमि आदि कृतियों पर फिल्म निर्माण हुआ। लेकिन ये फ़िल्में सुनहरे परदे पर तो रंग जमाने में नाकाम ही रहीं, प्रेमचंद भी अपनी रचनाओं के फ़िल्मी प्रस्तुतीकरण से प्रायः नाखुश ही रहे। फिल्म नगरी को लेकर उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा है, ‘यह एक बिल्कुल नई दुनिया है। साहित्य से इसका बहुत कम सरोकार है। उन्हें तो रोमांच कथाएँ, सनसनीखेज तस्वीरें चाहिए। अपनी ख्याति को खतरे में डाले बगैर मैं जितनी दूर तक डायरेक्टरों की इच्छा पूरी कर सकूंगा, उतनी दूर तक करूंगा... जिंदगी में समझौता करना ही पड़ता है। आदर्शवाद महँगी चीज है, बाज दफा उसको दबाना पड़ता है।’
1936 में प्रेमचंद की मृत्यु हो गई और इस तरह सिनेमा में उनकी यात्रा अधिक समय तक नहीं चल पाई लेकिन उनके उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि वे सिनेमा को अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप माध्यम न मानने के बावजूद भी अपने आदर्शवाद को दबाकर इस क्षेत्र में काम करने का मन बना रहे थे।
प्रेमचंद के बाद भगवती चरण वर्मा, उपेन्द्रनाथ अश्क, पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र, अमृतलाल नागर भी मुंबई अपनी किस्मत आजमाने पहुँचे। लेकिन शायद इनके साहित्यिक आदर्शों का तालमेल भी सिनेमा की जरूरतों से नहीं बैठा और आगे-पीछे सब असफल ही लौट गए। यद्यपि भगवतीचरण वर्मा के उपन्यास ‘चित्रलेखा’ पर समान नाम से केदारनाथ शर्मा ने दो-दो बार फ़िल्में बनाई और पहली फिल्म सफल भी रही, लेकिन इससे वर्मा जी को सिनेमा जगत में कोई स्थायी आधार नहीं मिल पाया।
साठ के बाद के दौर में फिल्म लेखन में यदि किसी का सिक्का चला तो वो गुलशन नंदा थे। वे निस्संदेह हिंदी साहित्य के सबसे बड़े सिनेमा लेखक थे। उनके लिखे पर दो दर्जन से अधिक फिल्मों का निर्माण हुआ जिनमें से ज्यादातर कामयाब रहीं। एक समय तो यह स्थिति भी हो गई थी कि पहले फिल्म आती और उसके बाद वही कहानी उपन्यास के रूप में भी प्रकाशित होती। लेकिन तब भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। मगर इसे हिंदी का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि ऐसे कामयाब और लोकप्रिय लेखक को हिंदी साहित्य की मुख्यधारा ने कभी बतौर साहित्यकार स्वीकार ही नहीं किया। हिंदी साहित्य का यह लोकप्रियता विरोधी दृष्टिकोण भी उसकी वर्तमान दुर्दशा का एक प्रमुख कारण है।
सत्तर के बाद सिनेमा लेखन के परिदृश्य में जो साहित्यकार नजर आए उनमें राही मासूम रज़ा, धर्मवीर भारती, राजेन्द्र यादव, कमलेश्वर, मन्नू भण्डारी प्रमुख हैं। कमोबेश सबका सिनेमाई लेखन से जुड़ाव रहा। मगर इनमें जो कामयाबी कमलेश्वर ने पाई वो किसी और को नहीं मिली। उन्होंने साहित्य और सिनेमा दोनों की भूमिकाओं का सुंदर सामंजस्य किया। एक तरफ वे नई कहानी आंदोलन के प्रमुख स्तंभ रहे, तो दूसरी तरफ सिनेमा जगत में भी पूरी धूमधाम के साथ उनकी कलम चली। सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन का फिल्मफेयर उन्हें मिला तो साहित्य अकादमी से भी वे सम्मानित हुए। कुल मिलाकर साहित्यिक दायरे से लेकर बड़े परदे और टीवी तक कहीं उनकी कलम नाकाम नहीं हुई। सौ के लगभग फिल्मों में उन्होंने पटकथा, संवाद लिखे तो उनकी अनेक कृतियों पर भी सफल फिल्मों का निर्माण हुआ। इस क्रम में कुछ समस्याएँ भी आईं लेकिन कमलेश्वर कभी अपनी राह से डिगे नहीं और न ही साहित्यकार होने का व्यर्थ दम्भ ही उनमें आया। फिल्म जगत को लेकर उनका कहना था, ‘मैंने अपने-आप को वहाँ मिसफ़िट नहीं पाया... मेरे पास वही ज़ुबान थी, जिसकी ज़रूरत वहाँ होती है।’ वास्तव में, वे सिनेमा की जुबान समझते थे, इसलिए कामयाब हुए। जो नहीं समझते थे, वे बहुत आगे नहीं बढ़ पाए।
साहित्य पाठ का माध्यम है, जबकि सिनेमा दृश्य-विधान पर चलता है। इन दोनों की आवश्यकताएँ और तकनीकियाँ भिन्न हैं, जिसे उससे जुड़ा व्यक्ति ही ठीक ढंग से समझ सकता है। इस बात को इस उदाहरण से बेहतर समझ सकते हैं कि ख्वाजा अहमद अब्बास बड़े लेखक थे, लेकिन अपने लिखे पर उन्होंने जो भी फ़िल्में बनाईं वे अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त कर सकीं जबकि उनके ही लिखे पर राजकपूर ने जो फ़िल्में बनाई उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। बात यही है कि ख्वाजा अहमद मूलतः लेखन से जुड़े आदमी थे और एक घटना के बाद ताव में आकर फिल्म बनाने लगे थे, वहीं शोमैन राज कपूर खालिस सिनेमाई उत्पाद थे। ख्वाजा कागज पर कहानी गढ़ने में उस्ताद थे, लेकिन उसे सिनेमाई जरूरतों के मुताबिक़ कैमरे में दर्ज करने में मात खा जाते थे, जबकि राज कपूर सिनेमा की जरूरतों को समझते थे इसलिए उनकी फ़िल्में कामयाब रहीं। फिल्म लेखन में हाथ आजमाने वाले हर साहित्यकार को यह बुनियादी बात समझनी चाहिए और साहित्य के व्यर्थ श्रेष्ठताबोध से मुक्त होकर एक ‘प्रोफेशनल’ दृष्टिकोण के साथ ही सिनेमा लेखन की तरफ बढ़ना चाहिए। गुलजार ने सिनेमा के इस टेस्ट को समय रहते समझ लिया, इसीलिए एक तरफ उन्होंने मखमली नज्में लिखीं तो दूसरी तरफ ‘बीड़ी जलईले जिगर से पिया’ और ‘कजरारे’ जैसे गीत लिखने में भी उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। परिणाम देखिये कि वे आज हर तरह से कामयाब हैं।
वर्तमान दौर की बात करें तो यह देखना सुखद है कि हिंदी के तमाम युवा लेखक, सिनेमा की तरफ बढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य के ही उत्पाद मनोज मुंतशिर आज हिंदी सिनेमा के बड़े गीतकार के रूप में उभरते हुए बाहुबली के बाद आदिपुरुष जैसी मेगाबजट फिल्म में संवाद लिख रहे हैं, तो वहीं हिंदी के लोकप्रिय कवि कुमार विश्वास को महारथी कर्ण पर बनने जा रही वासु भगनानी की महत्वाकांक्षी फिल्म की पटकथा, गीत और संवाद लिखने के लिए साइन किया गया है। साथ ही सत्य व्यास के उपन्यास पर जहॉं एक वेब-सीरीज़ का प्रसारण हो चुका है वहीं नीलोत्पल मृणाल, नवीन चौधरी तथा दिव्य प्रकाश दुबे आदि और भी कई युवा लेखकों की रचनाओं पर सिनेमाई करार हुए हैं, जो आने वाले वक़्त में सामने आएँगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य और सिनेमा के संबंधों का अतीत भले ही बहुत चमकदार न रहा हो, लेकिन आज के इस नए दौर में हिंदी साहित्य और सिनेमा के संबंधों की तस्वीर भी बदल रही है, जो कि निश्चित ही आने वाले समय के लिए भरपूर उम्मीद जगाती है।
 |
पीयूष द्विवेदी (लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं) |