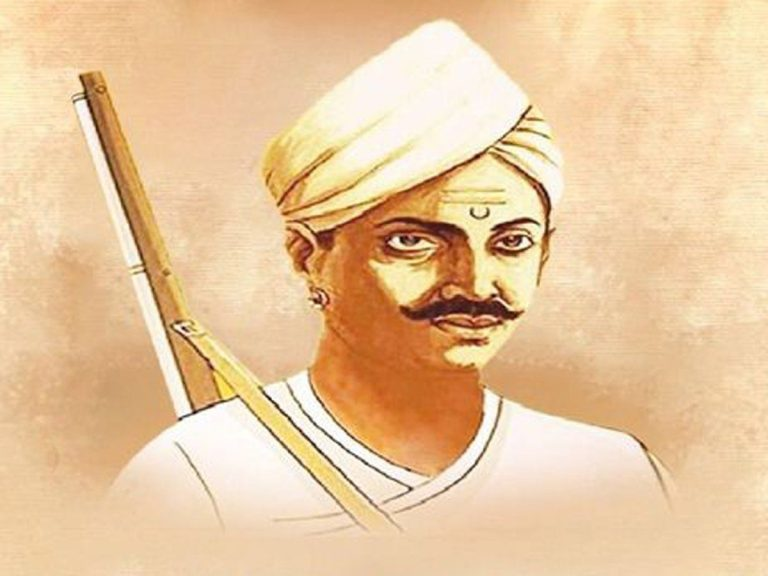ईएमआरएस को सीआईएल से 10 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन | छत्तीसगढ़ | 21 Jul 2025
चर्चा में क्यों?
जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) ने छत्तीसगढ़ में 68 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) को समर्थन देने के लिये कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के साथ साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य जनजातीय छात्रों की शिक्षा में सुधार करना है।
मुख्य बिंदु
साझेदारी के बारे में:
- CIL छत्तीसगढ़ में 68 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) को सहायता प्रदान करेगी, जिससे 28,000 से अधिक जनजातीय छात्र लाभान्वित होंगे।
- CIL की कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी (CSR) पहल के तहत कुल 10 करोड़ रुपए मंज़ूर किये गए हैं।
- यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत सरकार के प्रयासों के अनुरूप है, जो समाज के सभी वर्गों के लिये समान और समावेशी शैक्षिक अवसरों पर केंद्रित है।
- इस व्यापक हस्तक्षेप के उद्देश्य है:
- शैक्षिक अंतराल को पाटना
- करियर की तैयारी और उद्यमशीलता की मानसिकता को बढ़ावा देना
- आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिये जनजातीय युवाओं को आवश्यक उपकरणों से सशक्त बनाना
- EMRS में आधुनिक और नवीन शिक्षण वातावरण का निर्माण करन
- प्रमुख हस्तक्षेप
- डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा: कंप्यूटर लैब की स्थापना और छात्रों के लिये लगभग 3,200 कंप्यूटर तथा 300 टैबलेट का क्रय
- छात्राओं के लिये स्वास्थ्य एवं स्वच्छता: स्कूलों और छात्रावासों में लगभग 1,200 सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें और 1,200 भस्मक मशीनें स्थापित की जाएंगी
- छात्रों के लिये व्यापक मेंटरशिप: छात्रों को शैक्षणिक और व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन देने के लिये संरचित मेंटरशिप कार्यक्रम
- आवासीय उद्यमशीलता बूट कैंप: उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करने के लिये IIT, IIM और NIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में बूट कैंप का आयोजन
- कार्यान्वयन: इस परियोजना को जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) के बारे में
- EMRS: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) द्वारा वर्ष 1998 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य दूरदराज़ और जनजातीय बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक नि:शुल्क, गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना है।
- उद्देश्य: खेल, संस्कृति और कौशल प्रशिक्षण सहित समग्र विकास के साथ एकीकृत CBSE-आधारित निर्देश प्रदान करके आदिवासी और गैर-आदिवासी आबादी के बीच शैक्षिक अंतर को कम करना।
- पुनर्गठन और विस्तार: इस योजना को वर्ष 2018–19 में पुनर्गठित किया गया ताकि इसका दायरा बढ़ाया जा सके। अब EMRS उन ब्लॉकों में स्थापित किये जा रहे हैं, जहाँ 50% से अधिक ST आबादी है और कम-से-कम 20,000 जनजातीय व्यक्ति रहते हैं। इसका लक्ष्य वर्ष 2026 तक 728 स्कूलों की स्थापना करना है।
- शासन व्यवस्था: इन विद्यालयों का संचालन राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति (NESTS) द्वारा किया जाता है, जो कि MoTA के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है।
- प्रमुख विशेषताएँ:
- ये विद्यालय सहशैक्षिक और पूर्णतः आवासीय होते हैं, जिन्हें नवोदय विद्यालयों के तर्ज पर जनजातीय समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए स्थापित किया गया है।
- ये CBSE पाठ्यक्रम का पालन करते हैं और छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा के साथ-साथ सभी मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करते हैं।
- बुनियादी ढाँचा में कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर, खेल के मैदान और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये स्थान शामिल होते हैं।
- प्रत्येक विद्यालय की क्षमता 480 छात्रों की होती है, जिसमें लैंगिक समानता सुनिश्चित की जाती है।
- 10% तक सीटें गैर-जनजातीय (non-ST) छात्रों को आवंटित की जा सकती हैं।
- खेल कोटा के अंतर्गत 20% आरक्षण एथलेटिक्स और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी ST छात्रों के लिये निर्धारित है।
- जनजातीय शिक्षा हेतु अन्य पहल
कोल इंडिया लिमिटेड
- कोल इंडिया लिमिटेड (CIL), नवंबर 1975 में स्थापित एक सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन निगम है, जिसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है।
- यह विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है, जो भारत के कुल घरेलू कोयला उत्पादन में लगभग 80% का योगदान देती है।
- CIL की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL), गेवरा (छत्तीसगढ़) में एशिया की सबसे बड़ी खुली कोयला खदान का संचालन करती है।
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) से तात्पर्य समाज और पर्यावरण के प्रति कंपनी की ज़िम्मेदारी से है।
- यह एक स्व-विनियमन मॉडल है, जो यह सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय कल्याण पर अपने प्रभाव के लिये ज़वाबदेह बने रहें।
- कानूनी ढाँचा: भारत पहला देश है, जिसने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत CSR व्यय को अनिवार्य बनाया है, जो पात्र गतिविधियों के लिये एक संरचित ढाँचा प्रदान करता है।
- प्रयोज्यता: CSR नियम उन कंपनियों पर लागू होते हैं, जिनकी पिछले वित्तीय वर्ष में निवल संपत्ति 500 करोड़ रुपए से अधिक हो या कारोबार 1,000 करोड़ रुपए से अधिक हो या शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए से अधिक हो।
- ऐसी कंपनियों को पिछले 3 वित्तीय वर्षों (या यदि नई निगमित हुई हैं तो उपलब्ध वर्षों) के अपने औसत शुद्ध लाभ का कम-से-कम 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना होगा।
महिला आर्थिक सशक्तीकरण (WEE) सूचकांक | उत्तर प्रदेश | 21 Jul 2025
चर्चा में क्यों?
योजना विभाग द्वारा विकसित नवीनतम महिला आर्थिक सशक्तीकरण (WEE) सूचकांक, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में हुई महत्त्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
WEE सूचकांक के बारे में
- परिचय:
- यह योजना विभाग और उदयती फाउंडेशन की एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट है, जिसका उद्देश्य महिला-उन्मुख सरकारी योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करना तथा राज्य में लिंग-समावेशी और डाटा-आधारित नीति निर्माण को प्रोत्साहित करना है।
- WEE सूचकांक की संरचना: यह सूचकांक राज्य के सभी 75 ज़िलों का मूल्यांकन निम्नलिखित पाँच प्रमुख मानकों के आधार पर करता है:
- उद्यमिता
- रोज़गार
- शिक्षा एवं कौशल विकास
- आजीविका
- सुरक्षा एवं परिवहन अवसंरचना
- इन श्रेणियों में प्रदर्शन मापने के लिये 15 विभागों से प्राप्त 49 संकेतकों का विश्लेषण किया जाता है।
- ज़िला वर्गीकरण: ज़िलों को WEE सूचकांक में उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत किया गया:
- 'चैंपियंस': इन ज़िलों ने प्रभावी सरकारी योजनाओं, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और संरचनात्मक समर्थन के कारण अच्छे परिणाम प्रदर्शित किये हैं।
- इन ज़िलों की महिलाएँ उद्यमिता, शिक्षा और रोज़गार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं।
- इस सूची में शामिल हैं: लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, झाँसी, सुल्तानपुर, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, अयोध्या, सोनभद्र, रायबरेली, गोरखपुर, देवरिया, अंबेडकर नगर, आगरा, गाज़ियाबाद।
- 'लीडर': इन ज़िलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इन्हें अपनी गति बनाए रखने की ज़रूरत है।
- इस सूची में शामिल हैं: प्रतापगढ़, मुरादाबाद, बाराबंकी, अलीगढ़, बरेली।
- 'प्रतियोगी': इन ज़िलों ने कुछ प्रगति दिखाई है, लेकिन अभी भी अधिक प्रयासों की आवश्यकता है, विशेष रूप से कौशल प्रशिक्षण और रोज़गार के अवसरों के क्षेत्र में।
- इस सूची में शामिल हैं: गाज़ीपुर, जालौन, मुज़फ्फरनगर, बुलंदशहर।
- 'आकांक्षी': इन ज़िलों को ज़मीनी स्तर पर जागरूकता, शिक्षा, सुरक्षा और स्वरोज़गार जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन मुद्दों के समाधान के लिये विशेष अभियान चलाए जाएंगे।.
- इस सूची में शामिल हैं: चंदौली, बागपत, अमरोहा, बदायूं, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महोबा, संभल, श्रावस्ती।
- सूचकांक की मुख्य अंतर्दृष्टि:
- शिक्षा एवं कौशल विकास: शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- सार्वजनिक परिवहन समावेशन: सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं को ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में भर्ती करने की योजना ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और गतिशीलता को प्रोत्साहन दिया है।
- कार्यान्वयन योग्य उपाय
- WEE सूचकांक का एकीकरण: WEE सूचकांक को मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा ताकि वास्तविक समय में निगरानी की जा सके। यह नीति निर्माण और विभिन्न विभागों में परिणामों की ट्रैकिंग के लिये एक आधार उपकरण के रूप में कार्य करेगा।
- विभागीय योजनाएँ: सभी विभागों को महिला सशक्तीकरण पर केंद्रित कार्यान्वयन योग्य योजनाएँ तैयार करने तथा राज्य स्तरीय योजनाओं के प्रभाव को स्थानीय स्तर पर लागू करने हेतु ज़िला-स्तरीय रणनीतियाँ बनाने के निर्देश दिये गए हैं।
- लक्ष्यित अभियान: बाँदा, जालौन, जौनपुर, महोबा, श्रावस्ती और सीतापुर जैसे ज़िलों में ODOP मार्जिन मनी योजना के तहत महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये विशेष अभियान चलाए जाएंगे।
- भर्ती अभियान: होम गार्ड और शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसा कि पुलिस भर्ती के सफल मॉडल में देखा गया।
- महिला कार्यबल में भागीदारी का विस्तार: महिलाओं के लिये तकनीकी संस्थानों, व्यावसायिक कार्यक्रमों तथा कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में नामांकन बढ़ाने के प्रयास किये जाएंगे।
- री-एनरोलमेंट यूनिट्स की स्थापना की जाएगी ताकि कोर्स बीच में छोड़ चुकी महिलाओं को पुनः नामांकित किया जा सके।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में करियर हेतु सहयोग: पैरामेडिकल संस्थानों का विकास कर महिलाओं को स्वास्थ्य एवं सेवा क्षेत्र में करियर के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।
- सार्वजनिक परिवहन में भूमिका: महिलाओं को चालक और परिचालक के रूप में परिवहन क्षेत्र में शामिल करने हेतु विशेष प्रशिक्षण और सहायता सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।
मंगल पांडे जयंती | उत्तर प्रदेश | 21 Jul 2025
चर्चा में क्यों?
प्रधानमंत्री ने 19 जुलाई 2025 को महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की 198वीं जयंती पर उन्हें नमन किया।
मुख्य बिंदु
मंगल पांडे के बारे में:
- प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि:
- 19 जुलाई, 1827 को बलिया ज़िले (वर्तमान उत्तर प्रदेश) के नगवा गाँव में जन्मे मंगल पांडे एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार से थे।
- वह 22 वर्ष की आयु में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए और 3 वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री की 6वीं कंपनी में सेवा की।
- 1857 की क्रांति में भूमिका:
- उन्होंने एनफील्ड पैटर्न 1853 राइफल-मस्कट का प्रयोग करने से मनाकर दिया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इसके कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी।
- इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची, क्योंकि कारतूस लोड करने के लिये मुँह से काटना पड़ता था।
- 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने कोलकाता के पास बैरकपुर में अपनी रेजिमेंट के सर्जेंट मेजर पर गोली चलाकर विद्रोह की पहली चिंगारी भड़काई।
- इस अवज्ञापूर्ण कार्य ने 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह को जन्म दिया, जिसे अक्सर सिपाही विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा जाता है।
- इस विद्रोह के परिणामस्वरूप अंततः भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया तथा ब्रिटिश क्राउन ने वर्ष 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा और भारत सरकार अधिनियम, 1858 के अधिनियमन के माध्यम से अपने हाथ में प्रत्यक्ष नियंत्रण ले लिया, जिसके तहत गवर्नर-जनरल के स्थान पर एक वायसराय की नियुक्ति की गई।
- इस नई व्यवस्था के तहत लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने।
- मंगल पांडे को बाद में गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर के लाल बागान में कोर्ट मार्शल के आदेश से फाँसी दे दी गई।
- विद्रोह का विस्तार:
- मंगल पांडे की फाँसी के बाद 7वीं अवध रेजिमेंट ने भी विद्रोह किया, जिसे बाद में दबा दिया गया। असहमति जताने के कारण उनकी रेजिमेंट को भी बेहरामपुर की 19वीं इन्फैंट्री की तरह भंग कर दिया गया।
- विद्रोह अंबाला, लखनऊ और मेरठ की सैन्य छावनियों तक फैल गया।.
- 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह शुरू किया जिससे यह एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह में बदल गया।
- उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया और वृद्ध बहादुर शाह द्वितीय से प्रतीकात्मक सम्राट बनने का आग्रह किया। अनुनय-विनय के बाद, उन्होंने स्वीकार कर लिया और उन्हें शाह-ए-शाह-ए-हिंदुस्तान घोषित कर दिया गया।
- वह अंतिम मुगल सम्राट थे, जिन्हें विद्रोह की विफलता के बाद रंगून निर्वासित कर दिया गया था।
- 19 सितंबर 1857 को लाल किले पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया और वर्ष 1862 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई।
- महत्त्व:
- बैरकपुर में मंगल पांडे का विद्रोह कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि यह ब्रिटिश शासन के तहत धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण के प्रति सामूहिक आक्रोश का प्रतीक था।
- वे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार माने जाते हैं और उनकी बलिदानी विरासत को आज भी राष्ट्रीय प्रतिरोध और देशभक्ति के प्रतीक रूप में याद किया जाता है।
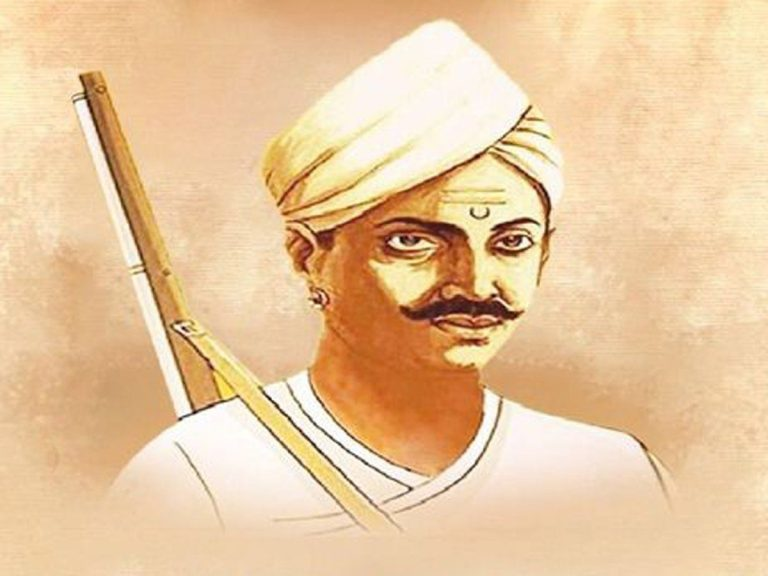
अवध के सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ के बारे में:
- मंगल पांडे अवध से थे, जो कंपनी भर्ती के लिये एक प्रमुख क्षेत्र था। अवध के 75,000 सिपाही ब्रिटिश सेना का हिस्सा थे और लगभग हर कृषक परिवार का एक सदस्य सेना में था।
- वर्ष 1856 में लॉर्ड डलहौज़ी द्वारा कुशासन (हड़प नीति के तहत नहीं) के आधार पर अवध पर कब्ज़ा कर लिया। इसके अतिरिक्त, भू-राजस्व व्यवस्थाओं ने भी व्यापक असंतोष को जन्म दिया।
- हड़प नीति (डॉक्ट्रिन ऑफ़ लैप्स) लॉर्ड डलहौज़ी (गवर्नर-जनरल, 1848-56) द्वारा लागू की गई थी। इसने दत्तक उत्तराधिकारियों को राज्यों के उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप सतारा (1848), पंजाब (1849), झाँसी और नागपुर (1854) जैसे राज्यों का विलय हुआ।
- ताल्लुकदारों की ज़मीनों की ज़ब्ती और कठोर राजस्व व्यवस्था के कारण सिपाहियों ने अपनी आर्थिक तंगी के विरोध में 14,000 याचिकाएँ दायर कीं। इस प्रकार पांडे का विद्रोह इस बढ़ते हुए किसान-सैन्य असंतोष का प्रतीक बन गया।
1857 के विद्रोह के अन्य प्रमुख नेताओं के बारे में
- नाना साहब (कानपुर): पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र; अंग्रेज़ों द्वारा पेंशन के अधिकार से वंचित। कानपुर में नेतृत्व संभाला; वर्ष 1859 में नेपाल भाग गए, जहाँ संभवतः उनकी मृत्यु हो गई।
- बेगम हज़रत महल (लखनऊ): नवाब वाज़िद अली शाह की विधवा; लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया। अपने बेटे बिरजिस कद्र को राजा बनाया। वर्ष 1879 में अपनी मृत्यु तक नेपाल में निर्वासित रहीं।
- वीर कुंवर सिंह (बिहार): भोजपुर के 80 वर्षीय ज़मींदार; गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया। वर्ष 1858 में घायल होने से पहले उन्होंने जगदीशपुर पर पुनः कब्ज़ा कर लिया।
- रानी लक्ष्मीबाई (झाँसी): हड़प नीति के तहत उत्तराधिकार से वंचित। वर्ष 1858 में जनरल ह्यूग रोज़ के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना से लड़ीं।
- खान बहादुर खान (बरेली): 82 वर्ष की आयु में बरेली में लंबे समय तक चले प्रतिरोध का नेतृत्व किया; सर कॉलिन कैंपबेल से लड़े।
- मौलवी लियाकत अली (इलाहाबाद): कुछ समय तक इलाहाबाद पर नियंत्रण रखा; खुसरो बाग को केंद्र बनाया। उन्हे वर्ष 1872 में गिरफ्तार कर अंडमान द्वीप भेज दिया गया।