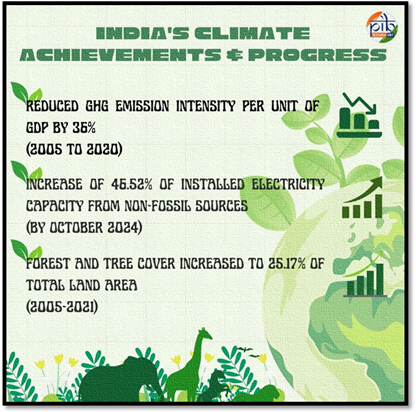COP30: वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्रवाई का नया अध्याय | 25 Nov 2025
यह एडिटोरियल 25/11/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित “At COP 30, a divided world finds common ground,” पर आधारित है। इस लेख में चर्चा की गई है कि किस प्रकार COP 30 ने वैश्विक मतभेदों और चुनौतियों के बावजूद, आर्थिक व सामाजिक जटिलताओं को संतुलित करते हुए जलवायु अनुकूलन, न्यायसंगत परिवर्तन तंत्र एवं समान ऊर्जा परिवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिये विविध देशों के हितों को जोड़कर महत्त्वपूर्ण बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त किया।
प्रिलिम्स के लिये: COP 30, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC), न्यायोचित संक्रमण तंत्र, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरेवर फैसिलिटी (TFFF), ग्लोबल मुतिराओ अग्रीमेंट, उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट- 2025, कार्रवाई क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
मेन्स के लिये: बेलेम, ब्राज़ील में COP30 के प्रमुख परिणाम, देशों को वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने से रोकने वाली प्रमुख बाधाएँ, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये भारत सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल
COP 30 ने वैश्विक जलवायु-परिवर्तन कार्रवाई में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिसने भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद बहुपक्षीय सहयोग की शक्ति को प्रदर्शित किया। इस सम्मेलन में ऐतिहासिक वित्तीय प्रतिबद्धताएँ, वर्ष 2035 तक अनुकूलन निधि को तिगुना करने का संकल्प और न्यायसंगत परिवर्तन तथा वनों की कटाई को रोकने के लिये अभिनव पहलों की शुरुआत की गई। यद्यपि जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने संबंधी उद्देश्य पर अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी, फिर भी COP 30 ने महत्त्वाकांक्षी, समता-आधारित जलवायु रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया, जो सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लक्ष्यों को एक सहयोगात्मक वैश्विक कार्यढाँचे में समाहित करती हैं।
ब्राज़ील के बेलेम में COP30 के मुख्य परिणाम क्या हैं?
- बेलेम पैकेज का अंगीकरण: COP30 में बेलेम पैकेज को अपनाया गया, जिसमें 29 निर्णय शामिल थे, जिनका उद्देश्य जलवायु वित्त, अनुकूलन ट्रैकिंग, लैंगिक समावेशन और वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करके पेरिस समझौते के कार्यान्वयन को त्वरित करना था।
- यह पैकेज मात्र संकल्पों से आगे बढ़कर उन्हें कार्यान्वयन-उन्मुख प्रक्रियाओं में रूपांतरित करने की दिशा को रेखांकित करता है।
- जलवायु वित्त प्रतिबद्धताएँ और अनुकूलन निधि: COP30 के पक्षों ने जलवायु-परिवर्तन कार्रवाई के लिये वर्ष 2035 तक प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर संग्रहण की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें कमज़ोर देशों को सहायता देने के लिये अनुकूलन निधि को तीन गुना बढ़ाने तथा पिछले समझौतों में लंबे समय से चली आ रही वित्तीय कमियों को दूर करने पर ज़ोर दिया गया है।
- वैश्विक कार्यान्वयन त्वरक और बेलेम मिशन 1.5°C: जलवायु लक्ष्यों की दिशा में राष्ट्रीय प्रगति की निगरानी के लिये शुरू की गई इन पहलों का उद्देश्य NDC की स्केलेबल ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करके, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को बढ़ावा देकर उत्सर्जन अंतर को कम करना है।
- जीवाश्म ईंधन पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं के लिये न्यायोचित संक्रमण तंत्र: इसे बेलेम एक्शन मैकेनिज़्म के रूप में भी जाना जाता है, यह जीवाश्म ईंधन से स्थायी अर्थव्यवस्थाओं की ओर संक्रमण करने वाले श्रमिकों एवं देशों का समर्थन करता है।
- निर्वनीकरण और जीवाश्म ईंधन संक्रमण के लिये रोडमैप: ब्राज़ील ने दो प्रमुख रोडमैप पेश किये: एक वनों की कटाई को रोकने और पुनः वनीकरण के लिये और दूसरा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करते हुए न्यायसंगत, समतामूलक जीवाश्म ईंधन संक्रमण को आगे बढ़ाने के लिये।
- बेलेम स्वास्थ्य कार्य योजना: यह जलवायु-परिवर्तन कार्रवाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य को जोड़ने वाली पहली वैश्विक योजना है जो जलवायु-प्रेरित स्वास्थ्य जोखिमों से बचाव करने और क्लाइमेट जस्टिस पर बल देने पर आधारित है, जिसका उद्देश्य विश्व भर में समुत्थानशील स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करना है।
- ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरेवर फैसिलिटी: एक प्रदर्शन-आधारित, दीर्घकालिक निधि जो वन संरक्षण के लिये देशों को पुरस्कृत करती है, कम से कम 20% निधि स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को आवंटित करती है, जैवविविधता, आजीविका एवं जलवायु लक्ष्यों को संरेखित करती है।
- समानता और समावेशी शासन को सुदृढ़ करना: COP30 ने लैंगिक-संवेदनशील नीतियों और स्वदेशी नेतृत्व को एकीकृत करते हुए समानता, क्लाइमेट जस्टिस, पारदर्शिता एवं अंतर-पीढ़ीगत अधिकारों को मज़बूत किया।
- जलवायु-व्यापार वार्ता: यह जलवायु उद्देश्यों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने, कार्बन सीमा समायोजन जैसे विवादों को कम करने तथा संधारणीय, निष्पक्ष बदलावों को बढ़ावा देने की एक पहल है।
- ग्लोबल मुतिराओ अग्रीमेंट: सामूहिक कार्रवाई की भावना को बढ़ावा देते हुए, इस समझौते का उद्देश्य भू-राजनीतिक विभाजनों के बीच बहुपक्षवाद और सामूहिक जिम्मेदारी को बढ़ाना है।
देशों को वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने से रोकने वाली प्रमुख बाधाएँ
- NDC प्रतिज्ञाओं और मार्ग के बीच अंतर: कई देशों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) अभी भी तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिये आवश्यक योगदान से कम हैं।
- UNEP के उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट- 2025 में कहा गया है कि वर्तमान NDC वर्ष 2019 के स्तर की तुलना में वर्ष 2035 तक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में केवल 15% की कमी कर पाएंगे, जबकि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के भीतर रहने के लिये 45%-60% की कमी की आवश्यकता है।
- केवल 19 देशों ने ही पेरिस लक्ष्यों के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित किये हैं तथा चीन और अमेरिका जैसे प्रमुख उत्सर्जक देश कुछ क्षेत्रों में विस्तार की योजना बना रहे हैं।
- महत्त्वाकांक्षा की इस कमी के कारण वर्ष 2100 तक तापमान में 2.3-2.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान है।
- कार्यान्वयन में अंतराल: जहाँ लक्ष्य मौजूद हैं, वहाँ भी कार्यान्वयन में विलंब हो रहा है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के अनुसार वर्ष 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन आवश्यक कटौती से 29-32 गीगाटन CO₂e अधिक होने की राह पर है, जो कार्यान्वयन में एक गंभीर अंतराल की ओर संकेत करता है।
- यद्यपि नवीकरणीय क्षमता बढ़ रही है, फिर भी जीवाश्म ईंधन के बुनियादी अवसंरचना में निवेश जारी है, और कई देश कोयले के प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में विलंब कर रहे हैं, जिससे डीकार्बोनाइज़ेशन की गति प्रभावित हो रही है।
- कई निगम और व्यवसाय जलवायु-परिवर्तन कार्रवाई में पिछड़ रहे हैं। EY ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन बैरोमीटर- 2025 के अनुसार जहाँ 64% कंपनियों के पास नेट-ज़ीरो योजनाएँ हैं, वहीं केवल 12% ने वर्ष 2025 तक पर्याप्त प्रगति की है।
- लगभग दो-तिहाई व्यवसाय वास्तविक उत्सर्जन कटौती के बजाय कार्बन क्रेडिट पर निर्भर हैं, विशेष रूप से परिवहन एवं वित्तीय सेवाओं में, जिससे व्यापक जलवायु प्रयास कमज़ोर हो रहे हैं।
- अपर्याप्त जलवायु वित्त: विकासशील देशों को शमन और अनुकूलन के लिये पर्याप्त वित्त पोषण की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें दीर्घकालिक कमी का सामना करना पड़ता है।
- यद्यपि COP30 ने वर्ष 2035 तक प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर देने का वादा किया था, लेकिन वर्तमान में केवल लगभग 115 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष (विकसित देशों द्वारा) जलवायु वित्त के रूप में प्रवाहित होता है, जो वर्ष 2020 एवं भविष्य की जरूरतों के लिये निर्धारित 300 बिलियन डॉलर के लक्ष्य से काफी कम है।
- अनुकूलन निधि विशेष रूप से अपर्याप्त है तथा आवश्यक राशि का एक तिहाई से भी कम प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण सुभेद्य देशों को जलवायु प्रभावों और समुत्थानशक्ति निर्माण के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है।
- भू-राजनीतिक तनाव और उत्तरदायित्व विवाद: वैश्विक राजनीतिक विभाजन जीवाश्म ईंधन के प्रयोग की चरणबद्ध समाप्ति और न्यायसंगत वित्त साझेदारी जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति में बाधा डालते हैं।
- COP30 ने जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिये बाध्यकारी समझौते के अभाव के कारण इस तथ्य को उजागर किया।
- विकसित एवं विकासशील देशों के बीच दायित्वों के संतुलन के साथ-साथ निगरानी और जवाबदेही के कार्यढाँचों पर भी देशों के बीच मतभेद हैं। इस मुद्दे पर अमेरिका-चीन सहयोग असंगत रहा है, जिससे वैश्विक गति प्रभावित हो रही है।
- इसके अलावा, भारत ग्लोबल साउथ की ओर से जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से न्यूनतम करने का आह्वान करता है।
- तकनीकी बाधाएँ और क्षमता अंतराल: उन्नत स्वच्छ प्रौद्योगिकियों तक अभिगम्यता असमान है।
- कई विकासशील देशों में नवीकरणीय ऊर्जा को प्रभावी ढंग से लागू करने या कार्बन कैप्चर तकनीकों को अपनाने के लिये बुनियादी अवसंरचना और विशेषज्ञता का अभाव है। इससे महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- उदाहरण के लिये, वर्ष 2024 में अफ्रीका की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता केवल 70 गीगावाट तक पहुँच पाई, जबकि यूरोप में यह 800 गीगावाट से अधिक है, जो बढ़ते प्रौद्योगिकी अंतराल को उजागर करता है।
- डेटा पारदर्शिता और रिपोर्टिंग की कमियाँ: उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाइयों पर सटीक, समय पर डेटा वैश्विक जवाबदेही के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- कई देशों को व्यापक ग्रीनहाउस गैस सूची और पारदर्शी रिपोर्टिंग में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे विश्वास कमज़ोर हो रहा है तथा नीति समायोजन में बाधा आ रही है।
- एकसमान रिपोर्टिंग मानकों का अभाव असंगत प्रगति ट्रैकिंग में योगदान देता है।
- वर्ष 1997 से वर्ष 2019 तक 133 विकासशील देशों को कवर करने वाले एक अध्ययन में पाया गया कि आधे से अधिक देशों ने अपनी GHG इन्वेंट्री क्षमताओं में सुधार करने में बहुत कम या कोई प्रगति नहीं की तथा कई देश आवश्यकता पड़ने पर इन्वेंट्री प्रस्तुत करने में विफल रहे।
- सामाजिक-आर्थिक और न्यायसंगत संक्रमण चुनौतियाँ: जीवाश्म ईंधन से संक्रमण कोयला, तेल और गैस से जुड़े उद्योगों में लाखों श्रमिकों को प्रभावित करता है।
- पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा और पुनः कौशलीकरण योजनाओं के बिना प्रतिरोध बढ़ता है, जिससे नीति निर्माण में विलंब होता है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक हरित क्षेत्रों में लगभग 24 मिलियन नौकरियों का सृजन होगा, लेकिन जीवाश्म ईंधन उद्योगों में लाखों लोगों के विस्थापन का खतरा है, विशेष रूप से पोलैंड, भारत व अमेरिका के कुछ हिस्सों जैसे कोयला-निर्भर क्षेत्रों में।
जलवायु परिवर्तन से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये भारत सरकार ने कौन-सी प्रमुख पहल की है?
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC): वर्ष 2008 में शुरू की गई, इसमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, संधारणीय आवास, जल, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, हरित भारत, सतत् कृषि और जलवायु ज्ञान को लक्षित करने वाले आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं।
- राष्ट्रीय सौर मिशन: जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने तथा स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, ताकि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके।
- प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना: अतिरिक्त बचत के लिये व्यापार योग्य क्रेडिट के साथ उद्योग में बाज़ार आधारित ऊर्जा दक्षता सुधारों को लागू करना।
- कार्बन बाज़ार विकास: उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करने के लिये वर्ष 2026 तक अपेक्षित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना की स्थापना।
- वन संरक्षण और वनीकरण कार्यक्रम: NAPCC मिशन और ग्रीन इंडिया मिशन के तहत, भारत का लक्ष्य 6 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनरोपण करना तथा वन आवरण को 23% से बढ़ाकर 33% करना है।
- भारत का ‘कूलिंग एक्शन प्लान’ (ICAP): इसका उद्देश्य शीतलक उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग को कम करने, स्वास्थ्य व समता में सुधार लाने के लिये संधारणीय शीतलन समाधान की तलाश करना है।
- राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा मिशन: ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और उत्सर्जन को कम करने के लिये नवीकरणीय विकल्प के रूप में जैव-ऊर्जा को बढ़ावा देता है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP): इसका उद्देश्य जलवायु लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने वाले विनियामक उपायों का उपयोग करके वायु प्रदूषण को कम करना है।
- मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटैट्स एंड टैन्जिबल इनकम्स (MISHTI) पहल: मैंग्रोव पर निर्भर सामुदायिक आजीविका को बढ़ाते हुए तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करता है।
- कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण (CCUS): नवीन CO₂ कैप्चर और पुनः एकीकरण प्रौद्योगिकियों के माध्यम से औद्योगिक डीकार्बोनाइज़ेशन का समर्थन करता है।
- मियावाकी शहरी वनरोपण तकनीक: बेहतर हरित आवरण और वायु गुणवत्ता के लिये शहरी क्षेत्रों में घनी स्थानीय वनस्पति का प्रसार।
विश्व भर में न्यायसंगत और प्रभावी जलवायु-परिवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिये कौन-सी प्रमुख वैश्विक कार्रवाइयाँ आवश्यक हैं?
- मज़बूत NDC के साथ महत्त्वाकांक्षा अंतराल को दूर करना: अधिकांश वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान को सीमित करने के लिये अपर्याप्त हैं।
- भारत सहित अन्य देशों को अधिक महत्त्वाकांक्षी, विज्ञान-आधारित लक्ष्य अपनाने की आवश्यकता है तथा उन्हें अंतर्निहित जवाबदेही के साथ नियमित रूप से संशोधित करने की आवश्यकता है।
- उदाहरण के लिये, समावेशी हितधारक सहभागिता के साथ लक्ष्यों को व्यापक बनाने की कोलंबिया की पुनरावृत्तीय प्रक्रिया प्रभावी महत्त्वाकांक्षा वृद्धि का उदाहरण है।
- फिट फॉर 55 पैकेज के अंतर्गत यूरोपीय संघ के कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती का अनुकरण करके ऐसी महत्त्वाकांक्षा को संस्थागत रूप दिया जा सकता है।
- सुदृढ़ शासन और निगरानी के माध्यम से कार्यान्वयन अंतराल को दूर करना: देशों को अपनी प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट समयसीमा और अनुपालन प्रोत्साहन के साथ लागू करने योग्य नीतियों में परिवर्तित करना चाहिये।
- डोमिनिकन रिपब्लिक की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय परिषद समन्वित कार्रवाई के लिये सरकारी विभागों का सफलतापूर्वक समन्वय करती है।
- भारत और अन्य देश ऐसे केंद्रीय निकायों की स्थापना या सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं, जिन्हें डिजिटल MRV (आकलन, रिपोर्टिंग और सत्यापन) प्रणालियों द्वारा संपूरित किया जा सकता है, ताकि प्रगति पर पारदर्शी रूप से नज़र रखी जा सके तथा कम प्रदर्शन पर दंड लगाया जा सके, जिससे वैश्विक कार्यान्वयन घाटे में कमी आएगी।
- पारदर्शिता और नवाचार के साथ जलवायु वित्त का विस्तार: वित्तीय कमी को दूर करने के लिये ग्रीन बॉण्ड, मिश्रित वित्त और जलवायु निधि जैसे विविध साधनों की आवश्यकता है। ज़ाम्बिया के ग्रीन बॉण्ड और दक्षिण अफ्रीका के सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड प्रभावी विस्तार रणनीतियों का उदाहरण हैं।
- भारत को घरेलू हरित वित्त बाज़ारों को बढ़ावा देना चाहिये, UNFCCC रिपोर्टिंग मानकों का पालन करना चाहिये तथा ऐसे नीतिगत वातावरण का निर्माण करना चाहिये जो निजी निवेश को आकर्षित करें और यह सुनिश्चित करें कि अनुकूलन निधि कमज़ोर आबादी तक तत्काल पहुँचे।
- बहुपक्षीय सहयोग और न्यायसंगत जिम्मेदारी साझाकरण को मज़बूत करना: भू-राजनीतिक विभाजन को समाप्त करने में पेरिस समझौते के तहत पारदर्शिता एवं जवाबदेही कार्यढाँचे को मज़बूत करना शामिल है, जबकि सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों (CBDR) को क्रियान्वित करना शामिल है।
- केन्या की जलवायु वित्त इकाई और थाईलैंड की राष्ट्रीय रणनीतियाँ समान रूप से समर्थन जुटाने के सफल मॉडल प्रदर्शित करती हैं।
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग में भारत की भूमिका महत्त्वाकांक्षा एवं समानता के बीच संतुलन बनाने तथा विभिन्न पक्षों के बीच विश्वास को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- प्रौद्योगिकी अंतरण और क्षमता निर्माण में निवेश: प्रौद्योगिकी अंतराल को समाप्त करने के लिये सहकारी अनुसंधान एवं विकास, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता योजनाओं की आवश्यकता है।
- उदाहरण के लिये, फिजी ने स्थानीय विशेषज्ञता विकसित करने और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिये गठबंधन बनाए हैं। भारत मिशन इनोवेशन जैसी साझेदारियों का विस्तार कर सकता है और स्वच्छ प्रौद्योगिकी अंगीकरण में तीव्रता लाने तथा नवीकरणीय क्षमताओं में असमानताओं को दूर करने के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण में निवेश कर सकता है।
- डेटा पारदर्शिता और रिपोर्टिंग कठोरता में वृद्धि: एकरूप, विश्वसनीय डेटा जवाबदेही को मज़बूत करता है।
- पेरू और नेपाल जैसे देशों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके जलवायु रिपोर्टिंग को विकास संकेतकों के साथ एकीकृत किया है।
- भारत को IPCC-अनुरूप कार्यप्रणाली अपनानी चाहिये, AI और उपग्रह निगरानी लागू करनी चाहिये, तथा घरेलू विश्वास एवं अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता बनाने के लिये ओपन डेटा तक अभिगम्यता को सक्षम करना चाहिये, जिससे गतिशील नीति संशोधन की सुविधा मिल सके।
- सामाजिक सुरक्षा के साथ न्यायोचित परिवर्तन सुनिश्चित करना: सामाजिक सुरक्षा संजाल और पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करने से जीवाश्म ईंधन से संक्रमण आसान हो जाता है तथा व्यापक समर्थन प्राप्त होता है।
- जर्मनी के कोयला क्षेत्र में व्यापक श्रमिक पुनर्कौशलीकरण और सामाजिक संवाद पर आधारित परिवर्तन सफल न्यायसंगत परिवर्तन मॉडल के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
- भारत और अन्य देशों को हरित क्षेत्रों में समावेशी अवसर उत्पन्न करने तथा सामाजिक प्रतिरोध को कम करने के लिये स्थानीय समुदायों को सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिये।
- जवाबदेही के साथ कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्रिय करना: प्रकटीकरण और कार्बन मूल्य निर्धारण को अनिवार्य करने वाले मज़बूत नियामक कार्यढाँचे (हरित नवाचार के लिये प्रोत्साहन के साथ) कॉर्पोरेट जलवायु उत्तरदायित्व को सुदृढ़ कर सकते हैं।
- थाईलैंड के सस्टेनिबिलिटी-लिंक्ड बॉण्ड और कोटे डी आइवर की सार्वजनिक-निजी भागीदारी ने निजी कार्रवाई को उत्प्रेरित किया है।
- भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ऑफसेट तक सीमित रहने के बजाय कॉर्पोरेट नेट-शून्य प्रतिबद्धताएँ वास्तविक उत्सर्जन में ठोस कमी के रूप में परिलक्षित हों और हाल के अध्ययनों द्वारा रेखांकित कमियों को प्रभावी रूप से दूर कर सकें।
निष्कर्ष:
वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्रवाई को 1.5°C लक्ष्य प्राप्त करने के लिये तत्काल एवं रूपांतरकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के आठवें महासचिव बान की-मून ने कहा है, “हम पहली ऐसी पीढ़ी हैं जो गरीबी समाप्त कर सकती है तथा अंतिम जो अनियंत्रित जलवायु परिवर्तन को रोक सकती है।”
इसलिये राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) की महत्त्वाकांक्षा को सुदृढ़ करना, पारदर्शी वित्तीय प्रवाह का विस्तार, प्रौद्योगिकी अंतरण को प्रोत्साहन, न्यायसंगत संक्रमण सुनिश्चित करना तथा आँकड़ों की जवाबदेही को मज़बूत बनाना अनिवार्य है। ये सभी उपाय संयुक्त रूप से SDG 7 (सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा), SDG 13 (जलवायु परिवर्तन कार्रवाई) तथा SDG 17 (लक्ष्य हेतु भागीदारी) को आगे बढ़ाते हुए वैश्विक स्तर पर न्यायपूर्ण जलवायु-अनुकूलन को प्रोत्साहित करते हैं।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. COP30 पेरिस समझौते के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। सम्मेलन के दौरान शुरू की गई प्रमुख पहलों का विश्लेषण कीजिये तथा वैश्विक महत्त्वाकांक्षा और क्रियान्वयन के अंतर को कम करने में उनकी महत्ता का मूल्यांकन कीजिये। |
प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1. ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित COP30 का प्राथमिक परिणाम क्या था?
COP30 ने बेलेम पैकेज (29 निर्णय) का अंगीकरण किया, जिसमें जलवायु वित्त, अनुकूलन, न्यायसंगत परिवर्तन, वनों की कटाई को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा पेरिस समझौते के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिये वैश्विक सहयोग को मज़बूत किया गया।
प्रश्न 2. जलवायु वित्त अभी भी वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं के लिये एक बड़ी बाधा क्यों है?
COP30 द्वारा वर्ष 2035 तक प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता के बावजूद, वर्तमान प्रवाह लगभग 80 बिलियन डॉलर बना हुआ है तथा अनुकूलन वित्त का वित्तपोषण बहुत कम है, जिससे विकासशील देशों में समुत्थानशीलता लाने के प्रयास सीमित हो रहे हैं।
प्रश्न 3. वैश्विक जलवायु-परिवर्तन कार्रवाई में निरंतर महत्त्वाकांक्षा और कार्यान्वयन अंतराल की क्या व्याख्या है?
अधिकांश NDC 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिये अपर्याप्त हैं तथा कोयले के प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में विलंब, जीवाश्म ईंधन में निवेश में वृद्धि, कमज़ोर MRV प्रणाली तथा वास्तविक उत्सर्जन में कटौती की दिशा में धीमी कॉर्पोरेट प्रगति के कारण वैश्विक उत्सर्जन की गति अभी भी धीमी बनी हुई है।
प्रश्न 4. जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये भारत ने कौन-सी प्रमुख पहल की है?
भारत की कार्रवाइयों में NAPCC मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, PAT योजना, NCAP, कार्बन बाज़ार, ग्रीन इंडिया वनरोपण, जैव-ऊर्जा, CCUS और MISHTI मैंग्रोव पुनर्स्थापन पहल शामिल हैं।
प्रश्न 5. न्यायसंगत और प्रभावी जलवायु-परिवर्तन कार्रवाई के लिये कौन-सी वैश्विक कार्रवाइयाँ आवश्यक हैं?
देशों को NDC महत्त्वाकांक्षा को मज़बूत करने, सुदृढ़ शासन और MRV का निर्माण करने, पारदर्शी जलवायु वित्त का विस्तार करने, प्रौद्योगिकी अंतरण को बढ़ावा देने, न्यायसंगत परिवर्तन सुनिश्चित करने तथा बहुपक्षीय सहयोग (CBDR) को गहन करने की आवश्यकता है।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)
प्रिलिम्स
प्रश्न 1. वर्ष, 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)
- 1. इस समझौते पर UN के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किये और यह वर्ष 2017 से लागू होगा।
- 2. यह समझौता ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग-पूर्व स्तर (Pre-industrial levels) से 2 ºC या कोशिश करें कि 1.5 °C से भी अधिक न होने पाएँ।
- 3. विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिये विकासशील देशों की सहायता के लिये 2020 से प्रतिवर्ष 1000 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई।
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (b)
मेन्स
प्रश्न 1. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021)
प्रश्न 2. नवंबर, 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में सी.ओ.पी. 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, आरम्भ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिये। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई.एस.ए.) में यह विचार पहली बार कब दिया गया था ? (2021)