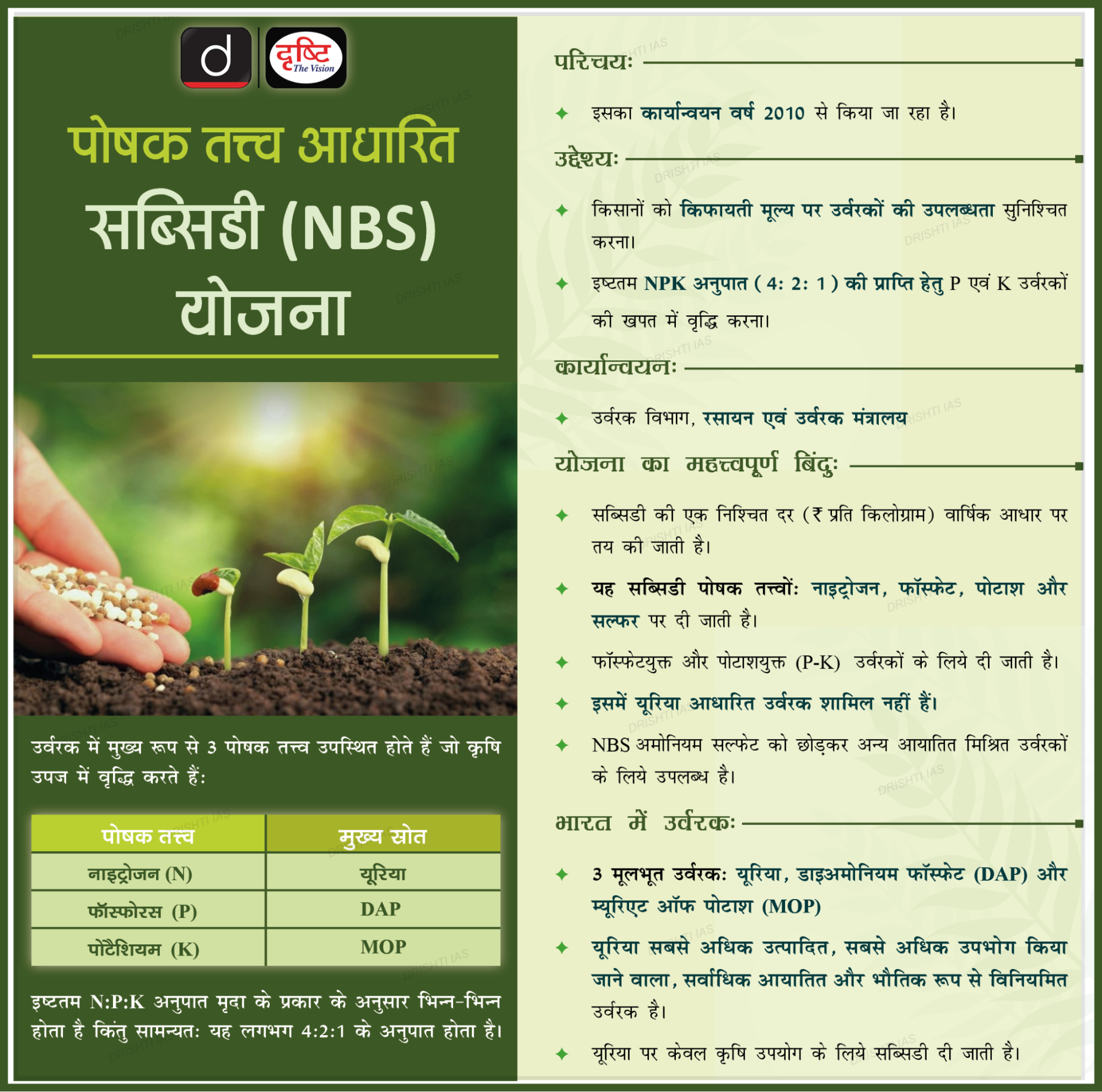भारत में उर्वरक क्षेत्र | 26 Aug 2025
प्रिलिम्स के लिये: वन नेशन वन फर्टिलाइज़र, नैनो उर्वरक, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र
मेन्स के लिये: उर्वरक क्षेत्र, आत्मनिर्भर भारत और रणनीतिक क्षेत्र।
चर्चा में क्यों?
संसदीय समिति ने सरकार से आग्रह किया है कि उर्वरक क्षेत्र को पुनः ‘रणनीतिक’ श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएँ। समिति ने इसकी वर्तमान ‘गैर-रणनीतिक’ स्थिति की आलोचना करते हुए कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत के स्वावलंबन लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है, विशेषकर बढ़ती आयात निर्भरता और खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए।
उर्वरक क्षेत्र पर संसदीय समिति के अवलोकन और सिफारिशें क्या हैं?
अवलोकन
- खाद्य सुरक्षा से संबंध: उर्वरक कृषि उत्पादकता और खाद्य संप्रभुता के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। समिति ने उल्लेख किया कि भारत की उच्च आयात निर्भरता (यूरिया के लिये 25%, फॉस्फेट के लिये 90% और पोटाश के लिये 100%) घरेलू उत्पादन, मूल्य स्थिरता, आपदा-रोधी क्षमता और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा हेतु उर्वरक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSU) को मज़बूत बनाना आवश्यक बनाती है।
- निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने खाद्य सुरक्षा में इस क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद उर्वरक क्षेत्र को रणनीतिक दर्जा देने से इंकार कर दिया।
- कम PSU बाज़ार हिस्सेदारी: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU) यूरिया उर्वरक उत्पादन में केवल ~25% तथा गैर-यूरिया उर्वरक उत्पादन में ~11% का योगदान करते हैं।
- निजी क्षेत्र इस उद्योग में प्रमुख भूमिका निभाता है और वर्ष 2023–24 में कुल उत्पादन में इसका योगदान 57% से अधिक है।
- समिति ने कहा कि PSU विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों के लिये सरकारी सब्सिडी के तहत वितरण द्वारा मूल्य स्थिरकर्त्ता (Price Stabilizers) का कार्य करते हैं, जिससे यह आवश्यकता रेखांकित होती है कि उर्वरक क्षेत्र को रणनीतिक माना जाएँ।
सिफारिशें
- नीतिगत समर्थन: क्षेत्र को ‘रणनीतिक’ घोषित किया जाएँ ताकि सतत् निवेश आकर्षित किया जा सके और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित हो।
- उर्वरक PSU का पुनरोद्धार: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पाद विविधीकरण और सतत् प्रथाओं को अपनाने हेतु एक विशेष मिशन शुरू किया जाएँ।
- समिति ने उल्लेख किया कि पुनर्जीवित उर्वरक PSU ने सफल बदलाव हासिल किया है, जहाँ बंद इकाइयों के पुनः संचालन से वार्षिक यूरिया उत्पादन में 7.62 मिलियन टन का योगदान हुआ है।
भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था में उर्वरकों की भूमिका कितनी अहम है?
- कृषि का आर्थिक प्रभाव: कृषि और संबद्ध क्षेत्र भारत के GDP में लगभग 16% का योगदान करते हैं और देश की 46% से अधिक आबादी की आजीविका का आधार हैं, जिससे यह आर्थिक जीवनयापन का एक मूल स्तंभ बनता है।
- उर्वरक उत्पादन और उपभोग की प्रवृत्तियाँ: भारत वैश्विक स्तर पर उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- कुल उर्वरक उत्पादन वर्ष 2014–15 में 385.39 लाख मीट्रिक टन (LMT) से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 503.35 LMT हो गया है।
- वर्ष 2023–24 में उर्वरक उत्पादन में निजी क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक (57.77%) रहा, इसके बाद सहकारी क्षेत्र (24.81%) और सार्वजनिक क्षेत्र (17.43%) का स्थान रहा।
- आयात निर्भरता: वर्ष 2023–24 में भारत ने कुल 601 LMT उर्वरकों की खपत की, जिसमें से 503 LMT घरेलू उत्पादन था और 177 LMT का आयात किया गया।
- स्वावलंबन का स्तर यूरिया में 87%, NPK (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश) में 90% और DAP (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) में केवल 40% रहा, जबकि म्युरिएट ऑफ पोटाश (MOP) पूरी तरह (100%) आयात पर निर्भर है।
भारत का उर्वरक क्षेत्र स्थिरता और आत्मनिर्भरता की दिशा में कैसे विकसित हो रहा है?
- ONOF के तहत ब्रांड एकीकरण: वन नेशन वन फर्टिलाइज़र (ONOF) पहल के तहत सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों जैसे ‘भारत यूरिया’, ‘भारत DAP’ आदि में एक समान ब्रांडिंग की जाती है, ताकि भ्रम दूर हो, गुणवत्ता समान रहे और सरकारी सहयोग सुनिश्चित हो।
- सतत उर्वरक प्रथाएँ:
- नैनो-उर्वरक (नैनो यूरिया, नैनो DAP): सूक्ष्म कणों में पोषक तत्त्व समाहित रहते हैं, जो धीरे-धीरे मृदा में घुलते हैं, पौधों द्वारा बेहतर अवशोषण सुनिश्चित करते हैं और अपव्यय को न्यूनतम करते हैं।
- नीम-कोटेड यूरिया (NCU): नाइट्रोजन दक्षता बढ़ाता है, जिससे समान परिणाम पाने के लिये लगभग 10% कम यूरिया की आवश्यकता होती है। इससे हानि कम होती है और मृदा का स्वास्थ्य बेहतर होता है।
- पीएम-प्रणाम योजना: रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी को बढ़ावा देती है, जैविक विकल्पों को प्रोत्साहित करती है और राज्यों को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- जैव-उर्वरक और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना: संतुलित पोषक तत्त्व आपूर्ति और परीक्षण आधारित मृदा प्रबंधन पर बल देती है, जिससे किसानों को मार्गदर्शन तथा बेहतर उर्वरक उपयोग सुनिश्चित होता है।
- प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल अवसंरचना:
- iFMS (एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली): उत्पादन से लेकर खुदरा स्तर तक उर्वरकों की आवाजाही का रीयल-टाइम ट्रैकिंग सक्षम बनाती है।
- mFMS (मोबाइल FMS): डीलर पंजीकरण, स्टॉक निगरानी को सुगम बनाती है और मोबाइल के माध्यम से सुलभ MIS डैशबोर्ड के जरिये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का समर्थन करती है।
उर्वरक क्षेत्र को ‘रणनीतिक’ घोषित करने में क्या चुनौतियाँ हैं?
- वैश्विक एकीकरण और आपूर्ति विविधीकरण: भारत ने सऊदी अरब और मोरक्को के साथ DAP आपूर्ति के दीर्घकालिक समझौते किये हैं, जिससे बड़े रणनीतिक उत्पादन भंडार बनाए रखने का दबाव कम हुआ है।
- प्रौद्योगिकीय अप्रचलन: पुरानी PSU इकाइयाँ कम दक्षता, उच्च इनपुट लागत और आधुनिकीकरण के लिये भारी पूंजीगत आवश्यकता जैसी समस्याओं का सामना कर रही हैं।
- इससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि क्या रणनीतिक दर्जा मिलने पर भी बड़े सुधारों के अभाव में उत्पादकता में वास्तविक लाभ मिलेगा।
- कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कच्चे माल की कमी, मूल्य निर्धारण में विसंगति या पुरानी प्रौद्योगिकी के कारण कम क्षमता पर कार्य करना जारी रखे हुए हैं, जिससे रणनीतिक मामला और कमज़ोर हो रहा है।
- नीतिगत असंगति और क्षेत्रीय अस्पष्टता: कृषि मंत्रालय द्वारा उर्वरकों को खाद्य सुरक्षा के लिये अनिवार्य मानना और दूसरी ओर DIPAM द्वारा इसे गैर-रणनीतिक वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में देखना, नीतिगत असंगति को दर्शाता है।
- इससे मंत्रालयों के बीच सहमति बनाना कठिन हो जाता है और सुधारों की गति धीमी पड़ जाती है।
भारत अपने उर्वरक क्षेत्र को आत्मनिर्भर कैसे बना सकता है?
- घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना: नई निवेश नीति (NIP) 2012 के तहत मौजूदा इकाइयों को लाभकारी रूप से संचालित करना सुनिश्चित किया जाएँ और बंद संयंत्रों को पुनर्जीवित कर आयात पर निर्भरता घटाई जाएँ।
- नवाचार एवं स्थिरता: नई उर्वरक संरचनाओं, पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन और संसाधनों के कुशल उपयोग हेतु अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश किया जाएँ।
- पीएम-प्रणाम योजना और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के माध्यम से जैव-उर्वरकों व नैनो-उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएँ।
- सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा: नवाचार, निवेश और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये साझेदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- क्षेत्रीय विनिर्माण केंद्र: प्रमुख कृषि क्षेत्रों के निकट फर्टिलाइज़र क्लस्टर स्थापित किये जाएँ ताकि परिवहन लागत घटे और वितरण तेज़ी से हो सके।
- वित्तीय प्रोत्साहन: नैनो-उर्वरक उत्पादन के लिये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना लागू की जाएँ, जिससे निर्माता प्रोत्साहित हों और अपनाने की गति तीव्र हो।
- राष्ट्रीय पोषक प्रबंधन कार्यक्रमों में नैनो-उर्वरकों को शामिल किया जाएँ ताकि परंपरागत उर्वरकों का पूरक बन सके और आयात निर्भरता कम हो।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत की खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत एजेंडे के संदर्भ में उर्वरक क्षेत्र को रणनीतिक के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता की आलोचनात्मक जाँच कीजिये। |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)
प्रिलिम्स
प्रश्न. भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)
- वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाज़ार-संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है।
- अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है, वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है।
- सल्फर, जो फॉस्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिये कच्चा माल है, वह तेल शोधन कारखानों का उपोत्पाद है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (b)
प्रश्न. भारत सरकार कृषि में 'नीम-लेपित यूरिया' (Neem-coated Urea) के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? (2016)
(a) मृदा में नीम तेल के निर्मुक्त होने से मृदा सूक्ष्मजीवों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण बढ़ता है
(b) नीम लेप, मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है
(c) नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एक ग्रीनहाउस गैस है, फसल वाले खेतों से वायुमंडल में बिलकुल भी विमुक्त नहीं होती है
(d) विशेष फसलों के लिये यह एक अपतृणनाशी (वीडिसाइड) और एक उर्वरक का संयोजन है
उत्तर: (b)