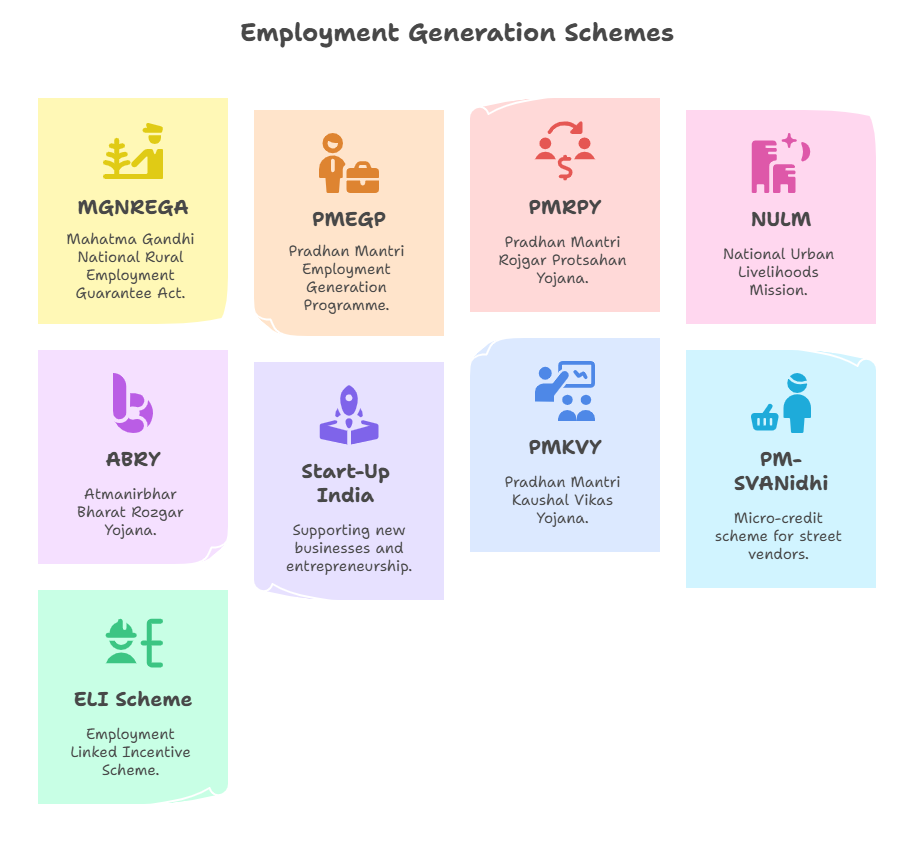समावेशी एवं सतत् रोज़गार नीतियों का निर्माण
यह एडिटोरियल 13/08/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “Debunking the Myth of Job Creation,” पर आधारित है। यह भारत में रोज़गार सृजन की निरंतर चुनौतियों पर प्रकाश डालता है और देश भर में स्थायी रोज़गार सृजन एवं आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिये अधिक समावेशी, कौशल-केंद्रित नीतियों की आवश्यकता पर बल देता है।
प्रिलिम्स के लिये: कौशल भारत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, EPFO, अटल पेंशन योजना, PMGDISHA
मेन्स परीक्षा के लिये: भारत में रोज़गार सृजन: संबंधित चुनौतियाँ और आगे की राह
भारत में हाल के वर्षों में रोज़गार सृजन के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी पहलों के कारण रोज़गार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालाँकि, कौशल असंतुलन, वेतन असमानताएँ और अनौपचारिक श्रम बाज़ार का प्रभुत्व जैसे मुद्दे अधिक स्थायी तथा समावेशी रोज़गार अवसरों के सृजन को सीमित कर रहे हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिये, भारत को ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो कौशल विकास एवं समावेशिता पर केंद्रित हों तथा सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण रोज़गार सृजन सुनिश्चित करें।
भारत में रोज़गार की वर्तमान स्थिति क्या है?
- श्रम बल भागीदारी दर: PLFS के आँकड़ों (जुलाई 2023-जून 2024) के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिये श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) सत्र 2017-18 में 49.8% से बढ़कर सत्र 2023-24 में 60.1% हो गई है।
- इसी अवधि के दौरान, श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) 46.8% से बढ़कर 58.2% हो गया।
- महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) सत्र 2017-18 में 23.3% से बढ़कर सत्र 2023-24 में 41.7% हो गई है।
- उल्लेखनीय रूप से, महिला बेरोज़गारी 5.6% से घटकर केवल 3.2% रह गई है, जो अधिक समावेशिता और आर्थिक सशक्तीकरण की ओर परिवर्तन को दर्शाता है।
- रोज़गार बाज़ार का औपचारिकीकरण: EPFO अंशदान में निवल वृद्धि दोगुने से भी अधिक हो गई है, जो वित्त वर्ष 2019 में 61 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 131 लाख हो गई है, जो रोज़गार बाज़ार के औपचारिकीकरण का संकेत है।
- कार्यबल में स्व-नियोजित श्रमिकों का अनुपात सत्र 2017-18 में 52.2% से बढ़कर सत्र 2023-24 में 58.4% हो गया है, जो बढ़ती उद्यमशीलता गतिविधि एवं लचीली कार्य व्यवस्थाओं के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है।
- इसके अलावा, भारत का लगभग 80% श्रम बल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है और शेष 20% औपचारिक क्षेत्र (वर्ष 2021) में कार्यरत है।
- क्षेत्रीय रोज़गार रुझान: आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, रोज़गार में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 2017-18 में 44.1% थी, जो सत्र 2023-24 में बढ़कर 46.1% हो गई है।
- इसकी तुलना में, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में रोज़गार हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र 12.1% से घटकर 11.4% तथा सेवा क्षेत्र इसी अवधि में 31.1% से घटकर 29.7% रह गया।
- बेरोज़गारी दर: 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिये बेरोज़गारी दर सत्र 2017-18 में 6% से लगातार घटकर सत्र 2023-24 में 3.2% हो गई है।
- उल्लेखनीय गिरावट के बावजूद, श्रम बाज़ार में कौशल असंगतता, अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व एवं अल्परोज़गार जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
भारत में रोज़गार सृजन को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?
- बेरोज़गार वृद्धि: भारत की आर्थिक वृद्धि अब तीव्र हो रही है, लेकिन इसके साथ पर्याप्त रोज़गार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं, जिससे बेरोज़गारी में वृद्धि हो रही है।
- IT और वित्त जैसे क्षेत्र GDP में योगदान बढ़ा रहे हैं, जबकि कम श्रमिकों को रोज़गार दे रहे हैं, जो श्रम-प्रधान वृद्धि के बजाय पूंजी-प्रधान वृद्धि को दर्शाता है।
- उदाहरण के लिये, एक हालिया शोध के अनुसार, वर्ष 2011 और 2021 के बीच, भारत की GDP वृद्धि दर औसतन लगभग 5.3% रही, जबकि रोज़गार वृद्धि दर मात्र 0.39% प्रति वर्ष रही, जो आर्थिक विस्तार एवं रोज़गार सृजन के बीच एक महत्त्वपूर्ण अंतर को उजागर करती है।
- हालाँकि, EPFO द्वारा दर्ज औपचारिक नौकरियों में हालिया वृद्धि, विकास का संकेत देती है, फिर भी यह बढ़ती कार्यशील आबादी को उत्पादक रूप से नियोजित करने के लिये वर्ष 2030 तक सालाना आवश्यक अनुमानित 7.85 मिलियन गैर-कृषि नौकरियों से कम है।
- IT और वित्त जैसे क्षेत्र GDP में योगदान बढ़ा रहे हैं, जबकि कम श्रमिकों को रोज़गार दे रहे हैं, जो श्रम-प्रधान वृद्धि के बजाय पूंजी-प्रधान वृद्धि को दर्शाता है।
- विनिर्माण क्षेत्र में मंदी: ऐतिहासिक रूप से रोज़गार सृजन का एक प्रमुख क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, भारत की बढ़ती श्रम शक्ति को समाहित करने के लिये आवश्यक विस्तार के स्तर का अनुभव नहीं कर पाया है।
- सेवाओं और प्रौद्योगिकी-आधारित विकास पर ध्यान केंद्रित करने से विनिर्माण क्षेत्र से ध्यान हट गया है, जो आमतौर पर अधिक रोज़गार सृजित करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 के बाद गैर-कृषि रोज़गार में उल्लेखनीय गिरावट आई है और विनिर्माण क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है।
- मेक इन इंडिया अभियान जैसे प्रयासों के बावजूद, विनिर्माण क्षेत्र का रोज़गार हिस्सा 12-14% पर स्थिर बना हुआ है और ब्लू-कॉलर कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अपर्याप्त वेतन अर्जित कर रहा है।
- कौशल बेमेल और रोज़गार संकट: स्नातकों की बढ़ती संख्या के बावजूद, श्रम शक्ति का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा अर्द्ध-कुशल या प्राथमिक नौकरियों में अल्प-रोज़गार है।
- आर्थिक सर्वेक्षण सत्र 2024-25 से पता चलता है कि केवल 8.25% स्नातक ही अपनी योग्यता के अनुरूप भूमिकाओं में कार्यरत हैं।
- इसके अलावा, 53% स्नातक और 36% स्नातकोत्तर निम्न-कौशल वाली नौकरियों में कार्यरत हैं, जो भारत की शिक्षा-से-रोज़गार पाइपलाइन की अक्षमता तथा उपलब्ध नौकरियों एवं श्रमिकों के कौशल के बीच निरंतर बेमेल को दर्शाता है।
- भारत के 5% से भी कम कार्यबल औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जबकि जापान एवं दक्षिण कोरिया में यह 80% से 96% तक है।
- आर्थिक सर्वेक्षण सत्र 2024-25 से पता चलता है कि केवल 8.25% स्नातक ही अपनी योग्यता के अनुरूप भूमिकाओं में कार्यरत हैं।
- कार्यबल भागीदारी में लैंगिक असमानता: FLFPR में उल्लेखनीय सुधार के बावजूद, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर अभी भी पुरुषों की LFPR की आधी है तथा वैश्विक औसत महिला LFPR 47.2% से काफी कम है।
- हालाँकि हाल की नीतियों और आर्थिक सुधारों ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया है, लेकिन सामाजिक मानदंड, सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और कामकाज़ी महिलाओं के लिये समर्थन की कमी (जैसे: बाल देखभाल सुविधाएँ) कार्यबल में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित करती रहती हैं, विशेषकर औपचारिक क्षेत्र की नौकरियों में।
- यह विसंगति न केवल संभावित कार्यबल को सीमित करती है, बल्कि आधी आबादी की प्रतिभा और कौशल का पूरी तरह से उपयोग न करके आर्थिक विकास को भी बाधित करती है।
- हालाँकि हाल की नीतियों और आर्थिक सुधारों ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया है, लेकिन सामाजिक मानदंड, सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और कामकाज़ी महिलाओं के लिये समर्थन की कमी (जैसे: बाल देखभाल सुविधाएँ) कार्यबल में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित करती रहती हैं, विशेषकर औपचारिक क्षेत्र की नौकरियों में।
- अनौपचारिक क्षेत्र के औपचारिकीकरण में कमियाँ: IMF के अनुसार, अनौपचारिक क्षेत्र भारत के 80% से अधिक कार्यबल को रोज़गार देता है, लेकिन यह सामाजिक सुरक्षा, नौकरी के स्थायित्व एवं औपचारिक अनुबंधों जैसे नीतिगत लाभों से बहुत हद तक वंचित है।
- अनौपचारिक क्षेत्र भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 45% का योगदान देता है, जो अर्थव्यवस्था में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। हालाँकि औपचारिकीकरण के प्रयास चल रहे हैं, वे सीमित रहे हैं, जिससे अनौपचारिक श्रमिक कम वेतन एवं नौकरी की असुरक्षा के प्रति संवेदनशील हैं।
- इसके अतिरिक्त, बढ़ता हुआ गिग कार्यबल, जिसमें अब वित्तीय वर्ष 2024-25 तक लगभग 12 मिलियन श्रमिक शामिल हैं, समान चुनौतियों का सामना कर रहा है।
- इसके अलावा, जबकि अनौपचारिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास किये गए हैं, जैसे कि अटल पेंशन योजना, जिसमें जुलाई 2025 तक 8 करोड़ से अधिक ग्राहक नामांकित हैं, व्यापक कवरेज एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- अनौपचारिक क्षेत्र भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 45% का योगदान देता है, जो अर्थव्यवस्था में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। हालाँकि औपचारिकीकरण के प्रयास चल रहे हैं, वे सीमित रहे हैं, जिससे अनौपचारिक श्रमिक कम वेतन एवं नौकरी की असुरक्षा के प्रति संवेदनशील हैं।
- डिजिटल व्यवधान और नौकरी विस्थापन: डिजिटल प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से AI और स्वचालन की तीव्र प्रगति, भारत के रोज़गार बाज़ार में महत्त्वपूर्ण रूप से बदलाव ला रही है।
- ये प्रौद्योगिकियाँ जहाँ नवाचार और दक्षता के अवसर प्रदान करती हैं, वहीं ये चुनौतियाँ भी पेश करती हैं, विशेषकर पारंपरिक और कम-कुशल भूमिकाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये।
- अगस्त 2025 में, TCS ने 12,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की, जो उसके कार्यबल का लगभग 2% है। कंपनी ने इस निर्णय का श्रेय कौशल असंतुलन और AI तकनीकों के बढ़ते उपयोग को दिया।
- मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि स्वचालन वर्ष 2030 तक भारत के विनिर्माण क्षेत्र में 6 करोड़ तक कर्मचारियों को बेरोज़गार कर सकता है, जिसका वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की नौकरियों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
- ये प्रौद्योगिकियाँ जहाँ नवाचार और दक्षता के अवसर प्रदान करती हैं, वहीं ये चुनौतियाँ भी पेश करती हैं, विशेषकर पारंपरिक और कम-कुशल भूमिकाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये।
- भू-आर्थिक बदलाव और बढ़ते व्यापार तनाव: अमेरिका द्वारा जारी टैरिफ ने भारत के व्यापार और औद्योगिक रोज़गार को प्रभावित किया है।
- एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत के निर्यात और औद्योगिक उत्पादन पर अमेरिकी टैरिफ के नकारात्मक प्रभावों का हवाला देते हुए, वित्त वर्ष 2026 के लिये भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर के अनुमान को पहले के 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया है।
- इन व्यापार व्यवधानों का प्रभाव संभावित रूप से औद्योगिक रोज़गार पर भी पड़ सकता है, विशेष रूप से वैश्विक व्यापार पर निर्भर क्षेत्रों, जैसे वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण में।
- एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत के निर्यात और औद्योगिक उत्पादन पर अमेरिकी टैरिफ के नकारात्मक प्रभावों का हवाला देते हुए, वित्त वर्ष 2026 के लिये भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर के अनुमान को पहले के 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया है।
- जलवायु भेद्यता और आजीविका के लिये खतरा: जलवायु परिवर्तन आजीविका के लिये गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है, विशेष रूप से अनौपचारिक श्रमिकों के लिये, जो प्रायः सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं।
- वर्ष 2001 और 2020 के दौरान, भारत ने जलवायु प्रभावों के कारण सालाना लगभग 259 बिलियन श्रम घंटे खो दिये, जिसमें अकेले अत्यधिक गर्मी के कारण 181 बिलियन श्रम घंटों का नुकसान हुआ।
- यह अनौपचारिक श्रमिकों को असमान रूप से प्रभावित करता है, विशेष रूप से कृषि, निर्माण एवं अन्य श्रम-प्रधान क्षेत्रों में बाहर काम करने वाले श्रमिकों को, जहाँ उनके पास जलवायु के कठोर प्रभावों से पर्याप्त सुरक्षा का अभाव है।
- वर्ष 2001 और 2020 के दौरान, भारत ने जलवायु प्रभावों के कारण सालाना लगभग 259 बिलियन श्रम घंटे खो दिये, जिसमें अकेले अत्यधिक गर्मी के कारण 181 बिलियन श्रम घंटों का नुकसान हुआ।
भारत में रोज़गार सृजन और कार्यबल विकास को बढ़ाने के लिये कौन-सी रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं?
- अनौपचारिक क्षेत्र के औपचारिकीकरण को सुदृढ़ करना: चूँकि अनौपचारिक क्षेत्र भारत के कार्यबल के एक बड़े हिस्से को रोज़गार देता है, इसलिये सामाजिक सुरक्षा, रोज़गार स्थायित्व एवं औपचारिक अनुबंधों तक अभिगम्यता सुनिश्चित करके इस क्षेत्र को औपचारिक बनाना अत्यंत आवश्यक है।
- अनौपचारिक से औपचारिक रोज़गार कार्यढाँचों में बदलाव करने वाले व्यवसायों को प्रोत्साहन प्रदान करने से स्थिर एवं सुरक्षित रोज़गार सृजित हो सकते हैं, साथ ही श्रमिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत किया जा सकता है।
- असंगठित श्रमिकों के लिये एक राष्ट्रीय डेटाबेस के रूप में ई-श्रम पोर्टल, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभों, कौशल विकास कार्यक्रमों एवं औपचारिक रोज़गार के अवसरों से जोड़कर इस क्षेत्र को औपचारिक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- सूक्ष्म वित्त, ज़मानत-मुक्त ऋण और छोटे व्यवसायों के लिये ऋण सुविधाओं तक अभिगम को बढ़ाने से अनौपचारिक क्षेत्र का विकास होगा, साथ ही श्रमिकों को अधिक सुरक्षित रोज़गार भी मिलेगा।
- इससे यह सुनिश्चित होगा कि अनौपचारिक श्रमिकों की स्वास्थ्य बीमा, पेंशन योजनाओं और न्यूनतम श्रम जैसे बुनियादी लाभों तक अभिगम हो।
- अनौपचारिक से औपचारिक रोज़गार कार्यढाँचों में बदलाव करने वाले व्यवसायों को प्रोत्साहन प्रदान करने से स्थिर एवं सुरक्षित रोज़गार सृजित हो सकते हैं, साथ ही श्रमिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत किया जा सकता है।
- सेवा क्षेत्र का आधुनिकीकरण: आर्थिक विकास को गति देने और गुणवत्तापूर्ण रोज़गार सृजित करने के लिये, भारत के सेवा क्षेत्र का आधुनिकीकरण आवश्यक है।
- स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और शिक्षा जैसे उच्च-विकासशील सेवा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये और कार्यबल को उद्योग की माँगों के अनुरूप नौकरी के लिये तैयार कौशल से लैस करने पर ज़ोर दिया जाना चाहिये।
- सेवा वितरण में वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये समर्पित केंद्रों की स्थापना से यह सुनिश्चित होगा कि श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाए।
- इसके अतिरिक्त, भारत वेलनेस टूरिज़्म जैसे उभरते क्षेत्रों के लिये विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर सकता है, जिससे कुशल श्रमिकों की बढ़ती माँग को पूरा किया जा सके तथा इन क्षेत्रों में नए रोज़गार के अवसरों का सृजन किये जा सके।
- कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को सक्षम बनाना: महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाने के लिये एक समग्र, व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिये MUDRA योजना और महिला शक्ति केंद्र जैसे कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिये, जो संपार्श्विक मुक्त ऋण और कौशल विकास प्रदान करते हैं।
- लघु और मध्यम उद्यम (SME) जेंडर न्यूट्रल वेतन, समान पदोन्नति के अवसर एवं सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने जैसी प्रथाओं को लागू करके महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये इवन कार्गो (एक महिला-संचालित लॉजिस्टिक्स कंपनी) और फार्म दीदी (एक ग्रामीण महिला-संचालित फूड स्टार्टअप) जैसे सफल उदाहरणों को दोहराया जाना चाहिये।
- समुत्थानशक्ति और समावेशिता के लिये श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन में तीव्रता: भारत को अपनी श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन में तेज़ी लानी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे आज के उभरते रोज़गार बाज़ार की आवश्यकता के अनुसार अधिक समावेशी और अनुकूल हों।
- साथ ही, गिग रोज़गार, संविदा श्रम और अनौपचारिक कार्यों में अधिक समुत्थानशीलता सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ एवं पेंशन योजनाओं जैसी कानूनी सुरक्षा प्रदान कर सकता है।
- व्यापार-सुगमता को बढ़ावा देने के लिये श्रम संहिता को सरल बनाने तथा साथ ही श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने से रोज़गार के औपचारिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे नियोक्ताओं के लिये गुणवत्तापूर्ण, अच्छे वेतन वाली नौकरियाँ सृजित करना अधिक आकर्षक हो जाएगा।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को सुदृढ़ बनाना: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) सार्वजनिक क्षेत्र के समर्थन और निजी क्षेत्र के नवाचार, दोनों का लाभ उठाकर स्थायी रोज़गार के अवसर सृजित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से, सरकार कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करने, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने और बुनियादी ढाँचे, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों का सृजन करने के लिये निजी उद्यमों के साथ साझेदारी कर सकती है।
- कौशल भारत मिशन और PMKVY जैसी पहल निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता से लाभान्वित होती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रदान किया गया प्रशिक्षण उद्योग की ज़रूरतों के अनुरूप हो एवं रोज़गार क्षमता को बढ़ाए।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को समर्थन देकर उद्यमिता को भी बढ़ावा दे सकती है, जिससे अंततः रोज़गार सृजन एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से, सरकार कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करने, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने और बुनियादी ढाँचे, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों का सृजन करने के लिये निजी उद्यमों के साथ साझेदारी कर सकती है।
- ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा: ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये, वित्तीय सहायता, कौशल विकास एवं बाज़ार अभिगम प्रदान करके ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना आवश्यक है।
- ग्रामीण नवाचार केंद्र बनाना, स्थानीय कृषि-आधारित उद्योगों को समर्थन देना और डिजिटल तकनीकों को एकीकृत करना उत्पादकता एवं व्यावसायिक स्थायित्व को बढ़ा सकता है।
- ये प्रयास रोज़गार सृजन, शहरी क्षेत्रों में पलायन को कम करने तथा ग्रामीण भारत की अप्रयुक्त क्षमता का सदुपयोग करने में सहायता करेंगे।
- सामान्य सेवा केंद्र (CSC) डिजिटल बुनियादी अवसंरचना, प्रशिक्षण एवं सरकारी सेवाओं तक अभिगम प्रदान करके ग्रामीण उद्यमिता को और बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे रोज़गार सृजन, शहरी पलायन को कम करने तथा ग्रामीण भारत की क्षमता को उजागर करने में सहायता मिलेगी।
- ग्रामीण नवाचार केंद्र बनाना, स्थानीय कृषि-आधारित उद्योगों को समर्थन देना और डिजिटल तकनीकों को एकीकृत करना उत्पादकता एवं व्यावसायिक स्थायित्व को बढ़ा सकता है।
- डिजिटल साक्षरता और प्रौद्योगिकी अंगीकरण को बढ़ावा देना: डिजिटल अर्थव्यवस्था में रोज़गार के बढ़ते अवसरों के साथ, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में निवेश करना, विशेष रूप से महिलाओं एवं ग्रामीण युवाओं के लिये, अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म तक अभिगम प्रदान करने से श्रमिकों को डिजिटल अर्थव्यवस्था के अनुकूल होने में सहायता मिलेगी।
- PMGDISHA के तहत, लगभग 7.35 करोड़ उम्मीदवारों का पंजीकरण हुआ और 6.39 करोड़ व्यक्तियों को डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को डिजिटल तकनीकों के अंगीकरण के लिये प्रोत्साहित करने से उत्पादकता बढ़ेगी तथा औपचारिक अर्थव्यवस्था में अधिक रोज़गार सृजित होंगे।
- प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म तक अभिगम प्रदान करने से श्रमिकों को डिजिटल अर्थव्यवस्था के अनुकूल होने में सहायता मिलेगी।
- भविष्य के लिये तैयार भारत के लिये हरित कार्यबल का पोषण: एक स्थायी और भविष्य के लिये तैयार कार्यबल के निर्माण के लिये, हरित ऊर्जा रोज़गार में निवेश करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- उदाहरण के लिये, आंध्र प्रदेश ने आगामी पाँच वर्षों में 3 लाख हरित ऊर्जा रोज़गार सृजित करने का एक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है तथा सौर, पवन एवं ऊर्जा दक्षता जैसे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में रोज़गार वृद्धि के लिये इस मॉडल को अन्य राज्यों द्वारा अपनाया जा सकता है।
- हरित कार्यबल को बढ़ावा देकर, भारत सतत् विकास में योगदान दे सकता है तथा वैश्विक पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप दीर्घकालिक रोज़गार के अवसरों का सृजन कर सकता है।
- उदाहरण के लिये, आंध्र प्रदेश ने आगामी पाँच वर्षों में 3 लाख हरित ऊर्जा रोज़गार सृजित करने का एक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है तथा सौर, पवन एवं ऊर्जा दक्षता जैसे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में रोज़गार वृद्धि के लिये इस मॉडल को अन्य राज्यों द्वारा अपनाया जा सकता है।
निष्कर्ष
भारत का भावी रोज़गार सृजन 3 ‘E’ पर निर्भर करता है: Enablement through policy reforms and infrastructure development (नीतिगत सुधारों और बुनियादी अवसंरचना के विकास के माध्यम से क्षमता निर्माण), Empowerment via skill development, entrepreneurship & digital literacy (कौशल विकास, उद्यमिता और डिजिटल साक्षरता के माध्यम से सशक्तीकरण) और Equity by ensuring opportunities for all (सभी के लिये समान अवसर सुनिश्चित करना)। कार्यबल को प्रासंगिक कौशल से लैस करके और क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करके, भारत एक गतिशील, समतामूलक कार्यबल का निर्माण कर सकता है, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास एवं संवहनीयता को गति प्रदान करेगा।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. भारत में रोज़गार सृजन की प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये तथा सतत् एवं समावेशी रोज़गार के लिये रणनीतियों का सुझाव दीजिये। |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)
प्रिलिम्स
प्रश्न 1. प्रधानमंत्री MUDRA योजना का लक्ष्य क्या है? (2016)
(a) लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना
(b) निर्धन कृषकों को विशेष फसलों की कृषि के लिये ऋण उपलब्ध कराना
(c) वृद्ध एवं निस्सहाय लोगों को पेंशन देना
(d) कौशल विकास एवं रोज़गार सृजन में लगे स्वयंसेवी संगठनों का निधीयन (फंडिंग) करना
उत्तर: (a)
प्रश्न 2. प्रच्छन्न बेरोज़गारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि (2013)
(a) लोग बड़ी संख्या में बेरोज़गार रहते हैं
(b) वैकल्पिक रोज़गार उपलब्ध नहीं है
(c) श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है
(d) श्रमिकों की उत्पादकता नीची है
उत्तर: (c)
मेन्स
प्रश्न 1. हाल के समय में भारत में आर्थिक संवृद्धि की प्रकृति का वर्णन प्रायः नौकरीहीन संवृद्धि के तौर पर किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिये। (2015)
प्रश्न 2. भारत में सबसे ज्यादा बेरोज़गारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में बेरोज़गारी की गणना के लिये अपनाई गई पद्धति का परीक्षण कीजिये और सुधार के सुझाव दीजिये। (2023)