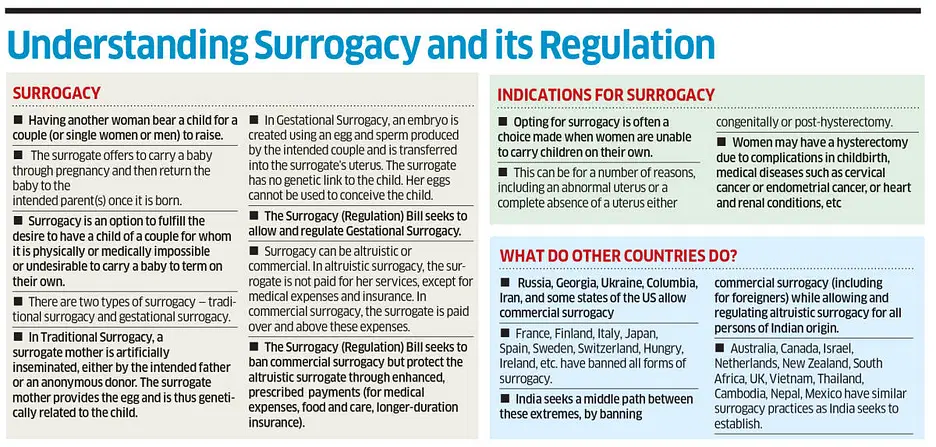भारत में सरोगेसी कानून: अधिकार और सीमाएँ | 17 Nov 2025
प्रिलिम्स के लिये: सरोगेसी कानून, सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021, परोपकारी सरोगेसी, वाणिज्यिक सरोगेसी, संविधान का अनुच्छेद 21।
मेन्स के लिये: सरोगेसी कानून और संबंधित चुनौतियाँ, इन कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिये गठित तंत्र, कानून, संस्थान और निकाय।
चर्चा में क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय इस बात की जाँच करने के लिये सहमत हो गया है कि क्या सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत दूसरे बच्चे के लिये सरोगेसी के उपयोग पर प्रतिबंध, विशेष रूप से द्वितीयक बाँझपन के मामलों में प्रजनन स्वायत्तता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
भारत के सरोगेसी कानून की सीमाओं को कानूनी चुनौती क्यों दी जा रही है?
- सरोगेसी अधिनियम, 2021 पर विचार: सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 4(iii)(C)(II) उन दंपतियों को सरोगेसी का विकल्प चुनने से रोकती है, जिनके पास पहले से ही एक बच्चा है - जैविक, गोद लिया हुआ या सरोगेसी के माध्यम से, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहाँ मौजूदा बच्चा किसी विकलांगता, जानलेवा या किसी लाइलाज बीमारी से प्रभावित है।
- द्वितीयक बाँझपन से पीड़ित दंपतियों का तर्क है कि यह प्रतिबंध उन्हें सरोगेसी तक पहुँच से वंचित करता है तथा प्रजनन स्वायत्तता के उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
- याचिकाकर्त्ताओं द्वारा तर्क: द्वितीयक बाँझपन, हालाँकि कम चर्चा में है, भावनात्मक और चिकित्सकीय रूप से कष्टदायक है।
- जब राष्ट्रीय स्तर पर एक-संतान नीति नहीं है तथा गोद लेने संबंधी कानून पहले से ही दूसरे या तीसरे बच्चे की अनुमति देते हैं (उदाहरण के लिये हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956, किशोर न्याय अधिनियम, 2015) तो सरोगेसी से इनकार नहीं किया जाना चाहिये।
- यह प्रतिबंध प्रजनन स्वायत्तता में राज्य के अतिक्रमण के समान है, जो अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।
- सरकार का रुख:
- सरोगेसी मौलिक अधिकार नहीं: सरोगेसी में किसी अन्य महिला के गर्भ का उपयोग शामिल है। संविधान किसी अन्य व्यक्ति के शरीर पर अधिकार को मान्यता नहीं देता। सरोगेसी एक वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक नहीं।
- प्रतिबंध उचित और आवश्यक: जब दंपति के पास पहले से ही स्वस्थ, जीवित बच्चा हो तो यह अनावश्यक सरोगेसी को रोकता है। गैर-आवश्यक मामलों में सरोगेट माताओं को गर्भधारण से सुरक्षा प्रदान करता है।
- संतुलित प्रावधान: प्रावधान गंभीर चिकित्सा स्थितियों के लिये अपवाद की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वास्तविक आवश्यकता को पूरा किया जाए और सरोगेसी का दुरुपयोग न हो।
- सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन: न्यायालय ने भारत की बढ़ती जनसंख्या से संबंधित चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि यह प्रतिबंध "उचित" प्रतीत होता है।
- फिर भी इसने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह निर्धारित करने के लिये विस्तृत जाँच की आवश्यकता है कि क्या यह प्रावधान प्रजनन स्वतंत्रता, शारीरिक स्वायत्तता और गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
भारत में सरोगेसी से संबंधित प्रमुख कानूनी ढाँचे क्या हैं?
- सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021:
- अनुमति: सरोगेसी केवल परोपकारी उद्देश्यों के लिये ही अनुमत है तथा प्रमाणित बाँझपन वाले दंपतियों के लिये वाणिज्यिक सरोगेसी पूर्णतः निषिद्ध है।
- पात्रता की आवश्यकता: केवल कानूनी रूप से विवाहित भारतीय दंपति पुरुष (26–55 वर्ष) और महिला (25–50 वर्ष) या विधवा/तलाकशुदा महिला (35–45 वर्ष) ही सरोगेसी का विकल्प चुन सकते हैं और उनके पास पहले से कोई जैविक, गोद लिया हुआ या सरोगेसी से जन्मा बच्चा नहीं होना चाहिये।
- सरोगेट माँ के लिये मानदंड: निकट संबंधी होना चाहिये विवाहित होना चाहिये, कम-से-कम एक बच्चा होना चाहिये, 25-35 वर्ष की आयु होनी चाहिये तथा केवल एक बार सरोगेट के रूप में कार्य करना चाहिये।
- जन्म के समय कानूनी स्थिति: बच्चा कानूनी रूप से इच्छुक दंपति का जैविक बच्चा होता है, गर्भपात के लिये सहमति की आवश्यकता होती है तथा MTP अधिनियम का पालन करना होता है।
- नियम 7 (दाता अंडे पर प्रतिबंध): नियम 7 दाता शुक्राणु पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मेयर-रोकिटांस्की-कुस्टर-हाउसर (MRKH) सिंड्रोम से जुड़े एक विशिष्ट मामले में इसके संचालन पर रोक लगा दी है।
- सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 में संशोधन: इसके तहत दाता युग्मकों के साथ सरोगेसी की अनुमति दी गई है, बशर्ते इच्छुक दंपति में से किसी एक को ज़िला चिकित्सा बोर्ड द्वारा किसी चिकित्सीय स्थिति के कारण दाता युग्मकों की आवश्यकता के लिये प्रमाणित किया गया हो।
- इसका अर्थ है कि यदि दोनों साथियों को कोई चिकित्सीय समस्या है तो दंपति अभी भी सरोगेसी का विकल्प नहीं चुन सकते।
- सरोगेसी का विकल्प चुनने वाली तलाकशुदा या विधवा महिलाओं के लिये यह दाता शुक्राणु के साथ महिला के स्वयं के अंडों के उपयोग को अनिवार्य बनाता है।
भारत के सरोगेसी फ्रेमवर्क में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?
- शोषण का जोखिम बनाम स्वायत्तता: व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध महिलाओं के प्रजनन विकल्पों को सीमित करता है तथा सुरक्षा और स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई उत्पन्न करता है।
- पितृसत्तात्मक सुदृढ़ीकरण: प्रजनन श्रम पर महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करके, कानून अप्रत्यक्ष रूप से पितृसत्तात्मक मानदंडों को बनाए रखता है और अनुच्छेद 21 के अधिकारों को प्रभावित करता है।
- परोपकारी सरोगेसी में भावनात्मक दबाव: परिवार-आधारित सरोगेसी भावनात्मक तनाव उत्पन्न कर सकती है, संबंधों को प्रभावित कर सकती है और इच्छुक सरोगेट्स की संख्या सीमित रखती है।
- पेशेवर समर्थन की कमी: एजेंसियों को बहिष्कृत करने से संरचित समन्वय, वित्तीय स्पष्टता और सरोगेट व इच्छुक माता-पिता दोनों के लिये भावनात्मक समर्थन की कमी होती है।
- बहिष्करणकारी पात्रता नियम: अविवाहित व्यक्ति, अकेले पुरुष, समलैंगिक जोड़े और लिव-इन रिलेशनशिप में साथी प्रतिबंधित हैं, जो विभिन्न पारिवारिक रूपों के खिलाफ भेदभाव उत्पन्न करते हैं।
भारत के सरोगेसी फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करने हेतु किन सुधारों की आवश्यकता है?
- पात्रता मानदंडों का तर्कसंगत सुधार: सरकार और विधायिका को प्रतिबंधात्मक प्रावधानों, विशेषकर द्वितीयक बाँझपन, दाता युग्मक और अविवाहित व्यक्तियों के बहिष्कार पर पुनर्विचार करना चाहिये, ताकि कानून बदलती पारिवारिक संरचनाओं एवं संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप हो।
- सुरक्षा उपायों को मज़बूत करना: प्रतिबंधात्मक नियमों के बजाय ध्यान मज़बूत नियामक तंत्र पर होना चाहिये, जो सरोगेट माताओं के लिये सूचित सहमति, चिकित्सकीय सुरक्षा, व्यय का उचित मुआवज़ा और शोषण से सुरक्षा सुनिश्चित करे।
- परामर्श और समर्थन तंत्र: इच्छुक माता-पिता और सरोगेट माताओं के लिये अनिवार्य मनोवैज्ञानिक, कानूनी तथा चिकित्सकीय परामर्श भावनात्मक दबाव को कम कर सकता है, बलपूर्वक करने से रोकता है तथा सभी पक्षों को जटिल निर्णयों में मार्गदर्शन करता है।
- सांस्थानिक तंत्र: ज़िला और राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्डों को बेहतर निगरानी उपकरण, शिकायत निवारण तंत्र तथा पारदर्शी प्रक्रियाओं के साथ सशक्त किया जाना चाहिये, ताकि सरोगेसी क्लीनिक, एजेंसियों एवं मेडिकल बोर्डों का नियमन किया जा सके।
- अधिकार-आधारित नीति ढाँचा: भविष्य के सुधारों में अनुच्छेद 21 के अधिकारों का संरक्षण, शारीरिक स्वायत्तता का सम्मान और सुरक्षा के साथ सशक्तीकरण का संतुलन सुनिश्चित होना चाहिये ताकि सरोगेसी इकोसिस्टम नैतिक, समावेशी एवं संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप बना रहे।
निष्कर्ष
जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान प्रतिबंधों की पुनःसमीक्षा करता है, भारत के पास यह अवसर है कि वह अपने सरोगेसी फ्रेमवर्क को परिष्कृत कर नैतिक सुरक्षा और प्रजनन स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करे। एक अधिक समावेशी, अधिकार-आधारित और सुव्यवस्थित प्रणाली सरोगेट माताओं की सुरक्षा, इच्छुक माता-पिता का समर्थन और कानून को बदलती सामाजिक वास्तविकताओं तथा संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप बनाए रखने में सक्षम हो सकती है।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 शोषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पितृसत्तात्मक धारणाओं को मज़बूत करता है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 4(iii)(C)(II) के तहत मुख्य प्रतिबंध क्या है?
इसमें उन दंपति को सरोगेसी का उपयोग करने से रोका गया है जिनका पहले से एक बच्चा है, सिवाय इसके कि उस बच्चे को गंभीर दिव्यांगता या जानलेवा बीमारी हो।
2. द्वितीयक बाँझपन वाले दंपति धारा 4(iii)(C)(II) को चुनौती क्यों दे रहे हैं?
वे तर्क देते हैं कि यह प्रावधान उनके प्रजनन स्वायत्तता और अनुच्छेद 21 के तहत उनकी निजता का उल्लंघन करता है।
3. सरकार का रुख क्या है?
सरकार का कहना है कि सरोगेसी मौलिक अधिकार नहीं है और यह प्रतिबंध अनावश्यक सरोगेट उपयोग को रोकता है।
4. सर्वोच्च न्यायालय का निरीक्षण क्या है?
इसने इस प्रतिबंध को ‘युक्तिसंगत’ कहा है, लेकिन प्रजनन स्वतंत्रता पर इसके प्रभाव की जाँच भी करेगा।
5. क्या भारतीय कानून व्यावसायिक सरोगेसी की अनुमति देता है?
नहीं, केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति है, जो केवल चिकित्सा लागत की प्रतिपूर्ति तक सीमित है।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)
प्रश्न. मानव प्रजनन प्रौद्योगिकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में "प्राक्केंद्रिक स्थानांतरण ”(Pronuclear Transfer) का प्रयोग किस लिये होता है। (2020)
(a) इन विट्रो अंड के निषेचन के लिये दाता शुक्राणु का उपयोग
(b) शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का आनुवंशिक रूपांतरण
(c) स्टेम (Stem) कोशिकाओं का कार्यात्मक भ्रूूणों में विकास
(d) संतान में सूत्रकणिका रोगों का निरोध
उत्तर: (d)